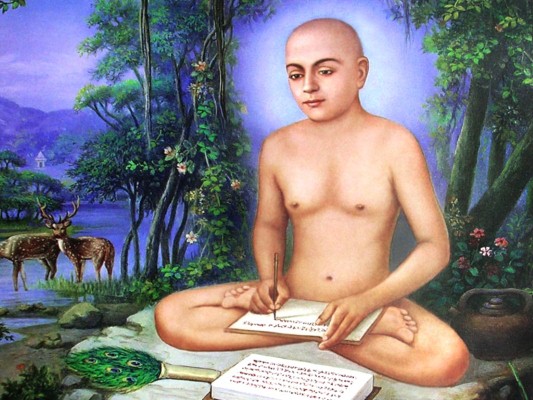- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 3) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 4) करता हूं मैं अभिनंदन
- 5) चरणों में आ पडा हूं
- 6) जब एक रत्न अनमोल
- 7) जिन बैन सुनत मोरी
- 8) जिनवर की वाणी से
- 9) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 10) जिनवाणी अमृत रसाल
- 11) जिनवाणी को नमन करो
- 12) जिनवाणी जग मैया
- 13) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 14) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 15) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 16) जिनवाणी माता दर्शन की
- 17) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 18) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 19) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 20) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 21) जिनवानी जान सुजान
- 22) तू कितनी मनहर है
- 23) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 24) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 25) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 26) परम उपकारी जिनवाणी
- 27) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 28) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 29) मंगल बेला आई आज श्री
- 30) मन भाया, तेरे दर आया
- 31) महिमा है अगम
- 32) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 33) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 34) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 35) माता तू दया करके
- 36) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 37) म्हारी माँ जिनवाणी
- 38) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 39) वीर हिमाचल तें निकसी
- 40) शरण कोई नहीं जग में
- 41) शांती सुधा बरसाये
- 42) शास्त्रों की बातों को मन
- 43) सांची तो गंगा
- 44) सारद तुम परसाद तैं
- 45) सीमंधर मुख से
- 46) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 47) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 48) हम लाए हैं विदह से
- 49) हमें निज धर्म पर चलना
- 50) हे जिनवाणी माता तुमको
- 51) हे शारदे माँ
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 8) गुरु समान दाता नहिं
- 9) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 10) गुरुवर तुम बिन कौन
- 11) जंगल में मुनिराज अहो
- 12) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 13) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 14) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 15) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 16) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 17) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 18) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 19) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 20) परम दिगम्बर यती
- 21) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 22) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 23) मुनिवर को आहार
- 24) मैं परम दिगम्बर साधु
- 25) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 26) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 27) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 28) वनवासी सन्तों को नित ही
- 29) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 30) वेष दिगम्बर धार
- 31) शान्ति सुधा बरसा गये
- 32) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 33) श्री मुनि राजत समता संग
- 34) संत साधु बन के विचरूँ
- 35) सम आराम विहारी साधुजन
- 36) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 37) हे परम दिगम्बर यति
- 38) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 39) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनशासन बड़ा निराला
- 6) जैन धर्म के हीरे मोती
- 7) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 8) भावों में सरलता रहती है
- 9) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 10) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 11) ये धर्म हमारा है हमें
- 12) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 13) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 14) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 15) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 16) हर पल हर क्षण हर दम
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
- 1) करना मन ध्यान महामंत्र
- 2) जप जप रे नवकार मंत्र
- 3) जप ले मंत्र सदा नवकार
- 4) जय जय जय कार परमेष्ठी
- 5) जो मंगल चार जगत में हैं
- 6) णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं
- 7) णमोकार नाम का ये कौन मंत्र
- 8) णमोकार मंत्र
- 9) णमोकार मन्त्र को प्रणाम हो
- 10) नमन हमारा अरिहंतों को
- 11) नवकार मंत्र रागों में
- 12) पंच परम परमेष्ठी देखे
- 13) बने जीवन का मेरा आधार रे
- 14) मंत्र जपो नवकार मनुवा
- 15) मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा
- 16) मंत्र नवकारा हृदय में धर
- 17) महामंत्र णमोकार की रचना
- 18) म्हारा पंच प्रभु भगवान
- 19) ये तो सच है कि नवकार
- 20) श्री अरिहंत सदा मंगलमय
- 21) समरो मन्त्र भलो नवकार
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अब हम अमर भये
- 9) अरे मोह में अब ना
- 10) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 11) आओ झूलें मेरे चेतन
- 12) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 13) आज खुशी है आज खुशी है
- 14) आज सी सुहानी
- 15) आतम अनुभव आवै
- 16) आतम अनुभव करना रे भाई
- 17) आतम अनुभव कीजै हो
- 18) आतम जानो रे भाई
- 19) आतमरूप अनूपम है
- 20) आतमरूप सुहावना
- 21) आत्म चिंतन का ये समय
- 22) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 23) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 24) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 25) आनंद स्रोत बह रहा
- 26) आया कहां से
- 27) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 28) इस नगरी में किस विधि
- 29) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 30) ऐ आतम है तुझको नमन
- 31) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 32) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 33) ओ जाग रे चेतन जाग
- 34) ओ जाननहारे जान जगत है
- 35) ओ जीवड़ा तू थारी
- 36) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 37) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 38) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 39) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 40) कर कर आतमहित रे
- 41) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 42) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 43) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 44) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 45) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 46) कृत पूरब कर्म मिटे
- 47) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 48) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 49) कोई राज महल में रोए
- 50) कोई लाख करे चतुराई
- 51) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 52) क्या तन मांझना रे
- 53) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 54) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 55) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 56) गुरुवर जो आपने बताया
- 57) घटमें परमातम ध्याइये
- 58) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 59) चतुर नर चेत करो भाई
- 60) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 61) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 62) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 63) चलो रे भाई अपने वतन
- 64) चेतन अपनो रूप निहारो
- 65) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 66) चेतन जाग रे
- 67) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 68) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 69) चेतन है तू ध्रुव
- 70) चेतना लक्षणम् आनंद
- 71) चेतो चेतन निज में आओ
- 72) चैतन्य के दर्पण में
- 73) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 74) जगत में सम्यक उत्तम
- 75) जन्म जन्म तन धरने
- 76) जब चले आत्माराम
- 77) जहां सत्संग होता है
- 78) जानत क्यों नहिं रे
- 79) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 80) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 81) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 82) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 83) जिया कब तक उलझेगा
- 84) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 85) जीव तू समझ ले आतम
- 86) जीवन के किसी भी पल में
- 87) जीवन के परिनामनि की
- 88) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 89) जैन धरम के हीरे मोती
- 90) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 91) जो आज दिन है वो
- 92) जो इच्छा का दमन
- 93) जो जो देखी वीतराग
- 94) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 95) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 96) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 97) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 98) तू जाग रे चेतन देव
- 99) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 100) तू निश्चय से भगवान
- 101) तू ही शुद्ध है तू ही
- 102) तेरे अंतर में भगवान है
- 103) तोड़ विषयों से मन
- 104) तोरी पल पल
- 105) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 106) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 107) थोड़ा सा उपकार कर
- 108) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 109) देख तेरी पर्याय की हालत
- 110) देखा जब अपने अंतर को
- 111) देखो भाई आतमराम
- 112) देखोजी प्रभु करमन की
- 113) धन धन जैनी साधु
- 114) धनि ते प्रानि जिनके
- 115) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 116) धिक धिक जीवन
- 117) धोली हो गई रे काली कामली
- 118) नर तन को पाकर के
- 119) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 120) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 121) परणति सब जीवन
- 122) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 123) परिग्रह डोरी से झूठ
- 124) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 125) पल पल बीते उमरिया
- 126) पाना नहीं जीवन को
- 127) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 128) पावन हो गई आज ये धरती
- 129) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 130) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 131) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 132) प्रभु पै यह वरदान
- 133) प्रभु शांत छवि तेरी
- 134) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 135) भगवंत भजन क्यों
- 136) भरतजी घर में ही वैरागी
- 137) भला कोई या विध मन
- 138) भले रूठ जाये ये सारा
- 139) भले रूठ जाये ये सारा
- 140) भव भव के दुखड़े हजार
- 141) भूल के अपना घर
- 142) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 143) मन महल में दो
- 144) ममता की पतवार ना तोडी
- 145) ममता तू न गई मोरे
- 146) महावीर--वीर भज ले रे
- 147) माया में फ़ंसे इंसान
- 148) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 149) मितवा रे सुवरण अवसर
- 150) मुझे है स्वामी उस बल
- 151) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 152) मेरा आज तलक प्रभु
- 153) मेरे शाश्वत शरण
- 154) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 155) मैं क्या माँगू भगवान
- 156) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 157) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 158) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 159) मैं निज आतम कब
- 160) मैं राजा तिहुं लोक का
- 161) मैं हूँ आतमराम
- 162) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 163) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 164) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 165) मोह की महिमा देखो
- 166) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 167) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 168) यही इक धर्ममूल है
- 169) या संसार में कोई सुखी
- 170) ये प्रण है हमारा
- 171) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 172) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 173) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 174) वन्दे जिनवरम्
- 175) विराजै रामायण घटमाहिं
- 176) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 177) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 178) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 179) संसार महा अघसागर
- 180) संसार में सुख सर्वदा
- 181) सजधज के जिस दिन
- 182) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 183) सब जग को प्यारा
- 184) समकित सुंदर शांति अपार
- 185) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 186) समझ मन स्वारथ का संसार
- 187) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 188) साधना के रास्ते आत्मा के
- 189) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 190) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 191) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 192) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 193) सुन सतगुरु की सीख
- 194) सुमर सदा मन आतमराम
- 195) सोते सोते ही निकल
- 196) स्वारथ का व्यवहार जग
- 197) हठ तजो रे बेटा हठ
- 198) हम अगर वीर वाणी
- 199) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 200) हम न किसीके कोई न हमारा
- 201) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 202) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 203) हे चेतन चेत जा अब तो
- 204) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 205) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 206) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 207) हे सीमंधर भगवान शरण
- 208) होली--जे सहज होरी के
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) वे कोई अजब तमासा
- 60) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 61) सब विधि करन उतावला
- 62) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 63) सीमंधर स्वामी
- 64) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 65) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 66) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 67) सो गुरुदेव हमारा है
- 68) सो मत सांचो है मन मेरे
- 69) स्वामीजी सांची सरन
- 70) होरी खेलूंगी घर आए
- 71) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
- 1) अरे उड़ चला हंस सैलानी
- 2) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 1) अवधू सूतां क्या इस मठ
- 2) क्योंकर महल बनावै पियारे
- 3) भोर भयो उठ जागो मनुवा
- 1) अरे मन पापनसों नित डरिये
- 2) इक योगी असन बनावे
- 3) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 4) जड़ता बिन आप लखें
- 5) लिया आज प्रभु जी ने
- 6) हिंसा झूठ वचन अरु
- 1) अष्ठाह्निका--जय सिद्धचक्र देवा
- 2) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 3) तुम सुनो सुहागन नार
- 4) भाग्य बिना कछु हाथ न आवे
- 5) मोहि सुन सुन आवे हाँसी
- 6) ये आत्मा क्या रंग दिखाता
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) कुमति को छाड़ो भाई
- 3) चिदानंद भूलि रह्यो सुधि
- 4) जीव तू भ्रमत भ्रमत
- 5) जीव निज रस राचन खोयो
- 6) देखो पुद्गल का परिवारा
- 7) देखो भूल हमारी हम
- 8) निज घर नाय पिछान्या
- 9) महावीर--सिद्धारथ राजा दरबारे
- 10) विषय रस खारे इन्हैं छाड़त
- 1) चिद्रूप हमारा इसका
- 2) भैया मेरे नरभव विषयों
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 18) महावीर जयंती आई
- 19) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 20) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 21) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 22) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 23) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 24) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 25) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 26) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 27) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 28) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 29) होरी खेलूंगी घर आए
- 30) होली--अब घर आये चेतनराज
- 31) होली--अरे मन कैसी होली
- 32) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 33) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 34) होली--और सब मिलि होरि
- 35) होली--कहा बानि परी पिय
- 36) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 37) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 38) होली--खेलौंगी होरी आये
- 39) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 40) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 41) होली--चेतन खेलै होरी
- 42) होली--जे सहज होरी के
- 43) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 44) होली--निजपुर में आज मची
- 45) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 46) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 47) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 1) आरती--बाहुबली भगवान
- 2) बाहुबली भगवान
- 3) हम यही कामना करते हैं
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 1) क्षमावणी
- 2) अक्षय-तृतीया--पण्डित-राजमल-पवैया
- 3) दीपावली-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 4) रक्षाबंधन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 5) वीरशासन-जयन्ती--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) श्रुतपंचमी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 1) अर्घ्य
- 2) महाअर्घ्य
- 3) समुच्चय-महाअर्घ्य
- 4) शांति-पाठ
- 5) शांति-पाठ-भाषा
- 6) विसर्जन-पाठ
- 7) भगवान-आदिनाथ-चालीसा
- 8) भगवान-महावीर-चालीसा
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर जी 'मुख्तार'
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
- 1) छहढाला--पण्डित-द्यानतराय
- 2) छहढाला--पं-दौलतराम
- 3) छहढाला--पं-बुधजन
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
- 1) पंच-परमेष्ठी-आरती--पण्डित-द्यानतराय
- 2) भगवान-चंदाप्रभु-आरती
- 3) भगवान-पार्श्वनाथ-आरती
- 4) भगवान-महावीर-आरती
- 5) भगवान-बाहुबली-आरती
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
- 1) लब्धिसार--नेमिचंद्र-आचार्य
- 2) गोम्मटसार-जीवकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 3) गोम्मटसार-कर्मकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 4) आस्रव-त्रिभंगी--श्रुतमुनी
- 5) भाव-संग्रह--वामदेव-आचार्य
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
- 1) आप्त-मीमांसा
- 2) लघीयस्त्रय--भट्टाकलंकदेव
- 3) परीक्षामुख
- 4) आलापपद्धति--देवसेनाचार्य
- 5) युक्त्यनुशासन--समंतभद्राचार्य
- 6) सन्मतितर्क--सिद्धसेनाचार्य
- 1) श्रुतावतार--इंद्रनंदी-आचार्य
- 2) दर्शनसार--देवसेनाचार्य
- 1) Notes
- 2) Stories
- 3) लोकप्रिय-कथाएँ
- 4) Remember
- 5) समयसार-नाटक
- 6) अर्धकथानक--बनारसीदास
ॐ
🙏

ꣽ
श्री
卐
देव
- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
शास्त्र
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 3) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 4) करता हूं मैं अभिनंदन
- 5) चरणों में आ पडा हूं
- 6) जब एक रत्न अनमोल
- 7) जिन बैन सुनत मोरी
- 8) जिनवर की वाणी से
- 9) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 10) जिनवाणी अमृत रसाल
- 11) जिनवाणी को नमन करो
- 12) जिनवाणी जग मैया
- 13) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 14) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 15) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 16) जिनवाणी माता दर्शन की
- 17) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 18) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 19) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 20) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 21) जिनवानी जान सुजान
- 22) तू कितनी मनहर है
- 23) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 24) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 25) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 26) परम उपकारी जिनवाणी
- 27) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 28) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 29) मंगल बेला आई आज श्री
- 30) मन भाया, तेरे दर आया
- 31) महिमा है अगम
- 32) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 33) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 34) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 35) माता तू दया करके
- 36) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 37) म्हारी माँ जिनवाणी
- 38) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 39) वीर हिमाचल तें निकसी
- 40) शरण कोई नहीं जग में
- 41) शांती सुधा बरसाये
- 42) शास्त्रों की बातों को मन
- 43) सांची तो गंगा
- 44) सारद तुम परसाद तैं
- 45) सीमंधर मुख से
- 46) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 47) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 48) हम लाए हैं विदह से
- 49) हमें निज धर्म पर चलना
- 50) हे जिनवाणी माता तुमको
- 51) हे शारदे माँ
गुरु
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 8) गुरु समान दाता नहिं
- 9) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 10) गुरुवर तुम बिन कौन
- 11) जंगल में मुनिराज अहो
- 12) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 13) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 14) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 15) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 16) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 17) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 18) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 19) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 20) परम दिगम्बर यती
- 21) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 22) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 23) मुनिवर को आहार
- 24) मैं परम दिगम्बर साधु
- 25) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 26) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 27) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 28) वनवासी सन्तों को नित ही
- 29) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 30) वेष दिगम्बर धार
- 31) शान्ति सुधा बरसा गये
- 32) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 33) श्री मुनि राजत समता संग
- 34) संत साधु बन के विचरूँ
- 35) सम आराम विहारी साधुजन
- 36) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 37) हे परम दिगम्बर यति
- 38) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 39) होली खेलें मुनिराज शिखर
धर्म
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनशासन बड़ा निराला
- 6) जैन धर्म के हीरे मोती
- 7) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 8) भावों में सरलता रहती है
- 9) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 10) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 11) ये धर्म हमारा है हमें
- 12) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 13) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 14) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 15) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 16) हर पल हर क्षण हर दम
तीर्थ
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
कल्याणक
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
महामंत्र
- 1) करना मन ध्यान महामंत्र
- 2) जप जप रे नवकार मंत्र
- 3) जप ले मंत्र सदा नवकार
- 4) जय जय जय कार परमेष्ठी
- 5) जो मंगल चार जगत में हैं
- 6) णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं
- 7) णमोकार नाम का ये कौन मंत्र
- 8) णमोकार मंत्र
- 9) णमोकार मन्त्र को प्रणाम हो
- 10) नमन हमारा अरिहंतों को
- 11) नवकार मंत्र रागों में
- 12) पंच परम परमेष्ठी देखे
- 13) बने जीवन का मेरा आधार रे
- 14) मंत्र जपो नवकार मनुवा
- 15) मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा
- 16) मंत्र नवकारा हृदय में धर
- 17) महामंत्र णमोकार की रचना
- 18) म्हारा पंच प्रभु भगवान
- 19) ये तो सच है कि नवकार
- 20) श्री अरिहंत सदा मंगलमय
- 21) समरो मन्त्र भलो नवकार
अध्यात्म
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अब हम अमर भये
- 9) अरे मोह में अब ना
- 10) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 11) आओ झूलें मेरे चेतन
- 12) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 13) आज खुशी है आज खुशी है
- 14) आज सी सुहानी
- 15) आतम अनुभव आवै
- 16) आतम अनुभव करना रे भाई
- 17) आतम अनुभव कीजै हो
- 18) आतम जानो रे भाई
- 19) आतमरूप अनूपम है
- 20) आतमरूप सुहावना
- 21) आत्म चिंतन का ये समय
- 22) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 23) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 24) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 25) आनंद स्रोत बह रहा
- 26) आया कहां से
- 27) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 28) इस नगरी में किस विधि
- 29) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 30) ऐ आतम है तुझको नमन
- 31) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 32) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 33) ओ जाग रे चेतन जाग
- 34) ओ जाननहारे जान जगत है
- 35) ओ जीवड़ा तू थारी
- 36) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 37) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 38) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 39) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 40) कर कर आतमहित रे
- 41) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 42) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 43) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 44) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 45) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 46) कृत पूरब कर्म मिटे
- 47) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 48) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 49) कोई राज महल में रोए
- 50) कोई लाख करे चतुराई
- 51) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 52) क्या तन मांझना रे
- 53) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 54) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 55) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 56) गुरुवर जो आपने बताया
- 57) घटमें परमातम ध्याइये
- 58) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 59) चतुर नर चेत करो भाई
- 60) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 61) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 62) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 63) चलो रे भाई अपने वतन
- 64) चेतन अपनो रूप निहारो
- 65) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 66) चेतन जाग रे
- 67) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 68) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 69) चेतन है तू ध्रुव
- 70) चेतना लक्षणम् आनंद
- 71) चेतो चेतन निज में आओ
- 72) चैतन्य के दर्पण में
- 73) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 74) जगत में सम्यक उत्तम
- 75) जन्म जन्म तन धरने
- 76) जब चले आत्माराम
- 77) जहां सत्संग होता है
- 78) जानत क्यों नहिं रे
- 79) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 80) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 81) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 82) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 83) जिया कब तक उलझेगा
- 84) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 85) जीव तू समझ ले आतम
- 86) जीवन के किसी भी पल में
- 87) जीवन के परिनामनि की
- 88) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 89) जैन धरम के हीरे मोती
- 90) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 91) जो आज दिन है वो
- 92) जो इच्छा का दमन
- 93) जो जो देखी वीतराग
- 94) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 95) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 96) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 97) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 98) तू जाग रे चेतन देव
- 99) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 100) तू निश्चय से भगवान
- 101) तू ही शुद्ध है तू ही
- 102) तेरे अंतर में भगवान है
- 103) तोड़ विषयों से मन
- 104) तोरी पल पल
- 105) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 106) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 107) थोड़ा सा उपकार कर
- 108) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 109) देख तेरी पर्याय की हालत
- 110) देखा जब अपने अंतर को
- 111) देखो भाई आतमराम
- 112) देखोजी प्रभु करमन की
- 113) धन धन जैनी साधु
- 114) धनि ते प्रानि जिनके
- 115) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 116) धिक धिक जीवन
- 117) धोली हो गई रे काली कामली
- 118) नर तन को पाकर के
- 119) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 120) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 121) परणति सब जीवन
- 122) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 123) परिग्रह डोरी से झूठ
- 124) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 125) पल पल बीते उमरिया
- 126) पाना नहीं जीवन को
- 127) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 128) पावन हो गई आज ये धरती
- 129) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 130) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 131) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 132) प्रभु पै यह वरदान
- 133) प्रभु शांत छवि तेरी
- 134) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 135) भगवंत भजन क्यों
- 136) भरतजी घर में ही वैरागी
- 137) भला कोई या विध मन
- 138) भले रूठ जाये ये सारा
- 139) भले रूठ जाये ये सारा
- 140) भव भव के दुखड़े हजार
- 141) भूल के अपना घर
- 142) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 143) मन महल में दो
- 144) ममता की पतवार ना तोडी
- 145) ममता तू न गई मोरे
- 146) महावीर--वीर भज ले रे
- 147) माया में फ़ंसे इंसान
- 148) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 149) मितवा रे सुवरण अवसर
- 150) मुझे है स्वामी उस बल
- 151) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 152) मेरा आज तलक प्रभु
- 153) मेरे शाश्वत शरण
- 154) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 155) मैं क्या माँगू भगवान
- 156) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 157) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 158) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 159) मैं निज आतम कब
- 160) मैं राजा तिहुं लोक का
- 161) मैं हूँ आतमराम
- 162) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 163) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 164) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 165) मोह की महिमा देखो
- 166) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 167) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 168) यही इक धर्ममूल है
- 169) या संसार में कोई सुखी
- 170) ये प्रण है हमारा
- 171) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 172) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 173) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 174) वन्दे जिनवरम्
- 175) विराजै रामायण घटमाहिं
- 176) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 177) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 178) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 179) संसार महा अघसागर
- 180) संसार में सुख सर्वदा
- 181) सजधज के जिस दिन
- 182) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 183) सब जग को प्यारा
- 184) समकित सुंदर शांति अपार
- 185) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 186) समझ मन स्वारथ का संसार
- 187) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 188) साधना के रास्ते आत्मा के
- 189) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 190) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 191) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 192) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 193) सुन सतगुरु की सीख
- 194) सुमर सदा मन आतमराम
- 195) सोते सोते ही निकल
- 196) स्वारथ का व्यवहार जग
- 197) हठ तजो रे बेटा हठ
- 198) हम अगर वीर वाणी
- 199) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 200) हम न किसीके कोई न हमारा
- 201) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 202) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 203) हे चेतन चेत जा अब तो
- 204) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 205) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 206) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 207) हे सीमंधर भगवान शरण
- 208) होली--जे सहज होरी के
पं दौलतराम कृत
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
पं भागचंद कृत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
पं द्यानतराय कृत
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
पं सौभाग्यमल कृत
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
पं भूधरदास कृत
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) वे कोई अजब तमासा
- 60) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 61) सब विधि करन उतावला
- 62) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 63) सीमंधर स्वामी
- 64) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 65) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 66) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 67) सो गुरुदेव हमारा है
- 68) सो मत सांचो है मन मेरे
- 69) स्वामीजी सांची सरन
- 70) होरी खेलूंगी घर आए
- 71) होली--अहो दोऊ रंग भरे
पं बुधजन कृत
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
पं मंगतराय कृत
पं न्यामतराय कृत
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
पं बनारसीदास कृत
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
पं ज्ञानानन्द कृत
पं नयनानन्द कृत
पं मख्खनलाल कृत
पं बुध महाचन्द्र
सहजानन्द वर्णी
पर्व
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 18) महावीर जयंती आई
- 19) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 20) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 21) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 22) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 23) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 24) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 25) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 26) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 27) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 28) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 29) होरी खेलूंगी घर आए
- 30) होली--अब घर आये चेतनराज
- 31) होली--अरे मन कैसी होली
- 32) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 33) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 34) होली--और सब मिलि होरि
- 35) होली--कहा बानि परी पिय
- 36) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 37) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 38) होली--खेलौंगी होरी आये
- 39) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 40) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 41) होली--चेतन खेलै होरी
- 42) होली--जे सहज होरी के
- 43) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 44) होली--निजपुर में आज मची
- 45) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 46) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 47) होली खेलें मुनिराज शिखर
चौबीस तीर्थंकर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
बाहुबली भगवान
बधाई
दस धर्म
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
बच्चों के भजन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
मारवाड़ी
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
selected
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
प्रारम्भ
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
नित्य पूजा
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
तीर्थंकर
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
पर्व पूजन
विसर्जन
पाठ
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर जी 'मुख्तार'
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
स्तोत्र
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
ग्रंथ
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
चरणानुयोग
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
इतिहास
Notes
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
Youtube -- शास्त्र गाथा
Youtube -- Animations
- भगवान नमिनाथ
- भगवान बाहुबली
- सुकुमाल मुनि
- कुन्दकुन्द आचार्य
- रक्षाबंधन की कथा
- समवसरण
- चार-गति
- श्रुत-पंचमी
- अक्षय-तृतीया
- उद्दायन राजा
- राजा श्रेणिक और मेंढक
- अंजन-चोर की कथा
- पांच-पाप
- जीव-दया
- गर्भ-कल्याणक
- जन्म-कल्याणक
- तप-कल्याणक
- णमोकार-मंत्र
- कुलाचार
- स्थावर-जीव
- तीर्थंकर
- जीव-अजीव
- चतुर्विध-संघ
- प्रात:कालीन वन्दना
प्रमाण
PDF शास्त्र
- गोम्मटसार-जीवकांड
- तत्त्वार्थसूत्र-चार्ट
- तत्त्वार्थसूत्र-English
- पाहुड-दोहा
- तत्त्वानुशासन
- लघुतत्त्व-स्फोट
- परम-अध्यात्म-तरंगिनी
- ज्ञानार्णव
- भगवती-आराधना
- आराधानासार
- जैन-सिद्धांत-प्रवेशिका
- समयसार
- योगसार
- प्रवचनसार
- पन्चास्तिकाय
- द्रव्यसंग्रह
- दर्शनसार
- तत्त्वार्थसूत्र
- आलापपद्धति
- इष्टोपदेश
- परमात्मप्रकाश
- पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
- बारसणुपेक्_खा
- रत्नकरण्ड-श्रावकाचार
- श्रीअष्टपाहुड
- समाधितन्त्र
- स्वरूप-संबोधन
- उत्तर-पुराण
- आदि-पुराण
- आराधना-कथा-कोश
Jain Comics
- FruitsOfAuspiciousActs
- JeevandharSwami
- अज्ञात-प्रतिमा-की-खोज
- आटे-का-मुर्गा
- ऋषभदेव
- कविवर-बनारसीदास
- कुन्दकुन्दाचार्य
- गए-जा-गीत-अपन-के
- गोमटेश्वर-बाहुबली
- चंदनबाला
- चौबीस-तीर्थंकर-१
- चौबीस-तीर्थंकर-२
- जनक-नन्दिनी-सीता
- जीवंधर-स्वामी
- जो-करे-सो-भरे
- टीले-वाले-बाबा
- ताली-एक-हाथ-से-बजती-रही
- तीन-दिन-में
- धर्म-के-दश-लक्षण
- पुण्य-का-फल
- प्रद्युम्न-हरण
- प्रेय-की-भभूत
- महादानी-भामाशाह
- महाबली-हनूमान
- महारानी-चेलना-की-विजय
- मुनि-रक्षा
- राजुल
- रूप-जो-बदला-नहीं-जाता
- सिकन्दर-और-कल्याण-मुनि
Print Granth
Kids Games
छहढाला
मंगलाचरण
कविवर बुधजन कृत
सर्व द्रव्य में सार, आतम को हितकार हैं
नमो ताहि चितधार, नित्य निरंजन जानके ॥
सर्व द्रव्य में सार, आतम को हितकार हैं
नमो ताहि चितधार, नित्य निरंजन जानके ॥
अन्वयार्थ : जो समस्त द्रव्यों में सार है एवं आत्मा को हितकार है, ऐसे नित्य-निरंजन स्वरूप को जानकर उसे चित्त मे धारण करके मैं नमस्कार करता हूँ ।
ढाल-1
अथिर-भावना
आयु घटे तेरी दिन-रात, हो निश्चिंत रहो क्यों भ्रात
यौवन तन धन किंकर नारि, हैं सब जल बुदबुद उनहारि ॥१॥
यौवन तन धन किंकर नारि, हैं सब जल बुदबुद उनहारि ॥१॥
अन्वयार्थ : हे भाई! तेरी आयु दिन-रात घटती ही जा रही है फिर भी तू निश्चिंत कैसे हो रहा है ? यह यौवन, शरीर, लक्ष्मी, सेवक, स्त्री आदि सभी पानी के बुलबुले समान क्षण-भंगुर हैं ।
अशरण-भावना
पूरण आयु बढे छिन नाहिं, दिये कोटि धन तीरथ मांहि
इन्द्र चक्रपति हू क्या करैं, आयु अन्त पर वे हू मरैं ॥२॥
इन्द्र चक्रपति हू क्या करैं, आयु अन्त पर वे हू मरैं ॥२॥
अन्वयार्थ : आयु समाप्त होने पर एक क्षण भी बढती नहीं, भले करोडों रुपया-धनादि तीर्थों पर दान करो । इन्द्र चक्रवर्ती भी क्या करे ? आयु पूर्ण होने पर वे भी मरते हैं ।
संसार-भावना
यों संसार असार महान, सार आप में आपा जान
सुख से दुख, दुख से सुख होय, समता चारों गति नहिं कोय ॥३॥
सुख से दुख, दुख से सुख होय, समता चारों गति नहिं कोय ॥३॥
अन्वयार्थ : इस प्रकार यह संसार अत्यन्त असार है, उसमें अपना आत्मा ही मात्र सार है । संसार में सुख के पश्चात दुःख एवं दुःख के पश्चात सुखरूप आकुलता होती ही रहती है । चारों गतियों में कहीं भी लेशमात्र सुख शान्ति नहीं है ।
एकत्व-भावना
अनंतकाल गति-गति दुख लह्यो, बाकी काल अनंतो कह्यो
सदा अकेला चेतन एक, तो माहीं गुण वसत अनेक ॥४॥
सदा अकेला चेतन एक, तो माहीं गुण वसत अनेक ॥४॥
अन्वयार्थ : इस जीव ने अनादिकाल से चारों ही गतियों मे दुख ही पाया और बाकी अनन्तकाल पर्यन्त चारों-गतियां रहने वाली है। चारों-गति मे जीव अकेला ही रहता है। तू चेतन एक है तो भी उसमें अनन्त गुण बसते हैं - सदाकाल विद्यमान रहते हैं ।
अन्यत्व-भावना
तू न किसी का तेरा न कोय, तेरा सुख दुख तोकों होय
याते तोकों तू उर धार, पर द्रव्यनतें ममत निवार ॥५॥
याते तोकों तू उर धार, पर द्रव्यनतें ममत निवार ॥५॥
अन्वयार्थ : तू अन्य किसी का नहीं और अन्य भी तेरा कोई नहीं है । तेरा सुख-दुख तुझको ही होता है, इसलिये पर-द्रव्य पर-भावों से भिन्न अपने स्वरूप को तू अन्तर मे धारण कर एवं समस्त पर-द्रव्य, पर-भावों से मोह छोड ।
अशुचि-भावना
हाड़ मांस तन लिपटी चाम, रुधिर मूत्र- मल पूरित धाम
सो भी थिर न रहे क्षय होय, याको तजे मिले शिव लोय ॥६॥
सो भी थिर न रहे क्षय होय, याको तजे मिले शिव लोय ॥६॥
अन्वयार्थ : हाड-मांस से भरा हुआ यह शरीर ऊपर से चमड़ी से मढा हुआ है, अन्दर तो रुधिर मल-मूत्रादि से भरा हुआ धाम है । ऐसा होने पर भी वह स्थिर तो रहता ही नहीं, निश्चयकर क्षय को प्राप्त हो जाता है । देह से एकत्व-ममत्व हटते ही जीव को मोक्षमार्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ।
आस्रव-भावना
हित अनहित तन कुलजन मांहि, खोटी बानि हरो क्यों नाहिं
याते पुद्गल-करमन जोग, प्रणवे दायक सुख-दुख रोग ॥७॥
याते पुद्गल-करमन जोग, प्रणवे दायक सुख-दुख रोग ॥७॥
अन्वयार्थ : शरीर, कुटुम्बी-जन इत्यादि मे हित-अनहितरूप मिथ्या प्रवृत्ति को तू क्यों नही छोडता? इस मिथ्या प्रवृत्ति से तो पुद्गल कर्मों का आस्रव-बन्ध होता है, जो कि साता-असतारूप सुखदुख रोग को देने वाला होकर परिणमता है ।
संवर-भावना
पांचों इन्द्रिन के तज फ़ैल, चित्त निरोध लाग शिव- गैल
तुझमे तेरी तू करि सैल, रहो कहा हो कोल्हू बैल ॥८-संवर॥
तुझमे तेरी तू करि सैल, रहो कहा हो कोल्हू बैल ॥८-संवर॥
अन्वयार्थ : तू पाँचो-इन्द्रियो के विषयों को रोककर, चित्त निरोध करके (संकल्प-विकल्प रूप मिथ्याभावों का परिहार करके) मोक्षमार्ग मे लग जाना । तू अपने को जड-पत्थर सदृश कर अपने पुरुषार्थ मे देरी क्यो कर रहा है ? व्यर्थ ही कोल्हू के बैल की भान्ति क्यो भटक रहा है ।
निर्जरा-भावना
तज कषाय मन की चल चाल, ध्यावो अपनो रूप रसाल
झड़े कर्म-बंधन दुखदान, बहुरि प्रकाशै केवलज्ञान ॥९॥
झड़े कर्म-बंधन दुखदान, बहुरि प्रकाशै केवलज्ञान ॥९॥
अन्वयार्थ : तू कषाय एवं मन की चंचल वृत्ति को छोडकर, आनन्द-रस से भरे हुये अपने निज-स्वरूप को ध्याओ, जिससे कि दुखदायी कर्म झड जावे और केवल-ज्ञान प्रकाश प्रगट हो ।
लोक-भावना
तेरो जन्म हुओ नहिं जहां, ऐसा खेतर नाहीं कहाँ
याही जन्म-भूमिका रचो, चलो निकसि तो विधि से बचो ॥१०॥
याही जन्म-भूमिका रचो, चलो निकसि तो विधि से बचो ॥१०॥
अन्वयार्थ : सम्पूर्ण लोक मे ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नही जहाँ तेरा जन्म न हुआ हो । तू इसी जन्मभूमि मे मोहित होकर क्यो मगन हो रहा है ? तू सम्यक् पुरुषार्थी बनकर इस लोक से निकल अर्थात् अशरीरी जो सिद्धपद उसमे स्थिर हो । तभी तू सकल कर्म-बन्धन से छूट सकेगा ।
बोधि-भावना
सब व्यवहार क्रिया को ज्ञान, भयो अनंती बार प्रधान
निपट कठिन 'अपनी' पहिचान, ताको पावत होत कल्याण ॥११॥
निपट कठिन 'अपनी' पहिचान, ताको पावत होत कल्याण ॥११॥
अन्वयार्थ : सर्व व्यवहार-क्रियाओं का ज्ञान तो तुझे अनन्ती बार हुआ, परन्तु जिसकी प्राप्ति से कल्याण होता है ऐसे निज-चिदानन्द घनस्वरुप की पहचान अत्यन्त दुर्लभ है । अत: उसही की पहचान करना योग्य है, ऐसा तू जान ।
धर्म-भावना
धर्म स्वभाव आप सरधान, धर्म न शील न न्हौंन न दान
'बुधजन' गुरु की सीख विचार, गहो धाम आतम सुखकार ॥१२॥
'बुधजन' गुरु की सीख विचार, गहो धाम आतम सुखकार ॥१२॥
अन्वयार्थ : निज-स्वभाव का श्रद्धान करना ही धर्म है । धर्म न तो बाह्य शीलादि पालने मे है,न स्नान करने में है और न दानादि देने मे है । हे बुधजन ! तुम श्रीगुरु के इस उपदेश पर विचार करो और निज-स्वरुप का निर्णय करके आत्मधर्म को ग्रहण करो ।
ढाल-2
सुन रे जीव कहत हूँ तोकों, तेरे हित के काजै
हो निश्चल मन जो तू धारे, तब कछु-इक तोहि लाजे ॥
जिस दुख से थावर तन पायो, वरन सको सो नाहीं
अठदश बार मरो अरु जीयो, एक स्वास के माहीं ॥१॥
हो निश्चल मन जो तू धारे, तब कछु-इक तोहि लाजे ॥
जिस दुख से थावर तन पायो, वरन सको सो नाहीं
अठदश बार मरो अरु जीयो, एक स्वास के माहीं ॥१॥
अन्वयार्थ : हे जीव! ध्यान पूर्वक सुन, तेरे हित के लिये तुझको कहता हूँ । जो यह हित की बात स्थिर-चित्त होकर तू अब धारण करेगा तो तुझे कुछ तो लज्जा आवेगी कि अरे! अभी तक यह मैंने क्या किया? अज्ञान से मैं कितना दुखी हुआ। एकेन्द्रिय स्थावर शरीर धारण कर जो अत्यन्त दुख भोगे, उसे शब्दों मे वर्णन किया जा सके - ऐसा नहीं है ।
काल अनतानंत रह्यो यों, पुनि विकलत्रय हूवो
बहुरि असैनी निपट अज्ञानी, छिनछिन जीओ मूवो ॥
ऐसे जन्म गयो करमन-वश, तेरो जोर न चाल्यो
पुन्य उदय सैनी पशु हूवो, बहुत ज्ञान नहिं भाल्यो ॥२॥
बहुरि असैनी निपट अज्ञानी, छिनछिन जीओ मूवो ॥
ऐसे जन्म गयो करमन-वश, तेरो जोर न चाल्यो
पुन्य उदय सैनी पशु हूवो, बहुत ज्ञान नहिं भाल्यो ॥२॥
अन्वयार्थ : हे जीव ! इसप्रकार तू अनन्तानन्त काल पर्यन्त एकेन्द्रिय पर्याय मे रहा, पश्चात कभी दो इन्द्रियादि विकलत्रय पर्याय वाला हुआ, कदाचित् पंचेन्द्रिय-पर्याय भी पाई तो असंज्ञी महा-अज्ञानी रहा और क्षण-क्षण मे जन्म-मरण किया । इस प्रकार अज्ञान से कर्मोदय वश होकर तूने अनन्त जन्म धारण किये, वहाँ तेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं हो सका, पश्चात पुण्योदय से कदाचित् संज्ञी-पशु भी हुआ तो भी वहां तू भेदज्ञान प्राप्त नहीं कर सका ।
जबर मिलो तब तोहि सतायो, निबल मिलो ते खायो
मात त्रिया-सम भोगी पापी, तातें नरक सिधायो ॥
कोटिन बिच्छू काटत जैसे, ऐसी भूमि तहाँ है
रुधिर-राध जल छार बहे जहां, दुर्गन्ध निपट तहाँ है ॥३॥
मात त्रिया-सम भोगी पापी, तातें नरक सिधायो ॥
कोटिन बिच्छू काटत जैसे, ऐसी भूमि तहाँ है
रुधिर-राध जल छार बहे जहां, दुर्गन्ध निपट तहाँ है ॥३॥
अन्वयार्थ : तुझ से बलवान पशुओं ने तुझे सताया और निर्बल मिला तो तूने उसे मारकर खाया । पशु दशा मे तूने माता को स्त्री समान भोगा, इसलिये तू पापी होकर नरकों मे जा पडा । जहाँ की भूमि ऐसी कठोर है कि उसका स्पर्श होते ही मानों करोडों बिच्छू काटते हो - ऐसा दुख होता है और जहाँ अत्यन्त दुर्गन्ध-युक्त सड़े लहू से भरी खारे-जल जैसी वैतरणी नदी बहती है ।
घाव करै असिपत्र अंग में, शीत ऊष्ण तन गाले
कोई काटे करवत कर गह, कोई पावक जालें ॥
यथायोग सागर-थिति भुगते, दुख को अंत न आवे
कर्म-विपाक इसो ही होवे, मानुष गति तब पावै ॥४॥
कोई काटे करवत कर गह, कोई पावक जालें ॥
यथायोग सागर-थिति भुगते, दुख को अंत न आवे
कर्म-विपाक इसो ही होवे, मानुष गति तब पावै ॥४॥
अन्वयार्थ : नरक मे असिपत्र अंग पर पडते ही घाव कर देते हैं । अत्यधिक शीत एवं प्रचन्ड गर्मी देह को गला देती है । कोई नारकी दूसरे नारकी को पकडकर करोंत से काट डालते हैं और अग्नि मे जला देते हैं । आयु बन्धन वश सागरोपम की स्थिति पर्यन्त इस प्रकार के महादु:खों को भोगते पार नही आता - वहाँ कर्म का विपाक ऐसा ही होता है । उसे पूर्णकर कदाचित मन्द-कषाय अनुसार शुभ-कर्म का विपाक होने पर कोई नारकी नरक मे से निकलकर मनुष्यगति प्राप्त करता है ।
मात उदर मे रहो गेंद ह्वै, निकसत ही बिललावे
डंभा दांत गला विष फोटक, डाकिन से बच जावे ॥
तो यौवन में भामिनि के संग, निशि-दिन भोग रचावे
अंधा ह्वै धंधे दिन खोवै, बूढा नाड़ हिलावे ॥५॥
डंभा दांत गला विष फोटक, डाकिन से बच जावे ॥
तो यौवन में भामिनि के संग, निशि-दिन भोग रचावे
अंधा ह्वै धंधे दिन खोवै, बूढा नाड़ हिलावे ॥५॥
अन्वयार्थ : मनुष्यगति मे भी माता के गर्भ में संकुचित होकर गेन्द की तरह नव-मास तक रहता है और पीछे जन्मते समय त्रास से बिल्लाता है । बालकपन मे अनेक प्रकार के रोग जहरीले फोडे, चेचक, दाँत-गले आदि के रोग आदि से कदाचित बच जावे तो जवानी में निशदिन पत्नी के साथ भोग-विलास मे ही मग्न रहता है, नये-नये भोग रुचाता है और व्यापार धन्धों में अन्धा होकर जिन्दगी व्यतीत कर देता है । जब वृद्ध हो जाता है तब मस्तक आदि अंग कांपने लग जाते हैं -- इस प्रकार मूढ मोही जीव, आत्मा के हित का उपाय किये बिना मनुष्य-भव व्यर्थ ही गंवा देता है ।
जम पकडे तब जोर न चाले, सैनहि सैन बतावै
मंद कषाय होय तो भाई, भवनत्रिक पद पावै ॥
पर की संपति लखि अति झूरे, कै रति काल गमावै
आयु अंत माला मुरझावै, तब लखि लखि पछतावे ॥६॥
मंद कषाय होय तो भाई, भवनत्रिक पद पावै ॥
पर की संपति लखि अति झूरे, कै रति काल गमावै
आयु अंत माला मुरझावै, तब लखि लखि पछतावे ॥६॥
अन्वयार्थ : जब मरण काल आ उपस्थित हो तब इस जीव का कुछ भी जोर नही चलता, बोल भी नहीं सकता, अत: मन की बात इशारा कर-करके बतलाता है । इस प्रकार कुमरण भाव से मरकर जो मन्द-कषाय रुप भाव हो तो भवनवासी-व्यन्तर या ज्योतिषी - इन हल्की जाति के देवों मे उत्पन्न होता है । वहाँ अन्य दूसरे बडे वैभववान देवों की सम्पदा देखकर खूब कुढ़ता है । अथवा विषय-क्रीडा रुप रति मे ही काल गंवाता है । आयु का अन्त आने पर उस देव की मन्दार-माला मुरझाने लगती है, उसे देखकर वह जीव बहुत ही पछताता है ।
तह तैं चयकर थावर होता, रुलता काल अनन्ता
या विध पंच परावृत पूरत, दुख को नाहीं अन्ता ॥
काललब्धि जिन गुरु-कृपा से, आप आप को जानो
तबही 'बुधजन' भवदधि तिरके, पहुँच जाय शिव-थाने ॥७॥
या विध पंच परावृत पूरत, दुख को नाहीं अन्ता ॥
काललब्धि जिन गुरु-कृपा से, आप आप को जानो
तबही 'बुधजन' भवदधि तिरके, पहुँच जाय शिव-थाने ॥७॥
अन्वयार्थ : और वह देव आर्तध्यान पूर्वक देवलोक से चयकर स्थावर हो जाता है । इसप्रकार अज्ञान से संसार मे भ्रमते-भ्रमते जीव ने अनन्त काल पर्यन्त पंच-परावर्तन किया और अनन्त दुख पाया । निज काल-लब्धि रूप सुसमय आने पर जिन गुरु की कृपा से जब आत्मा स्वयं अपना स्वरूप जानले, मानले और अनुभव करले तव वह जीव भव-समुद्र से तिर कर निवार्ण रुप सिद्धपद मे पहुँच जाता है, जहाँ पाश्वत सुखी रहता है ।
ढाल-3
(पद्धरि छंद)
इस विधि भववन के मांहि जीव, वश मोह गहल सोता सदीव
उपदेश तथा सहजै प्रबोध, तबही जागै ज्यों उठत जोध ॥१॥
इस विधि भववन के मांहि जीव, वश मोह गहल सोता सदीव
उपदेश तथा सहजै प्रबोध, तबही जागै ज्यों उठत जोध ॥१॥
अन्वयार्थ : इस प्रकार संसाररूपी वन मे मोह-वश पडा जीव बेसुध होकर सदा गहरी निद्रा मे सोया हुआ है । परन्तु जब आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से अथवा पूर्व-संस्कार के बल से वह मोह-निद्रा से जागा / जिस प्रकार रण मे मूर्छित हुआ योद्धा फिर से जाग गया हो, उसी प्रकार यह संसारी-जीव मोह-निद्रा दूर करके जाग गया ।
जब चिंतवत अपने माहिं आप, हूँ चिदानन्द नहिं पुन्य-पाप
मेरो नाहीं है राग भाव, यह तो विधिवश उपजै विभाव ॥२॥
मेरो नाहीं है राग भाव, यह तो विधिवश उपजै विभाव ॥२॥
अन्वयार्थ : आत्मभान करके जब यह संसारी मोही-जीव जाग गया तब ही अपने अन्तरंग मे अपने स्वरूप का ऐसा चिन्तवन करने लगा कि 'मैं चिदानन्द हूँ, पुण्य-पाप मैं नही हूँ, रागभाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, वह तो कर्मवश उत्पन्न हुआ विभाव भाव है' ।
हूँ नित्य निरंजन सिद्ध समान, ज्ञानावरणी आच्छाद ज्ञान
निश्चय सुध इक व्यवहार भेव, गुण-गुणी अंग-अंगी अछेव ॥३॥
निश्चय सुध इक व्यवहार भेव, गुण-गुणी अंग-अंगी अछेव ॥३॥
अन्वयार्थ : मैं सिद्ध-समान नित्य अविनाशी जीव-तत्त्व है, द्रव्य-कर्म, नोकर्म और भावकर्म से रहित हूँ । ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मेरा ज्ञान अप्रगट है । निश्चय से मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, गुण-गुणी भेद अथवा अंश-अंशी भेद आदि सर्व-भेद कल्पना तो व्यवहार से है । मैं तो अभेद हूँ ।
मानुष सुर नारक पशुपर्याय, शिशु युवा वृद्ध बहुरूप काय
धनवान दरिद्री दास राय, ये तो विडम्ब मुझको न भाय ॥४॥
धनवान दरिद्री दास राय, ये तो विडम्ब मुझको न भाय ॥४॥
अन्वयार्थ : तथा मनुष्य-देव नारकी व पशु पर्याय अथवा बालक, जवान, वृद्ध इत्यादि अनेक रूप शरीर की ही अवस्थाये हैं तथा धनवानपना, दासपना, राजापना ये सभी औपाधिक भाव विडम्बना है - उपाधि है, वे कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है, मेरे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप में ये कुछ भी शोभता नहीं ।
रस फरस गंध वरनादि नाम, मेरे नाहीं मैं ज्ञानधाम
मैं एकरूप नहिं होत और, मुझमें प्रतिबिम्बत सकल ठौर ॥५॥
मैं एकरूप नहिं होत और, मुझमें प्रतिबिम्बत सकल ठौर ॥५॥
अन्वयार्थ : स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण आदि अथवा व्यवहार नाम आदि मेरे नहीं, ये सभी तो पुद्गल द्रव्य के हैं, मैं तो ज्ञानधाम हूँ । मैं तो सदाकाल एकरूप रहने वाला परमात्मा हूँ, अन्यरूप कभी भी नहीं होता । मेरे ज्ञान-दर्पण में तो समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ।
तन पुलकित उर हरषित सदीव, ज्यों भई रंकगृह निधि अतीव
जब प्रबल अप्रत्याख्यान थाय, तब चित परिणति ऐसी उपाय ॥६॥
जब प्रबल अप्रत्याख्यान थाय, तब चित परिणति ऐसी उपाय ॥६॥
अन्वयार्थ : ऐसा भेदविज्ञान पूर्वक सम्यक श्रद्धान होने पर जीव सदा ही अतिशय प्रसन्न होता है, आनन्दित होता है । हृदय में निरन्तर हर्ष वर्तने से शरीर भी पुलकित हो जाता है । जिस प्रकार दरिद्री के घर मे अत्यधिक धन-निधि के प्रगट होने पर वह प्रसन्न होता है, उसी प्रकार यह सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर मे निजानन्द मूर्ति भगवान आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है । ऐसा सम्यकदर्शन हो जाने पर जब तक अप्रत्याख्यान कषाय की प्रबलता रूप उदय रहता है तब तक उस सम्यग्दृष्टि की चित्त परिणति कैसी होती है - उसे अब यहां पर कहते हैं ।
सो सुनो भव्य चित धार कान, वरणत हूँ ताकी विधि विधान
सब करै काज घर मांहि वास, ज्यों भिन्न कमल जल में निवास ॥७॥
सब करै काज घर मांहि वास, ज्यों भिन्न कमल जल में निवास ॥७॥
अन्वयार्थ : हे भव्य जीवों ! तुम चित्त लगाकर उस भेद-विज्ञानी की परिणति को सुनो । उस अविरत सम्यक्दृष्टि के विधि-विधान का मैं वर्णन करता हूँ । स्वानुभव बोध का जिसे लाभ हुआ है, ऐसा वह जीव घर-कुटुम्ब के बीच में रहता है तथा सभी गृहकार्य, व्यापार आदि भी करता दिखाई देता है, परन्तु जैसे जल में कमल का वास होने पर भी वह जल से भिन्न अलिप्त रहता है । उसी प्रकार गृहवास में रहता होने पर भी धर्मी जीव उस घर, कुटम्ब, व्यापार आदि से भिन्न-अलिप्त एवं उदास रहता है ।
ज्यों सती अंग माहीं सिंगार, अति करत प्यार ज्यों नगर नारि
ज्यों धाय चखावत आन बाल, त्यों भोग करत नाहीं खुशाल ॥८॥
ज्यों धाय चखावत आन बाल, त्यों भोग करत नाहीं खुशाल ॥८॥
अन्वयार्थ : जैसे शीलवान स्त्री के शरीर का श्रंगार पर-पुरुष के प्रति राग के लिए नही होता, जैसे वेश्या अतिशय-प्रेम दिखाती है परन्तु वह अन्तरंग का प्रेम नही होता और जैसे धाय-माता अन्य दूसरे के बालक को दूध पिलाती है, परन्तु अन्तरंग में वह धाय उस बालक को पराया ही जानती है; ठीक उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव संसार के भोगों को भोगता हुआ दिखता है, तथापि उसे उन भोगों में खुशी नहीं, उनमें वह सुख नहीं मानता, उनसे तो वह अन्तरंग श्रद्धान में विरक्त ही है ।
जब उदय मोह चारित्र भाव, नहिं होत रंच हू त्याग भाव
तहाँ करै मंद खोटी कषाय, घर में उदास हो अथिर थाय ॥९॥
तहाँ करै मंद खोटी कषाय, घर में उदास हो अथिर थाय ॥९॥
अन्वयार्थ : जबतक उसे चारित्र-मोह रूप कर्म प्रकृति का तीव्र उदय रहता है तबतक वह जीव रंचमात्र भी त्याग भावरूप व्रत-धारण नही कर सकता है । परन्तु वह अशुभ रूप कषायों को शुभभाव रूप करता है और वह अस्थिरपने वश उदास चित्त वाला होकर घर मे रहता हुआ दिखता है ।
सबकी रक्षा युत न्याय नीति, जिनशासन गुरु की दृढ़ प्रतीति
बहु रुले अर्द्ध-पुद्गल प्रमान, अंतरमुहूर्त ले परम थान ॥१०॥
बहु रुले अर्द्ध-पुद्गल प्रमान, अंतरमुहूर्त ले परम थान ॥१०॥
अन्वयार्थ : और वह सम्यग्दृष्टि जीव सभी जीवों की रक्षा-सहित न्याय-नीति से प्रवर्त्तता है, सर्वज्ञ भगवान के उपदेश को एवं सच्चे-गुरु की द्रढ़-प्रतीति करता है । यदि सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जावे तो यह अधिक से अधिक अर्द्ध पुदगल-परावर्तन प्रमाण काल तक संसार में रह सकता है और यदि उग्र पुरुषार्थ साधे तो शीघ्र ही अन्तरमुहूर्त मात्र काल में परमधाम रूप निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है ।
वे धन्य जीव धन भाग सोय, जाके ऐसी परतीत होय
ताकी महिमा ह्वै स्वर्ग लोय, बुधजन भाषे मोतैं न होय ॥११॥
ताकी महिमा ह्वै स्वर्ग लोय, बुधजन भाषे मोतैं न होय ॥११॥
अन्वयार्थ : जिसे सम्यग्दर्शन हुआ है, वे जीव धन्य हैं, वही धन्य भाग्य हैं । स्वर्गलोक मे भी उनकी प्रशंसा होती है, ज्ञानी-जन भी उनकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु बुधजन कवि कहते हैं कि मुझसे तो ऐसे आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है ।
ढाल-4
(सोरठा)
ऊग्यो आतम सूर, दूर भयो मिथ्यात-तम
अब प्रगटे गुणभूर, तिनमें कछु इक कहत हूँ ॥१॥
ऊग्यो आतम सूर, दूर भयो मिथ्यात-तम
अब प्रगटे गुणभूर, तिनमें कछु इक कहत हूँ ॥१॥
अन्वयार्थ : सम्यक्त्व होते ही आत्मारूपी सूर्य उदित हो गया और मिथ्यात्व रूपी अन्धकार दूर हुआ, वहीं पर अनन्त गुणों का समूह भगवान-आत्मा भी प्रगट हो गया, उनमें से कुछ एक गुणों को यहाँ पर कहता हूँ ।
शंका मन में नाहिं, तत्वारथ सरधान में
निरवांछा चित मांहि, परमारथ में रत रहै ॥२॥
नेक न करत गिलान, बाह्य मलिन मुनि तन लखे
नाहीं होत अजान, तत्त्व कुतत्त्व विचार में ॥३॥
उर में दया विशेष, गुण प्रकटैं औगुण ढंके
शिथिल धर्म मे देख, जैसे - तैसे दृढ़ करै ॥४॥
साधर्मी पहिचान, करैं प्रीति गौ वत्स सम
महिमा होत महान्, धर्म काज ऐसे करै ॥५॥
निरवांछा चित मांहि, परमारथ में रत रहै ॥२॥
नेक न करत गिलान, बाह्य मलिन मुनि तन लखे
नाहीं होत अजान, तत्त्व कुतत्त्व विचार में ॥३॥
उर में दया विशेष, गुण प्रकटैं औगुण ढंके
शिथिल धर्म मे देख, जैसे - तैसे दृढ़ करै ॥४॥
साधर्मी पहिचान, करैं प्रीति गौ वत्स सम
महिमा होत महान्, धर्म काज ऐसे करै ॥५॥
अन्वयार्थ : ऐसे आत्मज्ञानी जीव के मन में कभी भी
- तत्त्वार्थ श्रद्धान में शंका नहीं होती, मुक्ति मार्ग साधने मे रत रहते हैं
- चित्त मे दूसरी अन्य कोई वांछा नही होती है।
- मुनिजनों के देह की मलिनता देखकर जरा भी ग्लानि नही करते हैं।
- तत्त्व और कुतत्त्व के निर्णय मे मूर्ख नही रहते हैं।
- अन्तर हृदय मे सर्व जीवों के प्रति विशेष दया रुप कोमल परिणाम रहता है, धर्मात्मा के गुणों को प्रसिद्ध करते हैं तथा अवगुणों को ढांकते हैं।
- धर्मात्मा जीवों को धर्म मे शिथिल होता जाने तो हर सम्भव उपाय के द्वारा उन्हे मोक्षमार्ग मे स्थिर करते हैं।
- साधर्मी बन्धुओं को देखकर उनके प्रति गौ-वत्स समान प्रीति करते हैं।
- ऐसे सभी धर्म कार्यों को करते हैं कि जिससे धर्म की अतिशय महिमा प्रसिद्ध हो -
मद नहिं जो नृप तात, मद नहिं भूपति माम को
मद नहिं विभव लहात, मद नहिं सुन्दर रूप को ॥६॥
मद नहिं जो विद्वान, मद नहिं तन में जोर को
मद नहिं जो परधान, मद नहिं संपति कोष को ॥७॥
हूवो आतम ज्ञान, तज रागादि विभाव पर
ताको ह्वै क्यों मान, जात्यादिक वसु अथिर को ॥८॥
मद नहिं विभव लहात, मद नहिं सुन्दर रूप को ॥६॥
मद नहिं जो विद्वान, मद नहिं तन में जोर को
मद नहिं जो परधान, मद नहिं संपति कोष को ॥७॥
हूवो आतम ज्ञान, तज रागादि विभाव पर
ताको ह्वै क्यों मान, जात्यादिक वसु अथिर को ॥८॥
अन्वयार्थ : सम्यग्दृष्टि जीव का
- पिता राजा होय तो उसका भी कुलमद नहीं होता है।
- मामा राजा होय तो उसका भी जातिमद नही होता है।
- वैभव धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होने का भी मद नही होता है।
- सुन्दर रुप लावण्य का भी मद नहीं होता है।
- ज्ञान का भी मद नही होता है।
- शरीर में विशेष ताकत बल होय उसका भी मद नही होता है।
- लोक में कोई मुखिया प्रधान पद वगैरह अधिकार का भी मद नही होता है।
- धन-सम्पति कोष का भी मद नही होता है।
बन्दत हैं अरिहंत, जिन-मुनि जिन-सिद्धान्त को
नमें न देख महन्त, कुगुरु कुदेव कुधर्म को ॥९॥
नमें न देख महन्त, कुगुरु कुदेव कुधर्म को ॥९॥
अन्वयार्थ : सम्यग्दृष्टि जीव अरिहन्त जिनदेव, जिन मुद्राघारी मुनि मौर जिन सिद्धान्त को ही वन्दन करता है, परन्तु कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को चाहे वे लोक मे कितने ही महान दिखाई देते हो तो भी उन्हें वन्दन नहीं करता है - इस प्रकार ज्ञानी जीव को तीन मूढताओं का अभाव होता ही है ।
कुत्सित आगम देव, कुत्सित गुरु पुनि सेवकी
परशंसा षट भेव, करै न सम्यकवान हैं ॥१०॥
परशंसा षट भेव, करै न सम्यकवान हैं ॥१०॥
अन्वयार्थ : सम्यग्दृष्टि जीव कुगरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक तथा कुधर्म सेवक - यह छह अनायतन दोष कहलाते हैं, उनकी भक्ति-विनय और पूजनादि तो दूर रही, किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नही करता, क्योकि उनकी प्रशंसा करने से भी सम्यक्त्व मे दोष लगता है । इस प्रकार शंकादि आठ दोष, आठ मद, तीन मूढता और छह अनायतन - ये पच्चीस दोष जिसमे नहीं पाये जाते, वह जीव सम्यग्दृष्टि है ।
प्रगटो ऐसो भाव, कियो अभाव मिथ्यात्व को
बन्दत ताके पाँय, 'बुधजन' मन-वच-कायतैं ॥११॥
बन्दत ताके पाँय, 'बुधजन' मन-वच-कायतैं ॥११॥
अन्वयार्थ : जिस जीव ने ऐसा निर्मल भाव प्रगटाया है और मिथ्यात्व का अभाव किया है, उस ज्ञानी के चरणों की मैं (बुधजन) मन-वचन-काया से वन्दना करता हूँ ।
ढाल-5
(चाल छंद)
तिर्यंच मनुज दोउ गति में, व्रत धारक श्रद्धा चित में
सो अगलित नीर न पीवै, निशि भोजन तजत सदीवै ॥१॥
तिर्यंच मनुज दोउ गति में, व्रत धारक श्रद्धा चित में
सो अगलित नीर न पीवै, निशि भोजन तजत सदीवै ॥१॥
अन्वयार्थ : सम्यग्दर्शन सहित व्रत धारण करने वाले संयमी-जीव तिर्यंच और मनुष्य इन दो गति मे ही होते हैं। वे अणुव्रत धारी श्रावक बिना छना हुआ पानी नहीं पीते और रात्रि-भोजन भी सदा के लिये छोड देते हैं ।
मुख वस्तु अभक्ष न लावै, जिन भक्ति त्रिकाल रचावै
मन वच तन कपट निवारै, कृत कारित मोद संवारै ॥२॥
मन वच तन कपट निवारै, कृत कारित मोद संवारै ॥२॥
अन्वयार्थ : मुख मे कभी भी अभक्ष वस्तु नही लाते, सदैव जिनेन्द्र देव की भक्ति में अपने को लीन रखते है, मन-वचन-काया से मायाचारी छोड़ देते है और पाप-कार्यों को न स्वयं करता है, न कराता और न उनकी अनुमोदना करता है ।
जैसी उपशमत कषाया, तैसा तिन त्याग कराया
कोई सात व्यसन को त्यागै, कोई अणुव्रत में मन पागै ॥३॥
कोई सात व्यसन को त्यागै, कोई अणुव्रत में मन पागै ॥३॥
अन्वयार्थ : उस आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि को जितनी-जितनी कषायें उपशमती जाती हैं, उतने-उतने प्रमाण मे उसको हिंसादि पापों का त्याग होता जाता है । कोई-कोई तो सात व्यसन का सर्वथा त्याग कर देते हैं और कोई-कोई अणुव्रत धारण करके शुभाशुभ भावों से रहित तप मे लग जाते हैं ।
त्रस जीव कभी नहिं मारै, विरथा थावर न संहारै
परहित बिन झूठ न बोले, मुख सांच बिना नहिं खोले ॥४॥
परहित बिन झूठ न बोले, मुख सांच बिना नहिं खोले ॥४॥
अन्वयार्थ : ऐसे श्रावक त्रस जीवों को कभी नही मारते और स्थावर जीवों का भी निष्प्रयोजन कभी भी संहार नहीं करते । पर-हित सिवाय कभी झूठ नहीं बोलते (अर्थात कदाचित् किसी धर्मात्मा से कोई दोष हो गया होय उसे बचाने के लिए अथवा कोई निरपराधी फंस रहा होय उसे निकालने के लिये इन प्रसंगों के सिवाय वह कभी झूठ नहीं बोलते) और सत्य सिवाय कभी भी मुख नहीं खोलते ।
जल मृतिका बिन धन सबहू, बिन दिये न लेवे कबहू
ब्याही वनिता बिन नारी, लघु बहिन बड़ी महतारी ॥५॥
ब्याही वनिता बिन नारी, लघु बहिन बड़ी महतारी ॥५॥
अन्वयार्थ : जिनकी मनाई नही - ऐसा पानी व मिट्टी के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु जो उसे दी नहीं गई हो कभी भी लेता नहीं है। अपनी विवाहिता नारी के अलावा अन्य दूसरी लधुवय स्त्रियों को बहिन समान एवं अपने से बडी स्त्रियों को माता समान समझता है ।
तृष्णा का जोर संकोचै, ज्यादा परिग्रह को मोचै
दिश की मर्यादा लावै, बाहर नहि पाँव हिलावै ॥६॥
दिश की मर्यादा लावै, बाहर नहि पाँव हिलावै ॥६॥
अन्वयार्थ : वह श्रावक विषय-पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाली जो तष्णा, उसके जोर को संकोचता है, ममता को घटाकर अधिक-परिग्रह को छोड देता है, परिग्रह का प्रमाण कर लेता है । दिशाओं में गमन करने की अथवा किसी को बुलाने, लेन-देन आदि करने की मर्यादा कर लेता है और मर्यादा से बाहर पग भी नहीं निकालता है ।
ताहू में गिरि पुर सरिता, नित राखत अघ तें डरता
सब अनरथ दंड न करता, छिन-छिन निज धर्म सुमरता ॥७॥
सब अनरथ दंड न करता, छिन-छिन निज धर्म सुमरता ॥७॥
अन्वयार्थ : पाप से डरने वाला श्रावक दिग्व्रत मे निश्चित की हुई मर्यादा में भी पर्वत, नगर, नदी आदि तक गमनादि-व्यापारादि करने की मर्यादा कर लेता है तथा किसी भी प्रकार का अनर्थ दंड (खोटा पाप निष्प्रयोजन हिंसादि) नहीं करता एवं प्रतिक्षण जिन-धर्म का स्मरण करता रहता है ।
द्रव्य क्षेत्र काल सुध भावै, समता सामायिक ध्यावै
सो वह एकाकी हो है, निष्किंचन मुनि ज्यों सोहै ॥८॥
सो वह एकाकी हो है, निष्किंचन मुनि ज्यों सोहै ॥८॥
अन्वयार्थ : वह श्रावक द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव की शुद्धि-पूर्वक समतारुप सामायिक को ध्याता है । अष्टमी, चतुर्दशी प्रोषध उपवास के दिन एकान्त मे रहता है और निष्परिग्रही मुनि समान शोभता है ।
परिग्रह परिमाण विचारै, नित नेम भोग को धारै
मुनि आवन बेला जावै, तब जोग अशन मुख लावै ॥९॥
मुनि आवन बेला जावै, तब जोग अशन मुख लावै ॥९॥
अन्वयार्थ : वह श्रावक परिग्रह की मर्यादा का विचार करता है और भोग-उपभोग की मर्यादा का भी हमेशा नियम करता है । मुनिवरों को प्रतिदिन आहार-दान देने की भावना भाता है और जब मुनिवरों के आहार का समय बीत जावे तब ही स्वयं योग्य शुद्ध भोजन करता है ।
यों उत्तम किरिया करता, नित रहत पाप से डरता
जब निकट मृत्यु निज जाने, तब ही सब ममता भाने ॥१०॥
जब निकट मृत्यु निज जाने, तब ही सब ममता भाने ॥१०॥
अन्वयार्थ : इस प्रकार धर्मी श्रावक सदा ही उत्तम कार्य करता है और पाप से सदा ही डरता रहता है । तथा जब मरण का काल समीप आया जानता है, तब तत्काल समस्त परिग्रह की ममता को छोड देता है ।
ऐसे पुरुषोत्तम केरा, 'बुधजन' चरणों का चेरा
वे निश्चय सुरपद पावैं, थोरे दिन में शिव जावैं ॥११॥
वे निश्चय सुरपद पावैं, थोरे दिन में शिव जावैं ॥११॥
अन्वयार्थ : बुधजन कहते हैं कि हम तो ऐसे उत्तम पुरुषों के चरणों के दास हैं । वे धर्मात्मा श्रावक तो नियम से देव होकर अल्पकाल मे ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं ।
ढाल-6
(षटपद छंद)
अथिर ध्याय पर्याय, भोग ते होय उदासी
नित्य निरंजन जोति, आत्मा घट में भासी ॥
सुत दारादि बुलाय, सबनितैं मोह निवारा
त्यागि शहर धन धाम, वास वन-बीच विचारा ॥१॥
अथिर ध्याय पर्याय, भोग ते होय उदासी
नित्य निरंजन जोति, आत्मा घट में भासी ॥
सुत दारादि बुलाय, सबनितैं मोह निवारा
त्यागि शहर धन धाम, वास वन-बीच विचारा ॥१॥
अन्वयार्थ : सम्यग्दृष्टि जीव को नित्य निरन्जन चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अन्तरंग मे प्रगट भाषित हुआ है, वह देह (पर्याय) को अस्थिर नाशवान समझकर संसार-शरीर भोगों से उदासीन हो जाता है । वह स्त्री-पुत्रादि को धर्म सम्बोधन करके समस्त चेतन अचेतन परिग्रह के प्रति मोह ममत्व छोड देता है और नगर-धन-मकानादि सब परिग्रह छोडकर वन के बीच एकान्त निर्जन वन मे वास करने का विचार दृढ कर लेता है ।
भूषण वसन उतार, नगन ह्वै आतम चीना
गुरु ढिंग दीक्षा धार, सीस कचलोच जु कीना ॥
त्रस थावर का घात, त्याग मन-वच-तन लीना
झूठ वचन परिहार, गहैं नहिं जल बिन दीना ॥२॥
गुरु ढिंग दीक्षा धार, सीस कचलोच जु कीना ॥
त्रस थावर का घात, त्याग मन-वच-तन लीना
झूठ वचन परिहार, गहैं नहिं जल बिन दीना ॥२॥
अन्वयार्थ : पश्चात वह विरागी श्रावक श्री निर्ग्रन्थ गुरु के पास जाकर समस्त आभूषण एवं वस्त्र उतारकर नग्न दिगम्बर वेष धारण कर दीक्षा लेकर केशलोच करके आत्म-ध्यान मे मग्न हो जाता है । समस्त त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा का मन-वच-काया से त्याग कर देता है, मिथ्या वचनादि बोलने का भी त्यागकर देता है तथा बिना दिया हुआ पानी भी नही लेता है ।
चेतन जड़ तिय भोग, तजो भव-भव दुखकारा
अहि-कंचुकि ज्यों जान, चित तें परिग्रह डारा ॥
गुप्ति पालने काज, कपट मन-वच-तन नाहीं
पांचों समिति संवार, परिषह सहि है आहीं ॥३॥
अहि-कंचुकि ज्यों जान, चित तें परिग्रह डारा ॥
गुप्ति पालने काज, कपट मन-वच-तन नाहीं
पांचों समिति संवार, परिषह सहि है आहीं ॥३॥
अन्वयार्थ : तथा सर्वप्रकार की चेतन व अचेतन स्त्रियों के उपभोग को भव-भव मे दुखकारी जानकर छोड़ दिया है । तथा चित्त मे निर्ममत्व होकर सर्प की कांचली के समान सर्वप्रकार के परिग्रह को भी भिन्न जानकर छोड दिया है । त्रिगुप्ति के पालने के लिए मन-वचन-काया से कपट भाव छोड दिया है । ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन -- इन पांच समिति के पालने मे सावधान हो वर्तन करते हैं और बाईस प्रकार के परिषह को सहन करने लगे ।
छोड़ सकल जंजाल, आप कर आप आप में
अपने हित को आप, करो ह्वै शुद्ध जाप में ॥
ऐसी निश्चल काय, ध्यान में मुनि जन केरी
मानो पत्थर रची, किधों चित्राम उकेरी ॥४॥
अपने हित को आप, करो ह्वै शुद्ध जाप में ॥
ऐसी निश्चल काय, ध्यान में मुनि जन केरी
मानो पत्थर रची, किधों चित्राम उकेरी ॥४॥
अन्वयार्थ : और कैसे हैं वे मुनिराज ? सकल जगजाल को छोडकर उन्होने अपने द्वारा अपने को अपने मे ही एकाग्र किया है । अपने स्वयं हित के लिए अपने स्वयं का ध्यान स्वयं ने शुद्ध किया है अर्थात् शुद्धात्मा का ध्यान करके निज स्वरूप मे ही लीन हुए हैं । अहा ! शुद्धोपयोग ध्यान में लीन मुनिराज का शरीर भी ऐसा स्थिर हुआ है कि मानो पत्थर की मूर्ति अथवा चित्र ही हो । इस प्रकार अडौलपने द्वारा आत्म-ध्यान मे एकाग्र हैं ।
चार घातिया नाश, ज्ञान मे लोक निहारा
दे जिनमत उपदेश, भव्य को दुख तें टारा ॥
बहुरि अघाती तोरि, समय में शिव-पद पाया
अलख अखंडित जोति, शुद्ध चेतन ठहराया ॥५॥
दे जिनमत उपदेश, भव्य को दुख तें टारा ॥
बहुरि अघाती तोरि, समय में शिव-पद पाया
अलख अखंडित जोति, शुद्ध चेतन ठहराया ॥५॥
अन्वयार्थ : इस प्रकार शुद्धात्म ध्यान द्वारा चार घाति कर्मों का घात करके केवलज्ञान मे लोकालोक को जान लिया और केवलज्ञान के अनुसार उपदेश देकर भव्य जीवों को दुख से छुडाया अर्थात् मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया । पश्चात चार अघाति कर्मों का भी नाश करके एक समय मात्र मे सिद्धपद प्राप्त किया तथा इन्द्रिय ज्ञान से जो जानने मे नहीं आता ऐसा अलख अतीन्द्रिय अखंड आत्म-ज्योति शुद्ध-चेतना रूप होकर स्थिर हो गई ।
काल अनंतानंत, जैसे के तैसे रहिहैं
अविनाशी अविकार, अचल अनुपम सुख लहिहैं ॥
ऐसी भावन भाय, ऐसे जे कारज करिहैं
ते ऐसे ही होय, दुष्ट करमन को हरिहैं ॥६॥
अविनाशी अविकार, अचल अनुपम सुख लहिहैं ॥
ऐसी भावन भाय, ऐसे जे कारज करिहैं
ते ऐसे ही होय, दुष्ट करमन को हरिहैं ॥६॥
अन्वयार्थ : ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त करके वह जीव अनन्तानन्त काल पर्यन्त ऐसे के ऐसे रहता है तथा अविनाशी, अविकार, अचल, अनुपम सुख का निरन्तर अनुभव किया करता है। जो कोई भव्यजीव ऐसी आत्म-भावना भाकर श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र का कार्य करते हैं, वे भी इस अनुपम अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त करते है और दुष्ट कर्मों को नाश कर देते हैं ।
जिनके उर विश्वास, वचन जिन-शासन नाहीं
ते भोगातुर होय, सहैं दुख नरकन माही ॥
सुख दुख पूर्व विपाक, अरे मत कल्पै जीया
कठिन कठिन ते मित्र, जन्म मानुष का लीया ॥७॥
ते भोगातुर होय, सहैं दुख नरकन माही ॥
सुख दुख पूर्व विपाक, अरे मत कल्पै जीया
कठिन कठिन ते मित्र, जन्म मानुष का लीया ॥७॥
अन्वयार्थ : जिन के मन मे जिनशासन के वचनों का (सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का) विश्वास नहीं है, वह जीव विषय-भोगों मे मग्न पश्चात नरकों मे दुख भोगते हैं । संसार में सुख-दुख तो पूर्व कर्मों के उदय अनुसार होता है । अत: हे जीव ! इससे तू डर मत (अन्यथा कल्पना मत कर) उदय में जो कर्म आया हो उसे सहन कर । हे मित्र ! बहुत ही अधिक कठिनता से यह मनुष्य जन्म तुझे मिला है ।
सो बिरथा मत खोय, जोय आपा पर भाई
गई न लावैं फेरि, उदधि में डूबी राई ॥
भला नरक का वास, सहित समकित जो पाता
बुरे बने जे देव, नृपति मिथ्यामत माता ॥८॥
गई न लावैं फेरि, उदधि में डूबी राई ॥
भला नरक का वास, सहित समकित जो पाता
बुरे बने जे देव, नृपति मिथ्यामत माता ॥८॥
अन्वयार्थ : इसलिये इसे तू व्यर्थ यों ही विषयों में मत गवां । हे भाई ! इस नर-भव में तू स्व-पर के विवेकरुप भेद-विज्ञान प्रगट कर, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र मे डूबा हुआ राई का दाना पुन मिलना अत्यन्त कठिन है, उसीप्रकार इस दुर्लभ मनुष्य-जन्म बीत जाने के बाद पुन: प्राप्त करना कठिन है । सम्यक्त्व की प्राप्ति सहित तो नरकवास भी भला है परन्तु सम्यक्त्व रहित मिथ्यात्व भाव से भरा हुआ जीव देव अथवा राजा भी हो जाय तो भी वह बुरा ही है ।
नहीं खरच धन होय, नहीं काहू से लरना
नहीं दीनता होय, नहीं घर का परिहरना ॥
समकित सहज स्वभाव, आप का अनुभव करना
या बिन जप तप वृथा, कष्ट के माहीं परना ॥९॥
नहीं दीनता होय, नहीं घर का परिहरना ॥
समकित सहज स्वभाव, आप का अनुभव करना
या बिन जप तप वृथा, कष्ट के माहीं परना ॥९॥
अन्वयार्थ : सम्यक्त्व वह तो आत्मा का सहज स्वभाव है, उसमें न तो कुछ धन खर्च होता है और न ही किसी से लडना पड़ता है । न तो किसी के पास दीनता करनी पड़ती है और न ही घरबार छोडना पडता है । अपना एक रूप त्रिकाली सहज स्वभाव - ऐसे आत्मा का अनुभव करना वही सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व के बिना जप-तप आदि व्यवहार क्रियारुप आचरण निरर्थक है, कष्ट मे पडना है ।
कोटि बात की बात अरे, 'बुधजन' उर धरना
मन-वच-तन सुधि होय, गहो जिन-मत का शरना ॥
ठारा सौ पच्चास, अधिक नव संवत जानों
तीज शुक्ल वैशाख, ढाल षट शुभ उपजानों ॥१०॥
मन-वच-तन सुधि होय, गहो जिन-मत का शरना ॥
ठारा सौ पच्चास, अधिक नव संवत जानों
तीज शुक्ल वैशाख, ढाल षट शुभ उपजानों ॥१०॥
अन्वयार्थ : ग्रन्थ की पूर्णता करते हुए पण्डित बुधजन अन्तिम पद मे कहते हैं कि अरे भव्य आत्माओं - बुधजनों ! करोडों बात की सार रुप यह बात तुम अन्तरंग मे धारण करो, मन-वचन-काया की पवित्रता पूर्वक जिन-धर्म की शरण ग्रहण करो । 'ढाल' - इस नाम की शुभ उपमा वाला यह छह पदों की रचना 'छहढाला' सम्वत 1856 की बैशाख शुदि तीज को समाप्त हुई ।