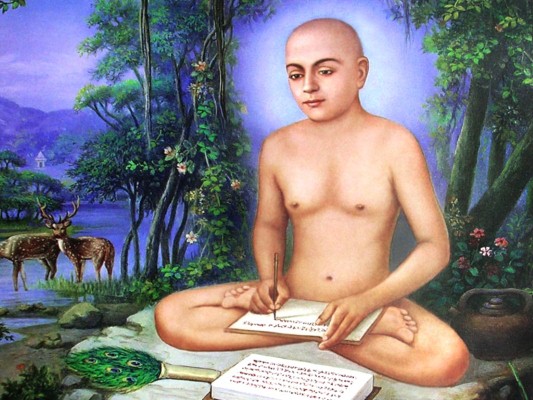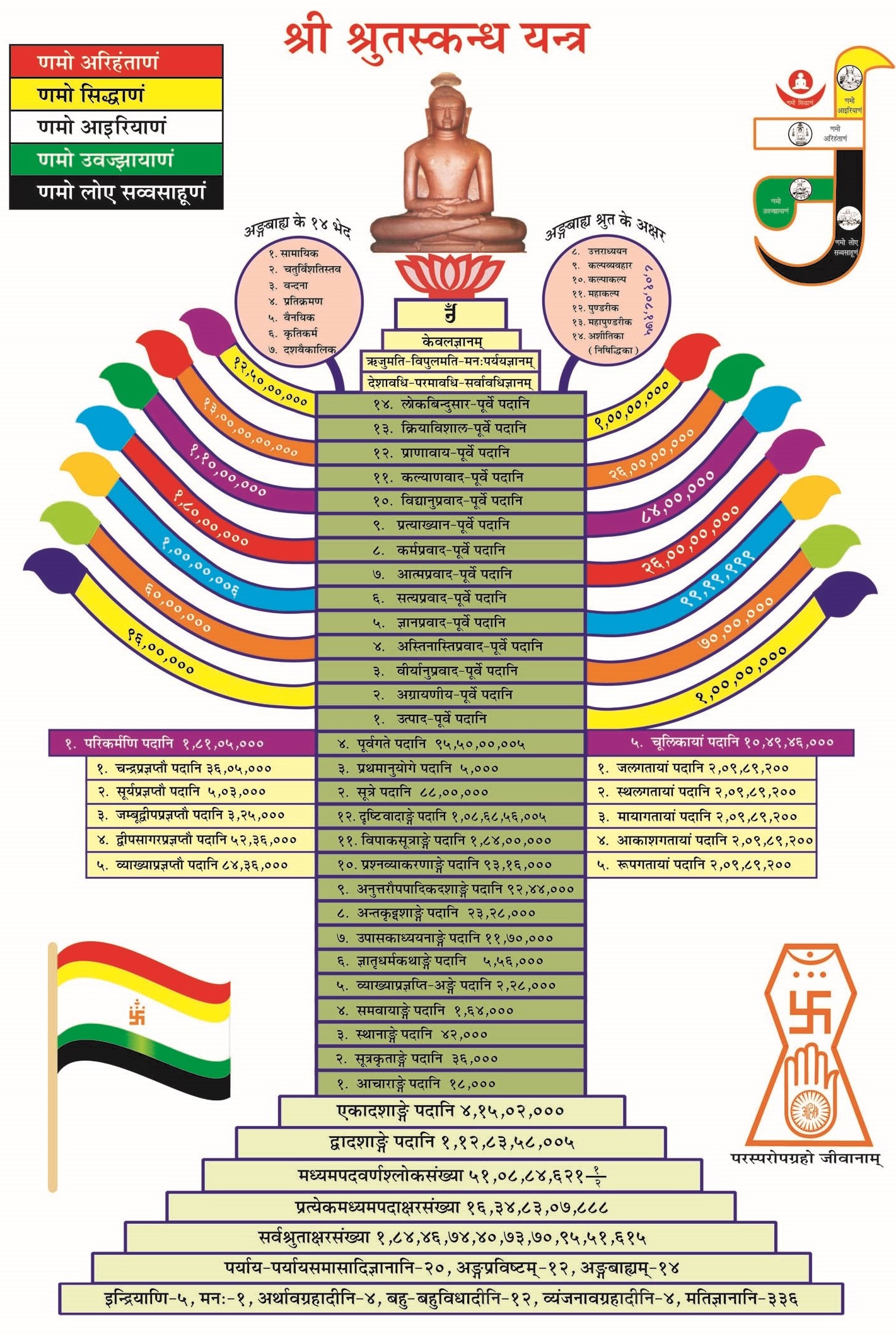nikkyjain@gmail.com
Date : 17-Nov-2022
Index

| गाथा / सूत्र | विषय |
|---|
| 001) | श्री अकलंक-देव कृत मंगलाचरण |
| 002) | शंकाकार कहता है कि सर्वथैकांतवादी भी सुगत आदि को धर्म का तीर्थंकर मानना अविरुद्ध ही है क्योंकि बाधक प्रमाण का अभाव है । उनके तीर्थ में भी तो प्रमाण आदि के लक्षण का प्रतिपादन संभव है । ऐसे पक्ष का निराकरण करते हुए स्याद्वादमार्ग की निष्कंटक शुद्धि के लिए आचार्य कहते हैं |
| 003) | इस प्रकार से कण्टक शुद्धि को करके संबंध अभिधेय, अनुष्ठान और इष्टप्रयोजन के निर्देशपूर्वक प्रमाण के लक्षण और भेदों को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं |
| 004) | आपने ‘प्रत्यक्ष का लक्षण विशद है’ ऐसा कहा है, वह ज्ञान की विशदता कैसी है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं |
| 005) | अब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण और भेद का निर्णय करने के लिए आचार्य कहते हैं - |
| 006) | अब ज्ञान के भेद और प्रमाण तथा फल के व्यवहार को बतलाते हैं - |
| 007) | अब प्रमाण के विषय के विसंवाद को दूर करने के लिए आगे कहते हैं - |
| 008) | एकांत में अर्थक्रिया का विरोध ही है, इसी बात को और स्पष्ट करते हैं - |
| 009) | एक में अनेकाकार को व्याप्त करके रहना और अनेक अर्थक्रिया को करना कैसे है ? अथवा अनेकत्व में एकत्व कैसे होगा ? क्योंकि विरोध आता है। इस प्रकार की आशंका को निवारण करते हुए श्री भट्टाकलंक देव अनेकांत में विरोध के स्वभाव को दिखलाते हैं - |
| 010) | वस्तु के इसी अनेकांत स्वरूप का सौगत के द्वारा मान्य चित्रज्ञान के दृष्टांत के बल से समर्थन करते हैं |
| 011) | अब इस समय परोक्ष प्रमाण के कारण और भेद को कहते हैं। |
| 012) | अविनाभाव का प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निर्णय हो जाता है। पुन: तर्क नाम के एक भिन्न प्रमाण को क्यों आपने कल्पित किया है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं - |
| 013) | पुन: अनुमान प्रमाण क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर इस सूत्र को कहते हैं - |
| 014) | तादात्म्य और तदुत्पत्ति से अविनाभाव होता है इसलिए व्यापक का व्याप्य ही लिंग है और कारण का कार्य ही लिंग है। इस प्रकार विधि हेतु दो प्रकार के ही हैं। इस तरह सौगत के विसंवाद का निराकरण करते हुए कारण को भी लिंगत्व हेतुपना सिद्ध करते हैं |
| 015) | अब पूर्वचर को भी हेतुपना सिद्ध करते हुए कहते हैं |
| 016) | अब दृश्यानुपलब्धि ही निषेध साधन है, अदृश्यानुपलब्धि नहीं है, इस एकांत का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 017) | स्याद्वादियों के यहाँ भी अनेकांतात्मक तत्त्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने से अनुमान प्रमाण की विफलता का प्रसंग आ जाता है, इस प्रकार की आशंका होने पर आचार्य अगली कारिका को कहते हैं |
| 018) | बौद्ध के मत में ‘अनुपलब्धि हेतु मत सिद्ध होवे किन्तु कार्य हेतु और स्वभाव हेतु ये दो हेतु होवेंगे परन्तु वे दोनों हेतु भी नहीं घटते हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं |
| 019) | और दूसरी बात यह है कि अनुमान विकल्पात्मक है वह सौगत के मत में सिद्ध ही नहीं हो सकता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं |
| 020) | आप जैन के यहाँ भी प्रमाण के दो विध का नियम नहीं टिकता है क्योंकि आपने उपमान नाम के एक भिन्न प्रमाण को संगृहीत नहीं किया है। इस प्रकार से कहने वाले नैयायिक आदि की व्यवस्था को आड़े हाथ लेते हुए उनके मत में भी संख्या के नियम को विघटित करते हैं |
| 021) | इसी उपर्युक्त कथन का ही समर्थन करते हैं |
| 022) | न केवल ये ही प्रमाणांतर है अपितु अन्य भी हैं, ऐसा दिखलाते हैं |
| 023) | इस प्रकार सम्यग्ज्ञान लक्षण प्रमाण, प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद, द्रव्य पर्यायात्मक अर्थ विषय और अज्ञाननिव्रत्ति आदि फल, इन चारों को प्रतिपादित करके इस समय प्रमाणाभास का निरूपण करते हुए कहते हैं - |
| 024) | इस समय जो सौगतों ने विकल्पज्ञान को प्रत्यक्षाभास कल्पित किया है, उसका निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 025) | स्वसंवेदन आदि प्रत्यक्ष ज्ञान में विकल्प नहीं हैं क्योंकि वे दिखते नहीं हैं, इस पक्ष का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 026) | इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं - |
| 027) | अब इस समय श्रुतज्ञान में प्रमाण आरै प्रमाणाभास की व्यवस्था को प्रतिपादित करते हैं - |
| 028) | श्रुत को सर्वत्र अप्रमाण की आशंका करने पर अतिप्रसंग दोष को दिखलाते हैं |
| 029) | सर्वत्र श्रुत में अविश्वास होने पर और भी अनिष्ट को बताते हैं |
| 030) | सुगत के वचन को भी अप्रमाणता हो जावे क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाणता है क्योंकि पुरुषों के विचित्र अभिप्राय होने से अर्थ में व्यभिचार आता है, इस प्रकार की दाशबल की शंका का निरसन करते हैं |
| 031) | अब इस समय प्रमाण और प्रमाणाभास की परीक्षा करके नय और नयाभास के लक्षण की परीक्षा के लिए कहते हैं |
| 032) | देश, काल और आकार के भेद से अत्यंत भिन्न ही भाव परमार्थसत् हैं किन्तु सत् सामान्य नहीं हैं। इस प्रकार की बौद्ध की मान्यता का निराकरण करते हुए कहते हैं- |
| 033) | उस सत्सामान्य के नय का निरूपण करते हैं |
| 034) | प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध है पुन: अभेद नयरूप संग्रह मिथ्या है क्योंकि प्रत्यक्ष से बाधित है। इस प्रकार की सौगत की विचारधारा का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 035) | इस प्रकार सत्सामान्य लक्षण शुद्ध द्रव्य का समर्थन करके अब ऊध्र्वता सामान्य लक्षण अशुद्ध द्रव्य का समर्थन करते हैं |
| 036) | कार्य कारण का भिन्न काल होने से क्षणिक में ही अर्थक्रिया संभव है नित्य में नहीं, इस प्रकार के बौद्ध के वाक्यों को शोधन करते हुए कहते हैं |
| 037) | एक ही अनेक कार्य को करने वाला और धर्मों में व्याप्त होकर रहने वाला कैसे हो सकता है क्योंकि परस्पर में विरोध है ? इस आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 038) | इस प्रकार सत्सामान्य रूप पर द्रव्य को और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य से युक्त अपर द्रव्य को प्रतिपादित करके उसमें पर द्रव्य को विषय करने वाले परसंग्रह को और तदाभास को दिखलाते हुए कहते हैं |
| 039) | अब इस समय नैगमनय और तदाभास का निरूपण करते हैं |
| 040) | गुण-गुणी आदि में समवाय संबंध है ही है इस प्रकार के यौगमत का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 041) | ब्रह्मवाद और भेदवाद में भी प्रमाण आदि व्यवहार संभव हैं अत: वे संग्रहावास और नैगमाभास कैसे हैं ? इस प्रकार के आक्षेप को समाप्त करते हुए कहते हैं |
| 042) | अब उनके सुनयत्व को प्रतिपादित करते हैं |
| 043) | अब ऋजुसूत्र नय का निरूपण करते हैं |
| 044) | अब शब्द, समभिरूढ़ और इत्यंभूत इन तीनों नयों का भी निरूपण करते हैं |
| 045) | शब्द और अर्थ में संकेत ग्रहण का अभाव होने से शब्द के भेद से अर्थ में भेद कैसे हो सकता है ? प्रत्यक्ष से संकेत का ग्रहण होने पर भी वह व्यवहार में उपयोगी नहीं है क्योंकि गृहीत और संकेत उसी समय नष्ट हो जाते हैं। स्मृति भी संकेत को विषय नहीं करती है क्योंकि वे दोनों अतीत हो चुके हैं। इस प्रकार सौगत की आशंका का निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं |
| 046) | शब्द और अर्थ में संबंध का अभाव होने से शब्द की प्रमाणता कैसे होगी ? कि जिससे उसके विषय में शब्दादिक नय समीचीन होवें ? ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए आचार्य कहते है |
| 047) | काल, कारक और लिंग के भेद से शब्द अर्थ में भेद करने वाला है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसको ग्रहण करने वाले प्रमाण का अभाव है। ऐसी आशंका का निरसन करते हुए आचार्य कहते हैं |
| 048) | एकांत में भी एक में षट्कारक की व्यवस्था का होना कैसे घट सकता है ? ऐसी आशंका के होने पर आचार्य कहते हैं |
| 049) | नय विकल्पात्मक है इसलिए वे तत्त्वों के ज्ञान की सिद्धि नहीं करा सकते हैं। जैसेस्मृति आदि तत्त्वों के ज्ञान को कराने में असमर्थ हैं, इस प्रकार की सौगत की आशंका का निरसन करते हुए प्रकरण के उपसंहार को कहते हैं |
| 050) | सौगत आदि के मत में भी तत्त्वों का ज्ञान होता है, इस प्रकार की आशंका के होने पर कहते हैं |
| 051) | अब इस समय आगम के स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रवचन प्रवेश की आदि में और ग्रंथ के मध्य में मंगलभूत इष्ट देवता के गुणों की स्तुति करते हैं |
| 052) | अब कहे गये प्रमाण आदि का लक्षण कहते हैं - |
| 053) | ‘विषय अकारण नहीं होता है’ इस बौद्धमत का निराकरण करने के लिए अर्थ को कारण मानने का खंडन करते हैं |
| 054) | अनुमान से ज्ञान की उत्पत्ति की सिद्धि हो जावेगी, ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं - |
| 055) | अज्ञानरूप भी सन्निकर्ष प्रमाण है इस आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 056) | अब आलोक को ज्ञान के कारणपने का निराकरण करते हुए कहते हैं |
| 057) | अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति न मानने पर संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने का प्रसंग हो जावेगा क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं |
| 058) | ज्ञान जिस अर्थ से उत्पन्न होता है, जिस आकार का अनुकरण करता है और जिसके विषय में निश्चय को उत्पन्न करता है, उसी विषय में उस ज्ञान की प्रमाणता है किन्तु सर्वत्र नहीं है, ऐसी सौगत की आशंका का आचार्य खंडन करते हैं |
| 059) | इसलिए अपने कारण समूहों से उत्पन्न होता हुआ प्रकाशरूप ज्ञान स्वत: ही अर्थ को ग्रहण करने वाला है, अब आचार्य इस बात को कहते है - |
| 060) | ‘ज्ञानं प्रमाणं आत्मादे:’- अब ज्ञान प्रमाण है वह आत्मा आदि को विषय करता है, इसी ही अर्थ को और स्पष्ट करते हैं |
| 061) | इस समय उस प्रमाण की संख्या को कहते हैं |
| 062) | अब श्रुत के व्यापार भेद को दिखाते हैं |
| 063) | ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:’ इत्यादि वाक्यों में, शास्त्र में अथवा लोक में स्यात्कार का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है कि जिससे सर्वत्र वाक्य का अर्थ अनेकांत होवे ? इस प्रकार का आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं |
| 064) | वर्ण, पद और वाक्यात्मक शब्द विवक्षा के विषय हैं, पुन: स्यात्कार अर्थापत्ति से कैसे प्रतीति का विषय होगा ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं |
| 065) | अब नय के भेदों को कहते हैं |
| 066) | अब पहले कहे गये भी नैगम आदि नयों को मंदमति वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए पुन: कहने की इच्छा रखते हुए पहले नैगम और नैगमाभास का निरूपण करते हैं |
| 067) | अब संग्रहनय और संग्रहाभास को कहते हैं |
| 068) | अब व्यवहारनय का निरूपण करते हैं - |
| 069) | अब ऋजुसूत्रनय और तदाभास का प्ररूपण करते हैं |
| 070) | अब उक्त नयों के विशेषण और विशेष नय स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं |
| 071) | अब निक्षेप के स्वरूप को निरूपण करते हुए शाध्Eा अध्ययन के फल का निर्देश करते हैं |
| 072) | अब पुन: शास्त्र के अध्ययन के फल को दिखलाते हैं - |
| 073) | अब पुन: परार्थ संपत्ति का निर्देश करते हैं |
| 074) | श्री अभयचंद्रसूरि के उद्गार |

!! श्रीसर्वज्ञवीतरागाय नम: !!
स्वामी-श्री-अकलंकाचार्य-देव-विरचित
श्री
लघीयस्त्रय
मूल संस्कृत गाथा, अभयचन्द्र-सूरि कृत टीका सहित
🏠
!! नम: श्रीसर्वज्ञवीतरागाय !!ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नम: ॥1॥
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलंका
मुनिभिरूपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् ॥2॥
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥3॥
॥ श्रीपरमगुरुवे नम:, परम्पराचार्यगुरुवे नम: ॥सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमन: प्रतिबिधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीलघीयस्त्रय नामधेयं, अस्य मूलाग्रन्थकर्तार: श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार: श्रीगणधरदेवा: प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीअकलंकाचार्यदेव विरचितं, श्रोतार: सावधानतया शृणवन्तु ॥
मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥
🏠
धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नम:
वृषभादिमहावीरान्तेभ्य: स्वात्मोपलब्धये ॥1॥
अन्वयार्थ : [धर्मतीर्थकरेभ्य:] धर्मतीर्थ के करने वाले [स्याद्वादिभ्य:] स्याद्वादी, [वृषभादि महावीरांतेभ्य:] वृषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत तीर्थंकरों को [स्वात्मोपलब्धये] अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए [नमो नमोऽस्तु] मेरा पुन:-पुन: नमस्कार होवे ॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
अवयव अर्थ के ज्ञानपूर्वक समुदाय के अर्थ का ज्ञान होता है । इस न्याय से इस आदि श्लोक का सबसे प्रथम अवयव अर्थ कहते हैं। वृषभदेव को आदि लेकर वर्धमान पर्यंत सभी तीर्थंकरों को पुन:-पुन: अथवा अतिशयरूप से नमस्कार होवे । यहाँ 'नम:' शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति है । यहाँ नमस्कार के करने में आस्तिक्य भावना व्यक्त की गई है और 'नमो नम:' ऐसा दो बार कहने से नमस्कार में अतिशय रुचि दिखाई गई है ।
यहाँ कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करना ही परम मंगल है । मलं-पाप को जो गालन करे-ध्वंस करे अथवा जो मंगं-पुण्य को लाता है-देता है वह मंगल है ऐसा निरुक्ति अर्थ है ।
शंका – जिनेन्द्र नमस्कार के समान श्रुत आदि का नमस्कार भी मंगलरूप है पुन: ग्रंथकार ने उन्हें भी नमस्कार क्यों नहीं किया ?
समाधान – नहीं, ऐसी बात नहीं है । इस श्लोक में 'धर्मतीर्थकर' ऐसा जो पद है, उससे उनको भी नमस्कार हो जाता है । धर्म ही 'तीर्थ' है, अथवा धर्म के प्रतिपादक को 'तीर्थ' कहते हैं अथवा धर्म के लिए जो प्रवर्तन है वह तीर्थ है । इस लक्षण से धर्म-तीर्थ से प्रवचन-परमागम भी कहे जाते हैं । जो इस धर्म-तीर्थ को करते हैं - अपनी वाणी द्वारा प्रतिपादन करते हैं, वे धर्म-तीर्थकर कहलाते हैं ।
प्रश्न – यह धर्म क्या है ?
उत्तर – उत्तम क्षमा आदि दशलक्षण वाला धर्म है । जीवादि वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है । जीव को सुख देने वाला धर्म है और शुभ धर्मरूप पुद्गल का जो परिणाम है वह धर्म है। यह धर्म ही तीर्थ है क्योंकि संसार से पार करने में कारण है । धर्म और तीर्थ का उत्तम क्षमादि के साथ सामानाधिकरण अविरुद्ध है । तस्य तीर्थं उस का तीर्थ (धर्म के प्रतिपादक तीर्थ) ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जीवादि तत्त्वों का प्रतिपादन करने वाला होने से प्रवचन भी तीर्थ है । तस्मै तीर्थं उसके लिए जो है वह तीर्थ है (धर्म के लिए जो प्रवर्तन है वह तीर्थ है) यह अर्थ भी हमें इष्ट ही है क्योंकि परमागम नवीन पुण्य के आस्रव को कराने वाला है । इसलिए परमागम को तीर्थ माना है । इसलिए यह बात ठीक ही है कि 'वृषभादि महावीर पर्यंत तीर्थंकर अर्हंत भगवान ही स्वहित इच्छुकों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, क्योंकि वे धर्मतीर्थ के करने वाले हैं। जो अर्हंत नहीं हैं वे धर्मतीर्थ के करने वाले भी नहीं हैं । जैसे-पागल पुरुष । और ये धर्मतीर्थंकर हैं इसीलिए ये ही नमस्कार के योग्य हैं ।' इस प्रकार से अविनाभाव नियम से निश्चय एक लक्षण वाले हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है । इसमें बाधा नहीं आती है ।
शंका – आपका यह 'धर्म तीर्थकरत्वात्' हेतु अनैकांतिक है क्योंकि जो अर्हंत नहीं हैं ऐसे सुगत आदि में भी देखा जाता है । वे भी अपने-अपने इष्ट धर्म-रूपी आगम के प्रतिपादक-रूप से उन-उन वादियों द्वारा कहे जाते हैं ?
समाधान – ऐसी बात नहीं है । उनका व्यवच्छेद करने के लिए ही तो श्लोक में 'स्याद्वादिभ्य:' ऐसा विशेषण दिया गया है । स्यात्-कथंचित्-सत् असत्रूप वस्तु को वंदतीति-कहने वाले स्याद्वादी कहलाते हैं । तथाहि - 'अर्हंत ही धर्म तीर्थ को करने वाले हैं क्योंकि स्याद्वादी हैं ।' अर्हंत से अतिरिक्त जीवों में स्याद्वादी-पना बन नहीं सकता है कि जिससे उन्हें धर्म-तीर्थकर कहा जा सके । क्योंकि क्षणिक, नित्यत्व आदि सर्वथा एकांत-वादी होने से उनमें स्याद्वादी-पना विरुद्ध ही है ।
प्रश्न – शास्त्र-कार ने यहाँ मंगल किसलिए किया है ?
उत्तर – 'स्वात्मोपलब्धये' अपने नमस्कार करने वाले का आत्मा अनंतज्ञानादि स्वरूप है उसकी उपलब्धिसिद्धि के लिए यहाँ नमस्कार किया गया है । 'सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि:' ऐसा कथन भी है अर्थात् अपने आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाना ही सिद्धि है, ऐसा पूज्यपाद-स्वामी ने कहा है और ज्ञानावरण आदि कर्म-मल का अभाव हो जाने से अनंतज्ञानादि स्वरूप का लाभ होना ही मंगल का फल कहलाता है । यहाँ यह बात सिद्ध हुई है ।
🏠
सन्तानेषु निरन्वयक्षणिकचित्तानामसत्स्वेव चे-
त्तत्त्वाहेतुफलात्मनां स्वपरसज्र्ल्पेन बुद्ध: स्वयम् ॥
सत्त्वार्थं व्यवतिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मक: ।
स्यान्नित्यत्ववदेव तत्र समये नार्थक्रिया वस्तुन: ॥2॥
अन्वयार्थ : [तत्त्वाहेतुफलात्मनां] वास्तविक कार्यकारण भाव से रहित [निरन्वयक्षणिकचित्तानां] निरन्वय क्षणिक चित्त-ज्ञानक्षणों की [असत्सु एवं संतानेषु] असत्रूप संततियों में ही [बुद्ध: स्वयं स्वपरसंकल्पेन] बुद्ध स्वयं स्व पर के संकल्प से [मिथ्याविकल्पात्मक:] मिथ्या विकल्प करते हुए [करुणया सत्त्वार्थं] करुणा बुद्धि से प्राणियों के उद्धार के लिए [व्यवतिष्ठते] ठहरते हैं [नित्यत्ववदेव] नित्यत्व के समान ही [तत्र समये] उस क्षणिक सिद्धांत में [वस्तुन: अर्थक्रिया न स्यात्] वस्तु में अर्थक्रिया नहीं हो सकती है ॥२॥
अभयचन्द्रसूरि :
क्षणिकैकांतवादी बुद्ध यदि स्वयं अपने स्वरूप से ठहरता है, निर्वाण को नहीं जाता है । किसलिए ? सभी के लिए-दु:ख से शिष्यजनों का उद्धार करने के लिए करुणा बुद्धि से ठहरता है । 'तिष्ठंत्येव पराधीना येषां तु महती कृपा' ऐसा वाक्य है । प्रतिपादक बुद्ध तो स्व है और प्रतिपाद्य दिङ्नाग आदि आचार्य पर हैं, स्वपर के संकल्प से-असत् में सत् का आरोप करके वह बुद्ध भगवान ठहरता है । अवास्तविक कार्य कारण स्वरूप परस्पर में भिन्न निरन्वय क्षणिक चित्तों की असत् रूप संततियों के होने पर भी वह स्वपर का संकल्प करता है अर्थात् स्व और पर जब दोनों ही क्षणिक हैं, निरन्वय हैं फिर भी पर में करुणा करके आप स्वयं ठहरता है । पुन: वह बुद्ध धर्मतीर्थंकर कैसे हो सकता है ? यहाँ यह अभिप्राय है । क्योंकि मिथ्या-असत्यरूप संकल्प करने वाला वह बुद्ध स्वयं मिथ्या विकल्पस्वरूप है । यहाँ प्रथमांत में भी हेतु का प्रयोग संभव है अत: मिथ्याविकल्पात्मक होने से वह बुद्ध धर्म तीर्थंकर नहीं है । ऐसा अर्थ होता है । जिस प्रकार से सर्वथा नित्यत्व में परमार्थसत् की व्यवस्था करने वाले ईश्वर कपिल और ब्रह्मा धर्मतीर्थंकर नहीं होते हैं क्योंकि वे मिथ्या विकल्प वाले हैं उसी प्रकार बुद्ध भी नहीं हैं, यह अर्थ सिद्ध हुआ ।
वेदांती - आपका यह सभी कथन हमें इष्ट ही है क्योंकि हमारे द्वारा मान्य प्रतिभासाद्वैत-ब्रह्माद्वैत सिद्धांत ही परमार्थ से सत रूप है ।
जैन - समय अर्थात् सम्-संगत संपूर्ण ज्ञानों में अनुगत अय-प्रतिभास को समय कहते हैं । मतलब संपूर्ण ज्ञानों में या जीवों में अनुगत-अन्वयरूप से रहने वाले ज्ञान या ब्रह्म को समय कहते हैं । इस निरुक्ति के अनुसार समय का अर्थ प्रतिभासाद्वैत हो गया है । यह तुम्हारा प्रतिभासाद्वैत-ब्रह्माद्वैतवाद सिद्धांत में भी ठीक नहीं है । सभी वस्तु को अद्वैत-एकरूप मान लेने पर तो अर्थ क्रियारूप अनुभव नहीं हो सकता है क्योंकि मिथ्या-विकल्प दोनों जगह समान ही है ।
माध्यमिक - स्वप्न और इंद्रजाल के ज्ञान के समान सभी ज्ञान निरालंबन हैं पुन: अनुमान ज्ञान को प्रमाणता कैसे हो सकती है कि जिससे आप अर्हंत भगवान् को तीर्थंकर सिद्ध कर सकें ?
जैन - सम-स्वप्न और जाग्रत दशा में समान रूप से होने वाला अय-ज्ञान समय है । इस निरुक्ति से आप माध्यमिक की मान्यता समय कहलाती है । ऐसे इस आप के समय-सिद्धांत में हेयोपादेयरूप अर्थ में त्याग और ग्रहण लक्षण क्रिया परमार्थ से नहीं हो सकती है । यहाँ श्लोक में वस्तुन: की जगह वस्तुत: पाठ भी मिलता है उसके आधार से यह अर्थ किया है क्योंकि अप्रमाण से त्याग और ग्रहण लक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती है अन्यथा अतिप्रसंग दोष हो जावेगा ।
इसी कथन से विभ्रमैकांत-वाद का भी खंडन हो गया है अत: जैसे क्षणिकत्व, नित्यत्व आदि एकांत मत मिथ्या-विकल्प -- गलत कल्पनारूप हैं। उसी प्रकार यथा-अवसर शास्त्र-कार स्वयमेव आगे कहेंगे, इसलिए हम यहाँ विराम लेते हैं ।
भावार्थ – बौद्धों का सिद्धांत है कि महात्मा बुद्ध जीवों के उद्धार की करुणा बुद्धि से जगत में रुकते हैं, मुक्ति में नहीं जाते हैं पुन: उनके यहाँ सभी को निरन्वय क्षणिक माना है इसलिए आचार्य कहते हैं कि आपके यहाँ सर्वथा क्षणिक मान्यता में स्व-पर की कल्पना भी कैसे बनेंगी क्योंकि आप भी क्षण-क्षण में नष्ट हो रहे हैं और आपके शिष्यादि भी क्षण-क्षण में नष्ट हो रहे हैं। तब तो बुद्ध कैसे तो ठहरेंगे और किसको तो उपदेश देंगे कुछ समझ में नहीं आता है । ब्रह्माद्वैत-वाद में भी सर्वथा अद्वैत होने से किसको तो छोडना और किसको ग्रहण करना इत्यादि अर्थ-क्रिया असंभव है । ऐसे ही माध्यमिक स्वप्न-ज्ञान के समान ही सारे ज्ञानों को निरालंब कहता है क्योंकि बाह्य पदार्थों को सर्वथा ही काल्पनिक कह दिया है पुन: उसके त्यागोपादान-रूप अर्थ-क्रिया असंभव है । इन-इन मतों का यथा-संभव आगे खंडन किया जायेगा ।
🏠
प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं। मुख्यसंव्यवहारत:॥
परोक्षं शेषविज्ञानं। प्रमाणे इति संग्रह:॥3॥
अन्वयार्थ : [मुख्य संव्यवहारत:] मुख्य और संव्यवहार के भेद से [विशदं ज्ञानं प्रत्यक्षं] विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है [शेष विज्ञानं परोक्षं] अविशद ज्ञान परोक्ष है। [प्रमाणे इति संग्रह:] प्रमाण शब्द द्विवचन निर्देश से प्रमाण के दो भेदों का संग्रह हो जाता है॥३॥
अभयचन्द्रसूरि :
शिष्य के भेद
प्रतिपादन के योग्य शिष्य चार प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न, संदिग्ध और विपर्यस्त। उनमें से आदि के एवं अंत के-व्युत्पन्न और विपर्यस्त ऐसे दो प्रकार के शिष्य तो समझाने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनमें व्युत्पन्न होने की-समझने की इच्छा का अभाव है। अव्युत्पन्न-अज्ञानी में तो लोभ, भय आदि से समझने की इच्छा उत्पन्न करके समझाना चाहिए अर्थात् स्वर्ग, मोक्ष आदि का लोभ और संसार आदि से भय दिखाकर उस अज्ञानी में समझने की इच्छा उत्पन्न करके समझाना योग्य है और जो संदिग्ध हैं, उन्हें अपने संदिग्ध अर्थ के विषय में प्रश्न करने पर समझाना योग्य है। (शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है)। यहाँ पर अव्युत्पन्न और संदिग्ध इन दो प्रकार के शिष्यों के प्रति प्रमाण के उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा का प्रतिपादन करते हैं क्योंकि शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है।
उनमें से अर्थ के नाम मात्र का कथन करना उद्देश है। जिसका उद्देश किया गया है उसके असाधारण स्वरूप का निरूपण करना लक्षण है और प्रमाण के बल से उस लक्षण के विसंवाद पक्ष का निराकरण करना परीक्षा है। उनमें प्रमिति-प्रमाण को कहना है इतना मात्र कथन उद्देश है क्योंकि सभी शून्यवादी भी अपने इष्ट के साधन और अनिष्ट के दूषण की अन्यथानुपपत्ति से प्रमाण को स्वीकार करते हैं, यह बात प्रसिद्ध है और वह प्रमाण ज्ञान ही होता है यह लक्षण निर्देश है क्योंकि यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। प्रमाणत्व की अन्यथानुपपत्ति अन्य प्रकार से प्रमाणता नहीं हो सकती है। इस प्रकार हेतुवाद को परीक्षा कहते हैं क्योंकि उस परीक्षा से ही उस लक्षण के विसंवाद का निराकरण होता है। उसी को कहते है।
प्रमाण का लक्षण
‘प्रकर्षेण’-प्रकृष्ट रूप से-संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय का व्यवच्छेद-निराकरण करके स्व और पर स्वरूप को जो ‘मिमीते जानाति’ जानता है, या ‘मीयतेऽनेन’ जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा ‘मितिमात्रं’ जानना मात्र प्रमाण है। प्रमाण शब्द की ऐसी व्युत्पत्ति होती है। निश्चय और व्यवहारनय के द्वारा द्रव्य और पर्याय में अभेद और भेद की विवक्षा से उस प्रकार की संभव है अर्थात् निश्चयनय से द्रव्य और पर्याय में अभेद होने से ‘प्रकर्षेण मिमीते इति प्रमाणं’ जो प्रकर्ष रीति से जानता है वह जानने वाला आत्मा ही प्रमाण है क्योंकि ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है और व्यवहारनय से द्रव्य-पर्याय में भेद होने से ‘मीयतेऽनेनेति प्रमाणं’ जिसके द्वारा जाना जाय वह प्रमाण है, यहाँ आत्मा कर्तारूप और ज्ञान करण रूप होने से आत्मा से ज्ञान में कथंचित् भेद विवक्षित है।
अज्ञान को प्रमाण मान लेने से उस अज्ञान से संशय आदि मिथ्या ज्ञानों का निराकरण करना शक्य नहीं है क्योंकि वे अज्ञान के अविरोधी हैं। जो जिसका विरोधी होता है वही उसको अलग कर सकता है ,अन्य नहीं कर सकता है। जैसे कि प्रकाश अंधकार का विरोधी होने से उसे दूर कर देता है। अज्ञानस्वरूप सन्निकर्षादि संशय आदि मिथ्याज्ञान के निराकरण करने वाले नहीं हैं इसलिए वे सन्निकर्ष आदि प्रमाणता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं ?
सन्निकर्षवाद का खंडन-रूप के समान रस में भी चक्षु इंद्रिय का संयुक्त समवाय लक्षण सन्निकर्ष विद्यमान है। फिर भी वह सन्निकर्ष-संबंध उसके ज्ञान में हेतु नहीं है अर्थात् जैसे चक्षु रूप को देख रही है वैसे ही रस को भी देख रही है, रस के साथ भी उसका सन्निकर्ष लक्षण संबंध मौजूद है फिर भी वह चक्षु रस का ज्ञान नहीं कर पाती है। रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से ही तो होता है।
चक्षु इन्द्रिय का भी रूप के साथ सन्निकर्ष-स्पर्श करके जानने रूप संबंध नहीं है, क्योंकि वह चक्षु इंद्रिय अप्राप्त-बिना स्पर्श किये ही पदार्थों का प्रकाशन करती है। देखिये! पर्वत आदि को देखते समय चक्षु पर्वत आदि अर्थरूप प्रदेश के पास नहीं जाती है और न वे पर्वत आदि चक्षु इंद्रिय के स्थान तक आते हैं जिससे कि चक्षु का पदार्थ के साथ संयोग इन दोनों का अपने-अपने योग्य प्रदेश में अवस्थित रहना ही प्रतीति में आ रहा है।
वैशेषिक-उस चक्षु के तेज का संयोग है ही है।
जैन-ऐसा आप नहीं कर सकते। तेज का संयोग होने से तो अंधकार का ही विच्छेद होगा न कि संशयादि मिथ्या ज्ञानों का। क्योंकि तेज का संशय आदि से कोई विरोध नहीं है, ऐसा मैंने पहले ही कह दिया है। इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, अचेतन होने से घट आदि के समान।
भावार्थ-वैशेषिक कहता है कि इंद्रियों का पदार्थ को छूकर जानना सन्निकर्ष है और वही प्रमाण है। तब आचार्य ने कहा जैसे चक्षु का रूप से संबंध है वैसे ही रस से भी है पुन: रूप को तो जान लें और रस को न जाने यह क्या बात है। दूसरी बात यह है कि चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, पर्वत आदि प्रदेश बहुत दूर हैं। उन पर अग्नि जल रही है चक्षु ने देख लिया है किन्तु न पर्वतादि चक्षु से स्पर्शित हुए हैं और न चक्षु ही उनके पास गई है। ये लोग चक्षु में एक तेजोद्रव्य मानते हैं वह भी कल्पना निराधार है तथा यदि चक्षु में तेज मान भी लें तो भी वह तेज अंधकार को दूर करेगा न कि संशयादि को। इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है।
नैयायिककारक साकल्य को प्रमाण मानते हैं उसका निराकरण
कारकसाकल्य भी प्रमाण नहीं है क्योंकि वह भी अचेतन है सन्निकर्षादि के समान। यदि कारक साकल्य को प्रमाण मानेंगे तो कर्ता, कर्म आदि को पृथक् करने का अभाव होने से वह प्रमाण अवलंबनरहित और निष्कल हो जावेगा।
नैयायिक-कारक और उनके साकल्य में अत्यंत भेद होने से यह दोष नहीं आता है।
जैन-यदि आप अत्यंत भेद मान लेते हैं तब तो प्रमाण (कारक) और उसकी सकलता में अभेद कैसे होगा ? क्योंकि प्रमाण को करणरूप से मानने से वह तदात्मक नहीं हो सकेगा।
नैयायिक - करणरहित ही प्रमाण है।
जैन - ऐसा आप नहीं कह सकते, अन्यथा क्रिया और कारक से भिन्न प्रमाण की सिद्धि हो जाने पर तो वह प्रमाण अर्थक्रिया से शून्य हो जावेगा, आकाश पुष्प के समान।
नैयायिक - कारकों का समुदाय ही प्रमाण है।
जैन - ऐसा पक्ष स्वीकार करने पर भी उस कारक समुदायरूप प्रमाण के जानने में कारक साकल्य लक्षण एक और प्रमाण मानना पड़ेगा, पुन: उसके भी जानने के लिए एक और कारक साकल्य नाम वाला प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से तो अनवस्था का प्रसंग आ जावेगा इसलिए कारक साकल्य भी प्रमाण नहीं है क्योंकि वह भी अज्ञानरूप ही है।
भावार्थ - एक जरन्नैयायिक कहलाते हैं वे लोग कारक-कर्ता कर्म करण आदि कारकों की सफलतापूर्णता को प्रमाण कहते हैं। तब आचार्य ने कहा है कि वास्तव में सभी कारक मिलकर भी अचेतन ही रहते हैं पुन: वे प्रमाण कैसे हो सकेंगे। हाँ, ये कारक ज्ञान को उत्पन्न करने में सहकारी कारण हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें उपचार से प्रमाण माना जा सकता है किन्तु मुख्यरूप से ज्ञान ही प्रमाण है।
सांख्य द्वारा मान्य प्रमाण का खंडन
सांख्य -‘इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणं’-इंद्रियों का व्यापार ही प्रमाण है।
जैन] - प्रमाण का यह लक्षण भी असंभव है, क्योंकि अचेतन रूप होने से यह भी विशेष नहीं है सन्निकर्ष के समान। बात यह है कि इंद्रियों का व्यापार का आप क्या अर्थ करते हैं-उन्मीलन आदि व्यापार या संशयादि का निराकरण। प्रथम पक्ष में प्रमाणता नहीं है क्योंकि व्यभिचार दोष आता है, कहीं संशय आदि में भी इंद्रियों का उन्मीलन आदि व्यापार देखा जाता है। यदि संशयादि का निराकरण होना रूप दूसरा पक्ष लेते हो तब तो ‘ज्ञान ही प्रमाण है’ यह बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि अज्ञान से संशयादि का निराकरण हो नहीं सकता है इसलिए इन्द्रियवृत्ति प्रमाण नहीं है। हाँ, इन्द्रियाँ ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं इसलिए उपचार से प्रमाण हैं यह बात सर्वत्र मान्य ही है।
प्रभाकर द्वारा मान्य प्रमाण का खंडन
प्रभाकर - ज्ञाता का व्यापार ही प्रमाण है।
जैन - प्रश्न यह होता है कि वह ज्ञाता का व्यापार ज्ञानात्मक है या अज्ञानात्मक। यदि वह ज्ञानात्मक है तब तो बात ठीक ही है। पुन: वही ज्ञान ही प्रमाण सिद्ध हो जाता है। यदि आप उसे अज्ञानस्वरूप कहेंगे तब तो वहाँ संशयादि को दूर करने वाले किसी भिन्न प्रमाण का अनुसरण करना ही पड़ेगा और यदि वह अज्ञानस्वरूप है तो पुन: उसके लिए एक प्रमाण ढूंढ़ना पड़ेगा, ऐसे अनवस्था आ जावेगी। अत: यह प्रमाण का लक्षण भी ठीक नहीं है।
शंका - अज्ञानरूप भी सन्निकर्ष आदि संशय आदि को दूर करने में कारण हो जावें, क्या दोष है ?
समाधान - ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संशयादि अज्ञान विशेष होने से ज्ञान सामान्य से व्याप्त हैं और व्यापक के द्वारा व्याप्य का निराकरण नहीं किया जा सकता है अन्यथा व्याप्यव्यापक भाव में विरोध हो जावेगा।
शंका - संशयादि ज्ञान विशेषरूप होने से ज्ञान सामान्य के साथ व्याप्त हैं तो पुन: ज्ञान के साथ उनका विरोध कैसे है ?
समाधान - ऐसा नहीं है। यहाँ सम्यग्ज्ञान ही ज्ञानरूप से विवक्षित है और संशयादि मिथ्याज्ञानरूप हैं, इसलिए इनका सम्यग्ज्ञान के साथ विरोध सिद्ध है।
इसलिए यह ठीक नहीं है कि ‘ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति अन्यथा-अन्य प्रकार से नहीं सकती है।
बौद्ध द्वारा मान्य प्रमाण का निरसन
सौगत - ज्ञान प्रमाण होवे, ठीक है किन्तु वह विज्ञानाकार गोचर में ही प्रमाण है।
जैन - वह ज्ञान निर्विकल्प ही है क्योंकि विकल्प अवस्तु को विषय ही करता है।
जैन - यहाँ विज्ञान का ऐसा अर्थ करना चाहिए। वि-विशेष जाति आदि आकार का ज्ञान निश्चय है जिसके वह विज्ञान है किन्तु निर्विकल्पक दर्शन विज्ञान नहीं है क्योंकि उस दर्शन का व्यवहार में उपयोग नहीं होता है। छोड़ना, ग्रहण करना आदि रूप जो व्यवहारी लोगों का फल है वह निर्विकल्पदर्शन से नहीं बन सकता है अन्यथा निश्चय को विफल होने का प्रसंग आ जायेगा।
‘सभी विभ्रम ही है’ इस प्रकार के विभ्रमैकांत पक्ष में भी संव्यवहार विशेष नहीं बन सकता है। संशय आदि का निराकरण करने से ही ज्ञान संव्यवहार में हेतु है किन्तु भ्रांति से नहीं है, जिससे कि सभी ज्ञान भ्रांत हो सकें अर्थात् सभी ज्ञान भ्रांत नहीं हैं।
विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध - निश्चय को कराने वाला भी ज्ञान बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेने वाला नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थों का ही अभाव है।
यौगादि - ज्ञान पदार्थों का ही निश्चय कराने वाला है किन्तु वह अपने स्वरूप को नहीं जानता है क्योंकि अपने में क्रिया का विरोध है।
भावार्थ - विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध बाह्य पदार्थों को नहीं मानते हैं केवल ज्ञान मात्र को ही स्वीकार करते हैं और यौग आदि कहते हैं कि ज्ञान बाह्य पदार्थों को ही जानने वाला
वह स्वयं को नहीं जानता है। आगे आचार्य इन दोनों के मत का निराकरण करने के लिए निरुक्ति अर्थपूर्वक विज्ञान शब्द की व्याख्या करते हैं।
विज्ञानाद्वैतवादी का खंडन
जैन - वि-विविध स्व और अपूर्व अर्थ को विषय करने वाला, ज्ञान अवबोध है जिसका वह ‘विज्ञान’ है। इस प्रकार से व्याख्या की गई है।
बाह्य अर्थ से शून्य ज्ञान प्रमाण नहीं है कि जिससे बाह्य अर्थ शून्यता उस ज्ञान के सिद्ध हो सके, क्योंकि उस बाह्य अर्थ की शून्यता को सिद्ध करने वाला अनुमान बाह्य अर्थ के अवलंबनपूर्वक ही होता है अन्यथा साध्य और साधन दोनों समान हो जावेंगे। दूसरी बात यह है कि आप बौद्ध ज्ञान के अस्तित्व को अंतर्मुख अनुभव के बल से स्वीकार करते हुए बहिर्मुख अनुभव के बल से ज्ञेय के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो कोई एक महान आश्चर्य है। एक को समीचीन और दूसरे को मिथ्या कहना भी स्वच्छंद मान्यता ही है किन्तु विचारशीलता नहीं है, क्योंकि दोनों जगह कोई अंतर नहीं है। इसलिए ज्ञान बाह्य अर्थ से शून्य नहीं है।
प्रमाणान्तर से निश्चित भी संशय आदि से सहित अपूर्वार्थ है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसी में ही प्रमाण की सफलता है।
यौग का खंडन
ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला अस्वसंवेदी है। ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान प्रकाशरूप है। वह ज्ञान स्व और पर को विषय करने वाला-जानने वाला है यह बात प्रतीति से सिद्ध है। इस ‘नील’ आदि को ‘मैं’ जानता हूँ। इस प्रकार से ‘मैं’ शब्द से अंतरंग का और ‘नीलादि’ शब्द से बाह्य पदार्थों का अनुभव सिद्ध है।
अन्यथा-यदि नहीं मानोगे तो बाह्य पदार्थों के अनुभव का भी अभाव हो जायेगा।
यौग - स्वात्मा में क्रिया का विरोध है अर्थात् अपने आप में क्रिया न हो सकने से ज्ञान अपने आपको कैसे जानेगा ?
जैन - यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध दो में से किसी एक के अभाव से सिद्ध होता है अर्थात् शीत और उष्ण इन दोनों का विरोध है अत: शीत के अभाव में रहता हुआ उष्ण शीत का विरोध करता है यह बात सिद्ध है किन्तु ज्ञान में तो ऐसी बात है नहीं कि वह अपने में रहते हुए अपने आपका ही विरोध करे। इसलिए ज्ञान की जानने रूप क्रिया का स्वयं ज्ञान में विरोध नहीं है।
ज्ञान में स्वरूप और जानना ये दोनों बातें उपलब्ध हो रही हैं। देखो! जिस प्रकार से प्रदीप और प्रकाशन का एक जगह अविरोध सभी लोगों को मान्य है, उसी प्रकार से स्वरूप और जानना इन दोनों का भी अविरोध स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि न्याय से यह बात सिद्ध है अन्यथा पक्षपात का प्रसंग आ जाता है इसलिए ठीक ही कहा है कि अपना और अपूर्व अर्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान ही विज्ञान है। ( यहाँ तक आचार्यों ने प्रमाण के निर्दोष लक्षण को सिद्ध किया है। अब आगे प्रमाण की संख्या के विसंवाद को दूर करते हैं) -
वह प्रमाण एक प्रत्यक्ष ही है, इस प्रकार चार्वाक विसंवाद करते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण हैं’ इस प्रकार सौगत और वैशेषिक कहते हैं। सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाण को मानते हैं। नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ऐसे चार मानते हैं। प्रभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति ऐसे पाँच मानते हैं। भाट्ट प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव ऐसे छह मानते हैं। इन सभी के विसंवाद को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं कि ‘प्रमाणे इति संग्रह:’- सकल प्रमाण के भेद-प्रभेदों की संख्या को संग्रह करने वाले प्रमाण के दो प्रकार ही हैं किन्तु उपर्युक्त माने गये एक, दो, तीन आदि नहीं हैं क्योंकि इन दो प्रमाणों में ही अन्य सभी भेद गर्भित हो जाते हैं। संक्षेप से अथवा समस्त रूप से ग्रहण करना ‘संग्रह’ शब्द का अर्थ है, यहाँ ऐसा समझना।
शंका - ‘प्रमाण है’ इस एक संख्या से ही बस हो उसी एक में ही ये संख्याये गर्भित हो जायेंगी, पुन: प्रमाण को दो मानने से क्या प्रयोजन है ?
समाधान - ऐसा नहीं कहना, क्योंकि भेदों की गणना ही संख्या कहलाती है और एक तो अभेदरूप है। हाँ, द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से वह प्रमाण एक ही है किन्तु पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से तो प्रमाण के सभी भेदों को दो प्रमाण में ही संग्रहीत किया गया है अर्थात् द्रव्यार्थिक नय से सामान्यतया प्रमाण एक है और पर्यायार्थिकनय से प्रमाण के दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन दो में ही सारे प्रमाण के भेद-प्रभेद गर्भित हो जाते हैं।
प्रमाण के दो भेद होवें ठीक ही है किन्तु प्रत्यक्ष और अनुमान के भेद से दो भेद होते हैं। इस प्रकार की सौगत की आशंका को दूर करते हुए प्रत्यक्ष, परोक्ष के भेद से दो भेद हैं, ऐसा मन में करके श्री भट्टाकलंक देव उनमें से प्रथम को पहले कहते हैं-
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण
‘प्रत्यक्षं विशदं’ जो विशद-स्पष्ट प्रतिभास वाला ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ‘अक्ष्णेति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष-आत्मा’ अक्ष धातु का अर्थ है व्याप्त होना-जानना, जो व्याप्त होता है जानता है वह अक्ष-आत्मा है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसको है अथवा ज्ञानावरण कर्म का क्षय जिसके हो गया है। ऐसी उस आत्मा के प्रति जो नियत-निश्चित है-उस आत्मा से उत्पन्न होता है और पर की अपेक्षा नहीं रखता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है अर्थात् आत्मा में आवरण कर्म के क्षयोपशम से या क्षय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है क्योंकि अविशदस्वरूप-अस्पष्ट प्रतिभास वाला प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जावेगा।
प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद का कथन
वह प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्य और संव्यवहार के निमित्त से दो प्रकार का है। उसमें मुख्य प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं-अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान। ये ज्ञान अशेष रूप से विशद-स्पष्ट प्रतिभासी हैं और इन्द्रिय आदि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। अपने-अपने आवरण विशेष के पृथक् होने से उत्पन्न होते हैं इसलिए ये मुख्य रूप से ‘प्रत्यक्ष’ इस नाम को प्राप्त करने वाले होते हैं। ‘प्रत्यक्षमन्यत्’ इस सिद्धान्त के अनुरोध से इनकी प्रत्यक्षता अनुपचरित-वास्तविक है, उपचरित नहीं है।
जो इन्द्रिय और मन के निमित्त से होने वाला मतिज्ञान है, वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है क्योंकि वह एकदेश विशद-स्पष्ट-निर्मल है। समीचीन प्रवृत्तिरूप व्यवहार संव्यवहार कहलाता है। उसको आश्रय लेकर प्रवृत्ति होने से इस मतिज्ञान में प्रत्यक्षता मानी गई है। यह प्रत्यक्षता उपचार से ही है अर्थात् यह मतिज्ञान उपचार से ही प्रत्यक्ष है।‘आद्ये परोक्षम्’ इस सूत्र में जो मतिज्ञान को परोक्ष कहा है वह मुख्य कथन है अर्थात् मतिज्ञान मुख्यरूप से परोक्ष ही है इसलिए यहाँ उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मानने में सिद्धान्त विरुद्ध कथन नहीं है। ऐसा समझना चाहिए।
भावार्थ - सिद्धान्त ग्रंथ तत्त्वार्थसूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण से अवधि आदि तीन ज्ञान लिये हैं और परोक्ष से मति, श्रुत इन दो ज्ञानों को लिया है। यहाँ पर अकलंकदेव ने प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद किये हैं-मुख्य और सांव्यवहारिक। मुख्यरूप से अवधि आदि तीनों ज्ञानों को ले लिया है और सांव्यवहारिक से मतिज्ञान को लिया है। टीकाकार अभयचंद्रसूरि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सांव्यवहारिक मतिज्ञान उपचार से ही प्रत्यक्ष है, मुख्य रूप से नहीं। इसलिए यहाँ सिद्धान्त विरुद्ध कथन करने का दोष नहीं आता है।
अब परोक्ष प्रमाण का लक्षण कहते हैं
शेष विज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। शेष-प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप से भिन्न अविशद स्वभाव वाला ज्ञान परोक्ष प्रमाण कहलाता है। उसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क , अनुमान और आगम ऐसे पाँच भेद हैं। यह परोक्ष ज्ञान पर कारणों की अपेक्षा से प्रवृत्त होता है। स्मृति आदि में प्रत्यक्ष आदि निमित्त माने गये हैं अर्थात् स्मृति ज्ञान पूर्व में अनुभव किये गये प्रत्यक्ष की अपेक्षा रखता है। प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों की अपेक्षा करता है इत्यादिरूप से पर की अपेक्षा रखने से ही ये ज्ञान परोक्ष कहलाते हैं।
( ग्रंथ में संबंध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन ये चार चीजें होना आवश्यक हैं। इसलिए इन्हीं चारों का स्पष्टीकरण करते हैं-)
‘प्रमाणे’ इस कथन से इस शास्त्र को अभिधेय वाला सूचित किया है अर्थात् इस ग्रंथ के अभिधेयवाच्य विषय को बतलाया है। ‘प्रमाण’ इस कथन से इस ग्रंथ प्रमाण, नय और निक्षेपों का कथन है क्योंकि इनसे शून्य ग्रंथ आदरणीय नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ‘बंध्या का पुत्र जाता है’ इत्यादि को कहने वाले शास्त्र आदरणीय नहीं हैं।
वाच्य वाचक भावलक्षण संबंध तो सुघटित ही है क्योंकि शास्त्र और उसका वाच्य प्रमाण इन दोनों के संबंध का सद्भाव है अन्यथा दश अनार, छह पुये इत्यादि वाक्य के समान यह ग्रंथ अप्रयोजक ही रहेगा अर्थात् किसी ने बिना किसी संबंध के दश अनार, छह पुये आदि यद्वा-तद्वा वाक्य कहा तो उसका वह कथन संबंध रहित होने से अप्रयोजनीभूत है।
शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो प्रमाण आदि के विषय में अज्ञान की निवृत्ति लक्षण साक्षात् फल देखा ही जाता है, शास्त्र के अध्ययन के अनंतर ही (उस विषयक) अज्ञान का अभाव हो जाता है। परम्परा से हान, उपादानादिरूप फल होता है क्योंकि प्रवचन-शास्त्र हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराने में समर्थ होता है। जो शास्त्र निष्प्रयोजन होते हैं वे प्रवृत्ति के कारण नहीं होते हैं। जैसे कौवे के दांत की परीक्षा करना निष्प्रयोजन ही है।
इसलिए ‘प्रत्यक्षं विशदं’ इत्यादि रूप से जो कथन किया गया है वह ठीक ही है।
भावार्थ - इस ग्रंथ के उद्देश्य को बतलाते हुए आचार्य ने यहाँ पर सबसे प्रथम शिष्यों के भेद बतलाये हैं। पुन: इस ग्रंथ में प्रमाण का वर्णन है, ऐसा संकेत करते हुए यह बताया है कि शास्त्र की प्रवृत्ति उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा इन तीन प्रकार होती है। पुन: प्रमाण का लक्षण करके अन्य मतावलंबियों द्वारा मान्य प्रमाण के लक्षण का निराकरण किया है। प्रमाण के भेदों के विसंवाद को दूर करके दो भेद सिद्ध किये हैं एवं उन्हीं में सभी प्रमाणों के अंतभूर्त होने का संकेत किया है। अनंतर यह बात भी स्पष्ट की है कि ग्रंथ में संबंध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान और इष्टप्रयोजन ये चार चीजें अवश्य होनी चाहिए अन्यथा उसका आदर नहीं होता है।
इनको बतलाते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसको अध्ययन करने के अनंतर ही उस विषय का ज्ञान होने से अज्ञान का अभाव हो जाता है यह साक्षात् फलरूप इष्ट प्रयोजन है और परम्परा से त्याग करने योग्य को छोड़ना, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना इन दोनों से रहित में अपेक्षा करना यह फल है, इसलिए यह प्रमाणभूत है।
🏠
अनुमाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्।
तद्वैशद्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमत: परम् ॥4॥
अन्वयार्थ : [अनुमानाद्यतिरेकेण] अनुमान आदि के बिना [विशेष प्रतिभासनं] जो विशेष प्रतिभास होता है [तद् बुद्धे: वैशद्यं मतं] वह ज्ञान की विशदता है [अत: परं अवैशद्यं] इससे भिन्न अविशदता है॥४॥
अभयचन्द्रसूरि :
अनुमान, आगम आदि के बिना जो वस्तु के विशेष-वर्ण संस्थान आदि आकारों का प्रतिभासन-जानना होता है अथवा जो भिन्न प्रतीति के व्यवधान के बिना जानना होता है, वह विशेष प्रतिभासन कहलाता है और वही ज्ञान की विशदता-निर्मलता है। विशद के भाव को विशदता या वैशद्य कहते हैं। यहाँ पर वही स्याद्वादियों को इष्ट है।
अनुमान आदि में साधारण ऐसा विशेष प्रतिभासन प्रत्यक्ष में प्रतीत नहीं होता है कि जिससे उन अनुमान आदि ज्ञानों में भी विशदता हो सके इसलिए उपर्युक्त लक्षण वाली विशदता से अन्य व्यवहित (तिरोहित) प्रतिभासन-ज्ञान अविशद कहलाते हैं। वह अविशदता-अस्पष्टता अनुमान आदि सभी परोक्ष ज्ञान के भेदों में व्यवस्थित है। इस प्रकार से बाह्य अर्थ की अपेक्षा से ही ज्ञान में स्पष्टता-अस्पष्टता होती है, ऐसा श्री भट्टाकलंकदेव ने कहा है। स्वरूप की अपेक्षा से तो सभी ज्ञान विशद ही हैं क्योंकि स्वसंवेदन-स्व को जानने में किसी भी ज्ञान में भिन्न ज्ञान का व्यवधान नहीं आता है।
उन ज्ञान की प्रमाणता और अप्रमाणता भी बाह्य अर्थ की अपेक्षा से ही है न कि स्वरूप की अपेक्षा से।अपने स्वरूप का अनुभव करने में सभी ज्ञान में अप्रमाणता का अभाव है।
भाव-अपने स्वरूप के प्रमेय की अपेक्षा होने पर प्रमाणाभास का अभाव है तथा बाह्य प्रमेय की अपेक्षा में प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों होते हैं, ऐसा श्री समंतभद्रस्वामी ने कहा है।
भावार्थ - यहाँ खास बात यह समझने की है कि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से ही ज्ञान में स्पष्टता-अस्पष्टता होती है, अपने स्वरूप को जानने में नहीं। अपने स्वरूप के जानने में सभी ज्ञान स्पष्ट ही हैं तथा दूसरी बात यह है कि ज्ञान का जब अपना स्वरूप ही प्रमेय-विषय है तब उसमें प्रमाणाभास नहीं होता है क्योंकि यदि संशय ज्ञान अपने स्वरूप में विपरीत है तो वह असंशय रूप हो जावेगा। इसी प्रकार से चाहे समीचीन ज्ञान हो चाहे मिथ्या, अपने-अपने स्वरूप से सभी उसी रूप होने से समीचीन ही हैं किन्तु बाह्य पदार्थों को प्रमेय-विषय करने की अपेक्षा से ज्ञान में प्रमाण और प्रमाणाभास ये दो विकल्प हो जाते हैं। जो ज्ञान बाह्य पदार्थों को बाधारहित या संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ग्रहण करते हैं वे समीचीन कहलाते हैं और जो ज्ञान पदार्थों को बाधा सहित संशय आदि सहित ग्रहण करते हैं वे प्रमाणाभास कहे जाते हैं। इस बात को यहाँ बतलाया है।
🏠
अक्षार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधी:।
अवग्रहे विशेषाकांक्षेहाऽवायो विनिश्चय:॥5॥
धारणा स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्।
अन्वयार्थ : [अक्षार्थयोगे] इंद्रिय और पदार्थ का योग होने पर सत्तामात्र का आलोक दर्शन है [अर्थाकारविकल्पधी:] पुन: अर्थ के आकार के विकल्प वाला ज्ञान [अवग्रह] है [अवग्रहे विशेषाकांक्षा ईहा] अवग्रह के विषय में विशेष आकांक्षा का होना ईहा है [विनिश्चय:] विशेष का निश्चय [अवाय:] अवाय है [स्मृति हेतु: धारणा] स्मृति का हेतु धारणा है [तत् मतिज्ञानं चतुर्विधं] वह मतिज्ञान चार प्रकार का है॥५॥ [१/२]
अभयचन्द्रसूरि :
सूत्र उपस्कार सहित होते हैं। इस नियम से यहाँ उत्पद्यते-उत्पन्न होता है; इस क्रिया का अध्याहार होता है अर्थात् सत्तालोक-दर्शन उत्पन्न होता है ऐसा संबंध है। सत्ता-संपूर्ण पदार्थों में साधारण रूप से रहने वाले, ऐसे सत्त्वसामान्य-अस्तित्व सामान्य को, आलोक-निर्विकल्प ग्रहण करना दर्शन कहलाता है। सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं, ऐसा आगम में कथित है।
प्रश्न - यहाँ मतिज्ञान के प्रकरण में दर्शन अप्रकृत है अर्थात् यहाँ दर्शन का कोई प्रकरण नहीं है पुन: इसका वर्णन क्यों किया ?
उत्तर - ऐसा नहीं कहना। ज्ञान से पूर्व के परिणाम को बतलाने के लिए यहाँ उसका ग्रहण किया गया है क्योंकि छद्मस्थ जीवों को दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, ऐसा आगम वचन है।
प्रश्न - सिद्धान्त में स्वरूप के ग्रहण करने को दर्शन कहा है पुन: यहाँ सत्तामात्र ग्रहण को दर्शन कहा है। इस कथन के सिद्धान्त से विरोध क्यों नहीं आता है ?
उत्तर - विरोध नहीं आता है क्योंकि अभिप्राय में भेद है। पर के विसंवाद को दूर करने के लिए ही न्यायशास्त्र होते हैं। इन न्यायशास्त्रों से पर के द्वारा स्वीकृत निर्विकल्प दर्शन ही प्रमाणता का खंडन करने के लिए स्याद्वादियों ने सामान्यग्रहण (सत्तामात्र ग्रहण) को दर्शन कहा है। स्वरूप ग्रहण की अवस्था में छद्मस्थजीवों को बाह्यपदार्थ विशेष के ग्रहण का अभाव है और प्रमाणता का विचार तो बाह्यपदार्थ की अपेक्षा से ही किया गया है क्योंकि वह व्यवहार में उपयोगी है। देखो! व्यवहारी लोग स्वरूप के प्रकाशन के लिए प्रदीप का अन्वेषण नहीं करते हैं इसलिए दर्शन बाह्य पदार्थ विशेष के व्यवहार के लिए अनुपयोगी है। उसमें तो ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि वही बाह्य पदार्थ विशेष के व्यवहार में उपयोगी है तथा वह विकल्पात्मक है।
परमार्थ से तो स्वरूप का ग्रहण करना ही दर्शन है क्योंकि केवली जीवों से दर्शन और ज्ञान इन दोनों की युगपत् प्रवृत्ति होती है अन्यथा ज्ञान के सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय करने के अभाव का प्रसंग आ जावेगा अर्थात् सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय है और यदि ज्ञान को वस्तु के विशेष अंश को विषय करने वाला ही मानेगें तो फिर सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय नहीं हो सकेगी।
भावार्थ-सभी पदार्थों में सामान्य और विशेष ऐसे दो धर्म पाये जाते हैं। जैसे-वृक्षों में वृक्षत्व यह सामान्य धर्म है आरै सभी वृक्षों में पाया जाता है नीम, आम, जामुन आदि विशेष धर्म है कोई न कोई विशेष धर्म भी सभी वृक्षों में मौजूद ही है। दर्शन का लक्षण है सामान्य अस्तित्व मात्र को ग्रहण करना और ज्ञान का लक्षण है वस्तु के विशेष आकारादि को ग्रहण करना किन्तु सिद्धान्त ग्रंथों में दर्शन का लक्षण है स्वरूप को ग्रहण करना और ज्ञान का लक्षण है बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना। ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण का विषय है सामान्य विशेषात्मक वस्तु।
यहाँ पर आचार्य ने सत्तामात्र ग्राहक दर्शन को माना है तब शंकाकार ने शंका की है कि आपके इस कथन से सिद्धांत में विरोध आता है। इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य ने कहा कि न्यायग्रंथ पर के द्वारा माने गये विपरीत प्रकरणों को निराकरण करने वाले होते हैं। बौद्ध ने ज्ञान को निर्विकल्प माना है, उसकी मान्यता का खंडन करने के लिए न्याय ग्रंथों में दर्शन को स्वरूप को ग्रहण करने वाला कहा है। यह भी बताया है कि वह बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वह व्यवहार में उपयोगी नहीं है और ज्ञान प्रमाण है। वही बाह्य वस्तु के व्यवहार में उपयोगी है। पुन: यह भी स्पष्ट कह दिया है कि दर्शन के विषय में जो सिद्धांत की मान्यता है, वही वास्तविक है।
(दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है ?)
शंका - सत्तामात्र अवलोकन रूप दर्शन कैसे उत्पन्न होता है ?
समाधान - इंद्रिय और पदार्थ का योग होने पर होता है। अक्ष-इन्द्रियाँ-स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इंद्रियाँ हैं और मन यह छठी इन्द्रिय है (इसे अनिंद्रिय भी कहते हैं)। उन इन्द्रियों के दो भेद हैं-द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। उसमें पुद्गलपरिणाम को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। उसके भी निर्वृत्ति और उपकरण दो भेद हैं। जीव के परिणाम को भावेन्द्रिय कहते हैं। उसके लब्धि और उपयोग ऐसे दो भेद हैं।
अर्थ ग्रहण की शक्ति का नाम लब्धि है और अर्थ ग्रहण के व्यापार का नाम उपयोग है।
(इन्द्रिय के आकार की रचना को निर्वृत्ति तथा उनके सहायक अवयवों को उपकरण कहते हैं।)
‘निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्, लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्१’ ऐसा सूत्रकार का वचन है।
शंका-मन को इंद्रिय कैसे कहा है ?
समाधान-अंत:करण रूप होने से मन का इन्द्रियपने से विरोध नहीं है।
विषय को अर्थ कहते हैं। उन इन्द्रिय और अर्थ का योग्य देश में अवस्थान होना योग कहलाता है, उसके होने पर होता है अर्थात् इन्द्रिय और विषय के योग्य देश में रहने पर वह दर्शन उत्पन्न होता है।
शंका - ऐसा मानने पर तो इन्द्रिय के समान पदार्थ भी दर्शन की उत्पत्ति में कारण हो जावेंगे ?
समाधान - ऐसा नहीं कहना, क्योंकि पदार्थ में व्यापार नहीं देखा जाता है और दर्शन का पदार्थ के साथ अन्वय व्यतिरेक भी नहीं है, केश में मच्छर के ज्ञान के समान अर्थात् जहाँ-जहाँ पदार्थ हो वहीं-वहीं पर दर्शन उत्पन्न हो और जहाँ-जहाँ पदार्थ न हो वहाँ-वहाँ दर्शन उत्पन्न न हो, इसको अन्वय-व्यतिरेक कहते हैं। यह नहीं देखा जाता है प्रत्युत् केश में मच्छर का ज्ञान हो जाता है। यदि पदार्थ के निमित्त से दर्शन या ज्ञान उत्पन्न होते तो केशों में केश का ही ज्ञान होता, न कि मच्छर का।
देखिये! नेत्र आदि के व्यापार के समान पदार्थ का व्यापार ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं देखा जाता है क्योंकि वे पदार्थ तो उदासीनरूप ही हैं।
(ज्ञान की उत्पत्ति और भेद)
पुन: उसके अनन्तर वही दर्शन अवग्रह हो जाता है। वह वैâसा है ? अर्थाकार के विकल्पात्मक ज्ञानरूप है अर्थात् अर्थ-विषय के आकार-वर्ण आदि विशेष का निश्चय कराने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। अर्थ यह हुआ कि दर्शन ही ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम विशेष से सहित हुआ पदार्थ विशेष के ग्रहण लक्षण वाले अवग्रह रूप से परिणत हो जाता है। जैसे कि ‘आकाश में यह वस्तु है’, इस प्रकार का ज्ञान।
अनंतर वही अवग्रह पुन: ईहा हो जाता है। वह किस रूप है ? विशेष आकांक्षारूप है अर्थात् विशेष बगुला को जानने की जो इच्छा है। वह ‘भवितव्यता-होना चाहिए’ इस ज्ञानरूप है। जैसे कि (आकाश में जो श्वेत कुछ दिखा था) वह बगुला होना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान ईहा है।
अनंतर वही ईहाज्ञान अवाय हो जाता है। वह किस लक्षण वाला है ? विशेष निश्चय लक्षण वाला है अर्थात् आकांक्षित विषय का निर्णय हो जाना अवाय है। जैसे कि ‘यह बगुला ही है।’ यह ज्ञान निश्चयरूप है।
पुन: वही अवायज्ञान धारणा हो जाता है। उसका क्या लक्षण है ? वह स्मृति में हेतु है अर्थात् वह धारणा भूतकाल के पदार्थ के परामर्शरूप स्मृति का कारण है। यही संस्कार का लक्षण है जो कि कालांतर में भी विस्मरण न होना। मतलब कालांतर में भी नहीं भूलने रूप संस्कार ज्ञान को धारणा कहते हैं। इस प्रकार से यह मतिज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का होता है और यह प्रत्येक इन्द्रिय से होता है, ऐसा जानना चाहिए।
भावार्थ - यहाँ दर्शन और मतिज्ञान का लक्षण तथा मतिज्ञान के चारों भेदों का लक्षण बतलाया गया है। इन्द्रियाँ अपने स्थान पर अवस्थित हैं तथा पदार्थ भी यथायोग्य अपने स्थान पर अवस्थित हैं। इन इन्द्रिय और पदार्थ के यथायोग्य अवस्थित रहने पर आत्मा में जो सत्तामात्र का-अस्तित्व मात्र का अवभास होता है, वह दर्शन है। वास्तव में यह इतना अव्यक्त है कि इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। अनंतर उसी आत्मा को किसी इन्द्रिय के अवलंबन से यह मालूम होता है कि ‘यह है’ तब आत्मा का वही दर्शन ज्ञानरूप परिणत हो जाता है। ऐसे ही वही-वही ज्ञान आगे-आगे विशेष-विशेष को ग्रहण करने से अगले-अगले नामों को प्राप्त कर लेता है अर्थात् जीव का लक्षण है उपयोग। उसके दो भेद हैं-दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ऐसा जानना चाहिए।
🏠
बह्वाद्यवग्रहाद्यष्टचत्वारिंशत्स्वसंविदाम्॥6॥
पूर्वपूर्वप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्॥
अन्वयार्थ : [स्वसंविदां] स्वसंवेदन ज्ञानों में [बह्वाद्यवग्रहाद्यष्ट चत्वारिंशत्] बहु आदि बारह भेदों के अवग्रह आदि चार भेद होने से अड़तालीस भेद होते हैं। [इनमें] [पूर्वपूर्वप्रमाणत्वं] पूर्व-पूर्व के ज्ञान प्रमाण हैं और [उत्तरोत्तर] आगे-आगे के ज्ञान [फलं स्यात्] फल हैं॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
(मतिज्ञान के विशेष भेद)
तात्पर्यवृत्ति-बहु है आदि में जिनके वे बहु आदि अर्थ विशेष हैं। उनके बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनि:सृत,अनुक्त, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी-अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, नि:सृत, उक्त और अध्रुव ये बारह भेद हैं। इनमें प्रत्येक के अवग्रह आदि चार अर्थ विशेष को ग्रहण करने वाले होते हैं अत: उनके अड़तालिस भेद हो गये अर्थात् बहु आदि बारह से अवग्रह आदि चार को गुणित करने से अड़तालिस भेद हो जाते हैं। प्रत्येक इन्द्रिय के प्रति ये भेद संभव होने से इन्हें छह इंद्रियों से गुणा करने से अर्थ के प्रति दो सौ अठ्यासी भेद हो जाते हैं।
व्यंजन के प्रति अवग्रह ही होता है। चक्षु और मन से रहित चार इन्द्रियों से बहु आदि बारह को गुणित करने से अड़तालिस भेद हो जाते हैं क्योंकि व्यंजन में ईहा आदि असंभव हैं अर्थात् व्यंजनावग्रह के अड़तालिस भेद हो गये हैं। अव्यक्त शब्दादि समूह का व्यंजनावग्रह होता है।
(बहु आदि का लक्षण)
अब बहु आदि का किंचित अर्थ कहते हैं।
‘बहु’ का अर्थ अनेक होता है। जैसे बहुजन। उससे प्रतिपक्षी उल्टे का एक अर्थ होता है जैसे एक जन। अनेक जाति से भिन्न- भिन्न को बहुविध कहते हैं। जैसे बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उससे विपरीत एकविध है जैसे ब्राह्मण लोग। क्षिप्र-शीघ्रता यह ज्ञान का विशेषण है। जैसे एक बार में ग्रहण करना। उससे विपरीत धीरे-धीरे ग्रहण करना अक्षिप्र है। प्रगट हुए को संवृत, अप्रगट को अनि:सृत कहते हैं। जैसे-जल में डूबे हुए हाथी की सूंड मात्र ऊपर है। इससे विपरीत प्रगट-खुले हुए को नि:सृत कहते हैं। जल में हाथी पूरा निकला हुआ है । आभ्f ाप्राय से समझने को अनुक्त कहते हैं जैसे - अग्नि के लाने में सकोरा आदि को बिना कहे ही समझ लिया। प्रतिपादित को उक्त कहते हैं। जैसे-स्पष्ट रीति से ‘लाओ’ ऐसा कहने पर लाना। अवस्थित रहने को ध्रुव कहते हैं यह ज्ञान का विशेषण है। अनवस्थित को अध्रुव कहते हैं। जैसे-फूटे बर्तन का जल। अथवा स्थिर पर्वत आदि ध्रुव हैं और बिजली आदि अस्थिर पदार्थ अध्रुव हैं। इनके विषय रूप से अवग्रह आदि विशिष्ट रूप होते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन में भी लगा लेना चाहिए। अर्थावग्रह, ईहा आदि के २८८ भेद और व्यंजनावग्रह के ४८ भेद इन दोनों को जोड़ देने से मतिज्ञान के तीन सौ छत्तीस भेद हो जाते हैं।
भावार्थ-अवग्रह ज्ञान के दो भेद हैं-व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। दर्शन के अनंतर जो शब्दादि का अव्यक्त ग्रहण होता है, वह व्यंजनावग्रह है। इसके आगे ईहा आदि नहीं होते हैं और यह अव्यक्त ज्ञान चक्षु और मन से भी नहीं होता है इसलिए अवग्रह को शेष चार इन्द्रियों से गुणने से १५४=४ भेद हुये। पुन: यह ज्ञान भी बहु आदि को विषय करता है अत: इससे बारह को गुणने से १२*४=४८ भेद हो जाते हैं। अनंतर व्यक्त-स्पष्ट को ग्रहण करने वाला अर्थावग्रह ज्ञान होता है। इसके आगे ईहा आदि भेद भी व्यक्त को ग्रहण करने वाले होते हैं। ये चारों ज्ञान बहु आदि को विषय करते हैं। अत: १२ को ४ से गुणित करके ६ इंद्रियों से गुणने से १२*४*६=२८८ भेद होते हैं। इनको जोड़ देने से २८८+४८=३३६ भेद हो जाते हैं। ये सब मतिज्ञान के भेद हैं।
(ज्ञान स्वसंवेदी भी हैं)
शंका-बाह्य पदार्थों के अवलंबन लेने से ही ज्ञान के ये भेद संभव हैं। अत: ज्ञान स्वव्यवसायात्मक - स्व को जानने वाला कैसे होगा ?
समाधान-ऐसी बात नहीं है। ये भेद स्वसंवेदन के होते हैं। कारिका में ‘स्वसंविदाम्’ पद है। पुन: यहाँ पर ‘अपि’ शब्द का अध्याहार करना चाहिए। तब ऐसा अर्थ निकलता है कि ये भेद केवल अर्थ संवेदन के ही नहीं है किन्तु स्वसंवेदन के भी अवग्रह आदि होते हैं। स्व-ज्ञानस्वरूप का, संविद-वेदन, भिन्न ज्ञानों की अपेक्षा न करके अनुभव होना जिनमें है वे ज्ञान स्वसंवेदन कहलाते हैं। यहाँ ऐसा व्याख्यान है।
ज्ञान अस्वसंवेदी नहीं है अन्यथा अर्थ के संवेदन का भी विरोध हो जावेगा। यदि आप ऐसा कहें कि ज्ञान अपने स्वरूप को दूसरे ज्ञान से जानता है, तब तो अनवस्था का प्रसंग आ जावेगा। इस कथन से ‘ज्ञान परोक्ष है’ ऐसा कहने वाले मीमांसक, ‘ज्ञान ज्ञानांतर से प्रत्यक्ष है’ ऐसा कहने वाले यौग, ‘ज्ञान अचेतन है’ऐसा कहने वाले सांख्य और ज्ञान पृथ्वी आदि भूतचतुष्टय का परिणाम है ऐसा कहने वाले चार्वाक इन सभी का खंडन कर दिया गया है क्योंकि इन सबके मत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित हैं।
भावार्थ-प्रश्न यह उठा था कि ये मतिज्ञान के बहु आदि की अपेक्षा करके अवग्रह आदि ज्ञान के ३३६ भेद हुए हैं। ये सब भेद बहु आदि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से ही तो हुए हैं अत: ज्ञानत्व को जानने वाला नहीं है मात्र पर पदार्थों को ही जानने वाला है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा कि ये भेद पदार्थों को ग्रहण करने वाले ज्ञान के ही नहीं हैं किन्तु स्व को अनुभव करने वाले स्वसंवेदी ज्ञान के भी ये सभी भेद होते हैं क्योंकि ज्ञान स्व-पर प्रकाशी है। यदि ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो वह परपदार्थों को भी नहीं जान सकेगा। इस पर नैयायिक ने कहा कि ज्ञान अपने स्वरूप को दूसरे ज्ञान से जानता है। तब आचार्य ने कहा कि ऐसी मान्यता में पुन: उस दूसरे ज्ञान के स्वरूप को तीसरे ज्ञान से जानेगा आदि। ऐसी व्यवस्था में तो अनवस्था आ जावेगी अत: ज्ञान को स्व परवेदी मानना उचित है।
मीमांसक परोक्ष ही है वह पदार्थ को जानता है किन्तु वह स्वयं किसी से नहीं जाना जाता है। यौग ज्ञान को दूसरे ज्ञान से वेद्य मानता है। सांख्य कहता है कि ज्ञान अचेतन है, वह प्रकृति-जड़ का परिणाम है। चार्वाक कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन भूतचतुष्टय से आत्मा बनता है आरै ज्ञान भी इन्हीं का परिणाम है । यहाँ पर ज्ञान को स्व पर को जानने वाला सिद्ध कर देने से इन सभी की मान्यता का निराकरण हो जाता है।
(प्रमाण का फल)
शंका-अवग्रह ज्ञान को प्रमाण मान लेने पर फल के अभाव का प्रसंग आ जाता है ?
समाधान-ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पूर्व-पूर्व के ज्ञान प्रमाण हैं।
दो बार पूर्व शब्द का ग्रहण वीप्सा अर्थ में है। जिस प्रकार से पूर्व-पूर्व के अवग्रह आदि ज्ञान को प्रमाणता है, उसी प्रकार से उत्तर-उत्तर के ईहा आदि ज्ञान साक्षात् फल हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रमाण और फल में कथंचित् अभेद है। यदि प्रमाण और उनके फल में सर्वथा भेद अथवा सर्वथा अभेद मान लिया जाय तो इनकी अर्थक्रिया नहीं हो सकेगी। विवक्षा से कारक की प्रवृत्ति होती है, ऐसा न्याय है।
जो चेतन द्रव्य, अन्वय ज्ञान के बल से अनुगताकार और अखंड प्रसिद्ध है। वही पूर्वाकार का परिहार, उत्तराकार की प्राप्ति और मूल स्वभाव की स्थिति लक्षण परिणाम से परिणमन करता हुआ व्यतिरेक ज्ञान के बल से प्रत्येक पर्यायों में भिन्न-भिन्न अनुभव में आता है। इस प्रकार से प्रमाण और फल का व्यवहार बन जाता है।
प्रमाण का परम्पराफल तो हान-उपादान आदि सर्वत्र साधारण ही है अर्थात् ज्ञान का फल है कि छोड़ने योग्य को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना तथा इन दोनों में विपरीत में उपेक्षा करना। सच्चे ज्ञान से हेय, उपादेय वस्तुओं को जानकर परम्परा से उनका त्याग आदि किया जाता है, यही परम्परा फल है।
वह ज्ञान की प्रमाणता-सच्चाई अभ्यस्त विषय में तो स्वत: सिद्ध है क्योंकि जाने हुए विषय में भिन्नज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है किन्तु अनभ्यस्त विषय में पर से-भिन्न प्रमाण से सिद्ध होती है क्योंकि जिस विषय को नहीं जानते हैं, उनमें अनुमान आदि की अपेक्षा करनी पड़ती है। सर्वथा पर से ही प्रमाणता हो ऐसी बात नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जावेगा और अनवस्था दोष आ जावेंगे। इसलिए ठीक ही कहा है कि अवग्रह आदि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं।
भावार्थ-बात यह है कि प्रमाण फल वाला ही होना चाहिए और यहाँ पर अवग्रह ज्ञान प्रमाण है उसका फल आगे का ईहाज्ञान है। पुन: ईहा ज्ञान प्रमाण है तब उसका फल अवाय है, ऐसे ही आगे समझना। यह फल अपने प्रमाण से कथंचित् भिन्न है, कथंचित् अभिन्न। समीचीन जानना यह प्रमाण है और उसके ‘उसी क्षण में अज्ञान का दूर होना तथा कालांतर में हेय-उपादेय का छोड़ना, ग्रहण करना, ये फल हैं। ये फल अपने लक्षण से, नाम से, कार्य से कथंचित् प्रमाण से भिन्न हैं तथा जिस आत्मा ने जाना है उसी के अज्ञान का अभाव हुआ है और उसी ने छोड़ा या ग्रहण किया है। इस दृष्टि से प्रमाण से उसका यह फल अभिन्न है। यह स्याद्वाद व्यवस्था है।
यह प्रमाण की सच्चाई का वर्णन जाने-बूझे विषयों में स्वत: हो जाता है। जैसे-कोई प्यासा मनुष्य अपने परिचित के कुएं से पानी भर लेता है। इसमें पानी है या नहीं इस बात को किसी से नहीं पूछता है तथा अपरिचित विषय में प्रमाण की सच्चाई पर से जानी जाती है। जैसे-अपरिचित स्थान में प्यासा मनुष्य अवश्य ही पास के कृषक आदि से पूछता है कि इस कुएं में जल है या नहीं। कोई कहते हैं कि प्रमाण की प्रमाणता पर से ही होती है, सो एकांत मान्यता गलत ही है।
श्लोकार्थ - जो अकलंक चन्द्रमा से विशद प्रतिभासित है, उस सभी को आप लोगों के लिए प्रभा के बल से सूरि की तात्पर्यवृत्ति व्यक्त कर रही है।।१।।
भावार्थ - भट्टाकलंक देव को यहाँ चन्द्रमा की संज्ञा दी है जैसे चन्द्रमा का निर्मल प्रतिभास होता है ऐसे ही भट्टाकलंकदेवरूपी चन्द्र के द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्ष प्रमाण का विशद लक्षण प्रतिभासित हो रहा है अर्थात् इन्होंने प्रत्यक्ष का लक्षण विशद किया है और उसका विशद-स्पष्टरूप से विवेचन किया है और प्रभाचंद्राचार्य ने इस लघीयस्त्रय की न्यायकुमुदचन्द्र नाम से टीका रची है। उस टीका रचना के मनन के अनन्तर श्री अभयचंद्रसूरि ने यह तात्पर्यवृत्ति बनाई है। यह सूरि द्वारा रचित तात्पर्यवृत्ति आप लोगों को इस प्रत्यक्ष प्रमाण का सभी अर्थ स्पष्ट कर रही है ऐसा यहाँ अभिप्राय है।
इस प्रकार से अभयचंद्रसूरि कृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण
नामक तात्पर्यवृत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण नाम का
पहला परिच्छेद पूर्ण हुआ।
🏠
अथ द्वितीय परिच्छेद:
तद्द्रव्यपर्यायात्मार्थो बहिरन्तश्च तत्त्वत:॥7॥
अन्वयार्थ : [तत्त्वत:] परमार्थ से [तद्-द्रव्यपर्यायात्मा] उस प्रमाण का द्रव्य पर्यायात्मक [बहि:अंत: च] बहिरंग और अंतरंग पदार्थ [अर्थ:] विषय है॥७॥
अभयचन्द्रसूरि :
भावार्थ-प्रमाण और फलभूत अवग्रह आदि क्रम से होते हैं फिर भी उनमें तादात्म्य है और उसका विषय भी अभिन्न है इस बात को पहले कहा जा सकता है अब यहाँ उसी विषय को बतलाते हुए कहते हैं कि अंतरंग और बहिरंग रूप चेतन-अचेतन पदार्थ ही जिस प्रकार से वास्तव में प्रमाण के विषय हैं अथवा विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध ने अंतस्तत्व को प्रमाण का विषय माना है वेैसे ही बाह्य वस्तु भी प्रमाण का विषय है यहाँ चकार को टीकाकार ने इव अर्थ में लिया है।
तात्पर्यवृत्ति -‘प्रमाणं’ यह अनुवृत्ति में चला आ रहा है। यहाँ पर तद् शब्द से वह ग्रहण किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ती का संबंध होता है तब ‘तस्य प्रमाणस्य’ ऐसा हो जाता है। जो ‘अर्यते गम्यते ज्ञायते’- जाना है उसे अर्थ कहते हैं, यह धातु से बना है। इस प्रकार से विषय को अर्थ कहते हैं। अचेतन घट, पटादि बाह्य पदार्थ और चेतन रूप अंतरंग उस प्रमाण के विषय हैं क्योंकि प्रमाण स्व और पर अर्थ को जानने वाला है ऐसा प्रतिपादित किया गया है।
(सभी पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक हैं)
अन्विताकार (यह वही है) द्रव्य और व्यावृत्ताकार (यह वह नहीं है) पर्याय है। ये द्रव्य और पर्याय जिसके स्वभाव-धर्म हैं वह द्रव्यपर्यायात्मक कहलाते हैं। चेतन-अचेतन सभी पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक ही होते हैं। वे परमार्थरूप से वैसे होते हैं न कि कल्पना मात्र से क्योंकि अन्यथारूप से अर्थ-पदार्थ हो नहीं सकते हैं। उसी का स्पष्टीकरण - प
प्रमाण के विषयभूत जीवादि पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक हैं क्योंकि वे प्रमाण के विषय हैं। जो द्रव्य पर्यायात्मक नहीं होता है वह प्रमाण का विषय भी नहीं होता है। जैसे-बन्ध्या का पुत्र। और प्रमाण के विषय जीवादि हैं इसलिए वे द्रव्य पर्यायात्मक हैं। इस अनुमान वाक्य से प्रमाण के विषय जीवादि पदार्थ द्रव्य पर्यायात्मक सिद्ध हो जाते हैं।
एकांत से द्रव्य ही अथवा पर्याय ही अथवा परस्पर में निरपेक्ष ये दोनों ही अर्थक्रिया में समर्थ नहीं हैं, जिससे कि वे प्रमाण के विषय हो जावें क्योंकि उस-उस एकांत में क्रम और युगपत् का अभाव होने से अर्थ-क्रिया नहीं हो सकती है। ये क्रम और युगपत् दोनों ही अनेकांत से व्याप्त हैं अत: अनेकांत के बिना नहीं हो सकते हैं।
इन क्रम युगपत् से अर्थक्रिया व्याप्य है और उस अर्थक्रिया से प्रमेय व्याप्य है तथा व्यापक का अभाव परम्परा से भी व्याप्य के अभाव को सिद्ध कर ही देता है। व्याप्य का सद्भाव व्यापक को सिद्ध करता है अत: हमें इसकी चिंता से क्या प्रयोजन है।
शंका -अर्थक्रिया प्रमेय से कैसे व्यापक है ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की परिणतिरूप लक्षण वाली अर्थक्रिया में ही अथवा बहिरंग-अंतरंग पदार्थ में प्रमाण की प्रवृत्ति होती है अन्यथा गृहीत को ग्रहण करने वाले होने से सभी ज्ञान अप्रमाणीक हो जावेंगे और विषय रहित होने से असत् रूप हो जावेंगे क्योंकि उस प्रकार की अर्थक्रिया के बिना स्वप्न में भी अस्तित्व उपलब्ध नहीं होता है और असत् अभाव प्रमेय नहीं होता है।
शंका-अनेकांत क्रम और युगपत् में कैसे व्यापक है ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना। पर्याय की अपेक्षा से देश, काल का क्रम और द्रव्य की अपेक्षा से युगपत् संभव है अर्थात् सभी वस्तुओं में पर्याय की अपेक्षा से देश और काल का क्रम देखा जाता है और द्रव्य की अपेक्षा से अक्रम रहता है।
भावार्थ-अपने कार्य का करना अर्थक्रिया कहलाती है। जैसे-घट की जलधारण अर्थक्रिया है। ज्ञान की हेयोपादेय के त्याग और ग्रहणरूप अर्थक्रिया है। यहाँ यह बतलाया है कि केवल अकेला द्रव्य या मात्र स्वतंत्र पर्यायें या परस्पर में एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हुए दोनों ही अर्थ में क्रिया को नहीं कर सकते हैं इसलिए प्रमाण के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं। पुन: यह बतलाया है कि एकांत में क्रम और अक्रम न होने से अर्थक्रिया नहीं है क्योंकि ये क्रम-अक्रम दोनों ही अनेकांत से व्याप्त हैं। (संबंध रखते हैंअनेकांत के होने पर ही होते हैं) और इन क्रम-अक्रम से अर्थक्रिया व्याप्य है और उस अर्थक्रिया से प्रमेय प्रमाण का विषय व्याप्य है। ‘व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च’ व्यापक तत् और अतत् दोनों में रहता है और व्याप्य तत् में ही निष्ठ रहता है। जैसे-वृक्षत्व ये व्यापक है नीम आदि सभी वृक्षों में है और नीम व्याप्य है वह उसी में रहता है।
व्यापकरूप वृक्षत्व का अभाव अपने व्याप्यरूप नीम के अभाव को ही सिद्ध करता है। यहाँ क्रम और अक्रम अनेकांत से व्याप्त है इसलिए अनेकांत व्यापक है और उनसे अर्थक्रिया व्याप्य है।
वैशेषिक-हमारे यहाँ द्रव्य और पर्याय में एकांत से भेद मानने पर भी उनका प्रमेय होना अविरुद्ध ही है। उसी का स्पष्टीकरण -
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छह पदार्थ भावरूप हैं। इनमें द्रव्य के नव भेद हैं। गुण चौबीस होते हैं, कर्म पाँच हैं। सामान्य दो हैं, विशेष अनेक हैं और समवाय एक है। अभावरूप चार हैं-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और अत्यंताभाव। यह सत-असत् रूप पदार्थों का वर्ग परस्पर में अत्यंत भिन्न है और प्रमाण का विषय है।
भावार्थ-वैशेषिक के द्वारा मान्य छह पदार्थों में द्रव्य के नव भेद हैं। उनके नाम-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। गुण के चौबीस भेद हैं। उनके नाम-रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कर्म के पाँच भेद हैं-उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आक्रुन्चन, प्रतारण और गमन। सामान्य के दो भेद हैं-पर सामान्य और अपर सामान्य। विशेष केवल नित्य द्रव्यों में रहता है और वह अनंत है। पूर्वोक्त नव द्रव्य और परमाणु नित्य माने गये हैं। समवाय एक ही है। अनेक भेदों को लिए हुये ये छहों पदार्थ अस्तित्व रूप हैं और प्रागभाव आदि चार प्रभाव के अभाव सर्वथा अभावनास्तित्व रूप हैं। ये द्रव्यगुण आदि परस्पर में, सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं, इस प्रकार के पदार्थों को प्रमाण जानता है। ऐसा वैशेषिक ने कहा है।
जैन -ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि इन सभी में अत्यंत भेद होने पर संबंध नहीं बन सकता है।
वैशेषिक-इनमें समवाय संबंध पाया जाता है।
जैन -नहीं, वह समवाय सभी में साधारणरूप से रहने से नियामक नहीं है। जैसे ज्ञान आदि का आत्मा में समवाय होता है वैसे पृथ्वी आदि में भी ज्ञान के समवाय का प्रसंग हो जावेगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से द्रव्य से भिन्न सभी गुण अद्रव्य हैं उसी प्रकार से सत्तासामान्य से भिन्न द्रव्य आदि का भी असत्व क्यों नहीं हो जाता है ? इसमें कोई अंतर नहीं है।
यदि आप कहें कि द्रव्य अनुगत स्वरूप है अर्थात् अन्वयरूप स्वरूप है। तब तो वह सामान्य ही है अर्थात् वही अन्वय स्वभाव ही तो द्रव्य होता है जो कि सत्सामान्य रूप से अस्तित्व सहित है। पुन: द्रव्य सत्सामान्य से भिन्न कहाँ रहे ? यदि आप कहें कि द्रव्य व्यावृत्त स्वरूप है, तब तो वह व्यावृत्त स्वरूप भी (पररूप से नहीं होना) विशेष ही है अर्थात् अनुगतस्वरूप और व्यावृत्तस्वरूप कहो या सामान्यस्वरूप, विशेषस्वरूप कहो एक ही बात है, इनमें कुछ अन्तर नहीं है।
इसी प्रकार से गुणादि में भी लगा लेना चाहिए अन्यथा पदार्थद्वैत का प्रसंग आ जाता है।
(अभाव प्रमाण के विषय नहीं हैं)
नीरूप-स्वरूपरहित अभाव तो प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है अन्यथा केश में मच्छर के ज्ञान आदि विषयशून्य ज्ञान भी प्रमाणीक हो जायेंगे।
वैशेषिक-अभाव प्रमाणभाव विषय है।
जैन -यदि ऐसा कहो तो केश में मच्छर के ज्ञान में भी केश में मच्छर का ज्ञान है। उसे भी प्रमाण का विषय मानो, क्योंकि दोनों जगह कोई अंतर नहीं है।
वैशेषिक-वहाँ केश में मच्छर की तो कल्पना मात्र है, इसलिए वह ज्ञान मिथ्यारूप है।
जैन- यदि आप ऐसा कहते हैं तब तो अभाव भी नि:स्वभाव होने से वह मिथ्यारूप क्यों न हो जावे ? इसलिए दुराग्रह का ग्रहण छोड़कर कथंचित् भावाभावात्मक ही प्रमाण का विषय स्वीकार करना चाहिए अत: आप वैशेषिक का मत सुमत नहीं है क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आता है।
(नैयायिकाभिमत भेदैकांत का खंडन)
नैयायिक-हमारे यहाँ प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान ये सोलह पदार्थ हैं। इन पदार्थों में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दु:ख और अपवर्ग के भेद से बारह प्रकार का प्रमेय बन जाता है।
जैन -ऐसा नहीं मानना। यहाँ पर भी भेदैकांत में संबंध नहीं बनता है और इन्द्रिय, बुद्धि तथा मन की सामर्थ्य की उपलब्धि रूप साधन से प्रमेय नहीं हो सकता है तथा आत्मा प्रमाता है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति ये अंतर्भेद स्वीकार किये गये हैं।
संशय आदि को प्रमेय नहीं मानने पर व्यवस्था नहीं बन सकती। भेदैकांत पक्ष में संग्रह का विरोध है और प्रत्यक्ष आदि का अंतर्भाव हो भी नहीं सकता है इसलिए आपके द्वारा मान्य सोलह पदार्थ की व्यवस्था संभव नहीं है।
भावार्थ-यौग के दो भेद हैं-वैशेषिक और नैयायिक। प्राय: इनकी मान्यतायें मिलती जुलती हैं। इन दोनों ने अपने माने हुए पदार्थों में परस्पर में सर्वथा भेद माना है पुन: उनमें समवाय से संबंध माना है किन्तु यह कल्पना बिल्कुल गलत है।
जैसे-जीव का ज्ञान गुण जीव से बिल्कुल भिन्न है किन्तु समवाय से उसका संबंध हो रहा है। इस पर आचार्यों का कहना है कि भाई! जीव और ज्ञान पहले अलग-अलग दिखे, फिर उन्हें अलग मानकर उनका संबंध करना चाहिए किन्तु ज्ञान के बिना जीव का, उष्णगुण के बिना अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है इसलिए द्रव्यगुण आदि को भिन्न ही मानना नितांत गलत सिद्धांत है।
(चार्वाक के भेदैकांत का खंडन)
चार्वाक-हमारे यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चार तत्त्व ही प्रमेय हैं और ये परस्पर में अत्यंत भिन्न हैं।
जैन -ऐसा नहीं है क्योंकि पाँचवे जीवतत्त्व का सद्भाव देखा जाता है और उन चार तत्त्वों में परस्पर में अत्यंत भेद असंभव है। अत: तत्त्व दो ही व्यवस्थित होते हैं अर्थात् जीव और पृथ्वी आदि अजीव ऐसे दो ही तत्त्व हैं।
चार्वाक-पृथ्वी आदि का विकार ही चैतन्य है किन्तु भिन्न तत्त्व नहीं है।
जैन -यह तो महान आश्चर्य है कि जो आप अत्यंत विलक्षणभूत चेतन में अभेद मान रहे हैं और सदृश लक्षण वाले पृथ्वी आदि में भेद कहते हैं। देखो! ज्ञान लक्षण वाला चैतन्य है। स्पर्श आदि लक्षण वाले भूतचतुष्टय हैं तथा चारों में भेद है फिर भी स्पर्शादि वाले होने से उन चारों में अभेद प्रतीत हो रहा है।
भावार्थ-चार्वाक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनको भूतचतुष्टय कहता है और इन चारों से ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है तथा इन चारों में परस्पर में अत्यंत भेद स्वीकार करता है किन्तु जैनाचार्यों काकहना है कि मुख्यरूप से जीव और अजीव रूप से दो ही तत्त्व हैं। पृथ्वी, जलादि चारों ही अजीव तत्त्व हैंऔर चेतन आत्मा जीव तत्त्व है। चेतन का अचेतन से सर्वथा भेद है क्योंकि इनके लक्षण जुदे-जुदे हैं। चेतन का लक्षण है ज्ञान और अचेतन का लक्षण है स्पर्श, रस आदि और वैसा ही अनुभव आ रहा है इसलिए चार्वाक का मान्य भेदैकांत गलत है।
(ब्रह्माद्वैतवादी और ज्ञानाद्वैतवादी का खंडन)
अद्वैतवादी-भेदैकांत में ये दोष होवें, ठीक ही है किन्तु हमारे यहाँ अभेदैकांत में यह बात नहीं है।द्रव्य और पर्याय को सर्वथा अभिन्न-एकरूप ही मानने पर इनका प्रमेयरूप होना युक्त है क्योंकि भेद तो अविद्या से कल्पित हैं और भेदों के मानने से अनवस्था भी आ जाती है।
अनंत भेद प्रमाण के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं क्योंकि अनंत का जानना अशक्य है। प्रत्यक्ष के द्वारा निर्विशेष भेद से रहित वस्तु ही जानी जाती है पुन: उसमें कल्पना ही भेदों को कल्पित कर देती है इसलिए अद्वैत ही तत्त्व है।
जैन -इस प्रकार से आप ब्रह्माद्वैतवादी और ज्ञानाद्वैतवादी दोनों की मान्यता प्रमाण से बाधित ही है। क्रिया और कारकरूप भेदों के अभाव में अर्थक्रिया नहीं हो सकती है क्योंकि वह असत् रूप है। ‘यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्’ जो अर्थक्रियाकारी है, वही परमार्थ सत् है ऐसा आप लोगों का ही कहना है।
‘अद्वैत शब्द अपने वाक्य से विपरीत (द्वैत शब्द) का अविनाभावी है, क्योंकि वह नञ् समास पूर्व वाले अखंड पदरूप है जैसे कि ‘अगौ’ इत्यादि पद। इत्यादि रूप अनुमान वाक्य से आपका अद्वैत बाधित हो जाता है। कर्म, उसका फल और परलोक आदि भेदों का भी विरोध हो जाता है।
भावार्थ-अद्वैत शब्द अपने वाच्य अर्थ से विपरीत अर्थ को कहने वाले द्वैत शब्द के बिना नहीं हो सकता है। जैसे-जैन के बिना अजैन शब्द नहीं बनता है। क्योंकि इसमें नञ् समास हुआ है-‘‘न जैन: अजैन:’’ जो जैन नहीं है वह अजैन है। ‘‘न द्वैत: अद्वैत:’’ जो द्वैत नहीं है वह अद्वैत है अर्थात् अद्वैत शब्द अपने विरोधी द्वैत के बिना नहीं होने से द्वैत के अस्तित्व को सिद्ध ही कर रहा है। उपर्युक्त प्रकार के अनुमान से भी अद्वैत सिद्ध नहीं होता है तथा जो कर्मफल परलोकादि रूप या ग्राम, नगर, चेतन, अचेतन आदि रूप से भेद दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे भी विरुद्ध हो जावेंगे।
दूसरी बात यह है कि आप इस अद्वैत को हेतु से सिद्ध करते हो या हेतु के बिना ही। यदि हेतु से कहो तो द्वैत का प्रसंग आ जाता है क्योंकि साध्य और साधन की भेद रूप से ही प्रवृत्ति होती है अर्थात् अद्वैत साध्य को सिद्ध करने वाला साधन हेतु कहलाता है पुन: साध्य और साधन दो चीज हो जाने से द्वैत हो ही गया। यदि आप कहें कि हेतु के बिना ही अद्वैत को सिद्ध करते हैं तब तो वचनमात्र से ही आप अद्वैत को सिद्ध कर रहे हैं पुन: वचनमात्र से सभी लोगों का सभी इष्ट तत्त्व यथेष्ट रूप से सिद्ध हो जावेगा अर्थात् सभी लोग वचनमात्र से अपने-अपने सिद्धांत को सिद्ध कर लेंगे इसलिए अद्वैत एकांत में प्रमेय-प्रमाण का विषय सिद्ध नहीं होता है क्योंकि प्रमाण से विरोध आता है।
(सांख्य द्वारा मान्य अभेदैकांत पक्ष का खंडन)
सांख्य-हमारे द्वारा मान्य अभेद एकांत में प्रकृति आदि तत्त्व प्रमेय बन जाते हैं क्योंकि सर्वत्र आविर्भाव-तिरोभाव के निमित्त से प्रधान का परिणाम संभव है।
जैन -यह आपका कथन भी असंगत है क्योंकि अभेदरूप एकांत के मानने पर तो आविर्भाव और तिरोभाव ही असंभव है, पुन: किससे परिणाम होगा। प्रकृति और पुरुष के भी अभाव का प्रसंग आ जावेगा और अर्थक्रिया भी नहीं बन सकेगी। अभेदैकांत में अर्थक्रिया संभव ही नहीं है क्योंकि उसमें (अभेद में) क्रम का अभाव है।
इस प्रकार से भेदैकांत के समान अभेदैकांत में भी प्रमेयत्व का होना असंभव है इसलिए परमार्थ से चेतन-अचेतनरूप सभी प्रमेय द्रव्य पर्यायात्मक ही हैं, यह बात सुस्थित हो गई।
उपसंहार-कारिका के इस उत्तरार्ध में प्रमाण का विषय बतलाया गया है। आचार्य ने इस बात को स्पष्ट किया है कि परमार्थ से चेतन, अचेतन रूप सभी द्रव्य पर्यायस्वरूप हैं और वे ही ज्ञान के विषय हैं। सांख्य केवल द्रव्य को ही मानता है, बौद्ध केवल पर्याय को मानता है और यौगादि द्रव्य-पर्याय को मानकर भी इन्हें परस्पर में अत्यंत भिन्न मानते हैं। आचार्य ने इन्हें समझाया है कि इस एकांत से इस प्रकार केवल द्रव्य या केवल पर्याय अथवा परस्पर में निरपेक्ष दोनों ही ज्ञान के विषय नहीं होते हैं। इनमें क्रम और अक्रम के न होने से अर्थ क्रिया असंभव है और अर्थक्रिया के बिना ज्ञान के विषय नहीं हो सकते हैं। चूँकि क्रम से युगपत् से कार्य आदि का होना अनेकांत में ही संभव है इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु ज्ञान से जानी जाती है।
इतना कहने के अनंतर वैशेषिक ने और नैयायिक ने कहा कि हम लोगों ने द्रव्य और पर्याय में सर्वथा भेद माना है फिर भी वे ज्ञान से जाने जाते हैं। आचार्य ने कहा कि यह तुम्हारा कथन गलत है। पहले तो तुम्हारे द्वारा मान्य द्रव्य, गुण आदि परस्पर में भिन्न सिद्ध ही नहीं होते हैं। क्या कहीं उष्णत्व के बिना अग्नि का अस्तित्व दिख रहा है ? अत: जब तुम्हारे मान्य तत्त्व ही सिद्ध नहीं हैं तब वे ज्ञान के विषय कैसे हो सकेंगे।
चार्वाक ने भी अपने द्वारा मान्य भूतचतुष्टय को तो भिन्न मान करके उन्हें प्रमाण का विषय चाहा किन्तु आचार्य ने उसके मान्य भूतचतुष्टय को तो एक अजीव तत्त्व कह करके चेतन तत्त्व को अलग सिद्ध कर दिया और समझाया कि जब तुम्हारी मान्यता ही गलत है, तब तुम्हारे मान्य तत्त्व ज्ञान से कैसे जाने जायेंगे।
ब्रह्माद्वैतवादी ने और ज्ञानाद्वैतवादी ने तथा सांख्य ने एकांत से सभी तत्त्वों में अभेद सिद्ध करना चाहा किन्तु आचार्य ने स्पष्ट बतला दिया कि न तो अद्वैत तत्त्व ही सिद्ध है और न प्रकृति पुरुष का एकत्व ही सिद्ध है अत: अभेदैकांत के मान्य तत्त्व भी ज्ञान के विषय नहीं हैं प्रत्युत् द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थ ही प्रमाण के विषय हैं, ऐसा समझना।s
🏠
अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो:।
क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता॥1॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[नित्यक्षणिकपक्षयो:] नित्य और क्षणिक पक्ष में [अर्थ क्रिया न युज्येत] अर्थक्रिया घटित नहीं होती है, [सा] क्योंकि वह अर्थक्रिया [भावानां] पदार्थों में [क्रमाक्रमाभ्यां] क्रम और यौगपद्य के द्वारा [लक्षणतया मता] लक्षणरूप से मानी गई है॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-कार्य को ‘अर्थ’ कहते हैं और ‘क्रिया’ का अर्थ है करना या निष्पन्न होना। चेतन-अचेतन पदार्थों को ‘भाव’ कहते हैं। ‘क्रम’ देश और काल से व्याप्त है, युगपत् को अक्रम कहते हैं। वस्तु को सर्वथा कूटस्थ मानना नित्य पक्ष है, सर्वथा अनित्य का दुराग्रह क्षणिक पक्ष कहलाता है। अभिप्राय यह हुआ कि नित्य और क्षणिक पक्ष में अर्थक्रिया असंभव है क्योंकि पदार्थों में क्रम-अक्रम का होना ही अर्थक्रिया है।
(नित्यपक्ष में अर्थक्रिया का अभाव)
कूटस्थ नित्य में क्रम से कार्य करना बन नहीं सकता है। एक कार्य के उत्पादन काल में ही सभी कार्यों का उत्पादन कर देने की सामथ्र्य नित्य में पायी जाती है। उसमें सहकारी कारणों का मिलना भी अकिंचित्कर है। सहकारी कारण के बिना कार्यों को करने की साम्यर्थ का अभाव होने पर तो नित्यपने की हानि का प्रसंग आ जाता है क्योंकि असमर्थ स्वभाव का परित्याग और समर्थ स्वभाव को ग्रहण करके परिणमन करने वाले को ही तो अनित्य कहते हैं।
भावार्थ-जैसे मिट्टी को सर्वथा वूâटस्थ नित्य कहने पर तो पहली बात यह है कि उस मिट्टी से कुछ कार्य नहीं होगा। यदि आप जबरदस्ती मानें भी तो मिट्टी से एक घड़ा बनते ही उसी समय संपूर्ण मिट्टी से सारे घड़े बन जावेंगे तथा सहकारी कारण दंड, चाक, कुंभार आदि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि सर्वथा नित्यस्वभाव में ये कारण क्या परिवर्तन कर सकेंगे। यदि आप कहें कि सहकारी चक्र, कुंभार आदि कारणों के बिना घट को करने की सामथ्र्य मिट्टी में नहीं है, तब तो पूर्व के असमर्थ स्वभाव का त्याग करके और उत्तर के समर्थ स्वभाव को ग्रहण करके परिणत हुए को ही तो अनित्य कहा जाता है पुन: तुम्हारा नित्य एकांत पक्ष कहाँ रहा ?
इस नित्यपक्ष में युगपत से भी कार्य होना संभव नहीं है। पूर्व समय में कृतकृत्य होने से वह नित्य पदार्थ उत्तर समयों में भी कार्य करने से रहित है। पुन: अर्थक्रिया के बिना उसके अभाव का प्रसंग आ जाता है और स्वभाव में भी अनेक प्रकारता आ जाती है क्योंकि एक स्वभाव से ही अनेक कार्यों का होना युक्त नहीं है अति प्रसंग हो जाता है और कार्य में अभेद-एकत्व का भी प्रसंग आ जाता है।
सांख्य-सहकारी कारण के अनेक प्रकार होने से ही कार्य अनेक प्रकार के होते हैं।
जैन-यह कहना भी गलत है। जो स्वभाव में भेद करने वाले नहीं हैं उन्हें सहकारी कारण ही नहीं कहा जा सकता है इसलिए सर्वथा नित्यपक्ष में क्रम और अक्रम का अभाव होने से अर्थक्रिया का अभाव सिद्ध ही है अत: नित्य पदार्थ का अभाव ही है यह बात सिद्ध हो गई क्योंकि व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव को बतला ही रहा है।
भावार्थ-सांख्य ने कहा कि सभी पदार्थ कूटस्थ नित्य हैं तब आचार्य ने कहा इस नियम से पक्ष में अर्थ क्रिया-कार्य के करने का अभाव रहा तब उन पदार्थों का अस्तित्व वैâसे सिद्ध होगा। कार्य का करना मान भी लीजिए तो यह प्रश्न उठता है कि वह नित्य पदार्थ कार्य करने में समर्थ है या असमर्थ ? यदि समर्थ है तो एक साथ ही सारे कार्य हो जावेंगे और सहकारी कारणों की अपेक्षा भी नहीं रखेंगे क्योंकि वह नित्य पदार्थ हमेशा ही समर्थ स्वभाव वाला है। यदि आप कहें कि सहकारी के मिलने पर ही कार्य होते हैं तब तो तुम्हारा नित्य पदार्थ कार्य करने में स्वयं समर्थ नहीं रहा। सहकारी कारण मिलने पर पूर्व के असमर्थ स्वभाव को छोड़कर समर्थ स्वभाव को ग्रहण करने से वह नित्य कहाँ रहा ? अनित्य ही हो गया। नित्यपक्ष में क्रम से अर्थक्रिया मानने पर ये दोष आते हैं।
यदि आप नित्य पदार्थ में युगपत् अर्थक्रिया मानें तो एक समय में ही सारे कार्य हो जाने से आगे कुछ कार्य नहीं होगा अथवा आगे-आगे कार्य करने में अनेकों स्वभाव मानने पड़ेंगे क्योंकि एकस्वभाव अनेक समयों में अनेक कार्य करे यह संभव नहीं है। आप कहें कि सहकारी कारणों में भेद होने से कार्यों में भेद दिखता है तब तो सहकारी कारण नित्य के स्वभाव में भेद करता है अत: पदार्थ की नित्यता नहीं टिकती है और यदि स्वभाव में भेद नहीं करता है तो वह सहकारी कारण ही नहीं कहलायेगा क्योंकि जो कुछ सहायता करे वही तो सहकारी कारण है अत: नित्यपक्ष में क्रम-अक्रम से अर्थक्रिया का अभाव है।
(क्षणिकपक्ष में भी अर्थक्रिया असंभव है)
क्षणिक एकांत पक्ष में भी क्रम से कार्य करना नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें देश और काल के क्रम का अभाव है।
श्लोकार्थ-जो जहाँ पर है वह वहीं पर है, जो जिस काल में है वह उसी काल में है। पदार्थों की देशकाल में व्याप्ति नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है अर्थात् सर्वथा क्षणिकपक्ष में कोई भी पदार्थ एक क्षण ही टिकता है अनंतर क्षण में नष्ट हो जाता है अतएव वह जिस देश में रहेगा, वहीं उसी क्षण में नष्ट हो जायेगा, दूसरे क्षण टिकेगा ही नहीं पुन: अन्यत्र जायेगा कैसे ? वैसे जिस समय है उसी समय रहेगा, दूसरे क्षण में समाप्त हो जाता है। तब देश काल से उसकी व्याप्ति कैसे बनेगी ?
अन्यथा यदि व्याप्ति मानोगे तो क्षणिकपने का विरोध हो जावेगा।।१।।
बौद्ध-हमारे यहाँ संतान की अपेक्षा से क्रम माना गया है।
जैन-यह बात ठीक नहीं है। वह संतान तो अवस्तु है। दूसरी बात यह है कि संतान ही कार्यकारी है अथवा स्वलक्षण कार्यकारी है। प्रथम पक्ष में संतान को कार्य करने वाला मानने से तो वही वस्तु (वास्तविक) हो जावेगी पुन: क्षणिकवस्तु की कल्पना से क्या प्रयोजन रहा ?
द्वितीय पक्ष में-स्वलक्षण को कार्य करने वाला मानने पर तो संतान के अवस्तु होने से उसकी अपेक्षा रखने वाले स्वलक्षण का क्रम से कार्य करना भी अवास्तविक हो जावेगा। यदि आप तीसरा पक्ष लेते हैं अर्थात् न संतान कार्य करता है न स्वलक्षण किन्तु तीसरा ही कोई कार्य करता है, ऐसा मानने पर तो कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तु ही आ जाती है क्योंकि उन दो के सिवाय तीसरी चीज तो यही है और कुछ नहीं है, पुन: आप जैन हो जाते हैं। इसलिए क्षणिक में क्रम से कार्य करना नहीं घटता है।
इसमें युगपत् भी अर्थक्रिया संभव नहीं है क्योंकि विभ्रम का प्रसंग आ जाता है। कारण के काल में ही कार्य की उत्पत्ति हो जावेगी और उसके कार्य की भी उसी काल में उत्पत्ति हो जावेगी।
शंका-नित्य और क्षणिकपक्ष में अर्थक्रिया न होवे, तो न सही, क्या हानि है ?
समाधान-वह क्रिया भाव-सद्भूत पदार्थों की वह अर्थक्रिया ज्ञप्ति और उत्पत्ति लक्षण से जानी जाती है। चिन्ह को लक्षण कहते हैं। उस लक्षण के भाव को लक्षणता कहते हैं। सभी आस्तिक लोगों ने इसी लक्षण-चिन्ह रूप से उस अर्थक्रिया को स्वीकार किया है क्योंकि वह सभी पदार्थों में व्यापक है तथा व्यापक का अभाव नित्य और क्षणिकपक्ष में व्याप्य जो अस्तित्व है उसके निषेध को सिद्ध कर देता है, यहाँ यह अभिप्राय है क्योंकि उसी प्रकार का कथन किया गया है।
प्रत्यक्ष से सिद्ध बहिरंग और अंतरंग पदार्थ अस्तित्व अपने में व्यापक अर्थक्रिया को बतलाता है। वह उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परिणति लक्षण वाली अर्थक्रिया भी अपने में व्यापक क्रम और युगपत् का ज्ञान कराती है। वे क्रम-युगपत् अपने में व्यापक अनेकांत को सिद्ध करते हैं और क्रम-युगपत् से विरुद्ध सर्वथा एकांत का निषेध कर देते हैं, यह अभिप्राय हुआ इसलिए उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परिणाम वाली ही अर्थक्रिया के संभव होने से द्रव्य पर्यायात्मक (वस्तु) प्रमाण का विषय है, यह बात सुस्थित हो गई।
भावार्थ-इस कारिका की टीका में इस बात को स्पष्ट किया कि सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक पक्ष में क्रम या अक्रम दोनों प्रकार से कार्य होना संभव नहीं है इसलिए अनेकांतात्मक द्रव्य पर्यायस्वरूप पदार्थ ही ज्ञान से जाने जाते हैं।
🏠
नाभेदेऽपि विरुध्येत विक्रियाऽविक्रियैव वा॥
अन्वयार्थ : [अभेदे अपि] अभेद के होने पर भी [विक्रिया] विविध प्रकार की क्रिया [न विरुध्येत] विरुद्ध नहीं है, [वा अविक्रिया एव] अथवा अविक्रिया भी विरुद्ध नहीं है॥ [१/२]
अभयचन्द्रसूरि :
भावार्थ-वस्तु में या ज्ञान में एकत्व मानने पर भी परिणमन पाया जाता है। पूर्व आकार का परित्याग और अपने मूल स्वभाव को न छोड़ते हुए उत्तराकार की प्राप्ति इसी को विक्रिया, विकार या परिणाम कहते हैं।
तात्पर्यवृत्ति-वि-विशेष अर्थात् काल के भेद से जो क्रिया होती है वह विक्रिया कहलाती है। वह पूर्वाकार के परिहार, उत्तराकार के ग्रहण और स्थितिलक्षण परिणत रूप है। कथंचित् द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा से विवक्षित अन्वयरूप-अनुगताकार को अभेद कहते हैं। वह विक्रिया इस द्रव्यार्थिक नय से विवक्षित अभेद में भी प्रत्यक्षादि से बाधित नहीं होती है। केवल विक्रिया नहीं किन्तु युगपत् अनेकाकार में व्याप्ति लक्षण अविक्रिया विरुद्ध नहीं है क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु के धर्मों में अभेद है, जो ही मिट्टीरूप एक द्रव्य पिंड आदि आकार से परिणत हुआ है, वही द्रव्य उस पिंडादि आकार को छोड़ते हुए और आगे के घट के आकार को प्राप्त करते हुए प्रतीति में आ रहा है और प्रतीति में आने वाले विषय में विरोध की कल्पना करना शक्य नहीं है, क्योंकि वह विरोध अभाव से सिद्ध होता है।
कारिका में जो ‘अपि’ शब्द है, उससे भेद में भी विक्रिया विरुद्ध नहीं है, यह भी अर्थ ग्रहण किया जाता है। कथंचित् पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद में भी द्रव्य और पर्याय को अर्पित-विवक्षित करने से क्रम और युगपत् विरुद्ध नहीं हो सकते हैं कि जिससे अर्थक्रिया का विरोध हो सके अर्थात् नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्व के आकार का विनाश होते ही उत्तर पर्याय उत्पन्न हो जाती है अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो संकर आदि दोषों का प्रसंग आ जावेगा इसलिए तत्त्व को कथंचित भेदाभेदात्मक , नित्यानित्यात्मक आरै सदसदात्मक स्वीकार करना चाहिए। उसी में अर्थक्रिया संभव है अन्यथा ऐसा नहीं मानने से विरोध आता है।
भावार्थ-कारिका के इस पूर्वार्ध की टीका में आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से उस वस्तु के सभी धर्म गौण हो जाते हैं और तब सभी वस्तुएं एक अभेद रूप ही रहती हैं और पर्यायार्थिकनय से द्रव्य गौण हो जाता है और उसके अनेकों धर्म दिखते हैं अर्थात् द्रव्यार्थिक नय वस्तु के अभेदरूप (द्रव्य) को ग्रहण करता है और पर्यायार्थिक नय वस्तु की भेदरूप (पर्यायों) को ग्रहण करता है। अत: अभेद में भी क्रम से और युगपत् कार्य होने रूप अर्थक्रिया पायी जाती है तथा भेद में भी क्रम और युगपत् से अर्थक्रिया पायी जाती है इसलिए तत्त्व भेदाभेदस्वरूप आदि रूप ही है।
🏠
मिथ्येतरात्मकं दृश्यादृश्यभेदेतरात्मकं॥4॥
चित्तं सदसदात्मैकं तत्त्वं साधयति स्वत:॥
अन्वयार्थ : [मिथ्येतरात्मकं] असत्य सत्यात्मक, [दृश्यादृश्ये] दृश्य और अदृश्यरूप तथा [भेदेतरात्मकं] भेद और अभेदरूप [चित्तं] ज्ञान [स्वत: एकं तत्त्वं] स्वत: एक तत्त्व को [सदसदात्मकं]सत् असत् रूप [साधयति] सिद्ध कर देता है॥४॥ [१/२]
अभयचन्द्रसूरि :
भावार्थ-कोई बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान बहिर्मुखाकार से मिथ्या है किन्तु सच्चेतन आदि आकार से सत्य है तो उन्होंने भी ज्ञान में सत्य-असत्य ऐसे दो स्वभाव स्वीकार कर लिये हैं, दूसरे कहते हैं कि ग्राह्य-ग्रहण करने योग्य आकार से उस ज्ञान में भेद है अर्थात् ज्ञान में ग्राह्य-ग्राहक ऐसी दो अवस्थाएं हैं किन्तु उसमें वह भेद प्रतिभासित होने पर भी प्रतिभासित नहीं होता है क्योंकि भ्रांति हो रही है, तीसरे कहते हैं कि ज्ञान ग्राह्य, ग्राहक संवेदनात्मक होने से भेदाभेदात्मक है तब आचार्य ने कहा भाई! आपके द्वारा मान्य इस प्रकार का ज्ञान तो स्वत: जीवादि तत्त्व को भावाभावात्मक सिद्ध कर देता है।
तात्पर्यवृत्ति-विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध इस प्रकार मानते हैं-
ज्ञान बाह्य वस्तु के आकार के विषयरूप से मिथ्या है और स्वरूप के अवलंबनरूप से अमिथ्यासच्चा है। वही ज्ञान ग्राह्य आकार की अपेक्षा से दृश्य है और स्वरूप की अपेक्षा से अदृश्य है। ग्राह्य ग्राहक आकार की अपेक्षा से भेदरूप है और संवेदन की अपेक्षा से अभेदरूप है।
इस प्रकार मिथ्या-अमिथ्यारूप, दृश्य-अदृश्यरूप और भेद-अभेदरूप ज्ञान अपने स्वरूप से जीव-अजीवादि तत्त्व को सत् असत् रूप सिद्ध कर देता है।
वैशेषिक-द्रव्यादि सत् रूप और प्रागभाव आदि असत् रूप ये भिन्न होने से दो ही तत्त्व सिद्ध हैं।
जैन-प्रमाण की अपेक्षा से तत्त्व अभिन्न-एक है फिर भी द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से सत्-असत् रूप जीवादि तत्त्व प्रसिद्ध है। यह बात प्रमाण के बल से सिद्ध है, चित्रज्ञान के समान। जिस हेतु से चित्रज्ञान एक होते हुए भी मिथ्या-अमिथ्या आदि अनेक रूप अविरुद्ध है। उसी प्रकार से जीवादि भी बिना विरोध के सत्-असत् रूप उपलब्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार वस्तु को न्याय के बल से एकानेकात्मक और नित्यानित्यात्मक स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य परिणति लक्षण अर्थक्रिया का अन्य प्रकार से अभाव है। इस प्रकार विरोध के अभाव से वैयधिकरण्य दोष का भी निराकरण हो ही जाता है क्योंकि एक अधिकरणरूप से सत्-असत् आदि धर्मों की उपलब्धि हो रही है।
शंका-जिस रूप से अस्तित्व है उसी रूप से अस्तित्व-नास्तित्व दोनों का अनेकांत होने से संकर दोष का प्रसंग आता है ?
समाधान-ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्पणा-विवक्षा से भेद है। स्वरूप आदि की अर्पणा से अस्तित्व का ही और पररूपादि की अर्पणा से नास्तित्व का ही विधान है। प्रमाण की अर्पणा से ही उभयात्मक का प्रतिपादन किया जाता है। इसी कथन से अनेकांत में व्यतिरेक दोष का भी निराकरण कर दिया गया है क्योंकि स्वद्रव्यादि की विवक्षा से असत्त्व का प्रतिपादन नहीं किया जाता है।
शंका-वस्तु से सत्त्व-असत्त्व का भेदाभेद है पुन: सत्त्व और असत्त्व का वस्तु से भेदाभेद होने से पुन: उन सत्त्व-असत्त्व का उस वस्तु से अन्य एक भेदाभेद कल्पित करने पर अनवस्था का प्रसंग आता है।
समाधान-बिना समझे ही आपका यह कथन है। देखो! द्रव्यार्थिकनय से वस्तु निश्चित ही अभेदरूप प्रतिपादित की जाती है और द्रव्य को ही अभेद कहते हैं, उस द्रव्य में अन्य कोई द्रव्यांतर रूप नहीं है किन्तु पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से वह वस्तु भेदरूप है। वह भेद पर्याय ही है और उस पर्याय में अन्य पर्यायांतर रूप नहीं है की जिससे अनवस्था आ सके क्योंकि आदेश के वश से (नयों की अपेक्षा से) प्रतिनियत धर्मों की व्यवस्था होती है।
प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु अनेकांतात्मक है उसमें अनवस्थान भी दोष नहीं है, क्योंकि मूल की क्षति-हानि का अभाव है। व्यवहारोपयोगी स्वरूप को ही मूल कहते हैं। वह द्रव्य पर्याय अथवा तदात्मक द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु उस-उस नय अथवा प्रमाण की प्रधानता से सिद्ध हुई व्यवहार के लिए मानी जाती है। वस्तु में अनंत धर्मों के व्यवहार का उपयोग तो हो नहीं सकता कि जिससे उनकी अनवस्था दोष के लिए हो सके अर्थात् उन अनंत धर्मों का अनवस्था दोष के लिए नहीं है। ज्ञाता के शक्ति की विकलता (कमी) होने से वस्तु के धर्मों का अनवस्थान होता है अर्थात् जानने वाले में शक्ति की कमी होने से वस्तु के अनंत धर्मों की व्यवस्था नहीं बन सकती है। यह अव्यवस्था-अनवस्थादोष के लिए नहीं है किन्तु किसी जीव में उन धर्मों की सभी सकलता-परिपूर्णता सुस्थित ही है अर्थात् केवली भगवान उन सभी वस्तु के अनंत-अनंत धर्मों को जानते ही हैं इसलिए उनके ज्ञान में उन धर्मों की व्यवस्था होने से अनवस्था नहीं है क्योंकि वह ज्ञान संपूर्ण प्रमाण और प्रमेय के विस्तार में व्याप्त होकर रहता है अत: अनेकांत में अनवस्था दोष संभव नहीं है।
शंका -अनेकांतात्मक वस्तु में ‘यह इस प्रकार है’ ऐसे निर्णय का अभाव होने से वह संशय अनेकांत रूप है क्योंकि उस संशयरूप ही उसका अस्तित्व सिद्ध है।
समाधान -ऐसा नहीं कहना। नय की विवक्षा करने पर स्वरूपादिचतुष्टय-स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से सभी सत्रूप ही हैं। पररुपादिचतुष्टय-परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से सभी असत् रूप ही हैं। इस प्रकार से निर्णय का सद्भाव है तथा प्रमाण की अर्पणा करने पर सभी अनेकांतात्मक हैं, ऐसा भी निर्णय होता है।
असत् आरोप को संशय कहते हैं और यह अनेकांत असत्रूप नहीं है क्योंकि प्रमाण से सिद्ध है। जिस कारण से वह उभयात्मक को ग्रहण करने वाला संशय होता है उस कारण से वह वस्तु का भाव-स्वभाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि निर्णीत वस्तु ही भावात्मक-सत्रूप होती है इसलिए विरोध आदि दोषों से रहित अनेकांतात्मक वस्तु को उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक होने से इक्यासी भेदों से सहित समझना चाहिए।
भूत, वर्तमान और भविष्यत् काल के भेद से प्रत्येक स्थिति आदि के तीन भेद होने से नव भेद हो जाते हैं। जैसे-ठहरा था, ठहरता है, ठहरेगा। उत्पन हुआ था, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होगा। नष्ट हुआ था, नष्ट होता है और नष्ट होगा, ये नव भेद हुए। तीन काल के परिणामरूप स्थिति आदि नव भेदों में भी प्रत्येक के ठहरा था, ठहरा है, ठहरेगा, इत्यादि नव प्रकार संभव होने से इक्यासी भेद बन जाते हैं, इसलिए यह बात सुस्थित हो गई कि चेतन-अचेतन पदार्थ प्रमाण के विषय हैं और वे द्रव्यपर्यायात्मक हैं।
भावार्थ - आचार्य बौद्ध से कहते हैं कि जैसे आपने चित्रज्ञान को एक कहा है और उसको सत्य असत्यरूप आदि उभयात्मक भी माना है, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। आपके इस चित्रज्ञान के सदृश ही हमारे यहाँ सभी वस्तुएँ अभिन्न एकरूप भी हैं और भावाभावात्मक नित्यानित्यात्मक आदि रूप भी हैं। पुन: कहते हैं कि जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से तो नित्य है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है इसलिए अनेकांत में विरोध दोष नहीं है। एक ही जीवादि आधार में अनेकों सत्-असत्, नित्य - अनित्य आदि धर्म एक साथ रहते हैं अत: वैयधिकरण्य दोष भी नहीं है। जिस रूप से एक वस्तु में सत् धर्म है उसी रूप से सत्-असत् दोनों धर्म आ जावें तो संकर दोष आ जावे सो भी बात नहीं है। स्वरूपादि से ही असत् धर्म माना जावे तो व्यतिकर दोष आता है सो भी नहीं है ऐसे ही अनवस्था और संशय आदि दोष इस अनेकांत में संभव नहीं हैं।
अनत्ंर यह बतलाया है कि जो विरोध आदि दोषों से रहित अनेकांत स्वरुप वस्तु है उसके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप होने से इक्यासी भेद हो जाते हैं। एक उत्पाद में तीन काल की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य घटित करने से ३*३=९ भेद हो जाते हैं पुन: इन नव भेदों में से प्रत्येक में तीन काल की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य घटित करने से ९*९=८१ भेद हो जाते हैं। ऐसे अनेकांतात्मक चेतन-अचेतन पदार्थ ही ज्ञान से जाने जाते हैं और वे द्रव्यपर्यायात्मक ही हैं क्योंकि द्रव्य पर्याय को छोड़कर नहीं रहता है और पर्याय द्रव्य को छोड़कर नहीं रहती है। यहाँ खास बात यह ध्यान रखने की है कि प्रमाणरूप ज्ञान अनेकांतात्मक वस्तु को विषय करता है और नय वस्तु के एक-एक अंश को विषय करते हैं जैसे द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को आरै पर्यायार्थिक नय पर्याय को विषय करते हैं ।
श्लोकार्थ-अकलंक-निर्दोष प्रभा से व्यक्त अखिल प्रमेय को पुन: प्रबुद्ध हुए, शुद्ध दृष्टि वाले मुझ जैसे लोग क्या नहीं देखते हैं ? अर्थात् देखते ही देखते हैं।।१।।
यहाँ पर श्लेषालंकार है। निर्दोष वीतराग की वाणी से व्यक्त अखिल प्रमेय को अथवा श्री भट्टाकलंक देव के द्वारा रचित कारिका से और श्रीप्रभाचंद्राचार्य कृत टीका से स्पष्ट ऐसे सम्पूर्ण प्रमेय को मुझ जैसे प्रबुद्ध हुए सम्यग्दृष्टी लोग क्या नहीं देख सकते हैं ? अर्थात् श्री अभयचंद्रसूरि का ऐसा अभिप्राय है कि जब अकलंकदेव ने इस ग्रन्थ में बढ़िया प्रमेय का वर्णन किया है और पुनः प्रभाचंद्राचार्य ने न्यायाकुमुदचंद्र टीका से उसे आरै भी सरल कर दिया है तो क्या हम जैसे लोग उसके अर्थ को नहीं समझ सकेंगे ? अवश्य ही समझ लेंगे।
इस प्रकार श्री अभयचंद्रसूरि कृत लाघियस्त्र्य की स्याद्वादभूषण संज्ञक तात्पर्यवृत्ति में ‘प्रमाणविषय’ नाम वाला द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ।
🏠
ज्ञानमाद्यं मतिस्संज्ञा चिंता चाभिनिबोधनं॥
प्राङ्नामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्॥1॥
अन्वयार्थ : [ज्ञानं मति:] मतिज्ञान, [संज्ञा चिंता च आभिनिबोधिकं] संज्ञा, चिंता और आभिनिबोधिक ज्ञान [नामयोजनात् प्राङ्] नाम योजना से पहले [आद्यं] आदि के सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं और [शब्दानुयोजनात्] शब्द योजना होने पर [श्रुतं शेषं] श्रुत हैं अत: परोक्ष हैं॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
जो अविशद परोक्ष ज्ञान है वह ‘शेष’ शब्द से कहा गया है। उसके कितने भेद हैं ? स्मृति, संज्ञा, चिंता, आभिनिभोधक और श्रुत ऐसे पाँच भेद होतें हैं । कारिका के ‘च’ शब्द से स्मृति का ग्रहण किया गया है। ये पाँच प्रकार का परोक्ष ज्ञान शब्द प्रयोग के पूर्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार ‘उत्पद्यते’ क्रिया का अध्याहार किया गया है।
केवल इसी प्रकार नहीं किन्तु शब्दोच्चारण से भी होता है। ‘च’ शब्द भिन्न प्रकरण रूप से यहाँ भी संबंधित किया जाता है।
उस ज्ञान की उत्पत्ति के कारण को कहते हैं - मतिसंज्ञक साम्व्यव्हारिक प्रत्यक्ष ज्ञान आद्य-कारण है । उसमें धारणा के बल से उत्पन्न हुई अतीत अर्थ को विषय करने वाली ‘तत्-वह’ इस शब्द की परामर्शिनी स्मृति है।
प्रश्न-स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि गृहीत को ग्रहण करने वाली है ?
उत्तर-नहीं! तत् यह अतीताकार विषय प्रत्यक्ष आदि से गृहीत नहीं है।
प्रश्न-‘असत्’ (अर्थ) में प्रवृत्त होने से स्मृति में प्रमाणता नहीं है ?
उत्तर-यह कथन भी सुन्दर नहीं है। वह स्मृति देश आदि के विशेष से सत् को ही ग्रहण करती है क्योंकि सर्वथा असत् की अनुपपत्ति (अभाव) है इसलिए ‘स्मृति प्रमाण है’ क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के प्रमाणता की अन्यथा अनुपपत्ति है अर्थात् स्मृति को प्रमाण माने बिना प्रत्यभिज्ञान की प्रमाणता सिद्ध नहीं हो सकती है।
प्रश्न-पुन: वह प्रत्यभिज्ञान क्या है?
उत्तर-प्रत्यक्ष और स्मृतिहेतुक जोड़रूप-अनुसंधान ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसी का नाम संज्ञा है। जैसे-यह वही देवदत्त है, गाय के सदृश रोझ है, गाय से विलक्षण महिष है, यह इससे अल्प है, यह बहुत है, यह इससे दूर है, यह इससे पास है, यह वृक्ष है इत्यादि। पूर्वोत्तराकार में व्यापी, ‘तत्’ को विषय करने वाला द्रव्य दर्शन और स्मरण के द्वारा गृहीत नहीं है और इस प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क प्रमाण के नहीं हो सकने से यह प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है। अन्यथा देना-लेना आदि संपूर्ण व्यवहार समाप्त हो जावेगा।
प्रश्न-तर्क क्या है ?
उत्तर-अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा जो व्याप्ति का ज्ञान है, वह तर्वâ है। वह दर्शन-स्मरण के द्वारा अगृहीत प्रत्यभिज्ञान में कारण है। उसे चिंता भी कहते हैं। जैसे-अग्नि के होने पर ही धूम होता है उसके अभाव में नहीं होता है।
भावार्थ-यहाँ पर अविशद लक्षण वाले परोक्ष ज्ञान के पाँच भेद बताये हैं और यह बताया है कि ये पाँचों ज्ञान शब्द प्रयोग के पहले उत्पन्न होते हैं। पुन: कहा है कि केवल इतनी ही बात नहीं है किन्तु ये ज्ञान शब्दोच्चारण से भी उत्पन्न होते हैं। अनंतर सांव्यवहारिक मतिज्ञान को स्मृति में कारण बतलाया है। वह स्मृति प्रत्यभिज्ञान में कारण है और प्रत्यभिज्ञान तर्वâज्ञान में कारण है ऐसा सिद्ध किया है तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्वâ इन तीनों को प्रमाणीक सिद्ध किया है।
🏠
अविकल्पधिया लिंगं न किन्चित्संप्रतीयते।
नानुमानादसिद्धत्वात् प्रमाणांतरमांजसं॥2॥
अन्वयार्थ : [अविकल्पधिया] निर्विकल्प ज्ञान से [विंâचित् लिंगं न प्रतीयते] कुछ हेतु लिंग प्रतीति में नहीं होता है। [अनुमानात् न] अनुमान से भी वह प्रतीत नहीं होता है [असिद्धत्वात्] क्योंकि वह असिद्धरूप है, [आंजसं प्रमाणांतरं] अत: वास्तविक प्रमाणांतर सिद्ध हो जाता है॥२॥
अभयचन्द्रसूरि :
साध्य-साधन के अविनाभाव को लिंग कहते हैं। सौगत द्वारा मान्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष से किन्चित् भी अविनाभाव प्रतीत नहीं होता है और पूर्णरूप से भी नहीं जाना जाता है। जितना कुछ भी धूम है वह सभी अग्नि से उत्पन्न होने वाला ही है अथवा अनग्नि से उत्पन्न होने वाला नहीं होता है। इस तरह वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष इतने विकल्प से रहित है अन्यथा वह सविकल्प हो जावेगा।
प्रश्न-सविकल्प प्रत्यक्ष से अविनाभाव का निर्णय हो जावे, क्या बाधा है ?
उत्तर-यह कथन भी अयुक्त है क्योंकि वह सविकल्पक अपने से संबंधित वर्तमान को विषय करता है। भिन्न-भिन्न देश, काल से व्यवहित (दूरवर्ती) ऐसे साध्य और साधन विशेष में होने वाली व्याप्ति का विकल्प नहीं कर सकता है इसलिए प्रत्यक्ष से अविनाभाव का निर्णय नहीं होता है।
अनुमान से भी नहीं होता है क्योंकि वह असिद्धरूप है। व्याप्ति के ग्रहणपूर्वक ही अनुमान उत्पन्न होता है। यदि आप भिन्न अनुमान से उसमें भी अविनाभाव का निर्णय मानें तब तो अनवस्था आ जाती है।
यदि आप कहें कि प्रथम अनुमान से दूसरे अनुमान में व्याप्ति का निर्णय हो जावेगा तब तो परस्पराश्रय दोष आ जाता है इसलिए अनुमान भी व्याप्ति को ग्रहण करने वाला नहीं है। इसलिए उस व्याप्ति को ग्रहण करने वाला ‘तर्क’ नाम का एक भिन्न प्रमाण और स्वीकार करना चाहिए और उसको पारमार्थिक मानना चाहिए न कि विकल्पात्मक मिथ्यारूप। अन्यथा-यदि आप इसको नहीं मानेंगे तब तो अनुमान की प्रमाणता भी नहीं बन सकेगी।
भावार्थ-पूर्व की कारिका में परोक्ष प्रमाण के भेद करके स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का लक्षण और उनकी सार्थकता बताई है। इस कारिका में तर्वâ प्रमाण का लक्षण और उपयोगिता सिद्ध की है और यहस्पष्ट बताया है कि तर्वâ प्रमाण को माने बिना अनुमान ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि वह व्याप्ति के ज्ञानपूर्वक ही होता है और व्याप्ति को ग्रहण करने वाला तर्वâ ही है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में जैन के सिवाय किसी ने भी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्वâ इन तीनों को पृथक् प्रमाण नहीं माना है और चार्वाक के सिवाय अनुमान को प्रमाण सभी मानते हैं। तर्कादि को प्रमाण माने बिना वह प्रमाण व्यवस्था भी बिगड़ जाती है।
🏠
लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात्।
लिंगिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धय:॥3॥
अन्वयार्थ : [साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षणात्] साध्य के साथ अविनाभाव के निर्णयरूप एक प्रधान लक्षण वाले [लिंगात्] हेतु से [लिंगिधी:] साध्य का ज्ञान [अनुमानं] अनुमान है और [हानादिबुद्धय:] हान-उपादान आदि बुद्धि का होना [तत् फलं] उसका फल है॥३॥
अभयचन्द्रसूरि :
(अनुमान का लक्षण)
लिंग-अविनाभाव संबंध जिसका हो वह लिंगी-साध्य कहलाता है। अनुमान साध्य के साथ अविनाभाव नियमरूप प्रधान लक्षण वाले साधन से उस साध्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी का नाम अनुमान है। वह अनुमान प्रमाण होता है।
इष्ट, अबाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं। अन्य प्रकार से न होने रूप नियम को अविनाभाव कहते हैं। उसके अभि-अभित: भिन्न देशकाल की व्याप्ति के निबोध-निर्णय को अभिनिबोध कहते हैं। वह है एक-प्रधान लक्षण-स्वरूप जिसका उसे अभिनिबोध एक लक्षण कहते हैं। ऐसे साध्य के साथ अविनाभाव नियमरूप प्रधान लक्षण वाले साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वही अनुमान है।
प्रश्न-यह अनुमान तो तर्वâ का फल है, पुन: प्रमाण वैâसे होगा ?
उत्तर-उस अनुमान का फल हानादि बुद्धि है। परिहार को हान कहते हैं और ‘आदि’ शब्द से उपादान-ग्रहण और उपेक्षा को ग्रहण करना है। जो उन हानादि का विकल्प है वही उस अनुमान का फल होता है इसलिए फल का हेतु होने से वह अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष के समान। यहाँ यह अभिप्राय हुआ है।
(अनुमान को प्रमाण न मानने से दोष)
इसको अप्रमाण मानने पर प्रत्यक्ष ज्ञान को भी प्रमाणता नहीं बन सकेगी क्योंकि अगौणत्व आदि हेतु के प्रयोग नहीं बन सकते हैं। कहीं अभ्यस्त विषय में स्वत: प्रमाणता की सिद्धि होने पर भी उसकी (प्रत्यक्ष की) अनभ्यस्त विषय में अनुमान से ही प्रमाणता की सिद्धि होती है। परलोक आदि का निषेध भी अनुपलब्धि हेत से साध्य होने से अनुमान का अभाव करना उचित नहीं है अर्थात् चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है और परलोक आदि का निषेध करता है उसमें यह निषेध अनुपलब्धि हेतु से ही तो करता है।
अथवा पर के चैतन्य के ज्ञान में व्यवहार आदि लिंग से उत्पन्न हुआ अनुमान प्रमाण है इसलिए अनुमान को अप्रमाण नहीं कहना चाहिए क्योंकि युक्ति से विरोध आता है।
(निर्दोष हेतु का कथन)
शंका-पक्ष में धर्म, सपक्ष में तत्त्व और विपक्ष से व्यावृत्ति ये तीन रूप हेतु के लक्षण हैं। पुन: आपके द्वारा मान्य अविनाभाव रूप एक लक्षण उसका नहीं बन सकता है ? अन्यथा असिद्ध, विरुद्ध और अनैकांतिक दोषों का निराकरण नहीं हो सकेगा ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि असाधारणस्वरूप ही लक्षण होता है। निश्चित ही ये तीन रूप असाधारण नहीं हैं। देखिये-‘वह श्याम है क्योंकि उसका पुत्र है’ इत्यादि हेत्वाभास में भी ये तीन रूप देखे जाते हैं। विवाद की कोटि में आये हुए उसके पुत्र में और अन्यत्र श्याम में ‘उस पुत्र होनारूप’ हेतु पाया जाता है और कहीं अश्याम में उसके पुत्रत्व का अभाव है।
बौद्ध-यहाँ पर विपक्ष से व्यावृत्ति होने रूप नियम का अभाव है अत: यह हेतु के लक्षण नहीं हैं।
जैन-ऐसा नहीं कहना। क्योंकि वही अविनाभाव उस हेतु का लक्षण हो जावे, पुन: अन्य ‘अंतर्गडु’ से (व्यर्थ के अंतर्विकल्पों से) क्या प्रयोजन है ? उसी को कहा भी है-
‘अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्’ जहां अन्यथानुपपत्ति-अन्य प्रकार से न होना यह अविनाभाव मौजूद है वहाँ इन तीनों से क्या प्रयोजन है ?
इसी कथन से ‘असत्प्रतिपक्षत्व और अबाधित विषयत्व उस हेतु के लक्षण हैं, इस मान्यता का भी खंडन हो गया है क्योंकि अविनाभाव के अभाव में ये लक्षण साध्य के गमक-बतलाने वाले नहीं हैं।
भावार्थ-बौद्ध ने हेतु के तीन रूप माने हैं-पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्ष व्यावृत्ति। आचार्य ने कहा कि हेतु में यदि ये तीन रूप हैं भी और अविनाभाव नहीं है तो वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकेगा। यदि अविनाभाव है और रूप नहीं है फिर भी वह साध्य को सिद्ध कर देगा। उसी प्रकार नैयायिक हेतु के इन्हीं तीन रूपों में असत्प्रतिपक्षत्व और अबाधित विषयत्व ये दो रूप और जोड़कर हेतु के पाँच रूप मानते हैं किन्तु इनके खंडन में भी यही बात है कि जब इन पाँचों के होने पर भी अविनाभाव के बिना हेतु गमक नहीं होता है और अविनाभाव लक्षण के होने पर ये हों चाहे न हों, हेतु साध्य को सिद्ध कर देता है। तब इन पाँचों के मानने से कोई प्रयोजन नहीं है।
(अविनाभाव के भेद)
उस अविनाभाव के दो भेद हैं-सहभाव और क्रमभाव।
सहचारी रूप और रस तथा व्यापक वृक्षत्व और शिंशिपात्व साध्य-साधन में सह अविनाभाव होता है।
पूर्वचर-उत्तरचररूप रोहिणी के उदय और कृत्तिका के उदय में तथा कार्य-कारणरूप धूम और अग्नि में क्रम अविनाभाव है।
भावार्थ-यहाँ पर आचार्य ने अनुमान का लक्षण बतलाते हुए साध्य एवं साधन का लक्षण भी बतलाया है। जो इष्ट, अबाधित और असिद्ध है वह साध्य है क्योंकि अनिष्ट और बाधित को कोई सिद्ध करना नहीं चाहेगा और असिद्ध विशेषण परवादी की अपेक्षा है क्योंकि स्वयं को तो सिद्ध है किन्तु अन्य को असिद्ध है, तभी तो उसे साध्य की कोटि में रखकर सिद्ध करते हैं। साधन-हेतु का अन्यथानुपपत्ति रूप किया है क्योंकि हेतु में तीनरूप या पाँचरूप होने पर भी यदि अन्य प्रकार से नहीं होने रूप ऐसा साध्य के साथ- अविनाभाव नहीं है तो वह साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता और यदि यह एक लक्षण मौजूद है तो भले ही अन्य रूप नहीं भी होवे तो भी वह हेतु साध्य को सिद्ध कर देता है।
अनंतर अविनाभाव के सहभावी और क्रमभावी ऐसे दो भेद करके उनके उदाहरण दिये हैं। जो व्याप्य और व्यापक में साथ ही रहे वह सहभावी है। जैसे-‘अयं वृक्ष: शिंशिपात्वात्’ यह वृक्ष है क्योंकि सीसम है। जो क्रम से हो, वह क्रमभावी है। जैसे-‘अयं पर्वतोऽग्निमान धूमवत्त्वात्’ यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है। ऐसे ही रूप और रस में सहभाव नियम और पूर्वचर-उत्तरचर में क्रमभाव नियम अविनाभाव पाया जाता है।
🏠
चंद्रादेर्जलचंद्रादिप्रतिपत्तिस्तथाऽनुमा॥4॥
अन्वयार्थ : [तथा] उसी प्रकार [चंद्रादे:] चंद्र आदि से [जलचंद्रादिप्रतिपत्ति:] जल में चंद्र आदि का ज्ञान होना भी [अनुमा] अनुमान ज्ञान है॥४॥
अभयचन्द्रसूरि :
चंद्रादि में आदि शब्द से सूर्य आदि को लेना चाहिए। इन चंद्र, सूर्य आदि कारण हेतु से स्वच्छ जल में चंद्र, सूर्य आदि के प्रतिबिंब का ज्ञान अनुमान ज्ञान है ऐसा स्वीकार करना चाहिए क्योंकि व्यभिचार दोष नहीं है। जैसे कि कार्यहेतु से कारण का ज्ञान होना अनुमान होता है। अविनाभाव गम्य और गमक भाव का कारण है, वह कार्यरूप अथवा अन्यरूप नहीं है क्योंकि अविकल सामथ्र्य वाले कारण कार्य को उत्पन्न करने के प्रति अव्यभिचारी हैं।
वृक्ष में आतप और छाया का व्यभिचार नहीं है अथवा मणि, मंत्र आदि से जिसकी शक्ति रोकी नहीं गई है, ऐसी अग्नि में स्फोट आदि का व्यभिचार नहीं है। अन्यथा-यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। पुन: इस तरह तो अर्थक्रिया के अभाव से वस्तु का अभाव ही हो जायेगा।
भावार्थ-बौद्ध विधि साधक हेतु के दो भेद मानता है-स्वभाव हेतु और कार्य हेतु। यहाँ आचार्य ने जलचंद्र का दृष्टांत देकर कारण हेतु का समर्थन किया है। कुमारिलभट्ट की ऐसी मान्यता है कि जलादि वस्तुओं में जो मुख आदि के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वे प्रतिबिंब नहीं हैं किन्तु हमारी नयनरश्मियां जल से टकरा कर लौटती हुई हमारे ही मुख को देखती हैं, उसे हम भ्रांतिवश जलगत बिंब का देखना समझ लेते हैं। न्यायकुमुदचंद्र में इसका ऊहापोह विशेष किया है और सिद्ध किया है कि वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ सकता है।
🏠
भविष्यत्प्रतिपद्येत शकटं कृत्तिकोदयात्॥
श्व आदित्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति॥5॥
अन्वयार्थ : [कृत्तिकोदयात्] कृत्तिकोदय हेतु से [भविष्यत् शकटं] भविष्य में होने वाला रोहिणी नक्षत्र [प्रतिपद्येत] जाना जाता है। [श्व: आदित्य: उदेता] आगे कल सूर्य उदित होगा [वा] अथवा [ग्रहणं] सूर्य का ग्रहण [भविष्यति] होवेगा [इति] इस प्रकार ज्ञान होता है॥५॥
अभयचन्द्रसूरि :
सूत्र उपस्कार सहित ही होते हैं। उसी का व्याख्यान करते हैं। ‘शकट-रोहिणीनक्षत्र’ धर्मी हैं, ‘मुहूर्त के अंत में होना’ यह साध्य धर्म है, क्यों ? क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है यह हेतु अर्थात् ‘मुहूर्तांते शकटं उदेष्यति कृत्तिकोदयात्१’’ एक मुहूर्त के बाद रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा, क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय हो रहा है, यह पूर्वचर हेतु है।
यहाँ कृत्तिकोदय हेतु रोहिणी के उदय का कार्य अथवा स्वभाव नहीं है। केवल अविनाभाव के बल से अपने उत्तरचर का ज्ञान कराता ही है, इस प्रकार से सभी लोग मानते हैं। उसी प्रकार ‘कल प्रात: आदित्यसूर्य उदित होगा क्योंकि आज सूर्य का उदय हो रहा है’ यह जाना है। अथवा ‘कल ग्रहण-राहु स्पर्श होगा, क्योंकि ज्योतिर्विद के गणित के नियम से जाना जाता है’ ऐसा ज्ञान होता है। इन सभी में व्यभिचार दोष नहीं है। क्रमभावी नियम अविनाभाव कार्य कारण के समान पूर्वचर और उत्तरचर में भी अविरुद्ध है इसलिए पक्षधर्मत्व आदि के बिना भी हेतु अन्यथानुपपत्ति की सामथ्र्य से साध्य का ज्ञान करा देता है।
इस कथन से ‘कार्य, कारण और स्वभाव के भेद से हेतु के तीन ही भेद हैं’ इस सौगत की मान्यता का भी निराकरण कर दिया गया है और इसी से ही ‘कारण, कार्य, संयोगी, समवायी और विरोधी ये पाँच प्रकार के हेतु हैं’ इस नैयायिक मत का भी खंडन हो गया है क्योंकि उपर्युक्त कहे हुए हेतु (पूर्वचर आदि) इनमें अंतर्भूत नहीं हो सकते हैं। मात्रा मात्रिक, कार्य, विरोध, सहचारी, स्वामी, बध्य-घातक और संयोगी के भेद से सात प्रकार का हेतु है। इस प्रकार सांख्य द्वारा कल्पित हेतु की संख्या का नियम भी संभव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।
विशेषार्थ-कारण से कार्य का अनुमान होना। जैसे-जलते हुए र्इंधन को देखकर भस्म होवेगा ऐसा समझना, यह कारण हेतु है।
कार्य से कारण का अनुमान, जैसे-नदी पूर (प्रवाह) के देखने से वृष्टि का ज्ञान होना, यह कार्य हेतु है। संयोगी के देखने से संयोगी का अनुमान, जैसे-धूम के देखने से अग्नि का ज्ञान, यह संयोगी हेतु है। समवायी के देखने से समवायी का अनुमान, जैसे-शब्द से आकाश का अनुमान, यह समवायी हेतु है।
विरोधी के देखने से दूसरे विरोधी का अनुमान जैसे विस्पूâर्जित (उत्तेजित) नकुल के देखने से निकट के सर्प का ज्ञान, यह विरोधी हेतु है। इन पाँचों हेतुओं में पूर्वचर आदि हेतु गर्भित नहीं हो सकते हैं अत: यह संख्या ठीक नहीं है।
इनमें यदि अविनाभाव नियम नहीं है तो ये हेत्वाभास हैं, अव्याप्ति आदि दोषों से दूषित हैं तथा संयोगी और समवायी हेतु तो सिद्ध ही नहीं है।
सांख्य ने सात हेतु माने हैं। उनका लक्षण-(१) मात्रामात्रिकानुमान, जैसे-चक्षु के ज्ञान का अनुमान। (२) कार्य से कारण का अनुमान, जैसे-विद्युत् देखने से कारण का ज्ञान। (३) प्रकृतिविरोधी देखने से भिन्न विरोधी का अनुमान, जैसे-मेघ नहीं बरसेगा क्योंकि उल्टी हवा चल रही है। (४) सहचरानुमान, जैसे-दो चकवे पक्षी में से एक को देखने से दूसरे का ज्ञान। (५) स्व (धन) देखने से स्वामी का अनुमान, जैसे-छत्र विशेष से राजा का अनुमान। (६) बध्य-घातानुमान, जैसे-प्रसन्न नकुल को देखने से ‘इसने सर्प को मारा है’ ऐसा ज्ञान। (७) संयोगी अनुमान, जैसे-समुदाय के मध्य पारिव्राजक होने पर ‘पारिव्राजक कौन है’ ऐसा संशय होने पर त्रिदण्ड के देखने से ‘यह पारिव्राजक है’ ऐसा ज्ञान। इन सात हेतु से अनुमान ज्ञान होता है।
यह मान्यता भी गलत है क्योंकि कृतिकोदयादि हेतुओं का इनमें अंतर्भाव न होने से संख्या ठीक नहीं है तथा यदि अविनाभाव संबंध इनमें नहीं है तो ये अहेतु ही हैं, ऐसा समझना।
🏠
अदृश्यपरचित्तादेरभावं लौकिका विदु:।
तदाकारविकारादेरन्यथानुपपत्तित:॥6॥
अन्वयार्थ : [अदृश्य पर चित्तादे:] नहीं दिखने योग्य ऐसे अन्य के चैतन्य आदि के [अभावं] अभाव को [लौकिका: विदु:] लौकिकजन भी जानते हैं [तदाकारविकारादे:] क्योंकि उसके आकार [उष्णस्पर्श, उच्छ्वास] आदि के विकार [अन्यथानुपपत्तित:] अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
(अदृश्यानुपलब्धि हेतु की सिद्धि)
तात्पर्यवृत्ति-पर-आतुर के जनों के चित्त-चैतन्य आदि शब्द से भूत, ग्रह, व्याधि आदि ग्रहण किये जाते हैं। ये अदृश्य-हम, आपको दिखने योग्य नहीं हैं क्योंकि इनका स्वभाव सूक्ष्म है। ऐसे अदृश्यपने के चैतन्यभूत, ग्रह व्याधि आदि के अभाव को लौकिकजन, आबाल, गोपाल आदि भी जानते हैं पुन: परीक्षकजनों की तो बात ही क्या ? यहाँ ‘अपि’ को ग्रहण ले लेना चाहिए।
कैसे जानते हैं ? उन पर के चैतन्य आदि के कार्यभूत अविनाभावी उष्ण स्पर्शादि लक्षण को ‘आकार’ कहते हैं। उस आकार का विकार-अन्य प्रकार होना आदि शब्द से वचन विशेष आरोग्य श्वासोच्छ्वास आदि होने रूप हेतु से जान लेते हैं। अन्यथा-पर चैतन्यादि के अभाव बिना कैसे जानते हैं ? अर्थात् किसी रोगी आदि के शरीर को निश्चेष्ट, उच्छ्वासरहित और ठंडा देखकर जान लेते हैं कि इसमें चैतन्य का अभाव हो गया है तथा किसी रोगी के वचन विशेष और आरोग्य को देखकर यह भी जान लेते हैं कि इसमें भूत या पिशाच का प्रकोप नहीं है अथवा रोग का अभाव हो गया है। इन बातों को आबाल-गोपाल भी जान लेते हैं फिर परीक्षकजनों की तो बात ही क्या है ?
पर जीवों के भूत व्याधि आदि दिखते तो हैं नहीं क्योंकि वे सूक्ष्म हैं। अदृश्य का अभाव सिद्ध करना भी अशक्य नहीं है अन्यथा संस्कार करने वाले-जलाने वालों की पातकी कहना पड़ेगा तथा चैतन्य आदि होने पर भी विश्वास नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार उष्ण, स्पर्श आदि आकार की उपलब्धि होने से पर के चैतन्य आदि का भाव (होना) सिद्ध किया जाता है। उसी प्रकार उष्ण, स्पर्शादि आकार विशेष की उपलब्धि न होने से पर के चैतन्य आदि का अभाव भी सिद्ध किया जाता है।
शंका-कार्य की उपलब्धि से कारण का अस्तित्व सिद्ध करना सुघटित है किन्तु कार्य की उपलब्धि न होने से कारण का अभाव सिद्ध करना शक्य नहीं है, क्योंकि कारण का कार्य के साथ अविनाभाव नहीं है।
समाधान-नहीं, इस प्रकार के निर्बंध का अभाव है। कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ जो कारण है, उसका कार्य के साथ अविनाभाव सुघटित है। समर्थ कारण के होने पर कार्य अवश्य ही होता है। अन्यथायदि ऐसा न मानोगे तो कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार तो सभी में अर्थक्रिया को करने का अभाव होने से शून्यता का प्रसंग आ जावेगा।
(हेतु के भेद-प्रभेद)
इसलिए उपलब्धि और अनुपलब्धि के भेद से हेतु के दो भेद हैं। उनमें विधि को साध्य करने में उपलब्धि हेतु के छह भेद हैं और प्रतिषेध को साध्य करने में भी छह भेद हैं।
अनुपलब्धि के प्रतिषेध को सिद्ध करने में सात भेद हैं और विधि के सिद्ध करने में तीन भेद सुव्यवस्थित हैं। उन सभी हेतुओं में अविनाभाव नियम निश्चयरूप एक लक्षण के बल से गमकत्व-सिद्ध है अर्थात् ये सभी हेतु अविनाभाव नियमरूप निश्चित एक लक्षण के बल से अपने-अपने साध्य को सिद्ध करने वाले हैं।
शंका-अदृश्यानुपलब्धि हेतु से अभाव को सिद्ध करने में संशय ही बना रहेगा ?
समाधान-नहीं, इस प्रकार से तो उपलब्धि हेतु से अपने चैतन्य के अभाव में भी संशय का प्रसंग आ जावेगा।
दूसरी बात यह है कि बहिरंग और अंतरंग निरंश तत्त्व प्रमाण की पदवी पर आरोहण नहीं कर सकता है। क्रम और अक्रम से अनेक स्वभाव वाले बहिरंग और अंतरंगरूप चेतन-अचेतन तत्त्व में प्रमाण की प्रवृत्ति होती है इसलिए प्रमाण से बाधित विषय वाला होने से बौद्ध के द्वारा परिकल्पित सभी सत्त्व आदि हेतु अविंâचित्कर अभाव विरुद्ध ही हो जाते हैं। इस तरह उनके मन में अनुमान को प्रमाणता कैसे हो सकेगी ?
विशेषार्थ-किसी भी वस्तु के अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। उसके दो भेद हैं-दृश्यानुपलब्धि और अदृश्यानुपलब्धि। दिखने योग्य पदार्थ के अभाव को दृश्यानुपलब्धि और नहीं दिखने योग्य पदार्थ के अभाव को अदृश्यानुपलब्धि कहते हैं। जैसे-कमरे में पुस्तक थी, किसी ने वहाँ से हटा दी तब उस कमरे में पुस्तक की दृश्यानुपलब्धि है तथा कमरे में भूत था, चला गया, उस भूत के अभाव को या पर की आत्मा, ज्ञान, व्याधि आदि भी दिखने योग्य नहीं है, उनके अभाव को अदृश्यानुपलब्धि कहते हैं।
यहाँ बौद्ध दृश्यानुपलब्धि को ही मानता है उसके एकांत का निराकरण करने के लिए श्री भट्टाकलंक देव ने कहा कि अन्य के चैतन्य आदि अदृश्य हैं, उनका अभाव लौकिक जन भी मानते हैं। उनके श्वांस आदि को नहीं देखकर कह देते हैं कि इनमें से जीव निकल गया है अन्यथा उसको जलाने वाले को पापी, मनुष्यघाती कहना पड़ेगा परन्तु ऐसा तो है नहीं, इसलिए अदृश्यानुपलब्धि भी सिद्ध है।
पुन: किसी ने कहा कि नदीपूर आदि कार्य देखकर मेघ वर्षा आदि कारण को जानना ठीक है किन्तु किसी कार्य के अभाव में कारण को जानना असंभव है। तब श्री वृत्तिकार आचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है, देखो! अश्रद्धान रूप कार्य के अभाव में मिथ्यात्व रूप कारण का अभाव जाना जाता है तथा मुख का कड़ुवापन आदि के अभाव में पित्त ज्वर आदि के अभाव को जाना जाता है। बस! हेतु में साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित होना चाहिए।
अनंतर हेतु के बाईस भेद किये हैं -
परीक्षामुख ग्रन्थ में श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने इनका स्पष्टीकरण किया है
हेतु के उपलब्धि और अनुपलब्धि से दो भेद हैं। उपलब्धि के दो भेद हैं-अविरुद्धोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि। अनुपलब्धि के भी दो भेद हैं-अविरुद्धानुपलब्धि और विरुद्धानुपलब्धि।
अविरुद्धोपलब्धि के व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर के भेद से छह भेद हैं-
(१) शब्द परिणामी होता है क्योंकि वह किया हुआ है, यह अविरुद्धव्याप्योपलब्धि का उदाहरण है।
(२) इस प्राणी में बुद्धि है क्योंकि बुद्धि के कार्य, वचन आदि पाये जाते हैं, यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है।
(३) यहाँ छाया है क्योंकि छत्र मौजूद हैं, यह अविरुद्ध कारणोपलब्धि है।
(४) एक मुहूर्त के बाद रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है, यह पूर्व चरोपलब्धि है।
(५) एक मुहूर्त के पहले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है, यह उत्तर चरोपलब्धि है।
(६) इस बिजौरे में रूप है क्योंकि रस पाया जाता है यह सद्चरोपलब्धि का उदाहरण है।
विरुद्धोपलब्धि के भी ऐसे ही छह भेद हैं-
(१) यहाँ शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि उससे विरुद्ध अग्नि की व्याप्य उष्णता मौजूद है, यह विरुद्ध व्याप्योपलब्धि का उदाहरण है।
(२) यहाँ शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि उससे विरुद्ध अग्नि का कार्य धूम मौजूद है यह विरुद्ध कार्योपलब्धि है।
(३) इस जीव में सुख नहीं है क्योंकि उससे विरुद्ध दुख का शल्य मौजूद है, यह विरुद्ध कारणोपलब्धि है।
(४) एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा क्योंकि उसके विरुद्ध अश्विनी नक्षत्र के पूर्वचर रेवती नक्षत्र का उदय हो रहा है, यह विरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि है।
(५) एक मुहूर्त के पहले भरणी का उदय नहीं हुआ है क्योंकि अभी पुण्य का उदय हो रहा है, यह विरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है।
(६) इस दीवाल में उस तरफ के भाग का अभाव नहीं है क्योंकि इस तरफ का भाग दिख रहा है, यह विरुद्ध सहचरोपलब्धि का उदाहरण है।
अविरुद्धानुपलब्धि के प्रतिषेध में सात भेद हैं-स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर।
(१) इस भूतल पर घट नहीं है क्योंकि वह दिखता नहीं है, यह अविरुद्ध स्वभावानुपलब्धि है।
(२) यहाँ सीसम नहीं है क्योंकि उसके व्यापक वृक्ष का अभाव है, यह अविरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है।
(३) यहाँ बिना सामथ्र्य रुकी अग्नि नहीं है क्योंकि धूम नहीं पाया जाता है, यह अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि है।
(४) यहाँ धूम नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं है, यह अविरुद्ध कारणानुपलब्धि है।
(५) एक मुहूर्त बाद रोहिणी का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय नहीं हुआ है, यह अविरुद्ध पूर्वचरानुपलब्धि है
(६) एक मुहूर्त पहले भरणी का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी कृतिका का उदय नहीं हुआ है, यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि हेतु है।
(७) इस तराजू में ऊँचापन नहीं है क्योंकि नीचेपन का अभाव है, यह अविरुद्ध सहचरोपलब्धि हेतु है।
विरुद्धानुपलब्धि के विधि में तीन भेद हैं-कार्य, कारण और स्वभाव।
(१) इस प्राणी में कोई रोग है क्योंकि नीरोग चेष्टा नहीं पायी जाती है, यह विरुद्ध कार्यानुपलब्धि है।
(२) इस प्राणी में दुख है क्योंकि इष्ट संयोग का अभाव है, यह विरुद्ध कारणानुपलब्धि है।
(३) वस्तु अनेकांतात्मक है क्योंकि उसमें नित्य आदि एकांत स्वरूप का अभाव है, यह विरुद्ध स्वभावानुपलब्धि हेतु का उदाहरण है।
इस प्रकार से हेतु के बाईस भेदों का वर्णन करके आचार्य ने कहा है कि गुरु परम्परा से और भी जो हेतु संभव हो सकते हों, उनका पूर्वोक्त साधनों में ही अंतर्भाव करना चाहिए।
🏠
वीक्ष्याणुपारिमांडल्यक्षणभंगाद्यवीक्षणं॥
स्वसंविद्विषयाकारविवेकानुपलंभवत्॥7॥।
अन्वयार्थ : [वीक्ष्याणुपारिमांडल्य क्षण भंगाद्यवीक्षणं] स्थूल के अणुओं की गोलाई और क्षण-क्षण में नाश होना आदि दिखते नहीं हैं [स्वसंविद्विषयाकार विवेकानुपलम्भवत्] जैसे स्वसंवेदन के विषयाकार के भेद की उपलब्धि नहीं होती है॥७॥
अभयचन्द्रसूरि :
उपलब्धि लक्षण प्राप्त स्थूल को ‘वीक्ष्य’ कहते हैं। उसके सूक्ष्म अवयवों को ‘अणु’ कहते हैं। उन अणुओं का वर्तुलाकार परिमंडल कहलाता है। ये अणु परस्पर में भिन्न-भिन्न रहते हैं। क्षण-क्षण में भंग-नाश होना क्षण भंग है अर्थात् एक समय में नष्ट हो जाना। क्षणभंगादि में आदि शब्द से कार्य- कारण की सामथ्र्य आदि को लेना चाहिए। इनका अवीक्षण-प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होना अर्थात् निश्चित ही सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष से वेक्षणभंग आदि नहीं दिखते हैं किन्तु उसके द्वारा स्थिर स्थूल साधारण आकार ही देखा जाता है। योगी प्रत्यक्ष ही उनको (क्षणवर्ती पर्यायों को) देखनें में समर्थ होता है इसलिए वहाँ-उस सूक्ष्म परमाणु आदि के आकार को और क्षणिक आदि को जानने में अनुमान ही जागता-प्रगट होता है। वही उनके निर्णय की सामथ्र्य रखता है।
सत्त्वात्, प्रमेयत्वात्, अर्थक्रियाकारित्वात् इत्यादि हेतुओं में कथंचित् अनेक, अनित्यादि धर्म व्याप्य होने से उनका अविनाभाव प्रसिद्ध है। इस प्रकृत अर्थ में दृष्टांत देते हैं-जैसे स्वसंवेदन के विषयाकार- घटादि आकार से विवेक-व्यावृत्ति की उपलब्धि नहीं होती है अर्थात् प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है। जिस प्रकार आप सौगत के यहाँ ज्ञान के स्वरूप प्रतिभासन में बाह्य अर्थाकार का अभाव, विद्यमान होने से भी प्रतिभासित नहीं होता है क्योंकि उस ज्ञान में उस प्रकार के सामथ्र्य का अभाव है। उसी प्रकार बहिरंग- अंतरंग, अणु के वर्तुलाकार आदि प्रत्यक्ष से प्रतिभासित नहीं होते हैं, क्योंकि वैसी शक्ति का अभाव है इसलिए अनेकांत मत में अनुमान सफल है, यह अर्थ हुआ।
भावार्थ-‘अदृश्यपरचित्तादे’ इत्यादि कारिका की टीका में श्री अभयचंद्रसूरि ने अंत में कहा कि बौद्ध के यहाँ प्रमाण से बाधित विषय के होने से ‘सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्’ इत्यादि अनुमानों में हेतु अकिंचित्कर या विरुद्ध ही हैं इसलिए उनके मत में अनुमान प्रमाण नहीं बनता है। तब उसने भी कह दिया कि आप स्याद्वादियों के यहाँ भी अनेकांतात्मक तत्त्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है पुन: आपके यहाँ भी अनुमान प्रमाण मानना व्यर्थ ही रहा।
तब आचार्यदेव ने उत्तर दिया कि आपके द्वारा मान्य अणु आदि के आकार और क्षण-क्षण का विनाश भी तो प्रत्यक्ष से ही नहीं दिख रहा है। उसको जानने के लिए अनुमान की आवश्यकता है ही है।
अर्थात् बौद्ध का कहना है कि प्रत्येक दिखने योग्य स्थिर स्थूल घट आदि वस्तु में जितने भी परमाणु हैं वे प्रत्येक वर्तुलाकार हैं और परस्पर में भिन्न-भिन्न हैं तथा प्रत्येक पदार्थ एक क्षण ठहरता है। अनंतर क्षण में ही नष्ट हो जाता है तथा कार्य और कारण की शक्ति भी दिखती नहीं है।
आचार्यों का कहना है कि इन अदृश्य वस्तुओं के जानने के लिए अनुमान प्रमाण मानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान से उन सूक्ष्मादि का प्रतिभासन नहीं होता है प्रत्युत् स्थिर, स्थूल आदि का और अनेक क्षण रहने वाली वस्तु का ही ज्ञान होता है।
🏠
अनंशं बहिरंतश्च प्रत्यक्षं तदभासनात्।
कस्तत्स्वभावो हेतु: स्यात्किं तत्कार्यं यतोऽनुमा॥8॥
अन्वयार्थ : [बहिरंत: च अनंशं] बहिरंग और अंतरंग निरंश तत्त्व [अप्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष नहीं है [तत्अभासनात्] क्योंकि वह प्रतिभासित नहीं होता है पुन: [तत्स्वभाव: क: हेतु:] उस अनंश का कौन स्वभाव हेतु [स्यात्] होगा [तत्कार्यं किं] और उसका क्या कार्य होगा [यत: अनुमा] कि जिससे अनुमान [स्यात्] हो सके अर्थात् नहीं हो सकता है॥८॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-सौगत के द्वारा परिकल्पित जो बाह्य-अचेतन और अंतरंग-चेतन वस्तुएं हैं जो कि निरंश हैं वे प्रत्यक्ष के ज्ञान का विषय नहीं हैं। यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के विभाग को अंश कहते हैं उनसे निष्क्रांत-रहित वस्तु निरंश कहलाती है।
प्रश्न-ये निरंश चेतन-अचेतन आदि क्यों प्रमाण के विषय नहीं हैं ?
उत्तर-क्योंकि वह निरंशपना प्रतिभासित नहीं होता है अर्थात् अनुभव में नहीं आता है। द्रव्य, क्षेत्र आदि के विभाग से रहित चेतन अथवा अचेतन तत्त्व प्रत्यक्षज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। उस ज्ञान में नित्यानित्यादि अनेक अंशों में व्यापी होने रूप वस्तु की प्रतीति होती है इसलिए प्रत्यक्ष से असिद्ध उस निरंश वस्तु का कौन स्वभाव-धर्म हेतु हो सकेगा अर्थात् कोई भी स्वभाव हेतु नहीं होगा क्योंकि जो प्रमाण से असिद्ध है वह अहेतु है-हेतु नहीं हो सकता है।
और उस निरंश का क्या कार्य है जो कि हेतु हो सके क्योंकि सर्वथा निरंश और अपरिणामी में काय कारण भाव का अभाव है। ‘प्यतोऽनुमा’-कि जिससे अनुमान हो सके यह आक्षेप वचन है अर्थात् किसी प्रकार से भी अनुमान नहीं बन सकता है इसलिए सौगत के मत में अनुमान, प्रमाणता को नहीं प्राप्त होता है। अनुपपत्ति होने से अर्थात् इनके यहाँ अनुमान प्रमाण घटित नहीं होता है।
भावार्थ-बौद्ध ने चेतन-अचेतन सभी वस्तुओं को द्रव्यक्षेत्रादि अंश भागों से रहित निरंश माना है अतएव आचार्य कहते हैं कि उस निरंश का स्वभाव तो क्या है और कार्य भी क्या है ? उसमें कुछ स्वभाव मानें तो अंश कल्पना हो जायेगी और उसका कुछ कार्य मानें तो कार्य-कारण भाव से भी अंशकल्पना हो जाती है और जब उसका स्वभाव तथा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तब स्वभाव हेतु कार्य हेतु के बिना अनुमान का होना सुतरां असंभव है जैसे कि बंध्या के पुत्र के बिना उसको आकाश के पूâलों की माला पहनाना असंभव है।
🏠
धीर्विकल्पाविकल्पात्मा बहिरंतश्च किं पुन:॥
निश्चयात्मा स्वत: सिद्ध्यत्परतोऽप्यनवस्थिते:॥9॥
अन्वयार्थ : [बहि: अंत: च] बहिरंग और अंतरंग पदार्थ में [विकल्पाविकल्पात्मा] विकल्परूप और अविकल्पस्वरूप [निश्चयात्मा धी:] अनुमान ज्ञान [किं पुन: स्वत: सिद्ध्येत्] क्या पुन: स्वत: सिद्ध हो सकता है [परतोऽपि] पर से भी [अनवस्थिते:] क्योंकि अनवस्था आती है॥९॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-अनुमान ज्ञान को निश्चयात्मा कहते हैं। विकल्प को व्यवसाय निश्चय और अविकल्प को अव्यवसाय कहते हैं। बाह्य-घट पटादि के विषय में विकल्पात्मक और अंत:स्वरूप में निर्विकल्पात्मक अनुमान ज्ञान पुन: वैâसे सिद्ध हो सकता है अर्थात् सिद्ध नहीं हो सकता है।
प्रश्न-कैसे सिद्ध नहीं होता है ?
उत्तर-स्वत: अर्थात् स्वसंवेदन से सिद्ध नहीं होता है ? क्योंकि वह स्वसंवेदन निर्विकल्प होने से विकल्प को विषय नहीं करता है। ‘‘सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्’’ अर्थात् सभी ज्ञान क्षणों का स्वरूप संवेदन ही स्वसंवेदन है ऐसा आप बौद्धों का वचन है। केवल स्वत: ही नहीं किंतु पर से भी कैसे सिद्ध होगा ? अर्थात् पर-विकल्पांतर से भी सिद्ध नहीं होता है।
प्रश्न-पर से क्यों नहीं सिद्ध होता है ?
उत्तर-अनवस्था आ जाने से सिद्ध नहीं होता है अर्थात् विकल्पात्मक अनुमान को सिद्ध करने के लिए एक दूसरा विकल्प ज्ञान लाये, पुन: उसकी सिद्धि के लिए तीसरा विकल्पज्ञान लाना पड़ेगा क्योंकि वह भी विकल्प को विषय न करने से स्वत: सिद्ध नहीं है और उस तीसरे को सिद्ध करने के लिए पुन: एक विकल्पांतर की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से बहुत दूर जाकर कहीं पर भी उपरति न होने से अनवस्था आ जाती है इसलिए अनुमान की सिद्धि न होने से बौद्ध के द्वारा कल्पित प्रमाण की संख्या (दो) का नियम भी कैसे घटित हो सकेगा, अर्थात् नहीं हो सकेगा यह भाव हुआ।
भावार्थ-बौद्धों का कहना है कि अनुमान ज्ञान निश्चयात्मक है और वह बाह्य पदार्थों का निश्चय करता है किन्तु अपने स्वरूप में निर्विकल्प है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ऐसा अनुमान ज्ञान स्वत: तो सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि स्वसंवेदन में तो वह निर्विकल्प ही रहा तथा पर से सिद्धि मानने से तो उस पर की सिद्धि पर से पुन: पर की सिद्धि पर से मानते चलिए, कहीं भी विराम न होने से अनवस्था आ जाती है अत: आप बौद्धों के यहाँ अनुमान ज्ञान के सिद्ध न होने से आपके द्वारा मान्य प्रमाण की दो संख्या का नियम समाप्त हो जाता है।
🏠
उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्र्यात्साध्यसाधनं॥
तद्वैधम्र्यात्प्रमाणं विंâ स्यात्संज्ञिप्रतिपादनं॥10॥
अन्वयार्थ : [प्रसिद्धार्थ साधम्र्यात् साध्यसाधनं] प्रसिद्ध अर्थ की सदृशता से साध्य को सिद्ध करने वाला [उपमानं] उपमान है। पुन: [वैधम्र्यात्] विसदृशता से [तत् किं प्रमाणं स्यात्] वह क्या प्रमाण होगा ? [संज्ञिप्रतिपादनं] तथा संज्ञी-वाच्य का प्रतिपादन करने वाला ज्ञान संज्ञा-संज्ञी का संबंध ज्ञान [तत् किं प्रमाणं स्यात्] वह क्या प्रमाण होगा ?॥१०॥
अभयचन्द्रसूरि :
यहाँ पर ‘यत्’ इस पद का अध्याहार करना चाहिए। प्रसिद्ध प्रमाण से निश्चित गोरूप अर्थ के सादृश्य धर्म से उत्पन्न हुआ साध्य-ज्ञेयरूप उस सादृश्य धर्म से विशिष्ट गवयलक्षण को सिद्ध करता है अर्थात् ‘गाय के सदृश गवय है’ इस प्रकार का जो ज्ञान है वह उपमान नाम का भिन्न प्रमाण है। यदि आप नैयायिक इस तरह उपमान को भिन्न प्रमाण स्वीकार करते हैं तब तो आपको उस गाय के रूप से वैधम्र्य से प्रसिद्ध हुई अर्थ की विसदृशता से उत्पन्न हुआ और साध्य को सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है वह ‘गाय से विलक्षण महिष है’ इस प्रकार का ज्ञान कौन सा प्रमाण है ? अर्थात् उसका क्या नाम है ? इसको भी आप उपमान ही नहीं कह सकते क्योंकि उसके लक्षण का अभाव है। इसे आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह भिन्न विषय वाला है और भिन्न सामग्री से उत्पन्न हुआ है।
उसी प्रकार से संज्ञी-वाच्य प्रतिपादन करना, विवक्षित संज्ञा के विषय रूप से संकलन करना; जैसे-‘यह वृक्ष है’। ऐसा ज्ञान, वह भी किस नाम वाला प्रमाण होगा ? अर्थात् उपमान प्रमाण को पृथक् मानने से तो आपको अनेकों प्रमाण मानने पड़ेंगे। संज्ञा और संज्ञी (नाम-नाम वाले) के संबंध का ज्ञान अप्रमाण भी नहीं है अन्यथा आगम प्रमाण का लोप हो जावेगा और उपमान भी अप्रमाण हो जावेगा।
भावार्थ-नैयायिक उपमान को एक पृथक् प्रमाण मानता है किन्तु आचार्यों का कहना है कि इस तरह तो विसदृश धर्म आदि के निमित्त से हुए ज्ञानों को आप भिन्न -भिन्न प्रमाण मानते चलिए, यह दूषण दिया है। वास्तव में हम जैनों के यहाँ तो इस उपमान आदि प्रमाणों को प्रत्यभिज्ञान प्रमाण में गर्भित किया है और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान आदि नाम दिये हैं इसलिए हमारे यहाँ कोई दूषण नहीं आता है।
🏠
प्रत्यक्षार्थांतरापेक्षा संबंधप्रतिपद्यत:॥
तत्प्रमाणं न चेत्सर्वमुपमानं कुतस्तथा॥11॥
अन्वयार्थ : [यत:] जिस ज्ञान से [प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा] प्रत्यक्ष से भिन्न अर्थ की अपेक्षा रखने वाला [संबंध प्रतिपत्] वाच्य-वाचक भावरूप संबंध का ज्ञान होता है [चेत् तत् प्रमाणं न] यदि वह ज्ञान प्रमाण नहीं है, तो [तथा सर्वं उपमानं कुत:] उसी प्रकार से सभी उपमान प्रमाण कैसे होंगे ?॥११॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष अर्थांतर-उससे भिन्न अर्थ की अपेक्षा करने वाला वाच्य- वाचक भावरूप संबंध का ज्ञान होता है अर्थात् प्रकृत शब्द लक्षण से भिन्न अर्थ अर्थांतर है, ‘वृक्षादि’ प्रत्यक्ष अर्थांतर हैं, उनकी अपेक्षा जिस ज्ञान को है, वह प्रत्यक्ष अर्थांतर की अपेक्षा वाला ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान यदि प्रमाण न होवे, तब तो सभी नैयायिक, मीमांसक आदि के द्वारा कल्पित सभी उपमान कैसे प्रमाण हो सकते हैं ? क्योंकि दोनों जगह कोई अंतर नहीं है। सादृश्य संबंधी ज्ञान प्रमाण है किन्तु वाच्य वाचक संबंधी ज्ञान प्रमाण नहीं है, इस प्रकार का अंतर तो है नहीं। इसलिए संज्ञा और संज्ञी का संकलन-जोड़ रूप ज्ञान भी एक भिन्न प्रमाण हो ही जायेगा इसलिए आप लोगों के द्वारा मान्य प्रमाण की संख्या का नियम कैसे बनेगा ?
🏠
इदमल्पं महद् दूरमासन्नं प्रांशु नेति वा॥
व्यपेक्षात: समक्षेऽर्थे विकल्प: साधनांतरं॥12॥
अन्वयार्थ : [इदं अल्पं महत्] यह अल्प है, बहुत है, [दूरं आसन्नं] दूर है, निकट है, [प्रांशुं वा न ति] यह दीर्घ है अथवा दीर्घ नहीं है-ह्रस्व है, इस प्रकार [व्यपेक्षात:] अपेक्षा से [समक्षे अर्थे] प्रत्यक्ष अर्थ में [विकल्प:] जो विकल्प हैं [साधनांतरं] वे प्रमाणांतर हैं॥१२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-यह इससे अल्प है, यह इससे महान् है, यह इससे दूर है, यह इससे आसन्न है, यह इससे दीर्घ है, यह इससे दीर्घ नहीं है। यहाँ कारिका में ‘वा’ शब्द परस्पर समुच्चय अर्थ में है। किस विषय में ? प्रत्यक्ष पदार्थ में व्यपेक्षा से-विरुद्ध-प्रतिपक्ष की अपेक्षा से कथंचित अजहद्वृत्ति-कथंचित् अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए जो विकल्प-निश्चय होता है, वह भिन्न प्रमाण है।
इस प्रकार अल्प महत्व आदि का जोड़रूप ज्ञान पर के द्वारा मान्य प्रमाण की संख्या के नियम को विघटित कर देता है।
[शंका-आप स्याद्वादियों के यहाँ भी इस प्रकार प्रमाण की संख्या का विधान वैâसे नहीं होता है ?
समाधान-हमारे यहाँ तो परोक्ष के भेदरूप प्रत्यभिज्ञान में सादृश्य संकलन आदि सभी का अंतर्भाव हो जाता है।
शंका-अर्थापत्ति को प्रमाणांतर मानना ही चाहिए , क्योंकि उसका कहीं पर भी अंतर्भाव नहीं हो सकता है ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि अनुमान में उसका अंतर्भाव हो जाता है। नदीपूर आदि से अनंतर वृष्टि आदि के अविनाभावी रूप से लिंगत्व है और लिंग से उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुमान है।
शंका-पक्षधर्मत्व का अभाव होने से उसको लिंगपना नहीं है ?
समाधान-नहीं, पक्ष में जिसका धर्म नहीं है ऐसा अपक्ष धर्म वाला भी हेतु समर्पित है। गम्य गमक भाव निमित्तक ही अविनाभाव है, अन्य नहीं है और वह अविनाभाव यहाँ भी है इसलिए अर्थापत्ति अनुमान ही है। इस कथन से अभाव भी एक भिन्न प्रमाण है’ ऐसा मानने वालों का भी खंडन कर दिया गया है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण में ही भावाभावात्मक वस्तु को विषय करने से वैसा व्यवहार होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाव को ग्रहण करने वाला प्रमाण अथवा अभाव को विषय करने वाला प्रमाण कोई हो क्योंकि उससे अर्थक्रिया नहीं हो सकती है।
यदि अभाव स्वतंत्र होता तब तो उसको ग्रहण करने वाला एक भिन्न प्रमाण कल्पित करना ही चाहिए। उसमें ‘घट नहीं है’ इस प्रकार भाव के आश्रित की उपलब्धि होती है। भाव को ग्रहण करने वाले के द्वारा ही उसका ग्रहण होता है।
दूसरी बात यह है कि भावग्राहक ज्ञान से अभावग्राहक ज्ञान अन्य ही है। ऐसा मानने पर तो सामान्य ग्राहक ज्ञान से विशेष ग्राहक ज्ञान और नित्यत्वग्राहक ज्ञान से अनित्यत्वग्राहक ज्ञान भी भिन्न-भिन्न प्रमाण ही हो जावेंगे और इस प्रकार से तो कहीं पर भी अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिए ‘अभाव’ नाम का कोई भिन्न प्रमाण नहीं है क्योंकि उसके विषय का अभाव है, केशों में मच्छर ज्ञान के समान। इसलिए यहाँ यह सुस्थित हो गया कि ‘स्मृति आदि ज्ञान परोक्ष हैं क्योंकि वे अविशद ज्ञान हैं और इसी परोक्ष में ही सकल अस्पष्ट ज्ञानों का अंतर्भाव हो जाता है।
भावार्थ-यह छोटा है, यह बड़ा है। इन दोनों ज्ञानों में एक-दूसरे की अपेक्षा है। जैसे-आंवले की अपेक्षा बेल बड़ा है और बेल की अपेक्षा आंवला छोटा है, यहाँ अपेक्षा से होने वाला ज्ञान भी संकलनजोड़ रूप है इसे भी एक अलग प्रमाण कहना चाहिए। वैसे ही दूर-निकट के जोड़रूप, ह्रस्व-दीर्घ के जोड़रूप, आदि अनेकों भिन्न-भिन्न प्रमाण मानने चाहिए और उनके नाम बताने चाहिए। तब आप नैयायिक, मीमांसक आदि की मान्य संख्या खत्म हो जाती है तब उन लोगों ने कहा कि यह दोष तो आप जैनों को भी संभव है, किन्तु आचार्य ने कहा कि हमारे यहाँ परोक्ष के अंतर्गत एक प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है जिसमें ये सभी भेद सम्मिलित हो जाते हैं।
मीमांसक ने कहा कि ‘अर्थापत्ति’ को तो अलग प्रमाण मानना ही पड़ेगा। अर्थापत्ति-इसके होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, जैसे-देवदत्त मोटा है किन्तु दिवस में नहीं खाता है, मतलब रात्रि में खाता है, इसे अर्थापत्ति कहते हैं। यह अनुमान में अंतर्भूत है क्योंकि इस अर्थापत्ति के बिना अनुमान होता ही नहीं है।
पुन: मीमांसक ने अभाव को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहा तब आचार्य ने कहा कि यदि भाव के विपक्षी अभाव का ग्राहक एक अभाव प्रमाण है तो नित्य के विपक्षी अनित्य आदि को ग्राहक प्रमाण भी मानना पड़ेगा। किन्तु ऐसा तो है नहीं अत: प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही भाव और अभावरूप सभी वस्तुओें को ग्रहण करने वाले हैं इसलिए जितने भी अस्पष्ट ज्ञान हैं वे सभी परोक्ष प्रमाण में शामिल हैं।
श्लोकार्थ-श्री भट्टाकलंकदेवरूपी चंद्रमा से प्रगट हुई किरणों के द्वारा विशदेतर-परोक्ष प्रमाण का स्पर्श किया गया है-स्पष्ट हुआ है। इस प्रमाण के भेद में श्री अभयचंद्रसूरि की वाणी प्रतिभासित करने वाली क्यों नहीं होगी ? अर्थात् श्री अकलंकदेव ने परोक्ष प्रमाण का स्पष्टरूप से वर्णन किया है, मेरे द्वारा बनाई गई तात्पर्यवृत्ति से आप सभी लोगों को उस प्रमाण का प्रतिभास-ज्ञान हो जावेगा।।१।।
इस प्रकार श्री अभयचंद्रसूरि कृत लघीयध्Eाय की स्याद्वादभूषण नामक तात्पर्यवृत्ति में परोक्ष प्रमाण का वर्णन करने वाला तृतीय परिच्छेद पूर्ण हुआ।
🏠
चतुर्थ परिच्छेद
प्रत्यक्षाभं कथंचित्स्यात्प्रमाणं तैमिरादिकं॥
यद्यथैवाविसंवादि प्रमाणं तत्तथा मतं॥1॥
अन्वयार्थ : [प्रत्यक्षाभं] प्रत्यक्षाभास [तैमिरादिकं] तैमिर आदि ज्ञान [कथंचित्] कथंचित् [प्रमाणं स्यात्] प्रमाण हैं, [यत्] जो ज्ञान [यथा एव] जिस प्रकार से ही [अविसंवादि] अविसंवादी है [तत्] वह [तथा] उसी प्रकार से [प्रमाणं मतं] प्रमाण माना गया है॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
(संशय आदि कथंचित् प्रमाण हैं)
तात्पर्यवृत्ति-अक्ष-इंद्रिय और अनिंद्रिय के प्रति जो नियत है वह प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र है उसके समान जो आभासित होता है वह प्रत्यक्षाभ-प्रत्यक्षाभास कहलाता है। वह कैसा है ? तिमिर से उत्पन्न हुआ ज्ञान तैमिरिक है, ऐसे ही और भी शीघ्र भ्रमण आदि ज्ञान होते हैं, वे प्रमाण हैं। वे कैसे प्रमाण हैं ? कथंचित् भाव प्रमेय की अपेक्षा से अथवा द्रव्य की अपेक्षा से वे सर्वथा प्रमाणाभास ही नहीं हैं किन्तु प्रमाण भी हैं। बाह्य पदार्थ के आकार को विषय करने में ही ज्ञान में विसंवाद आता है किन्तु स्वरूप की अपेक्षा उन ज्ञानों में विसंवाद नहीं है। इस विषय में अविनाभाव दिखलाते हैं -
जो ज्ञान जिस प्रकार ही-जितने विषय को जानने प्रकार से अविसंवादी है अर्थात् गृहीत अर्थ के विषय में व्यभिचार होना विसंवाद है उससे रहित अविसंवादी वह ज्ञान उसी प्रकार-उतने विषय को जानने के प्रकार से परीक्षकों ने प्रमाण इष्ट किया है-माना है। उसी को कहते हैं -
‘सभी प्रमाणाभास संशय आदि ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से अथवा द्रव्य की अपेक्षा से प्रमाण होते हैं क्योंकि उस विषय में अविसंवादी हैं। जो जिस विषय में अविसंवादी है वह उस विषय में प्रमाण है जैसे रस में रसज्ञान और संशय आदिक ज्ञान स्वरूप के विषय में अथवा द्रव्य रूपादि को विषय करने में अविसंवादी हैं इसलिए उन विषयों में वे कथंचित् प्रमाण हैं।
विसंवाद ही निश्चित रूप से अप्रमाणता का कारण है और अविसंवाद ही प्रमाणता का कारण है। इस प्रकार न्याय सभी वादीजनों सम्मत है। सर्वथा प्रमाणाभासता न्याय से शून्य है। ‘‘बहि:१ प्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभं च ते’’ बाह्य प्रमेय की अपेक्षा में प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों होते हैं, ऐसा वचन है। ज्ञान अपने स्वरूप से विसंवादी नहीं है। क्योंकि वे ‘अहं प्रत्ययं’ से (मैं इस ज्ञान से) सिद्ध हैं और प्रसिद्ध विषय में प्रवर्तमान होते हुए अप्रमाण कैसे हो ?
भावार्थ-आचार्यश्री का ऐसा कहना है कि यदि संशय ज्ञान अपने स्वरूप में भी अप्रमाण हो जावे तब तो संशय न रहकर असंशय-सच्चा हो जावेगा अत: सभी ज्ञान अपने-अपने स्वरूप को बताने में सच्चे ही हैं आरै द्रव्यदृष्टि से ज्ञान सामान्य की अपेक्षा भी सच्चे ही हैं। हाँ, बाह्य पदार्थों को जानने के विषय में जहाँ पर विसंवादी होता है वहीं पर झूठा कहलाता है और जहाँ पर विसंवाद रहित होता है वहीं पर सच्चा कहा जाता है ऐसा समझना।
🏠
स्वसंवेद्यं विकल्पानां विशदार्थावभासनं॥
संहृताशेषचिंतायां सविकल्पावभासनात्॥2॥
अन्वयार्थ : [विकल्पानां] विकल्पों में [विशदार्थावभासनं] विशद अर्थ को प्रतिभासित करने वाला ज्ञान [स्वसंवेद्यं] स्वसंवेद्य है, [संहृताशेषचिंतायां] वह अशेष विकल्पों के नष्ट हो जाने पर [सविकल्पावभासनात्] सविकल्प रूप के प्रतिभास से होता है॥२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-स्व-तत्त्वज्ञानरूप से संवेद्य-ग्राह्य अर्थात् ज्ञान का स्वरूप स्वसंवेद्य कहलाता है क्योंकि इसमें वेद्य और वेदक इन दोनों आकार का विरोध नहीं है अन्यथा ज्ञान अवस्तु हो जावेगा। वह ज्ञान कैसा है ? विशद अर्थ का अवभासी है विशद-स्पष्ट और परमार्थ सत्-वास्तविक पदार्थ का अवभासित करने वाला ज्ञान विशद अर्थावभासी है। किनमें विशद अर्थ प्रतिभासन होता है ? यह घट है, यह गौ है, यह शुक्ल है, यह गायक है इत्यादि विकल्पों का-निश्चय ज्ञानों में विशद अर्थ प्रतिभासन होता है। कैसे प्रतिभासित होता है ? विकल्प-जाति आदि आकार वाले ज्ञान सहित जो सविकल्पक ज्ञान है, उसके प्रतिभासन-अनुभव से प्रतिभासित होता है। कब प्रतिभासित होता है ? अशेष स्मृति आदि चिंताविकल्पों के नष्ट हो जाने पर होता है अर्थात् चक्षु आदि के ज्ञान में जाति आदि आकार विशेष का जानना अप्रतिहत-निर्विघ्न रूप से होता है इसलिए विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्षाभास कहना गलत है, यह अर्थ हुआ।
भावार्थ-‘यह गौ है, यह घट है’ इत्यादि विषयों में जो स्पष्ट रूप से पदार्थों का प्रतिभासन होता है वह स्वसंवेद्य है अर्थात् ज्ञानस्वरूप है। वह ज्ञान संपूर्ण स्मृति आदि विकल्पों की समाप्त दशा में जाति आदि आकार के विकल्प सहित होने वाले अनुभव से होता है इसलिए यह विकल्पों से अर्थ को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान सविकल्पक है वह सच्चा है, प्रमाणाभास-असत्य नहीं है।
🏠
प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्यया: सत्योऽपि कल्पना:॥
प्रत्यक्षेषु न लक्षेरंस्तत्स्वलक्षणभेदवत्॥3॥
अन्वयार्थ : [ प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्यया:] प्रत्येक में अनुभव में आते हुए उत्पत्ति और व्ययरूप [कल्पना:] विकल्प [सत्य: अपि] विद्यमान होते हुए भी [प्रत्यक्षेषु] प्रत्यक्ष ज्ञानों में [तत् न लक्षेरन्] वे लक्षित नहीं होते हैं [स्वलक्षण भेदवत्] जैसे स्वलक्षण में भेद नहीं जाना जाता है॥३॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-स्वसंवेदन आदि प्रत्यक्ष ज्ञानों में विद्यमान रहते हुए भी वे विकल्प लक्षितविवेचित नहीं किये जाते हैं अर्थात् उन्हें कह नहीं सकते हैं। वे कैसे हैं ? उत्पत्ति-आत्मलाभ और व्यय-अभाव प्रतिसंविदित-प्रत्येक प्राणियों में उपलब्ध होने वाले ऐसे ये उत्पत्ति और व्ययरूप विकल्प हैं।
क्योंकि सत्त्व के बिना उत्पादव्ययवत्त्व अनुभव में नहीं आता है अन्यथा अतिप्रसंग हो जावेगा और विकल्पों में उत्पाद, व्ययपना असिद्ध भी नहीं है क्योंकि वह कार्य कारण के संबंध में प्रवर्तमान है। निर्विकल्प से विकल्प का होना भी शक्य नहीं है। वह निर्विकल्प अकिन्चित्कर है, विकल्प को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित है।
शंका-विकल्पों के मौजूद होने पर भी प्रत्यक्षज्ञान में नहीं दिखते हैं। इसका क्या कारण है ?
समाधान-जानने वाले का शक्ति का अप्रणिधान-उधर न लगना ही है ऐसा हम कहते हैं। इस विषय में दृष्टांत-उन विकल्पों के स्वलक्षण-स्वरूप का सजातीय विजातीय से व्यावृत्त होना भेद कहलाता है उसके स्वलक्षण के भेद के समान। यहाँ यह अर्थ हुआ कि जिस प्रकार प्रतीति के विषयभूत उत्पाद, व्यय विद्यमान होते हुए भी स्वलक्षण से व्यावृत्तिरूप कल्पनाओं में लक्षित नहीं होते हैं, वे अनुमान से ही सिद्ध हैं उसी प्रकार से निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञानों में कल्पना में भी लक्षित नहीं होती हैं।
शंका-तब तो नहीं दिखती हुई उन कल्पनाओं का उस ज्ञान में वैâसे अस्तित्व सिद्ध होगा ?
समाधान-ऐसा नहीं कहना, पुन: उस विषय के स्मरण की अन्यथानुपपत्ति से वे कल्पनाएं सिद्ध हैं अर्थात् ज्ञान में यदि कल्पनाएं न हों तब तो पुन: उनके विषय का स्मरण कैसे हो सकेगा ? इसलिए उनका अस्तित्व सिद्ध है।
संहृतसकल विकल्पावस्था अर्थात् अश्व का विकल्प करते हुए गौ को देखने की अवस्था है, उसमें भी गोदर्शन निश्चयात्मक ही है क्योंकि पुन: उसके विषय के स्मरण की अन्यथानुपपत्ति है। जहाँ निश्चय का अभाव है वहाँ स्मरण नहीं उत्पन्न होता है, जैसे-चलते हुए तृण का स्पर्श हो जाने पर स्मरण नहीं उत्पन्न होता है और पुन: उनका स्मरण होता है, इसलिए अनुमान में विकल्पों का अस्तित्व सिद्ध है। जैसे-उस विकल्प के स्वरूप की व्यावृत्ति सिद्ध है। उसकी व्यावृत्ति भी प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है क्योंकि वैसा अनुभव नहीं आता है। इसलिए यह बात सिद्ध हो गई कि निश्चय-विकल्पज्ञान प्रमाण है क्योंकि वह अविसंवादी है।
🏠
अक्षधीस्मृतिसंज्ञाभिश्चिंतयाऽऽभिनिबोधिकै:॥
व्यवहाराविसंवादस्तदाभासस्ततोऽन्यथा॥4॥
अन्वयार्थ : [अक्षधी:] इंद्रियज्ञान-मतिज्ञान [स्मृतिसंज्ञाभि:] स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, [चिंतया] तर्क और [आभिनिबोधकै:] अनुमान ज्ञानों के द्वारा [व्यवहाराविसंवाद:] व्यवहार में अविसंवादी है [तत:] इनसे [अन्यथा] अन्य प्रकार से-व्यवहार में विसंवादी होने से [तदाभास:] प्रमाणाभास हैं॥४॥
अभयचन्द्रसूरि :
(प्रमाण और प्रमाणाभास)
तात्पर्यवृत्ति-‘प्रमाण’ यह अनुवृत्ति में चला आ रहा है। उससे अभिसंबंध करने से अक्षधी आदि में प्रथमान्त विभक्ति करके अर्थ करना चाहिए। यहाँ ‘अर्थवशाद्विभक्तिविपरिणाम:’ इस न्याय से अर्थ के निमित्त से विभक्ति में परिवर्तन हो गया है। इससे इस प्रकार व्याख्यान किया जाता है-अक्षधी, स्मृति, संज्ञा से, चिंता से और आभिनिबोधिक से हानोपादान रूप व्यवहार में अविसंवाद-अव्यभिचार सकल व्यवहारीजनों में प्रतीति से सिद्ध है इसलिए वे ज्ञान प्रमाण होते हैं, यह अर्थ हुआ।
अक्ष-इंद्रियों से उत्पन्न हुआ धी-ज्ञान अक्षधी है अर्थात् सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष को अक्षज्ञान कहते हैं। अतीत अर्थ का अवमर्श करने वाला ज्ञान स्मृति है। संज्ञा-प्रत्यभिज्ञान, चिंता-तर्वâ और आभिनिबोधिक- अनुमान। आभिनिबोध अर्थात् हेतु के अन्यथानुपपत्ति नियम का निश्चय, उसमें होने वाला आभिनिबोधिक है ऐसा व्याख्यान किया गया है। इन ज्ञानों के द्वारा प्रमेय-जानने योग्य विषय प्रवर्तन करता हुआ छोड़ने- ग्रहण करने आदि फल में विसंवाद को प्राप्त नहीं होता है इसलिए उन ज्ञानों को प्रमाणता क्यों नहीं होगी ?
शंका-इस प्रकार से उन ज्ञानों में प्रमाणता कैसे होगी ?
समाधान-ऐसे आशंका को हम दूर करते हैं उसी व्यव्हार में विसंवाद नहीं होने से वे प्रमाण हैं अन्यथा उस व्यवहार मिएँ विसंवाद होने से वे अक्षधी - साम्व्यव्हारिक प्रत्यक्ष, स्मृति आदि ज्ञान तदाभास-प्रमाणाभास हो जाते हैं। निश्चित ही अर्थक्रिया से व्यभिचरित होने वाले को प्रमाणता नहीं है अन्यथा अति प्रसंग आ जावेगा।
(प्रमाणाभास के लक्षण)
संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय और अदर्शन आदि प्रत्यक्षाभास कहलाते हैं। जो वह नहीं है उसमें ‘वह’ इस प्रकार का परामर्शी ज्ञान स्मृत्याभास है। जो उस सदृश नहीं है उसमें ‘यह उसके सदृश हैं’ और जो वह नहीं है उसमें ‘यह वहीं है’ इत्यादि ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभास हैं। जिसका आपस में संबंध नहीं है ऐसे असंबद्ध में व्याप्ति को ग्रहण करना तर्काभास है। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिन्चित्कर ये हेत्वाभास हैं। प्रत्यक्ष आदि से बाधित साध्याभास है। साध्य विकल, साधन विकल और उभयविकल ये दृष्टांताभास हैं। विस्तार से इनका लक्षण परीक्षामुखालंकार आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए।
🏠
प्रमाणं श्रुतमर्थेषु सिद्धं द्वीपांतरादिषु॥
अनाश्वासं न कुर्वीरन् क्कचित्तद्व्यभिचारत:॥5॥
अन्वयार्थ : [द्वीपांतरादिषु] द्वीपान्तर आदि [अर्थेषु] पदार्थों में [श्रुतं] श्रुतज्ञान [प्रमाणं सिद्धं] प्रमाण सिद्ध है [क्वचित् तद् व्यभिचारत:] कहीं पर उसमें व्यभिचार होने से [अनाश्वासं] अविश्वास [न कुर्वीरन्] नहीं करना चाहिए॥५॥
अभयचन्द्रसूरि :
(श्रुत की प्रमाणता-अप्रमाणता)
तात्पर्यवृत्ति-व्यवहार में अविसंवाद यह अनुवृत्ति में चला आ रहा है। आप्त के वचन आदि के निमित्त से होने वाला मतिपूर्वक अर्थज्ञान श्रुत कहलाता है और वह प्रमाण सिद्ध ही है।
प्रश्न-किस प्रकार से सिद्ध है ?
उत्तर-व्यवहार-त्याग-ग्रहण आदि में अविसंवादी होने से प्रत्यक्षादि ज्ञानों के समान प्रमेय अर्थों को जानने में वह प्रमाण सिद्ध है।
प्रश्न-वे प्रमेय क्या हैं ?
उत्तर-द्वीपान्तर आदि प्रमेय हैं। उन्हीं का स्पष्टीकरण करते हैं। प्रकृत जंबूद्वीप है, उससे अन्य धातकीखंड आदि द्वीपांतर कहलाते हैं। आदि शब्द से काल से और स्वभाव से व्यवहित-अत्यंत परोक्ष पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात् देशकाल और आकार से विप्रकृष्ट-अत्यंत दूरवर्ती-पदार्थों में श्रुतज्ञान प्रमाण है।
श्रुत से अर्थ को जानकर प्रवृत्ति करता हुआ कोई भी पुरुष रसायन आदि क्रिया में अथवा ग्रहण आदि करने में या मलय-चंदन आदि की प्राप्ति में विसंवाद को प्राप्त नहीं होता है इसलिए परीक्षकजनों को अनाश्वास-अविश्वास नहीं करना चाहिए।
प्रश्न-कहीं-कहीं व्यभिचार देखा जाता है। जैसे-किसी नदी के किनारे लड्डू रखे हुए हैं इत्यादि रूप से प्रतिपादन करने पर उस श्रुत में व्यभिचार-विसंवाद देखा जाता है ?
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कहीं पर विसंवाद होने से ज्ञान को अप्रमाण मानने पर सभी जगह अप्रमाण की आशंका नहीं करना चाहिए अन्यथा प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों में भी वैसे ही अप्रमाणता का प्रसंग हो जाने से सकल व्यवहार का ही लोप हो जावेगा।
प्रश्न-श्रुत के विषय में वादियों को विसंवाद देखा जाता है, इसलिए वह अप्रमाण है ?
उत्तर-प्रत्यक्षादि ज्ञानों में भी उसी हेतु से अप्रमाणता आ जावे, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से पर लोक, पुण्य, पाप, सर्वज्ञादि जो श्रुतज्ञान के विषय हैं इनमें वादियों को विसंवाद है उसी प्रकार से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान के विषयभूत जीवादि पदार्थों में भी सत्-असत्, नित्य-अनित्य आदि रूप से विसंवाद होते हैं। इसलिए अविसंवाद (और विसंवाद) से की गई प्रमाणता और अप्रमाणता की व्यवस्था श्रुतज्ञान में अथवा अन्य ज्ञान में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही न्याय रूप है।
भावार्थ-कुछ लोग आगम को प्रमाण नहीं मानते हैं इसलिए यहाँ आचार्य ने स्पष्ट किया है कि जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान आदि ज्ञान जहाँ-जहाँ जिस-जिस विषय में अव्यभिचारी हैं वहाँ-वहाँ उस-उस विषय में प्रमाण हैं अन्यत्र व्यभिचारित होने से अप्रमाण हैं। वैसे ही श्रुतज्ञान भी सूक्ष्म-परमाणु आदि अंतरित राम, रावणादि और दूरवर्ती-हिमवान्, सुमेरु आदि विषयों में अविसंवादी होने से प्रमाण है और जहाँ व्यभिचारी हो जाता है वहाँ अप्रमाण है।
🏠
प्राय: श्रुतेर्विसंवादात्प्रतिबंधमपश्यतां।
सर्वत्र चेदनाश्वास: सोऽक्षलिंगधियां सम:॥6॥
अन्वयार्थ : [प्राय: श्रुते: विसंवादात्] कदाचित् आगम में विसंवाद होने से [प्रतिबंधं अपश्यतां] शब्द और अर्थ के संबंध को नहीं जानने वालों को [चेत् सर्वत्र अनाश्वास:] यदि सभी आगम में अविश्वास है तो [स:] वह अविश्वास [अक्षलिंगधियां सम:] इंद्रिय ज्ञान और अनुमान ज्ञान में समान है॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-प्रतिबंध को नहीं देखने वालों को अर्थात् शब्द और अर्थ के सहज योग्यता लक्षण संबंध को नहीं समझने वाले सौगतों को प्राय: क्वचित्-कदाचित् श्रुत-आगम के विसंवाद से यदि सर्वत्र-अविसंवादी श्रुत की प्रमाणता में विसंवाद हो जावे, तब तो वह अविश्वास समान है।
प्रश्न-किसके समान है ?
उत्तर-अक्ष-इन्द्रियाँ और लिंग-हेतु इनसे उत्पन्न होने वाले सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानों के समान है अर्थात् इन प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञानों में भी क्वचित्-कदाचित् व्यभिचारी दिखने से अविश्वास हो जावेगा, यह अर्थ हुआ है।
प्रश्न-अदुष्ट-निर्दोष कारण से जन्य प्रत्यक्ष अथवा अनुमान ज्ञान पदार्थों में विसंवाद को प्राप्त नहीं होते हैं ?
उत्तर-यदि ऐसी बात है तो अदुष्ट-निर्दोष आप्त वचन से उत्पन्न हुआ श्रुत भी विसंवाद को क्यों प्राप्त होगा ? इस प्रकार दोनों जगह समान ही है।
भावार्थ-सौगत आगम को प्रमाण नहीं मानता है। आचार्यों ने समझाया है कि शब्द और अर्थ में एक सहज योग्यता लक्षण संबंध पाया जाता है। इस निमित्त से वह श्रुतज्ञान सर्वत्र अप्रमाणीक नहीं है अन्यथा प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान भी सर्वत्र अप्रमाणीक हो जावेंगे। यदि कोई कहे कि निर्दोष कारण से उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान नहीं है, तब तो हमारे यहाँ भी निर्दोष कारणरूप आप्त के वचन से उत्पन्न हुआ आगम रूप श्रुतज्ञान प्रमाणीक है, यह अर्थ हुआ।
🏠
आप्त्तोक्तेर्हेतुवादाच्च बहिरर्थाविनिश्चये॥
सत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुत:॥7॥
अन्वयार्थ : [ आप्त्तोक्ते:] आप्त के वचन से [हेतुवादात् च] और हेतुवाद से [बहि: अर्थाविनिश्चये] बाह्य अर्थ का निश्चय न मानने पर तो [सत्येतर व्यवस्था का] सत्य-असत्य की व्यवस्था क्या होगी ? और [साधनेतरता कुत:] साधन-असाधन की व्यवस्था कैसे होगी ?॥७॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-सत्य-सुगत के वचन और इतर-असत्य कपिल आदि के वचन इन दोनों की व्यवस्था-विभाग क्या होगा ? अर्थात् कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार साधन-अपने इष्ट की सिद्धि निमित्तक सत्त्वादि हेतु और इतर-हेत्वाभास इन दोनों का भाव साधनेतरता भी कैसे व्यवस्थित होगी ?
प्रश्न-कब ये दोष आएंगे ?
उत्तर-जो जहाँ पर अवंचक है वह वहाँ पर आप्त है, उसके वचन से, केवल आप्त के वचन से ही नहीं किन्तु हेतुवाद-साधन के प्रयोग से इन दोनों से बाह्य अर्थ विप्रकृष्ट-अत्यंत परोक्ष प्रमेय का निश्चय नहीं होने पर उपर्युक्त सत्य-असत्य व्यवस्था और साधन-साधनाभास की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अर्थ यह हुआ कि आप्त के कथन से यदि अर्थ की प्रतीति नहीं मानोगे तब तो आपके सुगत के वचन सत्य हैं और कपिलादि के वचन असत्य हैं यह व्यवस्था वैâसे बनेगी ? क्योंकि अर्थ को विषय नहीं करना दोनों जगह समान है और हेतुवाद से भी बाह्य अर्थ का निश्चय नहीं मानने पर साधन-साधनाभास की व्यवस्था भी कैसे बनेगी, क्योंकि बाह्य अर्थ की शून्यता दोनों जगह समान है।
भावार्थ-यहाँ पर आचार्य ने सौगत को लक्ष्य करके ही श्रुत को प्रमाण मानने की पुष्टि की है कि यदि आप बुद्ध के वचन को प्रमाण नहीं मानोगे तो आपके बुद्ध सत्य हैं और उनके वचन सत्य हैं। अन्य संप्रदाय वालों के ईश्वर और उनके वचन असत्य हैं यह विभाग भी कैसे बनेगा ? अत: श्रुत को प्रमाण मान लेना उचित है।
🏠
पुंसश्चित्राभिसंधेश्चेद्वागर्थव्यभिचारिणी॥
कार्यं दृष्टं विजातीयाच्छक्यं कारणभेदि किं॥8॥
अन्वयार्थ : [चेत् चित्राभिसंधे:] यदि नाना अभिप्राय से [पुंस: वाक् अर्थ व्यभिचारिणी] पुरुष के वचन अर्थ को व्यभिचारित करते हैं, तब तो [विजातीयात् कार्यं दृष्टं] विजातीय कारण से कार्य विरोध रहित हो जावेगा [कारण भेदि किम् शक्यं] पुन: कारण में भेद करना क्या शक्य होगा ?॥८॥
अभयचन्द्रसूरि :
भावार्थ-यदि पुरुष के अभिप्राय भिन्न-भिन्न हैं अत: उनके वचन अर्थ में विसंवाद करते हैं इसलिए किसी को आप्त नहीं माना जा सकता, न उनके वचन ही अर्थ को सही कहने वाले माने जा सकते हैं तब तो गेहूँ के बीज से शालिधान्य उत्पन्न हो जावेंगे, पुन: कारण में भेद कुछ भी नहीं रह सकेगा।
तात्पर्यवृत्ति-पुरुष-वक्ता के चित्र-सत्य-असत्य आदि नानारूप अभिसंधि-अभिप्रायविवक्षा से यदि वाक्-आप्त के वचन अर्थ में व्यभिचारी हैं-बाह्य पदार्थ में विसंवादी हैं अर्थात् ‘‘सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टंते’’ सराग भी वीतराग के समान चेष्टा करते हैं ऐसा वचन है। तब तो विजातीय कारण से भी कार्य दृष्ट-अविरुद्ध हो जावें पुन: उस कारण में भेद करना अर्थात् कारण के प्रतिनियत-स्वात्मलाभ के निमित्त को अलग करना-विजातीय से भेद करना क्या शक्य होगा ? अर्थात् नहीं होगा।
तब उस कार्य के जिस किसी से उत्पन्न होने में विरोध नहीं होगा, निश्चित ही अनियत कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य कारण के भेद को नहीं बतलाता है क्योंकि उसमें वैसी शक्ति नहीं है। पुन: कार्य में कारण का व्यभिचार होने से वह अहेतु हो जावेगा, इस तरह अनुमान का उच्छेद हो जावेगा, यह भाव हुआ।
सौगत-विवेकपूर्वक होने वाले कार्य कारण का उल्लंघन नहीं करते हैं।
जैन-यदि ऐसा कहो, तो सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त हुए वचन भी यथार्थ विवक्षा का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार से अर्थ में व्यभिचार कैसे होगा ?
प्रश्न-विवक्षा में अधिरूढ़ ही वचन का अर्थ है, बाह्य अर्थ नहीं है अर्थात् कहने की इच्छा तक ही वचन का अर्थ सीमित है, बाह्य पदार्थ को नहीं कहता है।
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि विवक्षा का उससे व्यभिचार नहीं है। बोलने की इच्छा विवक्षा है। उस बोलने की इच्छा का नियम बाह्य अर्थ के नियम से युक्त नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग आ जावेगा।
हाथ की अंगुली के अग्रभाग के आधार पर तो हाथी के अस्तित्व आदि के प्रतिपादक वचन प्रतारण करने वाले-ठगने वाले होने से अप्रमाण सिद्ध हैं क्योंकि राग, द्वेष, मोह से आक्रांत पुरुष के वचन आगमाभास हैं इसलिए द्वीपांतर आदि अर्थों में विसंवाद का अभाव होने से श्रुतज्ञान प्रमाणरूप सिद्ध है, यह बात ठीक ही कही है।
भावार्थ-पुरुषों के मनोगत भावों में और वचनों में अंतर देखकर सर्वत्र वचन को अर्थ का व्यभिचारी कहना ठीक नहीं है अन्यथा विजातीय गेहूँ के बीज से शालिधान्य का अंकुर उत्पन्न हो जावेगा, पुन: कोई भी कारण अपने कार्य का नियामक नहीं हो सकेगा। इसलिए सर्वथा अर्थशून्य अथवा विरोधी वचनों को देखकर सर्वत्र सत्य आगम में भी अविश्वास करना, उसे प्रमाण नहीं मानना अयुक्त है। हमारे यहाँ तो आगम प्रमाण सबसे बलवान है, वही तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि की प्रमाणता को सिद्ध करता है। पिता को प्रमाण न मानकर बेटे को प्रमाण मानना कहाँ तक उचित है।
श्लोकार्थ-श्री भट्टाकलंकदेव और प्रभाचंद्राचार्य से अंजित-स्पष्ट किये कथंचित् प्रमाणाभास को ‘स्यात्’-स्याद्वाद मत का आश्रय लेकर श्री अभयचंद्रसूरि के वचन विशेष रूप से वर्णन कर देते हैं अर्थात् कारिका में श्री भट्टाकलंकदेव ने कथंचित् प्रमाणाभास का वर्णन किया है। पुन: श्री प्रभाचंद्राचार्य ने न्यायकुमुदचंद्र टीका और उसका विशद विवेचन किया है।।१।।
यहाँ पर उन दोनों के आधार से और स्याद्वादमत का आश्रय लेकर श्री अभयचंद्रसूरि ने तात्पर्यवृत्ति में उसका ही स्पष्ट और संक्षेप विवेचन कर दिया है।
इस प्रकार से अभयचंद्रसूरि कृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण नामक तात्पर्यवृत्ति में प्रमाणाभास नाम का चतुर्थ परिच्छेद पूर्ण हुआ।
इस प्रकार भट्टाकलंक शशांक से स्मृत लघीयस्त्रय में प्रमाण प्रवेश नाम का प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ।
🏠
पंचम परिच्छेद
नमो नमन्मरुन्मौलिमिलत्पदनखांशवे॥
स्वांतध्वांतप्रतिध्वंस प्रशंसाय जिनांशवे॥1॥
अथेदानीं प्रमाणं तदाभासं परीक्ष्य नयतदाभासलक्षणपरीक्षार्थमाह—
भेदाभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसंधय:॥
एतेऽपेक्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्यंते नयदुर्नया:॥1॥
अन्वयार्थ : अर्थ-नमस्कार करते हुए देवों के मुकुट से स्पर्शित है चरण नख किरणें जिनकी, ऐसे हृदय के अंधकार को ध्वंस करने में प्रशंसित जिन चंद्रमा को मेरा नमस्कार होवे॥१॥
अन्वयार्थ-[भेदाभेदात्मके ज्ञेये] भेदाभेदात्मक ज्ञेय पदार्थ में [भेदाभेदाभिसंधय:] जो भेद और अभेदरूप अभिप्राय हैं [एते] ये [अपेक्षानपेक्षाभ्यां] अपेक्षा और अनपेक्षा के द्वारा [नयदुर्नया:] नय और दुर्नयरूप [लक्ष्यंते] निश्चित किये जाते हैं॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-प्रतिपक्ष धर्म की आकांक्षारूप अपेक्षा से और इससे विपरीत सर्वथा एकांतरूप अनपेक्षा से ये नय और नयाभास लक्षित-निश्चित किये जाते हैं।
प्रश्न-ये किन विशेषताओं से सहित हैं ?
उत्तर-ये भेद और अभेद के अभिप्राय रूप हैं। विशेष, पर्याय और व्यतिरेक को भेद कहते हैं। सामान्य, एकत्व और सादृश्य को अभेद कहते हैं। इन भेद और अभेद के अभिप्राय रूप हैं अर्थात् ये नय श्रुतज्ञानी के विकल्प रूप हैं। भेदाभेदात्मक जीवादि ज्ञेय-प्रमेय के जानने में ये भेदाभेद विकल्प होते हैं।
निश्चित ही एकांतरूप से भेदात्मक अथवा अभेदात्मकरूप प्रमेय उपलब्ध नहीं है। अनुवृत-व्यावृत्त प्रत्यय के बल से उभयात्मक ही उपलब्ध हो रहा है क्योंकि प्रमाण अनेकांत को विषय करने वाला है। ‘अनेकांत: प्रमाणात्१’ अनेकांत प्रमाण से जाना जाता है।
(सुनय और दुर्नय का लक्षण)
उभयात्मक रूप से अर्पित-अपेक्षित वस्तु व्यवहार के योग्य नहीं है इसलिए व्यवहार के उपयोगी एकांत नय के आधीन होने से नय कहे जाते हैं। ‘२तदेकांतोऽर्पितान्नयात्’ अर्पित नय से व्यवहार के लिए उपयोगी एकांत होता है। इस प्रकार सिद्धांत में कहा है। वे नय परस्पर की अपेक्षा करने वाले ही व्यवहार के लिए समर्थ होते हैं अन्यथा परस्पर की अपेक्षा न रखने से उस व्यवहार के लोप करने में हेतु होने से दुर्नय हो जाते हैं। ३निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्’’ निरपेक्ष नय मिथ्या हैं और सापेक्ष होते हुए वे नय हे भगवन्! आपके यहाँ वस्तुभूत अर्थक्रियाकारी हैं, ऐसा श्री स्वामी समंतभद्राचार्य ने कहा है।
(नय के विषय)
वे नय दो प्रकार के हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य, सामान्य, अभेद, अव्यय और उत्सर्ग ये पर्यायवाची नाम हैं। यह द्रव्य जिसका अर्थ-विषय है, वे द्रव्यार्थिक नय हैं। पर्याय विशेष, भेद, व्यतिरेक, अपवाद ये पर्यायवाची नाम हैं। ये पर्याय अर्थ-विषय है जिसका वे पर्यायार्थिक नय हैं, ऐसा निरुक्ति अर्थ है।
द्रव्य के दो भेद हैं-शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। उसमें सत्सामान्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं और जीव तत्त्वादि पुन: अशुद्ध द्रव्य कहलाते हैं।
भावार्थ-प्रत्येक वस्तु में अनेक अंत अर्थात् धर्म पाये जाते हैं इसलिए वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रमाण अनेकांत को विषय करता है। अनेकांतात्मक वस्तु के एक धर्म अर्थात् एक अंश को एकांत कहते हैं। नय एकांत को विषय करता है। यह नय अपने से विपरीत अंश के ग्राहक नय की अपेक्षा रखता है तभी तक सुनय है। जब दूसरे की अपेक्षा न करके आग्रहपूर्वक एक अंश को ही ग्रहण करता है तब वह दुर्नय या नयाभास कहलाता है।
द्रव्य मात्र को जानने वाला द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय मात्र को जानने वाला पर्यायार्थिक नय है। द्रव्य में भी सत्सामान्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं और जीवादि तत्त्व को अशुद्ध द्रव्य कहते हैं।
🏠
जीवाजीवप्रभेदा यदंतर्लीनास्तदस्ति सत्।
एकं यथा स्वनिर्भासि ज्ञानं जीव: स्वपर्ययैः॥2॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[जीवाजीवप्रभेदा:] जीव और अजीव के प्रभेद [यत् अंतर्लीना:] जिसके अंतर्लीन हैं [तत् सत् अस्ति] वह सत् है। [यथा] जैसे [स्वनिर्भासि] स्वनिर्भासी [एकं ज्ञानं] एक ज्ञान और [स्वपर्ययै:] अपनी पर्यायों से [जीव:] जीव एक है॥२॥
अभयचन्द्रसूरि :
(सत् का लक्षण)
तात्पर्यवृत्ति-जीव का लक्षण चेतना है। अजीव पुन: उससे विपरीत पुद्गल आदि हैं। त्रस-स्थावर आदि अवांतर विशेष जीव के प्रभेद हैं। ये भेद-प्रभेद सहित सभी जीव-अजीव जिसमें अंतर्गर्भित हैं वह सत्-सत्तासामान्य है-मौजूद है-प्रतीति में आ रहा है।
निश्चित ही सत्त्व-अस्तित्व से व्यतिरिक्त द्रव्य अथवा पर्याय ‘अस्ति-है’ इस प्रकार कुछ भी व्यवहार करना शक्य नहीं है क्योंकि स्ववचन में विरोध आता है और अतिप्रसंग दोष आता है अर्थात् ‘अस्ति’ को ही ‘है’ इस शब्द से कहते हैं। जब द्रव्य या पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है तब यह द्रव्य है या पर्याय है ऐसा कहना तो ‘मैं मौनव्रती हूँ’ ऐसा बोलने वाले के समान स्ववचन बाधित ही है और अतिप्रसंग से आकाश के फूल, बंध्या के पुत्र आदि भी दिखने लगेंगे।
प्रश्न-एक ही अनेक जीवादि भेदों में व्यापक कैसे हो सकता है ?
उत्तर-जैसे आपके द्वारा मान्य एक ही ज्ञान चित्रपटाति को विषय करने वाला है स्वनिर्भासी है। स्व-अपने ज्ञानस्वरूप निर्भास-नीलादि आकार जिसमें हैं, वह स्वनिर्भासी कहलाता है और जिस प्रकार से एक जीव-आत्मा अपनी पर्यायों से सहित है। स्व-चिद्रूप पर्याय-रागादि परिणामों से आक्रांत-व्याप्त प्रतीति के पद पर आरूढ़ हुआ विरुद्ध नहीं है अर्थात् चैतन्य स्वरूप राग, द्वेषादि भावों से व्याप्त और प्रतीति में आता हुआ एक जीव द्रव्य सिद्ध है। उसी प्रकार से जीवादि अनेक भेदों से आक्रांत सत्त्व भी विरुद्ध नहीं है।
🏠
शुद्धं द्रव्यमभिप्रैति संग्र्रहस्तदभेदत:।
भेदानां नासदात्मैकोऽप्यस्ति भेदो विरोधत:॥3॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[संग्रह: तदभेदत:] संग्रहनय उस सामान्य के अभेद से [शुद्धं द्रव्यं] शुद्ध द्रव्य को [अभिप्रैति] स्वीकार करता है। [भेदानां] भेदों में [असदात्मा] असत्स्वरूप [एक: अपि भेद:] एक भी भेद [न अस्ति] नहीं है॥३॥
अभयचन्द्रसूरि :
(संग्रहनय का विषय)
तात्पर्यवृत्ति-संग्रहनय सत्सामान्य शुद्ध द्रव्य को विषय करता है क्योंकि उसमें अन्य उपाधि से रहित होने से ही शुद्धि संभव है। ‘सामान्य को विषय करने वाला ही नय संग्रह है वह स्वजाति के अविरोध से भेदों से सहित ऐसी पर्यायों में एकत्व को प्राप्त करके समस्त को ग्रहण करने वाला ‘संग्रह’ कहलाता है। ऐसा निरुक्ति सिद्ध अर्थ है।
क्योंकि वह तदभेदत:-उस सत्सामान्य लक्षण शुद्ध द्रव्य में अभेद रूप है। सभी जीव और अजीवों में अव्यतिरिक्त-अभिन्न है।
प्रश्न-प्रागभाव आदि सत्त्व से भिन्न हैं तो यह उनसे अभिन्न कैसे होगा ?
समाधान-जीवादि सत् विशेषों के मध्य में एक भी भेद जीव, उसकी पर्याय अथवा अन्य कोई असदात्मा-असत्वरूप नहीं है क्योंकि विरोध आता है। यदि असत् रूप है पुन: ‘है कैसे’ ? यदि ‘है’तो असत्स्वरूप कैसे है ? इस प्रकार स्ववचन में विरोध होता है अत: वह सत् सिद्ध है इसलिए प्रागभाव आदि हो अथवा अन्य कोई हो उसे कथंचित् प्रतीति के बल से सदात्मक-सत् रूप ही स्वीकार करना चाहिए।
भावार्थ-संग्रहनय सत् सामान्य को विषय करता है अर्थात् इसी नय की अपेक्षा से संपूर्ण चराचर जगत् एकरूप है। इस संग्रहनय के उदर में सारा लोकालोक समा गया है। इसी नय के एकांत दुराग्रह से ब्रह्माद्वैतवादी आदि अद्वैतवादियों ने सारे विश्व को एक सत्रूप-ब्रह्मरूप या ज्ञानरूप इत्यादि प्रकार से स्वीकार कर लिया है। यहाँ एक प्रश्न हुआ कि प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव आदि अभावों को संग्रहनय कैसे जानेगा ? तब आचार्य ने कहा है कि नैयायिक द्वारा मान्य अभाव तो तुच्छाभावरूप है किन्तु जैनों ने अभाव को भावांतर रूप से स्वीकार किया है जैसे ‘दीपस्तम:१ पुद्गलभावतोऽस्ति’ दीपक के बुझने से अंधकार हो गया तो भी जैसे प्रकाश पुद्गल की पर्याय थी वैसे ही अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है। अथवा ‘खे नास्ति२ पुष्पं तरुषु प्रसिद्धं’ आकाश में पुष्प नहीं है यह कथन सर्वथा अभाव रूप नहीं है क्योंकि पुष्प वृक्षों में तो प्रसिद्ध ही है।
अथवा जीव या उसकी कोई भी पर्याय ‘नहीं है’ ऐसा कहने पर तो यदि असत् स्वरूप है तो ‘है’ कैसे कहा ? और यदि ‘है’ तो असत्स्वरूप उसका कैसे रहा ? इसलिए सभी अभाव कथंचित् भावात्मक ही हैं। ‘न जैन: अजैन:’ जैन नहीं है वह अजैन है यहाँ पर भी नञ् समास में नहीं का अर्थ है कि वह जैन नहीं है किन्तु ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कुछ है।
🏠
प्रत्यक्षं बहिरंतश्च भेदाज्ञानं सदात्मना॥
द्रव्यं स्वलक्षणं शंसेद्भेदात्सामान्यलक्षणात्॥4॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[भेदाज्ञानं प्रत्यक्षं] भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान [सदात्मना] सत्रूप से [बहि: अंत: च] बहिरंग और अंतरंग पदार्थ में [सामान्य लक्षणात्] सामान्य लक्षण वाले [भेदात्] भेद से [द्रव्यं स्वलक्षणं] द्रव्य को वस्तुभूत [शंसेत्] कहता है॥४॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-इंद्रिय और मन से होने वाला विशद ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। वह भेदाज्ञान अर्थात् बौद्धों के द्वारा परिकल्पित भेदों को-निरंश क्षणों को नहीं जानता है-नहीं ग्रहण करता है, ऐसा वह भेद को नहीं ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान सद्रूप से बाह्य-अचेतन घटादि और अंतरंग चेतन में शुद्ध अथवा अशुद्ध द्रव्य को स्वलक्षण-वास्तविक कहता है, कल्पित नहीं कहता है क्योंकि पदार्थों में सत्रूप से भेद प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता है कि जिससे प्रत्यक्षज्ञान द्रव्य को (एकरूप) न कहे।
कैसे ? सामान्य-अन्वय, लक्षण-लिंग है जिसका उस सामान्य लक्षण भेद का आश्रय लेकर कहता है अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अन्य अनुमानादि प्रमाण भेदनिरपेक्ष अभेद को सिद्ध नहीं करते हैं क्योंकि वैसी उपलब्धि नहीं होती है। इस हेतु से प्रत्यक्ष भी द्रव्य सिद्धि का कारण ही है इसलिए संग्रहनय मिथ्या कैसे हो सकेगा ? अर्थात् नहीं हो सकेगा।
भावार्थ-प्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्रूप से किन्हीं भी चेतन-अचेतन पदार्थों में भेद को नहीं करते हुए सत् लक्षण वाले द्रव्य को सिद्ध कर देता है इसलिए सत्सामान्य-सबको एक सत् रूप ग्रहण करने वाला संग्रहनय मिथ्या नहीं है प्रत्युत् समीचीन ही है क्योंकि यहाँ अभेद भी भेद निरपेक्ष विवक्षित नहीं है।
🏠
सदसत्स्वार्थनिर्भासै: सहक्रमविवर्तिभि:॥
दृश्यादृश्यैर्विभात्येकं भेदै: स्वयमभेदकैः॥5॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-जैसे [सदसत् स्वार्थ निर्भासै:] सत्-असत् रूप और अर्थ के आकार से [एकं] ज्ञान एक है, वैसे ही [स्वयं अभेदवैâ:] स्वरूप से भेद नहीं करने वाले ऐसे [सहक्रम विवर्तिभि:] सहभावी और क्रमभावी से तथा [दृश्यादृश्यै:] व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्यायों से [एकं विभाति] एक द्रव्य प्रतिभासित होता है॥५॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-एक द्रव्य रूप से अभिन्न जीवादि वस्तु युगपत् होने वाली सहभावी और क्रम से काल के भेद से होने वाली, परिणमन करने वाली क्रमभावी भेद-गुण पर्यायों से विशेषरूप से प्रत्यक्षादि ज्ञान में प्रतिभासित होती है। ‘१गुणपर्ययवद्द्रव्यं-गुण पर्याय वाला द्रव्य है’ ऐसा सूत्रकार का कथन है। रागादि पर्याय में सहवर्ती हैं। स्वयं-स्वरूप से गुणपर्याय रूप से जिसमें गुण अथवा पर्याय का भेद नहीं है तथा ‘२द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा:’-जो द्रव्य के आश्रित हैं, निर्गुण हैं, वे गुण कहलाते हैं’’ ऐसा वचन है। गुण और पर्यायों को भी गुणपर्यायवत्त्व से द्रव्यत्व का प्रसंग आ जाता है क्योंकि द्रव्य उस लक्षण वाला ही है।
प्रश्न-वे पर्यायें कैसी हैं ?
उत्तर-स्थूल व्यंजन पर्यायों को दृश्य कहते हैं और सूक्ष्म, केवल आगम से जानने योग्य अर्थ पर्यायों को अदृश्य कहते हैं। इन उभयात्मक पर्यायों से द्रव्य अभिन्न है अत: एक है।
इसी अर्थ को पुष्ट करने में परप्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं। यहाँ कारिका के अर्थ में ‘यथा ज्ञान’ इतना पद अध्याहार करना चाहिए। जैसे-एक ज्ञान में स्व और अर्थ के निर्भास-जीवादि आकार सत्-असत् रूप हैं अर्थात् ज्ञानगत आकार सत्रूप हैं और नीलादि अर्थाकार असत् रूप हैं, इन सत्रूप-असत्रूप आकारों से सहित होकर भी चित्रज्ञान एक है यह बात विरुद्ध नहीं है। उसी प्रकार अर्थ व्यंजन पर्यायों से और सहक्रमवर्ती गुण, पर्यायों से सहित एक द्रव्य भी प्रतिभासित हो रहा है, यह बात विरुद्ध नहीं है क्योंकि विरोध तो अनुपलब्धि से सिद्ध होता है तथा द्रव्य और भेद तो उपलब्ध हो रहे हैं।
इसलिए जीवादि वस्तु भेदाभेदात्मक सिद्ध हैं क्योंकि उसी प्रकार से वे ज्ञान का विषय हैं और अर्थ क्रियाकारी हैं। निश्चित ही सर्वथा नित्य अथवा वस्तु अर्थक्रिया को करते हुए प्रतीति में नहीं आती है कि जिससे उसे परमार्थसत् माना जा सके अर्थात् उन नित्य अथवा क्षणिक को वास्तविक नहीं माना जा सकता है।
भावार्थ-सभी वस्तुएँ अपने-अपने अनंत गुण पर्यायों से सहित होकर भी कथंचित् सत् रूप से एक रूप हैं और कथंचित् अपने अस्तित्व से पृथक्-पृथक् होने से अनेक रूप भी हैं इसलिए सभी वस्तुएँ भेदाभेदात्मक ही हैं। सत्ता के दो भेद हैं-महासत्ता और अवांतरसत्ता। महासत्ता सत्सामान्य मात्र से सभी चेतन-अचेतन वस्तु को एकरूप ग्रहण करती है और अवांतर सत्ता अर्थात् प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग अस्तित्व यह सभी वस्तुओं को भेदरूप ग्रहण करता है अतएव वस्तु भेदाभेदात्मक है।
🏠
कार्योत्पत्तिर्विरुद्धा चेत्स्वयंकारणसत्तया॥
युज्येत क्षणिकेऽर्थेऽर्थक्रियासंभवसाधनम्॥6॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[चेत् स्वयं कारणसत्तया] यदि स्वयं कारण की सत्ता से [कार्योत्पत्ति: विरुद्धा:] कार्य की उत्पत्ति विरुद्ध होवे, तब [क्षणिके अर्थे] क्षणिक अर्थ में [अर्थक्रिया संभव साधनं] अर्थक्रिया का होना सिद्ध [युज्येत] किया जा सके॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
(सर्वथा क्षणिक में अर्थक्रिया संभव नहीं है)
तात्पर्यवृत्ति-कार्यरूप उत्तर परिणाम का स्वरूप लाभ होना कार्य की उत्पत्ति है। स्वयं कारणकार्य उत्पन्न करने वाला द्रव्य का स्वरूप उपादान है। उसे स्वयं कारण कहते हैं और उसका अस्तित्व स्वयं कारण सत्ता है। यदि स्वयं द्रव्य स्वरूप उपादान की सत्ता से कार्य की उत्पत्ति विरुद्ध होवे तब क्षणिक अर्थ में अर्थक्रिया के संभव का अनुमान हो सके।
अर्थ-अभिमत प्रयोजन की क्रिया-निष्पत्ति अर्थक्रिया है, उसका संभवसाधन-‘नित्यक्रम यौगपद्य विरहात्’ नित्य में क्रम और युगपत् का अभाव है’ इत्यादि अनुमान है। निरन्तर विनश्वर को क्षणिक कहते हैं अर्थात् क्षणिक-विनश्वर पदार्थ में वह अर्थक्रिया संभव नहीं है।
तथा वह कार्य की उत्पत्ति विरुद्ध नहीं है क्योंकि कार्य के समय सत् रूप ही कारण होता है अन्यथा कार्य को आकस्मिकपने का प्रसंग आ जाएगा और क्षणिवैâकांत में कार्य-कारणभाव का विरोध है। जिसके अभाव में जो उत्पन्न होता है और जिसके सद्भाव में जो उत्पन्न नहीं होता है, उनमें कार्य-कारण भाव नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जायेगा। इस हेतु से कथंचित् सत् को ही कारण अथवा कार्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक ही है, क्योंकि उसी में अर्थक्रिया संभव है।
भावार्थ-बौद्ध का कहना है कि कारण रूप मृत्पिंड का सर्वथा निमूल चूल नाश होकर घटरूप कार्य बनता है। इस पर आचार्यों का कहना है कि स्वयं उपादान कारणरूप मृत्पिंड ही घट कार्य रूप से परिणत होता है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है अतएव सर्वथा क्षणिक सिद्धांत में कार्य-कारण भाव सिद्ध नहीं होता है और न उस क्षणिक वस्तु में इष्ट प्रयोजन के होने रूप अर्थक्रिया ही संभव है अत: वस्तु कथंचित् नित्यानित्यात्मक स्वीकार करना चाहिए।
🏠
यथैकं भिन्नदेशार्थान्कुर्याद् व्याप्नोति वा सकृत्॥
तथैकं भिन्नकालार्थान्कुर्याद् व्याप्नोति वा क्रमात्॥7॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[यथा एकं] जैसे एक-क्षणिक स्वलक्षण [सकृत्] एक क्षण में [भिन्नदेशार्थान्] भिन्न देश वाले कार्यों को [कुर्यात्] करता है [वा] अथवा [व्याप्नोति] व्याप्त करता है [तथा] वैसे ही [एकं] एक द्रव्य [क्रमात्] क्रम से [भिन्न कालार्थान्] भिन्न कालवर्ती कार्यों को [कुर्यात्] करता है [वा व्याप्नोति] अथवा उनको व्याप्त करता है॥७॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जिस अविरोध प्रकार से एक सौगत के द्वारा स्वीकृत क्षणिक स्वलक्षण एक क्षण में भिन्न-विप्रकृष्ट देश वाले कार्यों को ‘स्वसंतानवर्ती को उपादानरूप से और भिन्न संतानवर्ती को निमित्त रूप से उत्पन्न करता है। अथवा जैसे एक ही ज्ञान भिन्न देशार्थ अर्थात् विप्रकृष्ट नीलादि आकारों को व्याप्त करता है इसमें विरोध नहीं है। वैसे ही एक अभिन्न द्रव्य क्रम से काल भेद से पूर्व और अपर काल में होने वाले कार्यों को करता है, पूर्वाकार का परिहार, उत्तर आकार की प्राप्ति और स्थितिरूप से परिणमन करता है अथवा उन्हीं को व्याप्त करता है-उनके साथ तादात्म्य का अनुभव करता है, यह बात विरुद्ध नहीं है।
एक के ही नाना देश के कार्यों को करना अविरुद्ध है किन्तु नाना काल के कार्य को करना विरुद्ध है। यह कथन भी अपने दर्शन का अनुराग मात्र ही है क्योंकि न्याय तो सर्वत्र समान होता है इसलिए जीवादि वस्तु एकानेकादि रूप से अनेकांतात्मक सिद्ध हैं अन्यथा अर्थक्रिया का विरोध हो जावेगा।
भावार्थ-बौद्ध का कहना है कि एक क्षणिक स्वलक्षण भिन्न देशवर्ती कार्यों को उत्पन्न करता है और एक निरंश ज्ञान भिन्न देशवर्ती नीलादि आकारों में व्याप्त होता है किन्तु आचार्य कहते हैं कि वैसे ही सत् रूप से अभिन्न एक द्रव्य पूर्वोत्तर कालवर्ती कार्यों को करता है और उन्हीं को व्याप्त करके उन्हीं में तादात्म्य का अनुभव भी करता है अत: एक अनेक कार्य को नहीं कर सकता या अनेक धर्मों में व्याप्त नहीं रह सकता है ऐसा दोष कहाँ रहा ? भाई, न्याय तो दोनों जगह समान ही रहेगा।
🏠
संग्रह: सर्वभेदैक्यमभिप्रैति सदात्मना॥
ब्रह्मावादस्तदाभास: स्वार्थभेदनिराकृते:॥8॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[संग्रह:] संग्रह नय [सदात्मना] सत्रूप से [सर्वभेदैक्यं] सभी भेदों में ऐक्य को [अभिप्रैति] स्वीकार करता है किन्तु [ब्रह्मवाद:] ब्रह्माद्वैतवाद [तदाभास:] संग्रहाभास है [स्वार्थ भेदनिराकृते:] क्योंकि वह अपने और अर्थ के भेदों का निराकरण करता है॥८॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-संग्रहनय सभी भेदरूप द्रव्यादि के ऐक्य-अभेद को ‘सर्वं सत्-सभी सत्रूप हैं’ इस सत्रूप से विषय करता है। ‘सत्सामान्यात्तु सर्वैक्यं१’ सत्सामान्य से सभी में ऐक्य-अभेद है’ ऐसा श्री समंतभद्रस्वामी का वचन है। सर्वथा सभी वस्तु एक रूप नहीं है क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती है।
शंका-इस प्रकार से तो आपने ब्रह्मवाद का ही समर्थन कर दिया है ?
समाधान-नहीं। वह सत्ता द्वैतरूप भावैकांत ही ब्रह्मवाद है अत: वह संग्रहाभास है।
शंका-क्यों ?
समाधान-क्योंकि वह अपने ब्रह्मवाद विषय के भेदों का निराकरण करने वाला है। स्व-अपने ब्रह्मवाद का अर्थ-विषय, सन्मात्र, उसके भेद-जीवादि विशेषों का निराकरण-निषेध करने वाला है। निश्चित ही सर्वथा सत्रूप में भेदों को अवकाश नहीं है और भेद रहित वह सामान्य कैसे रह सकता है क्योंकि निराश्रय रूप है और अर्थक्रिया से रहित है। नैवंâ२ स्वस्मात् प्रजायते-’ एक ही ब्रह्म अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकता है’ ऐसा न्याय है। उस ब्रह्माद्वैत में क्रिया कारक का भेद भी नहीं है कि जिससे अर्थक्रिया संभव हो सके अर्थात् नहीं हो सकती है।
भावार्थ-ब्रह्माद्वैतवादी का कहना है कि सभी चेतन-अचेतन रूप जगत् सत्रूप है वह सन्मात्र शरीरधारी परम ब्रह्म ही है।
🏠
अन्योन्यगुण भूतैकभेदाभेदप्ररूपणात्॥
नैगमोऽर्थांतरत्वोक्तौ नैगमाभास इष्यते॥9॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[अन्योन्यगुणभूतैकभेदाभेद प्ररूपणात्] परस्पर में गौणभूत और प्रधानभूत भेद तथा अभेद का प्ररूपण करने से [नैगम:] नैगमनय है। [अर्थांतरोक्तौ] और द्रव्य से गुणादि को भिन्न कहने पर [नैगमाभास:] नैगमाभास [इष्यते] माना जाता है॥९॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-निगम-मुख्य गौण कल्पना, उसमें होने वाला नय ‘‘नैगम’’ कहलाता है, ऐसा स्याद्वादियों ने स्वीकार किया है। अन्योन्य-परस्पर में गुणभूत-अप्रधानभूत और एक-प्रधानभूत भेद- अभेद का प्ररूपण करता है अर्थात् गुण-गुणी में, अवयव-अवयवी में, क्रिया-कारकों में और सामान्यसामान्यवान् में कथंचित् भेद को गौण करके अभेद का प्ररूपण करता है अथवा अभेद को गौण करके भेद को प्ररूपित करता है, यह नैगमनय इस प्रकार का है। प्रमाण में भेद और अभेद का अनेकांत ग्रहण होता है।
शंका-गुण-गुणी आदि में अत्यंत भेद ही है ?
[समाधान-गुण और गुणी में अर्थांतर-अत्यंत भेद प्ररूपित करने पर तो वह नैगमाभास माना जावेगा क्योंकि वह अत्यंत भेद प्रमाण से बाधित है। निश्चित ही द्रव्य से अत्यन्त भिन्न गुण आदि प्रतीति में नहीं आते हैं क्योंकि द्रव्य से गुणादि का अशक्य विवेचन होने से उनमें तादात्म्य प्रतीत हो रहा है और उन्हें अत्यन्त भिन्न मानने पर उनमें संबंध का अभाव है।
भावार्थ-वैशेषिक का कहना है कि अग्नि द्रव्य से उष्ण गुण सर्वथा भिन्न है, वस्त्र के सूतरूप अवयवों से वस्त्र अवयवी भी भिन्न है, सत् सामान्य से सत्सामान्य वाली वस्तु भी भिन्न है किन्तु आचार्यों का कहना है कि इस प्रकार से द्रव्यादि से गुणादि का अलग अस्तित्व प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए द्रव्य से गुणादि को भिन्न कहने में वह नैगमनय नहीं रहकर नैगमाभास हो जाता है।
🏠
स्वतोऽर्था: संतु सत्तावत्सत्तया किं सदात्मनां॥
असदात्मसु नैषा स्यात्सर्वथाऽतिप्रसंगत:॥10॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ सत्तावत् अर्था: स्वत: संतु] सत्ता के समान पदार्थ स्वत: विद्यमान होवें, पुन: [सदात्मनां सत्तया किं] सत्रूप पदार्थों में सत्ता से क्या प्रयोजन है ? [असदात्मसु एषा न स्यात्] असत् रूप पदार्थों में भी वह सत्ता नहीं हो सकती है [सर्वथा अतिप्रसंगत:] सब प्रकार से अतिप्रसंग दोष आता है॥१०॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-यौगमत में स्वत: सत् स्वरूप पदार्थों में सत्ता समवाय होता है या असत् स्वरूप पदार्थों में सत्ता समवाय है ? इस प्रकार के दो विकल्प को मन में रखकर प्रथम पक्ष में दूषण देते हैं-
स्वत: स्वरूप से सत्तावत् पदार्थ होवें अर्थात् जैसे सत्तांतर के बिना भी सत्ता-परसामान्य स्वत: ही है, उसी प्रकार द्रव्यादि भी स्वत: ही होवें और उस प्रकार से स्वत: सत् स्वरूप के सत्ता से क्या प्रयोजन है? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं है यह अर्थ हुआ क्योंकि उस सत्ता के बिना भी उन पदार्थों का सत्त्व है।
अब द्वितीय विकल्प को दूषित करते हुए कहते हैं -
सर्व था असत् स्वरूप द्रव्यादिकों में अन्य कोई सत्ता है नहीं अन्यथा अतिप्रसंग आ जावेगा। सर्वथा असत् रूप खर, विषाण आदि में भी सत्ता समवाय हो जाना चाहिए।
एवं द्रव्यत्वादि समवाय का भी इसी प्रक्रिया से विचार करना चाहिए अर्थात् प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य में स्वत: द्रव्यत्व है या नहीं ? यदि द्रव्य में स्वत: द्रव्यत्व है तो द्रव्यत्व का समवाय अनर्थक है और यदि नहीं है अर्थात् वह द्रव्य अद्रव्य है तब तो उसमें अद्रव्य में द्रव्यत्व का समवाय मानने पर अतिप्रसंग दोष आ जाता है।
दूसरी बात यह है कि अवयवी अवयवों में एकदेश से रहता है या सर्वात्मदेश से रहता है ? यदि प्रथम पक्ष लो कि वह अवयवी अवयवों में एकदेश से रहता है तब तो उस अवयवी को जितने कि अवयव हैं उतने ही अंशों से होना चाहिए अन्यथा सभी अवयवों को एकत्व का प्रसंग आ जावेगा। यहाँ पर भी रहना मानने पर तो फिर उस अवयवी के उतने ही अंश कल्पित करने पर अनवस्था हो जावेगी।
यदि आप कहें कि अवयवी अवयवों में संपूर्ण रूप से रहता है तब तो अवयवी को बहुत मानना पड़ेगा अन्यथा रहने का विरोध हो जावेगा इसलिए उन गुण-गुणी आदि में कथंचित् तादात्म्य लक्षण समवाय स्वीकार करना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं, यह बात व्यवस्थित हो गई।
विशेषार्थ-प्रत्येक वस्तु में कथंचित् तद्भाव लक्षण अभिन्न रूप एक संबंध दिख रहा है जैसे कि जीव का ज्ञान गुण जीव से अभिन्न है, तद्भावरूप है और अग्नि का उष्ण गुण भी अभिन्न है। इसे ही जैनों ने तादात्म्य लक्षण संबंध कहा है कि जिसको कभी भी वस्तु से अलग नहीं कर सकते हैं। यौग ने अकारण ही इस अभिन्न रूप अयुत लक्षण संबंध को समवाय नाम देकर पृथक् से सिद्ध करना चाहा था किन्तु जैनाचार्यों का कहना है कि कथंचित् तादात्म्य लक्षण संबंध को ही आप समवाय नाम दे दीजिए, कोई बाधा नहीं है।
🏠
प्रामाण्यं व्यवहाराद्धि स न स्यात्तत्त्वतस्तयो:।
मिथ्यैकांते विशेषो वा क: स्वपक्षविपक्षयो:॥11॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[व्यवहारात् हि प्रामाण्यं] निश्चित रूप से व्यवहार से प्रमाणता होती है। [तयो:] इन ब्रह्मवाद और भेद में [स: तत्त्वत: न स्यात्] वह व्यवहार वास्तविक नहीं है। [वा] अथवा [मिथ्यैकांते] इस व्यवहार को एकांत से मिथ्या मानने पर [स्वपक्ष विपक्षयो:] स्वपक्ष और विपक्ष में [का विशेष:] क्या अंतर रहेगा ?॥११॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-अपने इष्ट के साधन और अनिष्ट के दूषण में निमित्तक प्रत्यक्ष अथवा अन्य- अनुमान आदि प्रमाण हैं, इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा अतिप्रसंग आ जावेगा और वह प्रमाण व्यवहार से उन दोनों में वास्तविक नहीं है अर्थात् विधिपूर्वक अवहरण-विभाग करना-भेद कल्पना करना व्यवहार कहलाता है। इस व्यवहार का आश्रय लेकर संग्रहाभास और नैगमाभास में प्रमाणता परमार्थ से नहीं है।
निश्चित ही निरपेक्ष भावैकांत में प्रमाण आदि भेद व्यवहार नहीं है, इसका पहले निराकरण कर दिया है। भेदैकांत में भी प्रमाण और प्रमाण के फल का व्यवहार नहीं है क्योंकि उसमें संबंध का अभाव है।
प्रश्न-उनमें औपचारिक प्रमाण और फल का व्यवहार है ?
उत्तर-भेद एकांत के पक्ष में यदि आप प्रमाण और फल के व्यवहार को एकांत से अवास्तविक स्वीकार करते हैं तब तो स्वपक्ष और परपक्ष में क्या अंतर होगा ? अर्थात् कुछ भी अंतर नहीं होगा।
ब्रह्मवादी के पक्ष में ब्रह्मवाद स्वपक्ष है और क्षणिकवाद विपक्ष है। यौग के पक्ष में भेदवाद स्वपक्ष है और अद्वैतवाद विपक्ष है।
भेदैकांत में प्रमाण, फल आदि व्यवहार को मिथ्या मानने पर तो स्वपक्ष और परपक्ष में संकर का प्रसंग आ जावेगा इसलिए कथंचित् प्रमाणादि व्यवहार भी वास्तविक स्वीकार करना चाहिए।
विशेषार्थ-ब्रह्मवादी का कहना था कि हमारे यहाँ प्रमाणादि व्यवहार संभव हैं पुन: हमारे ब्रह्मवाद को विषय करने वाला नय संग्रहाभास कैसे होगा ? ऐसे ही यौग ने कहा कि हमारे भेद पक्ष में भी प्रमाणादि व्यवहार होते हैं पुन: हमारे मत के पदार्थों को जानने वाला नय नैगमाभास कैसे कहलाएगा ? आचार्यों ने कहा कि यह प्रमाण आदि का कथन व्यवहार मात्र से ही है अर्थात् कल्पित ही है किन्तु वास्तविक नहीं है, पुन: उस कल्पित मात्र प्रमाण आदि की व्यवस्था से स्वपक्ष और परपक्ष में अंतर सिद्ध करना असंभव हो जावेगा इसलिए प्रमाण आदि व्यवहार को आप कल्पित मत कहिए और वास्तविक प्रमाण आदि व्यवस्थाएँ जहाँ हैं वहाँ एकांत मान्यता को गुंजाइश नहीं है।
🏠
व्यवहारोऽविसंवादी नय: स्याद्दुर्नयोऽन्यथा।
बहिरर्थोऽस्ति विज्ञप्तिमात्रशून्यमितीदृश:॥12॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[बहि: अर्थ: अस्ति] ‘बाह्य पदार्थ है’ ऐसा [अविसंवादी व्यवहार:] अविसंवादी व्यवहार [नय:] स्यात् नय है। [अन्यथा] अन्य प्रकार से [विज्ञप्तिमात्र शून्यं] तत्त्व विज्ञानमात्र या शून्यमात्र है [इति ईदृश:] इस प्रकार ऐसा व्यवहार [दुर्नय:] दुर्नय है॥१२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-‘बाह्य अर्थ है’ इस प्रकार ग्रहण करने वाले होने से संग्रह आदि नय साध्य-साधन भावस्वरूप प्रमाणीक हैं क्योंकि ये व्यवहार में अविसंवादी हैं। कारण-कार्यभाव आदि व्यवस्था को व्यवहार कहते हैं, इस व्यवहार में ये विसंवादरहित, अव्यभिचारी हैं। व्यवहार के सुनयरूप होने पर उस व्यवहार के आधीन कारण-कार्यभाव आदि की सिद्धि होती है, अन्यथा-व्यवहार में विसंवादी होने से वे दुर्नय हो जाते हैं।
प्रश्न-कैसे दुर्नय होते हैं ?
उत्तर-विज्ञानमात्र ही तत्त्व है, अन्य कुछ नहीं है। सब कुछ शून्य ही है-समस्त ज्ञान और ज्ञेय का अभाव ही शून्य तत्त्व है। इस प्रकार कहने वाले नय दुर्नय हैं। यहाँ कारिका में ‘इति’ शब्द प्रकारवाची है, ‘सन्मात्र-परमब्रह्म ही तत्त्व है’। ‘विभ्रम ही तत्त्व है’ इत्यादि प्रकारों को सूचित करता है।
प्रश्न-सुनय कैसे है ?
उत्तर-संग्रहनय संग्रह रूप से ‘सब कुछ सत्रूप है क्योंकि सभी वस्तु में सत् से अभेद है’ इस प्रकार सभी में एकत्व स्वीकार करता है किन्तु व्यवहारनय उन्हीं में विधिपूर्वक भेद करता है, जैसे जो सत् है वह द्रव्य है अथवा पर्याय है। पुन: अपरसंग्रह ‘जीवादि द्रव्य हैं’ इस प्रकार संग्रह करता है तथा ‘ज्ञान और रागादिभाव पर्याये हैं’ इस प्रकार संग्रह करता है। पुन: अपर व्यवहारनय जो द्रव्य है वह जीव अथवा अजीव है और जो पर्याय हैं वे सहभावी तथा क्रमभावी होती हैं। इस प्रकार परसंग्रह-अपर संग्रह, पर व्यवहार-अपर व्यवहार की परम्परा चलती रहती है, जब तक कि ऋजुसूत्र का विषय नहीं आ जाता है।
विशेषार्थ-संग्रहनय वस्तु को संग्रहरूप से विषय करता है और व्यवहारनय उसमें भेद करता है। संग्रहनय के दो भेद हैं-परसंग्रह और अपरसंग्रह। इन्हीं को सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह भी कहते हैं। सामान्य संग्रह सामान्य से चेतन-अचेतन सभी वस्तु को सत् रूप से एकरूप ग्रहण करता है और विशेष संग्रह जीव को द्रव्यरूप से कहता है अथवा अजीव को द्रव्यरूप से कहता है। व्यवहार नय के भी मुख्य दो भेद हैं-पर व्यवहार, अपर व्यवहार। पर संग्रह से ग्रहण किये गये में भेद करने वाला पर व्यवहार है और अपर संग्रह से ग्रहण किये गये में भेद करने वाला अपर व्यवहार है। इन दोनों नयों की परम्परा तब तक चलती रहती है कि जब तक वर्तमान एक समय मात्र की एक पर्याय को विषय करने वाला ऋजुसूत्र नहीं आ जाता है।
इस प्रकार से एक ब्रह्ममात्र अथवा ज्ञानमात्र तत्त्व आदि को ग्रहण करने वाले दुर्नय कहलाते हैं और वस्तु के एक अंश-धर्म को ग्रहण कर अन्य धर्म का विरोध नहीं करने वाले सुनय कहे जाते हैं।
यहाँ पर वृत्तिकार ने द्रव्य और पर्यायों को ही ग्रहण करके पर्यायों में सहभावी-क्रमभावी ऐसे दो भेद दिखलाये हैं। उनमें सहभावी पर्यायें ही गुण कहलाती हैं और क्रमभावी पर्यायें पर्याय शब्द से जानी जाती हैं।
🏠
ऋजुसूत्रस्य पर्याय: प्रधानं चित्रसंविद:॥
चेतनाणुसमूहत्वात्स्याद्भेदानुपलक्षणं॥13॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ऋजुसूत्रस्य प्रधानं पर्याय:] ऋजुसूत्र का विषय पर्याय है और [चित्रसंविद:] चित्रज्ञान में [चेतनाणुसमूहत्वात्] ज्ञान के अंशों का समूह होने से उसमें [भेदानुपलक्षणं स्यात्] भेद उपलक्षित नहीं होता है॥१३॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-ऋजु अर्थात् प्रगुण-सरल वर्तमान पर्याय के लक्षण को जो सूचित करता है निरूपित करता है वह ऋजुसूत्रनय है अर्थात् ऋजुसूत्रनय का प्रधान-विषय वर्तमान पर्याय मात्र है क्योंकि अतीत पर्यायें विनष्ट हो चुकी हैं और भविष्यत् पर्यायें अभी-अभी उत्पन्न नहीं होने से असिद्ध हैं अत: ये अतीतानागत पर्यायें व्यवहार में उपयोगी नहीं हैं। ‘नय व्यवहार में अविसंवादी होते हैं’ ऐसा वचन है।
प्रश्न-एक चित्रज्ञान अनेकाकार है फिर भी व्यवहार में उपयोगी है।
उत्तर-नील, पीतादि नानारूप चित्र वाला संवेदन-ज्ञान चित्रज्ञान है, वह चेतना के अणुओं का समूह है अर्थात् चेतना-ज्ञान, उसके जो अणु-अंश-अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उन ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों का समुदाय है इसलिए यह चित्रज्ञान वास्तव में ऋजुसूत्र नय का विषय नहीं है क्योंकि समुदाय प्रतिनियत व्यवहार में उपयोगी नहीं होता है।
प्रश्न-यदि ऐसी बात है तो उस चित्रज्ञान में भेद उपलक्षित क्यों नहीं होता है ?
उत्तर-उस चित्रज्ञान का भेद उपलक्षित नहीं होता है क्योंकि सदृश पर-अपर की उत्पत्ति होने से भ्रम हो जाता है अर्थात् भेदों में अनेक प्रकार उपलक्षित नहीं हैं-दिखते नहीं हैं, उसमें कारण यही है कि सदृश अपर-अपर की उत्पत्ति होने से उन भेदों को ग्रहण करने में बुद्धि वंचित हो जाती है, ऐसा अर्थ है। जिस प्रकार लोहे के गोले आदि मेें पर्याय का भेद विद्यमान होते हुए भी भ्रमबुद्धि से निश्चित नहीं होता है उसी प्रकार से चित्रज्ञान में भी उसके अंश भेद रहते हुए भी दिखते नहीं हैं।
अथवा कथंचित् द्रव्य के साथ अविनाभावी पर्याय ही ऋजुसूत्र नय का विषय है क्योंकि द्रव्य से निरपेक्ष पर्याय अवस्तुरूप है। निरन्वय वस्तु को मानने वाले क्षणिवैâकांत मत में यह नय ऋजुसूत्राभास है अर्थात् द्रव्यनिरपेक्ष पर्याय को विषय करने वाला नय ऋजुसूत्राभास कहलाता है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए।
विशेषार्थ-बौद्धों ने निरन्वय एक क्षणवर्ती पर्याय को स्वलक्षण कहा है और परमार्थसत् कहते हैं तथा उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं किन्तु वास्तव में विचार करके देखा जाये तो जैनों द्वारा मान्य ऋजुसूत्रनय एक क्षणवर्ती पर्याय को विषय करता है इसी नय के विषय को एकांत से ग्रहण करने से ये बौद्ध एकांतवादी बन गये हैं इसलिए यह ऋजुसूत्रनय इनके मत से नयाभास हो जाता है।
🏠
कालकारकलिंगानां भेदाच्छब्दार्थभेदकृत्॥
अभिरूढस्तु पर्यायैरित्थंभूत: क्रियाश्रय:॥14॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[कालकारकलिंगानां] काल, कारक और लिंगों के [भेदात्] भेद से [शब्दार्थ भेद कृत्] अर्थ में भेद को करने वाला शब्दनय है [पर्यायै: तु अभिरूढ़:] और पर्यायवाची शब्दों से भेद करने वाला समभिरूढ़नय है तथा [क्रियाश्रय: इत्थंभूत:] क्रिया के आश्रय से भेद करने वाला एवंभूतनय है॥१४॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जो अर्थ-प्रमेय में भेद-नानात्व को करने वाला है वह शब्द नय है। कैसे भेद करता है ? काल, कारक और लिंगों के भेद से भेद करता है। यह कथन उपलक्षणमात्र है अत: संख्या, साधन और उपग्रह से भी यह नय अर्थ में भेद करता है, ऐसा समझना। उसमें काल भेद को दिखाते हैं -
जीव था, है और होगा यह काल भेद है क्योंकि सत्ता भेद के बिना अभूत-था आदि प्रयोग युक्त नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग हो जावेगा। कारक भेद से-देवदत्त देखता है, देवदत्त के द्वारा देखा जाता है, देवदत्त रक्षा करता है, देवदत्त के द्वारा दिया जाता है, देवदत्त से प्राप्त होता है, देवदत्त में पुरुषार्थ है। स्वातन्त्र आदि धर्म के भेद से अभेद में कर्ता आदि कारकों का प्रयोग युक्त नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग हो जावेगा।
लिंग भेद से-दारा पुल्लिंग है, कलत्र नपुंसकलिंग है और भार्या ध्Eाीलिंग है, इनमें पुल्लिंग आदि धर्म से भेद होने पर भी इनका प्रयोग करने पर सर्वत्र उसके नियम के अभाव का प्रसंग हो जावेगा।
संख्या के भेद से-जलं एक वचन है, आप: बहुवचन है, आम्रवनं एकवचन है, चैत्रमैत्रौ द्विवचन है, कुलं एक वचन है। यहाँ एकत्व आदि धर्म के भेद से ही उन वचनों में भेद पाया जाता है अन्यथा अतिप्रसंग ही होगा।
साधन के भेद से-देवदत्त पकाता है, तुम पकाते हो, मैं पकाता हूँ। इस प्रकार निश्चित ही अन्य अर्थ आदि के अभाव में प्रथम पुरुषादि का प्रयोग नहीं देखा जाता है अन्यथा अतिप्रसंग ही है। उपग्रह के भेद से भी अर्थ में भेद देखा जाता है। जैसे तिष्ठति-ठहरता है, वितिष्ठते-जाता है, अवतिष्ठते-बैठता है। इस प्रकार से ‘वि अव’ आदि उपसर्गों का परस्पर में भेद होने से अर्थ में भेद हो जाता है अन्यथा प्रतिष्ठते-प्रस्थान करता है, इत्यादि में भी वही ठहरता है, ऐसे अर्थ का प्रसंग आ जावेगा।
अब कारिका के उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हैं -
पर्यायवाची शब्दों से अर्थ में भेद को करने वाला समभिरूढ़ नाम का नय है। जैसे-चमकने से इंद्र,समर्थ होने से शक्र, पुरों में विभाग करने से पुरंदर इस प्रकार अर्थ होते हैं। यहाँ इंद्रन आदि धर्म में भेद का अभाव होने पर इंद्र आदि का प्रयोग करना शक्य नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग हो जाता है। अभि-अपने अर्थ की तरफ अभिमुख होकर जो रूढ़ है-प्रसिद्ध है वह अभिरूढ़ नय है ऐसा निरुक्ति अर्थ है।
पुन: इत्थंभूत नय को कहते हैं-यह नय क्रिया के आश्रित है, विवक्षित क्रिया को प्रधान करता हुआ अर्थ में भेद को करने वाला है। जैसे-जिस समय ही इंद्रन क्रिया से युक्त है उसी काल में इंद्र है। वह न अभिषेक करने वाला है, न पुजारी है। यदि अन्य प्रकार से भी उसका सद्भाव मानेंगे तो क्रिया के शब्द के प्रयोग का नियम नहीं रह सकेगा इसलिए अर्थ में भेद का अभाव होने पर भी कालादि का भेद अविरुद्ध है, इस प्रकार का वैयाकरण का जो एकांत है। वह शब्दनयाभास आदि रूप है।
प्रश्न-इस प्रकार से तो लोक समय-व्याकरणशास्त्र में विरोध आ जाता है ?
उत्तर-लोक समय में विरोध होता है तो होवे, यहाँ तो तत्त्व के विचार में लोक समय की इच्छा के अनुसरण का अभाव है। औषधि रोगी की इच्छा के अनुरूप नहीं होती है।
प्रश्न-पुन: उस विरोध का अभाव कैसे होगा ?
उत्तर-स्यात्कार के बल से उस विरोध की समाप्ति हो जाती है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि सर्वत्र प्रतिपक्ष की आकांक्षारूप उस स्यात्कार का अर्थ संभव है।
नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीन नय द्रव्य को विषय करने वाले होने से द्रव्यार्थिक हैं और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत ये चार नय पर्याय को विषय करने वाले होने से पर्यायार्थिक हैं। ये सभी नय परस्पर में एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हुए ही व्यवहार के लिए प्रवृत्त होते हैं परस्पर में निरपेक्ष होकर नहीं, इसलिए व्यवहार की उपलब्धि में किस प्रकार से विरोध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है।
नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार अर्थ नय कहलाते हैं तथा शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ये तीन नय शब्द नय कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्रवृत्ति शब्द के आश्रय से होती है।
विशेषार्थ-इस कारिका में शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत इन तीन नयों का स्वरूप बताया है। यहाँ तक नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत इन सात नयों का स्वरूप हो चुका है। पूर्व के तीन नय द्रव्य को जानने वाले हैं इसीलिए वे द्रव्यार्थिक कहलाते हैं तथा शेष ऋजुसूत्र आदि चार नय पर्याय को जानने वाले हैं इसलिए पर्यायार्थिक कहलाते हैं।
उसी प्रकार नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चारों पदार्थों को करने करने से अर्थ नय हैं और शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत ये नय शब्द के निमित्त से पदार्थ को विषय करते हैं अत: ये शब्दनय कहे जाते हैं।
🏠
अक्षबुद्धिरतीतार्थं वेत्ति चेन्न कुत: स्मृति:॥
प्रतिभासभिदैकार्थे दूरासन्नाक्षबुद्धिवत्॥15॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[चेत् अक्षधी:] यदि इंद्रियज्ञान [अतीतार्थं] अतीत अर्थ को [वेत्ति] जानता है तब तो [दूरासन्नार्थबुद्धिवत्] दूर और निकटवर्ती पदार्थ के ज्ञान के समान [एकार्थे] एक विषय में [प्रतिभासमिदा] प्रतिभास के भेद से [स्मृति: कुत: न] स्मृति ज्ञान प्रमाण कैसे नहीं होगा ?॥१५॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-सौगत के मत में विषय को ज्ञान का कारण माना है और कार्य के क्षण से पूर्व क्षणवर्ती को कारण कहते हैं। इस प्रकार से यदि ज्ञान अतीत अर्थ अर्थात् स्वकारणभूत शब्द और वाच्य को जानता है तब किस कारण से स्मृति भी अतीत अर्थ को नहीं जानती है ? अपितु जानती ही है।
शंका-इस प्रकार से तो स्मृति को प्रमाणता कैसे है क्योंकि वह तो गृहीत को ग्रहण करने वाली है ?
समाधान-एक-अभिन्न अतीतपने रूप विशेषता से रहित होने से साधारण जो शब्दार्थ लक्षण वाला विषय है वह अर्थ कहलाता है उस एक अर्थ में भी अतीताकार को परामर्श करने वाले प्रतिभास के भेद से वह स्मृति प्रमाण है।
प्रत्यक्ष से ही जो ‘यह’ इस प्रकार से अनुभव में आता है वही कालांतर में पुन: ‘तत्-वह’ इस आकार से स्मृतिज्ञान के द्वारा विषय किया जाता है। जैसे-दूर और निकटवर्ती पदार्थ का ज्ञान अर्थात् जिस प्रकार से दूरवर्ती वृक्ष में प्रत्यक्ष ज्ञान अस्पष्ट होता है और निकटवर्ती वृक्ष में स्पष्ट होता है। जैसे-दूर और निकटवर्ती वृक्षादि में प्रत्यक्ष ज्ञान अस्पष्ट और स्पष्ट प्रतिभास के भेद से प्रमाण है उसी प्रकार से स्मृति भी प्रमाण है यह अर्थ हुआ है।
🏠
अक्षशब्दार्थविज्ञानमविसंवादत: समं।
अस्पष्टं शब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानवत्॥16॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[अक्षशब्दार्थविज्ञानं] इंद्रिय से होने वाला अर्थ का ज्ञान और शब्द से होने वाला अर्थ का ज्ञान [अविसंवादत:] ये दोनों अविसंवाद की अपेक्षा से [समं] समान हैं, [शब्दज्ञानं] शब्दज्ञान [अनुमानवत्] अनुमान के समान [अस्पष्टं] अस्पष्ट [प्रमाणं] प्रमाण है॥१६॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-अक्षार्थ विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान समान प्रमाण है। अक्ष अर्थात् इंद्रिय, शब्द अर्थात् वर्ण पदवाक्यात्मक ध्वनि। अर्थ अर्थात् सामान्य विशेषात्मक वस्तु अर्थात् इंद्रिय से होने वाला वस्तु का ज्ञान और शब्द से होने वाला वस्तु का ज्ञान दोनों ही समान प्रमाण हैं। ये दोनों ही वि-विशिष्ट हैं अर्थात् संशयादि से रहित हैं और ये अविसंवादी हैं अर्थात् अर्थक्रिया में व्यभिचरित नहीं होते हैं। जैसे-इंद्रिय से उत्पन्न हुआ अर्थज्ञान अविसंवादी होने से प्रमाण है वैसे ही शब्द से उत्पन्न होने वाला अर्थज्ञान भी अविसंवादी होने से प्रमाण है, ऐसा अर्थ हुआ।
अनाप्त के वचन से उत्पन्न हुआ ज्ञान अर्थक्रिया में विसंवादी होने से अप्रमाण है, इसी प्रकार आप्त के वचन से उत्पन्न हुए ज्ञान को अप्रमाण कहना शक्य नहीं है क्योंकि इन्द्रियज्ञान में भी कहीं पर विसंवाद देखा जाता है और एक जगह विसंवाद देखकर सभी जगह अप्रमाणीक कहने पर तो सर्वत्र ही अप्रमाणता की आशंका बनी रहेगी।
शंका-इंद्रियज्ञान प्रमाण है क्योंकि वह स्पष्ट है, शब्द ज्ञान-आगमज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि वह अस्पष्ट है ?
समाधान-अस्पष्ट-अविशद भी शब्दज्ञान को प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि वह अविसंवादी है। कारण कि अविसंवाद हेतु ही प्रमाणता को घोषित करता है। स्पष्टता अथवा अस्पष्टता प्रमाणता और अप्रमाणता में निमित्त नहीं है क्योंकि इन प्रमाणता और अप्रमाणता में अविसंवाद और विसंवाद ही निमित्त है। जैसे-अनुमानज्ञान अस्पष्ट होते हुए भी विसंवाद का अभाव होने से प्रमाण माना जाता है। उसी प्रकार शब्द से होने वाला आगम ज्ञान भी भले ही अस्पष्ट हो किन्तु उसे प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि वह भी अविसंवादी है। यह अविसंवादी हेतु दोनों जगह समान ही है।
🏠
कालादिलक्षणं न्यक्षेणान्यत्रेक्ष्यं परीक्षितं।
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषात्मार्थनिष्ठितम्॥17॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[कालादिलक्षणं] काल आदि के लक्षण को [न्यक्षेण] विस्तार से [अन्यत्र परीक्षितं] अन्य ग्रंथों में परीक्षित को [ईक्ष्यं] देख लेना चाहिए [द्रव्यपर्याय सामान्य विशेषात्मार्थ निष्ठितं] जो कि द्रव्य-पर्याय और सामान्य विशेषरूप पदार्थ में विद्यमान है॥१७॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-काल, कारक, लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह आदि का असाधारण स्वरूप जो कि स्वामी समंतभद्र आदि आचार्यों के द्वारा परीक्षित है उसे न्यक्ष अर्थात् विस्तार से देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए ? अन्य तत्त्वार्थमहाभाष्य आदि ग्रंथों में देखना चाहिए। वह कैसा है ?
पूर्वापर परिणाम में व्यापक ऊध्र्वतासामान्य को द्रव्य कहते हैं और एक द्रव्य में क्रम से होने वाले जो परिणाम हैं वे पर्यायें कहलाती हैं। वे द्रव्य और पर्यायें तथा सामान्य और विशेष ये हैं स्वरूप जिसके उसे द्रव्यपर्याय सामान्य विशेषात्मक कहते हैं और वही अर्थ-पदार्थ है उसमें जो लक्षण निष्ठित अर्थात् स्थित है वह द्रव्य पर्याय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ में रहने वाला असाधारण लक्षण है उसे जानना चाहिए।
इस प्रकार के पदार्थ में ही अर्थक्रिया संभव हैं क्योंकि निरपेक्ष एकांत में उस अर्थक्रिया का विरोध है। पर्यायरहित केवल द्रव्य नहीं है अथवा द्रव्य से व्यतिरिक्त पर्याय भी नहीं है। विशेष से शून्य सामान्य नहीं है अथवा सामान्य से शून्य विशेष नहीं है अर्थात् ये एक-दूसरे से रहित होते हुए प्रमाण की पदवी पर आरोहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती है जिससे कि वे काल, कारक आदि एकांतरूप से हो सकें अर्थात् नहीं हो सकते हैं।
उनमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान के भेद से काल के तीन भेद हैं जो क्रिया का निर्वर्तक-करने वाला है वह कारक है उसके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के भेद से छह भेद हैं। शब्द की प्रवृत्ति में निमित्तभूत जो अर्थ का धर्म है वह लिंग कहलाता है, उसके भी स्त्री, पुरुष और नपुंसक के भेद से तीन भेद हैं। संख्या के भी एकत्व, द्वित्व और बहुत्व के भेद से तीन भेद हैं। साधन क्रिया के आश्रित है उसके भी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अर्थ के भेद से तीन भेद हैं। प्र, पर आदि उपसर्ग को उपग्रह कहते हैं वह अनेक प्रकार का है।
विशेषार्थ-यहाँ पर आचार्यश्री भट्टाकलंक देव का यह कहना है कि जो काल, कारक आदि का लक्षण है, जो कि द्रव्य पर्यायरूप सामान्य विशेषात्मक पदार्थ में रहता है उसको विस्तार से यदि आप जानना चाहते हैं तो श्री स्वामी समंतभद्राचार्य के द्वारा प्रणीत तत्त्वार्थ महाभाष्य नामक ग्रंथ में देखना चाहिए। यहाँ पर इनका लक्षण संक्षिप्त में कहा गया है।
🏠
एकस्यानेकसामग्रीसन्निपातात्प्रतिक्षणं॥
षट्कारकी प्रकल्प्येत तथा कालादिभेदत:॥18॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[एकस्य] एक में [अनेक सामग्री सन्निपातात्] अनेक सामग्री के सन्निधान से [प्रतिक्षणं]प्रतिक्षण [षट्कारकी] षट् कारकों की [प्रकल्प्येत] कल्पना होती है, [तथा कालादिभेदत:] वैसे ही काल आदि के भेद से भी षट्कारक की व्यवस्था होती है॥१८॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-एक जीवादि वस्तु में भी छहों कारकों के समुदायरूप षट्कारक व्यवस्था प्रत्येक समय में घटित हो जाती है। कैसे ? अनेक सामग्री के सन्निपात होने से अर्थात् अनेक अंतरंग और बहिरंग, सामग्री कारण कलापों की सन्निधि होने से षट्कारकी घटित होती है। उसी को कहते हैं-जिस काल में चाक, चीवर आदि की सन्निधि होने से देवदत्त घट को करता है उसी काल में अपने प्रेक्षकजन के सन्निधान से वही देखा जाता है इसलिए वह कर्म है। प्रयोजन की अपेक्षा से देवदत्त के द्वारा कराता है इसलिए करण है। देने योग्य द्रव्य की अपेक्षा से देवदत्त को देता है इसलिए संप्रदान है। अपाय की अपेक्षा से देवदत्त से दूर होता है यह अपादान है। वहाँ पर स्थित द्रव्य की अपेक्षा से देवदत्त में कुण्डल है इस प्रकार अधिकरण है, इस प्रकार अविरोध से वैसी प्रतीति हो रही है क्योंकि प्रतीति में आते हुए विषय में विरोध नाम की कोई चीज नहीं है।
उसी प्रकार से युगपत् के समान ही काल, देश और आकार के भेद से, क्रम से भी षट्कारक रूप व्यवस्था होती है। उसी को स्पष्ट करते हैं-देवदत्त ने किया, करता है अथवा करेगा, इस प्रकार से प्रतीति के बल से सिद्ध है अथवा उस प्रकार एक में षट्कारक को घटित करने के समान काल आदि को भी घटित करना चाहिए।
कैसे ? कथंचित् अर्थ के भेद से कालादि की कल्पना करना चाहिए क्योंकि सर्वथा अभिन्न में संपूर्ण काल, कारक आदि भेद नहीं हो सकते हैं इसलिए स्याद्वाद में ही श्रुतज्ञान के विकल्प से वे सब घटित होते हैं। सभी नैगमादि सुनय हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष और अनुमान से अविरोधी हैं, अन्यत्र वे दुर्नय हैं क्योंकि प्रत्यक्षादि से विरोधी हैं। इस प्रकार भी भट्टाकलंक देव ने ‘‘भेदाभेदात्मके ज्ञेये१......’’ आदि रूप बहुत ही ठीक कहा है।
प्रश्न-नैगमादि सिद्धांत में नय कहे गये हैं यहाँ तो संग्रह आदि कहे गये हैं पुन: आपका कथन सिद्धांत से विरुद्ध क्यों नहीं होगा ?
उत्तर-ऐसी बात नहीं है, अभिप्राय का भेद है। सबसे कम विषय वाला इत्थंभूतनय है वह क्रिया के भेद से ही अर्थ में भेद करता है। उससे अधिक विषय वाला समभिरूढ़नय है क्योंकि वह पर्यायवाची शब्दों के भेद से अर्थ में भेद करता है। उससे अधिकतर विषय वाला शब्दनय है क्योंकि वह काल आदि के भेद से भेद करता है। उससे पुन: ऋजुसूत्रनय अधिकतम विषय वाला है क्योंकि वह शब्द के गोचर-अगोचर विवक्षित पर्याय को विषय करता है। उससे भी अधिक विषय वाला व्यवहारनय है क्योंकि वह पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को ग्रहण करता है। उससे प्रचुर विषय वाला संग्रहनय है क्योंकि वह सकलद्रव्य और पर्याय में व्यापी है, सभी को ग्रहण करता है। पुन: उससे भी अधिक विषय वाला नैगमनय है क्योंकि वह सत्त्व और असत्त्व को गौण तथा मुख्यरूप से ग्रहण करता है इसलिए विषय की अपेक्षा से नैगम आदि नयों का पूर्व निपात सिद्धांत ग्रंथों में युक्त है किन्तु यहाँ पुन: न्यायशास्त्र में समस्त नास्तिकजनों के विसंवाद को दूर करने के लिए सकल पदार्थों के अस्तित्व को सूचित करने वाले संग्रहनय को पूर्व में रखने में विरोध का अभाव है।
विशेषार्थ-यहाँ पर आचार्य ने कारण सामग्री के मिलने से एक में ही षट्कारक व्यवस्था घटाई है। जैसे ‘वीर भगवान२’ सभी सुर-असुरों से पूजित हैं, वीर का बुद्धिमान लोग आश्रय लेते हैं, वीर ने अपने कर्मों के समूह को नष्ट कर दिया है,वीर के लिए भक्ति से मेरा नमस्कार होवे, वीर से यह धर्मतीर्थ प्रवृत्त हुआ है, वीर का तपश्चरण घोर-कठोर है, वीर में श्री, द्युति, कीर्ति, कांति और धृति रहती हैं, हे वीर! आपमें भद्र-कल्याण है। यहाँ पर संबोधन समेत आठ कारक हो गये हैं। षट्कारक में संबंध कारक और संशोधन कारक अपेक्षित नहीं रहते हैं।
यह षट्कारक व्यवस्था एक वस्तु में युगपत् भी घट जाती है और काल, देश, आकार आदि के क्रम से भी घटित होती है।
पुन: आचार्य ने कहा है कि नैगम आदि नय स्याद्वाद में, सुनय में और एकांत पक्ष में दुर्नय हैं। आगे प्रश्न यह हुआ है कि सिद्धांत ग्रंथों में इन नयों में नैगमनय सबसे प्रथम है। यहाँ आपने संग्रह को सबसे प्रथम लिया है इसलिए आपका कथन सिद्धांत से विरोधी है, इस पर आचार्यश्री ने उत्तर देते हुए कहा है कि नैगमनय का विषय सबसे अधिक है, उससे कुछ कम विषय संग्रहनय का है। आगे-आगे ये नय अल्प-अल्प विषय वाले होते हैं, इस अपेक्षा से सिद्धांत ग्रंथ में इनका क्रम नैगम से है किन्तु यहाँ न्यायशास्त्र में अन्य एकांतवादी जनों को समझाने की प्रधानता से कथन होता है। यहाँ पर नास्तिकवादी जनों की मान्यता का खंडन करने के लिए संपूर्ण अस्तित्व का ग्राहक संग्रहनय पहले कहा गया है इसलिए कोई दोष नहीं आता है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं-सिद्धांत ग्रंथ में मति, श्रुत दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है और न्याय में मतिज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। सिद्धांत में दर्शन२ को स्वरूप को ग्रहण करने वाला माना है और न्याय में उसे सत्तामात्र को अवलोकन करने वाला माना है। सिद्धांत में इंद्रियों का क्रम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र रूप से कहा है और मूलाचार में चक्षु, श्रोत, घ्राण आदि के अक्रम से कहा है। सिद्धांत में जीव, अजीव, आदााव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तत्त्वों का क्रम है किन्तु समयसार में जीव, अजीव, आदााव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ऐसा क्रम कर दिया है।
कहने का मतलब यह है कि सिद्धांत ग्रंथों का कथन हीरे के कांटे के समान है और अन्य ग्रंथों का कथन अपेक्षाकृत अक्रम से भी हो जाता है किन्तु इस बात से पूर्वापर विरोध दोष नहीं समझना चाहिए।
🏠
व्याप्तिं साध्येन हेतो: स्फुटयति न विना चिंतयैकत्रदृष्टि:।
साकल्येनैष तर्कोऽनधिगतविषयस्तत्कृतार्थैकदेशे॥
प्रामाण्ये चानुमाया: स्मरणमधिगतार्थादि1संवादि सर्वं।
संज्ञानं च प्रमाणं समधिगतिरत: सप्तधाख्यैर्नयौघै:॥19॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[दृष्टि:] प्रत्यक्षज्ञान [एकत्र] एक जगह [चिंतया बिना] तर्क के बिना [साध्येन हेतो:व्याप्तिं] साध्य के साथ हेतु की व्याप्ति को [न स्फुटयति] स्फुट नहीं कर सकता है, [एष: तर्को] यह तर्क [साकल्येन] सकलरूप से [अनधिगत विषय:] नहीं जाने हुए को विषय करने वाला है। [तत्कृतार्थैकदेशे] उसके द्वारा निश्चित विषय के एकदेश में [अनुमाया: च प्रामाण्येन] अनुमान की प्रमाणता होने पर [स्मरणमधिगतार्था दिसंवादि] स्मृति भी अधिगत अर्थादि के विषय में संवादी हैं [सर्वं संज्ञानं च प्रमाणं] और सभी प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हैं [अत: सप्तधाख्यै तथौघै:] इसलिए सात प्रकार के नय समूहों से [समाधिगति:] सम्यक् प्रकार से ज्ञान होता है॥१९॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-एकत्र-एक महानस-रसोई आदि स्थान में दृष्टि-साध्य और साधन का जो दर्शन-प्रत्यक्ष है, वह साध्य-अग्नि आदि के साथ साधन-धूमादि हेतु की व्याप्ति को प्रकाशित नहीं करता है। किस रूप से प्रकाशित नहीं करता है ? साकल्य से अर्थात् सकल-देश, काल से अंतरित साध्य और साधन के विशेषों का भाव साकल्य कहलाता है। चिंता-तर्क प्रमाण के बिना वह प्रत्यक्ष संपूर्ण रूप से साध्य-साधन के अविनाभाव को नहीं बता सकता है।
साध्य और साधन के संबंध का दर्शन-प्रत्यक्ष दृष्टांत धर्मी में सकलरूप से व्याप्ति को जानने में समर्थ नहीं है अन्यथा अनुमान व्यर्थ हो जावेगा और उस देखने वाले अभिज्ञत्व की आपत्ति आ जावेगी।
प्रश्न-तब कौन सा प्रमाण उस व्याप्ति को स्पष्ट करता है ?
उत्तर-यह तर्क प्रमाण है जो कि ज्ञान सकलरूप से साध्य-साधन की व्याप्ति को स्फुट करता है और वही ज्ञान सकल अनुमानिक जनों में प्रसिद्ध ‘तर्क’ इस नाम से कहा जाता है।
प्रश्न-यह तर्क तो गृहीत को ग्रहण करने वाला होने से अप्रमाण है ?
उत्तर-नहीं, यह नहीं जानते हुए को विषय करने वाला है। अनधिगत अर्थात् प्रमाणांतर से अनिश्चित जो अविनाभाव है वह इसका विषय है।
प्रश्न-कैसा संज्ञान-सम्यग्ज्ञान अर्थ के विषय प्रमाण होता है ?
उत्तर-स्मृति ज्ञान प्रमाण होता है क्योंकि वह अधिगत अर्थ के विषय में अविसंवादी है अर्थात् अधिगत-प्रत्यक्ष से अनुभूत जो अर्थ-विषय है उसमें यह विसंवादरहित है और यह अनुमान की प्रमाणता होने पर सम्यग्ज्ञान है। कहाँ पर है ? तत्कृत अर्थ के एकदेश में है अर्थात् तत्-उस तर्क से कृत-निश्चित जो अर्थ-अविनाभाव है उसका एकदेश-जो साध्य है उसमें वह अनुमान प्रमाण है क्योंकि वह स्मृति और तर्क प्रमाण के साथ अविनाभावी है, यह अर्थ हुआ।
अथवा संज्ञान-प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण है क्योंकि वह भी अविसंवादी है। केवल ये परोक्ष ही विकल्पात्मक हैं ऐसी बात नहीं है किन्तु सभी प्रत्यक्ष भी विकल्पात्मक प्रमाण हैं क्योंकि वे ही व्यवहार में उपयोगी होते हैं। निर्विकल्पक दर्शन तो किसी विषय में भी उपयोगी नहीं है। इस कारण से तर्क आदि के समान विकल्पात्मक ही नय समुदायों से जीवादि तत्त्वों का सम्यक् प्रकार से निर्णय होता है। वे नय कितने हैं ? नैगम आदि से सात प्रकार के हैं क्योंकि ‘प्रमाणनयैरधिगम:१’ ऐसा सूत्रकार का वचन है अर्थात् प्रमाण और नयों से तत्त्वों का ज्ञान होता है ऐसा कहा है।
प्रश्न-प्रमाण के द्वारा परिगृहीत अर्थ को विषय करने वाले होने से ये भी नय निर्विषय वाले हैं ?
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि द्रव्य पर्यात्मक वस्तु प्रमाण के द्वारा परिगृहीत है-जानी जाती है और नय उसके एक देशरूप द्रव्य अथवा प्रतिपक्ष की अविनाभावी पर्याय में प्रवृत्त होते हैं। ‘सकलादेश प्रमाणाधीन है और विकलादेश नयाधीन है’ ऐसा प्रवचन-आगम में कहा हुआ है।
🏠
सर्वज्ञाय निरस्तबाधकधिये स्याद्वादिने ते नम-।
स्तात्प्रत्यक्षमलक्षयन् स्वमतमभ्यस्याप्यनेकांतभाक्॥
तत्त्वं शक्यपरीक्षणं सकलविन्नैकांतवादी तत:।
प्रेक्षावानकलंक याति शरणं त्वामेव वीरं जिनम्॥20॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[स्याद्वादिने] स्याद्वादी [निरस्तबाधक धिये] ज्ञानावरणादि बाधक कारणों से रहित ऐसे ज्ञान वाले [ते सर्वज्ञाय नमस्तात्] आप सर्वज्ञ को नमस्कार होवे। [एकांतवादी] एकांतवादी बुद्ध आदि [स्वमतं अभ्यस्त अपि] अपने मत का अभ्यास करके भी [शक्य परीक्षणं] जिसका परीक्षण करना शक्य है ऐसे [अनेकांतभाव] अनेकांतात्मक [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्षरूप [तत्त्वं] तत्त्व को [अलक्षयन्] नहीं जानते हुए [सकलवित् न] सर्वज्ञ नहीं हैं। [तत:] इसलिए [अकलंक] हे कर्मकलंकरहित अकलंक देव! [प्रेक्षावान्] बुद्धिमानजन [त्वां जिनं वीरं एवं] आप जिनेन्द्र भगवान वीरप्रभु की ही [शरणं याति] शरण में आते हैं॥२०॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-एकांतवादी अर्थात् एकांतरूप केवल द्रव्य ही तत्त्व है अथवा पर्याय ही तत्व है, ऐसा कहने का जिन का स्वभाव है वे एकांतवादी बुद्ध, कपिल आदि जन त्रिकालगोचर अशेष द्रव्य पर्यायों को जानने वाले सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे अनेकांत स्वरूप को आत्मसात् करने वाले ऐसे जीवादि पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानते हैं। उन जीवादि पदार्थों के स्वरूप का परीक्षण करना संशय आदि का व्यवच्छेद करके उनका विवेचन करना यद्यपि शक्य है, लौकिकजनों के गोचर है, प्रत्यक्ष-स्पष्ट है फिर भी वे लोग नहीं जानते हैं। निरन्वय विनाश आदि भावना से सहित चित्र वाले वे लोग सर्वथैकांतरूप अपने मत का अभ्यास करके अनेकांत तत्त्व को जानने में समर्थ नहीं होते हैं पुन: उनको सर्वज्ञता कैसे हो सकती है ?
इस कारण से ज्ञानावरण आदि कलंक से रहित भो अकलंकदेव! आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे अकलंक भगवान् ? सर्वज्ञ हैं-लोग-अलोक के सभी वस्तु समुदाय को जानने वाले हैं ‘सर्वं जानातीति सर्वज्ञ:’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब कुछ जानने वाले हैं। पुन: वे कैसे हैं ?
बाधकरूप जो दोष और आवरण हैं, उनको अनेकांत तत्त्व की भावना के बल से नष्ट कर देने से बाधा रहित ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं। पुन: कैसे हैं ? स्यात्-कथंचित् सत्-असत् आदि अनेकांतात्मक तत्त्व को कहने वाले स्याद्वादी हैं। ऐसे आपको मेरा नमस्कार होवे।
केवल मैं ही आपको नमस्कार नहीं करता हूँ किन्तु सभी प्रेक्षावान्-परीक्षकजन आपकी शरण में आते हैं। नित्य प्रवृत्त होने वाले वर्तमान की अपेक्षा से इस प्रकार का वचन है।
क्या नाम वाले भगवान् की शरण में परीक्षक लोग आते हैं ? जिनका ‘वीर’ नाम है ऐसे जो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान हैं पुन: वे कैसे हैं ? जिन हैं-नानाविध विषम भव वन में भ्रमण के कारणभूत दुष्कृत को जो जीतते हैं, वे जिन कहलाते हैं। सभी लोग उनकी शरण को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे तीर्थंकर शास्त्रकारों का उपकार करने वाले हैं।
विशेषार्थ-यहाँ पर श्री भट्टाकलंक देव ने तीन विशेषणों से विशिष्ट देव को नमस्कार किया है। सर्वज्ञ, निरस्तबाधक धी और स्याद्वादी। ये तीनों विशेषण भगवान उमास्वामी के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र महाशास्त्र की आदि में किये गये मंगलाचरण के समान ही हैं। स्याद्वादी विशेषण मोक्षमार्ग के नेतृत्व को सूचित करता है, निरस्तबाधक धी विशेषण कर्म पर्वत के नेतृत्व को स्पष्ट कर रहा है और सर्वज्ञ विशेषण तत्त्वों के ज्ञातृत्व को बतला रहा है। ऐसे ही श्री समंतभद्रस्वामी ने आप्त के सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी ये तीन विशेष गुण बतलाये हैं सो यहाँ भी सर्वज्ञ से सर्वज्ञ, निरस्त बाधक बुद्धि से वीतरागता और स्याद्वादी से हितोपदेशिता सिद्ध हो जाता है। ऐसे तीन विशेषणों से विशिष्ट को नमस्कार करके श्री अकलंक देव ने अपने नाम को धारण करने वाले ऐसे कर्म कलंक रहित अकलंक भगवान को संबोधन करके कहा है कि हे अकलंक भगवन्! आप जिन वीर की शरण में सभी परीक्षक लोग आ जाते हैं।
(अब वृत्तिकार श्री अभयचंद्रसूरि श्री भट्टाकलंक देव और प्रभाचंद्राचार्य का स्मरण करते हुए इस परिच्छेद को पूर्ण करते हुए श्लोक कहते हैं)-
श्लोकार्थ-श्रीमान् भट्टाकलंकरूप चंद्रमा की प्रभा-किरणों से यह नय और दुर्नय के निरूपण रूप धान्य समूह पुष्टि को प्राप्त हुआ है। उसमें नय से निष्ठुर-कुशल यह श्री अभयचंद्रसूरि के द्वारा रचित तात्पर्यवृत्ति अखिल जनों के हित के लिए अर्थ के पाक की पटुता को प्राप्त होती है।।१।।
भावार्थ-धान्य आदि के खेत चंद्रमा की किरणों से पुष्टि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं, पुन: पक जाते हैं तब लोगों को फल देने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वृत्तिकार ने कहा है कि सुनय और दुर्नय का निरूपण करने वाला जो यह प्रकरण है वह धान्य का खेत है उसे श्री अकलंकदेव रूपी चंद्रमा के द्वारा प्रगट हुई किरणों ने अथवा प्रभाचंद्र सूरि की वाणी ने पुष्ट किया है, बढ़ाया है, पुन: मैंने जो तात्पर्यवृत्ति टीका की है उसने इस धान्य को पकाकर फल देने वाली कर दिया है अर्थात् सभी भव्य जीव इस टीका के आधार से सुनय-दुर्नय के मर्म को समझकर उसके फलस्वरूप सम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे।
इस प्रकार श्री अभयचंद्रसूरि कृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण संज्ञक तात्पर्यवृत्ति टीका में पाँचवां परिच्छेद पूर्ण हुआ।
नय प्रवेश नाम से द्वितीय प्रकरण वाला द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ।
🏠
प्रणिपत्य महावीरं स्याद्वादेक्षणसप्तकं।
प्रमाणनयनिक्षेपानभिधास्ये यथागमं॥1॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ स्याद्वादेक्षणसप्तकं] स्यात् अस्ति आदि सप्तभंग रूप स्याद्वाद के अवलोकन करने वाले [महावीरं] अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को [प्रणिपत्य] नमस्कार करके [प्रमाण नयनिक्षेपात्] मैं प्रमाण नय और निक्षेपों को [यथागमं] आगम के अनुसार [अभिधास्ये] कहूँगा॥१॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-आगम में अर्थात् प्रवचन का उल्लंघन न करके अनादि परम्परा से प्रसिद्ध आर्ष- ऋषि प्रणीत ग्रंथों में जिस प्रकार से उन प्रमाण आदि का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार से उस आगम के अनुसार ही मैं प्रमाण, नय और निक्षेपों को प्रतिपादन करूँगा किन्तु स्वरुचि से रचित को नहीं कहूँगा, यह अर्थ हुआ। क्या करके कहूँगा ? अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को प्रणाम करके कहूँगा। कैसे हैं वे भगवान्? स्याद्वाद-‘स्यात् अस्ति’ इत्यादि सप्तभंगमय वाद-कथन स्याद्वाद कहलाता है, ईक्षण के- अवलोकन के सात प्रकार ‘ईक्षण सप्तक’ कहलाते हैं, इन स्याद्वादरूपी सप्त भंगों का ईक्षण-अवलोकन जिनसे शिष्यों को इन स्याद्वादरूप सप्त भंगों का अवलोकन होता है वे महावीर भगवान ऐसे हैं अर्थात् शिष्यों को स्याद्वादरूप सप्तभंग का ज्ञान कराने वाले हैं क्योंकि निश्चितरूप से जो निरुपकार-उपकाररहित हैं वे प्रेक्षावान्-बुद्धिमानों को प्रमाण के योग्य नहीं हैं, अन्यथा अतिप्रसंग हो जावेगा।
भावार्थ-यहाँ पर स्याद्वाद के नायक श्री भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके आचार्यश्री ने आगम के अनुसार प्रमाण, नय और निक्षेपों को कहने की प्रतिज्ञा की है क्योंकि इन प्रमाणादि के बिना वस्तु तत्त्व का यथार्थ निर्णय नहीं होता है।
🏠
ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते॥
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रह:॥2॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[आत्मादे: ज्ञानं प्रमाणं] आत्मा आदि का ज्ञान प्रमाण है [उपाय: न्यास: इष्यते] उनके जानने का उपाय न्यास-निक्षेप माना जाता है और [ज्ञातु: अभिप्राय: नय:] ज्ञाता का अभिप्राय नय है [युक्तित: अर्थपरिग्रह:] इस प्रकार युक्ति से अर्थ का ज्ञान होता है॥२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-‘जानाति ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञप्तिमात्रं वा ज्ञानं’ जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जानना मात्र ही ‘ज्ञान’ कहलाता है। यहाँ द्रव्य और पर्याय में भेद-अभेद की विवक्षा के होने पर कर्ता आदि होते हैं अर्थात् द्रव्य और पर्याय में अभेद विवक्षा होने से ‘जो जानता है, वह ज्ञान है’ यह कर्तृत्व साधन होता है। द्रव्य पर्याय में भेद विवक्षा होने पर ‘जिसके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान है’ ऐसा करण साधन होता है तथा भाव साधन में जानना मात्र ही ज्ञान है ऐसा कहा जाता है।
आत्मादि अर्थात् आत्मा-स्वरूप है आदि में जिसके ऐसे बाह्य पदार्थ आत्मादि हैं इस कथन से स्व और अर्थ को ग्रहण किया है अर्थात् उपर्युक्त निरुक्ति से सिद्ध स्व और पर को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है। अथवा आत्मा-चैतन्य द्रव्य है, आदि शब्द से आवरणों का क्षयोपशम या क्षय अंतरंग है पुन: इंद्रियां और मन बहिरंग कहलाते हैं इन अंतरंग और बहिरंग हेतुओं से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रमाण माना गया है क्योंकि सकल विसंवादों का पहले ही निराकरण कर दिया है।
उसी प्रकार से ज्ञाता-श्रुतज्ञानी के अभिप्राय को-विवक्षा को नय कहते हैं और उपाय- अधिगम-ज्ञान के हेतुभूत, नाम आदि रूप न्यास-निक्षेप कहलाता है।
शंका-अर्थ स्वत: सिद्ध है पुन: इन प्रमाण आदिकों से क्या प्रयोजन है ?
समाधान-नहीं! युक्ति से-प्रमाण, नय और निक्षेपों से ही जीवादि पदार्थों का परिग्रह-जानना होता है, स्वत: नहीं होता है।
विशेषार्थ-यहाँ आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि प्रमाण, नय और निक्षेप के बिना जीवादि पदार्थों का समीचीन ज्ञान नहीं हो सकता है अत: पहले इन प्रमाण, नय, निक्षेपों के लक्षण को समझ लेना चाहिए, अनंतर इनके द्वारा जीवादि पदार्थों का निर्णय करना चाहिए।
🏠
अयमर्थ इति ज्ञानं विद्यान्नोत्पत्तिमर्थत:।
अन्यथा न विवाद: स्यात्कुलालादिघटादिवत्॥3॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ अयं अर्थ: इति ज्ञानं] यह अर्थ है इस प्रकार का ज्ञान [अर्थत: उत्पत्तिं] अर्थ से अपनी उत्पत्ति को [न विद्यात्] नहीं जानता है [अन्यथा] अन्यथा [कुलालादिघटादिवत्] कुंभकार आदि से घटादि उत्पत्ति के ज्ञान के समान [विवाद: न स्यात्] विवाद नहीं होना चाहिए॥३॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-‘यह अर्थ है’ इस प्रकार ज्ञान नहीं जानता है अर्थात् मैं इस घटादि अर्थ से उत्पन्न हुआ हूँ इस प्रकार ज्ञान अपने जन्म को नहीं जानता है। ये घटादि पदार्थ प्रमेय हैं यह बात प्रतीति सिद्ध ही है अन्यथा यदि ज्ञान अर्थ से अपनी उत्पत्ति को जानता है तब वादी और प्रतिवादी को विवाद नहीं होना चाहिए अर्थात् ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा विसंवाद नहीं होना चाहिए। जैसे-वुंâभकार आदि से घट आदि की उत्पत्ति होना प्रतीति से सिद्ध है तो उसमें किसी को विवाद नहीं है, उसी प्रकार से अर्थ से ज्ञान के उत्पन्न होने में विवाद नहीं होना चाहिए किन्तु विवाद देखा जाता है। स्याद्वादी लोग अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानते हैं।
विशेषार्थ-अर्थ१ और आलोक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं हैं वे तो ज्ञान के विषय हैं अंधकार के समान। ज्ञान की उत्पत्ति तो आत्मा के ज्ञानावरण आदि के क्षयोपशम या क्षय से ही होती है, ऐसा समझना।
🏠
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थश्चेत्कारणं विद:।
संशयादिविदुत्पाद: कौतस्कुत इतीक्ष्यतां॥4॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[चेत्] यदि [अन्वयव्यतिरेकाभ्यां] अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा [अर्थ: विद: कारणं] अर्थ ज्ञान का कारण है, तब तो [संशयादिवित् उत्पाद:] संशय आदि ज्ञान का उत्पाद [कौतुस्कुत:] किससे होगा ? [इति ईश्यतां] इस पर विचार कीजिए॥४॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-यदि अन्वय और व्यतिरेक से अर्थ-विषयभूत पदार्थ ज्ञान के कारण हैं। कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय है और नहीं होने पर नहीं होना व्यतिरेक है। उसी को स्पष्ट करते हैं-ज्ञान अर्थनिमित्तक है क्योंकि अर्थ का ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है। यदि ऐसी बात है तो संशय और विपर्यय ज्ञानों की उत्पत्ति कहाँ से हो गई है। इस पर आपको अपने मन में विचार करना चाहिए क्योंकि अर्थ के अभाव में भी संशय आदि ज्ञान उत्पन्न होते हैं। स्थाणु पुरुष रूप अथवा केश मच्छर स्वभाव वाले कोई भी पदार्थ नहीं हैं, जो कि उस संशय आदि के ज्ञान में व्यापार करते हों इसलिए यह ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक के अनुसरण रूप हेतु भागासिद्ध है, ऐसा समझना।
विशेषार्थ-जहाँ-जहाँ पदार्थ हों, वहीं-वहीं ज्ञान उत्पन्न होवे और जहाँ-जहाँ पदार्थ न हों वहाँ-वहाँ ज्ञान उत्पन्न न होवे। यह हुआ अर्थ के साथ ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक और यदि ऐसा अन्वय व्यतिरेक है तब स्थाणु में दूर से देखने पर यह पुरुष है या स्थाणु ? ऐसा संशय ज्ञान कैसे होगा ? क्योंकि वहाँ स्थाणु में स्थाणु और पुरुषरूप उभयात्मक वस्तु तो हैं नहीं। ऐसे ही केशों में अकस्मात् दूर से मच्छर का ज्ञान हो गया, यह विपरीत ज्ञान भी यदि केश मच्छर रूप नहीं है तो कैसे हुआ ?
जो आप बौद्धों ने कहा था कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है इस बात को अनुमान प्रमाण बताता है। उस अनुमान में आपका हेतु एकदेश असिद्ध होने से असिद्ध हेत्वाभास हो गया है इसलिए ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न होना मानना नितांत गलत है, बिना पदार्थ के भी ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता रहता है चूँकि वह आत्मा का स्वभाव है।
🏠
सन्निधेरिंद्रियार्थानामन्वयव्यतिरेकयो:॥
कार्यकारणयोश्चापि बुद्धिरध्यवसायिनी॥5॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[इंद्रियार्थानां] इंद्रिय और पदार्थों के [सन्निधे:] सन्निकर्ष का [अन्वय व्यतिरेकयो:] अन्वय-व्यतिरेक का [च] और [कार्यकारणयो: अपि] कार्य कारण का भी [अध्यवसायिनी] निश्चय कराने वाला [बुद्धि:] ज्ञान है॥५॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-ज्ञान ही केवल अर्थ का ही नहीं, सन्निकर्ष का भी निश्चय कराने वाला है। चक्षु आदि इंद्रियाँ हैं और रूपादि अर्थ हैं इनका सन्निधि-सन्निकर्ष और अन्वय-व्यतिरेक अर्थात् भाव और अभाव का सन्निकर्ष तथा कारण कार्य का भी सन्निकर्ष होता है। कार्य - सन्निकर्ष कारण-इन्द्रिय आदि हैं । इनका भी ज्ञान ही निश्चय कराने वाला है इसलिए वह ज्ञान ही प्रमाण है सन्निकर्षादि प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वे प्रमेयरूप हैं।
🏠
तमो निरोधि वीक्षंते तमसा नावृतं परं॥
कुड्यादिकं न कुड्यादितिरोहितमिवेक्षका:॥6॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ईक्षका:] देखने वाले [निरोधि तम:] घटादि के निरोधक ऐसे अंधकार को [वीक्षंते] देखते हैं किन्तु [तमसा आवृतं परं न] अंधकार से आच्छादित पर घटादि को नहीं [इव] जैसे [कुड्यादिकं] दीवाल आदि को देखते हैं, वैसे [कुड्यादितिरोहितं न] दीवाल आदि से तिरोहित को नहीं देखते हैं॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-ईक्षक-चक्षुष्मानजन, निरोधि-प्रमेयांतर को ढकने वाले तम-अंधकाररूप पुद्गलपर्याय को विशेष-नीलादिरूप से देखते हैं किन्तु वृत्त-आच्छादित हुए पर घटादिक तमसा- अंधकार से नहीं देखते हैं। तब आलोक ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है क्योंकि प्रकाश के अभाव में भी ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देते हैं-जैसे दर्शक लोग दीवाल आदि को देखते हैं किन्तु दीवाल आदि से तिरोहित घटादिकों को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से अंधकार को तो देख लेते हैं किन्तु उनसे ढके हुए घटादि वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं।
शंका-अंधकार के समान प्रकाश से ढके हुए भी घटादि को नहीं देख सकते हैं ?
समाधान-यदि ऐसी बात है तो होवे, यदि प्रकाश को अविशदपना है। जिस द्रव्य में विशदता है अर्थात् जो द्रव्य स्पष्ट है वह ढका हुआ भी नहीं ढके हुए के समान ही है, स्फटिक और अभ्रक आदि से ढके हुए के समान इसलिए आलोक के समान उससे ढके हुए को भी देख लेते हैं क्योंकि वह वैशद्य है-स्पष्ट है। पुन: अंधकार को तो देख लेते हैं किन्तु उससे ढके हुए को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वह अस्पष्ट रूप है। इसलिए आलोक ज्ञान का कारण नहीं है क्योंकि वह प्रमेयरूप है, पदार्थों के समान।
इस प्रकार से ज्ञान का अंतरंग कारण ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मों का क्षयोपशम है पुन: बहिरंग कारण इंद्रियां और मनरूप हैं यह बात सिद्ध हो गई है।
विशेषार्थ-बौद्ध अर्थ के समान प्रकाश को भी ज्ञान का कारण मानते हैं किन्तु जैनाचार्य कहते हैं कि प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है वह भी ज्ञान का विषय है। जैसे कि अंधकार ज्ञान का कारण नहीं है बल्कि ज्ञान का विषय अवश्य है, प्रत्येक प्राणी अंधकार को काले-काले रूप में देख रहा है किन्तु उससे ढके हुए पदार्थों को तो नहीं देख पाता है उसी प्रकार प्रकाश भी ज्ञान का विषय ही है। ज्ञान का कारण नहीं हो सकता है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है जो कि संसार अवस्था में कर्मों से ढका हुआ है इसलिए ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपशमरूप अंतरंग कारण से तथा इंद्रिय और मन के निमित्तरूप बहिरंग कारण से उत्पन्न होता है।
🏠
मलविद्धमणिव्यक्तिर्यथाऽनेकप्रकारत:॥
कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारत:॥7॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[यथा] जैसे [मलविद्धमणिव्यक्ति:] मल से आच्छादित मणि की व्यक्ति [अनेकप्रकारत:] अनेक प्रकार से होती है [तथा] वैसे ही [कर्मविद्धात्मविज्ञप्ति:] कर्म से आच्छादित आत्मा का ज्ञान भी [अनेकप्रकारत:] अनेक प्रकार से होता है॥७॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जिस प्रकार से कालिमा रेखा आदि से विद्ध हुए ऐसे जो पद्मराग आदि मणि विशेष हैं उनके तेज का प्रादुर्भाव अनेक प्रकार से होता है अर्थात् विशद्-अविशद्, दूर-निकट, प्रकाश्य-प्रकाशन आदि विशेष भेदों के आश्रित होता है उसी प्रकार से ज्ञानावरण आदि कर्मों से विद्ध-संबद्ध-संयुक्त जो आत्मा है उसकी विज्ञप्ति-आत्म पदार्थ की उपलब्धि अनेक प्रकार से होती है अर्थात् जो नाना रूप प्रत्यक्ष-परोक्ष, दूर-आसन्न पदार्थों के प्रतिभासन विशेष हैं, इंद्रिय, अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय शक्ति विशेष रूप क्षयोपशम विशेष हैं उनके आश्रय से जीवों का अनेक प्रकार से अनुभव आ रहा है और ज्ञानावरण कर्म के संपूर्ण तथा निरस्त हो जाने पर तो संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता ही है क्योंकि वह आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है।
भावार्थ-जैसे मल से आच्छादित मणि की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से देखी जाती है उसी प्रकार से कर्मों से आच्छादित आत्मा के ज्ञान का विकास भी हीनाधिकरूप से अनेक प्रकार का देखा जाता है।
🏠
न तज्जन्म न ताद्रूप्यं न तद्व्यवसिति: सह॥
प्रत्येकं वा भजंतीह प्रामाण्यं प्रति हेतुतां॥8॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[इह] ज्ञान में [प्रामाण्यं प्रति] प्रमाणता के प्रति [तज्जन्म] तदुत्पत्ति [हेतुतां न] हेतु नहीं है, [न ताद्रूप्यं] न तदाकारता है और [न तद् व्यवसिति:] न तद्ध्यवसाय ही है [सह प्रत्येकं वा भजंति] ये तीनों न मिलकर ही हेतु हैं न एक-एक ही हेतु होते हैं॥८॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-इस ज्ञान में प्रमाणता के प्रति निमित्त भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ? तज्जन्म-ज्ञान की उस अर्थ से उत्पत्ति होती है, इस मान्यता में उस ज्ञान में इंद्रियों से व्यभिचार आता है इसलिए पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त नहीं है, यह अर्थ हुआ है। ज्ञान में तद्रूपता भी नहीं है, उस अर्थ के समान रूप को-आकार को धारण करने वाला तद्रूप कहलाता है उसके भाव को ताद्रूप्य कहते हैं। उस तद्रूप का समानार्थ समनंतर ज्ञान के साथ व्यभिचार होता है और उसका व्यवसाय भी कारण नहीं है-उस अर्थ का निश्चय होना भी ज्ञान में कारण नहीं है क्योंकि द्विचंद्रादि के निश्चय के साथ व्यभिचार आता है। ये एक-एक या साथ में मिलकर प्रमाणता में हेतु नहीं होते हैं क्योंकि ये तीनों भी शुक्ल शंख में पीताकार ज्ञान के अनेक होने से समनंतर ज्ञान से व्यभिचारी होते हैं।
भावार्थ-बौद्धों ने तदुत्पत्ति, तद्रूपता और तदध्यवसाय को ज्ञान की प्रमाणता में कारण माना है किन्तु आचार्यदेव का कहना है कि न तो ये पृथक्-पृथक् ही ज्ञान की प्रमाणता में कारण हो सकते हैं और न तीनों मिलकर ही हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही व्यभिचरित हैं।
🏠
स्वहेतुजनितोऽप्यर्थ: परिच्छेद्य: स्वतो यथा॥
तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मकं स्वत:॥9॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[स्वहेतुजनित: अपि अर्थ:] अपने हेतु से उत्पन्न हुआ भी अर्थ [यथा स्वत:] जैसे स्वत: [परिछेद्य:] जानने योग्य है [तथा स्वहेतूत्थं ज्ञानं] वैसे ही अपने हेतु से उत्पन्न हुआ ज्ञान [स्वत:] स्वभाव से ही [परिच्छेदात्मकं] जानने रूप स्वभाव वाला है॥९॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जैसे घटादि पदार्थ स्वभाव से ही ज्ञेय हैं न कि ज्ञान से उत्पन्न होने आदि की अपेक्षा से और वे अपने हेतु से मिट्टी आदि सामग्री से उत्पन्न होते हैं-बनते हैं, ऐसे अपने कारणों से उत्पन्न होते हुए भी वे घटादि ज्ञान के विषय हैं, वैसे ही ज्ञान भी स्वभाव से ही पदार्थ को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है न कि अर्थ से उत्पन्न होने आदि की अपेक्षा से। वह ज्ञान कैसा है ? अपने हेतु से उत्पन्न होने वाला है, ज्ञान का अंतरंग हेतु आवरण के क्षयोपशमरूप है और बहिरंग हेतु इंद्रिय तथा मनरूप है, इन अंतरंग-बहिरंग हेतुओं से उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान स्वभाव से ही वस्तु को जानने का कार्य करता है। अर्थ को ग्रहण करने रूप स्वभाव वाला ज्ञान किसी के द्वारा शक्ति के आवृत्त होने पर कुछ-कुछ पदार्थों को ही जानता है और प्रतिबंधक आवरण कर्म क्षयोपशम या क्षय विशेष होने पर तो वही ज्ञान अपने विषय विशेष को जान लेता है।
🏠
व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतं॥
ग्रहणं निर्णयस्तेन मुख्यं प्रामाण्यमुश्नुते॥10॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[व्यवसायात्मकं ज्ञानं] निश्चयात्मक ज्ञान [आत्मार्थग्राहकं मतं] अपने को और अर्थ को ग्रहण करने वाला माना गया है [ग्रहणं] वह ज्ञान [निर्णय:] निर्णयरूप है [तेन] इसलिए वह [मुख्यं प्रामाण्यं] मुख्य प्रमाणता को [अश्नुते] प्राप्त होता है॥१०॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-विशेष-जाति आदि आकार का अवसाय-निश्चय व्यवसाय कहलाता है वह निश्चय ही आत्मा-स्वरूप जिसका है वह ज्ञान व्यवसायात्मक माना गया है। इस कथन से ‘प्रत्यक्ष ज्ञान कल्पना से रहित है’ ऐसी बौद्ध की मान्यता का खंडन हो जाता है पुन: वह ज्ञान आत्मा और अर्थ का ग्राहक है, आत्मा-स्वरूप और अर्थ-घटादि बाह्य पदार्थ इनको ग्रहण करने वाला है अर्थात् अपने स्वरूप और बाह्य पदार्थों का निर्णय कराने वाला है।
इस कथन से ज्ञान अर्थ का ही ग्राहक है स्वरूप का ग्राहक नहीं है अथवा ज्ञान अपने स्वरूप का ही ग्राहक है अर्थ का ग्राहक नहीं है, इन दोनोें ही एकांत मान्यताओं का निराकरण कर दिया गया है इसलिए यह ग्रहण-ज्ञान निर्णयरूप है अर्थात् स्वार्थ व्यवसायरूप है यह अर्थ हुआ, उसी हेतु से यह प्रमाणता को प्राप्त होता है और यह ज्ञान कैसा है ? मुख्य-अनुपचरित है क्योंकि ज्ञानरूप क्रिया के प्रति कारण है किन्तु इंद्रिय, लिंग आदि तो उपचार से ही प्रमाण होते हैं इसलिए यह बात ठीक ही कही है कि आत्मादि का ज्ञान प्रमाण है, ऐसा समझना।
🏠
तत्प्रत्यक्षं परोक्षं च द्विधैवात्रान्यसंविदां।
अंतर्भावान्न युज्यंते नियमा: परकल्पिता:॥11॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[तत् द्विधा] वह प्रमाण दो प्रकार का है [प्रत्यक्षं परोक्ष च] प्रत्यक्ष और परोक्ष। [अन्य संविद्यं] अन्य ज्ञानों का [अत्र] इसमें [एव] ही [अंतर्भावात्] अंतर्भाव हो जाने से [परिकल्पिता:] पर से परिकल्पित प्रमाणों का [नियमा:] नियम [न युज्यंते] युक्त नहीं है॥११॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जो सम्यग्ज्ञान स्वरूप प्रमाण है वह दो प्रकार का ही है-प्रत्यक्ष और परोक्ष।
प्रश्न-अनुमान आदि प्रमाण के भेदों की संख्या भी संभव है।
उत्तर-नहीं, जो आप बौद्धदि लोगों के द्वारा कल्पित दो, तीन, चार आदि संख्या का नियम है वह संभव नहीं है क्योंकि उन सभी अनुमान आदि ज्ञानों का इन्हीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप दो प्रमाणों में ही अंतर्भाव हो जाता है। उसमें से प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के भेद से तीन प्रकार का है।
स्पर्शन आदि इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष है। केवल मनोव्यापार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष है। ये दोनों ही सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं क्योंकि ये एकदेश विशदता को लिए हुए हैं।
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है। उसके अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद से तीन भेद हैं। उनमें से मूर्तिक द्रव्यों का अवलंबन लेने वाला अवधिज्ञान है, उसके भी देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से तीन भेद हैं। उन तीनों में से देव और नारकियों के देशावधि होती है और वह भवप्रत्यय ही होती है तथा तिर्यंच और मनुष्यों की अवधि गुणप्रत्यय कहलाती है। परमावधि-सर्वावधि ये दोनों अवधिज्ञान चरमशरीरी-उसी भव से मोक्ष जाने पर संयमी-मनुष्य के ही होते हैं और ये गुणप्रत्यय कहलाते हैं। ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मन:पर्ययज्ञान के दो भेद हैं। प्रगुण-सरणता से निर्वर्तित मन, वचन, कायगत सूक्ष्म द्रव्य का अवलंबन लेने वाला-जानने वाला ऋजुमति मन:पर्ययज्ञान है। सरल और कुटिलता से निर्वर्तित मन, वचन, कायगत सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ का अवलंबन लेने वाला विपुलमति मन:पर्यय ज्ञान है। त्रिकालगत अनंत पर्याय से परिणत जीव, अजीव द्रव्यों को युगपत् साक्षात् जानने वाला केवलज्ञान है, वह संपूर्ण आवरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के निरवशेष नष्ट हो जाने से होता है।
‘इस केवलज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई पुरुष विशेष है क्योंकि सुनिश्चितरूप से बाधक प्रमाण असंभव है, सुखादि के समान’ वास्तव में उस सर्वज्ञ को बाधित करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष उसमें प्रवृत्त ही नहीं हो सकता है।
प्रश्न-उससे निवर्तमान ही उसका बाधक है अर्थात् सर्वज्ञ प्रत्यक्ष का विषय नहीं है इसलिए तो वह नहीं है ?
उत्तर-यह कथन अयुक्त है, क्योंकि ऐसे तो दीवाल आदि के परभाग आदि का भी अभाव हो जावेगा। अनुमान भी सर्वज्ञ का बाधक नहीं है क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। साध्य-साधन के संबंध को ग्रहण करने पूर्वक ही अनुमान ज्ञान उत्पन्न होता है। वक्तृत्व आदि हेतु का सर्वज्ञत्व साध्य के साथ संबंध है इस बात को संपूर्ण रूप से जानना किसी को भी शक्य नहीं है, क्योंकि सभी लोग अल्पज्ञ हैं। आप कहें कि भिन्न अनुमान से उस साध्य-साधन के संबंध का ज्ञान हो जायेगा, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो अनवस्था आ जाती है इसलिए संदिग्धरूप से अनैकांतिक ऐसे वक्तृत्व आदि हेतु से सर्वज्ञ का निषेध सिद्ध नहीं हो सकता है।
आगम से भी ये सर्वज्ञ बाधित नहीं होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा मान्य इस आगम को अपौरुषेयपना सिद्ध नहीं है किन्तु उसको पौरुषेय ही सिद्ध किया है। इष्ट-प्रत्यक्ष और अदृष्ट-अनुमानादि से अविरुद्ध वचन ही आगम है, न कि सर्वज्ञ। और वह आगम सर्वज्ञदेव से प्रणीत ही हो सकता है न कि राग, द्वेष और मोह से व्याप्त पुरुषों से कथित वचनरूप, क्योंकि उनमें वैसे प्रत्यक्षादि से अविरुद्ध वचनों के प्रयोग का अभाव है, रथ्यापुरुष के समान-पागल पुरुष के समान।
प्रश्न-इस प्रकार का आगम तो सौगत आदि के यहाँ भी संभव है अत: अर्हंत ही उस आगम के प्रणेता संभव नहीं हैं ?
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वे सौगत आदि भी प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध वचन के बोलने वाले हैं। ‘अनेकांतस्वरूप वस्तु का प्रतिपादक प्रवचन प्रत्यक्ष और अनुमान से अविरोधी है क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसमें विसंवाद नहीं आता है।’ ऐसा समझना।
विशेषार्थ-यहाँ पर आचार्य ने प्रमाण के दो भेद बताये हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनमें से प्रत्यक्ष के भी सांव्यवहारिक और मुख्य ऐसे दो भेद किये हैं। सांव्यवहारिक में इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष ऐसे दो भेद होते हैं। अवधि में भी देशावधि, परमावधि और सर्वावधि से तीन भेद हो गये हैं। देशावधि के दो भेद हैं-भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय। देव, नारकियों के भवप्रत्यय देशावधि ही होती है तथा मनुष्य और तिर्यंचों के क्षयोपशम की मुख्यता से गुणप्रत्यय देशावधि ही होती है। परमावधि, सर्वावधि तद्भव मोक्षगामी परमसंयमी मुनियों के होती हैं। मन:पर्यय ज्ञान के भी ऋजुमती और विपुलमती दोनों भेद संयमी के ही होते हैं। ये दोनों ज्ञान देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं। केवलज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। यह जिनके होता है वे सर्वज्ञ कहलाते हैं।
कुछ लोग-मीमांसक आदि सर्वज्ञ का अस्तित्व नहीं मानते हैं। इस पर आचार्य ने कहा है कि ‘सर्वज्ञ नहीं है’ इस बात को जानने वाला इंद्रिय प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसका विषय सीमित है और वर्तमान का ही है, हाँ, यदि कोई अपने प्रत्यक्ष से तीनों लोकों और तीनों कालों को देखकर निर्णय दे दे कि कोई भी सर्वदर्शी नहीं है तो भाई! वह तो स्वयं ही सर्वदर्शी सर्वज्ञ बन गया है। वैसे ही अनुमान से भी ‘सर्वज्ञ नहीं है’ इस बात को सिद्ध करना कठिन है तथा आगम से निषेध करना चाहो सो भी ठीक नहीं है क्योंकि पहले आगम को प्रमाणीक सिद्ध करना चाहिए। आगम अपौरुषेय है अत: प्रमाणीक है इतना मात्र कहने से भी कुछ नही होगा क्योंकि अपौरुषेय आगम की सिद्धि नहीं है प्रत्युत् पुरुषकृत ही आगम सिद्ध हो रहे हैं। उनमें भी सर्वज्ञ प्रणीत आगम ही निर्दोष है, अल्पज्ञों के द्वारा प्रणीत नहीं है।
🏠
उपयोगौ श्रुतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ॥
स्याद्वाद: सकलादेशो नयो विकलसंकथा॥12॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[श्रुतस्य] श्रुतज्ञान के [स्याद्वादनयसंज्ञितौ] स्याद्वाद और नय इन नाम वाले [द्वौ उपयोगौ] दो व्यापार हैं। [सकलादेश:] संपूर्ण को कहने वाला [स्याद्वाद:] स्याद्वाद है और [विकलसंकथा] एक-एक अंश को सम्यक् प्रकार से कहने वाला [नय:] नय है॥१२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-श्रुत-आप्तवचनरूप आगम के दो उपयोग व्यापार हैं। वर्णपदवाक्यात्मक द्रव्यरूप का श्रवण करना श्रुत है अथवा भावश्रुत का श्रवण श्रुत है ऐसा श्रुत शब्द का निरुक्ति अर्थ है। श्रुत के दो व्यापार कौन से हैं ? स्याद्वाद और नय हैं।
(स्याद्वाद का व्यापार)
स्यात्-कथंचित् प्रतिपक्ष की अपेक्षा से जो कथन होता है वह २स्याद्वाद कहलाता है। नयनं-वस्तु के विवक्षित धर्म को प्राप्त कराने वाला नय३ है। अब इन दोनों के लक्षण को कहते हुए पहले स्याद्वाद को कहते हैं -
वह स्याद्वाद सकलादेशी है-सकल-अनेक धर्मात्मक वस्तु को आदेश कहना सकलादेश है। जैसे-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह अर्थ हैं। उनमें से ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन असाधारण धर्मों से, सर्वत्र प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, धर्मित्व, गुणित्व आदि साधारण धर्मों से तथा अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, असंख्यात प्रदेशत्व आदि साधारणासाधारण धर्मों से अनेकांतात्मक-अनेकों धर्म वाला जीव है। पुन: पुद्गल, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन असाधारण धर्मों से, सत्त्व आदि साधारण धर्मों से तथा अचेतनत्त्व, मूर्तत्त्व आदि साधारणासाधारण धर्मों से अनेकांतात्मक है। धर्मद्रव्य गतिहेतुरूप असाधारण धर्म से, सत्त्व आदि साधारण धर्मों से और अचेतनत्व आदि उभयरूप धर्मों से अनेकांतात्मक है। अधर्मद्रव्य स्थिति हेतुरूप असाधारण धर्म से, अस्तित्व आदि साधारण धर्मों से और अमूर्तत्व आदि साधारणासाधारण धर्मों से अनेकांतात्मक है। अवगाहनरूप असाधारण धर्म से, अस्तित्व आदि साधारण धर्मों से और अमूर्तत्वादि उभयरूप धर्मों से भी आकाश द्रव्य अनेकांतात्मक है। वर्तनालक्षण असाधारण धर्म से, अस्तित्व आदि साधारण धर्मों से और अमूर्तत्वादि साधारणासाधारण धर्मों से कालद्रव्य अनेकांतात्मक है अथवा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों से युक्त सत् होता है, स्याद्वाद ऐसा प्रतिपादन करता है।
(नय का व्यापार)
एक धर्म का सम्यक् कथन करना नय है। विकल-विवक्षित एक धर्म का सं-सम्यक् प्रकार से-प्रतिपक्ष की अपेक्षा से कथा-प्रतिपादन करना नय है, जैसे जीव ज्ञाता ही है, ऐसा देखना चाहिए इत्यादि।
प्रश्न-पहले आपने कहा है कि ज्ञाता का अभिप्राय नय है, पुन: इस समय ‘वचनात्मक नय हैं’ ऐसा आप कह रहे हैं, सो क्या बात है ?
उत्तर-उपचार से नय के हेतुभूत वचन को भी नयपना विरुद्ध नहीं है, जैसे कि श्रुतज्ञान के हेतुभूत वचन को श्रुत, ऐसा नाम कह देते हैं।
उसी का स्पष्टीकरण करते हैं -
कथंचित् जीव ही ज्ञानादि अनेक धर्मात्मक है, यह प्रमाणवाक्य है। कथंचित् अस्ति ही जीव है वह नय वाक्य है और यह सप्तभंगी से प्रतिष्ठित है।
स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् अस्ति रूप ही है। परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् अस्ति रूप ही है। स्वपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की क्रम से विवक्षा होने से कथंचित् जीव अस्तिनास्तिरूप ही है। युगपत् स्व और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् अवक्तव्य ही है। स्वद्रव्यादि चतुष्टय की विवक्षा के साथ युगपत् स्वपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् अस्तिअवक्तव्य ही है। परद्रव्यादि विवक्षा के साथ युगपत् स्वपर द्रव्य, क्षेत्र, काल,भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् नास्ति अवक्तव्य है। क्रम से स्वपर द्रव्यादि की विवक्षा के साथ युगपत् स्वपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विवक्षा से जीव कथंचित् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही है।
इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान के अविरोध रूप से विधि-प्रतिषेध के द्वारा सर्वत्र सप्तभंगी कल्पना संभव है। इसी प्रकार से एक-अनेक, नित्य-अनित्य और भेद-अभेद आदि में भी सप्तभंगी को लगा लेना चाहिए।
विशेषार्थ-यहाँ पर आगम के दो व्यापार बताये हैं-एक तो स्याद्वाद-प्रमाण, दूसरा नय। प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्मात्मक ग्रहण करने वाला स्याद्वाद नाम वाला प्रमाण वाक्य है और प्रत्येक वस्तु के विवक्षित किसी एक धर्म को उसके विरोधी धर्म की अपेक्षा के साथ ग्रहण करने वाला नय वाक्य है। जैसे जीव को अस्तित्व आदि साधारण धर्मों से, चेतनत्व आदि असाधारण धर्मों से और उभयात्मक धर्मों से सहित अनेक धर्म वाला कहना। यह प्रमाण वचन है। उसके अस्ति धर्म को स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से कहते हुए भी उसके प्रतिपक्षी नास्ति धर्म का निषेध नहीं करना किन्तु गौण करना यह सुनय का काम है। यदि नास्ति धर्म का निषेध करके यह दुराग्रह रूप एकांत से जीव को अस्तिरूप ही कहे तब यह दुर्नय हो जाता है। यह नयवाक्य सप्तभंगी से युक्त होता है। (ऐसा समझना)।
🏠
अप्रयुक्तेऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयते॥
विधौ निषेधेऽप्यन्यत्र कुशलश्चेत्प्रयोजक:॥13॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[चेत् प्रयोजक: कुशल:] यदि प्रयोगकर्ता कुशल है, तो [सर्वत्र] सभी जगह [विधौ निषेधे अपि] विधिवाक्य और निषेधवाक्य में भी [अन्यत्र] अन्य किसी में भी [अर्थात्] सामथ्र्य से [स्यात्कार:] स्यात्कार [अप्रयुक्ते अपि] बिना प्रयोग करने पर भी [प्रतीयते] प्रतीत हो जाता है॥१३॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-स्यात् यह पद अव्यय रूप है, ऐसा यह स्यात्कारपद सर्वत्र-शास्त्र में अथवा लोक में विधि को-अस्तित्व आदि को साध्य करने में प्रतीति में आता है-जाना जाता है। केवल विधि में ही नहीं किन्तु निषेध में भी-असत्त्व आदि को साध्य करने पर भी यह स्यात्कार प्रतीति में आता है। अन्यत्र भी-अन्य अनुवाद के अतिदेश आदि में भी यह प्रतीत होता है।
किस प्रकार का होता हुआ ? अप्रयुक्त भी ‘स्यात् अस्ति जीव:’ ऐसा कथन नहीं करने पर भी यह स्यात्कार अर्थ-सामथ्र्य से (अर्थापत्ति से) प्रतीत हो जाता है। उसी का स्पष्टीकरण -
मोक्ष्मार्ग को सम्यग्दर्शन आदि त्रयात्मक कहने पर उसमें एकत्व कैसे है ? अथवा एकत्व मानने पर तीनपना कैसे है ? इस प्रकार के विरोध में कथंचित् इस प्रकार से ही परिहार होता है किन्तु सर्वथा से नहीं। क्योंकि द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से मार्ग में एकत्व और अनेकत्व का विरोध नहीं है इसलिए ‘कथंचित्’ इस अर्थ की सामथ्र्य से उसका वाचक स्यात्कार प्रयुक्त न होते हुए भी प्रतीति में आता ही है। यदि प्रयोजक-प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कुशल है-व्यवहार में जानकार है, तो ऐसी बात है।
उसी प्रकार से एवकार भी प्रतीति में आता है। उसी हेतु से रत्नत्रय ही मोक्षमार्ग है, इस प्रकार के अवधारण के अभाव में सम्यग्दर्शन ही मार्ग हो जावेगा अथवा अन्य ही कोई अर्थात् ज्ञान ही या चारित्र ही मार्ग हो जावेगा, अथवा कोई भी दो ही मार्ग हो जावेंगे, इस प्रकार से अतिप्रसंग दोष दुर्निवार हो जावेगा अर्थात् एवकार का प्रयोग न होने पर भी सामथ्र्य से एवकार का अर्थ लेना चाहिए अन्यथा कुछ भी अर्थ हो जावेगा किन्तु ऐसी बात तो है नहीं क्योंकि असाधारण स्वरूप को ही लक्षण कहते हैं।
प्रश्न-इस प्रकार बिना प्रयुक्त भी यदि स्यात्कार और एवकार की सामथ्र्य से प्रतीति हो जाती है तब तो कोई भी कहीं पर इनको क्यों प्रयुक्त करते हैं ?
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि प्रतिपाद्य-शिष्य के अभिप्राय के निमित्त से उनका प्रयोग होता है।
भावार्थ-आचार्यों का यह स्पष्ट कहना है कि यद्यपि स्थल-स्थल पर वाक्य-वाक्य में स्यात्कार का प्रयोग नहीं होता है फिर अर्थापत्ति से लगा लेना चाहिए। जैसे किसी ने कहा जीव शुद्ध है तो समझ लेना चाहिए कि कथंचित् अशुद्ध भी है। ऐसे ही एवकार के विषय में भी प्रयुक्त न होने पर भी यथोचित् उसका भी अर्थ लेना चाहिए और जहाँ-जहाँ पर इनका स्पष्ट प्रयोग है वहाँ पर शिष्यों के अभिप्राय से आचार्यों ने प्रयोग कर दिया है।
🏠
वर्णा: पदानि वाक्यानि प्राहुरर्थानवांछितान्॥
वांछिताँश्च क्वचिन्नेत्ति प्रसिद्धिरियमीदृशी॥14॥
स्वेच्छया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते॥
वक्त्रभिप्रेतमात्रस्य सूचकं वचनं न्विति॥15॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[वर्णा: पदानि वाक्यानि] वर्ण, पद और वाक्य ये [अवांछितांन् वांछितान् च] अविवक्षित और विवक्षित [अर्थान् प्रादु:] अर्थों को कहते हैं और [क्वचित् ना इति] कहीं पर नहीं भी कहते हैं, [ईदृशी इयं प्रसिद्धि:] ऐसी यह प्रसिद्धि है [तो अतिक्रम्य एव] इस प्रसिद्धि को उल्लंघन करके ही [स्वेच्छया वदतां] स्वेच्छा से कहने वालों को [युज्यते] क्या यह युक्त है ? कि [वचनं] वचन [वक्त्रभिप्रेतमात्रस्य] वक्ता के अभिप्रायमात्र के [सूचकं] सूचक हैं [नु इति] अहो! इस प्रकार तो बड़ा आश्चर्य है॥१४-१५॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-गकार आदि अक्षर वर्ण हैं तथा गौ आदि शब्द पद कहलाते हैं और ‘गाय को लावो’ इत्यादि वाक्य संज्ञक हैं, ये अवांक्षित-अविवक्षित भूमि आदि को वांछित-विवक्षित सास्नादिमान् आदि अर्थ को-वाच्य को कहते हैं। किन्हीं मंदबुद्धि वाले शिष्यों में नहीं भी कहते हैं क्योंकि उनको इनसे अर्थ का बोध नहीं होता है, इस प्रकार से सर्वजन प्रतीति प्रसिद्ध है, ईदृशी-ऐसी विचित्र रूढ़ि को व्यवहारीजन स्वीकार करते हैं क्योंकि उसी प्रकार से ही अर्थक्रिया हो सकती है।
उनमें वर्ण, स्वर और व्यंजनरूप से चौंसठ हैं। परस्पर में सापेक्ष वर्गों का निरपेक्ष समुदाय पद कहलाता है, उसके अव्यय और अव्ययरहित की अपेक्षा से दो भेद हैं। उनमें भी अव्ययरहित के सुबंत और तिङंत की अपेक्षा से दो भेद हैं और तस्, आदि के भेद से अव्यय अनेक प्रकार का है। परस्पर सापेक्ष पदों का जो निरपेक्ष समुदाय है वह वाक्य है। उसके भी क्रिया प्रधान, कारक प्रधान और उभयात्मक ऐसे तीन भेद हैं।
इस प्रसिद्धि का अतिक्रमण करके ही-उल्लंघन करके ही स्वैर भाव से कहने वाले सौगतों को क्या यह कहना युक्त है कि शब्द वक्ता के अभिप्राय मात्र के सूचक हैं अर्थात् प्रयोजक की विवक्षा मात्र को ही कहने वाले हैं किन्तु बाह्य अर्थ को नहीं। नु-अहो! यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस कथन से यहाँ पर आक्षेप सूचित हो रहा है क्योंकि सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों की शब्द के प्रयोग से प्रतीति होती है, वे शब्द ही उस अर्थ को कहते हैं। उस शब्द से स्वप्न में भी अभिप्राय की प्रतीति नहीं होती है। जिससे जिस विषय में प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति का होना सम्यक् प्रकार से अनुभव में आता है, वह उसका अर्थ है, यह न्याय है।
भावार्थ-बौद्ध का कहना है कि शब्द बोलने वाले के अभिप्राय मात्र को ही कहते हैं न कि पदार्थों को। इस पर आचार्य आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसा कि लोकव्यवहार में अनुभव आ रहा है कि शब्द अपने वाच्य अर्थ को कहते भी हैं, पुन: प्रतीति के विरुद्ध कथन करना कहाँ तक उचित है ?
🏠
श्रुतभेदा नया: सप्त नैगमादिप्रभेदत:॥
द्रव्यपर्यायमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयानुगं॥16॥
निश्चयात्मकमन्योऽपि व्यतिरेकपृथक्त्वग:॥
निश्चयव्यवहारौ तु द्रव्यपर्यायमाश्रितौ॥17॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[श्रुतभेदा: नया:] श्रुतज्ञान के भेद नय हैं, वे [नैगमादिप्रभेदत:] नैगम आदि के भेद से [सप्त] सात हैं, [ते द्रव्य पर्याय मूला:] वे द्रव्य और पर्यायमूलक हैं। [एकं अन्वयानुगं द्रव्यं] एक और अन्वय का अनुसरण करने वाला द्रव्य है, [निश्चयात्मकं] वह निश्चय स्वरूप है और [अन्य: अपि] अन्य पर्याय भी [व्यतिरेक पृथक्त्वग:] व्यतिरेक तथा पृथक्त्व का अनुसरण करने वाली है। [निश्चय व्यवहारौ तु] निश्चय और व्यवहार तो [द्रव्यपर्यायमाश्रितौ] द्रव्य और पर्याय का आश्रय लेने वाले हैं॥१६-१७॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-वे पूर्वोक्त लक्षण वाले नय होते हैं, वे श्रुत-सकलादेशरूप आगम के भेदरूप हैं इसलिए वे विकलादेश कहलाते हैं। वे नैगम, संग्रह अदि प्रभेदों का आश्रय लेकर सात हो जाते हैं। वे द्रव्य और पर्याय को विषय करने वाले होने से द्रव्य पर्यायमूलक हैं।
(द्रव्य का स्वरूप)
द्रव्य सामान्य होता है, वह एक और अन्वय को अनुसरण करता है अर्थात् व्याप्त करता है। उसमेंअर्थ ता सामान्य पूर्वापर पर्याय में व्यापक है वह एकनुग-एक का अनुसरण करने वाला है और सदृश परिणाम लक्षण जो तिर्यक् सामान्य है वह अन्वयानुंग-अन्वय का अनुसरण करता है पुन: वह द्रव्य निश्चयात्मक है-निकल गया है पर्यायांतर का संकर जिससे, ऐसा जो निश्चय-पर्याय, वह जिसके स्वरूप हैं वैसा है अर्थात् पर्यायांतर के मिश्रण से रहित पर्याय स्वरूप है।
और पुन: अन्य पर्याय को विशेष कहते हैं, वह पर्याय व्यतिरेक और पृथक्त्व का अनुसरण करने वाला है, व्यतिरेक और पृथक्त्व को जो प्राप्त करता है, तादात्म्य रूप से परिणत होता है वह वैसा कहलाता है। उसमें एक द्रव्य में क्रम से होने वाली पर्याय को व्यतिरेक कहते हैं और अर्थांतरगत विसदृश परिणाम पृथक्त्व का अनुसरण करने वाला है।
प्रश्न-अन्य शास्त्रों में निश्चय और व्यवहार नयों को प्रतिपादन किया गया है, उनका क्या आलंबन विषय है ?
उत्तर-वे निश्चय और व्यवहार मूलनय हैं, वे द्रव्य और पर्याय का आलंबन लेते हैं अर्थात् निश्चयनय द्रव्य को विषय करता है और व्यवहारनय पर्याय को विषय करता है। द्रव्य का आश्रय लेने वाला निश्चयनय द्रव्यार्थिक कहलाता है तथा पर्यायाश्रित व्यवहारनय पर्यायार्थिक कहलाता है ऐसा अर्थ हुआ है। यहाँ कारिका में द्रव्यपर्यायं ऐसा पद है ‘उसमें’ ‘द्रव्यं च पर्यायश्च तयो: समाहार:’ ऐसा समाहार द्वंद्व समास करने पर नपुंसकलिंग और एकवचन हो जाता है। ऐसा व्याकरण शास्त्र का नियम है।
🏠
गुणप्रधानभावेन धर्मयोरेकधर्मिणि ॥
विवक्षा नैगमोऽत्यंतभेदोक्ति: स्यात्तदाकृति:॥18॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[धर्मयो:] एकत्व-अनेकत्वरूप दो धर्मों को [गुण प्रधान भावेन] गौण तथा प्रधानभाव से [एकधर्मिणि] एक धर्मी में [विवक्षा] कहने की इच्छा [नैगम:] नैगमनय है और [अत्यंतभेदोक्ति:] दोनों धर्मों में अत्यंत भेद का कथन करना [तदाकृति: स्यात्] नैगमाभास होता है॥१८॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-एकत्व और अनेकत्व ऐसे दो धर्मों को गौण और प्रधान भाव से अर्थात् मुख्य और अमुख्य भाव से एक-अभिन्न, धर्मी-द्रव्य में। कहने का जो अभिप्राय है वह नैगमनय है और अत्यंत रूप से भेद का कथन करना, अत्यंत-निरपेक्षरूप से नानात्व का जो कथन है, ऐसा जो नैयायिक आदि जनों का अभिप्राय नैगमाभास कहलाता है, यहाँ वह अर्थ हुआ है।
🏠
सदभेदात्समस्तैक्यसंग्रहात्संग्रहो नय:।
दुर्नयो ब्रह्मवाद: स्यात्तत्स्वरूपानवाप्तित:॥19।
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[सद्भेदात्] सत् सामान्य के अभेद से [समस्तैक्यसंग्रहात्] समस्त को एकरूप से संग्रह करने से [संग्रह: नय:] संग्रह नय होता है और [ब्रह्मवाद: दुर्नय:] ब्रह्माद्वैतवाद दुर्नय-संग्रहाभास [स्यात्] है [तत्स्वरूपानवाप्तित:] क्योंकि वह ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करने वाला नहीं है॥१९॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-समस्त-जीव-अजीव विशेष को एकरूप से संग्रह करने वाला-संक्षिप्तरूप से ग्रहण करने से संग्रहनय होता है।
प्रश्न-अनेक को संक्षेप से कैसे ग्रहण करता है ?
उत्तर-सत् अभेद से अर्थात् सत् सामान्यरूप जो अभेद है उसका आश्रय करके ग्रहण करता है। ‘सत्त्व से भिन्न किंचित भी वस्तु है’ ऐसा कहना शक्य नहीं है क्योंकि विरोध आता है अर्थात् जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको ‘यह है’ ऐसा कैसे कह सकते हैं ?
दुर्नय संग्रहाभास है, वह कौन है ? वह ब्रह्मवाद अर्थात् सत्ताद्वैत है। क्यों ? उसके स्वरूप को नहीं प्राप्त करने से अर्थात् उस पर परिकल्पित ब्रह्म का स्वरूप भेद के प्रपंचों से शून्य है और सत्तामात्र है उसकी अप्राप्ति होने से, प्रमाण से प्राप्ति न होने से वह दुर्नय है। वह वास्तव में प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राप्त नहीं किया जाता है क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती है।
🏠
व्यवहारानुकूल्यात्तु प्रमाणानां प्रमाणता॥
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसंगत:॥20॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[व्यवहारानुकूल्यात्तु] व्यवहार की अनुकूलता से ही [प्रमाणानां] ज्ञानों की [प्रमाणता] प्रमाणता है [अन्यथा न] अन्य प्रकार से नहीं है, [बाध्यमानानां] अन्यथा बाधित होने वाले [ज्ञानानां] ज्ञानों में भी [तत्प्रसंगत:] प्रमाणता का प्रसंग हो जावेगा॥२०॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-प्रमाणपने से स्वीकृत प्रमाणों की प्रमाणता-अविसंवादकता होती है। कैसे ? व्यवहार की अनुकूलता से अर्थात् संग्रह के विषय में भेद करने वाला व्यवहार है, उसकी अनुकूलता-अविसंवाद है उससे ही प्रमाणता है अन्यथा उसमें विसंवाद होने से प्रमाणता नहीं हो सकेगी। नहीं तो बाध्यमान-बाधित होने वाले संशय आदि विसंवादी ज्ञानों में भी प्रमाणता का प्रसंग आ जावेगा अर्थात प्रमाण आरै अप्रमाण की व्यवस्था का कारण होने से व्यवहारनय कहलाता है अन्यथा वह तदाभास कहलाता है, ऐसा अर्थ है।
🏠
भेदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन् ऋजुसूत्रनयो मत:॥
सर्वथैकत्वविक्षेपी तदाभासस्त्वलौकिक:॥21॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[प्राधान्यत:] प्रधानता से [भेदं] भेद को [अन्विच्छन्] स्वीकार करते हुए [ऋजुसूत्रनय: मत:] ऋजुसूत्रनय माना गया है और [सर्वथा] सब प्रकार से [एकत्वविक्षेपी] एकत्व का निषेध करने वाला [तु अलौकिक: तदाभास:] तो लोकव्यवहार से विरुद्ध तदाभास होता है॥२१॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-प्रधानता से-मुख्यता से भेद को-पर्याय को विषय करते हुए ऋजुसूत्र नय कहलाता है, यह गौणरूप से द्रव्य की भी अपेक्षा रखता है, ऐसा यहाँ अर्थ है। पुन: एकत्व-द्रव्य का निराकरण करने वाला तदाभास है क्योंकि यह सर्वथा प्रधानरूप से और अप्रधानरूप से द्रव्य को ग्रहण करता है और यह अलौकिक है अर्थात् लोकव्यवहार वह प्रयोजन जिसका है वह लौकिक है, उससे विपरीत अलौकिक कहा जाता है। यह तदाभास व्यवहार का विरोधी है, ऐसा अर्थ है। परस्पर में सजातीय-विजातीय से व्यावृत्त प्रतिक्षण विसरारू-जीर्ण होने वाले परमाणु परीक्षकजनों के द्वारा व्यवहार को नहीं प्राप्त होते हैं कि जिससे उसका विषय नयाभास न हो जावे अर्थात् बौद्धों द्वारा मान्य क्षणिक परमाणु व्यवहार में नहीं दिखते हैं इसीलिए उनका ग्राहक नय ऋजुसूत्र नयाभास है।
🏠
चत्त्वारोऽर्थनया ह्येते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्॥
त्रय: शब्दनया: सत्यपदविद्यां समाश्रिता:॥22॥
अकलंकप्रभाभारद्योतितं श्रुतमर्थत:॥
प्रमानयोपयोगात्म सौरी वृत्ति: प्रबोधयेत्॥1॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[ऐते ही चत्वार: अर्थनया:] निश्चितरूप से ये चार ही अर्थ नय हैं [जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्] क्योंकि जीवादि पदार्थों का आश्रय लेते हैं [त्रय: शब्दनया:] शेष तीन शब्दनय हैं, [सत्यपदविद्यां समाश्रिता:] क्योंकि ये व्याकरण शास्त्र का आश्रय लेने वाले हैं॥२२॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-पहले कहे गये जो नैगम आदि नय हैं, उनमें से चार नय अर्थ प्रधान होने से अर्थनय कहलाते हैं क्योंकि ये जीवादि पदार्थों का आश्रय लेते हैं। शेष शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ये तीन नय शब्द प्रधान होने से शब्दनय हैं। ये सत्यपद की विद्या के आश्रित हैं अर्थात् प्रमाणांतर से अबाधित, काल, कारक आदि भेद के वाची पद सत्यपद कहलाते हैं, उन सत्यपदों की विद्या-व्याकरण शास्त्र, उसको आश्रित करने वाले हैं वे व्याकरणशास्त्र के आश्रित हैं ऐसा अर्थ है। उनमें काल, कारक, लिंग आदि के भेद से अर्थ में भेद को करने वाला शब्दनय है। पर्यायवाची शब्दों के भेद से अर्थ में भेद को करने वाला समभिरूढ़नय है और क्रियावाची शब्द के भेद से अर्थ में भेद को करने वाला एवंभूत नय हैं।
भावार्थ-यहाँ पर सात नयों में से चार नयों का लक्षण तो कारिकाओं में कह ही दिया है अत: श्री अभयचंद्रसूरि ने शब्दादि तीन नयों का लक्षण संक्षेप से कह दिया है क्योंकि कारिका में भी श्री अकलंकदेव ने इन तीन नयों को सत्यपद की विद्यारूप शब्द शास्त्र के आश्रित कहा है।
श्लोकार्थ-अकलंक-निर्दोष प्रभा के भार से प्रकाशित श्रुत-आगम को जो कि अर्थ से प्रमाणनय और उपयोगस्वरूप है इसको सौरीवृत्ति-श्रीअभयचंद्रसूरि की वृत्ति प्रबोधित करती है।।१।।
भावार्थ-श्रीमान् भट्टाकलंकदेव ने कारिकाओं के द्वारा जिनके स्वरूप को कहा है और श्री प्रभाचंद्राचार्य ने न्यायकुमुद टीका के द्वारा उनका विशद विवेचन किया है पुन: उन दोनों के अभिप्राय को ज्ञातकर श्री अभयचंद्रसूरि ने संक्षेप से सारभूत इस आगम के परिच्छेद में प्रमाण, नय तथा उपयोग के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया है, ऐसा अर्थ है।
इस प्रकार श्री अभयचंद्रसूरि कृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण नामक तात्पर्यवृत्ति में श्रुतोपयोग नाम का छठा परिच्छेद पूर्ण हुआ।
🏠
श्रुतादर्थमनेकांतमधिगम्याभिसंधिभि:॥
परीक्ष्य ताँस्तान् तद्धर्माननेकान् व्यावहारिकान् ॥1।
नयानुगतनिक्षेपैरुपायैर्भेदवेदने ॥
विरचय्यार्थवाक्प्रत्ययात्मभेदान् श्रुतार्पितान्॥2॥
अनुयुज्यानुयोगैश्च निर्देशादिभिदागतै:॥
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनिवेशन:॥3॥
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतत्त्ववित्॥
तपोनिर्जीर्णकर्माऽयं विमुक्त: सुखमृच्छति॥4॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[श्रुतान] श्रुत से [अनेकांत] अनेकांतात्मक [अर्थं अधिगम्य] अर्थ को जानकर [तांस्तान्] उन-उन [अनेकात् व्यावहारिकान्] अनेक व्यावहारिक [तद्धर्मान्] उस-वस्तु के धर्मों की [अभिसंधिभि:] ज्ञाता के अभिप्रायरूप नयों से [परीक्ष्य] परीक्षा करके [उपायै:] ज्ञान के लिए उपायभूत [नयानुगतनिक्षेपै:] नयों का अनुसरण करने वाले ऐसे निक्षेपों से [भेदवेदने] भेदों के जानने में [श्रुतार्पितान्] श्रुत से विकल्पित [अर्थवाक्यप्रत्यात्म भेदान्] अर्थात्मक, वचनात्मक और ज्ञानात्मक भेदों का [विरचय्य] न्यास करके-कथन करके, [आत्मा] जीव [विवृद्धाभिनिवेशन:] वृद्धि को प्राप्त हुए सम्यग्दर्शन से सहित [निर्देशादिभिदागतै:] निर्देश आदि भेदों को प्राप्त हुए ऐसे [अनुयोगै:] अनुयोगों से [जीवादीनि] जीवादिक [द्रव्याणि] द्रव्यों को [अनुयुज्य] पूछ करके [जीवस्थानगुणस्थानमार्गणा स्यात् तत्त्ववित्] जीवस्थान, गुणस्थान और मार्गणा स्थानों के द्वारा तत्त्व-जीवादिस्वरूप को जानने वाला [तपोनिर्जीर्णकर्मा] तप से कर्मों को निर्जिर्ण कर दिया है जिसने [अयं] ऐसा यह [विमुक्त:] कर्मों से मुक्त हुआ [सुखं] सुख को [ऋच्छति] प्राप्त करता है॥१-२-३-४॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध आत्मा विमुक्त होता हुआ वि-विशेष रूप से (समस्त रूप से) मुक्त-कर्मरहित होता हुआ परम स्वास्थ्यरूप अनंतज्ञानादि गुणस्वरूप सुख को प्राप्त कर लेता है। वह कैसा है आत्मा ? तप से कर्म को जिसने निर्जीण कर दिया है, तप-यथाख्यात चारित्र लक्षण वाले व्युपरतक्रियानिवृत्तिरूप चतुर्थ शुक्लध्यान से जिसने ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म का और भावकर्म का निर्मूलन कर दिया है वह आत्मा ऐसा है। इस कथन से चारित्र और तप इन दो आराधनाओं को सूचित किया है। पुन: कैसा है ? जीवस्थान, गुणस्थान और मार्गणास्थान को जानने वाला है। समास, स्थान, योनि, अवगाहना और कुलों के भेद को जीवस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व आदि परिणामों के स्थान-पद को गुणस्थान कहते हैं और अन्वेषण के उपायभूत गति आदि मार्गणा के स्थान को मार्गणास्थान कहते हैं। इनके प्रत्येक के चौदह-चौदह भेद हैं अर्थात् जीवसमास चौदह हैं, गुणस्थान चौदह हैं और मार्गणास्थान भी चौदह हैं, इनके भेदों से तत्त्व को-जीव के स्वरूप को जो जानता है वह तत्त्ववित् कहलाता है। इस कथन से ज्ञान की आराधना को बतलाया है।
पुन: वह आत्मा कैसा है ?
वृद्धिंगत अभिनिवेश-श्रद्धान वाला है। वि-विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त क्षायिक रूप से परिणत है अभिनिवेश-सम्यग्दर्शन जिसका ऐसा वह आत्मा है। इस कथन से दर्शनाराधना का निरूपण किया है। इस प्रकार से इन चार आराधनाओं से ही मोक्षमार्ग बन सकता है क्योंकि १सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्षमार्ग है, ऐसा सूत्रकार का वचन है।
प्रश्न-सूत्र में रत्नत्रय को मोक्षमार्ग कहा है और आपने यहाँ पर आराधना चतुष्टय को मोक्षमार्ग प्रतिपादित किया है, इसलिए विरोध आता है ?
उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि तप चारित्र में अंतर्भूत हो जाता है अत: वैसा प्रतिपादन संभव है। चारित्र ही कर्मनिर्जरा में हेतु होने से तपरूप से प्रतिपादित किया जाता है। वास्तव में चारित्र को छोड़कर तप नहीं है अन्यथा वह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। बहिरंग तपश्चरण रत्नत्रय का साधन है और अंतरंग तपश्चरण तो चारित्रविशेषरूप है अतएव शास्त्र में उसका पृथक् निर्देश नहीं किया है।
प्रश्न-क्या करके विवृद्ध अभिनिवेश उत्पन्न होता है ?
[उत्तर-जीवादि द्रव्यों को अनुयुक्त करके-पूछ करके उत्पन्न होता है। ‘द्रवति द्रोष्यति अदुदु्रवत् इति द्रव्यं’ जो द्रवित होता है-परिणत होता है, होवेगा और होता था, वह द्रव्य है अथवा गुणपर्यय वाला द्रव्य है। इस द्रव्यलक्षण से लक्षित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन नाम वाले जीवादि द्रव्य होते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान इन छह अनुयोगों से- प्रश्नों से तथा सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ भेदों को प्राप्त हुए प्रश्नों से जीवादि द्रव्यों को जानना चाहिए।
उसी का स्पष्टीकरण करते हैं-
(निर्देश आदि का लक्षण)
क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है, जैसे-चेतना लक्षण वाला जीव है।
किसका है ? ऐसा पूछने पर ‘अपना है’ इस आधिपत्य का कथन करना स्वामित्व है।
किनके द्वारा ? ऐसा प्रश्न होने पर ‘अपने द्वारा’ इस प्रकार से करण का निरूपण करना साधन है।
किसमें ? ऐसा प्रश्न होने पर ‘अपने में’ ऐसे आधार का प्रतिपादन करना अधिकरण है।
कितने काल तक ? ऐसा प्रश्न होने पर ‘अनंत काल पर्यंत’ ऐसे काल का प्ररूपण करना स्थिति है।
कितने प्रकार ? ऐसा प्रश्न होने पर जीव चैतन्य सामान्य से एक प्रकार का है इस प्रकार से प्रकार का कथन करना विधान है।
इस प्रकार से निर्देश आदि छह अनुयोगों का व्याख्यान किया है। मध्यम रुचि वाले शिष्यों के अभिप्राय के निमित्त से ये अनुयोग संभव होते हैं। विस्तार रुचि वाले शिष्यों के अभिप्राय से पुन: सत् आदि का व्याख्यान करते हैं।
(सत् आदि का लक्षण)
उनमें द्रव्य पर्याय, सामान्य, विशेष और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य में जो व्यापक है वह सत् है, ऐसा कथन करना सत् का प्ररूपण है, जैसे जीव हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, सासादन सम्यग्दृष्टि हैं, सम्यग्मिथ्यादृष्टि हैं, असंयतसम्यग्दृष्टि हैं, देशसंयत हैं, प्रमत्तसंयत हैं, अप्रमत्तसंयत हैं, अपूर्वकरणसंयत हैं, अनिवृत्तिकरण बादरसांपराय संयत हैं, सूक्ष्मसांपराय संयत हैं, उपशांतकषाय छद्मस्थ वीतरागी हैं, क्षीणकषाय छद्मस्थ वीतरागी हैं, सयोगीकेवली हैं, अयोगीकेवली हैं और शुद्धात्मा सिद्ध हैं इत्यादि।
भेद की गणना करना संख्या है। जैसे जीव अनंतानंत हैं, मिथ्यादृष्टि अनंतानंत हैं इत्यादि।
वर्तमान के निवास को क्षेत्र कहते हैं। जैसे जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग है, संख्यातवें भाग है अथवा सर्वलोक है इत्यादि। उसी त्रिकालविषयक निवास को स्पर्शन कहते हैं। जैसे जीव का सर्वलोक आदि स्पर्श है। उतने काल रहने को काल कहते हैं। जैसे गुणस्थान का आयामकाल अंतर्मुहूर्त आदि है।
विवक्षित गुणस्थान को छोड़कर गुणस्थानांतर को प्राप्त हुए को, पुन: उस गुणस्थान की प्राप्ति जितने काल में होती है उतना काल अंतर कहलाता है, इसे विरहकाल भी कहते हैं, यह अंतर्मुहूर्त आदि के प्रमाण से होता है।
आत्मा के परिणाम को भाव कहते हैं। ये औदयिक आदि हैं।
परस्पर में संख्या की विशेषता को अल्पबहुत्व कहते हैं। ये सत् आदि आठ अनुयोग कहलाते हैं।
पूर्व में इनका न्यास करके अर्थात् अर्थ स्वभाव, वचन स्वभाव और ज्ञानस्वभाव वाले भेद व्यवहार को पूर्व में करके। उनमें से अर्थस्वभाव वाले के भेद द्रव्य और भाव ऐसे दो होते हैं क्योंकि ये अर्थ के धर्म हैं। वचनात्मक नाम व्यवहार है और ज्ञानस्वरूप स्थापना व्यवहार है क्योंकि वह संकल्परूप है अर्थात् नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार निक्षेप होते हैं। इनमें से नाम निक्षेप वचनस्वरूप है, स्थापनानिक्षेप ज्ञानस्वरूप है और द्रव्य तथा भावनिक्षेप अर्थस्वरूप हैं। इनसे भी जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। ये श्रुतार्पित-श्रुत-अनेकांत से विकल्पित हैं। ये चारों निक्षेप नय के अनुगत हैं अर्थात् नयों का-द्रव्य पर्याय रूप विषयों का अनुसरण करने वाले हैं और ये भेद के वेदन में-मुख्य गौणरूप विशेष के निर्णय में उपायभूत हैं-कारण हैं।
इन कारण भेदों से द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से विवक्षित धर्मों का विचार करके अर्थात् अनेकांतात्मक वस्तु के जो अस्तित्वादि अनंत धर्म हैं और व्यावहारिक हैं-हान, उपादान आदि प्रयोजन वाले हैं, उनको ज्ञाता के अभिप्रायरूप नयों के द्वारा प्रमेयरूप जीवादि पदार्थों को पहले जान करके। वे अर्थ अनेकांतात्मक हैं, अनेक अंत-सहभावी और क्रमभावी धर्म जिसमें पाये जाते हैं वह अनेकांत कहलाता है। उन अनेकांतात्मक जीवादि पदार्थों को श्रुत से-स्याद्वाद से जान करके श्रद्धान करते हैं क्योंकि ‘अनेकांत को प्रमाण से१’ जाना जाता है ऐसा वचन है। यहाँ पर संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के अभिप्राय के निमित्त से यह कहा गया है। यहाँ पर अभिप्राय यह हुआ है कि-
अनेकांतात्मक जीवादि पदार्थ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त सत् हैं इत्यादि को आगम से निश्चित करके पुन: संक्षेप रूप वाले ज्ञाता उन धर्मों की व्यवहार के लिए नैगम आदि नयों से परीक्षा करते हैं क्योंकि उनको उतने से ही तत्त्वों का बोध होना संभव है। पुन: मध्यम रुचि वाले शिष्य विशेष को जानने के लिए उपायभूत ऐसे नाम आदि निक्षेपों से अर्थ, वचन और ज्ञानरूप भेदों का न्यास करके-कथन करके निर्देश, स्वामित्व आदि अनुयोगों से प्रश्न करते हैं, समझते हैं क्योंकि उन लोगों को उतने विस्तार की आकांक्षा है तथा विस्तार रुचि वाले शिष्य जीवादि द्रव्यों में से प्रत्येक को सत्, संख्या, क्षेत्र आदि अनुयोगों से प्रश्न करके-समझ करके गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति आदि भेदों से तत्त्व को जानते हैं।
इससे विशुद्ध अधिगम सम्यग्दर्शन से सहित होते हुए जीव शुक्लध्यानरूपी अंतरंग तप से संपूर्ण कर्मों का निर्मूलन करके विमुक्त होते हुए उस ज्ञान के फलरूप सुख का अनुभव करते हैं।
प्रश्न-इस प्रकार से प्रमाण, नय और निर्देश आदि का स्वरूप तो जान लिया गया है, निक्षेप क्या हैं ? सो अब प्रतिपादित कीजिए ?
उत्तर-जो जानने के लिए उपायभूत हैं वे निक्षेप कहलाते हैं, वे चार हैं-नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भावनिक्षेप। उनमें से जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया यह नाम हैं, जैसे-प्रतीहार इत्यादि। एक जीव अनेक जीव नाम जैसे (कावड़ी को ढ़ोने वाला कहार) काकावलिकावाही हार इत्यादि, अनेक जीव एक जीव नाम जैसे-आंदोलक इत्यादि। अनेक जीव अजीव नाम, जैसे-नगर इत्यादि। नाम को प्राप्त हुए द्रव्य में वह यह है, इस प्रकार के संकल्प से व्यवस्थापित की गई स्थापना है। उसके दो भेद हैं-सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। उनमें मुख्यद्रव्य की आकृति को सद्भाव स्थापना कहते हैं जैसे-अर्हत्प्रतिमा आदि। तदाकार से शून्य असद्भाव स्थापना है जैसे-कौड़ी आदि में किसी की स्थापना करना आदि।
द्रव्यनिक्षेप के भी दो भेद हैं-आगम और नोआगम। उनमें से जो जीवादि के विषयक शास्त्र का ज्ञाता है किन्तु चिरकाल से दूसरों को प्रतिपादन आदि के उपयोग से रहित है ऐसा श्रुतज्ञानी आगमद्रव्य है। नोआगमद्रव्य के तीन भेद हैं-ज्ञायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। उसमें जीवादि प्राभृत के ज्ञाता के शरीर के भी तीन भेद हैं-भूत, भविष्यत् और वर्तमान। भूत शरीर के भी तीन भेद हैं-च्युत, च्यावित और त्यक्त। उसमें समाधिमरण से छूटे हुए शरीर को त्यक्त कहते हैं। उसके भी तीन भेद हैं-प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्तप्रत्याख्यान।
अपने आयु के पूर्ण होने के निमित्त से छूटा हुआ शरीर च्युत कहलाता है। वेदना आदि के निमित्त से आयु के खंडित हो जाने से छूटा हुआ शरीर च्यावित कहलाता है।
नोआगमद्रव्य के भावी भेद को कहते हैं-गत्यंतर में स्थित हुआ जीव जो मनुष्यत्व आदि के अभिमुख है उसे भावी कहते हैं। कर्म और नोकर्म के भेद से तद्व्यतिरिक्त के भी दो भेद हैं। उसमें आत्मा को परतंत्रता के निमित्त से जो ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार का कर्म है वह कर्मतद्व्यतिरिक्त है। तीन शरीर और छह पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परिणाम नोकर्म तद्व्यतिरिक्त है अर्थात् औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच शरीर हैं इनमें से आदि के तीन शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं ही नोकर्म हैं। औदारिक, वैक्रियिक और आहारक में तैजस का अंतर्भाव हो जाता है और विग्रहगति में कार्मण शरीर अंतर्भूत होता है।
भावनिक्षेप के भी आगम और नोआगम की अपेक्षा दो भेद हैं। उसमें जीवादिप्राभृत का ज्ञाता, जो कि उसमें उपयुक्त हुआ श्रुतज्ञानी है, वह आगमभाव जीव है। विवक्षित पर्याय से परिणत हुआ नोआगम जीव है।
प्रश्न-निक्षेप के अभाव में भी केवल प्रमाण और नयों में तत्त्वार्थ का स्वरूप जाना ही जाता है ?
उतर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ये निक्षेप अप्रकृत को निराकरण करने के लिए होते हैं और प्रकृत का प्ररूपण करने के लिए होते हैं। नामादि के अप्रकृत में प्रमाण और नय से जाने गये पदार्थ व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होते हैं क्योंकि मुख्य और उपचार के विभाग से ही उनकी सिद्धि होती है और नामादि निक्षेपों के बिना वह मुख्य-उपचार रूप विभाग संभव नहीं है कि जिससे उनके अभाव में भी तत्त्वों का बोध हो सके अर्थात् निक्षेप के बिना भी तत्त्वों का बोध नहीं हो सकता है।
विशेषार्थ-यहाँ पर आचार्य ने चार आराधना के फल को बतलाया है। तब प्रश्न यह हो गया है कि सूत्रकारों ने रत्नत्रय को ही मोक्ष का मार्ग कहा है और चार आराधनाओं से मोक्षफल प्राप्ति का संकेत किया है, यह क्या बात है ? इस पर टीकाकार ने समाधान कर दिया है कि जहाँ रत्नत्रय को मोक्षमार्ग कहा है वहाँ पर चारित्र में ही तप आराधना गर्भित है और जहाँ चार आराधना को मोक्षमार्ग कहा है वहाँ केवल भेद विवक्षा ही है।
पुन: सम्यक्त्व के विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानने के लिए जो उपाय है, उनका स्पष्टीकरण किया है। उनमें सबसे प्रथम निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोगों को बताया है अनंतर सत्, संख्या, क्षेत्र आदि आठ अनुयोगों को स्पष्ट किया है क्योंकि मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए निर्देश आदि छह प्रकार हैं, विस्तार रुचि वालों के लिए सत् आदि आठ प्रकार हैं। इसके बाद चार निक्षेपों से पदार्थों को जानने का उपदेश दिया है और प्रमाण तथा नयों से भी समझने को कहा है। यह संक्षेप रुचि वालों के लिए उपाय है। यहाँ पर उन चार निक्षेपों के प्रभेदों का अच्छा स्पष्टीकरण है। प्रश्न यह होता है कि संक्षेप रुचि वाले शिष्य प्रमाण और नयों से ही पदार्थों को समझ लेते हैं पुन: निक्षेपों की क्या आवश्यकता है ? इस पर आचार्य ने कहा है कि बिना निक्षेप के मुख्य और उपचार की व्यवस्था असंभव है तथा प्रकृत का प्ररूपण और अप्रकृत का निराकरण यह भी निक्षेप से ही होता है।
🏠
भव्य: पंचगुरून् तपोभिरमलैराराध्य बुध्वाऽऽगमं।
तेभ्योऽभ्यस्य तदर्थमर्थविषयाच्छब्दादपभ्रंशत:॥
दूरीभूततरात्मकादधिगतो बोद्धाऽऽकलंकं पदं।
लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञो जिन: स्यात् स्वयं ॥5॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[भव्य:] भव्य जीव [अमलै: तपोभि:] निर्दोष तपश्चरण से [पंचगुरुन् आराध्य] पंच परम गुरुओं की आराधना करके, [आगमं बुद्ध्वा] आगम को जानकर, [तेभ्य: तदर्र्थं अभ्यस्य] उन गुरुओं से उस आगम के अर्थ का पुन:-पुन: अभ्यास करके [दूरी भूततरात्मकात्] दूरी भूततररूप [अर्थविषयात्] अर्थ को विषय करने वाले [अपभ्रंशत:] अपभ्रंश शब्दों से [आकलंकं पदं] निर्दोष-आर्हंत्यपद को [अधिगत: बोद्धा] प्राप्त हुआ ज्ञाता [लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञ:] लोक-अलोक के विभाग के अवलोकन में शक्ति और प्रकृष्ट ज्ञान से सहित हुआ [स्वयं] स्वयं ही [जिन:] ‘जिन’ [स्यात्] हो जाता है॥५॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-जो मोक्ष के हेतुभूत रत्नत्रयरूप से होगा-परिणमन करेगा, वह भव्य है क्योंकि अभव्य को मुक्ति में अधिकार ही नहीं है। ऐसा भव्य जीव षट्द्रव्य के समुदायरूप लोक और उसके बाहर केवल आकाशरूप अलोक, इन दोनों की कला-विभाग अथवा लोक, अलोक तथा कला-जीवादि पदार्थ इनके अवलोकन में बल-शक्ति और प्रज्ञा-प्रकृष्ट ज्ञान है जिनके, ऐसा लोकालोक की कला को जानने की शक्ति और ज्ञान से सहित हुआ स्वयं-इंद्रियादि की सहायता के बिना अपने आत्मा के द्वारा, अकलंकों का जो पद है-आर्हंत्यपद है उसको प्राप्त होता हुआ जिन हो जाता है।
प्रश्न-मुक्ति में जीव के ज्ञान का अभाव है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वभाव से रहित है ?
उत्तर-नहीं, मुक्ति में भी वह जीव बोद्धा है, ज्ञान स्वभाव वाला होने से जानने वाला है।
प्रश्न-पूर्व में क्या करके जानता है ?
उत्तर-पहले पंचपरमगुरु के निमित्त से अवधिभूत शब्द से-वर्ण, पद, वाक्यात्मक प्रयोग से जो अर्थ को-जीवादि वस्तु को विषय करने वाला है उन शब्दों से उस आगम को पढ़ करके और जान करके पुन: उस आगम के अर्थरूप जीवादि वस्तु का अभ्यास करके पुन:-पुन: भाषित करके-यहाँ शब्द से अर्थ को जानने के कथन से बौद्ध के कथन का निरसन किया है अर्थात् बौद्ध कहता है कि शब्द का विषय अन्यापोह है, यहाँ उसका निराकरण हो जाता है क्योंकि शब्द की अन्यापोह में प्रवृत्ति नहीं होती है।
प्रश्न-पुन: वे शब्द कैसे हैं ?
उत्तर-अपभ्रंश रूप हैं, भ्रंश-लक्षणदोष-व्याकरण के दोष से अप-रहित हैं। इस कथन से ‘यो जागार’ इत्यादि वाक्यों की अप्रमाणता का प्रतिपादन किया है।
प्रश्न-पुन: क्या करके वे ज्ञाता होते हैं ?
उत्तर-पूर्व में मिथ्यात्वादि मल दोषों से रहित, इच्छा निरोधरूप बाह्याभ्यंतर तपश्चरणों से अर्हंत, सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों की आराधना करके ऐसे ज्ञानी होते हैं क्योंकि पंचपरमगुरु के चरण ही परम मंगल स्वरूप हैं। उनके गुण समूह का अनुस्मरण शास्त्र की परिसमाप्ति में सफलीभूत है। इस प्रकार से यहाँ परमागम के अभ्यास से स्वार्थ संपत्ति का कथन किया गया है।
🏠
प्रवचनपदान्यभ्यस्यार्थांस्तत: परिनिष्ठिता-।
नसकृदवबुद्ध्येद्धाद्बोधाद्बुधो हतसंशय:॥
भगवदकलंकानां स्थानं सुखेन समाश्रित:।
कथयतु शिवं पंथानं व: पदस्य महात्मनां॥6॥
अन्वयार्थ : अन्वयार्थ-[प्रवचनपदानि] प्रवचन के पदों का [अभ्यस्य] अभ्यास करके [तत: परिनिष्ठितान् अर्थान्] उसमें व्यवस्थित अर्थों को [असकृत्] पुन:-पुन: [अवबुध्य] निश्चित करके [हतसंशय:] संशयादि दोषों से रहित [इद्धात् बोधात्] उज्ज्वल बोध से युक्त [बुध:] ज्ञानी [भगवदकलंकानां] भगवान् अकलंक- अर्हंतदेव के [स्थानं समाश्रित:] स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे [महात्मनां] सिद्ध आत्माओं के [पदस्य] पद के [शिवं पंथानं] कल्याणकारी मार्ग को [व:] आप लोगों के लिए [सुखेन] तालु आदि के व्यापार के क्लेश से रहित सुखपूर्वक [कथयतु] प्रतिपादित करें॥६॥
अभयचन्द्रसूरि :
तात्पर्यवृत्ति-बुध-ज्ञानी महात्मा के-संसारी से अतिरिक्त सिद्धात्माओं के पद के शिवमार्ग को-मोक्ष की प्राप्ति के उपाय को आप सभी शिष्यों के लिए प्रतिपादित करें। कैसे प्रतिपादित करें ? सुख से-तालु, ओष्ठपुट, व्यापार के क्लेश के अभाव से। कैसे होते हुए ? त्रिलोक में पूजा के योग्य और दोष-आवरणरूप कलंक से रहित अकलंक हैं ऐसे भगवान् अर्हंतदेव के स्थान को जो प्राप्त हो चुके हैं, न कि क्षणिक स्थान को क्योंकि वहाँ पर उपदेश का अभाव है।
वे कैसे होते हुए इस स्थान को प्राप्त हुए हैं ? संशयरहित होते हुए-यहाँ यह संशय शब्द उपलक्षण मात्र है इसलिए नष्ट हो गये हैं संशय आदि दोष जिनके ऐसे होते हुए। क्या करके नष्ट हुए हैं ? उन प्रवचन पदों में व्यवस्थित जीवादि पदार्थों को ज्ञान से पुन:-पुन: निश्चित करके-ध्या करके। वह ज्ञान कैसा है ? इद्ध-उज्ज्वल है-संकर व्यतिकर से रहित है, मैं-मैं इस रूप प्रकाशमान है।
क्या करके निश्चित करते हैं ? उन प्रवचन पदों का अभ्यास करके पुन:-पुन: उपयोग करके। वे प्रवचनपद कैसे हैं ? प्रकृष्ट पूर्वापर विरोध रहित वचन प्रवचन हैं अथवा प्रकृष्ट पुरुष के वचन प्रवचन हैं, उस प्रवचन के पद ‘सम्यग्दर्शन’ आदि अथवा ‘णमो अरिहंताणं’ इत्यादि हैं।
परमागम के अभ्यास से श्रुतज्ञानरूप परिणत होते हुए, पुन: शुक्लध्यानरूपी अग्नि से दग्ध कर दिया द्रव्य कलंक और भाव कलंक को जिसने ऐसे भगवान सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे पर के लिए मोक्षमार्ग के उपदेश में चेष्टा करें-प्रयत्न करें, ऐसा श्रीमान् भट्टाकलंक देव का अभिप्राय है।
भावार्थ-यहाँ पर आचार्यदेव ने प्रवचन के अभ्यास की महत्ता को स्पष्ट किया है। वास्तव में जिनागम के अभ्यास से ही भव्य जीव ज्ञान और वैराग्य शक्ति से अपने आत्मबल को बढ़ा लेते हैं और पुन: दुद्र्धर तपश्चरण आदि का अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचिन्तानिरोधरूप ध्यान से परिणत होकर घातिया कर्मों का नाश करके अर्हंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं पुन: वे ही हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर महापुरुष भव्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हुए असंख्यातों जीवों को संसार समुद्र से पार करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा परमागम का उपदेश सदैव हमें मोक्षमार्ग का प्रकाश करता रहे।
🏠
नाभ्यासस्तादृगस्ति प्रवचनविषयो नैव बुद्धिश्च तादृक।
नोपाध्यायोऽपि शिक्षानियमनसमयस्तादृशोऽस्तीह काले॥
विंâत्वेतन्मे मुनींदुव्रतिपतिचरणाराधनोपात्तपुण्यं।
श्रीमद्भट्टाकलंकप्रकरणविवृतावस्ति सामथ्र्यहेतु:॥1॥
माऽयं मदांध इति चेतसि कोपमाधु-।
र्माधुर्यमेव वहते सुधियां मदुक्ति:॥
किं कामिनीजनमदोत्कटचाटुवाणी।
प्राणेश्वरस्य रसनाटकनर्तकी न॥2॥
तथाऽप्येतत्परीक्षंतां। मदुक्तम् मत्सरोज्झिता:॥
हीनाधिकमभिव्यक्तु। मेते हि निकषोपमा:॥3॥
विरुद्धं दर्शनं यस्य। निह्नवस्तस्य विंâकर:।
तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यं किं। घूकशूकोऽर्वâमृच्छति॥4॥
-अंतिम आशीर्वाद:-
भद्रमस्तु जिनशासनश्रिये। श्रायसैकपदकार्यजन्मने॥
जन्मजन्मकृततापलोपन-। प्रायशुद्धनिजतत्त्ववित्तये॥1॥
अन्वयार्थ : [अर्थ]-न तो मेरा वैसा प्रवचनविषयक अभ्यास है और न वैसी मुझमें बुद्धि है, न इस पंचमकाल में नियमितरूप से आगम की शिक्षा देने वाले उपाध्याय ही हैं किन्तु फिर भी जो मुनीन्दु व्रतियों के स्वामी हैं उनके चरणों की आराधना से उपार्जित किया हुआ ही यह पुण्य है कि जो श्रीमान् भट्टाकलंकदेव के इस लघीयस्त्रय प्रकरण की विवृत्ति-वृत्तिरूप टीका के करने में समर्थवान हेतु है॥१॥
[अर्थ]-‘यह मदांध है’ इस प्रकार से चित्त में क्रोध को मत कीजिए क्योंकि मेरे वचन विद्वानजनों में मधुरता को ही धारण करते हैं। क्या कामिनी स्त्रियों के मद से उत्कट हुए चाटुकर वचन उनके पतिदेव के रस नाटक को नर्तन कराने वाले नहीं होते हैं॥२॥
[भावार्थ]-जैसे स्त्रियों के प्रिय वचन उनके पतिदेवों को मधुर लगते हैं वैसे ही मेरे ये टीका में कहे गये वचन भी विद्वानों को मधुर लगेंगे।
[अर्थ]-फिर भी मत्सरभाव से रहित बुधजन इन मेरे वचनों की परीक्षा करें क्योंकि ये हीनाधिक को प्रगट करने के लिए कसौटी के पत्थर के समान हैं॥३॥
[भावार्थ]-श्री अभयचंद्राचार्य कहते हैं कि जिनके हृदय में मत्सर, ईष्र्या आदि भाव नहीं हैं ऐसे बहुश्रुतज्ञानी इस मेरे ग्रंथ की समीक्षा करें क्योंकि जैसे कसौटी का पत्थर इस सुवर्ण में कितने अंश में अन्य धातु का मिश्रण है या नहीं है इस बात को स्पष्ट बता देता है ऐसे ही यह मेरा ग्रंथ भी हीनाधिक दोषों को स्पष्ट कर देता है अर्थात् यह ग्रंथ हीनाधिक दोषों से रहित, निर्दोष, सरल और संक्षिप्त है और न्याय के क्लिष्ट विषय का प्रतिपादन करने वाला होते हुए भी इसकी सुंदर कथन शैली से विषय मधुर बन गया है।
[अर्थ]-जिनका दर्शन-सिद्धांत विरुद्ध है, निन्हव उनका किंकर है, क्या किरणों से दुर्निरीक्ष्य जिसको देखना कठिन है ऐसे सूर्य को उल्लू का बालक देख सकता है ?॥४॥
[भावार्थ]-जिनका मत स्याद्वाद से विपरीत एकांतरूप है उनका नौकर निन्हव है अर्थात् वे हमेशा सच्चे तत्त्वों का अपलाप किया करते हैं, सो ठीक ही है क्योंकि उल्लू के बच्चे को संख्यातों किरणों से व्याप्त ऐसा तेजस्वी सूर्य नहीं दिख सकता है वैसे ही नयरूपी संख्यातों किरणों से व्याप्त ऐसे स्याद्वादरूपी सूर्य का दर्शन वे एकांतवादी लोग नहीं कर सकते हैं। इस कथन से यहाँ पर अनेकांत की दुर्लभता को बतलाया है।
इस प्रकार से श्री अभयचंद्रसूरिकृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण नामक तात्पर्यवृत्ति टीका में निक्षेप का प्ररूपण करने वाला सप्तम परिच्छेद पूर्ण हुआ।
प्रवचनप्रवेश नामक तृतीय महा अधिकार पूर्ण हुआ।
इस प्रकार से श्री भट्टाकलंकदेव रूपी चंद्रमा से अनुस्मृत लघीयस्त्रय नामक प्रकरण समाप्त हुआ है।
[अंतिम आशीर्वाद]
[श्लोकार्थ]-जन्म-जन्म में किये हुए ताप का लोप करने में प्राय: शुद्ध निजतत्त्व के ज्ञान स्वरूप, मोक्षरूप एक अद्वितीय पद उस पदस्वरूप कार्य को उत्पन्न करने वाली ऐसी जो जिनशासनरूपी लक्ष्मी है उसके लिए भद्र-कल्याण होवे॥१॥
[भावार्थ]-जो जिनशासन भव्यजीवों के जन्म-जन्म के संताप को दूर करने में समर्थ ऐसे शुद्ध आत्मा तत्त्व का बोध कराने वाला है और जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है उस जिनशासन का सदा ही कल्याण होवे अथवा वह सदैव हितस्वरूप होता हुआ जयशील रहे।
🏠