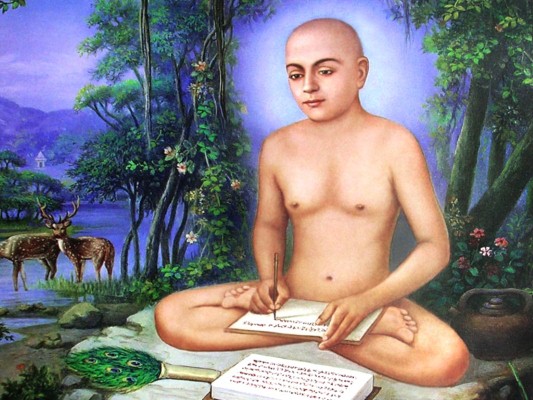ब्रह्मदेव सूरि : संस्कृत[मग्गणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया] जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए १४ जीवसमासों से जीवों के १४ भेद होते हैं उसी तरह मार्गणा और गुणस्थानों से भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए । मार्गणा और गुणस्थानों से कितनी संख्या वाले होते हैं? [चउदसहि] प्रत्येक से १४१४ संख्या वाले हैं किस अपेक्षा से? [अशुद्धणया] अशुद्धनय की अपेक्षा से । मार्गणा और गुणस्थानों से अशुद्ध नय की अपेक्षा चौदह-चौदह प्रकार के कौन होते हैं? संसारी संसारी जीव होते हैं । [सव्वे सुद्धा हुसुद्धणया] वे ही सब संसारी जीव शुद्ध यानि-स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप एक-स्वभावधारक हैं । किस अपेक्षा से? शुद्ध नय से अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से । अब शास्त्र प्रसिद्ध दो गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं -- १. मिथ्यात्व, २. सासादन, ३. मिश्र, ४. अविरतसम्यक्त्व, ५. देशविरत, ६. प्रमत्तविरत, ७. अप्रमत्तविरत, ८. अपूर्वकरण, ९. अनिवृत्तिकरण, १०. सूक्ष्मसाम्पराय,११. उपशांतमोह, १२. क्षीणमोह, १३.सयोगकेवली और १४. अयोगकेवली । इस तरह क्रम से चौदह गुणस्थान जानने चाहिए ॥२॥ अब इन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षेप से लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार - स्वाभाविक शुद्ध केवलज्ञान केवलदर्शन रूप अखण्ड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास-मय निजपरमात्मा आदि षट् द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थों में तीन मूढ़ता आदि पच्चीस दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नयविभाग से जिस जीव के श्रद्धान नहीं है वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है ॥१॥
- पाषाणरेखा (पत्थर में उकेरी हुई लकीर) के समान जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय से प्रथम-औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो, तब तक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव सासादन होता है ॥२॥
- जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वों को वीतराग सर्वज्ञ के कहे अनुसार मानता है और अन्य मत के अनुसार भी मानता है वह मिश्रदर्शनमोहनीय कर्म के उदय से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भाँति मिश्र-गुणस्थान वाला है ॥३॥
शंका - 'चाहे जिससे हो मुझे तो एक देव से मतलब है अथवा सब ही देव वन्दनीय हैं, निन्दा किसी भी देव की न करनी चाहिए' इस प्रकार वैनयिक और संशय मिथ्यादृष्टि मानता है; तब उनमें तथा मिश्र-गुणस्थानवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि में क्या अन्तर है?
उत्तर - वैनयिक मिथ्यादृष्टि तथा संशयमिथ्यादृष्टि तो सभी देवों में तथा सब शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है; उसको किसी एक देव में निश्चय नहीं है और मिश्रगुणस्थानवी जीव के दोनों में निश्चय है । बस, यही अन्तर है । - जो 'स्वाभाविक अनंतज्ञान आदि अनंतगुण का आधारभूत निज परमात्मद्रव्य उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि परद्रव्य त्याज्य हैं' इस तरह सर्वज्ञदेव-प्रणीत निश्चय व व्यवहारनय को साध्य-साधक भाव से मानता है, परन्तु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यानकषाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भाँति आत्मनिन्दादि सहित होकर इन्द्रिय-सुख का अनुभव करता है; यह अविरत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती का लक्षण है ॥४॥
- पूर्वोक्त प्रकार से सम्यग्दृष्टि होकर भूमि रेखादि के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषायों के उदय का अभाव होने पर अन्तरंग में निश्चयनय से एकदेश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनके एकदेश त्याग रूप पाँच अणुव्रतों में और दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तविरत, रात्रिभुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग ॥१॥ इस गाथा में कहे हुए श्रावक के एकादश स्थानों में से किसी एक में वर्तने वाला है वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होता है ॥५॥
- जब वही सम्यग्दृष्टि; धूलि की रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्याख्यानावरण तीसरी कषाय के उदय का अभाव होने पर निश्चय नय से अंतरंग में राग आदि उपाधि-रहित; निज-शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण रूप और बाहरी विषयों में सम्पूर्ण रूप से हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के त्याग रूप ऐसे पाँच महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत होता है ॥६॥
- वही जलरेखा के तुल्य संज्वलन कषाय का मन्द उदय होने पर प्रमादरहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर; सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्तसंयत होता है ॥७॥
- वही संज्वलन कषाय का अत्यन्त मन्द उदय होने पर; अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभव रूप अपूर्वकरण में उपशमक या क्षपक नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती होता है ॥८॥
- देखे, सुने और अनुभव किये हुए भोगों की वांछादिरूप संपूर्ण संकल्प तथा विकल्प रहित अपने निश्चल परमात्मस्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता वे वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनिवृत्तिकरण उपशमक क्षपक संज्ञा के धारक; अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषाय आदि इक्कीस प्रकार की चारित्रमोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ नवम गुणस्थानवर्ती जीव हैं ॥९॥
- सूक्ष्म परमात्मतत्त्व भावना के बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ कषाय के उपशमक और क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवर्ती हैं ॥१०॥
- परम उपशममूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव के बल से सम्पूर्ण मोह को उपशम करने वाले ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥११॥
- उपशमश्रेणी से भिन्न क्षपक श्रेणी के मार्ग से कषायरहित शुद्ध आत्मा की भावना के बल से जिनके समस्त कषाय नष्ट हो गये हैं वे बारहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥१२॥
- मोह का नाश होने के पश्चात् अंतर्मुहूर्त काल में ही निज शुद्ध आत्मानुभव रूप एकत्ववितर्क अवीचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान में स्थिर होकर उसके अन्तिम समय में ज्ञानावरण; दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीनों को एक साथ एक काल में सर्वथा निर्मूल करके मेघपटल से निकले हुए सूर्य के समान सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञान किरणों से लोक अलोक के प्रकाशक तेरहवें गुणस्थानवर्ती जिन भास्कर (सूर्य) होते हैं ॥१३॥
- और मन, वचन, कायवर्गणा के अवलम्बन से कर्मों के ग्रहण करने में कारण जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द रूप योग है उससे रहित चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जिन होते हैं ॥१४॥
तदनंतर निश्चय रत्नत्रयात्मक कारणभूत समयसार नामक जो परम यथाख्यात चारित्र है उससे पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानों से रहित, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों से रहित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों में गर्भित निर्नाम (नाम रहित), निर्गोत्र (गोत्र रहित) आदि, अनन्त गुण सहित सिद्ध होते हैं । यहाँ शिष्य पूछता है कि केवलज्ञान हो जाने पर जब मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिए, सयोगी और अयोगी इन दो गुणस्थानों में रहने का कोई समय ही नहीं है? इस शंका का परिहार करते हैं कि केवलज्ञान हो जाने पर यथाख्यात चारित्र तो हो जाता है किन्तु परम यथाख्यात चारित्र नहीं होता है । यहाँ दृष्टान्त है-जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता किन्तु उसको चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी तरह सयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्रमोह के उदय का अभाव है तो भी निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो तीन योगों का व्यापार है वह चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है । तीनों योगों से रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अंत समय को छोड़कर शेष चार अघातिया कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समय में उन अघातिया कर्मों का मन्द उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव हो जाने से अयोगी जिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार चौदह गुणस्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ । अब चौदह मार्गणाओं का कथन किया जाता है -- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी तथा आहार ॥१॥ इस तरह क्रम से गति आदि चतुर्दश मार्गणा जाननी चाहिए । - निज आत्मा की प्राप्ति से विलक्षण नारक, तिर्यक्, मनुष्य तथा देवगति भेद से गतिमार्गणा चार प्रकार की है ॥१॥
- अतीन्द्रिय; शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपक्षभूत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय भेद से इन्द्रियमार्गणा पाँच प्रकार की है ॥२॥
- शरीर रहित आत्मतत्त्व से भिन्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से कायमार्गणा छह तरह की होती है ॥३॥
- व्यापार रहित शुद्ध आत्मतत्त्व से विलक्षण मनोयोग, वचनयोग तथा काययोग के भेद से योगमार्गणा तीन प्रकार की है अथवा विस्तार से सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग के भेद से चार प्रकार का मनोयोग है । ऐसे ही सत्य, असत्य, उभय, अनुभय इन चार भेदों से वचनयोग भी चार प्रकार का है एवं औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कार्मण ऐसे काययोग सात प्रकार का है । सब मिलकर योगमार्गणा १५ प्रकार की हुई ॥४॥
- वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादिक दोषों से रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ऐसे तीन प्रकार की वेदमार्गणा है ॥५॥
- कषाय रहित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया, लोभ भेदों से चार प्रकार की कषायमार्गणा है । विस्तार से अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन भेद से १६ कषाय और हास्यादिक भेद से ९ नोकषाय ये सब मिलकर पच्चीस प्रकार की कषायमार्गणा है ॥६॥
- मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, पाँच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ये तीन अज्ञान, इस तरह ८ प्रकार की ज्ञानमार्गणा है ॥७॥
- सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात ये पाँच प्रकार का चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्षी; ऐसे संयममार्गणा सात प्रकार की है ॥८॥
- चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शन इन भेदों से दर्शनमार्गणा चार प्रकार की है ॥९॥
- कषायों के उदय से रँगी हुई जो मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है, उससे भिन्न जो परमात्मद्रव्य है; उस परमात्मद्रव्य से विरोध करने वाली कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्य और शुक्ल ऐसे ६ प्रकार की लेश्यामार्गणा है ॥१०॥
- भव्य और अभव्य भेद से भव्य-मार्गणा दो प्रकार की है ॥११॥ यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि 'शुद्ध पारिणामिक परमभावरूप शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से जीव गुणस्थान तथा मार्गणास्थानों से रहित है' ऐसा पहले कहा गया है और अब यहाँ भव्य अभव्य रूप से मार्गणा में भी आपने पारिणामिक भाव कहा; सो यह तो पूर्वापरविरोध है? अब इस शंका का समाधान करते हैं - पूर्व प्रसंग में तो शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मार्गणा का निषेध किया है और यहाँ पर अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणा में भी घटित होते हैं ।
यदि कदाचित् ऐसा कहो कि- 'शुद्ध अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नहीं है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है' तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि यद्यपि सामान्य रूप से पारिणामिक भाव शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसी कारण जीवभव्याभव्यत्वानि च इस तत्त्वार्थसूत्र (अ० २, सू. ७) में जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदों से पारिणामिक भाव तीन प्रकार का कहा है । उनमें शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । तथा जो कर्म से उत्पन्न दश प्रकार के प्राणों रूप जीवत्व है वह जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व के भेद से तीन तरह का है और ये तीनों विनाशशील होने के कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिकभाव कहे जाते हैं । इनकी अशुद्धता किस प्रकार से है?' इस शंका का उत्तर यह है - यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक व्यवहारनय से संसारी जीव में हैं, तथापि सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया इस वचन से ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा नहीं हैं और मुक्त जीवों में तो सर्वथा ही नहीं है; इस कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भाव में से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यान के समय ध्येय (ध्यान करने योग्य) होता है, ध्यानरूप नहीं होता क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है; और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप होने के कारण अविनाशी है, यह सारांश है । सम्यक्त्व के भेद से सम्यक्त्वमार्गणा तीन प्रकार की है । - औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक और मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन विपक्ष भेदों के साथ छह प्रकार की भी सम्यक्त्वमार्गणा जाननी चाहिए ॥१२॥
- संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व से विलक्षण परमात्मस्वरूप से भिन्न संज्ञिमार्गणा संज्ञी तथा असंज्ञी भेद से दो प्रकार की है ॥१३॥
- आहारक अनाहारक जीवों के भेद से आहार-मार्गणा भी दो प्रकार की है ॥१४॥
इस प्रकार चौदह मार्गणाओं का स्वरूप जानना चाहिए । इस रीति से पुढविजलतेयवाऊ इत्यादि दो गाथाओं और तीसरी गाथा णिक्कम्मा अट्टगुणा के तीन पदों से -- गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा चौदह मार्गणा और उपयोगों से इस प्रकार क्रमशः बीस प्ररूपणा कही हैं ॥१॥ इत्यादि गाथा में कहा हुआ स्वरूप धवल, जयधवल और महाधवल प्रबन्ध नामक जो तीन सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनके बीज-पद की सूचना ग्रन्थकार ने की है । सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया इस तृतीय गाथा के चौथे पाद से शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रकाशक पंचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन तीनों प्राभृतों का बीजपद सूचित किया है । यहाँ गुणस्थान और मार्गणाओं में केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों तथा क्षायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्ध आत्मा के स्वरूप हैं, अतः साक्षात् उपादेय हैं; और जो शुद्ध आत्मा के सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप कारण समयसार है वह उसी उपादेयभूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय द्वारा साधक होने से परम्परा से उपादेय है, इसके सिवाय और सब हेय हैं । और जो अध्यात्म ग्रन्थ का बीजपदभूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकार जीवाधिकार में शुद्ध, अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुईं ॥१३॥ अब निम्नलिखित गाथा के पूर्वार्द्ध द्वारा सिद्धों के स्वरूप का और उत्तरार्द्ध द्वारा उनके ऊर्ध्वगमन स्वभाव का कथन करते हैं --
[मग्गणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया] जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए १४ जीवसमासों से जीवों के १४ भेद होते हैं उसी तरह मार्गणा और गुणस्थानों से भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए । मार्गणा और गुणस्थानों से कितनी संख्या वाले होते हैं? [चउदसहि] प्रत्येक से १४-१४ संख्या वाले हैं किस अपेक्षा से? [अशुद्धणया] अशुद्धनय की अपेक्षा से । मार्गणा और गुणस्थानों से अशुद्ध नय की अपेक्षा चौदह-चौदह प्रकार के कौन होते हैं? "संसारी" संसारी जीव होते हैं । "सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया" वे ही सब संसारी जीव शुद्ध यानि-स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप एक-स्वभावधारक हैं । किस अपेक्षा से? शुद्ध नय से अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से ।
अब शास्त्र प्रसिद्ध दो गाथाओं द्वारा गुणस्थानों के नाम कहते हैं --
१. मिथ्यात्व, २. सासादन, ३. मिश्र, ४. अविरतसम्यक्त्व, ५. देशविरत, ६. प्रमत्तविरत, ७. अप्रमत्तविरत, ८. अपूर्वकरण, ९. अनिवृत्तिकरण, १०. सूक्ष्मसाम्पराय,११. उपशांतमोह, १२. क्षीणमोह, १३.सयोगकेवली और १४. अयोगकेवली । इस तरह क्रम से चौदह गुणस्थान जानने चाहिए ॥२॥
अब इन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षेप से लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार - स्वाभाविक शुद्ध केवलज्ञान केवलदर्शन रूप अखण्ड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास-मय निजपरमात्मा आदि षट् द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थों में तीन मूढ़ता आदि पच्चीस दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए नयविभाग से जिस जीव के श्रद्धान नहीं है वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है ॥१॥
- पाषाणरेखा (पत्थर में उकेरी हुई लकीर) के समान जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय से प्रथम-औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो, तब तक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव सासादन होता है ॥२॥
- जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वों को वीतराग सर्वज्ञ के कहे अनुसार मानता है और अन्य मत के अनुसार भी मानता है वह मिश्रदर्शनमोहनीय कर्म के उदय से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भाँति मिश्र-गुणस्थान वाला है ॥३॥
शंका – 'चाहे जिससे हो मुझे तो एक देव से मतलब है अथवा सब ही देव वन्दनीय हैं, निन्दा किसी भी देव की न करनी चाहिए' इस प्रकार वैनयिक और संशय मिथ्यादृष्टि मानता है; तब उनमें तथा मिश्र-गुणस्थानवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टि में क्या अन्तर है?
उत्तर – वैनयिक मिथ्यादृष्टि तथा संशयमिथ्यादृष्टि तो सभी देवों में तथा सब शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है; उसको किसी एक देव में निश्चय नहीं है और मिश्रगुणस्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है । बस, यही अन्तर है । - जो 'स्वाभाविक अनंतज्ञान आदि अनंतगुण का आधारभूत निज परमात्मद्रव्य उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि परद्रव्य त्याज्य हैं' इस तरह सर्वज्ञदेव-प्रणीत निश्चय व व्यवहारनय को साध्य-साधक भाव से मानता है, परन्तु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्याख्यानकषाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भाँति आत्मनिन्दादि सहित होकर इन्द्रिय-सुख का अनुभव करता है; यह अविरत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती का लक्षण है ॥४॥
- पूर्वोक्त प्रकार से सम्यग्दृष्टि होकर भूमि रेखादि के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषायों के उदय का अभाव होने पर अन्तरंग में निश्चयनय से एकदेश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा बाह्य विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनके एकदेश त्याग रूप पाँच अणुव्रतों में और दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तविरत, रात्रिभुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग ॥१॥ इस गाथा में कहे हुए श्रावक के एकादश स्थानों में से किसी एक में वर्तने वाला है वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होता है ॥५॥
- जब वही सम्यग्दृष्टि; धूलि की रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्याख्यानावरण तीसरी कषाय के उदय का अभाव होने पर निश्चय नय से अंतरंग में राग आदि उपाधि-रहित; निज-शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण रूप और बाहरी विषयों में सम्पूर्ण रूप से हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के त्याग रूप ऐसे पाँच महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत होता है ॥६॥
- वही जलरेखा के तुल्य संज्वलन कषाय का मन्द उदय होने पर प्रमादरहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर; सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्तसंयत होता है ॥७॥
- वही संज्वलन कषाय का अत्यन्त मन्द उदय होने पर; अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभव रूप अपूर्वकरण में उपशमक या क्षपक नामक अष्टम गुणस्थानवर्ती होता है ॥८॥
- देखे, सुने और अनुभव किये हुए भोगों की वांछादिरूप संपूर्ण संकल्प तथा विकल्प रहित अपने निश्चल परमात्मस्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता वे वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनिवृत्तिकरण उपशमक क्षपक संज्ञा के धारक; अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषाय आदि इक्कीस प्रकार की चारित्रमोहनीय कर्म की प्रकृतियों के उपशमन और क्षपण में समर्थ नवम गुणस्थानवर्ती जीव हैं ॥९॥
- सूक्ष्म परमात्मतत्त्व भावना के बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ कषाय के उपशमक और क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवर्ती हैं ॥१०॥
- परम उपशममूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव के बल से सम्पूर्ण मोह को उपशम करने वाले ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥११॥
- उपशमश्रेणी से भिन्न क्षपक श्रेणी के मार्ग से कषायरहित शुद्ध आत्मा की भावना के बल से जिनके समस्त कषाय नष्ट हो गये हैं वे बारहवें गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥१२॥
- मोह का नाश होने के पश्चात् अंतर्मुहूर्त काल में ही निज शुद्ध आत्मानुभव रूप एकत्ववितर्क अवीचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान में स्थिर होकर उसके अन्तिम समय में ज्ञानावरण; दर्शनावरण तथा अन्तराय इन तीनों को एक साथ एक काल में सर्वथा निर्मूल करके मेघपटल से निकले हुए सूर्य के समान सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञान किरणों से लोक अलोक के प्रकाशक तेरहवें गुणस्थानवर्ती जिन भास्कर (सूर्य) होते हैं ॥१३॥
- और मन, वचन, कायवर्गणा के अवलम्बन से कर्मों के ग्रहण करने में कारण जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द रूप योग है उससे रहित चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जिन होते हैं ॥१४॥
तदनंतर निश्चय रत्नत्रयात्मक कारणभूत समयसार नामक जो परम यथाख्यात चारित्र है उससे पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानों से रहित, ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों से रहित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों में गर्भित निर्नाम (नाम रहित), निर्गोत्र (गोत्र रहित) आदि, अनन्त गुण सहित सिद्ध होते हैं ।
यहाँ शिष्य पूछता है कि केवलज्ञान हो जाने पर जब मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय की पूर्णता हो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिए, सयोगी और अयोगी इन दो गुणस्थानों में रहने का कोई समय ही नहीं है? इस शंका का परिहार करते हैं कि केवलज्ञान हो जाने पर यथाख्यात चारित्र तो हो जाता है किन्तु परम यथाख्यात चारित्र नहीं होता है । यहाँ दृष्टान्त है-जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता किन्तु उसको चोर के संसर्ग का दोष लगता है, उसी तरह सयोग केवलियों के चारित्र का नाश करने वाले चारित्रमोह के उदय का अभाव है तो भी निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो तीन योगों का व्यापार है वह चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है । तीनों योगों से रहित जो अयोगी जिन हैं उनके अंत समय को छोड़कर शेष चार अघातिया कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समय में उन अघातिया कर्मों का मन्द उदय होने पर चारित्र में दोष का अभाव हो जाने से अयोगी जिन मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार चौदह गुणस्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ ।
अब चौदह मार्गणाओं का कथन किया जाता है --
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी तथा आहार ॥१॥
इस तरह क्रम से गति आदि चतुर्दश मार्गणा जाननी चाहिए । - निज आत्मा की प्राप्ति से विलक्षण नारक, तिर्यक्, मनुष्य तथा देवगति भेद से गतिमार्गणा चार प्रकार की है ॥१॥
- अतीन्द्रिय; शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपक्षभूत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय भेद से इन्द्रियमार्गणा पाँच प्रकार की है ॥२॥
- शरीर रहित आत्मतत्त्व से भिन्न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से कायमार्गणा छह तरह की होती है ॥३॥
- व्यापार रहित शुद्ध आत्मतत्त्व से विलक्षण मनोयोग, वचनयोग तथा काययोग के भेद से योगमार्गणा तीन प्रकार की है अथवा विस्तार से सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग के भेद से चार प्रकार का मनोयोग है । ऐसे ही सत्य, असत्य, उभय, अनुभय इन चार भेदों से वचनयोग भी चार प्रकार का है एवं औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कार्मण ऐसे काययोग सात प्रकार का है । सब मिलकर योगमार्गणा १५ प्रकार की हुई ॥४॥
- वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादिक दोषों से रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ऐसे तीन प्रकार की वेदमार्गणा है ॥५॥
- कषाय रहित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया, लोभ भेदों से चार प्रकार की कषायमार्गणा है । विस्तार से अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन भेद से १६ कषाय और हास्यादिक भेद से ९ नोकषाय ये सब मिलकर पच्चीस प्रकार की कषायमार्गणा है ॥६॥
- मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, पाँच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ये तीन अज्ञान, इस तरह ८ प्रकार की ज्ञानमार्गणा है ॥७॥
- सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात ये पाँच प्रकार का चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्षी; ऐसे संयममार्गणा सात प्रकार की है ॥८॥
- चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलदर्शन इन भेदों से दर्शनमार्गणा चार प्रकार की है ॥९॥
- कषायों के उदय से रँगी हुई जो मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है, उससे भिन्न जो परमात्मद्रव्य है; उस परमात्मद्रव्य से विरोध करने वाली कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्य और शुक्ल ऐसे ६ प्रकार की लेश्यामार्गणा है ॥१०॥
- भव्य और अभव्य भेद से भव्य-मार्गणा दो प्रकार की है ॥११॥ यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि 'शुद्ध पारिणामिक परमभावरूप शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से जीव गुणस्थान तथा मार्गणास्थानों से रहित है' ऐसा पहले कहा गया है और अब यहाँ भव्य अभव्य रूप से मार्गणा में भी आपने पारिणामिक भाव कहा; सो यह तो पूर्वापरविरोध है? अब इस शंका का समाधान करते हैं - पूर्व प्रसंग में तो शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान और मार्गणा का निषेध किया है और यहाँ पर अशुद्ध पारिणामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणा में भी घटित होते हैं ।
यदि कदाचित् ऐसा कहो कि- 'शुद्ध अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नहीं है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है' तो वह भी ठीक नहीं; क्योंकि यद्यपि सामान्य रूप से पारिणामिक भाव शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसी कारण जीवभव्याभव्यत्वानि च इस तत्त्वार्थसूत्र (अ० २, सू. ७) में जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदों से पारिणामिक भाव तीन प्रकार का कहा है । उनमें शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । तथा जो कर्म से उत्पन्न दश प्रकार के प्राणों रूप जीवत्व है वह जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व के भेद से तीन तरह का है और ये तीनों विनाशशील होने के कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिकभाव कहे जाते हैं । इनकी अशुद्धता किस प्रकार से है?' इस शंका का उत्तर यह है - यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक व्यवहारनय से संसारी जीव में हैं, तथापि सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया इस वचन से ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा नहीं हैं और मुक्त जीवों में तो सर्वथा ही नहीं है; इस कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भाव में से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यान के समय ध्येय (ध्यान करने योग्य) होता है, ध्यानरूप नहीं होता क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है; और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप होने के कारण अविनाशी है, यह सारांश है । सम्यक्त्व के भेद से सम्यक्त्वमार्गणा तीन प्रकार की है । - औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक और मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन विपक्ष भेदों के साथ छह प्रकार की भी सम्यक्त्वमार्गणा जाननी चाहिए ॥१२॥
- संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व से विलक्षण परमात्मस्वरूप से भिन्न संज्ञिमार्गणा संज्ञी तथा असंज्ञी भेद से दो प्रकार की है ॥१३॥
- आहारक अनाहारक जीवों के भेद से आहार-मार्गणा भी दो प्रकार की है ॥१४॥
इस प्रकार चौदह मार्गणाओं का स्वरूप जानना चाहिए । इस रीति से पुढविजलतेयवाऊ इत्यादि दो गाथाओं और तीसरी गाथा णिक्कम्मा अट्टगुणा के तीन पदों से --
गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा चौदह मार्गणा और उपयोगों से इस प्रकार क्रमशः बीस प्ररूपणा कही हैं ॥१॥
इत्यादि गाथा में कहा हुआ स्वरूप धवल, जयधवल और महाधवल प्रबन्ध नामक जो तीन सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उनके बीज-पद की सूचना ग्रन्थकार ने की है । सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया इस तृतीय गाथा के चौथे पाद से शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रकाशक पंचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन तीनों प्राभृतों का बीजपद सूचित किया है ।
यहाँ गुणस्थान और मार्गणाओं में केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों तथा क्षायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्ध आत्मा के स्वरूप हैं, अतः साक्षात् उपादेय हैं; और जो शुद्ध आत्मा के सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप कारण समयसार है वह उसी उपादेयभूत का विवक्षित एक देश शुद्ध नय द्वारा साधक होने से परम्परा से उपादेय है, इसके सिवाय और सब हेय हैं । और जो अध्यात्म ग्रन्थ का बीजपदभूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकार जीवाधिकार में शुद्ध, अशुद्ध जीव के कथन की मुख्यता से सप्तम स्थल में तीन गाथायें पूर्ण हुईं ॥१३॥
अब निम्नलिखित गाथा के पूर्वार्द्ध द्वारा सिद्धों के स्वरूप का और उत्तरार्द्ध द्वारा उनके ऊर्ध्वगमन स्वभाव का कथन करते हैं --
|