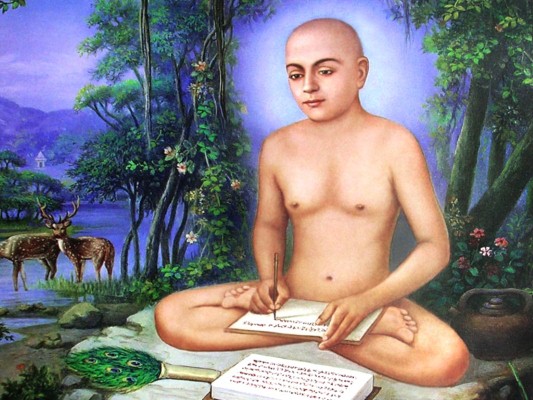ब्रह्मदेव सूरि : संस्कृत
सिद्धा सिद्ध होते हैं, इस रीति से यहाँ भवन्ति इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए । सिद्ध किन विशेषणों से विशिष्ट होते हैं?
णिक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरमदेहदो कर्मों से रहित, आठ गुणों से सहित और अन्तिम शरीर से कुछ छोटे ऐसे सिद्ध हैं । इस प्रकार सूत्र के पूर्वार्द्ध द्वारा सिद्धों का स्वरूप कहा । अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं ।
लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता वे सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद, व्यय से संयुक्त हैं ।
अब विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं -- कर्म शत्रुओं के विध्वंसक अपने शुद्ध आत्मसंवेदन के बल के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों के विनाश करने से आठों कर्मों से रहित सिद्ध होते हैं तथा सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्याबाध ये आठ गुण सिद्धों के होते हैं ॥१॥ इस गाथा में कहे क्रम से आठ कर्म रहित सिद्धों के आठ गुण कहे जाते हैं ।
- केवलज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है; इस प्रकार की रुचिरूप निश्चय-सम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण की अवस्था में भावित किया था उसके फलस्वरूप समस्त जीव आदि तत्त्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश (विरुद्ध अभिप्राय) से रहित परिणामरूप परम क्षायिक सम्यक्त्व गुण सिद्धों के कहा गया है ।
- पहले छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अवस्था में भावना किये हुए निर्विकार स्वानुभवरूप ज्ञान के फलस्वरूप एक ही समय में लोक तथा अलोक के सम्पूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवलज्ञान गुण है ।
- समस्त विकल्पों से रहित अपनी शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो दर्शन पहले भावित किया था उसी दर्शन के फलरूप एक काल में लोक-अलोक के सम्पूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवलदर्शन गुण है ।
- आत्मध्यान से विचलित करने वाले किसी अतिघोर परीषह तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलम्बन किया उसी के फलरूप अनन्त पदार्थों के जानने में खेद के अभावरूप अनन्तवीर्य गुण है ।
- सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवलज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं । यह पाँचवाँ गुण है ।
- एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है उसी तरह एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोष से रहित जो अनन्त सिद्धों को अवकाश देने की सामर्थ्य है वह अवगाहन गुण है ।
- यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु (भारी) हो तो लोहे के गोले के समान वह नीचे पड़ा रहेगा और यदि सर्वथा लघु (हल्का) हो तो वायु से प्रेरित आक की रुई की तरह वह सदा इधर-उधर घूमता रहेगा किन्तु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है इस कारण उनके अगुरुलघु गुण कहा जाता है ।
- स्वाभाविक शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न तथा राग आदि विभावों से रहित सुखरूपी अमृत का जो एकदेश अनुभव पहले किया था उसी के फलस्वरूप अव्याबाध रूप अनन्त सुख गुण सिद्धों में कहा गया है ।
इस प्रकार सम्यक्त्व आदि आठ गुण मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हैं । विस्तार रुचि वाले शिष्य के प्रति विशेष भेद नय के अवलम्बन से गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितता, योगरहितता, वेदरहितता, कषायरहितता, नामरहितता, गोत्ररहितता तथा आयुरहितता आदि विशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व प्रमेयत्वादि सामान्य गुण इस तरह जैनागम के अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिए और संक्षेपरुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नय की अपेक्षा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुखरूप तीन गुण अथवा केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो गुण हैं और साक्षात् अभेदनय से एक शुद्ध चैतन्य गुण ही सिद्धों का है । पुनः वे सिद्ध कैसे होते हैं? चरम
(अन्तिम) शरीर से कुछ छोटे होते हैं । वह जो किंचित्-ऊनता है सो शरीरोपांग से उत्पन्न नासिका आदि के छिद्रों के अपूर्ण
(खाली स्थान) होने से जिस समय सयोगी गुणस्थान के अन्त समय में तीस प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ उनमें शरीरोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः उसी समय किंचित् ऊनता हुई है । ऐसा जानना चाहिए ।
कोई शंका करता है कि जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि के हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा भी फैलकर लोकप्रमाण होनी चाहिए? इस शंका का उत्तर यह है-दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है किन्तु जीव का लोकप्रमाण असंख्यात-प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशों का लोकप्रमाण-विस्तार स्वभाव नहीं है । यदि यों कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए, आवरणरहित रहते हैं फिर जैसे प्रदीप के आवरण होता है उसी तरह जीवप्रदेशों के भी आवरण हुआ है? ऐसा नहीं है । किन्तु जीव के प्रदेश तो पहले अनादिकाल से सन्तानरूप चले आये हुए शरीर के आवरणसहित ही रहते हैं । इस कारण जीव के प्रदेशों का संहार नहीं होता तथा विस्तार व संहार शरीर नामक नामकर्म के अधीन ही है, जीव का स्वभाव नहीं है । इस कारण जीव के शरीर का अभाव होने पर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता ।
इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मुट्ठी के भीतर चार हाथ लम्बा वस्त्र बँधा
(भिंचा) हुआ है, अब वह वस्त्र, मुट्ठी खोल देने पर पुरुष के अभाव में संकोच तथा विस्तार नहीं करता; जैसा उस पुरुष ने छोड़ा वैसा ही रहता है । अथवा गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त होता जाता है किन्तु जब वह सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच व विस्तार को प्राप्त नहीं होता । इसी तरह मुक्त जीव भी, पुरुष के स्थानभूत अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में, संकोच विस्तार नहीं करता ।
कोई कहते हैं कि 'जीव जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहाँ ही रहता है', इसके निषेध के लिए कहते हैं कि पूर्व प्रयोग से, असंग होने से, बन्ध का नाश होने से, तथागति के परिणाम से, इन चार हेतुओं से तथा घूमते हुए कुम्हार के चाक के समान, मिट्टी के लेप से रहित तुम्बी के समान, एरंड के बीज के समान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन चार दृष्टान्तों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्व
(ऊपर को) गमन समझना चाहिए । वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है उससे आगे नहीं होता; क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है ।
सिद्ध नित्य हैं । यहाँ जो नित्य विशेषण है सो सदाशिववादी जो यह कहते हैं कि – '१०० कल्प प्रमाण समय बीत जाने पर जब जगत् शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवों का संसार में आगमन होता है ।' इस मत का निषेध करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए ।
उत्पाद, व्यय-संयुक्तपना जो सिद्धों का विशेषण है, वह सर्वथा अपरिणामिता के निषेध के लिए है । यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि सिद्ध निरन्तर निश्चल अविनश्वर शुद्ध आत्म-स्वरूप से भिन्न नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करते हैं इसलिए सिद्धों में उत्पाद-व्यय कैसे हो? इसका परिहार यह है कि
- आगम में कहे गये अगुरुलघु गुण के षट्-हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती हैं; उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पाद व्यय है । अथवा
- ज्ञेय पदार्थ अपने जिस-जिस उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप से प्रतिसमय परिणमते हैं उन उनके आकार से निरिच्छुक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी परिणमता है इस कारण भी उत्पाद-व्यय सिद्धों में घटित होता है । अथवा
- सिद्धों में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से संसार पर्याय का नाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्यपने से ध्रौव्य है । इस प्रकार नय विभाग से नौ अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिए ।
अथवा वही जीव बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भेदों से तीन प्रकार का भी होता है । निज शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध इन्द्रिय सुख में आसक्त बहिरात्मा है; उससे विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित निज शुद्ध आत्मद्रव्य की भावना रूप भेदविज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि पर द्रव्यों में जो एकत्व भावना से परिणत है (देह को ही आत्मा समझने वाला) बहिरात्मा है । बहिरात्मा से विरुद्ध (निज शुद्ध आत्मा को आत्मा जानने वाला) अन्तरात्मा है । अथवा, हेय-उपादेय का विचार करने वाला जो 'चित्त' तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि 'दोष' और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक 'आत्मा' इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चित्त, दोष, आत्मा इन तीनों में अथवा वीतराग सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष नयों द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वह बहिरात्मा है और उस बहिरात्मा से भिन्न अन्तरात्मा है । ऐसा बहिरात्मा, अन्तरात्मा का लक्षण समझना चाहिए ।
अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं क्योंकि पूर्ण निर्मल केवलज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोकालोक को जानता है या अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है, इस कारण वह परमात्मा विष्णु कहा जाता है । परमब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत से तृप्त होने के कारण उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हो सका अतः वह परमब्रह्म कहलाता है । केवलज्ञान आदि गुणरूपी ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञापालन करते हैं, अतः वह परमात्मा ईश्वर होता है । केवलज्ञान शब्द से वाच्य 'सु' उत्तम 'गत' यानि ज्ञान जिसका वह सुगत है । अथवा शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त हुआ सो सुगत है । तथा
'शिव यानि परम कल्याण, निर्वाण एवं अक्षय ज्ञानरूप मुक्त पद को जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है ॥१॥
इस श्लोक में कहे गये लक्षण का धारक होने के कारण वह परमात्मा शिव है । काम-क्रोधादि के जीतने से अनन्तज्ञान आदि गुणों का धारक जिन कहलाता है इत्यादि परमागम में कहे हुए एक हजार आठ नामों से कहे जाने योग्य जो है, उसको परमात्मा जानना चाहिए ।
इस प्रकार ऊपर कहे गये इन तीनों आत्माओं में जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमें केवल बहिरात्मा तो व्यक्ति रूप से रहता है और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से रहते हैं, भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी रहते हैं । मिथ्यादृष्टि अभव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्ति रूप से और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से ही रहते हैं; भावी नैगमनय की अपेक्षा अभव्य में अन्तरात्मा तथा परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते । कदाचित् कोई कहे कि यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व कैसे है? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में परमात्म शक्ति की केवलज्ञान आदि रूप से व्यक्ति न होगी इसलिए उसमें अभव्यत्व है । शुद्ध नय की अपेक्षा परमात्मा की शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनों में समान है । यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवलज्ञान न हो तो उसके केवलज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश यह है कि भव्य, अभव्य ये दोनों अशुद्ध नय से हैं । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा में नय विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया उसी प्रकार शेष तेरह गुणस्थानों में भी घटित करना चाहिए । इस प्रकार बहिरात्मा की दशा में अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं और भावी नैगमनय से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं ऐसा समझना चाहिए । अन्तरात्मा की अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से घृत के घट के समान और परमात्मा का स्वरूप शक्तिरूप से तथा भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्तिरूप से भी जानना चाहिए । परमात्म अवस्था में अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा भूतपूर्व नय की अपेक्षा जानने चाहिए ।
अब तीनों तरह के आत्माओं को गुणस्थानों में योजित करते हैं-मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मा जानना चाहिए; अविरत गुणस्थान में उसके योग्य अशुभ लेश्या से परिणत जघन्य अन्तरात्मा है और क्षीणकषाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । अविरत और क्षीणकषाय गुणस्थानों के बीच में जो सात गुणस्थान हैं उनमें मध्यम अन्तरात्मा है । सयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानों में विवक्षित एकदेश शुद्धनय की अपेक्षा सिद्ध के समान परमात्मा है और सिद्ध तो साक्षात् परमात्मा हैं ही । यहाँ बहिरात्मा तो हेय है और उपादेयभूत (परमात्मा) के अनन्त सुख का साधक होने से अन्तरात्मा उपादेय है और परमात्मा साक्षात् उपादेय है; ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार छह द्रव्य और पंच अस्तिकाय के प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि चौदह गाथाओं द्वारा, ९ मध्यस्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप प्रथम अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥
उसके पश्चात् यद्यपि शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा द्रव्य ही उपादेय है तो भी हेय रूप अजीव द्रव्य का आठ गाथाओं द्वारा निरूपण करते हैं । क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हेय तत्त्व का ज्ञान होने पर फिर उपादेय पदार्थ स्वीकार होता है । अजीव द्रव्य इस प्रकार है --
सिद्धा सिद्ध होते हैं, इस रीति से यहाँ भवन्ति इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए । सिद्ध किन विशेषणों से विशिष्ट होते हैं?
णिक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरमदेहदो कर्मों से रहित, आठ गुणों से सहित और अन्तिम शरीर से कुछ छोटे ऐसे सिद्ध हैं । इस प्रकार सूत्र के पूर्वार्द्ध द्वारा सिद्धों का स्वरूप कहा । अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं ।
लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता वे सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद, व्यय से संयुक्त हैं ।
अब विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं -- कर्म शत्रुओं के विध्वंसक अपने शुद्ध आत्मसंवेदन के बल के द्वारा ज्ञानावरण आदि समस्त मूल व उत्तर कर्म प्रकृतियों के विनाश करने से आठों कर्मों से रहित सिद्ध होते हैं तथा सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्याबाध ये आठ गुण सिद्धों के होते हैं ॥१॥ इस गाथा में कहे क्रम से आठ कर्म रहित सिद्धों के आठ गुण कहे जाते हैं ।
- केवलज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है; इस प्रकार की रुचिरूप निश्चय-सम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण की अवस्था में भावित किया था उसके फलस्वरूप समस्त जीव आदि तत्त्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश (विरुद्ध अभिप्राय) से रहित परिणामरूप परम क्षायिक सम्यक्त्व गुण सिद्धों के कहा गया है ।
- पहले छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अवस्था में भावना किये हुए निर्विकार स्वानुभवरूप ज्ञान के फलस्वरूप एक ही समय में लोक तथा अलोक के सम्पूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवलज्ञान गुण है ।
- समस्त विकल्पों से रहित अपनी शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो दर्शन पहले भावित किया था उसी दर्शन के फलरूप एक काल में लोक-अलोक के सम्पूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवलदर्शन गुण है ।
- आत्मध्यान से विचलित करने वाले किसी अतिघोर परीषह तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलम्बन किया उसी के फलरूप अनन्त पदार्थों के जानने में खेद के अभावरूप अनन्तवीर्य गुण है ।
- सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवलज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं । यह पाँचवाँ गुण है ।
- एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों का प्रकाश समा जाता है उसी तरह एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोष से रहित जो अनन्त सिद्धों को अवकाश देने की सामर्थ्य है वह अवगाहन गुण है ।
- यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु (भारी) हो तो लोहे के गोले के समान वह नीचे पड़ा रहेगा और यदि सर्वथा लघु (हल्का) हो तो वायु से प्रेरित आक की रुई की तरह वह सदा इधर-उधर घूमता रहेगा किन्तु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है इस कारण उनके अगुरुलघु गुण कहा जाता है ।
- स्वाभाविक शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न तथा राग आदि विभावों से रहित सुखरूपी अमृत का जो एकदेश अनुभव पहले किया था उसी के फलस्वरूप अव्याबाध रूप अनन्त सुख गुण सिद्धों में कहा गया है ।
इस प्रकार सम्यक्त्व आदि आठ गुण मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हैं । विस्तार रुचि वाले शिष्य के प्रति विशेष भेद नय के अवलम्बन से गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितता, योगरहितता, वेदरहितता, कषायरहितता, नामरहितता, गोत्ररहितता तथा आयुरहितता आदि विशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व प्रमेयत्वादि सामान्य गुण इस तरह जैनागम के अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिए और संक्षेपरुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नय की अपेक्षा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुखरूप तीन गुण अथवा केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो गुण हैं और साक्षात् अभेदनय से एक शुद्ध चैतन्य गुण ही सिद्धों का है । पुनः वे सिद्ध कैसे होते हैं? चरम
(अन्तिम) शरीर से कुछ छोटे होते हैं । वह जो किंचित्-ऊनता है सो शरीरोपांग से उत्पन्न नासिका आदि के छिद्रों के अपूर्ण
(खाली स्थान) होने से जिस समय सयोगी गुणस्थान के अन्त समय में तीस प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ उनमें शरीरोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः उसी समय किंचित् ऊनता हुई है । ऐसा जानना चाहिए ।
कोई शंका करता है कि जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि के हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा भी फैलकर लोकप्रमाण होनी चाहिए? इस शंका का उत्तर यह है- दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है, वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है किन्तु जीव का लोकप्रमाण असंख्यात-प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशों का लोकप्रमाण-विस्तार स्वभाव नहीं है । यदि यों कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए, आवरणरहित रहते हैं फिर जैसे प्रदीप के आवरण होता है उसी तरह जीवप्रदेशों के भी आवरण हुआ है? ऐसा नहीं है । किन्तु जीव के प्रदेश तो पहले अनादिकाल से सन्तानरूप चले आये हुए शरीर के आवरणसहित ही रहते हैं । इस कारण जीव के प्रदेशों का संहार नहीं होता तथा विस्तार व संहार शरीर नामक नामकर्म के अधीन ही है, जीव का स्वभाव नहीं है । इस कारण जीव के शरीर का अभाव होने पर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता ।
इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मुट्ठी के भीतर चार हाथ लम्बा वस्त्र बँधा
(भिंचा) हुआ है, अब वह वस्त्र, मुट्ठी खोल देने पर पुरुष के अभाव में संकोच तथा विस्तार नहीं करता; जैसा उस पुरुष ने छोड़ा वैसा ही रहता है । अथवा गीली मिट्टी का बर्तन बनते समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त होता जाता है किन्तु जब वह सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच व विस्तार को प्राप्त नहीं होता । इसी तरह मुक्त जीव भी, पुरुष के स्थानभूत अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में, संकोच विस्तार नहीं करता ।
कोई कहते हैं कि 'जीव जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहाँ ही रहता है', इसके निषेध के लिए कहते हैं कि पूर्व प्रयोग से, असंग होने से, बन्ध का नाश होने से, तथागति के परिणाम से, इन चार हेतुओं से तथा घूमते हुए कुम्हार के चाक के समान, मिट्टी के लेप से रहित तुम्बी के समान, एरंड के बीज के समान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन चार दृष्टान्तों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्व
(ऊपर को) गमन समझना चाहिए । वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है उससे आगे नहीं होता; क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है ।
सिद्ध नित्य हैं । यहाँ जो नित्य विशेषण है सो सदाशिववादी जो यह कहते हैं कि – '१०० कल्प प्रमाण समय बीत जाने पर जब जगत् शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवों का संसार में आगमन होता है ।' इस मत का निषेध करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए ।
उत्पाद, व्यय-संयुक्तपना जो सिद्धों का विशेषण है, वह सर्वथा अपरिणामिता के निषेध के लिए है । यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि सिद्ध निरन्तर निश्चल अविनश्वर शुद्ध आत्म-स्वरूप से भिन्न नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करते हैं इसलिए सिद्धों में उत्पाद-व्यय कैसे हो? इसका परिहार यह है कि
- आगम में कहे गये अगुरुलघु गुण के षट्-हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती हैं; उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पाद व्यय है । अथवा
- ज्ञेय पदार्थ अपने जिस-जिस उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप से प्रतिसमय परिणमते हैं उन उनके आकार से निरिच्छुक वृत्ति से सिद्धों का ज्ञान भी परिणमता है इस कारण भी उत्पाद-व्यय सिद्धों में घटित होता है । अथवा
- सिद्धों में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से संसार पर्याय का नाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्यपने से ध्रौव्य है । इस प्रकार नय विभाग से नौ अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिए ।
अथवा वही जीव बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा इन भेदों से तीन प्रकार का भी होता है । निज शुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध इन्द्रिय सुख में आसक्त बहिरात्मा है; उससे विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित निज शुद्ध आत्मद्रव्य की भावना रूप भेदविज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि पर द्रव्यों में जो एकत्व भावना से परिणत है (देह को ही आत्मा समझने वाला) बहिरात्मा है । बहिरात्मा से विरुद्ध (निज शुद्ध आत्मा को आत्मा जानने वाला) अन्तरात्मा है । अथवा, हेय-उपादेय का विचार करने वाला जो 'चित्त' तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि 'दोष' और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक 'आत्मा' इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चित्त, दोष, आत्मा इन तीनों में अथवा वीतराग सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष नयों द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वह बहिरात्मा है और उस बहिरात्मा से भिन्न अन्तरात्मा है । ऐसा बहिरात्मा, अन्तरात्मा का लक्षण समझना चाहिए ।
अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं क्योंकि पूर्ण निर्मल केवलज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोकालोक को जानता है या अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है, इस कारण वह परमात्मा विष्णु कहा जाता है । परमब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत से तृप्त होने के कारण उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हो सका अतः वह परमब्रह्म कहलाता है । केवलज्ञान आदि गुणरूपी ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञापालन करते हैं, अतः वह परमात्मा ईश्वर होता है । केवलज्ञान शब्द से वाच्य 'सु' उत्तम 'गत' यानि ज्ञान जिसका वह सुगत है । अथवा शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त हुआ सो सुगत है । तथा
'शिव यानि परम कल्याण, निर्वाण एवं अक्षय ज्ञानरूप मुक्त पद को जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है ॥१॥
इस श्लोक में कहे गये लक्षण का धारक होने के कारण वह परमात्मा शिव है । काम-क्रोधादि के जीतने से अनन्तज्ञान आदि गुणों का धारक जिन कहलाता है इत्यादि परमागम में कहे हुए एक हजार आठ नामों से कहे जाने योग्य जो है, उसको परमात्मा जानना चाहिए ।
इस प्रकार ऊपर कहे गये इन तीनों आत्माओं में जो मिथ्यादृष्टि भव्य जीव है उसमें केवल बहिरात्मा तो व्यक्ति रूप से रहता है और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से रहते हैं, भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी रहते हैं । मिथ्यादृष्टि अभव्य जीव में बहिरात्मा व्यक्ति रूप से और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्तिरूप से ही रहते हैं; भावी नैगमनय की अपेक्षा अभव्य में अन्तरात्मा तथा परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते । कदाचित् कोई कहे कि यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्यत्व कैसे है? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में परमात्म शक्ति की केवलज्ञान आदि रूप से व्यक्ति न होगी इसलिए उसमें अभव्यत्व है । शुद्ध नय की अपेक्षा परमात्मा की शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनों में समान है । यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवलज्ञान न हो तो उसके केवलज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश यह है कि भव्य, अभव्य ये दोनों अशुद्ध नय से हैं । इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा में नय विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया उसी प्रकार शेष तेरह गुणस्थानों में भी घटित करना चाहिए । इस प्रकार बहिरात्मा की दशा में अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं और भावी नैगमनय से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं ऐसा समझना चाहिए । अन्तरात्मा की अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से घृत के घट के समान और परमात्मा का स्वरूप शक्तिरूप से तथा भावी नैगमनय की अपेक्षा व्यक्तिरूप से भी जानना चाहिए । परमात्म अवस्था में अन्तरात्मा तथा बहिरात्मा भूतपूर्व नय की अपेक्षा जानने चाहिए ।
अब तीनों तरह के आत्माओं को गुणस्थानों में योजित करते हैं-मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानों में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मा जानना चाहिए; अविरत गुणस्थान में उसके योग्य अशुभ लेश्या से परिणत जघन्य अन्तरात्मा है और क्षीणकषाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । अविरत और क्षीणकषाय गुणस्थानों के बीच में जो सात गुणस्थान हैं उनमें मध्यम अन्तरात्मा है । सयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानों में विवक्षित एकदेश शुद्धनय की अपेक्षा सिद्ध के समान परमात्मा है और सिद्ध तो साक्षात् परमात्मा हैं ही । यहाँ बहिरात्मा तो हेय है और उपादेयभूत (परमात्मा) के अनन्त सुख का साधक होने से अन्तरात्मा उपादेय है और परमात्मा साक्षात् उपादेय है; ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार छह द्रव्य और पंच अस्तिकाय के प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि चौदह गाथाओं द्वारा, ९ मध्यस्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप प्रथम अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥
उसके पश्चात् यद्यपि शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा द्रव्य ही उपादेय है तो भी हेय रूप अजीव द्रव्य का आठ गाथाओं द्वारा निरूपण करते हैं । क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हेय तत्त्व का ज्ञान होने पर फिर उपादेय पदार्थ स्वीकार होता है । अजीव द्रव्य इस प्रकार है --