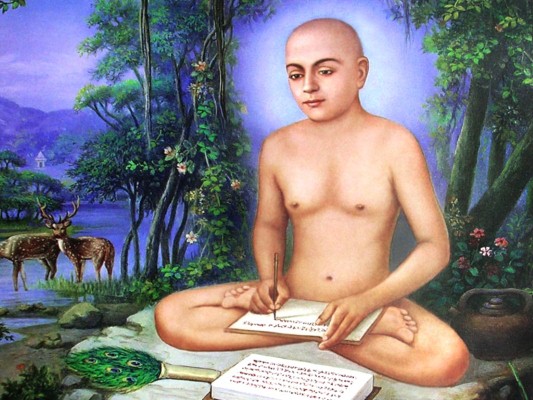


ग्रन्थ :
श्रावकों के उत्तरगुण अथ के ते उत्तरगुणाः अब श्रावकों के उत्तरगुण बतलाते हैं- अणुव्रतानि पञ्चैव त्रिप्रकारं गुणवतम् ।
पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये बारह उत्तरगुण हैं ॥314॥शिक्षाव्रतानि चत्वारि गुणाः स्युर्द्वादशोत्तरे ॥314॥ तत्र हिंसास्तेयानृताब्रह्मपरिग्रहविनिग्रहाः।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहका एक देश त्याग करनेको पाँच अणुव्रत कहते हैं ॥315 ॥एतानि देशतः पञ्चाणुव्रतानि प्रचक्षते ॥315॥ व्रत का लक्षण संकल्पपूर्वकः सेव्ये नियमो व्रतमुच्यते॥
सेवनीय वस्तु का इरादापूर्वक त्याग करना व्रत है। अथवा अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति और बुरे कार्यों से निवृत्ति को व्रत कहते हैं ॥316॥प्रवृत्तिविनिवृत्ती वा सदसत्कर्मसंभवे ॥316॥ (भावार्थ – किसी वस्तु के सेवन न करने का नाम व्रत नहीं है किन्तु उसका बुद्धिपूर्वक त्याग करके सेवन न करना व्रत कहलाता है, क्योंकि किसी वस्तु के सेवन नहीं करने में तो अनेक कारण हो सकते हैं। कोई अच्छी न लगने के कारण किसी वस्तु का सेवन नहीं करता। कोई न मिलने के कारण किसी वस्तु का सेवन नहीं करता। कोई स्वास्थ्य के अनुकूल न होने के कारण किसी वस्तु का सेवन नहीं करता। कोई बदनामी के भय से किसी वस्तु का सेवन नहीं करता । किन्तु यदि वह वस्तु उसे अच्छी लगने लगे, या बाजार में मिलने लगे, या स्वास्थ्यके अनुकूल पड़ने लगे या वदनामी का भय जाता रहे तो वह उस वस्तु को तुरन्त सेवन करने लगेगा। परन्तु जो किसी वस्तु के सेवन न करने का नियम ले लेता है वह अपने नियमकाल तक किसी भी अवस्था में उस वस्तुका सेवन नहीं करता। अतः केवल सेवन न करने का नाम व्रत नहीं है बल्कि समझ-बूझकर त्याग कर देनेका नाम व्रत है ।) पाँचों पापों में बुराई हिंसायामनृते चौर्यामब्रह्मणि परिग्रहे।
हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने और परिग्रह का संचय करने से इसी लोक में मुसीबत आती देखी जाती है और परलोक में भी दुर्गति होती है ॥317॥ दृष्टा विपत्तिरत्रैव परत्रैव च दुर्गतिः ॥317॥ (भावार्थ – भारतीय कोड में जिन जुर्मों के लिए सजा देने का विधान है वे सब जुर्म प्रायः इन पाँच पापों में ही सम्मिलित हैं। हिंसा करने से फाँसी तक हो जाती है। झूठी बात कहने, झूठी गवाही देने से जेलकी हवा खानी पड़ती है। चोरी करने से भी यही दण्ड भोगना पड़ता है। दुराचार करने से जेलखाने की साथ-ही-साथ बेतों की भी सजा मिलती है। और अनुचित तरीके से ज्यादा सामग्री इकट्ठी कर लेने पर भी सजा का भय बना ही रहता है । तथा परिग्रही को चोरों का डर भी सताता रहता है, इसके कारण वह रात को आराम से सो भी नहीं पाता। जब इसी लोक में इन पाँच पापों के कारण इतनी विपत्ति उठानी पड़ती है तब परलोक का तो कहना ही क्या है।) अहिंसा (अब अहिंसा धर्मका वर्णन करते हैं-) यत्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहापनम् ।
प्रमाद के योग से प्राणियों के प्राणों का घात करना हिंसा है और उनकी रक्षा करना अहिंसा है ॥318॥सा हिंसा रक्षणं तेषामहिंसा तु सतां मता ॥318॥ विकथाक्षकषायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च ।
जो जीव 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इन्द्रियाँ, निद्रा और मोह के वशीभूत है उसे प्रमादी कहते हैं ॥319॥ अभ्यासाभिरतो जन्तुः प्रमत्तः परिकीर्तितः ॥319॥ (भावार्थ – प्रमादके पन्द्रह भेद हैं-४ विकथा, 4 कषाय, 5 इन्द्रियाँ, एक निद्रा और एक मोह ।विकथा खोटी कथा को कहते हैं जैसे स्त्रियों की चर्चा करना, भोजन की चर्चा करना, चोरों की चर्चा करना, ये चर्चाएँ प्रायः कामुकता और मनोविनोद के लिए की जाती हैं और उनसे लाभ के बजाय हानि होती है । अतः जो मनुष्य इस प्रकार की चर्चाओं में रस लेता है वह प्रमादी है। क्रोध, मान, माया और लोभ को कषाय कहते हैं। जो क्रोध करता है, मान करता है, मायाचार करता है या लोभी है वह तो प्रमादी है ही, क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति सावधान नहीं रह सकता। इसी तरह जो पाँचों इन्द्रियों का दाग है उन्हीं की तृप्ति में लगा रहा है वह भी प्रमादी है। ऐसे लोग किसी का घात करते हुए नहीं सकुचाते । यही बात निद्रा और मोह के सम्बन्ध में जाननी चाहिए। अतः प्रमादके योग से जो प्राणों का घात किया जाता है वह हिंसा है किन्तु जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ किसी का घात हो जाने पर भी हिंसा नहीं कहलाती है । इसका खुलासा पहले कर आये हैं।) देवतातिथिपित्रर्थ मन्त्रौषधभयाय वा।
देवता के लिए, अतिथि के लिए, पितरों के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए, औषधि के लिए, अथवा भय से सब प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए । इसे अहिंसा व्रत कहते हैं ॥320॥न हिंस्यात्प्राणिनः सर्वानहिंसा नाम तद्वतम् ॥320॥ (भावार्थ – मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में मांस से- श्राद्ध करने का विधान है तथा यह भी बतलाया है कि किस मांस से श्राद्ध करने से कितने दिन तक पितृ लोग तृप्त रहते हैं। पाँचवें अध्याय में यज्ञ के लिए पशुवध करने का तथा मांस खाने का विधान है। उत्तर रामचरित में लिखा है कि जब वशिष्ठ ऋषि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनके आतिथ्य-सत्कार के लिए वाल्मीकि ऋषि ने गाय की बछियाका वध करवाया। ये सब कार्य हिंसा ही हैं। इसी तरहकी बातों को देखकर ग्रन्थकार ने देवता वगैरह के लिए पशुघात करने का निषेध किया है। आश्चर्य है कि धर्म के नाम पर भी हिंसा का पोषण किया गया है। जब कि हिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी तरह दवाई के लिए भी किसी का घात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरों के जीवन को नष्ट कर देने का हमें क्या अधिकार है ? ) पानी वगैरह को छानकर काम में लाओ गृहकार्याणि सर्वाणि रष्टिपूतानि कारयेत् ।
घर के सब काम देख-भाल कर करना चाहिए। और पतली वस्तुओं को कपड़े से छानकर ही काम में लाना चाहिए। आसन, शय्या, मार्ग, अन्न और भी जो वस्तु हो, समय पर उसका उपयोग करते समय बिना देखे उपयोग नहीं करना चाहिए ॥321-322॥द्रवद्रव्याणि सर्वाणि पटपूतानि योजयेत् ॥321॥ पासनं शयनं मार्गमन्त्रमन्यव वस्त यत। अदृष्टं तत्र सेवेत यथाकालं भजनपि ॥322॥ (भावार्थ – प्रत्येक वस्तु को देख-भाल कर काम में लाने की आदत डालने से तथा पानी वगैरह को छानकर काम में लाने से मनुष्य हिंसा से ही नहीं बचता, किन्तु बहुत- सी मुसीबतों से भी बच जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक वस्तु को देख-भाल कर काम में लाने की आदत से साँप, बिच्छू वगैरह से बचाव हो जाता है। शय्या को बिना झाड़े उपयोग में लाने से अनेक मनुष्य साँप के शिकार बन चुके हैं। बिना देखे चाहे जहाँ हाथ डाल देने से भी ऐसी ही घटनाएँ प्रायः घटती हैं। बिना छाने या बिना देखे-भाले पानी पी लेने से मुरादाबाद जिले के एक गाँव में एक लड़के के मुंहमें बिच्छू चला गया था और उसके कारण उस लड़के की मौत बिच्छू के डंक मारते रहने से बड़ी कष्टकर हुई थी। अतः प्रत्येक वस्तु को देखकर ही काम में लाना चाहिए और पानी वगैरह कपड़े से छानकर ही काम में लाना चाहिए। ) भोजन के अन्तराय दर्शनस्पर्शसंकल्पसंसर्गत्यक्तभोजिताः।
ताजा चमड़ा, हड्डी, मांस, लोहू और पीब वगैरह का देखना, रजस्वला स्त्री, सूखा चमड़ा, कुत्ता वगैरह से छू जाना, भोजन के पदार्थों में 'यह मांस की तरह है' इस प्रकार का बुरा संकल्प हो जाना, भोजन में मक्खी वगैरह का गिर पड़ना, त्याग की हुई वस्तु को खा लेना, मारने, काटने, रोने, चिल्लाने आदि की आवाज सुनना, ये सब भोजन में विघ्न पैदा करनेवाले हैं। अर्थात् उक्त अवस्थाओं में भोजन छोड़ देना चाहिए ॥323॥ ये अन्तराय व्रत रूपी बीज की रक्षा के लिए बाड़के समान हैं। इनके पालने से अतिप्रसङ्ग दोष की निवृत्ति होती है और तप की वृद्धि होती है ॥324॥हिंसनाकन्दनप्रायाः प्राशप्रत्यूहकारकाः ॥323॥ अतिप्रसङ्गहानाय तपसः परिवृद्धये । अन्तरायाः स्मृता सबितबीजविनिक्रियाः ॥324॥ (भावार्थ – भोजन करते समय यदि ऊपर कही हुई चीजों को देख ले या उनसे छू जाये या ऊपर बतलायी हुई बातों में से कोई और बात हो जाये तो भोजन छोड़ देना चाहिए। क्यों कि उस अवस्था में भी यदि भोजन नहीं छोड़ा जायेगा तो बुरी वस्तुओं से घृणा धीरे-धीरे दूर हो जायेगी और उसके दूर होने से मन कठोर होता जायेगा, बुरी वस्तुओं के प्रति अरुचि हटती जायेगी और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उन बुरी वस्तुओं में प्रवृत्ति होने लगे। इस तरह यह अतिप्रसङ्ग दोष उपस्थित हो सकता है। इससे बचने के लिए अन्तरायोंका पालन करना जरूरी है । तथा ऐसी अवस्था में भोजन के छोड़ देने से तप की वृद्धि भी होती है, क्योंकि इच्छा के रोकने को तप कहते हैं। भोजन के बीच में अन्तराय के आ जाने पर भी भूख तो भोजन चाहती है अतः मन भोजन के लिए लालायित रहता है। किन्तु समझदार व्रती भूख की परवाह न करके भोजन छोड़ देता है और इस तरह वह खाने की इच्छा पर विजय पाकर अपने तपको बढ़ाता है । अतः अन्तरायों का पालना आवश्यक है। वे व्रत रूपी बीज की बाड़के समान हैं। जैसे खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा के लिए चारों ओर काँटे वगैरह की बाड़ लगा देते हैं उससे कोई पशु वगैरह भीतर घुसकर खेती को नहीं चर पाता ; वैसे ही अन्तरायों का पालन भी व्रतों की रक्षा करता है। ) रात्रि- भोजन त्याग अहिंसावतरक्षार्थ मूलव्रतविशुद्धये।
अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए और मूल व्रतों को विशुद्ध रखने के लिए इस लोक और परलोक में दुःख देने वाले रात्रि-भोजन का त्याग कर देना चाहिए ॥325॥निशायां वर्जयेद्भुक्तिमिहामुत्र च दुःखदाम् ॥325॥ (भावार्थ – रात में भोजन करने से हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि सूर्य के सिवा अन्य जितने भी कृत्रिम प्रकाश हैं उनमें जीवों का बाहुल्य देखा जाता है। रात्रि में दीपक या बिजली की यदि रोशनी पर इतने जीव मँडराते देखे जाते हैं कि जिन की संख्या का अन्दाजा भी लगाना कठिन है। ऐसे समय मै रात में खाने वाला कैसे उनसे बच सकता है ? उसके भोजन में वे जीव बिना पड़े रह नहीं सकते। और इस तरह भोजन के साथ उनका भी भोजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में न तो अहिंसा व्रत की ही रक्षा हो सकती है और न अष्ट मूलगुण ही रह सकते हैं। - रात के खाने में केवल इतनी ही बुराई नहीं है । कभी-कभी तो विषेले जन्तुओं के संसर्ग से दूषित भोजन के कर लेने पर जीवन का ही अन्त हो जाता है। जैसा कि एक बार लाहौर में एक दावत में चायके साथ छिपकली के भी चुर जाने से बहुत-से आदमी उसे पीकर बेहोश हो गये थे ।यदि मकड़ी भोजन में चली जाये तो कोढ़ पैदा कर देती है। यदि बालों की जू पेट में चली जाये तो जलोदर रोग हो जाता है । अतः दिनमें सूर्यके प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए ।) आश्रितेषु च सर्वेषु यथावद्धिहितस्थितिः ।
गृहस्थ को चाहिए कि जो अपने आश्रित हों पहले उनको भोजन कराये पीछे स्वयं भोजन करे ॥326॥ अचार, पानक, धान्य, फूल, मूल, फल और पत्तों के जीवों की योनि होने से ग्रहण नहीं करना चाहिए । तथा जिसमें जीवों का वास हो ऐसी वस्तु भी काम में नहीं लानी चाहिए ॥327॥गृहाश्रमी समीहेत शारीरेऽवसरे स्वयम् ॥326॥ संधानं पानकं धान्यं पुष्पं मूलं फलं दलम् । जीवयोनि न संग्राह्यं यह जीवैरुपद्रुतम् ॥327॥ (भावार्थ – अधिक दिनों का मुरब्बा, अचार, मद्य और मांस के तुल्य हो जाता है अतः मर्यादा के भीतर ही उसका सेवन करना चाहिए। पेय भी सब ताजे और साफ होने चाहिए । अनाज घुना हुआ नहीं होना चाहिए और न इतना अन्न संग्रह ही करना चाहिए कि घुन लग जाये। फल, फूल, शाक-सब्जी वगैरह भी शोध कर ही काम में लाना चाहिए। गली सड़ी हुई या कीड़ा खायी सब्जी प्रत्येक दृष्टि से अभक्ष्य है।) अमिनं मिश्रमुत्सर्गि कालदेशदशाश्रयम् ।
जिनागम में कोई वस्तु अकेली त्याज्य बतलायी है, कोई वस्तु किसी के साथ मिल जाने से त्याज्य हो जाती है। कोई सर्वदा त्याज्य होती है और कोई अमुक काल, अमुक देश और अमुक दशा में त्याज्य होती है ॥328॥वस्तु किञ्चित्परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥328॥ अहिंसा पालन के लिए अन्य आवश्यक बातें यदन्तःशुषिरप्रायं हेयं नालीनलादि तत् ।
जिसके बीच में छिद्र रहते हैं ऐसे कमलडंडी वगैरह शाकों को नहीं खाना चाहिए। और जो अनन्तकाय हैं, जैसे लता, सूरण वगैरह, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए ॥329॥अनन्तकायिकमायं बल्लीकन्दोदिकं त्यजेत् ॥329॥ द्विदल द्विदलं प्राश्यं प्रायेणानवतां गतम् ।
पुराने मूंग, उड़द, चना वगैरह को दलने के बाद ही खाना चाहिए, बिना दले सारा मूंग, सारा उड़द वगैरह नहीं खाना चाहिए और जितनी साबित फलियाँ हैं चाहे वे कच्ची हों या आग पर पकायी गयी हों, उन्हें नहीं खाना चाहिए। उन्हें खोलकर शोधने के बाद ही खाना चाहिए ॥330॥ जहाँ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह है वहाँ अहिंसा कैसे रह सकती है ? तथा ठग और दुराचारी मनुष्य में दया नहीं होती ॥331॥शिम्बयः सकलास्त्याज्याः साधिताः सकलाच याः ॥330 ॥ तत्राहिंसा कुतो यत्र बहारम्भपरिग्रहः । वश च कुशीले च नरे नास्ति दयालुता ॥331॥ (भावार्थ – बहुत आरम्भ करने वाले और बहुत परिग्रह रखने वाले कभी अहिंसक हो ही नहीं सकते क्योंकि आरम्भ और परिग्रह हिंसा का मूल है। इसीलिए सागारधर्मामृत में लिखा है कि जो सन्तोष धारण करके अल्प आरम्भ करता है और अल्प परिग्रह रखता है उसी का मन शुद्ध रहता है और वही अहिंसाणु व्रत का पालन कर सकता है। इसी तरह व्यभिचारी और ठग भी निर्दय हो जाते हैं। जो दूसरों को सताते हैं, खूब क्रोध वगैरह करते हैं उनके परिणाम भी सदा खराब रहते हैं और उससे उन्हें अशुभ कर्म का बन्ध होता है। ) शोकसंतापसकन्दपरिदेवनदुःबधीः ।
जो मनुष्य स्वयं शोक करता है तथा दूसरों के शोकका कारण बनता है, स्वयं सन्ताप करता है तथा दूसरों के संताप का कारण बनता है, स्वयं रोता है तथा दूसरों को रुलाता या कलपाता है, स्वयं दुःखी होता है और दूसरों को दुःखी करता है, वह असातावेदनीय कर्म का बन्ध करता है ॥332॥ जिसके कषाय के उदय से अति संक्लिष्ट परिणाम होते हैं वह जीव चारित्र मोहनीय कर्म का बध करता है ॥333॥भवन्स्वपरयोजन्तुरसोर्चाय जायते ॥332॥ कषायोदयतीवात्मा भावो यस्योपजायते । जीवो जायेत चारित्रमोहस्यासौ समाश्रयः ॥333॥ मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना का स्वरूप मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाभ्यस्थानि यथाक्रमम् ।
सब जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए। जो गुणों में अधिक हों उनमें प्रमोद भाव रखना चाहिए । दुःखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। और जो निर्गुण हों, असभ्य और उद्धत हों उनके प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए ॥334॥ 'अन्य सब जीवों कों दुःख न हो' मन, वचन और काय से इस प्रकार का बर्ताव करने को मैत्री कहते हैं ॥335॥ तप आदि गुणों से विशिष्ट पुरुष को देखकर जो विनयपूर्ण हार्दिक प्रेम उमड़ता है उसे प्रमोद कहते हैं ॥336॥दयालु पुरुषों की गरीबों का उद्धार करने की भावना को कारुण्य कहते हैं। और उद्धत तथा असभ्य पुरुषों के प्रति राग और द्वेष के न होने को माध्यस्थ्य कहते हैं ॥337॥ जो प्राणी गृहस्थ होकर भी इस प्रकार का प्रयत्न करता है, स्वर्ग तो उसके हाथ में है और मोक्ष भी दूर नहीं है ॥338॥ पुण्य को प्रकाशमय कहते हैं और पाप को अन्धकारमय कहते हैं ।दयारूपी सूर्य के होते हुए क्या पुरुष में पाप ठहर सकता है ? ॥339 ॥ ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती। किन्तु हिंसा और अहिंसा के लिए गौण और मुख्य भावों की विशेषता है ॥340॥ संकल्प में भेद होने से धीवर नहीं मारते हुए भी पापी है और किसान मारते हुए भी पापी नहीं है ॥341॥सत्वे गुणाधिक क्लिष्टे निर्गुणेऽपि च भावयेत् ॥334॥ कायेने मनसा वाचाऽपरे सर्वत्र देहिनि । अदुःखजननी वृत्तिमैत्री मैत्रीविदां मता ॥335॥ तपोगुणाधिके पुंलि प्रश्रयाश्रयनिर्भरः । जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः ॥336॥ दीनाभ्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्यं करुणात्मनाम् । हर्षाम!ज्मिता वृत्तिर्माध्यस्थ्यं निर्गुणात्मनि ॥337॥ इत्थं प्रयतमानस्य गृहस्थस्यापि देहिनः । करस्थो जायते स्वर्गो नास्य दूरे च तत्पदम् ॥338॥ पुण्यं तेजोमयं प्राहुः प्राहुः पापं तमोमयम् । तत्पापं पुंसि किं तिष्ठेहयादीधितिमालिनि ॥336॥ सा क्रिया कापि नास्तीह यस्यां हिंसा न विद्यते । विशिष्यते परं भावावत्र मुख्यानुषङ्गिकौ ॥340॥ अनन्नपि भवेत्पापी निन्नन्नपि न पापभाक् । अभिध्यानविशेषेण यथा धीवरकर्षकौ ॥341॥ (भावार्थ – हिंसा और अहिंसा का विवेचन करते हुए पहले बतला आये हैं कि किसी का घात हो जाने से ही हिंसा का पाप नहीं लगता। संसार में सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्त से मरते भी हैं फिर भी मात्र इतने से ही उसे हिंसा नहीं कह सकते । वास्तव में तो हिंसा रूप परिणाम ही हिंसा है । जहाँ हिंसा रूप परिणाम है वहाँ किसी अन्य का घात न होने पर भी हिंसा होती है और जहाँ हिंसा रूप परिणाम नहीं है वहाँ अन्य का घात हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती। उदाहरणके लिए धीवर और किसान को उपस्थित किया जा सकता है। एक मच्छीमार धीवर मछली मारने के उद्देश्य से पानी में जाल डालकर बैठा है। उसके जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है फिर भी धीवर हिंसक है क्योंकि उसके परिणाम मछली मारने में लगे हैं। दूसरी ओर एक किसान है वह अन्न उपजाने की भावना से खेत में हल चलाता है। हल चलाते समय बहुत से जीव उसके हल से मरते जाते हैं किन्तु उसका भाव जीवों के मारने का नहीं है बल्कि खेत जोत-बोकर अन्न उत्पन्न करनेका है अतः वह मारते हुए भी पापी नहीं है। इसीलिए गृहस्थ को सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करना आवश्यक बतलाया है। ) कस्यचित्सन्निविष्टस्य दारान्मातरमन्तरा।
एक आदमी पत्नी के समीप बैठा है और एक आदमी माता के समीप बैठा है। दोनों ही नारी के अंग का स्पर्श करते हैं किन्तु दोनों की भावनाओं में बड़ा अन्तर है ॥342॥वपुःस्पर्शाविशेषेऽपि शेमुषी तु विशिष्यते ॥342॥ कहा भी है - "परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयो कुरालाः । (-आत्मानुशासन, श्लो० 23)तस्मात्पुण्योपचयः पापापचयच सुविधेयः" ॥343॥ कुशल मनुष्य परिणामों को ही-पुण्य और पापका कारण बतलाते हैं। अतः पुण्य का संचय करना चाहिए और पाप की हानि करनी चाहिए' ॥343॥ वपुषो वचसो वापि शुभाशुभसमाश्रया।
मन के निमित्त से ही शरीर और वचन की क्रिया भी शुभ और अशुभ होती है। मन की शक्ति अचिन्त्य है। इसलिए मन को ही शुद्ध करने का प्रयत्न करो ॥344 ॥ शरीर और वचन की क्रिया तो क्रम से होती हैं और कुछ ही वस्तुओं को अपना विषय बनाती हैं। किन्तु मनमें तो तीनों लोकों से भी बड़ी क्रिया क्षण-भर में हो जाती है। अर्थात् मन एक क्षण में तीनों लोकों के बारेमें सोच सकता है ॥345॥ क्रिया चित्तादचिन्त्येयं तदत्र प्रयतो भवेत् ॥344॥ क्रियान्यत्र क्रमेण स्यात्कियत्स्वेव च वस्तुषु । जगत्त्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया ॥345॥ तथा च लोकोक्तिः इसी विषयमें एक कहावत भी है "एकस्मिन्मनसः कोणे पुंसामुत्साहसालिनाम् ।
उत्साही मनुष्यों के मन के एक कोने में बिना किसी प्रयास के चौदह भुवन समा जाते हैं ॥346॥अनायासेन समान्ति भुवनानि चतुर्दश" ॥346॥ (भावार्थ – पहले बतला आये हैं कि जो काम अच्छे भावों से किया जाता है उसे अच्छा कहते हैं और जो काम बुरे भावों से किया जाता है उसे बुरा कहते हैं। अतः वचन की और काय की क्रिया तभी अच्छी कही जायेगी जब उसके कर्ताके भाव अच्छे हों। अच्छे इरादे से बच्चों को पीटना भी अच्छा है और बुरे इरादे से उन्हें मिठाई खिलाना भी अच्छा नहीं है। अतः मन की खराबी से वचन की और काय की क्रिया खराव कही जाती है और मन की अच्छाई से अच्छी कही जाती है । इसीलिए मन की शक्तिको अचिन्त्य बतलाया है। मन एक ही क्षण में दुनिया भर की बातें सोच जाता है किन्तु जो कुछ वह सोच जाता है उसे एक क्षण में न कहा जा सकता है और न किया जा सकता है ।अतः मनका सुधार करना चाहिए। ) भूपयःपवनाग्नीनां तृणादीनां च हिंसनम् ।
पृथ्वी, जल, हवा, आग और तृण वगैरह की हिंसा उतनी ही करनी चाहिए जितनेसे अपना प्रयोजन हो ॥347॥यावत्प्रयोजनं स्वस्य तावत्कुर्यादेजन्तु यत् ॥347॥ (भावार्थ-जीव दो प्रकार के बतलाये हैं त्रस और स्थावर । त्रस जीवों की हिंसा न करने के विषयमें ऊपर कहा गया है। स्थावर जीवों की भी उतनी ही हिंसा करनी चाहिए जितने के बिना सांसारिक काम न चलता हो। व्यर्थ जमीन का खोदना, पानी को व्यर्थ बहाना, व्यर्थ हवा करना व आग जलाना और बिना जरूरत के पेड़-पत्तों को तोड़ना आदि काम नहीं करना चाहिए । आशय यह है कि मिट्टी, पानी, हवा, आग और सब्जी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।) ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोकं प्रवर्तताम ।
नागरिक कार्यों में, स्वामी के कार्यों में और अपने कार्यों में लोकरीति के अनुसार ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों की भलाई और बुराई में लोक ही गुरु है। अर्थात् लौकिक कार्यों को लोकरीति के अनुसार ही करना चाहिए ॥348॥गुणदोषविभागेऽत्र लोक एव यतो गुरुः ॥348॥ प्रायश्चित्त का विधान दर्पण वा प्रमादाद्वा द्वीन्द्रियादिविराधने।
मद से अथवा प्रमाद से द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों का घात हो जाने पर दोष के अनुसार आगम में बतलायी गयी विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥349॥प्रायश्चित्तविधि कुर्यायथादोष यथागमम् ॥349॥ प्रायश्चित्त का स्वरूप प्राय इत्युच्यते लोकस्तस्य चित्तं मनो भवेत् ।
'प्रायः' शब्द का अर्थ ( साधु ) लोक है। उसके मन को चित्त कहते हैं। अतः साधु लोगों के मन को शुद्ध करने वाले काम को प्रायश्चित्त कहते हैं ॥350॥एतच्छुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तं प्रचक्षते ॥350॥ प्रायश्चित्त देने का अधिकार द्वादशाङ्गधरोऽप्येको न कृच्छ्र दातुमर्हति ।
द्वादशांग का पाठी होने पर भी एक व्यक्ति प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं है। अतः जो बहुश्रुत अनेक विद्वान् होते हैं वे ही प्रायश्चित्त देते हैं ॥351॥ तस्माद्बहुश्रुताः प्राज्ञाः प्रायश्चित्तप्रदाः स्मृताः ॥351॥ मनसा कर्मणा वाचा यदुष्कृतमुपार्जितम् ।
मन के द्वारा, वचन के द्वारा अथवा काय के द्वारा जो पाप किया है उसे मन के द्वारा, वचन के द्वारा अथवा कायके द्वारा ही छुड़वाना चाहिए ॥352॥मनसा कर्मणा वाचा तत् तथैव विहापयेत् ॥352॥ योग का स्वरूप, भेद और कार्य आत्मदेशपरिस्पन्दो योगो योगविदां मतः । मनोवाकायतलेधा पुण्यपापानवाश्रयः ॥353॥ योग के ज्ञाता पुरुष आत्मा के प्रदेशों के हलन-चलन को योग कहते हैं। वह योग मन, वचन और काय के भेद से तीन प्रकार का होता है और उसी के निमित्त से पुण्य कर्म और पाप कर्मका आस्रव होता है ॥353॥ (भावार्थ – जीवकाण्ड गोमट्टसार में योग का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है - पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय से युक्त जीव की जो शक्ति कर्मों के ग्रहण करने में कारण है उसे योग कहते हैं। इस योग शक्ति के द्वारा जीव शरीर, वचन और मन के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करता है और उनके ग्रहण करने से आत्मा के प्रदेशों में कम्पन होता है। यदि वह कम्पन काय-वर्गणा के निमित्त से होता है तो उसे काययोग कहते हैं, यदि वचन वर्गणा के निमित्त से होता है तो उसे वचन योग कहते हैं और यदि मनोवर्गणा के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहते हैं। इन योगों के होने पर जीव के पुण्य और पाप कर्मों का आस्रव होता है । ये तीनों योग शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकारके होते हैं। ) शुभाशुभ योग हिंसनाब्रह्मचौर्यादि काये कर्माशुभं विदुः ।
हिंसा करना, कुशील सेवन करना, चोरी करना आदि कायसम्बन्धी अशुभ कर्म जानना चाहिए ।झूठ बोलना, असभ्य वचन बोलना और कठोर वचन बोलना आदि वचनसम्बन्धी अशुभ कर्म जानना चाहिए ॥354॥ घमण्ड करना, ईर्ष्या करना, दूसरों की निन्दा करना आदि मनोव्यापार सम्बन्धी अशुभ कर्म हैं। तथा इससे विपरीत करने से काय, वचन और मन सम्बन्धी शुभ कर्म जानना चाहिए। अर्थात् हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना आदि कायिक शुभ कर्म हैं। सत्य और हित मित वचन बोलना आदि वचन सम्बन्धी शुभ कर्म हैं । अर्हन्त आदि की भक्ति करना, तप में रुचि होना, ज्ञान और ज्ञानियों की विनय करना आदि मानसिक शुभ कर्म हैं ॥355॥असत्यासभ्यपारुष्यप्रायं वचनगोचरम् ॥354॥ मासूयनादि स्यान्मनोव्यापारसंश्रयम् । एतद्विपर्ययाज्यं शुभमेतेषु तत्पुनः ॥355॥ पाप से बचने का उपाय हिरण्यपशुभूमीनां कन्याशय्यानवाससाम् ।
सोना, पशु, जमीन, कन्या, शय्या, अन्न, वस्त्र तथा अन्य अनेक वस्तुओं के दान देने से पाप शान्त नहीं होता ॥356॥जो रोग उपवास करने और औषधी का सेवन करने से दूर होते हैं जैसे उनके लिए केवल बाह्य उपचार व्यर्थ होता है वैसे ही पापके विषय में भी समझना चाहिए । अर्थात् मन वचन और काय को वश में किये बिना केवल बाह्य वस्तु का त्याग कर देने मात्र से पाप रूपी रोग शान्त नहीं होता ॥357॥ इसलिए पहले मन, वचन और काय को वशमें करके समस्त पाप के कारणों को दूर करो । फिर दान-पूजा वगैरह सब काम करो ॥358॥दानैर्बहुविधैश्चान्यैर्न पापमुपशाम्यति ॥356 ॥ लवनौषधसाध्यानां व्याधीनां बाघको विधिः । यथाकिञ्चित्करो लोके तथा पापोऽपि मन्यताम् ॥357॥ निहत्य निखिलं पापं मनोवाग्देहदण्डनैः । करोतु सकलं कर्म दानपूजादिकं ततः ॥358॥ रात्रि का कर्तव्य आप्रवृत्तनिवृत्तिमें सर्वस्येति कृतक्रियः।
रात्रि को जब सोओ तो सन्ध्याकाल का कृति कर्म करके यह प्रतिज्ञा करो कि जब तक मैं गार्हस्थिक कार्यों में फिर से न लगूं तब तक के लिए मेरे सबका त्याग है। और फिर पञ्च नमस्कार मंत्रका स्मरण करके निद्रा वगैरह लो ॥359 ॥ क्योंकि दैववश यदि आयु समाप्त हो जाये तो त्याग से बड़ा लाभ होता है। इसलिए व्रती को चाहिए कि जिस काल में वह भोग न करता हो उस कालको बिना व्रत के न जाने दे। अर्थात् उतने समयके लिए भोग का व्रत ले ले ॥360॥संस्मृत्य गुरुनामानि कुर्यान्निद्रादिकं विधिम् ॥359॥ दैवादायुविरामे स्यात्प्रत्याख्यानफलं महत् । भोगशून्यमतः कालं नावहेदव्रतं व्रती ॥360॥ जीव दया का महत्त्व एका जीवदयकत्र परत्र सकलाः क्रियाः ।
अकेली जीव दया एक ओर है और बाकी की सब क्रियाएँ दूसरी ओर हैं । अर्थात् अन्य सब क्रियाओं से जीव दया श्रेष्ठ है । अन्य सब क्रियाओं का फल खेती की तरह है और जीवदया का फल चिन्तामणि रत्न की तरह है जो चाहो सो मिलता है। अकेले एक अहिंसा व्रत के प्रताप से ही मनुष्य चिरजीवी, सौभाग्यशाली, ऐश्वर्यवान् , सुन्दर और यशस्वी होता है ॥361-362॥परं फलं तु पूर्व कृषेश्चिन्तामणेरिव ॥361॥ आयुष्मान्सुभगः श्रीमान्सुरूपः कीर्तिमानरः । अहिंसावतमाहात्म्यादेकस्मादेव जायते ॥362॥ अहिंसावत के पालक मृगसेन धीवर की कथा श्रूयतामत्र हिंसाफलस्योपाख्यानम्-अवन्तिदेशेषु सकललोकमनोहरागमारामे शिरीषप्रामे मृगसेनाभिधानो मत्स्यबन्धः स्कन्धावलम्बितगलजालाधुपकरणः पृथुरोमसमानयनोपनीतविहरणः कल्लोलजलप्लावितकूलशालेयमालवां सिमां सरितमनुसरनशेषमहर्षिपरिषद्वर्यमखिलमहाभागभूपतिपरिकल्पितसपर्य मिथ्यात्वविरहितधर्मचर्य श्रीयशोधराचार्य निचाय्य समासन्नसुकृतासाद्यहृदयत्वाहरादेव परित्यक्तपापसंपादनोपकरणग्रामः "ससंभ्रमं संपादितदीर्घप्रणामः प्रकामप्रगलदेनाः समाहितमनाः 'साधुसमाजसत्तम, समस्तमहामुनिजनोत्तम, दैवादुपपन्नपुण्यगृह्यभावोऽनुगृह्यतां कस्यचिद्वतस्य प्रदानेनायं जनः' इत्यभाषत। भगवान् - 'ननु कथमस्य 'पयःपतङ्गस्येव सदैव शकुलिविनाशनिःसंकाशयवशस्य व्रतग्रहणोपदेशे प्रवीणमन्तःकरणमभूत् । अस्ति हि लोके प्रवादः, न खलु प्रायेण प्राणिनां प्रकृतेर्विकृतिरायत्त्यां शुभमशुभं वा विना भवति' इत्युपयुक्तावधिः सम्यगवबुद्धसैविद्युतज्जीवितावर्धिस्तमेवमवादीत-'अहो शुभाशयायतन, अद्यतनाहनि यस्तवादावेवानाये मीनः समापतति स त्वया न प्रमायितव्यः। यावश्चात्म वृत्तिविषयमामिषं न प्राप्नोषि तावत्तव तन्निवृत्तिः'। अयं पुनः पश्चत्रिंशदक्षरपवित्रो मन्त्रः सर्वदा सुस्थितेन दुःस्थितेन च त्वया ध्यातव्यः' इति । मृगसेनः-'यथादिशति बहुमानस्तथास्तु' इत्यभिनिविश्य तां शैवलिनीमनुसृत्य जनितजालक्षेपोऽ कॉलक्षेपमत करणं वैसारिणमासाद्य स्मृतव्रतस्तस्य "श्रवसि चिह्नाय" चीरचीरी" निबध्यात्याक्षीत्" । पुनरपरावकाशे' तीरिणीप्रदेशे तथैवादूरतरशर्मा समाचरितकर्मा तमेवाषडक्षीणमक्षीणायुषमवाप्यामुञ्चत । तदेवमेतस्मिन्ननणिष्ठे पाठीनवरिष्ठे पञ्चकृत्वो लग्ने विपदमग्ने मुच्यमाने सति, "अस्तमस्तकमध्यास्त घेनघुसृणरसारुणितवरुणपुरपुरन्ध्रीकपोलकान्तिशाली गभस्तिमाली । तदनु तं गृहीतव्रतापरित्यागमोदमानचेतनं मृगसेनमधार्मिकलोकव्यतिरिक्त रिक्तमगिच्छन्तं परिच्छिंचे, अतुच्छकोपापरिहार्या तद्भार्या घण्टाख्या यमघण्टेव किमपि कर्णकटु क्वणन्ती कुटीरान्तःश्रितशरीरा निर्विवरमररं प्रदायास्थात् । मृगसेनोऽपि तया निरुद्धवेश्मप्रवेशनस्तन्मन्त्रस्मरणशक्तचित्तः पुराणतरतरुभिसमुच्छीर्षे विधाय सान्द्रं निद्रायन्नेतत्तरुभित्ताभ्यन्तरविनिःसृतेन सरोसपसुतेन दष्टः कष्टमवस्थान्तरमाविष्टो "व्युष्टसमये घण्टया दृष्टः। पुनरनेन सार्धमुर्षर्बुधमध्यानुगमोचितनिश्चययात्मनि विहितबहुनिन्दया शोचितश्च । ततः सा 'यदेवास्य व्रतं तदेव ममापि । जन्मान्तरे चायमेव मे पतिः' इत्यावेदितनिदाना समित्समिद्धमहसि द्रविणोदसि हव्यसमस्नेहं देहं जुहाव। __ अथ विलासिनीविलोचनोत्पलपुनरुक्तचन्दनमालायां विशालायां" पुरि विश्वगुणा महादेवीश्वरो विश्वम्भरो विश्वम्भरो नाम नृपतिः धनश्रीपतिः पिता च दुहितुः "सुबन्धोगुणपालो नाम श्रेष्ठी। तस्य किल गुणपालस्य मनोरथपान्थप्रीतिप्रपापालिकायामेतस्यां "कुलपालिकायामनेन मृगसेनेन समापन्नसत्त्वायां" सत्याम् , असौ वसुधापतिर्विटकथासंसृष्टतया प्रतिपन्नपाञ्चजनीनभावो नर्मभर्मनाम्नो नर्मसचिवस्य सुताय नर्मधर्मणे गुणपालश्रेष्ठिनमखिलकलाकलापालंकृतरूपसमन्वितां सुतामयाचत । श्रेष्ठी दुष्प्रक्षेन राज्ञा तथा याचितः 'यदि नर्मसचिवसुताय सुतां विरामि तदावश्यं कुलक्रमव्यतिक्रमो दुरपवादोपक्रमश्च । अथ "स्वामिशासनमतिक्रम्यात्रैवासे तदा सर्वस्वापहारः प्राणसंहारश्च' इति निश्चित्य प्रियसुहवः श्रीवत्तस्य वणिक्पतेनिकेतने समणिमेखलकलत्रं कलत्रमवस्थाप्य स्वापतेयसारं दुहितरं चात्मसात्कृत्य सुलभकेलिवनवनाशयनिवेशं कौशाम्बीदेशमयासीत् । . अत्रान्तरे श्रीमहरिद्रमन्दिरनिर्विशेषमाचरितचर्यापर्यटनौ शिवगुप्तमुनिगुप्तनामानौ मुनी श्रीदत्तप्रतिनिवेशनिवासिनोपासकेन यथाविधिविहितप्रतिग्रही कृतोपचारविग्रहौ च तामगणाश्रयां धनश्रियमपश्यताम् । तत्र मुनिगुप्तभगवान्किल केवलखलिस्नानपरुषवपुषमुद्गमनीयसंगतानाभोगविषमवैधव्यचिह्नदवरकमात्रालंकारजुषमाप्तकान्तापत्यपरिजनविरहदेहसादां गर्भगौरवखेदां च शिशिराजस्रवाञवशवर्तिनी स्थलकमलिनीमिव मलिनच्छविमुदवसितंपरिसरे परगृहवास'विशीर्यमाणमुखश्रियं धनश्रियं निध्याय' 'अहो, महीयसां खलु एनसामावासः कोऽप्यस्याः कुक्षौ महापुरुषोऽवतीर्णः, येनावतीर्णमात्रेणापि दुष्पुत्रेणेयं वराकी इयदावेशां दशामशिश्रयत्' इत्यभाषत । मुनिवृषा शिवगुप्तः–'मुनिगुप्त मैवं भाषिष्ठा यतो यद्यपीयं श्रेष्ठिनी कानिचिदिनान्येवम्भूता सती "पराधिष्ठाने तिष्ठति, तथाप्येतनन्दनेन सकलवणिक्पतिना राजश्रेष्ठिना निरवधिशेव धीश्वरेण विश्वम्भरेश्वरसुतावरेण च भवितव्यम्' इत्यवोचत् । एतच्च स्वकीयमन्दिरालिन्दगतः श्रीदत्तो निशम्य 'न खलु प्रायेणासत्यमिदमुक्तं भविष्यति महर्षेः' इत्यवधार्य सूचीमुखसर्पवहरीहितदत्तचेतोवृत्तिरासीत् । धनश्रीश्च परिप्राप्तप्रसवदिवसा सती सुतमसूत । श्रीदत्तः-''चित्रभानुरिवायमाश्रयाश: स्खलु बालिशः। तदसंजातस्नेहायामेवास्य जनन्यामुपांशुदण्ड: श्रेयान्' इति परामृश्य प्रसूतिदुःखेनातुच्छमूर्छापाश्रयां धनश्रियमाकलय्य निजपरिजनजरतीमुखेन 'प्रमीत एवायं तनयः संजातः' इति प्रसिद्धिं विधायाकार्य चैकमाचरितोपचारप्रपञ्चं श्वपचं जिलाझीरहस्यनिकेतः कृतापायसंकेतस्तं स्तन्यपमेतस्मै समर्पयामास। सोऽपि जनंगमः स्वर्भानुप्रभेण करेण रामरश्मिमिव तं स्तनन्धयमुपरुध्य निःशेलाकावकाशं देशमाश्रित्य पुण्यपरमाणुपुजमिव शुभशरीरभाजमेनमवेक्ष्य संजातकरुणारसप्रसरप्रसन्नमुखः सुखेन विनिधाय स्वकीयमेटीकत । पुनरस्यैवाधरभवभगिनीपतिरशेषापणिकपणपरमेष्ठी इन्द्रदत्तश्रेष्ठी विक्रयाडम्बरितशण्डमण्डलाधीनं पेठोपकण्ठगोष्ठीनमनुसृतो वत्सीयविषयसनीडक्रीडागतगोपालबालकलेपनपरम्परालापाद्वत्सेतरतानकसंतानपरिवृतमनेकचन्द्रकान्तोपलान्तरालनिलीनमरुणमणिनिधानमिव तं जातेमुपलभ्य स्वयमदृष्टनन्दनवदनत्वात्त बुद्धया साध्वनुरुभ्य 'स्तनन्धयावधानधृतबोधे राधे, तवायं गूढगर्भसंभवस्तनूद्भवः' इति प्रवर्धितप्रसिद्धिर्महान्तमपत्योत्पत्तिमहोत्सवमकार्षीत् । श्रीदत्तः श्रवणपरम्परया तमेनं वृत्तान्तमुपश्रुत्याश्रित्य च शिशुविनाशनाशयेन कीनाश इव तन्निवेशम् 'इन्द्रदत्त, अयं महाभागधेयो भागिनेयो ममैव तावद्धाम्नि वर्धताम्' इत्यभिधाय सभगिनीकं 'तोकमात्मावासमानीय पुरावत्करप्रक्षः संझपनार्थमन्तावसायिने' प्रायच्छत । सोऽपि दिवाकीर्तिरुपात्तपुत्रभाण्डः सत्त्वरमुपहरगहरानुसारी समीरवेशविगलितधनाम्बरावरणं हरिणकिरणमिव ईक्षणरमणीयं गुणपालतनयमालोक्य सदयहृदयः प्रबलविटपिसंकटे सरित्तटनिकटे परित्यज्य यथायथमश्वाल्लीत् । तत्राप्यसौ पुरोपार्जितपुण्यप्रभावादुपातृभिरिव एतद्वीक्षणात्तरत्क्षीरस्तनीभिरानन्दोदीरितनिर्भरहम्भाध्वनिभिः 'प्रचारायागताभिः कुण्डोनीभिर्बज लोकधेनुभिरुपर"सविधभागोऽपदान्तरमागतेन तद्रक्षणदक्षण गोपालजनेन "अस्तावतंसंभासिन्यशोकस्तबकसुन्दरे "सरोजसुहृदि सति विलोकितः। कथितश्च सकलगोष्ठज्येष्ठाय बल्लवकुलवरिष्ठाय निजाननापहसितारविन्दाय गोविन्दाय । सोऽपि पुत्रप्रेम्णा प्रमोदगरिम्णा चानीय जनितहृदयानन्दायाः सुनन्दायाः समर्पितवान् । अ(क)रोश्चास्येन्दिरामन्दिरस्य धनकीर्तिरिति नाम। ततोऽसौ क्रमेण मकरन्दपरित्यक्तशैशवदशः कमलेश इव युवजनमन:पण्यतारुण्योत्फुल्लबलवीलोचनालिकुलावे ले लावण्यमकरन्दममन्दानन्दकामदमतिकान्तरूपायतनं यौवनमासादितः पुनरपि प्राज्याज्यवणिज्योपार्जनसजागमनेन तेन श्रीदत्तेन दृष्टः । पृष्टश्च गोविन्द स्तदवाप्तिप्रपञ्चम् । श्रीदत्तः-गोविन्द, मदीये सदने किमपि महत्कार्यमात्मजस्य निवेद्यमस्ति । तदयं 'प्रबुरिमं लेखं प्राहयित्वा सत्वरं प्रहेतेव्यः।' गोविन्दः-'श्रेष्ठिन् , एवमस्तु । ' लेखं चैवमलिखत्-'अहो विदितसमस्तपौतवकल महाबल, एष खल्वस्मद्वंशविनाशवैश्वानरोऽवश्यं विष्यो मुशल्यो वा विधातव्यः' इति । धनकीर्तिस्तथा तातवणिक्पतिभ्यामादिष्टः सार्वष्टम्भं गलालङ्कारसखं लेखं कृत्वा गत्वा च जन्मान्तरोपकाराधीनमीनावतारसरसीमेकानी तत्प्रवेशपदिरपर्यन्तवर्तिनि वने पद्मश्रमापनयनाय "पिकप्रियालवालपरिसरे "निःसंज्ञमस्वाप्सीत् । । अत्रावसरे विहितपुष्पावचयविनोदा सपरिच्छदा निखिलविद्याविदग्धा पूर्वभवोपकारस्निग्धा संजीवनौषधिसमानानङ्गसेनानामिका गणिका तस्यैव सहकारतरोस्तलमुपदौक्य विलोक्य च निस्पन्दलोचना चिराय तमनङ्गमिव "मुक्तकुसुमास्त्रतन्त्रं "लोकान्तरमित्रमशेषलक्षणोपलक्षितमूर्ति धनकोतिं पुनरायुःश्रीसरस्वतीसमागमादेशरेखात्रयेणेव प्रकटवितर्कितकर्कोटत्रयेण बन्धुरमध्यप्रदेशात्कण्ठदेशादादायापायप्रतिपादनाक्षरालेख लेखमवाचयत् । लिलेख च तं वाणिजकापसदं हृदयेन "विकुर्वती लोचनाअनकरण्डादुपातेन वनवल्लिपल्लवनिर्यासरसद्रुतेन कजलेनार्जुनर्शलाकया तत्रैव परिम्लिष्टेपुरातनसूत्रे पत्रे लेखान्तरम् । तथा हि-'यदि श्रेष्ठिनी मामवधेयेवंचनं श्रेष्ठिनं मन्यते, महाबलश्च यदि मामनुल्लङ्घनीय वाक्प्रसरं पितरं गणयति, तदास्मै निकामं सप्तपुरुषपर्यन्तपरीक्षितान्वयसंपत्तये धनकीर्तये कूपदप्रक्रमेण 'विजदेवमुखसमक्षमविचारापेक्षं श्रीमतिर्दातव्या' इति । ततो यथाम्नातविशिखमिमं लेखमामुर्घ्य समाचरितगमनायामनगसेनायां धनकीर्तिश्चिरेण "विद्राणसान्द्रनिद्रोद्रेक सोत्सेकमुत्थाय प्रयाय च श्रीदत्तनिकेतनं जननीसमन्विताय महाबलाय प्रदर्शितलेखः श्रीमतीसखोऽभवत्। श्रीदत्तो वार्तामिमामाकर्ण्य प्रतूर्णे प्रत्यावर्त्य निधीय च तबधाय राजधानीबाहिरिकायां चण्डिकायतने कृतसंकेतं संनद्धवपुषं पुरुषं कश्चराचरणपिशाची "देवद्रीची च परिप्राप्तोदवसितो रहसि धनकीर्ति मुहुराहूय बहुकूटकपटमतिरेवमावभाषे–'वत्स, मदीये कुले किलैवमाचारो यदुत यामिनीमुखे कात्यायिनीप्रेमुखे प्रदेशे प्रतिपन्नाभिनवकङ्कणबन्धेन स्तनन्धयागोघेन महारजेनरसरकांकसमाश्रयः स्वयमेव मार्षमयमोरमौकुंलिबलिरुपहर्तव्यः।' धनकीर्तिः–'तात, यथा तातादेशः' इति निगीर्य गृहीतकुलदेवतादेयहन्तकारोपकरणस्तेन श्यालेन महाबलेन पुरप्रदेशाभिःसरमवलोकितः। समालापितध-'हहो धनकीत, प्रवर्धमानान्धकारावभ्यायामस्यां लायामवर्गणः कोचलितोऽसि । ' 'महाबल, मातुलनिदेशान मसितनिवेदनाय दुर्गालये । ' 'यद्येवं नगरजनासंस्तुतत्वात्त्वं निवासं प्रति निवर्तस्व । अहमेतदुपयाचितमैशान्याः स्पर्शयितुं प्रगच्छामि । यद्यत्र तातो रोषिष्यति तदा तद्रोषमहमपनेष्यामि । ' ततो धनकीर्तिमन्दिरमगात्, महायलश्च कृतान्तोदरकन्दरम् । श्रीदत्तः सुतमरणशोकातोपान्तः प्रकाशिताशेषवृत्तान्तः 'सकलनिकाय्यकार्यानुष्ठानपरमेष्ठिनि श्रेष्ठिनि मन्मनोहादचन्द्रलेखे विशाखे, कथमयं वैधेयो ममान्षयोपायहेतुः प्रयुक्तोपायविलोपनकेतुः प्रवाशयितव्यः।' विशाखा-'भेष्ठिन्, भेलभावात्सर्वमनुपपन्नं त्वया चेष्टितम् । अतः कुरुण्डतो भीतः कुक्कुटपोत इव तूष्णीमास्स्व । भविष्यति भवतोऽ. शेषं मनीषितम्' इत्याभाष्य अपरेधुर्दयितजीवितव्यतोदकेषु मोदकेषु विषं संचार्य 'सुते श्रीमते, य एते कुन्दकुमुदकान्तयो मोदकास्ते स्वकीयाय कान्ताय देयाः, "श्यावश्यामाकश्यामलरुचयश्च जनकाय' इति समर्पितसमया' समासनमरणसमया सरिति संवैनायानुससार । श्रीमतिः 'यञ्चोक्ष भक्ष्यन्तत् प्रतीक्ष्याय ताताय वितरीतव्यम्' इत्यवगत्याविज्ञातसवित्रीचित्तकौटिल्या निःशल्यहदया तानेतयोर्विपर्ययेणावीवृधत् । विशाखा पतिशन्यमरण्यसामान्यमगारमाप्य परिदेव्यय सुचिरं पुनः 'पुत्रि, किमन्यथा भवति महामुनिभाषितम् । केवलं तव "वापेन मया च' थेात्मीयान्वयविलोपाय कृत्योत्थापनमाचरितम्तदलमत्र बहुप्रलापेन । कल्पद्रुमेण कल्पलतेव त्वमनेन देवदेयदेहरक्षाविधानेन धवेन सार्धमाकल्पमिन्द्रियैश्वर्यसुखमनुभव' इति संभाविताशीर्वादा तमेकं मोदकमास्वाद्य पत्युः पथि प्रेतस्थे। ___एवं विहितदुरीहितवशादुपाचामिततोकशोकावस्थे दर्शमीस्थे तस्मिञ्श्वशुरे श्वश्रूजने च सति स पुरातनपुण्यमाहात्म्यादुल्लवितघोरप्रतिघंपञ्चकापत्प्रतिदिनमुदीयमानसंपदेकदा तेन विश्वम्भरेण तितीश्वरेण निरीक्षितः। तद्रूपसंपत्तौ जातबहुविस्मयेन तनूजया सह उभयेन विशामाधिपत्यपदेन योजितश्च । गुणपालः किंवदन्तीपरम्परया अस्य कल्याणपरम्परामुपश्रुत्य कौशाम्बीदेशात्पमार्वतीपुरमागत्य अनेनाश्चर्यैश्वर्यभाजा तुजी सह संजग्मे । अथान्यदा सकलत्रपुत्रमित्रतन्त्रेण धनकीर्तिना दर्शनायागतयानङ्गसेनया चानुगतिनिष्ठो गुणपालश्रेष्ठी मतिश्रुतावधिमनःपर्ययविषयसम्राजमखिलमुनिमण्डलोराजं श्रीयशोध्वजनामभाजं भगवन्तमभिवन्ध सबहुप्रश्रयमेवमपृच्छत्–'भगवन् , किं नाम जन्मान्तरे धर्ममूर्तिना धनकीर्तिना सुकृतमुपार्जितम्, येन बालकालेऽपि तानि तानि दैवैकशरणप्रतीकाराणि व्यस. नानि व्यतिक्रान्तः, येनास्मिन्न्यतिरिक्तरसारूपसंपन्नोऽभूत, येनाद भ्राभ्रियविभावसुप्रभासंभार इव देवानामप्यप्रतिहतमहः समजनि, येन चापरेषामपि तेषां तेषां महापुरुषकक्षा"वग्रहाणां गुणानां समवायोऽभवत् । तथा हि-स्थानं "वदन्यतायाः, समाश्रयो वदान्य भावस्य, निकेतनमवदानकर्मणः, क्षेत्र मैत्रेयिकायाः, स्वप्नेऽपि न स्वजनस्याजनि मनोमतः कन्तुरिव च कामिनीलोकस्य । तदस्य भदन्त, 'प्रापणिकपरिषत्प्रवणस्य निःशेषशास्त्रप्रवीणान्तःकरणस्य निसर्गादेव निखिलपरिजनालापनसक्तस्य विनेयजनमनःकुवलयानन्दिकथावतारामृत तः सुकीर्तेर्धनकीर्तेः पुरोपार्जितं सुकृतं कथयितुमर्हसि । ' भगवान्-'श्रेष्ठिन् , श्रूयताम् । ' तत्संबन्धसक्तं पूर्वोक्तं वृत्तान्तमचकथत्-'या चास्य पूर्वभवनिकटा घण्टा वधूटी सा कृतनिदानादनसिप्रवेशादियं संप्रति श्रीमतिः संजाता। यश्च स मीनः स कालक्रमेण व्यतिक्रम्य पूर्वपर्यायपर्वेयमनङ्गसेनाभूत्। अतोऽस्य महाभागस्यैकदिवसाऽहिंसाफलमेतद्विज़म्भते । धनकीर्तिरेतद्वचत्रपवित्रश्रोत्रवा तथा श्रीमतिरनङ्गसेना च पुराभवं भवं संभाल्योन्मूल्य च तमःसंतानतरुनिवेशमिव केशपाशं तस्यैव दोषेशंस्यान्तिके यथायोग्यताविकल्पं तपःकल्पमादाय जिनमार्गोंचितेनाचरितेन चिरायाराध्य रत्नत्रयं विधाय च विधिवन्निरजन्यमनोवर्तनं प्रायोपवेशनम् । तदनु धनकीर्तिः सर्वार्थसिद्धिसाधनकीर्तिबभूव । श्रीमतिरनङ्गसेना च'कल्पान्तरसंयोज्यं देवसायुज्यमभजत् । (अब अहिंसा व्रत के फल के सम्बन्ध में एक कथा सुनें) अवन्ति देश के शिरीष नामक गाँव में मृगसेन नाम का धीवर रहता था। एक दिन वह कन्धे पर जाल रखकर मछली लाने के लिए सिप्रा नदी की ओर चला। रास्ते में उसने मुनियों की परिषद्के बीच में बैठे हुए तथा राजाओं से पूजित और मिथ्यात्व से रहित धर्म का आचरण करने वाले आचार्य श्री यशोधर को देखा। अपने पापार्जन में सहायक जाल वगैरह उपकरणों को दूरसे ही छोड़कर वह आचार्य के पास गया और जल्दी से साष्टांग नमस्कार करके बड़ी धीरता के साथ बोला-'हे साधु-समाज में श्रेष्ठ और समस्त महामुनियोंमें उत्तम मुनिराज ! आज भाग्य से ही पुण्य संचय का यह अवसर मिला है अतः कोई व्रत देकर मुझे अनुगृहीत करें।' यह सुनकर मुनिराज सोचने लगे-' बगुले की तरह सदैव मछलियों के मारने में निःशङ्कचित्त इस धीव रका मन व्रतग्रहण करने के लिए कैसे हुआ ? लोकमें किंवदन्ती है कि प्रायः उत्तर काल में होनेवाले शुभाशुभ के बिना प्राणियों का स्वभाव नहीं बदलता' यह सोचकर उन्होंने अवधिज्ञान का उपयोग किया और उसे अल्पायु जानकर बोले- 'हे सदाशय ! आज तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आये उसे मत मारना । तथा जब तक अपनी जीविकारूप मांस तुम्हें प्राप्त न हो तब तकके लिए. तुम्हारे मांसका त्याग है। और यह पैंतीस अक्षरका पवित्र नमस्कार मन्त्र है, सदा सुख-दुःख में इसका ध्यान करना।' मृगसेन ने 'जो आज्ञा' कहकर व्रत ग्रहण कर लिये और नदी पर जाकर जाल डाल दिया। जल्दी ही उसके जाल में एक बड़ी मछली आ गयी ।उसने अपने व्रत को स्मरण करके पहचान के लिए उसके कानमें कपड़े की चिन्दी बाँधकर जल में छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे स्थान से नदी में जाल डाला किन्तु वही मछली जाल में फिर आ गयी। अतः उसे अबध्य जानकर छोड़ दिया। इस प्रकार पाँच बार वही मछली जाल में आयी और पाँचों बार उसने उसे जलमें छोड़ दिया । इतने में प्रचुर केसर से युक्त स्त्री के कपोल की तरह कान्तिवाला सूर्य अस्त हो गया । और मृगसेन स्वीकार किये हुए व्रत का पालन करने से प्रसन्नचित्त होता हुआ खाली हाथ घर लौटा॥उसे खाली हाथ आता देखकर उसकी पत्नी घण्टा बड़ी क्रुद्ध हुई और यमराज के घण्टे की तरह गाली-गलौज बकती-झकती अपनी झोपड़ी में चली गयी और अन्दर से दरवाजा बन्द करके बैठ गयी। मृगसेन भी अपनी पत्नी के द्वारा घर में प्रवेश करने से रोक दिये जाने पर पञ्च-नमस्कार मन्त्र का स्मरण करते हुए एक पुराने वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर गाढ़ नींद में सो गया । जब वह गाढ़ नींद में था तभी उस वृक्ष की जड़ से निकलकर एक साँपने उसे डस लिया और वह बड़े कष्ट से मर गया। प्रभात होने पर घण्टा ने उसे उस अवस्था में देखा ।उसने अपनी निन्दा करते हुए बड़ा पश्चात्ताप किया। और उसी के साथ अग्नि में जल जाने का निश्चय किया। तथा उसने निदान किया कि जो इसका व्रत था वही मेरा भी है और दूसरे जन्म में भी यही मेरा पति हो । उसके बाद उसने आग प्रदीप्त की और उसमें होम सामग्री के समान स्नेह से पूरित शरीर को होम दिया। विशाला नगरी में विश्वम्भर नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम विश्वगुणा था। वहीं गुणपाल नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनश्री था और पुत्रीका नाम सुबन्धु था। गुणपाल सेठ की पत्नी धनश्री गर्भवती हुई और मृगसेन धीवर का जीव उसके गर्भमें आया। राजा विश्वम्भर को विटों की संगति के कारण भाण्डजन बहुत प्रिय थे। अतः उसने नर्मभर्म नामके विदूषक के पुत्र नर्मधर्म के लिए गुणपाल से उसकी समस्त कलाओं में प्रवीण सुन्दरी कन्या की याचना की । दुर्बुद्धि राजा की इस माँग से गुणपाल विचार में पड़ गया । 'यदि विदूषक के पुत्र को कन्या देता हूँ तो अवश्य ही कुल परम्परा का लंघन होता है और अपवाद भी फैलता है। और यदि राजाज्ञा को न मानकर भी यहाँ रहता हूँ तो सर्वस्व अपहरणके साथ-साथ प्राण भी जाते हैं।' ऐसा सोचकर उसने रलजटित करधौनी से शोभित अपनी पत्नीको तो अपने प्रिय मित्र श्रीदत्त सेठ के घरमें रखा और पुत्री को साथ लेकर बाग-बगीचों से शोभित कौशाम्बीपुरी को चला गया। इसी बीच में धनी और गरीब के मकान का भेद न करके चर्या के लिए भ्रमण करते हुए शिवगुप्त और मुनिगुप्त नाम के दो मुनि श्रीदत्तके मकान के सामनेसे निकले । श्रीदत्त के पड़ोस में रहनेवाले गृहस्थ ने उन्हें विधिपूर्वक पड़गाहा ।और जब वे भोजन कर चुके तो आँगनमें बैठी हुई धनश्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। तेल के बिना स्नान करने से उसका शरीर रूक्ष हो गया था, केवल दो वस्त्र और सधवाके चिह्न स्वरूप बहुत थोड़े अलंकार पहने हुए थी, पति पुत्री और परिजनों के वियोगसे उसका शरीर खेद खिन्न था, गर्भ के भारसे पीड़ित थी, शीतऋतु के निरन्तर आगमन से कुम्हलायी हुई स्थलकमलिनीकी तरह उसकी कान्ति मलिन हो गयी थी, दूसरे के घरमें रहने से मुख की शोभा चली गयी थी। घर के आँगन में बैठी हुई धनश्री को इस रूप में देखकर मुनिगुप्त मुनि बोले-'इसकी कोख में कोई बड़ा पापी महापुरुष आया जान पड़ता है, जिसके गर्भ में आने मात्र से इस वेचारी की यह दुर्दशा हुई है।' यह सुनकर शिवगुप्त मुनि बोले-'मुनिगुप्त ! ऐसा मत कहो। यद्यपि यह सेठानी कुछ दिन तक इस तरह पराये घर में रहेगी, फिर भी इसका पुत्र समस्त वैश्यों का स्वामी और अपार सम्पत्तिशाली राजश्रेष्ठी होगा तथा राजा विश्वम्भर की पुत्री को वरण करेगा।' यह बात अपने मकान के बाहर चबूतरेपर खड़े श्रीदत्त ने सुनी। 'मुनियों का कथन झूठा नहीं होता' यह सोचकर श्रीदत्त ने विषधर सर्प की तरह अपना मन अपने दुष्ट संकल्प की ओर लगाया। पूरे दिन होनेपर धनश्री ने पुत्र को जन्म दिया। श्रीदत्त ने सोचा-'यह बालक आग की तरह अपने आश्रय को ही खाने वाला है। इसलिए माता का इस पर स्नेह उत्पन्न होने के पहले ही इसका गुप्त वध करा डालना श्रेष्ठ है।' प्रसूति के कष्ट से धनश्रीको एकदम बेहोश देखकर उसने अपने कुटुम्ब की एक बुढ़िया के द्वारा यह प्रसिद्ध करा दिया कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है। और घूस वगैरह देकर एक चाण्डाल को इस कार्यके लिए तैयार किया तथा उसे बुलाकर उस कुटिल भाषा के रहस्यमें विशारद श्रीदत्त ने उसे मारनेका संकेत करके बालक को सौंप दिया। राहु के समान हाथ के द्वारा सूर्य के समान उस बालक को उठाकर वह चाण्डाल एकान्त स्थान में ले गया। वहाँ पुण्य परमाणुओं के पुंज की तरह इस सुन्दर बालक को देखकर उसे दया आ गयी और प्रसन्न मुख होकर उसने उस बालकको वहीं सुख से लिटा दिया तथा अपने घर चला आया। श्रीदत्त का छोटा बहनोई इन्द्रदत्त श्रेष्ठी व्यापार के लिए उधर गया था। वहाँ उसने शिशु के पास खेलने के लिए आये हुए ग्वाल-बालकों के मुखसे उस बालकका समाचार सुना और वह उस स्थानपर गया ।वहाँ उसने अनेक बछड़ों से घिरे हुए उस शिशु को देखा जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो अनेक चन्द्रकान्त मणियों के बीच में स्थित लालमणि का खजाना है। उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः उसने उसे अपना पुत्र मानकर उठा लिया और पुत्र के लिए अत्यन्त लालायित अपनी पत्नी राधा से बोला-'राधे! तुम्हारे गूढ गर्भ से इस शिशुने जन्म लिया है।' उसने सर्वत्र यह बात फैला दी और पुत्रोत्पत्ति की खुशी में बड़ा भारी उत्सव किया । श्रीदत्तने कानों-कान यह समाचार सुना और बच्चे को मार डालने के विचार से यमराज की तरह इन्द्रदत्त के घर आया और बोला-'इन्द्रदत्त ! यह भाग्यशाली भानजा मेरे ही घर में बड़ा होना चाहिए।' यह कहकर बहिन के साथ बच्चे को अपने घर ले आया और पहले की ही तरह मार डालने के लिए उसे वधिक को दे दिया। वह बधिक भी उस बच्चे को लेकर शीघ्र ही एकान्त गुफा की ओर चल दिया। हवाके चलने से जिसके ऊपर से मेघपटलका आवरण हट गया है उस चन्द्रमा के समान नयनाभिराम उस बालक को देखकर उसका हृदय भी दयालु हो गया। और नदीके किनारे वृक्षों के एक झुण्ड में उस बालक को रखकर वह चला गया। इसके पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से वहाँ भी चरने के लिए जो गायें आयी थीं वे इसे देखते ही आनन्द से रभाती हुई इसके पास चली आयीं और उनके थनों से दूध झरने लगा। सन्ध्या के समय जब सूर्य डूबने लगा तो उन गायों के रखवाले ग्वालों ने यह कौतुक देखा और समस्त ग्वालों के सरदार गोविन्दसे कहा । पुत्र स्नेह वश आनन्द से गद्गद होता हुआ गोविन्द भी उस बालक को घर ले आया और अपनी पत्नी सुनन्दा को सौंप दिया ।बालक का नाम धनकीर्ति रखा गया । धीरे-धीरे बचपन को छोड़कर धनकीर्ति असीम आनन्द को देनेवाली तथा अत्यन्त मनोहर रूपकी दात्री युवावस्थाको प्राप्त हुआ। श्री कृष्णकी तरह युवाजनों के मन को खरीदने के लिये पण्य रूप तारुण्य से विकसित गोपिकाओं के लोचनरूपी भ्रमर उसके लावण्यरूपी मकरन्द का पान करने के लिए आकुल रहते थे। एक दिन घी के व्यापार के निमित्त से श्रीदत्त उधर आ निकला । उसने देखा और गोविन्दसे पूछा कि यह लड़का उसे कहाँ से मिला ? सुनकर श्रीदत्त बोला 'गोविन्द, मुझे अपने घर पर अपने लड़के से कुछ जरूरी बात कहलाना है । अतः इस लड़के को यह पत्र देकर शीघ्र भेज दो।' गोविन्द ने श्रीदत्तकी बात स्वीकार कर ली। पत्रमें लिखा था-'माप-तौल में कुशल महाबल! यह लड़का हमारे वंश का विनाश करने के लिए आग के समान है। अतः या तो इसे विष दे देना या मूसल से मार डालना।' पिता और वैश्यपति की आज्ञा पाकर उस मुद्राङ्कित पत्र को अपने गले में बाँधकर धनकीर्ति उस उज्जैनी नगरी की ओर चल दिया जिसमें उसके द्वारा पूर्व जन्म में उपकृत मछली ने जन्म लिया था। नगरी के निकट पहुँचकर वह नगरी के.प्रवेश मार्ग के निकटवर्ती वन में रास्ते की थकान दूर करने के लिए आम की क्यारियों के निकट गहरी नींद में सो गया। इसी बीचमें वस्त्रालंकार से सुसज्जित, समस्त विद्याओं में निपुण और पूर्व जन्मके उपकार से उपकृत अनङ्गसेना नामक वेश्या पुष्प चयन करके उसी आम के पेड़के नीचे आयी और कामदेव के समान सुन्दर समस्त लक्षणों से युक्त तथा पूर्व जन्म के मित्र धनकीर्ति को देखकर देखती ही रह गयी। उसके कण्ठमें तीन रेखाएँ थीं जो मानो आयु, लक्ष्मी और सरस्वती के आगमन को ही सूचित करती थीं। अचानक अनङ्गसेना की निर्निमेष दृष्टि गले में बँधे पत्र पर पड़ी। उसने उस अशुभ पत्र को खोलकर पढ़ा, और उस निकृष्ट वणिक का हृदय से तिरस्कार करते हुए अपने लोचन रूपी अञ्जन की डिबिया से काजल लेकर उसे लताओं की नयी कोंपलों के रसमें भिगोया तथा चाँदी की सलाई से अथवा तृण से उसी पत्रपर पहले के लेखको मिटाकर दूसरा लेख लिखा जो इस प्रकार था— 'यदि सेठानी मेरे वचनों को मानती है और यदि महाबल मुझे अपना पिता मानता है तथा मेरे वचनों को अनुल्लंघ्य समझता है तो इस धनकीर्ति को, जिसके वंशकी श्रेष्ठता की परीक्षा सात जनों के सामने कर ली गयी है, बिना किसी विचारके अग्नि की साक्षी पूर्वक दहेज के साथ श्रीमती को सौंप देना।' पहले की ही तरह इस लेख को उसके गले में बाँधकर अनङ्गसेना चली गयी। धनकीर्ति बहुत देर तक गहरी नींद में सोता रहा। फिर उठकर श्रीदत्त के घर पहुंचा और माता सहित महाबल को पत्र देकर श्रीमती का पति बन गया। श्रीदत्त इस समाचार को सुनकर शीघ्र ही लौट आया और राजधानी के बाहर स्थित चण्डीदेवी के मन्दिरमें धनकीर्ति को मारनेके लिए एक सशस्त्र मनुष्य को तथा कुत्सित काम करने में पिशाचीसमान देवीको नियुक्त करके घर आया । और एकान्त में धनकीर्ति को बुलाकर वह कपटी बोला-'वत्स ! मेरे कुल की ऐसी रीति है कि जिस कन्या का नया विवाह होता है उसका पति रात्रि के समय कुसुम्भे के रंग से रंगे हुए वस्त्र पहनकर स्वयं ही चण्डी के मन्दिरमें उड़द से बने हुए मोर और कौवे की बलि देता है।' 'जैसी आज्ञा' कहकर धनकीर्ति कुलदेवता को अर्पित करने की सामग्री लेकर घर से निकला। सामने से आते हुए उसके साले महाबल ने उसे देखा और पूछा- 'धनकीर्ति ! इस अन्धेरी रात में अकेले कहाँ जाते हो ?' । 'महाबल ! मामा की आज्ञा से बलि देने के लिए दुर्गा के मन्दिर को जाता हूँ।' 'यदि ऐसा है तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है ।नगरके आदमी क्या कहेंगे ! अतः तुम घरको लौट जाओ। देवी को यह भेंट समर्पित करने के लिए मैं जाता हूँ। यदि पिताजी रुष्ट होंगे तो उनके रोष को मैं दूर कर दूंगा।' इस बातचीत के बाद धनकीर्ति घर को चला गया और महावल यमराज के पेटमें समा गया। पुत्र-मरण के शोक से विह्वल होकर श्रीदत्त ने अपनी पत्नी विशाखा से सब समाचार कह दिया और बोला--सब गृहकार्यों के करने में चतुर सेठानी! यह अभागा मेरे वंश का अनिष्ट करने वाला है, इसके मारने का जो-जो उपाय किया जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। इसे कैसे मारना चाहिए।' 'सेठजी ! अविचार के कारण आपके सब उपाय व्यर्थ हुए। अतः बिलाव से डरे हुए मुर्गे के बच्चे की तरह आप चुप होकर बैठो। आपकी सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी।' । दूसरे दिन सेठानी ने अपने पति के जीवनको नष्ट करने वाले लड्डुओं में जहर मिलाकर अपनी पुत्री श्रीमती से कहा--'पुत्री ! ये जो सफेद कमल की तरह स्वच्छ लड्डू हैं इन्हें अपने पति को देना और ये जो काले धान्य के समान काले रंग के लड्डू हैं इन्हें अपने पिताको देना । ' इतना कहकर सेठानी नदी में स्नान करने चली गयी। श्रीमती को माता के चित्तकी कुटिलता का पता नहीं था। उसने सोचा कि जो सुन्दर लड्डू हैं उन्हें पूज्य पिता को देना चाहिए। अतः उसने जहर मिले सफेद लड्डू तो पिता को दिये और काले लड्डू अपने पति को दिये। जब विशाखा लौटी तो उसका पति मर चुका था। वह बहुत रोई फिर बोली-'पुत्री ! महामुनियों का कथन कैसे झूठा हो सकता है ? तेरे पिता ने और मुझ वृद्धा ने अपने वंश का नाश करने के लिए ही यह गढ़ा खोदा था । अब रोने से क्या होता है ? कल्पवृक्ष के साथ कल्पलता के समान तू अपने इस दैवरक्षित पति के साथ कल्पकाल तक ऐश्वर्य और इन्द्रिय सुखको भोग।' ऐसा आशीर्वाद देकर उसने भी एक जहरीला लड्डू खा लिया और पति की अनुगामिनी बन गयी। इस प्रकार पूर्व उपार्जित पुण्य के प्रताप से पाँच भयानक विपत्तियों से बचकर धनकीर्ति अपने ही द्वारा की गयी दुर्भावनाओं के कारणसे सास और श्वसुर के चल बसने पर प्रतिदिन सम्पत्तिशाली होने लगा। एक दिन राजा विश्वम्भर ने उसे देखा। उसका सौन्दर्य देखकर राजा को बहुत अचरज हुआ। उसने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे वैश्यों का अधिपति बना दिया। धनकीर्ति के पिता गुणपाल ने लोगों के मुख से जब अपने पुत्र के अभ्युदय का समाचार सुना तो वह कौशाम्बी नगरी से उज्जयिनी आकर आश्चर्यजनक सम्पत्तिशाली पुत्रसे मिला । एक बार मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञानके धारी श्री यशोध्वज मुनिराज वहाँ पधारे ।गुणपाल सेठ, सकुटुम्ब धनकीर्ति और उससे मिलने के लिए आयी हुई अनंगसेना के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए गया, और उन्हें नमस्कार करके विनयपूर्वक बोला—'भगवन् ! धर्ममूर्ति धनकीर्ति ने पूर्व जन्ममें कौन-सा पुण्य कमाया था, जिसके कारण बचपन में भी यह उन कष्टों को पार कर गया जो दैव के द्वारा ही दूर किये जा सकते थे तथा इस जन्म में इसने बड़ी भारी सम्पत्ति और सौन्दर्य पाया, सूर्यके तेज की तरह देवों से भी न रोका जा सकनेवाला इसे तेज प्राप्त हुआ ।इसके सिवाय महापुरुषों के योग्य अन्य भी गुण इसे प्राप्त हो सके । जैसे, यह बड़ा दानी है, प्रियवादी है, सत्कर्म करता है, मित्रता के उपयुक्त है, स्वप्न में भी स्वजनों के मन को कष्ट नहीं पहुँचाता और स्त्रियों के लिए तो मानो कामदेव ही है। इसलिए भगवन् ! समस्त शास्त्रों में प्रवीण और स्वभाव से ही समस्त कुटुम्बीजनों से मीठे वचन बोलने वाले इस वैश्यपति धनकीर्ति के पूर्वोपार्जित पुण्यको कथा कहें ।इसकी कथा सुनकर सबके मन प्रफुल्लित होंगे।' मुनिराजने धनकीर्ति के पूर्व जन्म की कथा कह सुनायी और बोले- 'इसके पूर्वभव की पत्नी घण्टा यह निदान करके कि 'जो इसका व्रत है वही मेरा भी व्रत है और मैं दूसरे भवमें भी इसकी पत्नी होऊँ ' अग्निमें जल मरी थी। वही मरकर श्रीमती हुई है। और जो मछली थी जिसे मृगसेन धीवर ने जलमें छोड़ दिया था, वह पूर्व पर्याय को छोड़कर अनङ्गसेना हुई है। अतः एक दिन हिंसा न करने का यह फल इस महाभाग को मिला है। ' पूर्वभव के इस वृत्तान्तको सुनकर धनकीर्ति, श्रीमती और अनंगसेना ने केशलोंच करके उन्हीं मुनिराज के पास में जिनदीक्षा ले ली। और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप ग्रहण करके जैनमार्ग के अनुसार चिरकाल तक रत्नत्रय का आराधन किया। तथा अन्त में विधिपूर्वक निर्विघ्न समाधि मरण करके धनकीर्ति तो सर्वार्थसिद्धि में देव हुआ और श्रीमती तथा अनंगसेना स्वर्गलोक में उत्पन्न हुई। इस कथा के विषयमें एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है - पञ्चकत्वः किलैकस्य मत्स्यस्याहिंसनात्पुरा ।
"पूर्व जन्ममें पाँच बार एक मछली को न मारने से धनकीर्ति पाँच बार आपत्ति से बचकर लक्ष्मी का स्वामी बना" ॥363॥ अभूत्पश्चापदोऽतीत्य धनकीर्तिः पतिः श्रियः ॥363॥ इत्युपासकाध्ययने अहिंसाफलावलोकनो नाम षड्विंशः कल्पः । इस प्रकार उपासकाध्ययन में अहिंसा का फल बतलाने वाला छब्बीसवाँ कल्प समाप्त हुआ। |