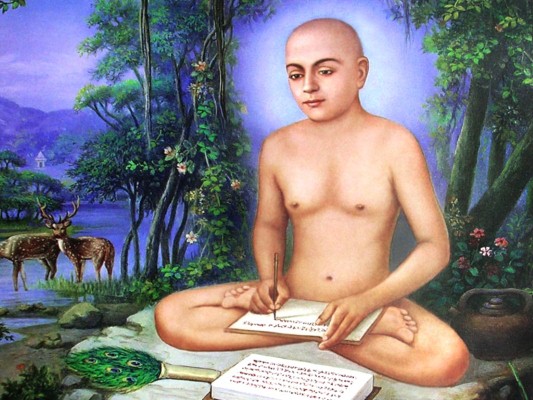


कथा :
सम्यक्त्व प्राप्त विष्णुश्रिय: कथा ततोऽर्हद्दासेन विष्णुश्री: पृष्टा-भो भार्ये! सम्यक्त्वकारणं कथां कथय । सा कथयति स्म । तद्यथा - भरतक्षेत्रे वत्सदेशे कौशाम्बी पुरी । राजाजितञ्जय: तस्य राज्ञी सुप्रभा, राजमंत्री सोमशर्मा, तस्य भार्या सोमा । स मन्त्री सोमशर्मा सर्वदा कुपात्रदानविषये रत: । तस्मिन्नेव नगरे समाधिगुप्तभट्टारक आगत: । तन्नगरबाह्यस्थितोपवनमध्ये मासोपवासस्य प्रतिज्ञा गृहीता तेन । तदतिशयात् तद्वनं सुशोभितं सञ्जातम् । यथाहि - तदनन्तर अर्हद्दास ने विष्णुश्री से कहा - हे प्रिये! सम्यक्त्व प्राप्ति में कारणभूत कथा कहो । वह कहने लगी - भरतक्षेत्र के वत्सदेश में कौशाम्बी नामक नगरी है उसके राजा का नाम अजितंजय, रानी का नाम सुप्रभा, राजमन्त्री का नाम सोमशर्मा और उसकी स्त्री का नाम सोमा था । वह सोमशर्मा मन्त्री सदा कुपात्रदान में तत्पर रहता था । उसी कौशाम्बी नगरी में किसी समय समाधिगुप्त नामक भट्टारक आये । उन्होंने नगरी के बाहर स्थित उपवन के मध्य में मासोपवास की प्रतिज्ञा की । उस अतिशय से वह वन अत्यन्त सुशोभित हो गया । जैसा कि कहा है- शुष्काशोक-कदम्बचूत-वकुला: खर्जुरकादिद्रुमा
अशोक, कदम्ब, आम, मौलश्री तथा खजूर आदि के जो वृक्ष पहले सूख गये थे, वे फूल फल व कोपलों से युक्त हो गये तथा शाखा और उपशाखाओं से व्याप्त हो गये । जिनके कमल सूख गये थे ऐसी जलवापिका आदि जलाशय जल से परिपूर्ण हो गये, उनमें राजहंस पक्षी निरन्तर क्रीड़ा करने लगे और कोकिलाएँ सुन्दर शब्द करने लगीं ॥287॥जाता: पुष्पफलप्रपल्लवयुता: शाखोपशाखाचिता: । शुष्काब्जा जलवापिकाप्रभृव्यो जाता पय:पूरिता: क्रीडन्त्येव सुराजहंसशिखिनश्चक्रु: स्वरं कोकिला: ॥287॥ पुनश्च- और भी कहा है - जातीचम्पक-पारिजातक-जपासत्केतकी-मल्लिका:
चमेली, चम्पा, पारिजात, जपा, उत्तम केतकी, मालती तथा कमलिनी आदि क्षण भर में खिल उठे, उनकी सुन्दर सुगन्ध को सूँघकर भौंरे मधुर शब्द करने लगे और पक्षी परस्पर गाने लगे । इस प्रकार वह वन सुशोभित हो उठा ॥288॥पद्मिन्य: प्रमुखा: क्षणाद्विकसिता: प्रापुद्र्विरेफास्तत: । कुर्वन्तो मधुरं स्वरं सुललितं तद्गन्धमाघ्राय ते गायन्ते विहगा परस्परपरे भातीदृशं तद्वनम् ॥288॥ स तपस्वी कीदृग्विध: ? वे तपस्वी भट्टारक कैसे थे ? साधवस्तु कृपावन्तो भवन्ति पुण्यचेतस: ।
पवित्र चित्त के धारक साधु परम दयालु होते हैं । अपकार करने पर भी वे सदा उपकार ही करते हैं ॥289॥ अपकृतों च सत्यां वै कुर्वन्त्युपकारकं सदा ॥289॥ तद्यथा- और भी कहा है- देहे निर्ममता गुरौ विनतता नित्यं श्रुताभ्यासता
साधु का लक्षण यह है - शरीर में ममता का अभाव, गुरु में नम्रता, निरन्तर शास्त्र का अभ्यास, चारित्र की निर्मलता, अत्यन्त शान्तवृत्ति, संसार से उदासीनता, अन्तर तथा बाह्य परिग्रह का त्याग, धर्मज्ञता और सज्जनता; यह उत्तम साधु का लक्षण है और यह लक्षण उनके संसार का विच्छेद करने वाला है ॥290॥चारित्रोज्जवलता महोपशमता संसार-निर्वेदता । अन्तरबाह्य-परिग्रहत्यजनता धर्मज्ञता साधुता साधो: साधुजनस्य लक्षणमिदं संसारविच्छेदकम् ॥290॥ पुन: परिग्रह: - फिर परिग्रह इस प्रकार है - क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदश्च चतुष्पदम् ।
खेत, मकान, धन, धान्य, दासी-दास आदि द्विपद, गाय, भैंस आदि चतुष्पद, वाहन, शय्या-आसन, वस्त्र और बर्तन; ये दश बाह्य परिग्रह हैं ॥291॥यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डश्चेति बहिर्दश ॥291॥ मिथ्यात्वं वेदहास्यादि षट्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च सङ्गा: स्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥292॥ मिच्छत्तं वेयतिगं हासाई छक्कयं च णायव्वम् । कोहादीण चउक्कं चउदस अब्भंतरा गंथा ॥293॥ मिथ्यात्व, वेद, हास्यादि छह नोकषाय, क्रोधादि चार कषाय, राग और द्वेष; ये चौदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥292॥ यही भाव प्राकृत गाथा में दर्शाया गया है-मिथ्यात्व तीनवेद, हास्यादिक छह नोकषाय और क्रोधादिक की चौकड़ी, ये सब मिलकर चौदह अन्तरंग परिग्रह हैं ॥293॥ प्रतिज्ञानन्तरमेवं गुणविशिष्टं समाधिगुप्तभट्टारकं चर्यार्थमागतं दृष्ट्वा लघुकर्मणा श्रद्धादिसप्तगुण-समन्वितेन, नव-विधान-युक्तेन, सोमशर्म-मन्त्रिणा मुनिप्रतिलम्भतोऽतिमोदमानेन मुनिं प्रतिष्ठाप्य चर्या कारिता । के सप्तगुणा इति चेत्? तद्यथा- प्रतिज्ञा के अनन्तर अर्थात् मासोपवास की प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर इस प्रकार के गुणों से युक्त समाधिगुप्त भट्टारक चर्या के लिए नगर में आये । उन्हें देख, जिसके कर्म अत्यन्त अल्प रह गये थे, जो श्रद्धा आदि सात गुणों से सहित था, नवधाभक्ति से युक्त था और मुनिराज की प्राप्ति से अत्यधिक हर्षित हो रहा था, ऐसे सोंमशर्मा मन्त्री ने पड़गाहन कर आहार कराया । वे सात गुण कौन-से हैं ? यह कहते हैं- श्रद्धा शक्तिरलोभित्वं दयाभक्ति: क्षमा तथा ।
श्रद्धा, शक्ति, निर्लोंभता, दया, भक्ति, क्षमा और विज्ञान; ये दाता के सात गुण माने गये हैं ॥294॥विज्ञानञ्चेति सप्तैते दातु: सप्तगुणा मता: ॥294॥ कश्च विधि:- और विधि क्या है ? यह कहते हैं - पडिगहमुच्चठ्ठाणं पादोदयमच्चणं हु पणमं च ।
पड़गाहन, उच्च स्थान पर विराजमान करना, पैर धुलाना, पूजा करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि का प्रकट करना तथा आहार जल की शुद्धि को बताना; यह नौ प्रकार की विधि है अर्थात् नवधाभक्ति है ॥295॥मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी हु णवविहं पुण्णं ॥295॥ ततो हस्तौ संयोज्य मन्त्री वदति स्म । हे मुने! अद्याहं धन्यो जात: । मयाद्य तीर्थंकरो दृष्ट: पूजितश्च । तथा चोक्तम्- तदनन्तर हाथ जोड़कर मन्त्री ने कहा कि-हे मुनिराज! आज मैं धन्य हो गया । मैंने आज तीर्थंकर को देखा है और उनकी पूजा की । जैसा कि कहा है - सम्प्रत्यस्ति न केवली कलियुगे त्रैलोक्यरक्षामणि: ।
इस समय कलिकाल में तीन लोक के महान् रक्षक केवली भगवान् नहीं है परन्तु भरतक्षेत्र में जगत् को प्रकाशित करने वाली उनकी उत्कृष्ट वाणी चल रही है । रत्नत्रय के धारक उत्तम मुनि उस वाणी के आधारभूत हैं; अत: जिनेन्द्र भगवान् के वचनों के पूज्य होने से वे मुनि पूज्य हैं । उनकी पूजा करने से ऐसा जान पड़ता है मानों साक्षात् जिनेन्द्र भगवान् की ही पूजा की हो ॥296॥तद्वाच: परमाश्चरन्ति भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिका:॥ सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बनं । तत्पूज्या जिनवाक्यपूजनव्या साक्षाज्जिन: पूजित: ॥296॥ मन्त्रिमन्दिरे मुनिदानफलेनामरविरचितानि पञ्चाश्चर्याणि जातानि । भट्टारकदत्ताहारदानफलातिशयं दृष्ट्वा मन्त्री स्वमनसि वदति-अहो, वैष्णवधर्मे यानि दानानि प्रतिपादितानि, तानि सर्वाण्यपि दीक्षिताग्नि- होतृ-श्रोत्रिय- त्रिपटकशासन-धर्मकथक-भागवत-तपस्विवन्दक-यौगीन्द्रादीनामनेकधा दत्तानि मया दानानि । तथा चोक्तम्- मन्त्री के महल में मुनि दान के फलस्वरूप देवों के द्वारा विरचित पञ्चाश्चर्य हुए । मुनिराज को दिये हुए आहारदान के फल का अतिशय देख मन्त्री मन में कहता है कि-अहो! वैष्णव धर्म में जो दान बतलाये गये हैं, वे सब मैंने दीक्षित, अग्निहोत्री, श्रोत्रिय, (वेदपाठी) त्रिपटक शासन, धर्मकथक, भागवत, तपस्वी, वन्दक तथा योगीन्द्र आदि अनेक प्रकार से दिये हैं । जैसा कि कहा है - कनकाश्वतिला नागो रथो दासी मही गृहम् ।
सुवर्णदान, अश्वदान, तिलदान, हस्तिदान, रथदान, दासीदान, पृथ्वीदान, गृहदान, कन्यादान और कपिला गाय का दान; ये दश महादान हैं ॥297॥कन्या च कपिलाधेनुर्महादानानि वै दश ॥297॥ परं तद्दानफलातिशय: कोऽपि नु दृष्टो मया । इत्येवं मनसि निश्चित्यापराह्नसमये स्वस्थानमागतस्य साधो: पार्श्वं गत्वा विधिपूर्वेण भट्टारकं वन्दित्वा तेन भट्टारक: पृष्ट:-भो: भगवन् दीक्षितादिदानफलातिशय: कोऽपि न दृष्टो मया किमिति कारणम्? भगवानाह-भो सचिव! ते दीक्षितादय: कुपात्रा आर्तरौद्रध्यानयुक्ता अत: न पात्रभूता:, तेषां दानानि देयानि न भवन्ति । योऽतिथिरात्मानं यजमानं च तारयति तस्य दानं दातव्यम् । तथा चोक्तम्- परन्तु उन दानों के फल का कुछ भी अतिशय मैंने नहीं देखा है । इस प्रकार का मन में निश्चय कर, अपराह्न समय में जब मुनिराज अपने स्थान पर आये तब उनके पास जाकर तथा विधिपूर्वक नमस्कार कर मन्त्री ने उनसे पूछा-हे भगवन्! दीक्षित आदि को दिये हुए दान के फल का कुछ भी अतिशय मैंने नहीं देखा है, इसका क्या कारण है? मुनिराज ने कहा कि-हे मन्त्री! वे दीक्षित आदि कुपात्र हैं, आर्त और रौद्रध्यान से युक्त हैं अत: पात्र नहीं हैं, उन्हें दान नहीं देना चाहिए । जो अतिथि अपने आपको तथा यजमान को तारता है, उसे ही दान देना चाहिए । जैसा कि कहा है - अवद्यमुक्ते पथि य: प्रवर्तते प्रवर्तयत्यन्यजनञ्च नि:स्पृह: ।
जो पाप रहित मार्ग में स्वयं प्रवर्तता है और नि:स्पृह भाव से दूसरे को भी प्रवर्ताता है, आत्मकल्याण के इच्छुक मनुष्य के द्वारा वही गुरु अपराधनीय है, ऐसा ही गुरु स्वयं तरता है और दूसरे को तारने में समर्थ है ॥298॥स एव सेव्य: स्वहितेच्छुना गुरु: स्वयं तरन् तारयितुं क्षम: परम् ॥298॥ अन्यच्च- और भी कहा है- दानं दातव्यं शीलवद्भ्य: प्रणम्य
स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक मनुष्य को शीलवन्त मुनियों के लिए प्रणाम कर दान देना चाहिए, बन्ध और मोक्ष को दिखलाने वाले ज्ञान को जानना चाहिए तथा राग-द्वेष से रहित देवों की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए ॥299॥ज्ञानं ज्ञातव्यं बन्धमोक्ष-प्रदर्शि । देवा: संसेव्या द्वेषरागप्रहीणा: स्वर्गं मोक्षं गन्तुकामेन पुंसा ॥299॥ उत्तमपात्रमध्यमपात्रजघन्यपात्राणामौषधाभयाहारशास्त्रदानानि यथायोग्यं दातव्यानि । तथा चोक्तम्- उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्रों के लिए यथायोग्य औषध, अभय, आहार और शास्त्र दान देना चाहिए । जैसा कि कहा है- उत्तमपत्तं साहू मञ्झिमपत्तं च सावया भणिया ।
उत्तमपात्र मुनि और मध्यमपात्र श्रावक कहे गये हैं । अविरत-सम्यग्दृष्टि जीवों को जघन्यपात्र जानना चाहिए ॥300॥अविरदसमाइठ्ठी जहण्णपत्तं मुणेयव्वं ॥300॥ पुनश्च- और भी कहा है - उत्कृष्ट-पात्रमनगारमणुव्रताढ्यं
महाव्रत को धारण करने वाले मुनि उत्तमपात्र हैं, अणुव्रत से सहित श्रावक मध्यम पात्र हैं और व्रत से रहित सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र हैं । सम्यग्दर्शन से रहित किन्तु व्रत समूह से युक्त मनुष्य कुपात्र हैं और सम्यग्दर्शन तथा व्रत-दोनों से रहित मनुष्य को अपात्र जानो ॥301॥ मध्यं व्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम् । निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्झितं नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥301॥ अभीतिरभयादाहुराहाराद् भोगवान् भवेत् ।
आरोग्यमौषधाज्ज्ञेयं शास्त्राद्धि श्रुतकेवली ॥302॥ पुनश्चोक्तं चतुर्विधदानफलम्- चतुर्विध दान का फल कहा भी है-अभयदान देने से मनुष्य निर्भय होता है, आहारदान देने से भोग युक्त होता है, औषधदान देने से आरोग्य-नीरोगता प्राप्त होती है और शास्त्रदान देने से श्रुतकेवली होता है ॥302॥ य: पुन: और अपात्रेभ्यो दानं ददाति स आत्मानं पात्रं च नाशयति "भस्मनि हुतमिवापात्रेष्वर्थ व्यय:" इति सोंमनीति: । तथा च- जो अपात्रों को दान देता है वह अपने आपको तथा पात्र को नष्ट करता है क्योंकि सोमदेव के नीति शास्त्र में कहा गया है कि - भस्म में किये हुए होम के समान अपात्रों में किया हुआ धन का व्यय व्यर्थ होता है और भी कहा है - जायते दन्दशूकाय दत्तं क्षीरं यथा विषम् ।
जिस प्रकार साँप के लिए दिया हुआ दूध विष होता है, उसी प्रकार जो दान अपात्र के लिए दिया जाता है, वह विष हो जाता है ॥303॥तथापात्राय यद्दत्तं तद्दानं तद्विषं भवेत् ॥303॥ उप्तं यथोषरे क्षेत्रे बीजं भवति निष्फलम् ।
जिस प्रकार ऊसर खेत में बोया हुआ बीज निष्फल होता है उसी प्रकार अपात्र के लिए दिया हुआ दान निष्फल होता है ॥304॥तथापात्राय यदद्त्तं तद्दानं निष्फलं भवेत् ॥304॥ अन्यच्च और भी कहा है - एकवापीजलं यद्वदिक्षौ मधुरतां व्रजेत् ।
जिस प्रकार एक ही वापिका का जल ईख में मधुरता को प्राप्त होता है और नीम में कडुवापन को प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्र और अपात्र में दिया दान विविध रूपता को प्राप्त होता है ॥305॥निम्बे कटुकतां याति पात्रापात्रेषु योजितम् ॥305॥ एतत् श्रुत्वा पुनरपि मन्त्री पृच्छति स्म-भो भगवन्! यथा मुनिदानफलातिशयो मया प्राप्तस्तथान्येन केनापि मुनिदानफलातिशय: प्राप्तो न वा । ततो भगवानाह-पूर्वं विश्वभूतिद्विजेन यथा लब्धं तथा शृणु । दक्षिणदेशे वराडनगरे राजा सोमप्रभ: । राज्ञी सोमप्रभा । स राजा ब्राह्मणभक्त: । स नित्यं सभामध्योपविष्ट: कथयति-विप्रान् विहायान्य: कोऽपि लोकानां तारको न भवतीति । तथा चोक्तम्- यह सुनकर मन्त्री ने पुन: पूछा-हे भगवन्! जिस प्रकार मुनि दान के फल का अतिशय मैंने प्राप्त किया है, उस प्रकार किसी अन्य ने भी प्राप्त किया है अथवा नहीं । तब भगवान्-मुनिराज बोले कि पहले विश्वभूति ब्राह्मण ने जैसा प्राप्त किया है उसे सुनो । दक्षिण देश के वराड नगर में राजा सोमप्रभ रहते थे । उनकी रानी का नाम सोमप्रभा था । वह राजा ब्राह्मण भक्त था । वह नित्य ही सभा के मध्य बैठकर कहा करता था कि-ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य कोई भी लोगों को तारने वाला नहीं है । जैसा कि कहा है- गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि: सत्यवादिभि: ।
गायों से, ब्राह्मणों से, वेदों से, पतिव्रता स्त्रियों से, सत्य बोलने वालों से, लोभहीन मनुष्यों से तथा दानी पुरुषों से-इन सात के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है-ये सात पृथ्वी के रक्षक हैं ॥306॥अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही ॥306॥ एकदा तेन राज्ञा स्वमनसि विचारितमहो, मया बहुद्रव्यमुपार्जितमस्ति । तस्य द्रव्यस्य दानाद्युपयोगो गृह्यतेऽन्यथा नाश एव भवति । तथा चोक्तम्- एक समय उस राजा ने अपने मन में विचार किया कि अहो ? मैंने बहुत द्रव्य उपार्जित किया है । उस द्रव्य का दान आदि में उपयोग लिया जाता है । अन्यथा उसका नाश ही होता है । जैसा कि कहा है - दानं भोगो नाशस्तिस्रो गव्यो भवन्ति वित्तस्य ।
दान, भोग और नाश, धन की ये तीन गतियाँ हैं जो न दान करता है और न भोगता है उसके धन की तीसरी गति-नाश होती है ॥307॥यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥307॥ किञ्च- और भी कहा है - त्यागो भोगो विनाशश्च विभवस्य त्रयी गति: ।
त्याग, भोग और विनाश, वैभव की ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । जिस पुरुष के आदि की दो अवस्थाएँ नहीं हैं, उसके एक नाश अवस्था ही शेष रहती है ॥308॥द्वे यस्याद्ये न विद्येते नाशस्तस्यावशिष्यते ॥308॥ इति विचार्य विप्रानुमत्या बहुसुवर्णनामा यज्ञ: कारित: । तस्मिन् यज्ञे आदिमध्यावसानेषु विप्राणां बहुसुवर्णं दीयते । यज्ञशालासमीपे विश्वभूतिनाम्नो द्विजस्य गृहं तिष्ठति । स विश्वभूतिर्भोगोंपभोगेषु यमनियमसंयमादियुक्तो नि:स्पृहचित्तश्च बभूव । तस्या भार्या सती । भोगोपभोंगस्वरूपमाह- ऐसा विचार कर ब्राह्मणों की अनुमति से उसने बहु सुवर्ण नाम का यज्ञ करवाया उस यज्ञ के आदि, मध्य और अन्त में ब्राह्मणों के लिए बहुत सुवर्ण दिया जाता है । यज्ञशाला के समीप ही विश्वभूति नामक ब्राह्मण का घर था । वह विश्वभूति भोग और उपभोग के विषय में यम, नियम, रूप, संयम आदि से युक्त तथा निस्पृह चित्त था । उसकी स्त्री पतिव्रता थी । भोग और उपभोग का स्वरूप ऐसा कहा है - य: सकृत् सेव्यते भाव: स भोगो भोजनादिक: ।
जो पदार्थ एक बार सेवन में आता है, वह भोग कहलाता है । जैसे भोजन आदि और जो बार-बार सेवन में आता है, वह परिभोग कहलाता है । जैसे आभूषण आदि ॥309॥भूषादि: परिभोग: स्यात्पौन:पुन्येन सेवनात् ॥309॥ पुनश्च यमनियमौ- यम और नियम का स्वरूप इस प्रकार है - यमश्च नियमश्चेति द्वेत्याज्ये वस्तुनि स्मृते ।
त्यागने योग्य वस्तु के विषय में यम और नियम के भेद से दो प्रकार का त्याग माना गया है । जीवनपर्यन्त के लिए जो त्याग होता है, उसे यम जानना चाहिए और जो समय की अवधि से सहित होता है, वह नियम कहा जाता है ॥310॥यावज्जीवं यमो ज्ञेय: सावधिर्नियम: स्मृत: ॥310॥ एकस्मिन् दिने तेन विश्वभूतिना खलं (धान्यस्थानं) गत्वा कपोतवृत्त्या यवा आनीता: । पेषयित्वा च तच्चूर्णस्य जलेन सह तेन पिण्डचतुष्टयं बद्धम् । एकेन पिण्डेनाग्निहोत्रं कृतवान् । द्वितीयपिण्डं स्वभोजनार्थं धृतम् । तृतीयं पिण्डं स्वभार्या-भोजननिमित्तं धृतम् । चतुर्थं पिण्डमतिथिभोजननिमित्तं धृतम् । एवं विश्वभूते: कालो गच्छति । तथा चोक्तम्- एक दिन वह विश्वभूति अनाज के स्थान स्वरूप खलिहान में जाकर कपोतवृत्ति से अर्थात् दाने बीनकर जो लाया, उन्हें पिसवाकर उसके चूर्ण को जल के साथ उसने चार पिण्ड बाँधे । एक पिण्ड से अग्नि का होम किया, दूसरा पिण्ड अपने भोजन के लिए रख लिया, तीसरा पिण्ड अपनी स्त्री के भोजन के लिए रख लिया और चौथा पिण्ड अतिथि के भोजन के लिए रखा । इस प्रकार विश्वभूति का समय व्यतीत हो रहा था । जैसा कि कहा है- देयं स्तोकादपि स्तोकं न व्यपेक्षा महोदये ।
अपने समीप थोड़ी सम्पत्ति है तो उस थोड़ी सम्पत्ति में से भी थोड़ा भाग दान में देना चाहिए । महान् अभ्युदय-बहुत भारी सम्पत्ति की अपेक्षा नहीं करना चाहिए क्योंकि इच्छानुसार सम्पत्ति कब किसके होती है? ॥311॥इच्छानुकारिणी शक्ति: कदा कस्य भविष्यति ॥311॥ एकस्मिन् दिने विश्वभूतिगृहे पिहितास्रवनामा मुनिश्चर्यार्थमागत: । परमानन्देन यथोक्तागमविधिना विश्वभूतिना प्रतिष्ठापित: । अतिथि-निमित्तं धृतं पिण्डं शोधितम् । स्वनिमित्तं धृतमपि पिण्डं शोधितम् तदनन्तरं भार्यामुखमवलोकितं द्विजेन व्योक्तमिङ्गिताकारज्ञया-धन्याहं तव प्रसादेन । ममापि पुण्यं घटयतु । ममापि घटितं मदीयं पिण्डं दीयतामेव, शोधय । तेन तदपि शोधितम् । तथा चोक्तम्- उस दिन विश्वभूति ब्राह्मण के घर पिहितास्रव मुनि चर्या के लिए आये । परम आनन्द से युक्त उस विश्वभूति ने आगम में कही विधि से उन मुनिराज को पड़गाहना तथा अतिथि के निमित्त जो पिण्ड रख छोड़ा था वह शोधा, पश्चात् अपने लिए रखा हुआ भी शोधा, तदनन्तर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के मुख की ओर देखा । अभिप्राय को जानने वाली स्त्री ने कहा कि - आपके प्रसाद से मैं धन्य हूँ मुझे भी पुण्य मिले, मेरे लिए पिण्ड रख छोड़ा है वह भी दिया जाय । ब्राह्मण ने वह पिण्ड भी शोध लिया । जैसा कि कहा है- वश्या: सुता वृत्तिकरी च विद्या नीरोगता सज्जनसंगतिश्च ।
आज्ञाकारी पुत्र, आजीविका करने वाली विद्या, नीरोगता, सज्जनों की संगति और अनुकूल चलने वाली स्त्री; ये पाँच दु:ख को जड़ से नष्ट करने वाले हैं ॥312॥इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुखस्य मूलोद्धरणानि पञ्च ॥312॥ पश्चात् मुनि दान का माहात्म्य जानकर मन्द कर्मोदय वाले सोमप्रभ राजा ने ब्राह्मणों के आगे ततो मुनेर्निरन्तराय आहारोऽजनि । तत: सुपात्रदानप्रभावात् तद्द्विजगृहे तन्नगरे च रत्नवृष्टि:, कुसुमवृष्टि:, सुगन्धिवायु:, देवदुन्दुभि:, साधुवादश्चेतिपञ्चाश्चर्यं देवै: कृतम् । भट्टारक: स्वस्थानं गत:, लोकैश्च स द्विज: प्रशंसित: । तानीमानि पञ्चाश्चर्याणि- तदनन्तर मुनि का निरन्तराय आहार हो गया । उस सुपात्रदान के प्रभाव से उस ब्राह्मण के घर तथा नगर में रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, सुगन्धित वायु, देवदुन्दुभि और उत्तम शब्द ये पञ्चाश्चर्य देवों ने किये । मुनिराज अपने स्थान पर चले गये । लोगों ने उस ब्राह्मण की बहुत प्रशंसा की । वे पञ्चाश्चर्य ये हैं- सुरजण साहुवकारो गंधोदयरयणपुप्फविठ्ठिओ ।
देवों के द्वारा "बहुत अच्छा-बहुत अच्छा" इस प्रकार के उत्तम शब्द का कहा जाना, गन्धोदक, रत्न और पुष्पों की वर्षा होना तथा दुन्दुभि का शब्द होना, ये पञ्चाश्चर्य जानना चाहिए ॥313॥तह दुन्दुहिणिग्घोसो पंचच्छरिया मुणेयव्वा ॥313॥ गन्धवायुस्ततो वाति वृष्टि: कुसुमरत्नयो: । देवदुन्दुभिनिर्घोष: साधुवाद: सुनिर्मल: ॥314॥ पात्रदान से सुगन्धित वायु बहती है, पुष्प और रत्नों की वृष्टि होती है, देव दुन्दुभियों का शब्द होता है और अत्यन्त निर्मल साधु-साधु शब्द की ध्वनि होती है ॥314॥ तदनन्तरं मिथ्यादृष्टिब्राह्मणैर्भणितम् राज्ञोऽग्रे-हे राजन् बहुसुवर्णयज्ञफलमेतत् । श्रुत्वा राजा संतुष्टो जात: । ततो राज्ञा तुष्टेन ब्राह्मणा: समादिष्टा:-भो द्विजवरा: । यूयमेव रत्नादिकं गृह्वीध्वम् । ततो हृष्टा द्विजा यावदागत्य गृह्वन्ति तावद् रत्नादिकमङ्गाररूपं सर्परूपं च जातम् । पश्चाद् राज्ञा स्वयमेवागत्य विलोकितम् । यदा राजा रत्नादिकं गृह्वाति तदा सर्पाङ्गाररूपं भवति, अन्यथा यथावस्थितम् । तत: केनचिद् विशिष्टे पुरुषेण नृपाग्रे भणितम्-भो भूपते बहुसुवर्ण-यज्ञफलं नैतत् । किं तर्हि? विश्वभूतिब्राह्मणेन मुनिदत्ताहारदानफलमेतत् । ततो मुनिदानमाहात्म्यं ज्ञात्वा लघुकर्मणा सोमप्रभेण राज्ञा ब्राह्मणानां पुरत: कथितम्-भो असत्यवादिनो द्विजा नैतद् यज्ञफलं, किन्तु सुपात्र दान फलं निश्चयव्या ज्ञातव्यमेव । ततोंऽवसरं प्राप्य जिनधर्मानुरक्तमन्त्रिणा कथितम्-हे नरेन्द्र! ये शुद्धभावयुक्तास्त एव दानयोग्या भवन्ति, न पुनरात्र्तरौद्रध्यानपरायणा गृहिणस्तेषां शुभभावाभावात् । तथा चोक्तम्- तदनन्तर मिथ्यादृष्टि ब्राह्मणों ने राजा के आगे कहा - हे राजन्! यह सब-सुवर्ण यज्ञ का फल है । राजा सुनकर संतुष्ट हो गया । पश्चात् संतुष्ट हुए राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी ब्राह्मणों! तुम लोग ही रत्नादिक को ले लों । तदनन्तर हर्षित ब्राह्मण आकर ज्योंही ग्रहण करते हैं त्योंही रत्नादिक अंगाररूप और सर्पादि रूप हो गये । पश्चात् राजा ने स्वयं आकर देखा । जब राजा रत्नादिक को ग्रहण करता तों वे सर्प और अंगाररूप हो जाते और जब ग्रहण नहीं करता तब जैसे थे वैसे हो जाते थे । तदनन्तर किसी विशिष्ट पुरुष ने राजा के आगे कहा - हे राजन्! यह बहुसुवर्ण यज्ञ का फल नहीं है, तो क्या है? यह विश्वभूति ब्राह्मण के द्वारा मुनि के लिए दिये हुए आहारदान का फल है । कहा है - असत्य बोलने वाले ब्राह्मणो! यह यज्ञ का फल नहीं है किन्तु सुपात्रदान का फल है यही निश्चय से जानना चाहिए । तदनन्तर अवसर पाकर जिनधर्म के अनुरागी मन्त्री ने कहा - हे राजन्! जो शुद्धभाव से युक्त हैं वे ही दान के योग्य होते हैं न कि आर्त और रौद्रध्यान में तत्पर रहने वाले गृहस्थ, क्योंकि उनके शुभ-भाव का अभाव रहता है । जैसा कि कहा है- नो शीलं परिपालयन्ति गृहिणस्तप्तुं तपो न क्षमा,
गृहस्थ लोग शीलपालन नहीं करते हैं, वे तप तपने में समर्थ नहीं हैं तथा आर्तध्यान से उज्जवल बुद्धि को नष्ट करने वाले गृहस्थों के शुभ भावना भी नहीं रहती है, इस प्रकार सावधान चित्त से अच्छी तरह विचार कर मैंने हर्षपूर्वक यह निश्चय किया है कि दानरूप आलम्बन के सिवाय संसाररूपी कूप से निकालने वाला दूसरा सुदृढ़ साधन नहीं है ॥315॥आर्तध्याननिराकृतोज्ज्वलधियां तेषां न सद्भावना । इत्येवं निपुणेन हन्त मनसा सम्यङ् मया निश्चितम् नोत्तारो भवकूपतोऽस्ति सुदृढों दानावलम्बात्पर: ॥315॥ अतएव मुनिभ्य: दानं दातव्यं, मुक्ते: कारणं त एव भवन्ति न गृहिण: । तथा चोक्तम्- इसलिए मुनियों को दान देना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के कारण वे ही हैं, गृहस्थ नहीं । जैसा कि कहा है - सन्त: सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं मुक्ते: परं कारणं,
शरीर के रहते हुए सत्पुरुष, समस्त सुरेन्द्र और असुरेन्द्रों के द्वारा पूजित, मुक्ति के उत्कृष्ट कारण तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले रत्नत्रय को धारण करते हैं । उस शरीर की वृत्ति उत्कृष्ट भक्तिपूर्वक दिये हुए जिन गृहस्थों के अन्न से होती है, उन गुणवान गृहस्थों का धर्म किसके लिए प्रिय नहीं है ? अर्थात् सभी के लिए प्रिय है ॥316॥रत्नानां दधति त्रयं त्रिभुवन-प्रद्योति काये सति । वृत्तिस्तस्य यदन्नत: परमया भक्त्यार्पिताज्जायते, तेषां सद्गृहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कस्य प्रिय:॥316॥ तदनन्तर करौ कुड्मलीकृत्य विश्वभूतिद्विजं प्रति राजा भणति-भो पुण्यात्मन् विश्वभूते! त्वं मुनिदत्ता-हारदानफलं ममार्धं प्रयच्छ । मदीयं बहु सुवर्णयज्ञफलार्धं गृहाण । ततो विश्वभूतिनाभाणि-भो राजन्! स्वर्गादिकं येन दानेन साध्यते तद् दानं कथं दीयते ? राज्ञोक्तम्-त्वं दरिद्रोंवाञ्छितमर्थं गृहीत्वा मुनिदत्ताहारदानफलार्धं दीयते । तेन कथितम्-भो भूपते दारिद्र्यपीडितोऽपि सत्पुरुषो नीतिं परित्यक्त्वान्यथा करोति किम्? तथा चोक्तम्- तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर राजा विश्वभूति ब्राह्मण से कहता है कि पुण्यात्मन् विश्वभूति! तुम मुनि को दिये हुए आहारदान का आधा फल मुझे दे दो और मेरे बहु सुवर्ण यज्ञ का आधा फल ले लो । तब विश्वभूति ने कहा - हे राजन्! जिस दान से स्वर्गादिक की सिद्धि होती है वह दान कैसे दिया जा सकता है । राजा ने कहा - तुम दरिद्र हो इसलिए मन चाहा धन लेकर मुनि को दिये हुए आहारदान का आधा फल दिया जा सकता है । उसने कहा - हे राजन्! दारिद्र्य से पीडि़त होने पर भी सत्पुरुष नीति को छोड़कर क्या अन्यथा काम करता है ? अर्थात् नहीं करता । जैसा कि कहा है- क्षुत्क्षामोऽपि तृषार्दितोऽपि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दशा-
मत्त गजराज के विदीर्ण किये हुए गण्डस्थल के ग्रास में जिसकी इच्छा लग रही है, ऐसा अभिमानी जीवों में प्रधान सिंह भले ही भूख से दुर्बल हो रहा हो, प्यास से पीडि़त हो, प्राय: शिथिल हो गया हो, कष्टमय अवस्था को प्राप्त हो रहा हो, कान्ति हीन हो गया हो और प्राण नष्ट हो रहे हों तो भी क्या जीर्ण तृण को खाता है ? ॥317॥मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि । मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भदलनग्रासैकबद्धस्पृह: किं जीर्णं तृणमत्त मानमहतामग्रेसर: केसरी॥317॥ अतएव स्वर्गापवर्गसाधकमहाराभयभैषज्यशास्त्रमितिदान-चतुष्टयं द्रविणार्थं न विक्रीयते । ततो मुनिनाथसमीपे गत्वा राज्ञाभाणि-भो भगवन्! दान चतुष्टयं गृहिणा किमर्थं दीयते यतिनोक्तम्-हे देव! आहारदानं देहस्थित्यर्थं दीयतेऽतएवाहारदानं मुख्यम् । येनाहारदानम् दत्तं तेन सर्वाणि दानानि दत्तानि । तथा चोक्तम्- इसलिए स्वर्ग और मोक्ष के साधक आहार, अभय, औषध और शास्त्र ये चार दान, धन के लिए नहीं बेचे जाते हैं ? पश्चात् मुनिराज के पास जाकर राजा ने कहा - हे भगवन्! गृहस्थ द्वारा चार दान किसलिए दिये जाते हैं ? मुनिराज ने कहा - हे राजन्! आहारदान शरीर की स्थिति के लिए दिया जाता है अतएव आहारदान मुख्य है । जिसने आहारदान दिया; उसने सब दान दिये । जैसा कि कहा है- तुरगशत-सहस्रं गोकुलं भूमिदानं,
एक लाख घोड़े, गायों का समूह, पृथ्वीदान, सुवर्ण और चाँदी के पात्र, समुद्रान्त पृथ्वी और देवांगनाओं के समान करोड़ों कन्याएँ, इन सबका जो दान दिया जाता है परन्तु वह अन्नदान के समान नहीं हैं क्योंकि अन्नदान ही प्रधान है ॥318॥कनकरजतपात्रं मेदिनी सागरान्ता । सुरयुवतिसमानं कोटिकन्या-प्रदानं, न हि भवति समानं त्वन्नदानात्प्रधानात् ॥318॥ किञ्च- और भी कहा है - अन्नदानसमं दानं समतासदृशं तप: ।
अन्नदान के समान दान, समता के समान तप, वीतराग के समान देव और दया के समान धर्म नहीं है ॥319॥वीतरागसमो देवो नास्ति धर्मो दयासम: ॥319॥ अन्नदातुरधस्तीर्थंकरोऽपि कुरुते करम् ।
अन्नदान देने वाले के हाथ के नीचे तीर्थंकर भी अपना हाथ करते हैं अत: अन्नदान की उपमा किस दान से की जाये, कहो ॥320॥तदन्नदानं दानेभ्यो वद केनोपमीयते ॥320॥ औषधदानमपि दातव्यं येन रोगविच्छितिर्भवत्ति । तदौषधदानेन रोग विनाशे सति मुक्ति तपो जपं संयमं च करोति, पुन: कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षं च गच्छति । तथा चोक्तम्- औषधदान भी देना चाहिए क्योंकि उससे रोग का अभाव होता है । उस औषधदान से रोग का नाश होने पर मुनि तप, जप और संयम करता है तथा पश्चात् कर्म क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होता है । जैसा कि कहा है- रोगिणो भैषजं देयं रोगो देहविनाशक: ।
रोगी के लिए औषध देना चाहिए, क्योंकि रोग शरीर को नष्ट करने वाला है, शरीर का नाश होने पर ज्ञान कैसे हो सकता है और ज्ञान के अभाव में निर्वाण नहीं होता है ॥321॥देहनाशे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निर्वृत्ति: ॥321॥ द्वारिका नगरी में श्रीकृष्ण ने एक मुनि के लिए औषधदान दिया था । उस औषधदान के फल से उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया था । द्वारवत्यां वासुदेवेन औषधदानं भट्टारकस्य दत्तं तेनौषधदानफलेन तीर्थंकरनामकर्मोपार्जितमत एवौषधदानमपि दातव्यम् । अभयदानमपि दातव्यम् । य एकं जीव रक्षति स सर्वदा निर्भयो भवति किं पुन: सर्वान् । तथा चोक्तम्- अभयदान देना चाहिए । जो एक जीव की रक्षा करता है वह सदा निर्भय रहता है फिर जो सब जीवों की रक्षा करता है उसका कहना ही क्या है ? जैसा कि कहा है- विधेयं सर्वदा दानमभयं सर्वदेहिनाम् ।
सब जीवों के लिए सदा अभयदान देना चाहिए क्योंकि अभयदान से जीव अन्य भव में निर्भय होता है ॥322॥यतोऽन्यस्मिन्भवे जीवो निर्भयोऽभयदानत: ॥322॥ अन्यच्च- और भी कहा है - यो दद्यात् र्कानं मेरं कृत्ऋां चापि वसुन्धराम् ।
जो मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण अथवा संपूर्ण पृथ्वी देता है और एक प्राणी को जीवनदान देता है उसको उन दानों में फल की समानता नहीं होती है ॥323॥एकस्य जीवितं दद्यात् फलेन न समं भवेत् ॥323॥ गोदानं हिरण्यदानं च भूमिदानं तथैव च ।
जो गोदान, सुवर्णदान, भूमिदान और एक प्राणी को जीवनदान देता है फल की अपेक्षा उसके वे दान समान नहीं होते हैं ॥324॥एकस्य जीवितं दद्यात्फलेन न समं भवेत् ॥324॥ अत्रार्थे यमपालचाण्डालभवदेवकैवर्तयोश्च कथा । जीवदयां विहाय योऽपात्राय दानं ददाति तद्दानं निष्फलं भवेत् सर्पमुख-निक्षिप्त-क्षीरवत् । शास्त्रदानमपि दातव्यं । यतो य: शास्त्रदानं ददाति स सप्ततत्त्व-नव पदार्थषड्द्रव्य-पञ्चास्तिकाय- देवनिश्चयगुरु-निश्चयरत्नत्रयलोकालोकादिस्वरूपं च जानाति । क्रमेण च कर्मक्षयं करोति । तथा चोक्तम्- इस विषय में यमपाल चाण्डाल और भवदेव धीवर की कथा प्रसिद्ध है । जो मनुष्य जीवदया को छोड़कर अपात्र के लिए दान देता है, उसका वह दान साँप के मुख में डाले हुए दूध के समान निष्फल होता है । शास्त्रदान भी देना चाहिए क्योंकि जो शास्त्रदान देता है वह सात तत्त्व, नौ पदार्थ, छहद्रव्य, पाँच अस्तिकाय, देव, निश्चय गुरु, निश्चय रत्नत्रय और लोकालोकादि के स्वरूप को जानता है तथा क्रम से कर्मों का क्षय करता है । जैसा कि कहा है - चतुर्थं शास्त्रदानं च सर्वशास्त्रेषु कथ्यते ।
चौथा शास्त्रदान, सब शास्त्रों में कहा गया है, जिसके द्वारा अज्ञानी पुरुष भी चराचर सहित तीनों लोकों को जान लेता है ॥325॥येन जानाति मूर्खोऽपि त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥325॥ लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुभ्यो दीयते श्रुतम् । व्याख्यायतेऽथवा स्वेन शास्त्रदानं तदुच्यते ॥326॥ क्षेत्रं ज्ञानाङ्क्वराणां निविडतरतमस्काण्डचण्डांशुबिम्बम् व्यापत्तापाम्बुवाह: कुमतमलभवासङ्गगङ्गाप्रवाह: । श्रेय:-श्रीवश्यमन्त्रं शिवपथपथिक-श्रेणि पीयूषसत्रम् । दु:खार्ताम्भोजमित्रो जयति जिनत्तारां सारणि: शास्त्रमेतत् ॥327॥ स्वयं लिखकर अथवा दूसरों से लिखवाकर साधुओं के लिए जो शास्त्र दिया जाता है अथवा स्वयं उसका व्याख्यान किया जाता है, वह शास्त्रदान कहलाता है ॥326॥ यह शास्त्र, ज्ञानरूपी अंकुरों की उत्पत्ति के लिए क्षेत्र है, अत्यन्त सघन अज्ञानान्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्यबिम्ब है, आपत्तिरूपी सन्ताप को नष्ट करने के लिए मेघ है, मिथ्यामतरूपी मैल से उत्पन्न होने वाली आसक्ति को नष्ट करने के लिए गंगा का प्रवाह है, मोक्ष लक्ष्मी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र है, मोक्षमार्ग के पथिक समूह के लिए अमृत का सदावर्त है, दु:ख से पीडि़त मनुष्यरूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य है तथा जिनवाणी को प्रसारित करने वाली नहर है । यह शास्त्र सदा जयवंत रहे ॥327॥ अन्यच्च- और भी कहा है - अन्यस्मिन् भवे जीवो बिभर्ति सकलं श्रुतम् ।
शास्त्रदान के फल से जीव, अन्य भव में समस्त श्रुत को धारण करता है अर्थात् श्रुतकेवली होता है और शास्त्रदान के फल से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥328॥मोक्ष-सौख्यमवाप्नोति शास्त्रदानफलान्नर:॥328॥ अन्यदपि ज्ञानसंयमोपकरणदानादिमुनिभ्यो देयम् । एतत् सर्वफलं दृष्ट्वा श्रुत्वा च सोमप्रभेण राजा भणितम्-भो मुनिनाथ । मम जैनव्रतं प्रयच्छ । मुनिना जैनव्रतं दत्तम् । तेन स्वीकृतम् । तदा जैनो भूत्वा राजा वदति- भो भगवन्! कीदृग्विधं दानं दातव्यं, कस्मै कस्मैच दातव्यम्? मुनिनोक्तम्-आगमोक्त-विधिना दानं दातव्यम् । तथा चोक्तम्- मुनियों के लिए उपर्युक्त चतुर्विधदान के सिवाय ज्ञान तथा संयम के उपकरण शास्त्र, पिच्छिका, कमण्डलु आदि भी देना चाहिए । इस समस्त फल को देख और सुनकर सोमप्रभ राजा ने कहा - हे मुनिराज! मुझे जैनव्रत दीजिए । मुनि ने जैनव्रत दिये और उन्होंने स्वीकृत किए । उस समय जैन होकर राजा कहता है कि हे भगवन्! कैसा दान देने योग्य है ? और किस-किसके लिए दिया जाना चाहिए । जैसा की कहा है - न दद्याद्यशसे दानं न भयान्नोपकारिणे ।
धर्मात्मा पुरुषों को यश के लिए दान नहीं देना चाहिए, न भय से देना चाहिए, न प्रत्युपकार करने वाले के लिए, न नृत्य-गान आदि करने वालों के लिए और न हँसाने वाले विदूषक आदि के लिए देना चाहिए अर्थात् ये दान के अपात्र हैं ॥329॥न नृत्यगीतशीलेभ्यो हासकेभ्यश्च धार्मिक:॥329॥ पुन: और भी कहा है- यथाविधि यथादेशं यथाद्रव्यं यथागमम् ।
गृहस्थों को विधि के अनुसार, देश के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, आगम के अनुसार, पात्र के अनुसार तथा समय-ऋतु के अनुसार दान देना चाहिए ॥330॥यथापात्रं यथाकालं दानं देयं गृहाश्रमै: ॥330॥ कीदृग्विधं दानमुनिभ्यो दातव्यम्? शृणु तथा च- कैसा दान मुनियों को देना चाहिए । सुनो-जैसा कि कहा है -- विवर्णं विरसं विद्धमसात्म्यं प्रसृतं च यत् ।
जो विवर्ण हो-जिसका वर्ण बदल गया हो, विरस हो-जिसका स्वाद बदल गया हो, घुना हो, अहितकर हो, इधर-उधर फैला हो और खाने पर रोग उत्पन्न करने वाला हो । ऐसा अन्न मुनियों के लिए नहीं देना चाहिए ॥331॥मुनिभ्योऽन्नं न तद्देयं यच्च भुक्तं गदावहम् ॥331॥ उच्छिष्टं नीचलोकार्हमन्योद्दिष्टं विगर्हितम् ।
जो जूठा हो, नीच लोगों के योग्य हो, अन्य लोगों के उद्देश्य से बनाया गया हो, निन्दनीय हो, दुर्जनों के द्वारा छुआ गया हो तथा यक्ष आदि देवों के लिए संकल्पित हो, दूसरे गाँवों से लाया गया हो, मन्त्र द्वारा बुलाया गया हो, कहीं से भेंट में आया हो, बाजार से खरीदा हो, प्रकृति के विरुद्ध हो और ऋतु के अनुकूल न हो, ऐसा आहार मुनियों के लिए नहीं देना चाहिए ॥332-333॥न देयं दुर्जन-स्पृष्टं देवयक्षादि-कल्पितम् ॥332॥ ग्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम् । न देयमापणक्रीतं विरुद्धं वाप्यथाऽर्तुकम् ॥333॥ बालानुग्रतप:क्षीणान् वृद्धान् व्याधि समन्वितान् । मुनीनुपचरेन्नित्यं यतस्ते स्युस्तप:क्षमा: ॥334॥ जो बालक हैं, कठिन तप से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो वृद्ध हैं और बीमारी से पीडि़त हैं, ऐसे मुनियों की निरन्तर वैयावृत्य करना चाहिए जिससे तप करने में समर्थ हो जावें ॥334॥ कृपादानं च सर्वेषामपि दातव्यम् । एतत्सर्वं श्रुत्वा सोमप्रभो राजातीव परिणत: श्रावको जात: । तथाहि- इन दोनों के अतिरिक्त दयादान सभी के लिए देना चाहिए । यह सब सुनकर राजा अत्यन्त सुदृढ़ परिणामी श्रावक हो गया । जैसा कि कहा है- श्रद्धालु र्भक्ति संपन्नो नित्यं षट्कर्मतत्पर: ।
श्रद्धालु, भक्ति सहित, निरन्तर छह कर्मों के पालन करने में तत्पर श्रुत-स्वाध्याय, शील, तप, दान तथा जिनपूजा करने में तत्पर हो गया ॥335॥श्रुतशीलतपोदानजिनपूजासमुद्यत: ॥335॥ जैसा कि कहा है - मिथ्यादृष्टिसहस्रेभ्यो परमेको जिनाश्रित: ।
हजारों मिथ्यादृष्टियों की अपेक्षा एक जैन अच्छा है और हजारों जैनों की अपेक्षा एक श्रावक अच्छा है ॥336॥जिनाश्रित-सहस्रेभ्यो वरमेको उपासक: ॥336॥ श्रावकाणां सहस्रेभ्यो वरमेको ह्यणुव्रती । अणुवती-सहस्रेभ्यो वरमेको महाव्रती ॥337॥ महाव्रति-सहस्रेभ्यो वरमेको जिनागमी । जिनागमिसहस्रेभ्यो वरमेक: स्वतत्त्ववित् ॥338॥ हजारों श्रावकों की अपेक्षा एक अणुव्रती अच्छा है और हजारों अणुव्रतियों की अपेक्षा एक महाव्रती अच्छा है ॥337॥ हजारों महाव्रतियों की अपेक्षा एक जिनागम का ज्ञाता अच्छा है और हजारों जिनागम के ज्ञाताओं की अपेक्षा एक आत्मतत्त्व को जानने वाला अच्छा है ॥338॥ स्वतत्त्ववित्सहस्रेभ्यो वरमेको दयान्वित: ।
हजारों आत्मतत्त्व को जानने वालों की अपेक्षा एक दया सहित मनुष्य अच्छा है क्योंकि दया सहित मनुष्य के समान अन्य मनुष्य न हुआ है और न होगा ॥339॥दयान्वितसमो यावन्न भूतो न भविष्यति ॥339॥ वशीकृतेन्द्रियग्राम: कृतज्ञो विनयान्वित: । निष्कषाय: प्रशान्तात्मा सम्यग्दृष्टिर्महाशुचि:॥340॥ जिसने इन्द्रियों के समूह को वश में कर लिया है, जो कृतज्ञ है, विनय से सहित है, जो कषाय रहित है, जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त है तथा जो सम्यग्दृष्टि है वह महापवित्र है ॥340॥ एवमादि गुणोपेत: सोमप्रभो राजा राज्यं त्यक्त्वा कालक्रमेणोग्रं तप: कृत्वा संयमं प्रपाल्यान्त: सुखी जात: । तथाहि- इत्यादि गुणों से सहित सोमप्रभ राजा, राज्य छोड़कर, कालक्रम से उग्र तपश्चरण कर तथा संयम का पालन कर अन्तरंग में सुखी हो गया । जैसा कि कहा है- प्राप्तश्चानशनं प्रान्ते कृत्वा स्वकर्मणां क्षयम् ।
वह अन्त समय अनशन को प्राप्त हो तथा कर्मों का क्षयकर कालक्रम से समीचीन ध्यान से मरकर परम पद को प्राप्त हुआ ॥341॥कालक्रमेण सद्ध्यानात् मृत्वागात्परमं पदम् ॥341॥ विश्वभूति भी समस्त सुखों को प्राप्त हो गया । विश्वभूतिरपि सर्वसौख्यभाक् समजनि । एतत्सर्वं विश्वभूतिदृष्टान्तं श्रुत्वा सोमशर्मा मन्त्री भणति-भो भगवन्! सम्प्रति मम तव पादौ शरणम् । अतो जिनधर्मे दीक्षायितुं प्रसादं कुरु । एतद्वचनं श्रुत्वा मुनिना दर्शनपूर्वकं श्रावक व्रतं दत्तम् । गृहीत-श्रावकव्रतो मन्त्री साधु विज्ञापयति-हे मुनिवर ममेह जन्मनि लोहायुधाधरणे नियमो दीयताम् । ततो मुनिनां दत्तो नियम: । नियमस्थिरीकरणाय प्रशंसितश्च । ततो मन्त्री मुनिं नत्वा गृहमागत: । तत: प्रभृति शुद्धं श्राद्धधर्मं पालयतस्तस्य मन्त्रिण: कालो गच्छत्येव । एवं बहुकालो जात: । एकदा केनचिद् दुष्टेन राज्ञोऽग्रे निरूपितम्-हे देव! सोमशर्मा मन्त्री काठखङ्गेन तव सेवां करोति, रिपुसंकटे लोहप्रहरणं विना संग्रामे कथं सुभटान् मारयति । अतएव देव तव भक्तो न भवत्यसौ सोमशर्मा । तथा चोक्तम्- यह सब विश्वभूति का दृष्टान्त सुनकर सोमशर्मा मन्त्री कहता है-हे भगवन्! इस समय मुझे आपके चरणों की ही शरण है इसलिए अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रसन्न होइये । यह वचन सुनकर मुनि ने उसे सम्यग्दर्शन पूर्वक श्रावक का व्रत दिया । श्रावक के व्रत को ग्रहण करने वाला मन्त्री मुनिराज से कहता है कि-हे मुनिवर! मुझे इस जन्म में लोहे का शस्त्र न धारण करने का नियम दीजिये । तदनन्तर मुनि ने उसे नियम दे दिया और नियम में स्थिर रहने के लिए उसकी प्रशंसा भी की । तदनन्तर मन्त्री, मुनि को नमस्कार कर घर आ गया । उस समय से शुद्ध श्रावक धर्म का पालन करते हुए मन्त्री का काल व्यतीत होने लगा । इस तरह उसका बहुत काल बीत गया । एक दिन किसी दुष्ट ने राजा के आगे कहा - हे देव! सोमशर्मा मन्त्री काठ की तलवार से तुम्हारी सेवा करता है । शत्रु का संकट उपस्थित होने पर लोहे के शस्त्र बिना संग्राम में योद्धाओं को किस प्रकार मारेगा ? इसलिए हे देव! यह सोमशर्मा तुम्हारा भक्त नहीं है । कहा भी है- त्यक्त्वापि निजप्राणान्परसुखविघ्नं खल: करोत्येव ।
दुष्ट मनुष्य अपने प्राण छोड़कर भी दूसरे के सुख में विघ्न करता है क्योंकि भोजन के ग्रास में पड़ी हुई मक्खी भोजन करने वाले को शीघ्र ही वमन करा देती है ॥342॥पतिता कवले सद्यो वमयति खलु मक्षिका हि भोक्तारम् ॥342॥ एतद् दुष्टवचनं श्रुत्वा स्वमनसि धृत्वा गंभीरव्या राजा तूष्णीं स्थित: । एकदा सभा स्थिते राज्ञा कृपाणवात्र्ता चालिता । तत: कोशात् निष्कास्य रत्नजटित-निज-कृपाणो राज्ञा समस्त कुमाराणामग्रे दर्शित: । तै राजपुत्रै: प्रशंसित: । तत: सभ्यै: स्वस्वप्रहरणं दर्शितम् । एवं राज्ञा समस्त राजकुमाराणां कृपाणान् दृष्ट्वा सोमशर्माणं मन्त्रिणं प्रति भणितम्-भो मन्त्रिन्! निजकृपाणं ममाग्रे दर्शय । तद्राजप्रश्नमिङ्गिताकारेण सकारणं मत्वा मन्त्रिणा स्वमनसि चिन्तितम्-अहो दुष्ट व्यापारोऽयं जात: । अन्यथा कथं मम कृपाण परीक्षां राजा करोति । तथा चोक्तम्- राजा, दुष्ट का यह वचन सुन गम्भीरता के कारण अपने मन में रखकर चुप रह गया । एक समय जब राजा सभा में बैठा हुआ था, तब उसने तलवार की बात चलाई । पश्चात् राजा ने म्यान से निकाल कर अपनी रत्नजटित तलवार समस्त कुमारों के आगे दिखलायी । राजकुमारों ने उस तलवार की प्रशंसा की । इसके बाद सब सभासदों ने अपना-अपना शस्त्र दिखाया । इस प्रकार समस्त राजकुमारों की तलवारें देखकर राजा ने सोमशर्मा मन्त्री से कहा - हे मन्त्रीजी! तुम भी अपनी तलवार मेरे आगे दिखलाओ । राजा के हृदय की चेष्टा तथा मुखाकृति से राजा के उस प्रश्न को कारण सहित मानकर अपने मन में विचार किया-अहो! यह किसी दुष्ट की चेष्टा है अन्यथा राजा मेरी तलवार की परीक्षा क्यों करता ? कहा भी है- उदीरितोऽर्थ: पशुनापि गृह्यते
प्रकट किया हुआ अर्थ पशु भी समझ लेता है प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी भी भार वहन करते हैं परन्तु पण्डित जन बिना कही बात को भी समझ लेते हैं । वास्तव में दूसरे के अभिप्राय को जान लेना ही बुद्धि का फल है ॥343॥हयाश्च नागाश्च वहन्ति नोदिता: । अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन: परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धय: ॥343॥ ततो मन्त्री देवं गुरं च स्वमानसे स्मृत्वा भणति स्वमनसि-यदि मम देवगुरुनिश्चयोऽस्ति तह्र्ययं कृपाणो लोहमयो भवतु । एवं संप्रधार्य सकोशोऽसिस्तेन राज्ञो हस्तेऽर्पित: । कोशात्कृपाणं राजा यदा निष्कासयति तदादित्यवद् देदीप्यमानो लोहमयो विलोकित: । ततो दुष्टमुखमवलोक्य राजा वदति-रे दुष्टात्मन् ! ममाग्रेऽप्यन्यथा निरूपितं त्वया । अहो! दुष्टस्वभावोऽयं परावगुणं कथयितुम् । राजा कुपित:, तदा मन्त्रिणोक्तम्-भो राजन्! राजा देवतास्वरूपस्तस्याग्रे यथा तथा कदाचिदपि न वक्तव्यम् । तथा चोक्तम्- तदनन्तर अपने मन में देव और गुरु का स्मरण कर मन्त्री ने अपने हृदय में कहा - यदि मुझे देव और गुरु का निश्चय है तो यह तलवार लोह निर्मित हो जाये । ऐसा विचार कर उसने म्यान सहित तलवार राजा के हाथ में सौंप दी । जब राजा म्यान से तलवार निकालता है तब वह सूर्य के समान चमकती हुई लोह निर्मित देखी गई । पश्चात् राजा ने दुष्ट के मुख की ओर देखकर कहा - अरे दुष्ट हृदय! मेरे आगे भी तूने झूठ कहा । दूसरे के अवगुण कहना-यह दुष्ट का स्वभाव है । राजा ने उसके प्रति क्रोध प्रकट किया । तब मन्त्री ने कहा - हे राजन्! राजा देवता स्वरूप है इसलिए उसके आगे जैसा तैसा कभी नहीं कहना चाहिए । जैसा कि कहा है- सर्वदेवमयो राजा वदन्ति विवुधा जना: ।
राजा समस्त देवतामय है ऐसा विद्वान् जन कहते हैं इसलिए उसको देव के समान देखना चाहिए, उसके साथ असत्य व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए ॥344॥तस्मात्तं देववत्पश्येत् न व्यलीकेन जातुचित् ॥344॥ किन्तु कारणमस्ति । अतएवास्योपरि कोपं मा कुरु । एतेन यदुक्तं तत् सर्वं सत्यमेव । राज्ञोक्तम्-अहो! सत्पुरुषोऽयम् अपकारिण्यपि पुरुषे शुभं चिन्व्यति । धिक् तं गुणकारिण्यप्यशुभं चिन्व्यति य: । तथाचोक्तम्- परन्तु इसके कहने में कारण है इसलिए इस पर क्रोध मत कीजिए । इसने जो कुछ कहा है वह सत्य ही है । राजा ने कहा - अहो, यह सत्पुरुष है क्योंकि अपकारी पुरुष का भी भला विचारता है । उसे धिक्कार हो जो उपकारी पुरुष का भी बुरा सोचता है । जैसा कि कहा है- अपकर्तर्यपि सन्त: शुभानि कर्माणि कर्तुमीहन्ते ।
सज्जन मनुष्य, अपकार करने वाले का भी भला करने की चेष्टा करते हैं । उस पुरुष को धिक्कार है कि जो सदा उपकार करने वाले का भी बुरा करता है ॥345॥धिक् तं पुरुषं सदोपकर्तरि यो योजयत्यशुभम् ॥345॥ विध्वस्तपरगुणानां भवति खलानामतीव निपुणत्वम् ।
दूसरे के गुणों को नष्ट करने वाले दुर्जनों की बड़ी चतुराई है क्योंकि अपने भीतर चन्द्रमा की किरणों को छिपाने वाले मेघों की भी अधिक मलिनता देखी जाती है ॥346॥अन्तरितशशिरुचामपि सलिलमुचां मलिनताभ्यधिका ॥346॥ दाता दत्ते गुणज्ञेऽर्थमदाता तं निषेधयेत् । राजकीयो वरो याति भाण्डागारी हि दुर्बल: ॥347॥ साधुर्धर्मधुरां धत्ते दोषं वदति दुर्जन: । धनी दोग्धि यतो धेनुं हस्तौ स्पृशति तस्कर: ॥348॥ दानी मनुष्य, गुणी मनुष्य के लिए धन देता है और अदानी मनुष्य उसे मना करता है । ठीक ही है क्योंकि राजा का धन जाता है परन्तु भण्डारी दुर्बल होता है ॥347॥ साधु पुरुष धर्म का भार धारण करता है और दुर्जन उसके दोष कहता है क्योंकि धनी मनुष्य गाय को दुहता है और चोर उसके हाथ पकड़ता है ॥348॥ पुनरपि राजा ब्रुते-भो सचिव! काठमयोऽयं कृपाणो लोहतामापन्न: कथं जात: मन्त्रिणा विज्ञप्तम्- भो नरेन्द्र! मया सत्पात्रदानातिशयं श्रुत्वा दृष्ट्वा च लोहदोषान् लोहप्रहरणे नियमो गृहीत: । तत्प्रभृत्यहं काठकृपाणं वहामि । साम्प्रतं धर्मप्रभावात् लोहमयो जात: । विचित्रं हि धर्ममाहात्म्यम् । तथा चोक्तम्- राजा ने फिर भी कहा - हे मन्त्री जी! यह लकड़ी की तलवार लोहमय कैसे हो गयी ? मन्त्री ने कहा - हे राजन्! मैंने सत्पात्र के लिए दिये हुए दान का अतिशय सुनकर तथा लोहे के दोष देखकर लोहे के शस्त्रों का नियम कर लिया था । उस समय से मैं काठ की तलवार धारण कर रहा हूँ । आज धर्म के प्रभाव से लोहे की हो गई है क्योंकि धर्म की महिमा विचित्र है । जैसा कि कहा है - धर्मो दुर्गतिसंगतिव्यतिकरव्याघातघोराशनि-
धर्म, दुर्गतियों की संगति कराने वाले व्यापार को नष्ट करने के लिए भयंकर वज्र है । धर्म, अनुपम दु:खरूपी दावानल को ज्वालाओं के समूह को बुझाने के लिए मेघ है । धर्म, प्राणियों को सुख देने वालों का दायित्व रखने वालों में प्रधान है और धर्म, मुक्तिरूपी स्त्री को मिलाने वाले कार्यों में बद्धादर है-तत्पर है ॥349॥र्धर्मो नि:समदु:खदावदहनज्वालावली-वारिद: । धर्म: शर्म-समर्पण-प्रतिभुवामग्रेसर: प्राणिनां । धर्म: सिद्धिपुरन्ध्रिसन्धिघटनव्यापारबद्धादर: ॥349॥ अतएव ममोपरि क्षमां कुरु । इति श्रुत्वा राज्ञा लोकैश्च मन्त्री प्रशंसित: पूजितश्च । देवैरपि पञ्चाश्चर्याणि कृत्वा मन्त्री पूजित: । तथा चोक्तम्- अतएव मेरे ऊपर क्षमा करो, यह सुन राजा तथा अन्य लोगों ने मन्त्री की प्रशंसा कर उसका सम्मान किया । देवों ने भी पंचाश्चर्य कर मन्त्री की पूजा की । जैसा कि कहा है- शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे-गजे ।
प्रत्येक पर्वत में माणिक्य नहीं होते, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते, सर्वत्र सज्जन नहीं होते और प्रत्येक वन में चन्दन नहीं होता है ॥350॥साधवो नैव सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥350॥ उपकारिषु य: साधु: साधुत्वे तस्य को गुण: ।
जो उपकारी जनों के विषय में साधु है उसके साधुपन में क्या गुण है ? जो अपकारी जनों के विषय में साधु है परमार्थ से विद्वानों द्वारा वही साधु कहा जाता है ॥351॥योऽपकारिषु साधु: स्यात् स साधु: कथ्यते बुधै: ॥351॥ दुर्जनवचनाङ्गारैर्दग्धोऽपि न विप्रियं वदत्यार्य: ।
सज्जन पुरुष, दुर्जनों के वचनरूपी अंगारों से दग्ध होता हुआ भी विरुद्ध नहीं बोलता है क्योंकि अगुरु चन्दन जलता हुआ भी अपनी स्वाभाविक गन्ध नहीं छोड़ता है ॥352॥अगुरुर्न दह्यमान: स्वभावगन्धं परित्यजति ॥352॥ एतत्सर्वं धर्ममाहात्म्यं दृष्ट्वा श्रुत्वा चाजितञ्जयो राजा लोकाग्रे निरूपयति-अहो लोका! जिनधर्मं विहायान्यो धर्मोदुर्गतिं न विदारयति । अस्मिन् भवेऽपि सुखं नास्ति । इत्येव धर्मप्रभावं भणित्वा वैराग्यपरायणेन राज्ञा स्वपुत्रं शत्रुञ्जयं राज्ये संस्थाप्य, सोमशर्मा मन्त्रिणा स्वपुत्रं देवशर्माणं, मन्त्रिपदे संस्थाप्य च बहुभिरन्यैर्जनै: सार्धं समाधिगुप्तभट्टारकसमीपे तपो गृहीतम् । केचन श्रावका जाता:, केचन भद्रपरिणामिनश्च बभूवु: । राह्या सुप्रभया, मन्त्रिभार्यया सोमया, अन्याभिश्च बह्वीभि: स्त्रीभिरभयमत्यार्यिकासमीपे तपो गृहीतम् । काश्चन श्राविका जाता: । विष्णुश्रिया भणितम्-भो स्वामिन्! एतन्मया सर्वमपि प्रत्यक्षेण दृष्टम् । तदनन्तरं मम दृढतरं सम्यक्त्वं जातम् । एतत्कथानकं श्रुत्वार्हद्दासेनोक्तम्- भो भार्ये! यत्त्वया दृष्ट: तत्सर्वमहं श्रद्दधामि, इच्छामि, रोचे अन्याभिश्च तथैव भणितम् । कुन्दलव्योक्तम्-एतत्सर्वमसत्यमतएव नाहं श्रद्धामि, नेच्छामि, न रोचे । एतद्- वृत्तान्तं राज्ञा मन्त्रिणा चौरेण च श्रुत्वा स्वमनसि भणितम्-विष्णुश्रिया प्रत्यक्षेण दृष्टं, तत्कथमियं पापिठा धर्मफलं व्यलीकमिति निरूपयति । प्रभातसमये गर्दभे चाटयित्वास्या निग्रहं करिष्यामो वयम् । पुनरपि चौरेण स्वमनसि चिन्तितम् । अहो, खलो जात्युत्तमोऽपि सन् स्वभावं न त्यजति । तथा चोक्तम्- यह सब धर्म का माहात्म्य देख व सुनकर अजितंजय राजा ने कहा - अरे मनुष्यों! जैनधर्म को छोड़कर अन्य धर्म दुर्गति को नष्ट नहीं करता है तथा अधर्म से इस भव में भी सुख नहीं होता है । इस प्रकार धर्म का प्रभाव कहकर वैराग्य में तत्पर रहने वाले राजा ने अपने पुत्र शत्रुञ्जय को राज्य पर और सोमशर्मा मन्त्री ने अपने पुत्र देवशर्मा को मन्त्रिपद पर आरूढ़ कर अन्य अनेक जनों के साथ, समाधिगुप्त भट्टारक के समीप तप ग्रहण कर लिया । कोई श्रावक हुए और कोई भद्रपरिणामी हुए । रानी सुप्रभा और मन्त्री की स्त्री सोमा ने अन्य बहुत स्त्रियों के साथ अभयमती आर्यिका के समीप तप ले लिया और कितनी ही स्त्रियाँ श्राविकायें हो गयीं । विष्णुश्री ने अर्हद्दास सेठ से कहा - हे स्वामिन्! यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है । उसके बाद ही मेरा सम्यक्त्व दृढ़ हुआ है । यह कथा सुनकर अर्हद्दास ने कहा - हे प्रिये! तुमने जो देखा है उसकी मैं श्रद्धा करता हूँ, उसे चाहता हूँ और उसकी रुचि करता हूँ । अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा ही कहा । परन्तु कुन्दलता ने कहा - यह सब असत्य है इसलिए मैं न श्रद्धा करती हूँ, न इसे चाहती हूँ और न इसकी रुचि करती हूँ । यह वृत्तान्त राजा, मन्त्री और चोर ने सुनकर अपने मन में कहा - विष्णुश्री ने जिसे प्रत्यक्ष देखा है उस धर्म के फल को यह पापिनी झूठ क्यों कहती है ? प्रात:काल गधे पर चढ़ा कर हम इसका निग्रह करेंगे । चोर ने फिर भी अपने मन में विचार किया-अहो! दुष्टपुरुष, जाति का उत्तम होने पर भी स्वभाव को नहीं छोड़ता है । जैसा कि कहा है - चन्दनादपि संभूतो दहत्येव हुताशन: ।
चूँकि चन्दन से भी उत्पन्न हुई अग्नि जलाती ही है इसलिए जो दुर्जन है वह विशिष्ट कुल में उत्पन्न होने पर भी दुर्जन ही रहता है ॥353॥विशिष्ट-कुलजातोऽपि य: खल: खल एव स: ॥353॥ यस्त्वेतस्माद्विपरीत: साधु: स मलिनकुलोद्भूतोऽपि लोकोत्तर महिमानमादधाति । तथा चोक्तम्- और इससे विपरीत जो सज्जन है वह नीच कुल में उत्पन्न होकर भी श्रेठ महिमा को धारण करता है । जैसा कि कहा है - जन्मस्थानं न खलु विमलं वर्णनीयो न वर्णो
कस्तूरी का जन्म स्थान निर्मल नहीं है, वर्ण भी प्रशंसनीय नहीं है और शरीर में लगाने पर शोभा तो दूर रही कीचड़ की शंका उत्पन्न करती है । यद्यपि यह ऐसी है तथापि समस्त सुगन्धित पदार्थों के गर्व को हरने वाली है । कौन जानता है कि कस्तूरी की सार वस्तु उसका सुगन्धि गुण है ॥354॥दूरे शोभा वपुषि निहिता पङ्कशङ्कां तनोति । यद्यप्येवं सकल-सुरभि - द्रव्यगर्वापहारी को जानीते परिमलगुणो वस्तु कस्तूरिकाया: ॥354॥ ॥इति चतुर्थी कथा॥ ॥ इस प्रकार चौथी कथा समाप्त हुई॥ |