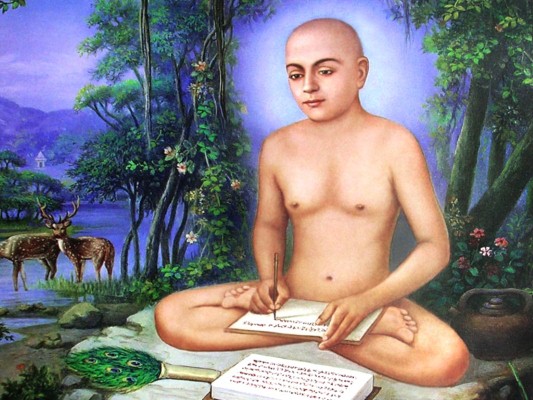


कथा :
सम्यक्त्व प्राप्त नागश्रिय: कथा ततो नागश्रियं प्रति श्रेष्ठिना भणितम्-भो भार्ये! स्वसम्यक्त्वग्रहणकारणं कथय । सा कथयति- काशीविषये वाराणस्या पुरि सोमवशोद्भूतो राजा जितारि:, राज्ञी कनकचित्रा, पुत्री मुण्डिका । सा मुण्डिका प्रतिदिनं मृत्तिकां भक्षयति । शनै: शनैरतिरोग-ग्रस्ता बभूव । राजमन्त्री सुदर्शनो भार्या सुदर्शना । एकदा वृषभश्रियार्यिकया सा मुण्डिका प्रतिबोध्य जैनी कृता । सत्पुरुषाणां स्वभावोऽयं यत् परोपकारं करोति । तदनन्तरं निरतिचारं श्रावकव्रतं पालयन्ती मुण्डिका व्रतमाहात्म्येन नीरोगा रूपवती च जाता । तदार्यिकयोक्तम्-हे पुत्रि । यो निरवद्यं व्रतं पालयति स स्वर्गापवर्गभाजनं भवति रूपस्य नीरोगस्य च का वार्ता? ततो व्रतमाहात्म्यं श्रुत्वा विशेषतो धर्मे सादरा जाता । एकदा जितारिणा राज्ञा नीरुजां पुत्रीं दृष्ट्वा विवाहनिमित्तं राजकुमारा आहूता: । पुत्र्या अग्रे विवाहार्थं सर्वेऽपि राजकुमारा दर्शिता: स्वयंवरे । परं तस्या मनसि कोऽपि न प्रतिभासते स्म । ततो राजपुत्रा: स्वस्थानं जग्मु: । एकदा तुण्डविषये चक्रकोटनाम्नि नगरे राजा भगदत्तो दानशूरो रूपलावण्यादिगुणोपेत: समस्तवस्तुपरिपूर्ण:, परन्तु जातिहीन: । तस्य राज्ञी लक्ष्मीमति:, मन्त्री सुबुद्धि: तस्य भार्या गुणवती । तेन भगदत्तेन सा मुण्डिका याचिता । जितारिणाऽभाणि-रे कुजन्मन्! या जात्यसुतोत्तमराजपुत्रेभ्यो न दत्ता, भगदत्त! दासी-पुत्रस्य तव पापिठस्य कथं तां पुत्रीं दास्यामि? तेनोक्तम्-भो राजन्! गुणेन भवितव्यम्, किं जन्मना? तथा चोक्तम्- तदनन्तर सेठ ने नागश्री से कहा कि-हे प्रिये! तुम अपने सम्यक्त्व प्राप्ति का कारण कहो । वह कहने लगी - काशीदेश की वाराणसी नगरी में सोमवंशीय राजा जितारि रहता था, उसकी रानी का नाम कनकचित्रा था और पुत्री का नाम मुण्डिका था । वह मुण्डिका प्रतिदिन मिट्टी खाती थी जिससे धीरे-धीरे अत्यधिक रोग से ग्रस्त हो गयी । राजा के मन्त्री का नाम सुदर्शन था और उसकी स्त्री का नाम सुदर्शना था । एक समय वृषभश्री आर्यिका ने सम्बोधित कर मुण्डिका को जैनी बना लिया । सत्पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे परोपकार करते हैं । तदनन्तर निरतिचार श्रावक के व्रतों का पालन करती हुई मुण्डिका व्रत के माहात्म्य से निरोग तथा रूपवती हो गयी । उस समय आर्यिका ने कहा कि - हे पुत्रि! जो निर्दोष व्रत का पालन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष का पात्र होता है, रूप और नीरोगता की क्या बात है ? तत्पश्चात् व्रत का माहात्म्य सुनकर वह विशेष रूप से धर्म में आदर सहित हो गयी । एक समय जितारि राजा ने पुत्री को नीरोग देख विवाह के निमित्त राजकुमार बुलाये और पुत्री के आगे विवाह के लिए सभी राजकुमार स्वयंवर में दिखलाये । परन्तु उसके मन में कोई भी रुचिकर नहीं लगा । पश्चात् राजपुत्र अपने स्थान पर चले गये । एक समय तुण्डदेश के चक्रकोट नामक नगर में राजा भगदत्त रहता था । वह दानशूर, रूप सौन्दर्य आदि गुणों से सहित तथा समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था परन्तु जाति से हीन था । उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमति, मन्त्री का नाम सुबुद्धि और स्त्री का नाम गुणवती था । उस भगदत्त ने मुण्डिका की याचना की । राजा जितारि ने कहा कि-हे कुजात! जो कन्या मैंने उच्च कुलीन उत्तम राजपुत्रों को नहीं दी है, अरे भगदत्त! वह कन्या तुझ पापी दासीपुत्र के लिए कैसे दूँगा ? उसने कहा - हे राजन्! गुण होना चाहिए जन्म में क्या रखा है ? जैसा कि कहा है - कौशेयं कृमिजं सुवर्णमुपलाद् दूर्वा च गोरोमत:
रेशमी वस्त्र कीड़ों से उत्पन्न होता है, सुवर्ण पाषाण से निकलता है, दूर्वा गाय के बालों से उत्पन्न होती है, कमल कीचड़ से जन्म लेता है, चन्द्रमा समुद्र से प्रकट होता है, नील कमल गोबर से उद्भूत होता है, अग्नि काठ से उत्पन्न होती है, मणि साँप के फण से उपलब्ध होती है और रोचन गाय के पित्त से प्रकट होता है । ठीक है गुणी मनुष्य, पुण्य के उदय से प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं अत: जन्म से क्या होता है ॥355॥पङ्कात्तामरसं शशाङ्कमुदधेरिन्दीवरं गोमयात् । काठादग्निरहे: फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचन: प्राकाश्यं सुदिनोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥355॥ किञ्च- और भी कहा है - गुणा: सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक: ।
गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं, पिता का वंश निरर्थक है । देखो, लोग वासुदेव-कृष्ण को नमस्कार करते हैं परन्तु उनके पिता वसुदेव को नहीं ॥356॥वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न ते जना: ॥356॥ जितारिणोक्तम्-तव गुणवतोऽपि सर्वथा न दास्ये । तथा चोक्तम्- जितारि ने कहा - तुम गुणवान् हो तो भी तुम्हें बिलकुल नहीं दूँगा । जैसा कि कहा है - सारमेय! यदि रत्नमालयालङ्कृतोऽसि खलु मन्दबुद्धिना ।
अरे कुक्कुर! यदि तू किसी मूर्ख द्वारा रत्नों की माला से अलंकृत कर दिया गया है तो मात्र गजराज को विदारण करने की क्रीड़ा करने वाले सिंह के साथ क्यों विरोध करता है? ॥357॥तत्करीन्द्र-दलनैककेलिना रे कथं च हरिणा विरुध्यसे ॥357॥ अथवा दैवयोगेन त्वं राजा धनवानभू: । तत्किं क्षत्रियपुत्राणां सार्धं स्पर्धां बिभर्षि रे ॥358॥ अथवा रे भगदत्त! यदि तू दैवयोग से धनवान राजा हो गया है तो क्षत्रिय पुत्रों के साथ ईर्ष्या क्यों करता है ॥358॥ ततो भगदत्तेन जल्पितम्-भो राजन! यदि राज्येन प्रयोजनं विद्यते तर्हि कन्यां प्रयच्छ । अन्यथा द्वयमपि बलाल्लप्स्ये । जितारिणोक्तम्-रणमध्ये तव वाञ्छितं सर्वमपि दास्यामि नान्यथा । एतद्वचनं श्रुत्वा महाकोपं कृत्वा भगदत्तो जितार्युपरि चलित: । अथ सुबुद्धिना मन्त्रिणा भणितम्-हे भगदत्त! समस्त युद्ध- सामग्रीमेकत्रितां कृत्वा गम्यते, अन्यथा नाश एव भवति । तथा चोक्तम्- तदनन्तर भगदत्त ने कहा कि-हे राजन्! यदि तुम्हें राज्य से प्रयोजन है तो कन्या देओ अन्यथा राज्य और कन्या दोनों को बलपूर्वक प्राप्त कर लूँगा । जितारि ने कहा - युद्ध में तुम्हारी अभिलषित सभी वस्तु दूँगा अन्यथा नहीं । यह वचन सुन तीव्र क्रोध कर भगदत्त जितारि के ऊपर चल पड़ा । तदनन्तर सुबुद्धि मन्त्री ने कहा - हे भगदत्त! युद्ध की समस्त सामग्री इकठ्ठी करके चले जाना है अन्यथा नाश ही होता है । जैसा कि कहा गया है - स्वकीयबलमज्ञात्वा संग्रामार्थं तु यो नर: ।
जो मनुष्य अपना बल जाने बिना युद्ध के लिए सम्मुख चल देता है वह अग्नि में शलभ के समान नाश को प्राप्त होता है ॥359॥गच्छत्यभिमुखो नाशं याति वह्नौ पतङ्गवत् ॥359॥ यथा राजा भृत्यैर्विना न शोभते, यथा च रविरंशु-रहितो न शोभते तद्वदेकेन बलवान् न । समुदायेन तु बलवान् भवेत् । यथा तृणै: रज्जुं कृत्वा नागो बध्यते । उक्तञ्च- जिस प्रकार राजा सेवकों के बिना शोभा नहीं देता और सूर्य किरणों से रहित होने पर सुशोभित नहीं होता उसी प्रकार बलवान् मनुष्य अकेला सुशोभित नहीं होता । किन्तु समुदाय से बलवान होता है । जैसा कि तृणों से रस्सी बनाने पर हाथी बाँधा जाता है । कहा भी है - एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्या: कार्या विचक्षणा: ।
ऐसा जानकर राजा को बुद्धिमान्, कुलीन, शूरवीर, समर्थ भक्त और कुल परम्परा से आये हुए लोगों को सेवक बनाना चाहिए ॥360॥कुलीना: शौर्यसंयुक्ता: शक्ता भक्ता: क्रमागता: ॥360॥ भगदत्तेन राज्ञोक्तम्-भो सुबुद्धे । हितरूपेण तदुक्तं त्वया तत् सर्वमपि सत्यम् । अतएव हितचिन्तकस्य वचनं स्वीकरणीयमन्या विरूपकमेव भवति । तत: सर्व सामग्रीं मेलयित्वा शुभमुहूर्ते निर्गमनोद्योग: कृत: । एतस्मिन् प्रस्तावे लक्ष्मीमत्या राह्या भणितम्-भो स्वामिन्! किमर्थं निरर्थको दुराग्रह: क्रियते यत्रोभयो: साम्यं तत्र विवाहमैत्र्यादिकं भवति, नान्यथा, अतएवायुक्तं न कर्तव्यम् । उक्तञ्च- भगदत्त राजा ने कहा - हे सुबुद्धि मन्त्री! तुमने जो कहा है वह सब कुछ सत्य है । इसलिए हितेच्छु के वचन स्वीकृत करना चाहिए अन्यथा अनर्थ होता है । पश्चात् सब सामग्री एकत्रित कर शुभ मुहूर्त में उसने प्रस्थान करने का उद्योग किया । इसी अवसर पर लक्ष्मीमति रानी ने कहा कि - हे नाथ! व्यर्थ ही दुराग्रह क्यों किया जाता है? जहाँ दोनों की समानता हो वहीं विवाह और मित्रता आदि होती है, अन्यथा नहीं । अतएव अयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए । कहा भी है - अव्यापारेषु व्यापारं यो नर: कर्तुमिच्छति ।
जो मनुष्य न करने योग्य कार्यों में उद्योग करता है वह कील को उखाड़ने वाले वानर के समान मरण को प्राप्त होता है ॥361॥स एव मरणं याति कीलोंत्पाटीव वानर: ॥361॥ भगदत्तेनोक्तम्-भो मूर्खे! पुरुष-पुरुषान्तरे कारणमस्ति । जितारिणा ममाग्रे निरूपितम्-युद्धमध्ये सर्वमपि दीयते । अद्याहं तथा न करोमि चेत् ततोऽन्येषामपि भूपतीनामहं न भवामि मान्य: । उक्तञ्च- भगदत्त ने कहा - हे मूर्ख! पुरुष-पुरुष के अन्तर में कारण है । जितारि ने मेरे सामने कहा था कि युद्ध के बीच सब कुछ दिया जाता है । यदि आज मैं वैसा नहीं करता हूँ-उस पर चढ़ाई नहीं करता हूँ तो अन्य राजाओं के लिए भी मैं मान्य नहीं रहूँगा । यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितैर्मनुष्यै:-
मनुष्य विज्ञान, शूरवीरता, वैभव तथा अन्य गुणों से युक्त होकर यदि क्षणभर के लिए भी जीवित रहते हैं तो सत्पुरुष उसे ही जीवित रहने का फल कहते हैं । वैसे तो कौआ भी चिरकाल तक जीवित रहता है और बलि-चढ़ोत्तरी को खाता है ॥362॥विज्ञान-शौर्यं-विभवार्यगुणै: समेतै: । तस्यैव जीवितफलं प्रवदन्ति सन्त: काकोऽपि जीवति चिरं च बलिं च भुङ् क्ते ॥362॥ ततो महासंभ्रमेण निर्गत्याविञ्छिन्न-प्रयाणकैर्जितारिदेशसीमां गतो भगदत्त: । लक्ष्मीमत्या राज्ञ्या चिन्तितं-यद्भाव्यं तद् भविष्यति । निर्गमनसमये शुभशकुनानि जातानि । तद्यथा-दधि दूर्वाक्षतपात्रं, जल-कुम्भेषु दण्डपद्मिनी, प्रसूतवती स्त्री, वीणाप्रभृतिकमग्रे सुदर्शनं जातम् । केनचिच्चरपुरुषेणागत्य जितारिराजाग्रे निरूपितमेकान्त-हे देव! भगदत्तस्य राज्ञो बलमागतम् । ततो गर्वान्वितेन राज्ञा भणितम्-रे वराक! स कोऽपि वीरो महीतलेऽस्ति यो ममोपरि चलति । अहं जितारिर्नामेति । तथा चोक्तम्- तदनन्तर बड़ी भारी तैयारी से निकल कर लगातार कई पड़ावों द्वारा भगदत्त, जितारि के देश की सीमा पर पहुँच गया । लक्ष्मीमति रानी ने विचार किया कि जो होनहार है वह होगा परन्तु प्रस्थान के समय शुभ शकुन हुए थे जैसे दही, दूर्वा और अक्षतों का पात्र, जल से भरे हुए कलशों पर रखी हुई डंठल सहित कमलिनी, प्रसूता स्त्री और वीणा आदि दर्शनीय पदार्थ आगे आये हैं । किसी गुप्तचर ने आकर जितारि राजा के आगे कहा - हे देव! भगदत्त राजा की सेना आ गयी है । तब गर्व से युक्त राजा ने कहा - अरे रंक! पृथ्वी पर वह कोई वीर है जो मेरे ऊपर चढ़ाई कर सके । मेरा जितारि नाम है-मैं शत्रुओं को जीतने वाला सचमुच का जितारि हूँ । जैसा कि कहा है- दृष्टं श्रुतं न क्षितिलोकमध्ये मृगा मृगेन्द्रोपरि संचलन्ति ।
पृथ्वी लोक के मध्य ऐसा न देखा गया है और न सुना गया है कि मृग सिंह पर चढ़ाई करते हैं, चन्द्रमा और सूर्य राहु पर आक्रमण करते हैं अथवा चूहे बिलाओं पर चढ़ते हैं ॥363॥विधुन्तुदस्योपरि चन्द्रमोऽर्को किं वा विडालोपरिमूषका: स्यु: ॥363॥ किं वेनतेयोपरि काद्रवेय: किं सारमेयोपरि लम्बकर्ण: ।
क्या साँप गरुड़ पर, गधे कुत्ते पर, प्राणिसमूह यमराज पर और कौए बाज पक्षी पर आक्रमण करते हैं ॥364॥किं वा कृतान्तोपरि भूतवर्ग: किं कुत्र श्येनोपरि वायसा: स्यु: ॥364॥ "यावद् भास्करो नोदेति तावत्तम: ।" इत्येवं यावद् भणति तावद् गुप्तवृत्त्यागत्य वाराणसीपुरं वेष्टितं भगदत्तेन राज्ञा । भगदत्तस्याभ्यागतस्य कोलाहलं श्रुत्वा महता संभ्रमेण चतुरङ्गबलेन सह निर्गतो जितारि: । निर्गमनसमयेऽपशकुनानि जातानि । तथा चोक्तम्- ठीक कहा है कि जब-तक सूर्य उदित नहीं होता है तभी तक अन्धकार रहता है । इस प्रकार जब-तक कहता है तब-तक गुप्त रूप से आकर भगदत्त राजा ने वाराणसी नगर घेर लिया । आये हुए भगदत्त का कोलाहल सुनकर जितारि बड़ी तैयारी से चतुरंग सेना के साथ बाहर निकला । निकलते समय उसे अपशकुन हुए । जैसा कि कहा है - अकालवृष्टिस्त्वथ भूमिकम्पो निर्घात उल्कापतनं प्रचण्डम् ।
अकाल-वृष्टि, पृथ्वी-कम्पन, वज्रपात और भयंकर उल्कापात, ये सब अनिष्ट अपशकुन प्रकट हुए मानों मित्र के समान उसे युद्ध से रोकने के लिए ही प्रकट हुए थे ॥365॥इत्याद्यनिष्टानि ततो बभूवुर्निवारणार्थं सुहृदो यथैव ॥365॥ अस्मिन् प्रस्तावे सुदर्शनमन्त्रिणा भणितम्-हे देव! कन्या दत्त्वा सुखेन स्थीयते । तथा चोक्तम्- इस अवसर पर सुदर्शन मन्त्री ने कहा - हे देव! कन्या देकर सुख से रहा जाये । जैसा कि कहा है - रक्षन्ति देशं ग्रामेण ग्राममेकं कुलेन च ।
बुद्धिमान् जन एक ग्राम का त्याग कर देश की, कुल का त्याग कर एक ग्राम की, एक व्यक्ति का त्याग कर कुल की और पृथ्वी का त्याग कर अपने आपकी रक्षा करते हैं ॥366॥कुलमेकेन चात्मानं पृथ्वीत्यागेन पण्डिता: ॥366॥ जितारिणोक्तम्-भो मन्त्रिवर्या: किमर्थं भयं कुरुथ ? मम खङ्गघातं सोढुं क: समर्थ: तथा चोक्तम्- जितारि ने कहा - हे श्रेठ मन्त्रियो! भय किसलिये करते हो ? मेरी तलवार का प्रहार सहन करने के लिए कौन समर्थ है? जैसा कि कहा है - कोऽस्मिन् लोके शिरसि सहते य: पुमान् वज्रपातं
इहलोक में ऐसा कौन पुरुष है जो शिर पर वज्रपात को सह सके, ऐसा कौन मनुष्य है जो भुजदण्डों के द्वारा अपार समुद्र को तैर सके ? ऐसा कौन है? जो अग्निशय्या पर सुख की नींद का सेवन करता हो ? और क्या ऐसा भी कोई है जो एक-एक ग्राम के द्वारा निरन्तर कालकूट विष का सेवन करता हो ॥367॥कोऽस्तीदृग्यस्तरति जलधिं बाहु दण्डेरपारम् । कोऽस्त्वस्मिन्यो दहनशयने सेवते सौख्यनिद्रां ग्रासैर्ग्रासै-र्गिलति सततं कालकूटं च कोऽपि ॥367॥ पुनर्मन्त्रिणाऽसम-सन्नाह-संयुक्तं परदलं दृष्ट्वा निरूपितम्-देव! बहुवलं समागतं, किं क्रियते? जितारिणोक्तम्-मन्त्रिन् सत्त्वेन सिद्धिर्जयश्च, न बहुसामग्रया । यदुक्तम्- पश्चात् अनुपम तैयारी से युक्त शत्रु सेना को देखकर मंत्री ने फिर कहा - हे देव! बहुत बड़ी सेना आयी है क्या किया जाये ? जितारि ने कहा - हे मन्त्री! पराक्रम से सिद्धि और विजय होती है बहुत सामग्री से नहीं । जैसा कि कहा है- रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता: सप्ततुरगा
सूर्य के रथ को एक ही चक्र है, घोड़े नागपाश से बद्ध हैं तथा गिनती के सात ही हैं, मार्ग आलम्बनरहित-निराधार आकाश है और सारथि भी चरणों से रहित-अनुरूप है फिर भी वह प्रतिदिन अपार आकाश के अन्त को प्राप्त होता है । इससे जान पड़ता है कि महापुरुषों की क्रियासिद्धि उनके पराक्रम में रहती है उपकरण सहायक सामग्री में नहीं ॥368॥निरालम्बो मार्गश्चरण-विकल: सारथिरपि । रविर्याति प्रान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस: क्रियासिद्धि: सत्त्वे वसतिमहतां नोपकरणे ॥368॥ घटो जन्म-स्थानं ग्रह-परिजनो भूर्जवसनो
अगस्त्य ऋषि का जन्म स्थान घट था, ग्रह समूह ही उनका परिवार था, भोजपत्र उनका वस्त्र था, वन में उनका निवास था, कन्दमूल भोजन था, शरीर अस्वस्थ था और स्वभाव के शान्त थे फिर भी उन्होंने अपार समुद्र को पी लिया । इससे सिद्ध होता है कि महापुरुषों की क्रियासिद्धि-कार्य की सफलता उनके पराक्रम में रहती है उपकरणों में नहीं ॥369॥वने वास: कन्दस्त्वशनमपि दु:स्थं वपुरपि । अतीव्रोऽगस्त्योऽयं यदपिबदपारं जलनिधिं क्रियासिद्धि: सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥369॥ विपक्ष: श्रीकण्ठो जडतनुरमात्य: शशधरों
महादेवजी काम के शत्रु हैं, शीतल शरीर को धारण करने वाला चन्द्रमा उसका मन्त्री है, बसन्त ऋतु सामन्त है, पुष्प बाण हैं, स्त्रियाँ सेना हैं और स्वयं अनंग-शरीर रहित है फिर भी वह तीन लोक को जीत लेता है । इससे जान पड़ता है कि महापुरुषों की क्रियासिद्धि उनके पराक्रम में रहती है उपकरणों में नहीं ॥370॥वसन्त: सामन्त: कुसुममिषव: सैन्यमबला: । तथापि त्रैलोक्यं जयति-मदनो देह-रहित: क्रिया-सिद्धि सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥370॥ स्वयं तिर्यग्योनि: करचरणरहित: पृथुशिरा:
शेषनाग स्वयं तिर्यर् योनि का है, हाथ पैरों से रहित है, विशाल शिर से सहित है, स्वभाव से ही उसमें आलस्य भरा हुआ है और वायुरूप ग्रास के भक्षण में निरत रहता है अर्थात् वायु ही उसका भोजन है फिर वह इस विश्व को फण की मणि पर धारण कर रहा है । इससे ज्ञात होता है कि महापुरुषों की क्रियासिद्धि उनके पराक्रम में रहती है उपकरण में नहीं ॥371॥स्वभावादालास्यं त्वशननिरतो वायुकवले । तथाप्येतद्विश्वं वहति फणिराज: फणमणौ क्रियासिद्धि: सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥371॥ ततो भगदत्तेन दूतलक्षणयुक्तो दूत: प्रेषित: । दूतलक्षणं यथा- पश्चात् भगदत्त ने दूत के लक्षणों से युक्त दूत भेजा । दूत का लक्षण यह है - मेधावी वाक्पटुश्चैवं परचित्तोपलक्षक: ।
जो बुद्धिमान् हो, वचन बोलने में चतुर हो, दूसरों के हृदय को देखने वाला हो, गम्भीर हो और सत्यवादी हो, वही दूत का लक्षण है ॥372॥धीरो यथोंक्तवादी च ह्येतद् दूतस्य लक्षणम्॥372॥ एतादृशो दूत: प्रस्थापित: । यत:- भगदत्त ने ऐसा दूत भेजा, क्योंकि - पुरा दूत: प्रकर्तव्य: पश्चाद् युद्ध: प्रकाश्यते ।
पहले दूत भेजना चाहिए पश्चात् युद्ध की घोषणा करनी चाहिए । उसका कारण यह है कि दूत के द्वारा सबल और निर्बल सेना का बोध हो जाता है ॥373॥दूतेन सबलं सैन्यं निर्बलं ज्ञायते ध्रुवम् ॥373॥ ततो दूतेन तेन जितारिराजस्याग्रे गत्वोक्तम्-हे राजन्! मुण्डिकां प्रदाय महामण्डलेश्वरस्य भगदत्तनरेन्द्रस्य सेवां च कृत्वा सुखेन राज्यं कुरु । अन्यथा नाश एव । यदुक्तं- तदनन्तर उस दूत ने जितारि राजा के आगे जाकर कहा कि-हे राजन्! मुण्डिका को देकर और महा मण्डलेश्वर भगदत्त नरेन्द्र की सेवा कर सुख से राज करो अन्यथा विनाश ही होगा । जैसा कि कहा है- अनुचित कर्मारम्भ: स्वजनविरोधो बलीयसां स्पर्धा ।
अनुचित कार्य का प्रारम्भ करना, आत्मीय जनों के साथ विरोध करना, बलिठ पुरुषों के साथ ईर्ष्या करना और स्त्रियों का विश्वास करना; ये मृत्यु के चार द्वार हैं ॥374॥प्रमदाजन-विश्वासो मृत्योद्र्वाराणि चत्वारि ॥374॥ जितारिणा राज्ञोक्तम्-रे वराक! किं जल्पसि रणे ममाग्रे न स्थास्यन्त्येते । अथवा यद् भावि तद् भवतु । किन्तु न ददामि सुतामिति स्वकीयां प्रतिज्ञां सर्वनाशेऽपि न त्यजामि । यन्महापुरुषेणाङ्गीकृतं तन्न त्यजति । तथा चोक्तम्- जितारि राजा ने कहा - अरे दीन! क्या कहता है ? युद्ध में मेरे आगे ये खड़े नहीं होंगे अथवा जो होना हो वह हो किन्तु "मैं पुत्री नहीं दूँगा" अपनी इस प्रतिज्ञा को सर्वनाश होने पर भी नहीं छोडूँगा । महापुरुष जिसे स्वीकृत कर लेते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं । जैसा कि कहा है - मार्तण्डान्वयजन्मना क्षितिभृता चाण्डाल-सेवा कृता
सूर्यवंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चन्द्र ने चाण्डाल की सेवा की, अद्भुत पराक्रम के धारक रामचन्द्रजी ने सघन कन्दरा का सेवन किया और चन्द्रवंशीय भी आदि उत्तम राजाओं ने रंक के समान दीनता की । इससे सिद्ध है कि पुरुषों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए क्या-क्या नहीं अंगीकृत किया है ? अर्थात् सभी कुछ किया है ॥375॥रामेणाद्भुत-विक्रमेण गहना संसेविता कन्दरा । भीमाद्यै: शशिवंशजैर्नृपवरैर्दैन्यं कृतं रङ्कवत् स्वाभाषापरिपालनाय पुरुषै: किं किं च नाङ्गीकृतम् ॥375॥ अद्यापि नोज्झति हर: किल कालकूटं
शंकरजी अब भी कालकूट विष को नहीं छोड़ रहे हैं, कछुआ अब भी अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण कर रहा है और समुद्र अब भी दुस्सह बड़वानल को धारण कर रहा है सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जन स्वीकृत बात का अच्छी तरह पालन करते हैं ॥376॥कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृठभागे । अम्भोनिधिर्वहति दुस्सहवाडवाग्नि- मङ्गीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति ॥376॥ तदैवं प्रजल्प्य कु्रद्धेन जितारिणा राज्ञा दूतमारणाय भटा: समादिष्टा: । ततो मन्त्रिणा मन्त्रितम्-दूतमारणमनुचितम् । उक्तञ्च-भो राजन्! दूतहननात् समन्त्री राजा नरकं व्रजति । राजानं विज्ञाप्य दूतो निर्घाटितो मन्त्रिणा । ततो दूतेनागत्य भगदत्ताग्रे कथितम्-देव जितारि: स्वभुजबलेन किमपि न गणयति । ततो भगदत्तो दलं संनाह्य युद्धार्थं चलित: । जितारिरपि सम्मुखो भूत्वा स्थित: । तस्मिन् समये किं किं जातम्? तद्यथा- उस समय ऐसा कहकर क्रोध से परिपूर्ण राजा जितारि ने दूत को मार डालने के लिए योद्धाओं को आज्ञा दी । पश्चात् मन्त्री ने विचार किया कि दूत का मारना अनुचित है । विचार कर उसने कहा भों-हे राजन्! दूत के मारने से मन्त्री सहित राजा नरक को जाता है । राजा से ऐसा कहकर मन्त्री ने दूत को बाहर निकाल दिया । तदनन्तर दूत ने आकर राजा भगदत्त के आगे कहा - हे देव! जितारि अपनी भुजाओं के बल से कुछ भी नहीं गिनता है । पश्चात् भगदत्त सेना को सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा । इधर जितारि भी सम्मुख होकर खड़ा हो गया । उस समय क्या-क्या हुआ? सो सुनो - दिक्चक्रं चलितं भयाज्जलनिधिर्जातो महाव्याकुल:
दिग्मण्डल भय से चलायमान हो गया, समुद्र अत्यन्त व्याकुल हो उठा, पाताल में शेषनाग चकित रह गया, पर्वत काँप उठे, पृथ्वी घूम गयी और बड़े-बड़े साँप भयंकर विष को उगलने लगे । सेनापति की सेना निकलते ही यह सब अनेक प्रकार के कार्य हुए ॥377॥पाताले चकितो भुजङ्गमपति: क्षोणीधरा: कम्पिता: । भ्रान्ता सुपृथिवी महाविषधरा: क्ष्वेडं वमन्त्युत्कटं वृत्तंसर्वमनेकधा दलपतेरेवं चमू-निर्गमे ॥377॥ भगदत्तसैन्यं विजयीं दृष्ट्वा मन्त्री जगाद-हे जितारे राजन्! पश्य, स्वसैन्ये त्रासोऽभूत् । अतो न स्थीयते । राज्ञा जल्पितम्-हे मन्त्रिन्! किमर्थं कातरो भवसि । उभयतोऽपि वरं जयिनि सति इहलोके सौख्यं मृते सति परलोके सौख्यं भविष्यति । उक्तञ्च- भगदत्त की सेना को विजयी देख मन्त्री ने कहा कि-हे जितारि राजन्! देखो, अपनी सेना में भय छा गया है इसलिए वह खड़ी नहीं रह सकेगी । राजा ने कहा कि-हे मन्त्री! कायर क्यों हो रहे हो? दोनों प्रकार से लाभ है विजयी होने पर इहलोक में सुख और मरने पर परलोक में सुख होगा । कहा भी है - जयिना लभ्यते लक्ष्मीर्मृतेनापि सुराङ्गना ।
सुभट यदि विजयी होता है तो उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है और मरता है तो देवांगना मिलती है । शरीर क्षणभंगुर है अत: रण में मरण होने की क्या चिन्ता है ॥378॥क्षणविध्वसिन: काया का चिन्ता मरणे रणे ॥378॥ पुनर्मन्त्रिणा निगदितम्-हे राजन् जीवन्नरो भद्रशतानि पश्येत् । मरणे किं साध्यम्? ततो जितारि: कथमपि व्याघुट्य गत: । चलतानेन राज्ञा भणितम्-दैवमेव प्रमाणम् । यत:- मन्त्री ने फिर कहा - हे राजन्! मनुष्य यदि जीवित रहता है तो सैकड़ों कल्याणों को देख सकता है मरने पर क्या साध्य है अर्थात् कुछ भी नहीं । पश्चात् जितारि किसी तरह लौटकर चला गया । जाते समय राजा जितारि ने कहा कि-भाग्य ही प्रमाण है- वही बलवान है, क्योंकि - नेता यत्र बृहस्पति: प्रहरणं वज्रं सुरा: सैनिका:
जहाँ बृहस्पति नायक था, वज्र शस्त्र था, देव सैनिक थे और स्वर्ग किला था, नारायण की कृपा थी और ऐरावत हाथी था, वहाँ इस प्रकार के आश्चर्यकारक बल से सहित होने पर भी इन्द्र युद्ध में दूसरों से पराजित हो गया, इससे जान पड़ता है कि निश्चय से दैव ही शरण है व्यर्थ के पौरुष को धिक्कार हो ॥379॥स्वर्गो दुर्गमनुग्रह: खलु हरेरैरावणो वारण: । इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभिद् भग्न: परै: संगरे तद्युक्तं ननु दैवमेव शरणं धिक् धिक् वृथा पौरुषम्॥379॥ भगदत्तो जितारिपृठे लग्न: । सुबुद्धिना मन्त्रिणा निषिद्ध: । भो भगदत्त! नोचितमिदम्-तथा चोक्तम्- भगदत्त, जितारि के पीछे लग गया तब सुबुद्धि मंत्री ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि हे भगदत्त! यह उचित नहीं है । जैसा कि कहा है - भीरु: पलायमानोऽपि नान्वेष्टव्यो बलीयसा ।
भागते हुए भयभीत शत्रु का बलवान मनुष्य को पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि मरण का निश्चय कर वह कभी शूरता को प्राप्त हो सकता है ॥380॥कदाचिच्छूरतां याति मरणे कृतनिश्चय:॥380॥ एतत्सर्वमपि वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च मुण्डिका जिनदेवं हृदि स्मृत्वा सावधिप्रत्याख्यानं कृत्वा पर- मेठिमन्त्रमुच्चार्य गम्भीरे कूपे पतिता । तस्या: सम्यक्त्वप्रभावाज्जलं स्थलं जातम् । तस्योपरि रत्नगृहं, तन्मध्ये सिंहासनम् । तस्योपरि निविष्टा सीतावत् स्थिता सुखेन सा मुण्डिका । देवै: पञ्चाश्चर्यं कृतम् । इतो भगदत्तेन राज्ञा प्रतोलीं विदार्य सर्वमपि पुरं लुण्टयितुमारभे । यावज्जितारिमन्दिरे भगदत्त: प्रविशति तावद् देवव्या स्तम्भित: । अस्मिन् प्रस्तावे केनचित् पुरुषेण भगदत्त-मण्डलेश्वरस्याग्रे मुण्डिकाया: सर्वोऽपि वृत्तान्तो निरूपित: । तच्छ्रुत्वा प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा मदवर्जितो भूत्वा विनयपूर्वं मुण्डिकाया: पादयो: पतितो भगदत्त उक्तवांश्च-भो भगिनि! यन्मया कृतं तदज्ञानव्या । तत्सर्वं सहनीयमित्यादिं निरूप्य धर्महस्तं दत्वा जितारिप्याकारित: । आगतस्य तस्याग्रे तथैवोक्तवान् । ततो वैराग्यभरभावितान्त: करणो भगदत्त: पठति स्म-जिनोक्त: सद्धर्म: प्राणिनां हितं किं किं न करोति? । यत उक्तम्-" "सेतु: संसारसिन्धौ निविडतरमहाकर्मकान्तारवह्नि:ङ्घङ्घ-एवं धर्म एव सहाय: । उक्तञ्च यथा- इस सभी वृत्तान्त को देख सुनकर मुण्डिका ने हृदय में श्री जिनेन्द्रदेव का स्मरण किया और समय की मर्यादा के साथ आहार-पानी का त्याग करके णमोकारमन्त्र का उच्चारण करती हुई गहरे कूप में गिर पड़ी । उसके सम्यक्त्व के प्रभाव से जल स्थल हो गया, उसके ऊपर रत्नों का घर और उसके बीच में सिंहासन प्रकट हो गया । उस सिंहासन पर वह मुण्डिका सीता के समान स्थित हो गयी । देवों ने पञ्चाश्चर्य किये । इधर राजा भगदत्त ने गोपुर को तोड़कर सभी नगर को लूटना प्रारम्भ कर दिया । जब भगदत्त राजा जितारि के भवन में प्रवेश करने लगा तब देवता ने उसे कील दिया । इसी अवसर पर किसी पुरुष ने राजा भगदत्त के आगे मुण्डिका का सभी समाचार कह सुनाया । उसे सुनकर और प्रत्यक्ष देखकर वह मद रहित हो विनयपूर्वक मुण्डिका के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा-हे बहिन! मैंने जो किया है वह अज्ञानता से किया है उस सबको क्षमा करो । इत्यादि कहकर उसने धर्मसूचक हाथ देकर जितारि को भी बुलवा लिया । आये हुए जितारि के सामने भी उसने उसी प्रकार कहा । तदनन्तर जो अपने हृदय में वैराग्य की भावना भा रहा था, ऐसे भगदत्त ने कहा कि-जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्म प्राणियों का क्या-क्या हित नहीं करता है ? क्योंकि कहा है- यह धर्म संसाररूपी समुद्र से पार करने वाला पुल है और कर्मरूपी सघन वन को जलाने के लिए अग्नि है । इस प्रकार धर्म ही सहायक है । जैसा कि कहा है - धर्मप्रभावात्सकला समृद्धि-
धर्म के प्रभाव से समस्त समृद्धि प्राप्त होती है, धर्म के प्रभाव से संसार में प्रसिद्धि होती है, धर्म के प्रभाव से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और धर्म के प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि होती है ॥381॥र्धर्म प्रभावाद् भुवने प्रसिद्धि: । धर्मप्रभावादणिमादि-सिद्धि- र्धर्मप्रभावान्निज-वंशवृद्धि:॥381॥ तत: स्वपुत्राय राज्यं वितीर्य भगदत्तजितारिमुण्डिकादिभि: प्रव्रज्या गृहीता । अन्येषां बहूनां जीवानां धर्मलाभो जात: । नागश्रिया भणितम्-हे स्वामिन् सर्वमेतत्प्रत्यक्षेण दृष्टम्, अतो मम दृढतरं सम्यक्त्वं जातम् । ततोऽर्हद्दासेनोक्तम्-यत्त्वया दृष्टम्, एतत्सत्यमतो भो भार्ये! रोचे, श्रद्दधामि, इच्छामि । अन्याभिश्च तथैवोक्तम् । तत: कुन्दलव्योक्तम्-सर्वमसत्यमतो न श्रद्दधामीति । राज्ञा मन्त्रिणा चौरेण च स्वस्वमनसि चिन्तितम् दुष्टेयम् । प्रभातसमये गर्दभं चाटयित्वास्या निग्रहं करिष्यामो वयम् । पुनरपि चौरेण स्वमनसि विमृष्टं दुर्जनस्वभावोऽयम् । यदुक्तम्- तदनन्तर अपने पुत्र के लिए राज्य देकर भगदत्त, जितारि तथा मुण्डिका आदि ने जिनदीक्षा ले ली और भी बहुत जीवों को धर्मलाभ हुआ । नागश्री ने कहा - हे स्वामिन्! यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है इसलिए मुझे अत्यन्त दृढ़ सम्यक्त्व हुआ है । पश्चात् अर्हद्दास ने कहा कि-जो तुमने देखा है वह सत्य है इसलिए हे प्रिये मुझे वह रुचता है, मैं उसकी श्रद्धा करता हूँ और इच्छा करता हूँ । अन्य स्त्रियों ने भी वैसा ही कहा । तदनन्तर कुन्दलता ने कहा - यह सब असत्य है, इसलिए मैं इसकी श्रद्धा नहीं करती हूँ । राजा, मन्त्री और चोर ने अपने-अपने मन में कहा कि-यह दुष्टा है । प्रभात समय गधे पर चढ़ाकर इसे हम लोग दण्डित करेंगे । चोर ने फिर भी अपने मन में विचार किया कि-यह दुर्जन का स्वभाव ही है । जैसा कि कहा है- न विना परिवादेन रमते दुर्जनो जन: ।
दुष्ट मनुष्य को निन्दा किये बिना चैन नहीं पड़ती क्योंकि कौआ समस्त रसों को छोड़कर अशुचि पदार्थ के बिना संतुष्ट नहीं होता ॥382॥काक: सर्वरसान् भुक्त्वा विना मेध्यं न तृप्यति ॥382॥ खल: सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति ।
दुष्ट पुरुष, दूसरों के सरसों बराबर दोषों को देखता है और अपने बेल के बराबर दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है ॥383॥आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥383॥ सर्प: क्रूर: खल: क्रूर: सर्पात्क्रूरतर: खल: ।
सर्प क्रूर है और दुर्जन भी क्रूर है परन्तु दुर्जन, सर्प की अपेक्षा अधिक क्रूर है क्योंकि सर्प तो मन्त्र से शान्त हो जाता है परन्तु दुर्जन किससे शान्त होता है ? अर्थात् किसी से नहीं ॥384॥मन्त्रेण शाम्यते सर्प: खल: केनोपशाम्यते ॥384॥ ॥ इति पञ्चमो कथा॥ ॥ इस प्रकार पाँचवीं कथा पूर्ण हुई ॥ |