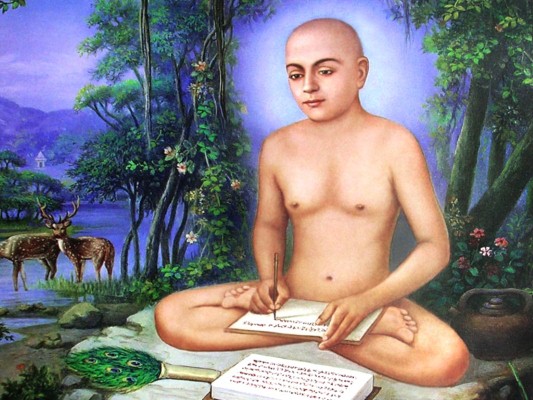


कथा :
सम्यक्त्व प्राप्तपद्मलता कथा । ततोऽर्हद्दास: पद्मलतां पृच्छति-भो भार्ये त्वमपि स्वसम्यक्त्वग्रहणकारणं कथय । सा करौ संयोज्य कथयति- अङ्गविषये चम्पापुरे राजा धाडिवाहन:, राज्ञी पद्मावती । तस्मिन्नेव नगरे श्रेठी वृषभदासों महासम्यग्दृष्टि: समस्त-गुण-सम्पन्नो निवसति । तस्य भार्या पद्मावती । व्यो: पुत्री पद्मश्री महारूपवती । सापि जिनधर्मवासितचित्ता गुणवती च बभूव । तस्मिन्नेव नगरेऽपर: श्रेठी बुद्धदासो बौद्धधर्ममध्ये प्रसिद्ध: दाता । भार्या सुबुद्धदासी । व्यो: पुत्रो बुद्धसंघ: । स बुद्धसंघो निजमित्रकामदेवेन सहैकदा कौतुकेन जिनचैत्यालये गत: । तत्र देवपूजां कुर्वती महारूपवती पद्मश्रीस्तेन बुद्धसंघेन दृष्टा । श्यामा सा रूपलावण्यसम्पन्ना, मधुरवाक् , कुम्भस्तनी, बिम्बोठी, चन्द्रवदना च । एवंविधं तस्या: पद्मश्रिया रूपमवलोक्य नीच: कामान्धो जात: । महता कष्टेन निजगृहं गत: शय्योपरि पतित: । चिन्ताप्रपन्नं तं पुत्रं दृष्ट्वा मात्रा भणितम्-रे पुत्र केन कारणेन तव भोजनादिकं न प्रतिभाति, महती चिन्ता च दृश्यते तव । कारणं कथय । ततो लज्जां मुक्त्वा बुद्धसंघेनोक्तम्-हे मार्व्यदा वृषभदास श्रेठपुत्रीं पद्मश्रियमहं विवाहयिष्यामि तदा मम जीवितं नान्यथा । एवं श्रुत्वा बुद्धदास्या निजस्वामिनोऽग्रे पुत्रवृत्तान्तं सर्वमपि निरूपितम् तत्र पित्राप्यागत्य भणितम् । रे पुत्र! मद्यमांसाहारिणोऽस्मान् स वृषभदासश्चाण्डालवत् पश्यति, तव कथं कन्यामेनां प्रयच्छति । अतएव साध्यवस्तुविषये विबुधैराग्रह: क्रियते नान्यत्र । अन्यच्च- तदनन्तर अर्हद्दास सेठ पद्मलता से पूछता है कि हे प्रिये! तुम भी अपने सम्यक्त्व ग्रहण का कारण कहो । वह हाथ जोड़कर कहती है - अंग देश के चम्पापुर नगर में राजा धाडिवाहन रहता था । उसकी रानी का नाम पद्मावती था । उसी नगर में एक वृषभदास नाम का सेठ रहता था, जो महान् सम्यग्दृष्टि तथा समस्त गुणों से सम्पन्न था । उसकी स्त्री का नाम पद्मावती था । उन दोनों के पद्मश्री नाम की अत्यधिक रूपवती पुत्री थी । पद्मश्री का चित्त जिनधर्म से युक्त था तथा वह अनेक गुणों को धारण करने वाली थी । उसी नगर में एक बुद्धदास नाम का दूसरा सेठ रहता था, जो बौद्धधर्म के बीच प्रसिद्ध दानी था । उसकी स्त्री का नाम बुद्धदासी था । उन दोनों के बुद्धसंघ नाम का पुत्र था । वह बुद्धसंघ एक दिन अपने मित्र कामदेव के साथ कौतूहलवश जैनमन्दिर गया । वहाँ उसने देवपूजा करती हुई परमरूपवती पद्मश्री को देखा । पद्मश्री यौवनवती थी, रूप और लावण्य से सम्पन्न थी, मधुर वचन बोलने वाली थी, कुम्भ के समान स्थूल स्तनों से युक्त थी, बिम्बाफल के समान लाल-लाल ओठों से सहित थी और चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख से सुशोभित थी । पद्मश्री के ऐसे रूप को देखकर नीच बुद्धसंघ काम से अन्धा हो गया । वह बड़े कष्ट से अपने घर पहुँचा और पहुँच कर शय्या पर पड़ रहा । पुत्र को चिन्तित देख माता ने कहा कि-हे पुत्र! किस कारण तुझे भोजनादिक नहीं रुच रहा है तथा बड़ी चिन्ता दिखायी दे रही है, कारण कहो । तदनन्तर लज्जा छोड़कर बुद्धसंघ ने कहा कि-हे माँ! जब मैं वृषभदास सेठ की पुत्री पद्मश्री को विवाह लूँगा तभी मेरा जीवन रहेगा, अन्यथा नहीं । ऐसा सुनकर बुद्धदासी ने अपने पति के आगे पुत्र का समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । पश्चात् पिता ने भी कहा - हे पुत्र! मद्य-मांस का आहार करने वाले हम लोगों को वह वृषभदास चाण्डाल के समान देखता है । वह तुम्हें यह कन्या कैसे दे देगा? इसीलिए प्राप्त होने योग्य वस्तु के विषय में ही विद्वानों द्वारा आग्रह किया जाता है अन्य वस्तु में नहीं । दूसरी बात यह भी है - ययोरेव समं शीलं ययोरेव समं कुलम् ।
जिनका समान शील होता है, जिनका समान कुल होता है और जिनमें गुणों की समानता होती है उन्हीं की निश्चित मित्रता होती है ॥385॥ययोरेव गुणै: साम्यं व्योर्मैत्री भवेद् धु्रवम् ॥385॥ पुत्रेणोक्तम्-किं बहुजल्पनेन, व्या बिना न जीवामि । पित्रोक्तम्-अहो विषमं कामस्य माहात्म्यम् । कामवह्निप्रदीपितोऽमृतसेचनेनापि न शाम्यति । उक्तञ्च- पुत्र ने कहा - अधिक कहने से क्या प्रयोजन है ? उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता । पिता ने कहा - अहो! काम का माहात्म्य विषम है । कामाग्नि से प्रदीप्त मनुष्य अमृत के सेवन से भी शान्त नहीं होता है । जैसा कि कहा है - सिक्तोऽप्यम्बुधरव्रातै: प्लावितोऽप्यम्बुराशिभि: ।
कामाग्नि से संतापित मनुष्य, मेघसमूह के द्वारा सींचे जाने पर भी तथा जलराशि के द्वारा डुबाये जाने पर भी संताप को नहीं छोड़ता है ॥386॥न हि त्यजति संतापं कामवह्निप्रदीपित: ॥386॥ तावद् धत्ते प्रतिष्ठां परिहरति मनश्चापलं चैव ताव-
मनुष्य तभी तक प्रतिष्ठा को धारण करता है, मन तभी तक चंचलता को छोड़ता है और समस्त तत्त्वों से देदीप्यमान सिद्धान्त सूत्र हृदय में तभी तक अत्यधिक रूप से स्फुरित रहता है जब तक क्षीरसागर की लहरों के समान सुशोभित स्त्रियों के कटाक्षों से ताडि़त होकर अत्यधिक र्चलता को धारण नहीं करता है ॥387॥त्तावत्सिद्धान्तसूत्रं स्फुरति हृदि परं विश्वतत्त्वैकदीपम् । क्षीराकूपारवेलावलयविलसितैर्मानिनीनां कटाक्षै:- यावन्नो हन्यमानं कलयति हृदयं दीर्घदोलायितानि ॥387॥ मात्रोक्तम्-मूर्खोऽयम् । सर्वमपि सुसाध्यं न तु मूर्खचित्तम् । "क्षितौ सर्वं सुसाध्यं स्यान्मूर्खस्य हृदयं न तु" । तथा चोक्तम्- माता ने कहा - यह मूर्ख है । सभी कार्य सुसाध्य है परन्तु मूर्ख का चित्त सुसाध्य नहीं है जैसी कि कहावत है - पृथ्वी पर सभी काम अच्छी तरह साध्य हैं परन्तु मूर्ख का हृदय साध्य नहीं है । जैसा कि कहा है - प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्टाङ्कुरात्
मगर के मुख के भीतर दाँढ़ रूप अंकुरों से मणि को बलपूर्वक निकाला जा सकता है, तरंगावली से व्याप्त समुद्र को तैरा जा सकता है और कु्रद्ध सर्प को भी फूल की तरह शिर पर धारण किया जा सकता है परन्तु हठी मूर्ख मनुष्य के चित्त की आराधना नहीं की जा सकती ॥388॥समुद्रमपि संतरेत्प्रचलदूर्मिमालाकुलम् । भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारये- न्नतु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् ॥388॥ यो यस्य स्वभावस्तं स शतेनापि शिक्षावचनैर्न त्यजति । पुन: पित्रोक्तम्-भो पुत्र! स्थिरो भव । तव कार्यं क्रमेण करिष्यामि । तथा चोक्तम्- जिसका जो स्वभाव होता है वह उसे सैकड़ों शिक्षा के वचनों से भी नहीं छोड़ता है । पिता ने फिर कहा कि-हे पुत्र! स्थिर रहो-धीरज धरो, तुम्हारा काम क्रम से करँगा । जैसा कि कहा है- क्रमेण वल्मीकशिखाभिवर्धते
वामी की शिखर क्रम से बढ़ती है, विनय के द्वारा विद्या क्रम से ग्रहण की जाती है, छल के द्वारा शत्रु क्रम से नष्ट किया जाता है और तप के द्वारा मोक्ष क्रम से प्राप्त किया जाता है ॥389॥क्रमेण विद्या विनयेन गृह्यते । क्रमेण शत्रु: कपटेन हन्यते क्रमेण मोक्षस्तपसाधिगम्यते॥389॥ इत्येवं निरूप्य महता प्रपञ्चेन पितापुत्रौ जैनौ जातौ । व्योर्जैनत्वं दृष्ट्वा वृषभदास श्रेठी महासंतुष्टो भूत्वा भणति-अहो एतौ, धन्यौ, मिथ्यात्वं परित्यज्य सन्मार्गे लग्नौ । इत्येकधर्मत्वाद् वृषभदास श्रेष्ठिनो बुद्धसंघेन सह परस्परं भोजनादिकं वितन्वतो बुद्धदासेन सह महती मैत्री जाता । तथा चोक्तम्- इस प्रकार कहकर पिता पुत्र-दोनों बड़े छल से जैनी हो गये । उनका जैनपन देखकर वृषभदास सेठ अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कहता है कि अहो! ये धन्य हैं जो मिथ्यात्व को छोड़कर सन्मार्ग में लग गये । एक धर्म के धारक होने से वृषभदास सेठ बुद्धसंघ के साथ परस्पर भोजनादिक करने लगा, जिससे बुद्धदास के साथ उसकी बड़ी मित्रता हो गयी । जैसा कि कहा है- ददाति प्रतिगृह्वाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।
देता है, लेता है, गुप्त बात कहता है, पूछता है, भोजन करता है और भोजन कराता है; ये छह प्रीति के लक्षण हैं ॥390॥भङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥390॥ एकदा तेन वृषभदास: श्रेष्ठिना बुद्धदास: स्वगृहे भोजनार्थं निमन्त्रित: । भोजन समये स बुद्धदासो भोजनं न करोति । वृषभदासेनोक्तम्-भो बुद्धदास किमर्थं भोजनं न करोषि? तेनोक्तम्-यदि मम पुत्राय स्वकीयां पुत्रीं ददाति चेत् तदा भुज्यते, नान्यथा । वृषभदासेनोक्तम्-अहो, सुहृदो येषां गृह आगच्छन्ति ते धन्या:, विशेषेण त्वत्सदृश: अतएव वयं धन्या: । अवश्यं दास्यामि तव पुत्राय पुत्रीम् । तत: शुभदिने विवाहो जात: । तत: पद्मश्रियं गृहीत्वा बुद्धसंघ: स्वगृहं गत: । पुनरपि तौ बुद्धभक्तौ जातौ । तत्सर्वं दृष्ट्वा श्रुत्वा च वृषभदासश्रेठी विखिन्नो भूत्वा वदत्यहों, गूढप्रपञ्चं कोऽपि न जानाति । उक्तञ्च- एक दिन उस वृषभदास सेठ ने बुद्धदास को अपने घर पर भोजन के लिए निमन्त्रित किया । भोजन के समय बुद्धदास ने भोजन नहीं किया । वृषभदास ने कहा - हे बुद्धदास! भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा - यदि मेरे पुत्र के लिए अपनी पुत्री देओ तो भोजन किया जायेगा अन्यथा नहीं । वृषभदास ने कहा - अहो! मित्र जिनके घर आते हैं, वे धन्य हैं और विशेष तुम्हारे जैसे । अतएव हम धन्य हैं । अवश्य ही तुम्हारे पुत्र के लिए पुत्री दूँगा । तदनन्तर शुभ दिन में विवाह हो गया और पद्मश्री को लेकर बुद्धसंघ अपने घर चला गया । विवाह के बाद पिता-पुत्र दोनों फिर से बुद्ध के भक्त हो गये । यह सब देख सुनकर वृषभदास सेठ ने अत्यन्त खिन्न होकर कहा - अहो । गूढ़ छल को कोई नहीं जानता है । कहा भी है- सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति ।
अच्छी तरह किये हुए कपट के अन्त को ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त कर सकता है । देखो, विष्णु के रूप में तन्तुवाय राजकन्या का सेवन करता रहा ॥391॥कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते ॥391॥ पुनश्च- और भी कहा है - मायामविश्वासविलासमन्दिरं दुराशयो य: कुरुते धनाशया ।
जो दुष्ट अभिप्राय वाला मनुष्य धन की आशा से अविश्वास के क्रीड़ागृह स्वरूप मायाचार को करता है वह पड़ते हुए बहुत भारी अनर्थ को उस तरह नहीं देखता है जिस तरह की दूध पीता हुआ बिलाव पड़ते हुए डंडे को नहीं देखता है ॥392॥सोऽनर्थसारं न पतन्तमीक्षते यथा विडालो लगुडं पय: पिबन् ॥392॥ ततो बुद्धदासबुद्धसंघावाकार्य वृषभदासेन कथितं गृहीत व्रतभङ्गदूषणं च प्रदर्शितम् । तथाहि- पश्चात् वृषभदास सेठ ने बुद्धदास और बुद्धसंघ को बुलाकर कहा तथा व्रतभंग का दोष दिखाया । जैसा कि कहा है - प्राणान्तेऽपि न भङ्गक्तव्यं युक्ताक्षिधृतं व्रतम् ।
गुरु की साक्षीपूर्वक लिया हुआ व्रत, प्राणान्त का अवसर आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि व्रत भंग दु:ख के लिए होता है परन्तु प्राण जन्म-जन्म में प्राप्त होते रहते हैं ॥393॥व्रतभङ्गो हि दु:खाय प्राणा जन्मनि जन्मनि॥393॥ परं किमपि न लग्नं व्योश्चेतसि । वृषभदास: कर्मपरिणतिं विचार्य तूष्णीं स्थित: । एकदा बुद्धदासस्य यो गुरु: पद्मसंघस्तेन पद्मश्रियं प्रति भणितम्-भो पुत्रि सर्वधर्माणां मध्ये बौद्धधर्म एव साधीयान् धर्मो नान्य: । पद्मश्रियोक्तम्-हे पद्मसंघ! सन्मार्गं परित्यज्य नीचमार्गं प्रति कथं मम मन: प्रवर्तते तथा चोक्तम्- परन्तु उन दोनों के चित्त में कुछ नहीं लगा । वृषभदास सेठ कर्मोदय का विचार कर चुप बैठा रहा । एक समय बुद्धदास का गुरु जो पद्मसंघ था उसने पद्मश्री से कहा - हे पुत्रि! सब धर्मों के मध्य में बौद्धधर्म ही सबसे श्रेठ धर्म है अन्य नहीं । पद्मश्री ने कहा - हे पद्मसंघ! सन्मार्ग को छोड़कर नीचमार्ग की ओर मेरा मन कैसे प्रवृत्त हो सकता है ? वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षका बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति ।
जिस प्रकार मृग का मांस खाने वाले सिंह वन में भूखे होने पर भी तृण नहीं खाते । इसी प्रकार कुलीन मनुष्य कष्ट से युक्त होने पर नीच कार्यों का आचरण नहीं करते हैं ॥394॥एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥394॥ अन्यच्च- और भी कहा है - "देव गुरुसमीपे गृहीतानि व्रतानि यस्त्यजति स इह परलोके दु:खी भवति" । नि:सौभाग्यों भवेन्नित्यं धनधान्यादि-विवर्जित: ।
देव तथा गुरु के समीप लिए हुए व्रतों को जो छोड़ता है वह इहलोक तथा परलोक में दु:खी होता है । व्रतहीन मनुष्य निरन्तर सौभाग्यहीन, धन-धान्यादि से रहित, भयभीत और दुखी होता है ॥395॥भीतमूर्ति: सदा दु:खी व्रतहीनश्च मानव:॥395॥ यद्हितं तदा चरणीयं किं लोकजल्पितेन । तथाच- जो काम हितकारी हो उसका आचरण अवश्य करना चाहिए । लोगों के कहने से क्या होता है? जैसा कि कहा है - आत्मना स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्प: ।
अपना हित स्वयं करना चाहिए बहुत बोलने वाले मनुष्य क्या कर लेंगे? क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सब लोगों को संतुष्ट करने वाला हो ॥396॥विद्यते न हि कश्चिदुपाय: सर्वलोक-परितोषकरो य: ॥396॥ एतत्पद्मश्रीवचनं श्रुत्वा पद्मसंघो मौनं कृत्वा स्वगृहं गत: । एवं काले गच्छति कियता कालेन पद्मश्रीपिता वृषभदास: श्रेठी कालधर्मं मत्वा स्वस्य, चतुर्विधसंघसाक्षिकं समस्तजीवेभ्य: क्षमां कृत्वा "मिथ्या मे दुष्कृतं भवत्वित्युच्चार्य चतु:शरणं प्रपद्य पापस्थानानि त्रिधा विसृज्यानशनपूर्वकं नमस्कारान् स्मृत्वा प्राणान् परित्यज्य च स्वर्गं गत: । तेन दु:खेन पद्मश्रीरतीव दु:खिता जाता । श्वसुरपक्षीया विधर्मत्वात् निर्जनीकृतत्वाच्च पराभवन्ति पद्मश्रियं तथापि सा निश्चलचित्ता जिनधर्मं न त्यजति । एकदावसरं प्राप्य बुद्धदासेनोक्तम्-हे वधु! मम गुरुणा तव पितुर्जन्म कथितम्-वृषभदासो मृत्वा, वनमध्ये मृगोऽभूत् । एतद्वचनं श्रुत्वा मनसि महाक्रोधं कृत्वा प्रतारणपरं वचनमभाणि पद्मश्रिया यदि भवतां गुरव एवंविधा ज्ञातारो भवेयुस्तर्हि मया बौद्धव्रतं गृह्यते । पद्मश्रिय एवं विधं वच: श्रुत्वा बुद्धदासो हर्षित: सन् पुनरप्याह-हे वधु ! कल्यं प्रथमं भोजनमस्मद् गुरुभ्य: प्रयच्छ पश्चाद् बुद्धधर्मोच्चारणं कुरु । व्या तथेति प्रतिपन्नम् । द्वितीयेऽह्नि व्या-तेषां बौद्धयतीनां भोजनार्थमामन्त्रणं दत्तम् । ते सर्वेऽपि हर्षिता: समागता: । ततो महतादरेण निजगृहमध्ये उपवेशिता आसनेषु पूजिताश्च । बाह्यप्रदेशस्थं तेषां वामपादस्यैकैकं पादत्राणं चेटिकया प्रच्छन्नं गृहीत्वा सूक्ष्मं यथा भवति तथोत्कृत्य तदीयं तमेनं हिंग्वादि-सुसंस्कृतं विधाय भोजनमध्ये निक्षिप्तम् सर्वेऽपि भोजनं कृत्वा प्रशंसितवन्त: । गन्धलेपनं ताम्बूलादिकं सर्वमपि वितीर्य भणितं व्या-अद्याहं कृतार्था जाता, ममजन्म सफलमभूत् । प्रातर्मया बौद्धव्रतं गृह्यते । तैरुक्तम्-तथास्तु-सर्वेऽपि निर्गमनसमये गुरव: स्वस्ववामपादत्राणं न पश्यन्ति स्म । सर्वत्र विलोकितमपि यदा न पश्यन्ति तदा ते सर्वेऽपि भृत्यादीन् पृच्छन्ति स्म । तैरप्युक्तम्-शपथपूर्वकं न जानीम: । तत: कोलाहलो जात: । सर्वे बुद्धदासादयो मिलिता: । तं कोलाहलं श्रुत्वा पद्मश्रिया भणितम् भवन्तो ज्ञानिन:, त्रिकालविषयं ज्ञानं भवतां स्फुरति । अतो भवद्भि: समस्तं वस्तु प्रदीपवत् प्रकटीक्रियते, पादत्राणस्य का वार्ता? अतो ज्ञानेन पश्यन्तु । तैरुक्तम्-एवं-विधं ज्ञानं नास्ति । पुन: पद्मश्रियाभाणि-भो पूज्या: भवद्भि: कोटिकं घटयितुं न ज्ञायते नन्द्या: सत्यंकार: कथं गृह्यते? इत्याभाणक: सत्यम् विधीयते । तैरुक्तम्-कथमिति । व्या कथितम्-स्वोदरस्थ-चरणत्राणं ज्ञातुं न समर्था: कथमुत्तमसमाधिमरण- प्राप्तस्वर्गस्य मम पितुस्र्व्यिग्गतिं जानन्ति भवन्त:? तदुल्लण्ठ वच: श्रुत्वा तै: सरोषमुक्तम्-रे वाचालि एवंविधमुल्लण्ठ-वचनं केन प्रमाणेन वदसि व्योक्तम् स्वबुद्धया । परं यूयं यतिवरा:, भवतां कोप: सर्वथा न युज्यते । क्रोधात्तपोभ्रंश: सुगति नाशश्च जायते । यदुक्तम्- पद्मश्री के यह वचन सुन पद्मसंघ चुपचाप अपने घर चला गया । इस प्रकार समय व्यतीत होने पर कुछ समय बाद पद्मश्री के पिता वृषभदास सेठ ने अपनी मृत्यु का समय निकट जान चतुर्विध संघ की साक्षीपूर्वक समस्त जीवों से क्षमा माँगी, "मेरे पाप मिथ्या हों" यह कहकर अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म-इन चार की शरण को प्राप्त किया, पाप स्थानों का मन, वचन, काय से त्याग किया, आहार का त्याग किया और पञ्च-नमस्कार-मन्त्र का स्मरण करते हुए, प्राण त्याग कर स्वर्ग प्राप्त किया । इस दु:ख से पद्मश्री अत्यन्त दुखी हो गयी । श्वसुर पक्ष के लोग विधर्मी होने से तथा इसके अकेली रह जाने से उसका तिरस्कार करने लगे परन्तु वह दृढ़चित्त रही और उसने जिनधर्म नहीं छोड़ा । एक समय अवसर पाकर बुद्धदास ने कहा कि-हे वधु! मेरे गुरु ने तुम्हारे पिता का जन्म कहा है-उन्होंने कहा है कि वृषभदास मरकर वन के मध्य हरिण हुआ है । यह वचन सुन मन में बहुत भारी क्रोध कर पद्मश्री ने मायापूर्ण वचन कहा कि-यदि आपके गुरु ऐसे ज्ञाता हैं तो मैं अवश्य ही बौद्धव्रत ग्रहण करती हूँ । पद्मश्री का इस प्रकार का वचन सुन बुद्धदास ने हर्षित होते हुए कहा कि-हे वधु! प्रात:काल पहले हमारे गुरुओं के लिए भोजन देओ पश्चात् बौद्धधर्म धारण करो । पद्मश्री ने बुद्धदास की बात स्वीकार कर ली । दूसरे दिन उसने बौद्ध साधुओं को भोजन के लिए निमन्त्रण दिया । वे सभी साधु हर्षित होकर आ गये । तदनन्तर उन सब साधुओं को अपने घर के भीतर बड़े आदर से आसनों पर बैठाया और सबकी पूजा की । इधर घर के बाहर रखे हुए उन साधुओं के बायें पैर का एक-एक जूता उसने चेटी के द्वारा गुप्तरूप से उठवा लिया और उनके सूक्ष्म टुकड़े कर उनका शाक बनाया तथा हींग आदि से बघार कर और भोजन के मध्य रखकर सब साधुओं को उनका भोजन करा दिया । भोजन के बाद पद्मश्री ने सबकी प्रशंसा की और कहा कि-मैं आज कृतार्थ हो गयी, मेरा जन्म सफल हो गया । गन्ध लेपन तथा पान आदि सब कुछ देकर उसने कहा कि-मैं प्रात:काल बौद्धधर्म ग्रहण करँगी । बौद्ध साधुओं ने "तथास्तु" कहकर स्वीकृति दी । उन सभी गुरुओं ने जब जाने लगे तब अपना बायें पैर का जूता नहीं देखा । सब जगह देखने पर भी जब उन्हें नहीं दिखा तब उन्होंने सेवकों आदि से पूछा । सेवकों ने भी कहा कि-हम लोग शपथपूर्वक कहते हैं कि हम आपके जूतों को नहीं जानते हैं । इससे कोलाहल हो गया और बुद्धदास आदि सभी लोग आ गये । उस कोलाहल को सुनकर पद्मश्री ने कहा कि-आप लोग तो ज्ञानी हैं, तीनों काल की बात को जानने वाला आपका ज्ञान देदीप्यमान है इसीलिए आप समस्त वस्तुओं को दीपक के समान प्रकट कर देते हैं फिर जूतों की बात ही क्या? अत: अपने ज्ञान से देखिये-जूते कहाँ हैं ? साधुओं ने कहा कि-ऐसा ज्ञान नहीं है । पद्मश्री ने पुन: कहा - हे पूज्य जनो! आप लोग, "कोड़ी तो जुटा नहीं सकते हैं, नांदिया का बयाना कैसे लिया जाता है ।" इस कहावत को सिद्ध कर रहे हैं । साधुओं ने कहा - यह कैसे ? पद्मश्री ने कहा कि-आप लोग अपने पेट में स्थित जूतों को जानने के लिए तो समर्थ नहीं हैं फिर उत्तम समाधिमरण के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हमारे पिता की तिर्यंच गति को कैसे जानते हैं ? पद्मश्री के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर साधुओं ने रोष सहित कहा कि-रे बकनेवाली! इस प्रकार का उद्दण्डतापूर्ण वचन किस प्रमाण से कहती है । पद्मश्री ने कहा कि-अपनी बुद्धि से । परन्तु आप लोग उत्तम साधु हैं अत: आपको क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध के कारण मनुष्य तप से भ्रष्ट हो जाता है और उसकी सुगति का नाश हो जाता है । जैसा कि कहा है- क्रोध: परतापकर: सर्वस्योद्वेगकारक: क्रोध: ।
क्रोध, दूसरों को संताप करने वाला है, क्रोध, सबको उद्वेग करने वाला है, क्रोध, वैर को उत्पन्न करने वाला है और क्रोध सुगति को नष्ट करने वाला है ॥397॥वैरानुषङ्गजनक क्रोध: क्रोध: सुगति-हन्ता ॥397॥ तैरुक्तम्-रे पापिठे दुरात्मन्! पादत्राणं किमस्माकमुदरेऽस्ति? व्याभाणि एवमेव, अत्र संदेहो नास्ति । तैरभाणि-चेन्न भविष्यति तदा तव किं कार्यम्? व्योक्तम्-यद्भवतां चित्ते रोचते । बौद्धैर्निरूपितम्-मस्तकं मुण्डयित्वा गृहान्निष्कासनं करिष्याम: । व्या जल्पितम्-एवमस्तु । परं चेद्भविष्यति तदा भवद्भिर्जैनोधर्म: सर्वधर्मनायक: सुगति-दायकोऽङ्गीकरणीय: । तै: कथितम्-एवमेव । पश्चान्मदनफलप्रयोगेण सर्वे वामितास्व्या । तत: सूक्ष्मचर्मखण्डान् स्वस्ववान्तिमध्ये दृष्टा लज्जिता: सन् सरोषं च स्वस्थानं गतवन्त: । तदनन्तरं स्वकीय- समुदायं मेलयित्वा बुद्धदासमाकार्यं कथितं तै: गुरुभि:-रे पापिठ! तवोपदेशेनास्माभि र्भोजनं मानितम् । त्वया स्ववधू-पार्श्वाद् तदवाच्यं कर्मास्माकं कारयितम् । बुद्धदासेन विज्ञप्तम्-हे पूज्य! न मयैतत् कारयितं सर्वथैव । तैरुक्तम्-यद्येवं तर्हि स्वगृहान्निष्कासयेमां पद्मश्रियम्! अन्यथा तव सकलकुटुम्बस्य क्षयो भविष्यति तच्छ्रुत्वा सभ्रान्तेन बुद्धदासेन सर्वं गृहीत्वा पद्मश्रीर्निष्कासिता । तत्स्नेहेन बुद्धसंघोऽपि निर्गतस्व्या सार्धम् । तत: पद्मश्रिया बुद्धसंघं प्रत्युक्तम्-हे स्वामिन्! मम मातृगृहमावां गच्छाव: । तेनोक्तम्-भिक्षाटनंकरोमि परं श्वसुरगृहे न गच्छामि । अस्मिन्नगरे स्थितस्य मम मानभङ्गो भविष्यति । उक्तञ्च- बौद्ध साधुओं ने कहा कि-अरी पापिन! दुरात्मन्! जूते क्या हम लोगों के पेट में हैं? उसने कहा कि-ऐसा ही है, इसमें संदेह नहीं है । साधुओं ने कहा कि-यदि नहीं होंगे तो क्या किया जायेगा? पद्मश्री ने कहा कि-जो आप लोगों के जी में रुचे । बौद्धों ने कहा कि-मस्तक मुड़ा कर घर से निकाल देंगे । उसने कहा - ऐसा हो, परन्तु यदि जूते पेट में होंगे तो आप लोगों को सब धर्मों में प्रमुख तथा सुगति को देने वाला जैनधर्म स्वीकृत करना होगा । उन्होंने कहा - ऐसा हो । पश्चात् मैनार का फल देकर उसने सबको वमन कराया । जिससे अपनी अपनी वान्ति के बीच चमड़े के सूक्ष्म खण्ड देखकर लज्जित होते हुए क्रोध सहित अपने स्थान पर चले गये । तदनन्तर उन बौद्ध गुरुओं ने अपने समुदाय को इकठ्ठा कर तथा बुद्धदास को बुलाकर कहा कि-हे घोर पापी! तेरे उपदेश से हम लोगों ने भोजन का निमन्त्रण माना था परन्तु तूने अपनी वधू की ओर से हम लोगों का वह अवाच्य कार्य कराया । बुद्धदास ने कहा कि-हे पूज्य! यह कार्य मैंने बिलकुल ही नहीं कराया है । बौद्धगुरुओं ने कहा कि-यदि ऐसा है तो इस पद्मश्री को अपने घर से निकाल दो, अन्यथा तुम्हारे सब कुटुम्ब का नाश हो जायेगा । यह सुन घबड़ाये हुए बुद्धदास ने सब कुछ छीनकर पद्मश्री को घर से निकाल दिया । उसके स्नेह से बुद्धसंघ भी उसके साथ निकल गया । तदनन्तर पद्मश्री ने बुद्धसंघ से कहा कि-हे स्वामिन्! हम दोनों हमारी माता के घर चलें । बुद्धसंघ ने कहा कि-भिक्षाटन कर लूँगा परन्तु श्वसुर के घर नहीं जाऊँगा । इस नगर में रहते हुए मेरा मानभंग होगा । क्योंकि कहा है वरं प्राणपरित्यागो न तु मान-विखण्डनम् ।
प्राण त्याग देना अच्छा है परन्तु मानभंग करना अच्छा नहीं है क्योंकि मृत्यु से तो क्षणभर के लिए दु:ख होता है परन्तु मानभंग से प्रतिदिन दु:ख होता है ॥398॥मृत्योश्च क्षणिकं दु:खं मानभङ्गाद्दिने दिने॥398॥ वसेन्मानाधिकं स्थानं मानहीनं विवर्जयेत् । भग्नमानं सुरै: साकं विमानमपि वर्जयेत् ॥399॥ जहाँ सम्मान हो उसी स्थान पर रहना चाहिए, मान रहित स्थान को छोड़ देना चाहिए । देवों के साथ मानरहित होकर विमान में भी बैठने को मिले तो उसे भी छोड़ देना चाहिए ॥399॥ बन्धुमध्ये धनहीनं जीवितं च न सतां रुचिकरम् । तथा चोक्तम्- बन्धुओं के बीच धनहीन जीवन व्यतीत करना सत्पुरुषों के लिए अच्छा नहीं लगता । जैसा कि कहा है - वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रुमालयं पत्रफलादिभोजनम् ।
जो वन व्याघ्र और गजेन्द्रों से भरा हुआ है, जिसमें वृक्ष ही घर है, पत्र तथा फल आदि का भोजन प्राप्त होता है, घास फू स ही शय्या है और वृक्षों के जीर्णशीर्ण वल्कल ही वस्त्र होते हैं ऐसा वन अच्छा है परन्तु बन्धुओं के मध्य धनहीन जीवन बिताना अच्छा नहीं है ॥400॥तृणेषु शय्या तरुजीर्णवल्कलं न बन्धु मध्ये धनहीनजीवनम् ॥400॥ और भी कहा है - किञ्च- उत्तम मनुष्य वे हैं जो अपने गुणों से प्रसिद्ध होते हैं, मध्यम वे हैं जो पिता के गुणों से प्रसिद्धि पाते हैं, अधम वे हैं जो मामा के गुणों से प्रख्यात होते हैं और अधमाधम वे हैं जो श्वसुर के गुणों से प्रसिद्ध होते हैं ॥401॥ इति विमृश्य व्या साकं देशान्तरं चलितो बुद्धसंघ: । ग्रामाद् बहि: सार्थवाहोऽस्य मिलित: । सार्थवाहोऽपि पद्मश्रीरूपं दृष्ट्वा रागान्धो जात: । तत: सार्थवाहेन स्वकार्याय बुद्धसंघस्य मानं दत्तं भोजनार्थं निमन्त्रितश्च । ततो बुद्धसंघ: सार्थवाह-प्रार्थितस्तदुत्तारके स्थित: । सार्थवाहेन वक्षारद्वयसहितायां पिठरिकायामन्नं कारयितम्-एकस्मिन् विषमिश्रितं द्वितीये शुद्धं च । ततो बुद्धसंघस्याकारणं प्रह्वितम् । अथ सार्थवाहबुद्धसंघावेकस्मिन् भाजने भोजनार्थमुपविष्टौ । संकेतितपुरुषेण पृथक्-पृथक् अन्नं परिवेषितम् । तदन्नं पृथग्भूतं दृष्ट्वा शङ्का प्रपन्नेन बुद्धसंघेनैकीकृतम् परस्परेण विषान्नं भुक्त्वा मूर्च्छां गतौ । यदुक्तम्- ऐसा विचार कर बुद्धसंघ पद्मश्री के साथ दूसरे देश को चल पड़ा । गाँव के बाहर उसे एक बंजारा सेठ मिल गया । वह बंजारा भी पद्मश्री का रूप देखकर राग से अन्धा हो गया । तदनन्तर बंजारे सेठ ने अपना कार्य बनाने के लिए बुद्धसंघ को बहुत सम्मान दिया और भोजन के लिए निमन्त्रित किया । पश्चात् बुद्धसंघ सेठ की प्रार्थना से उसके उतरने के स्थान पर जा बैठा । सेठ ने दो खण्ड वाली हण्डी में भोजन बनवाया । एक खण्ड में विषमिश्रित और दूसरे में विषरहित । जब भोजन तैयार हो गया तब सेठ ने बुद्धसंघ को बुलावा भेजा । तदनन्तर सेठ और बुद्धसंघ एक ही बर्तन में भोजन करने के लिए बैठे । जिसे पहले से ही संकेत कर दिया था ऐसे पुरुष ने बर्तन में पृथक्-पृथक् अन्न परोसा । उस अन्न को पृथक् -पृथक् देख बुद्धसंघ को शंका हो गयी इसलिए उसने दोनों अन्नों को इकठ्ठा कर मिला दिया । जिससे परस्पर का विष मिश्रित अन्न खाकर वे दोनों मूर्छा को प्राप्त हो गये । जैसा कि कहा है- अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खल: परव्यसनहृष्ट: ।
दूसरे के कष्ट से हर्षित होने वाला दुष्ट मनुष्य, अपने मरण को भी नहीं गिनता है । सिररहित धड़, युद्ध स्थल में हजारों योद्धाओं का नाश होने पर भी प्राय: नाचता रहता है ॥402॥प्राय: सहस्रनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्ध:॥402॥ निजस्वामिशोकं कुर्वन्त्या पद्मश्रिया कथमपि विभावरी निर्गमिता । प्रभाते बुद्धदासेन स्वपुत्रमूर्च्छनं लोकमुखाच्छ्रुत्वा महाशोकपरेण तत्रागत्य भणितम्-हे शाकिनि त्वया मम पुत्रो भक्षित: । एष सार्थवाहश्च । किं बहुनोक्तेन? मम पुत्रमुत्थापय, एवं सार्थवाहञ्च, अन्यथा तव निग्रहं करिष्यामीत्येवं निरूप्य तस्या: पादमूले पुत्रं संस्थाप्य रोदनं कुर्वन् स्थित: । पद्मश्रिया चिन्तितम्-अहो, मम य: कर्मोदय: समायात: स केन वार्यते? । एवं निश्चित्य कृताञ्जलि र्भूत्वा सा भणति स्म-यदि मम मनसि जिनधर्म-निश्चयोऽस्ति, यद्यहं पतिव्रता भवामि, यदा मया रात्रिभोजनादिकंत्यक्तं भवति तर्हि भो शासनदेवते मम भत्र्ता जीवतु! एष सार्थवाहोऽपि जीवतु । तत: शासनदेवव्या तस्या व्रतमाहात्म्येन सर्वेऽपि जीवन्त: कृता: । ततस्तद् दृष्टवा समस्त नगर-जनैराबालगोपालादिभि: प्रशंसिता । अहो धन्येयं, ईदृग्विधे रूपे वयसि च सत्यपि साधुत्वं धर्मज्ञता च, तदाश्चर्यम् । उक्तञ्च- अपने स्वामी का शोक करती हुई पद्मश्री ने किसी तरह रात्रि व्यतीत की । प्रात:काल बुद्धदास ने लोगों के मुख से अपने पुत्र के मूर्छित होने का समाचार सुना तो वह बहुत भारी शोक करता हुआ वहाँ आकर बोला कि अरी डायन! तूने मेरा पुत्र खा लिया और इस सेठ को भी । बहुत कहने से क्या प्रयोजन है ? तू मेरे पुत्र को खड़ा कर और इस सेठ को अन्यथा तेरा निग्रह करँगा-ऐसा कहकर वह उसके पादमूल में पुत्र को रखकर रोता हुआ बैठ गया । पद्मश्री ने विचार किया कि अहो! मेरा जो कर्मोदय आया है वह किसके द्वारा रोका जा सकता है ? ऐसा निश्चय कर उसने हाथ जोड़कर कहा कि-यदि मेरे मन में जिनधर्म का निश्चय है, यदि मैं पतिव्रता हूँ और यदि मैंने रात्रिभोजनादिक का त्याग किया है तो हे शासनदेवता! मेरा पति जीवित हो जाये और यह सेठ भी । तदनन्तर शासनदेवी ने उसके व्रत के माहात्म्य से सभी को जीवित कर दिया । पश्चात् यह देख नगर के समस्त आबाल गोपाल लोगों ने पद्मश्री की प्रशंसा की । अहो, यह धन्य है कि जो ऐसा रूप और ऐसी अवस्था के रहते हुए भी इसमें साधुता और धर्मज्ञता विद्यमान है । यह बड़ा आश्चर्य है । क्योंकि कहा है - किं चित्रं यदि राजनीतिनिपुणो राजा भवेद्धार्मिक:
यदि राजा, राजनीति में निपुण और धर्मात्मा है तो क्या आश्चर्य की बात है और यदि ब्राह्मण, वेदशास्त्र में निपुण तथा पण्डित है तो इसमें भी क्या आश्चर्य है किन्तु रूप और तारुण्य से युक्त स्त्री यदि साध्वी है तो आश्चर्य है । इसी प्रकार निर्धन मनुष्य यदि पाप नहीं करता है तो आश्चर्य है ॥403॥किं चित्रं यदि वेदशास्त्रनिपुणो विप्रो भवेत् पण्डित: । तच्चित्रं यदि रूप-यौवनवती साध्वी भवेत्कामिनी तच्चित्रं यदि निर्धनोऽपि पुरुष: पापं न कुर्यात् क्वचित् ॥403॥ एतदाश्चर्यं दृष्ट्वा पूजिता लोकैरपि । देवैश्च पञ्चाश्चर्यं दृष्ट्वा पूजिता पद्मश्री: । तत्प्रभावविलोकनाय राजापि सपौरजन: समायात: । महामहसा बुद्धदासेन पद्मश्री: स्वपुत्रेण सममानीता नगरमध्ये । तत्प्रत्यक्षधर्मफलं दृष्ट्वा बुद्धदासकुटुम्बं जिनधर्मानुरक्तं जातम् । एतत्सर्वं प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा च वैराग्यपर:सन् धाडि़वाहनो राजा वदति-अहो, जिनधर्म विहायान्यत्र सर्वेष्टं लभ्यते । अतएवासौ स्वीकत्र्तव्य: । तत: स्वपुत्रं नयविक्रमं राज्ये संस्थाप्य धाडि़वाहनेन राज्ञान्यैश्च बहुभिर्जनैर्यशोधर-मुनिपार्श्वे तपो गृहीतम् । बुद्धदासबुद्धसंघादयश्च श्रावका जाता: । केचन भद्रपरिणामिनो जाता: । बौद्धयव्यो जैना बभूवु: । राज्ञी पद्मावती, बुद्धदासी, वृषभदासभार्यापद्मावतीपद्मश्रीप्रभृव्यश्च सरस्वत्यार्यिकासमीपे तपो जगृहु । पद्मलव्योक्तम्-हे स्वामिन्! एतत् सर्वं मया प्रत्यक्षेण दृष्टमतो मम दृढतरं सम्यक्त्वं जातम् । एतच्छ्रुत्वार्हद्दासेन श्रेष्ठिनोक्तम्-भो भार्ये! यत्त्वया दृष्टं तदहं श्रद्दधामि, इच्छामि, रोचे, अन्याभिश्च तथैव भणितम्! कुन्दलतां प्रत्यपि श्रेष्ठिना भणितम्-हे कुन्दलते । त्वमपि निश्चल चित्ता सती नृत्यादिकं कुरु । तत: कुन्दलव्योक्तम्-सर्वमेतदसत्यम् । अतो नाहं श्रद्दधामि, नेच्छामि, न रोचे । एतत्सर्वमपि निशम्य राज्ञा मन्त्रिणा चौरेण च स्वस्वमनसि भणितम्-अहो, पद्मलव्या यत् प्रत्यक्षेण दृष्टं तदसत्यमिति कथमियं पापिठा कुन्दलता निरूपयति । प्रभातसमये गर्दभे चाटयित्वास्या निग्रहं करियामो वयम् । पुनरपि चौरेण स्वमनसि भणितम्-अहो, दुष्टस्वभावोऽयम् । तथा चोक्तम्- यह आश्चर्य देख लोगों ने पद्मश्री की पूजा की । देवों ने भी पञ्चाश्चर्य कर उसका सम्मान किया । उसका प्रभाव देखने के लिए राजा भी नगरवासियों के साथ आ गया । बुद्धदास, बड़े उत्साहपूर्वक बुद्धसंघ के साथ पद्मश्री को नगर के मध्य ले आया । धर्म के उस प्रत्यक्ष फल को देखकर बुद्धदास का कुटुम्ब जैनधर्म में अनुरक्त हो गया । यह सब प्रत्यक्ष रूप से देख सुनकर राजा धाडि़वाहन वैराग्य में तत्पर होता हुआ कहने लगा कि अहो! जिनधर्म को छोड़ कर अन्य धर्मों से समस्त इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए इसे स्वीकृत करना चाहिए । तदनन्तर अपने पुत्र नयविक्रम को राज्य पर स्थापित कर धाडि़वाहन राजा ने अन्य अनेक जनों के साथ यशोधर मुनि के पास तप ग्रहण कर लिया । बुद्धदास और बुद्धसंघ आदि भी श्रावक हो गये । कितने लोग भद्र परिणामी हो गये । बौद्धसाधु जैन बन गये । रानी पद्मावती, बुद्धदासी, वृषभदास सेठ की स्त्री पद्मावती तथा पद्मश्री आदि ने सरस्वती आर्यिका के समीप तप ग्रहण कर लिया । पद्मलता ने कहा कि-हे स्वामिन्! यह सब मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है इसलिए सुदृढ़ सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ है । यह सुनकर अर्हद्दास सेठ ने कहा कि-हे प्रिये! तुमने जो देखा है उसकी मैं श्रद्धा करता हूँ, उसे चाहता हूँ और उसकी रुचि करता हूँ । अन्य स्त्रियों ने भी ऐसा ही कहा । कुन्दलता के प्रति भी सेठ ने कहा कि-हे कुन्दलते! तुम भी निश्चल चित होकर नृत्यादि करो । पश्चात् कुन्दलता ने कहा कि-वह सब असत्य है इसलिए न मैं श्रद्धा करती हूँ और न इसकी रुचि करती हूँ । यह सब कुछ सुनकर राजा, मन्त्री और चोर ने अपने मन में कहा कि-अहो! पद्मलता ने जो प्रत्यक्ष देखा है उसे यह पापिनी कुन्दलता असत्य कहती है । प्रात:काल गधे पर चढ़ाकर हम लोग इसका निग्रह करेंगे । चोर ने अपने मन में फिर भी कहा कि-अहो! दुष्ट का यह स्वभाव ही है । जैसा कि कहा है - युक्तसङ्गममवेक्ष्य दुर्जन: कुप्यति स्वयमकारणं परम् ।
दुर्जन मनुष्य, योग्य संगम को देखकर स्वयं बिना कारण दूसरे के प्रति क्रोध करता है सो ठीक ही है क्योंकि आकाश में निर्मल चाँदनी को देखकर कुत्ते को छोड़ दूसरा कौन भौंकता है ? ॥404॥चन्द्रिकां नभसि वीक्ष्य निर्मलां क: परो भषति मण्डलाद् विना ॥404॥ ॥ इति षठ कथा॥ ॥इस प्रकार छठवीं कथा पूर्ण हुई॥ |