- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 3) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 4) करता हूं मैं अभिनंदन
- 5) चरणों में आ पडा हूं
- 6) जब एक रत्न अनमोल
- 7) जिन बैन सुनत मोरी
- 8) जिनवर की वाणी से
- 9) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 10) जिनवाणी अमृत रसाल
- 11) जिनवाणी को नमन करो
- 12) जिनवाणी जग मैया
- 13) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 14) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 15) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 16) जिनवाणी माता दर्शन की
- 17) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 18) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 19) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 20) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 21) जिनवानी जान सुजान
- 22) तू कितनी मनहर है
- 23) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 24) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 25) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 26) परम उपकारी जिनवाणी
- 27) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 28) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 29) मंगल बेला आई आज श्री
- 30) मन भाया, तेरे दर आया
- 31) महिमा है अगम
- 32) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 33) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 34) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 35) माता तू दया करके
- 36) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 37) म्हारी माँ जिनवाणी
- 38) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 39) वीर हिमाचल तें निकसी
- 40) शरण कोई नहीं जग में
- 41) शांती सुधा बरसाये
- 42) शास्त्रों की बातों को मन
- 43) सांची तो गंगा
- 44) सारद तुम परसाद तैं
- 45) सीमंधर मुख से
- 46) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 47) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 48) हम लाए हैं विदह से
- 49) हमें निज धर्म पर चलना
- 50) हे जिनवाणी माता तुमको
- 51) हे शारदे माँ
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 8) गुरु समान दाता नहिं
- 9) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 10) गुरुवर तुम बिन कौन
- 11) जंगल में मुनिराज अहो
- 12) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 13) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 14) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 15) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 16) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 17) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 18) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 19) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 20) परम दिगम्बर यती
- 21) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 22) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 23) मुनिवर को आहार
- 24) मैं परम दिगम्बर साधु
- 25) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 26) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 27) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 28) वनवासी सन्तों को नित ही
- 29) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 30) वेष दिगम्बर धार
- 31) शान्ति सुधा बरसा गये
- 32) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 33) श्री मुनि राजत समता संग
- 34) संत साधु बन के विचरूँ
- 35) सम आराम विहारी साधुजन
- 36) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 37) हे परम दिगम्बर यति
- 38) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 39) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनशासन बड़ा निराला
- 6) जैन धर्म के हीरे मोती
- 7) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 8) भावों में सरलता रहती है
- 9) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 10) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 11) ये धर्म हमारा है हमें
- 12) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 13) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 14) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 15) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 16) हर पल हर क्षण हर दम
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
- 1) करना मन ध्यान महामंत्र
- 2) जप जप रे नवकार मंत्र
- 3) जप ले मंत्र सदा नवकार
- 4) जय जय जय कार परमेष्ठी
- 5) जो मंगल चार जगत में हैं
- 6) णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं
- 7) णमोकार नाम का ये कौन मंत्र
- 8) णमोकार मंत्र
- 9) णमोकार मन्त्र को प्रणाम हो
- 10) नमन हमारा अरिहंतों को
- 11) नवकार मंत्र रागों में
- 12) पंच परम परमेष्ठी देखे
- 13) बने जीवन का मेरा आधार रे
- 14) मंत्र जपो नवकार मनुवा
- 15) मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा
- 16) मंत्र नवकारा हृदय में धर
- 17) महामंत्र णमोकार की रचना
- 18) म्हारा पंच प्रभु भगवान
- 19) ये तो सच है कि नवकार
- 20) श्री अरिहंत सदा मंगलमय
- 21) समरो मन्त्र भलो नवकार
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अब हम अमर भये
- 9) अरे मोह में अब ना
- 10) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 11) आओ झूलें मेरे चेतन
- 12) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 13) आज खुशी है आज खुशी है
- 14) आज सी सुहानी
- 15) आतम अनुभव आवै
- 16) आतम अनुभव करना रे भाई
- 17) आतम अनुभव कीजै हो
- 18) आतम जानो रे भाई
- 19) आतमरूप अनूपम है
- 20) आतमरूप सुहावना
- 21) आत्म चिंतन का ये समय
- 22) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 23) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 24) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 25) आनंद स्रोत बह रहा
- 26) आया कहां से
- 27) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 28) इस नगरी में किस विधि
- 29) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 30) ऐ आतम है तुझको नमन
- 31) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 32) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 33) ओ जाग रे चेतन जाग
- 34) ओ जाननहारे जान जगत है
- 35) ओ जीवड़ा तू थारी
- 36) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 37) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 38) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 39) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 40) कर कर आतमहित रे
- 41) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 42) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 43) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 44) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 45) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 46) कृत पूरब कर्म मिटे
- 47) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 48) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 49) कोई राज महल में रोए
- 50) कोई लाख करे चतुराई
- 51) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 52) क्या तन मांझना रे
- 53) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 54) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 55) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 56) गुरुवर जो आपने बताया
- 57) घटमें परमातम ध्याइये
- 58) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 59) चतुर नर चेत करो भाई
- 60) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 61) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 62) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 63) चलो रे भाई अपने वतन
- 64) चेतन अपनो रूप निहारो
- 65) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 66) चेतन जाग रे
- 67) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 68) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 69) चेतन है तू ध्रुव
- 70) चेतना लक्षणम् आनंद
- 71) चेतो चेतन निज में आओ
- 72) चैतन्य के दर्पण में
- 73) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 74) जगत में सम्यक उत्तम
- 75) जन्म जन्म तन धरने
- 76) जब चले आत्माराम
- 77) जहां सत्संग होता है
- 78) जानत क्यों नहिं रे
- 79) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 80) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 81) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 82) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 83) जिया कब तक उलझेगा
- 84) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 85) जीव तू समझ ले आतम
- 86) जीवन के किसी भी पल में
- 87) जीवन के परिनामनि की
- 88) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 89) जैन धरम के हीरे मोती
- 90) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 91) जो आज दिन है वो
- 92) जो इच्छा का दमन
- 93) जो जो देखी वीतराग
- 94) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 95) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 96) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 97) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 98) तू जाग रे चेतन देव
- 99) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 100) तू निश्चय से भगवान
- 101) तू ही शुद्ध है तू ही
- 102) तेरे अंतर में भगवान है
- 103) तोड़ विषयों से मन
- 104) तोरी पल पल
- 105) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 106) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 107) थोड़ा सा उपकार कर
- 108) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 109) देख तेरी पर्याय की हालत
- 110) देखा जब अपने अंतर को
- 111) देखो भाई आतमराम
- 112) देखोजी प्रभु करमन की
- 113) धन धन जैनी साधु
- 114) धनि ते प्रानि जिनके
- 115) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 116) धिक धिक जीवन
- 117) धोली हो गई रे काली कामली
- 118) नर तन को पाकर के
- 119) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 120) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 121) परणति सब जीवन
- 122) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 123) परिग्रह डोरी से झूठ
- 124) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 125) पल पल बीते उमरिया
- 126) पाना नहीं जीवन को
- 127) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 128) पावन हो गई आज ये धरती
- 129) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 130) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 131) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 132) प्रभु पै यह वरदान
- 133) प्रभु शांत छवि तेरी
- 134) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 135) भगवंत भजन क्यों
- 136) भरतजी घर में ही वैरागी
- 137) भला कोई या विध मन
- 138) भले रूठ जाये ये सारा
- 139) भले रूठ जाये ये सारा
- 140) भव भव के दुखड़े हजार
- 141) भूल के अपना घर
- 142) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 143) मन महल में दो
- 144) ममता की पतवार ना तोडी
- 145) ममता तू न गई मोरे
- 146) महावीर--वीर भज ले रे
- 147) माया में फ़ंसे इंसान
- 148) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 149) मितवा रे सुवरण अवसर
- 150) मुझे है स्वामी उस बल
- 151) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 152) मेरा आज तलक प्रभु
- 153) मेरे शाश्वत शरण
- 154) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 155) मैं क्या माँगू भगवान
- 156) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 157) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 158) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 159) मैं निज आतम कब
- 160) मैं राजा तिहुं लोक का
- 161) मैं हूँ आतमराम
- 162) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 163) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 164) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 165) मोह की महिमा देखो
- 166) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 167) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 168) यही इक धर्ममूल है
- 169) या संसार में कोई सुखी
- 170) ये प्रण है हमारा
- 171) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 172) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 173) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 174) वन्दे जिनवरम्
- 175) विराजै रामायण घटमाहिं
- 176) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 177) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 178) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 179) संसार महा अघसागर
- 180) संसार में सुख सर्वदा
- 181) सजधज के जिस दिन
- 182) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 183) सब जग को प्यारा
- 184) समकित सुंदर शांति अपार
- 185) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 186) समझ मन स्वारथ का संसार
- 187) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 188) साधना के रास्ते आत्मा के
- 189) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 190) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 191) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 192) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 193) सुन सतगुरु की सीख
- 194) सुमर सदा मन आतमराम
- 195) सोते सोते ही निकल
- 196) स्वारथ का व्यवहार जग
- 197) हठ तजो रे बेटा हठ
- 198) हम अगर वीर वाणी
- 199) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 200) हम न किसीके कोई न हमारा
- 201) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 202) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 203) हे चेतन चेत जा अब तो
- 204) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 205) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 206) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 207) हे सीमंधर भगवान शरण
- 208) होली--जे सहज होरी के
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) वे कोई अजब तमासा
- 60) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 61) सब विधि करन उतावला
- 62) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 63) सीमंधर स्वामी
- 64) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 65) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 66) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 67) सो गुरुदेव हमारा है
- 68) सो मत सांचो है मन मेरे
- 69) स्वामीजी सांची सरन
- 70) होरी खेलूंगी घर आए
- 71) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
- 1) अरे उड़ चला हंस सैलानी
- 2) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 1) अवधू सूतां क्या इस मठ
- 2) क्योंकर महल बनावै पियारे
- 3) भोर भयो उठ जागो मनुवा
- 1) अरे मन पापनसों नित डरिये
- 2) इक योगी असन बनावे
- 3) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 4) जड़ता बिन आप लखें
- 5) लिया आज प्रभु जी ने
- 6) हिंसा झूठ वचन अरु
- 1) अष्ठाह्निका--जय सिद्धचक्र देवा
- 2) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 3) तुम सुनो सुहागन नार
- 4) भाग्य बिना कछु हाथ न आवे
- 5) मोहि सुन सुन आवे हाँसी
- 6) ये आत्मा क्या रंग दिखाता
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) कुमति को छाड़ो भाई
- 3) चिदानंद भूलि रह्यो सुधि
- 4) जीव तू भ्रमत भ्रमत
- 5) जीव निज रस राचन खोयो
- 6) देखो पुद्गल का परिवारा
- 7) देखो भूल हमारी हम
- 8) निज घर नाय पिछान्या
- 9) महावीर--सिद्धारथ राजा दरबारे
- 10) विषय रस खारे इन्हैं छाड़त
- 1) चिद्रूप हमारा इसका
- 2) भैया मेरे नरभव विषयों
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 18) महावीर जयंती आई
- 19) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 20) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 21) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 22) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 23) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 24) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 25) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 26) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 27) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 28) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 29) होरी खेलूंगी घर आए
- 30) होली--अब घर आये चेतनराज
- 31) होली--अरे मन कैसी होली
- 32) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 33) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 34) होली--और सब मिलि होरि
- 35) होली--कहा बानि परी पिय
- 36) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 37) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 38) होली--खेलौंगी होरी आये
- 39) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 40) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 41) होली--चेतन खेलै होरी
- 42) होली--जे सहज होरी के
- 43) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 44) होली--निजपुर में आज मची
- 45) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 46) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 47) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 1) आरती--बाहुबली भगवान
- 2) बाहुबली भगवान
- 3) हम यही कामना करते हैं
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 1) क्षमावणी
- 2) अक्षय-तृतीया--पण्डित-राजमल-पवैया
- 3) दीपावली-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 4) रक्षाबंधन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 5) वीरशासन-जयन्ती--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) श्रुतपंचमी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 1) अर्घ्य
- 2) महाअर्घ्य
- 3) समुच्चय-महाअर्घ्य
- 4) शांति-पाठ
- 5) शांति-पाठ-भाषा
- 6) विसर्जन-पाठ
- 7) भगवान-आदिनाथ-चालीसा
- 8) भगवान-महावीर-चालीसा
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर जी 'मुख्तार'
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
- 1) छहढाला--पण्डित-द्यानतराय
- 2) छहढाला--पं-दौलतराम
- 3) छहढाला--पं-बुधजन
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
- 1) पंच-परमेष्ठी-आरती--पण्डित-द्यानतराय
- 2) भगवान-चंदाप्रभु-आरती
- 3) भगवान-पार्श्वनाथ-आरती
- 4) भगवान-महावीर-आरती
- 5) भगवान-बाहुबली-आरती
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
- 1) लब्धिसार--नेमिचंद्र-आचार्य
- 2) गोम्मटसार-जीवकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 3) गोम्मटसार-कर्मकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 4) आस्रव-त्रिभंगी--श्रुतमुनी
- 5) भाव-संग्रह--वामदेव-आचार्य
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
- 1) आप्त-मीमांसा
- 2) लघीयस्त्रय--भट्टाकलंकदेव
- 3) परीक्षामुख
- 4) आलापपद्धति--देवसेनाचार्य
- 5) युक्त्यनुशासन--समंतभद्राचार्य
- 6) सन्मतितर्क--सिद्धसेनाचार्य
- 1) श्रुतावतार--इंद्रनंदी-आचार्य
- 2) दर्शनसार--देवसेनाचार्य
- 1) Notes
- 2) Stories
- 3) लोकप्रिय-कथाएँ
- 4) Remember
- 5) समयसार-नाटक
- 6) अर्धकथानक--बनारसीदास
ॐ
🙏

ꣽ
श्री
卐
देव
- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
शास्त्र
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 3) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 4) करता हूं मैं अभिनंदन
- 5) चरणों में आ पडा हूं
- 6) जब एक रत्न अनमोल
- 7) जिन बैन सुनत मोरी
- 8) जिनवर की वाणी से
- 9) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 10) जिनवाणी अमृत रसाल
- 11) जिनवाणी को नमन करो
- 12) जिनवाणी जग मैया
- 13) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 14) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 15) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 16) जिनवाणी माता दर्शन की
- 17) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 18) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 19) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 20) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 21) जिनवानी जान सुजान
- 22) तू कितनी मनहर है
- 23) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 24) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 25) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 26) परम उपकारी जिनवाणी
- 27) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 28) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 29) मंगल बेला आई आज श्री
- 30) मन भाया, तेरे दर आया
- 31) महिमा है अगम
- 32) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 33) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 34) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 35) माता तू दया करके
- 36) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 37) म्हारी माँ जिनवाणी
- 38) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 39) वीर हिमाचल तें निकसी
- 40) शरण कोई नहीं जग में
- 41) शांती सुधा बरसाये
- 42) शास्त्रों की बातों को मन
- 43) सांची तो गंगा
- 44) सारद तुम परसाद तैं
- 45) सीमंधर मुख से
- 46) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 47) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 48) हम लाए हैं विदह से
- 49) हमें निज धर्म पर चलना
- 50) हे जिनवाणी माता तुमको
- 51) हे शारदे माँ
गुरु
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 8) गुरु समान दाता नहिं
- 9) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 10) गुरुवर तुम बिन कौन
- 11) जंगल में मुनिराज अहो
- 12) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 13) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 14) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 15) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 16) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 17) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 18) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 19) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 20) परम दिगम्बर यती
- 21) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 22) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 23) मुनिवर को आहार
- 24) मैं परम दिगम्बर साधु
- 25) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 26) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 27) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 28) वनवासी सन्तों को नित ही
- 29) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 30) वेष दिगम्बर धार
- 31) शान्ति सुधा बरसा गये
- 32) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 33) श्री मुनि राजत समता संग
- 34) संत साधु बन के विचरूँ
- 35) सम आराम विहारी साधुजन
- 36) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 37) हे परम दिगम्बर यति
- 38) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 39) होली खेलें मुनिराज शिखर
धर्म
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनशासन बड़ा निराला
- 6) जैन धर्म के हीरे मोती
- 7) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 8) भावों में सरलता रहती है
- 9) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 10) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 11) ये धर्म हमारा है हमें
- 12) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 13) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 14) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 15) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 16) हर पल हर क्षण हर दम
तीर्थ
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
कल्याणक
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
महामंत्र
- 1) करना मन ध्यान महामंत्र
- 2) जप जप रे नवकार मंत्र
- 3) जप ले मंत्र सदा नवकार
- 4) जय जय जय कार परमेष्ठी
- 5) जो मंगल चार जगत में हैं
- 6) णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं
- 7) णमोकार नाम का ये कौन मंत्र
- 8) णमोकार मंत्र
- 9) णमोकार मन्त्र को प्रणाम हो
- 10) नमन हमारा अरिहंतों को
- 11) नवकार मंत्र रागों में
- 12) पंच परम परमेष्ठी देखे
- 13) बने जीवन का मेरा आधार रे
- 14) मंत्र जपो नवकार मनुवा
- 15) मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा
- 16) मंत्र नवकारा हृदय में धर
- 17) महामंत्र णमोकार की रचना
- 18) म्हारा पंच प्रभु भगवान
- 19) ये तो सच है कि नवकार
- 20) श्री अरिहंत सदा मंगलमय
- 21) समरो मन्त्र भलो नवकार
अध्यात्म
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अब हम अमर भये
- 9) अरे मोह में अब ना
- 10) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 11) आओ झूलें मेरे चेतन
- 12) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 13) आज खुशी है आज खुशी है
- 14) आज सी सुहानी
- 15) आतम अनुभव आवै
- 16) आतम अनुभव करना रे भाई
- 17) आतम अनुभव कीजै हो
- 18) आतम जानो रे भाई
- 19) आतमरूप अनूपम है
- 20) आतमरूप सुहावना
- 21) आत्म चिंतन का ये समय
- 22) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 23) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 24) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 25) आनंद स्रोत बह रहा
- 26) आया कहां से
- 27) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 28) इस नगरी में किस विधि
- 29) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 30) ऐ आतम है तुझको नमन
- 31) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 32) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 33) ओ जाग रे चेतन जाग
- 34) ओ जाननहारे जान जगत है
- 35) ओ जीवड़ा तू थारी
- 36) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 37) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 38) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 39) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 40) कर कर आतमहित रे
- 41) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 42) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 43) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 44) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 45) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 46) कृत पूरब कर्म मिटे
- 47) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 48) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 49) कोई राज महल में रोए
- 50) कोई लाख करे चतुराई
- 51) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 52) क्या तन मांझना रे
- 53) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 54) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 55) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 56) गुरुवर जो आपने बताया
- 57) घटमें परमातम ध्याइये
- 58) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 59) चतुर नर चेत करो भाई
- 60) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 61) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 62) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 63) चलो रे भाई अपने वतन
- 64) चेतन अपनो रूप निहारो
- 65) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 66) चेतन जाग रे
- 67) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 68) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 69) चेतन है तू ध्रुव
- 70) चेतना लक्षणम् आनंद
- 71) चेतो चेतन निज में आओ
- 72) चैतन्य के दर्पण में
- 73) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 74) जगत में सम्यक उत्तम
- 75) जन्म जन्म तन धरने
- 76) जब चले आत्माराम
- 77) जहां सत्संग होता है
- 78) जानत क्यों नहिं रे
- 79) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 80) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 81) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 82) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 83) जिया कब तक उलझेगा
- 84) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 85) जीव तू समझ ले आतम
- 86) जीवन के किसी भी पल में
- 87) जीवन के परिनामनि की
- 88) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 89) जैन धरम के हीरे मोती
- 90) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 91) जो आज दिन है वो
- 92) जो इच्छा का दमन
- 93) जो जो देखी वीतराग
- 94) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 95) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 96) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 97) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 98) तू जाग रे चेतन देव
- 99) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 100) तू निश्चय से भगवान
- 101) तू ही शुद्ध है तू ही
- 102) तेरे अंतर में भगवान है
- 103) तोड़ विषयों से मन
- 104) तोरी पल पल
- 105) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 106) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 107) थोड़ा सा उपकार कर
- 108) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 109) देख तेरी पर्याय की हालत
- 110) देखा जब अपने अंतर को
- 111) देखो भाई आतमराम
- 112) देखोजी प्रभु करमन की
- 113) धन धन जैनी साधु
- 114) धनि ते प्रानि जिनके
- 115) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 116) धिक धिक जीवन
- 117) धोली हो गई रे काली कामली
- 118) नर तन को पाकर के
- 119) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 120) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 121) परणति सब जीवन
- 122) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 123) परिग्रह डोरी से झूठ
- 124) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 125) पल पल बीते उमरिया
- 126) पाना नहीं जीवन को
- 127) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 128) पावन हो गई आज ये धरती
- 129) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 130) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 131) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 132) प्रभु पै यह वरदान
- 133) प्रभु शांत छवि तेरी
- 134) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 135) भगवंत भजन क्यों
- 136) भरतजी घर में ही वैरागी
- 137) भला कोई या विध मन
- 138) भले रूठ जाये ये सारा
- 139) भले रूठ जाये ये सारा
- 140) भव भव के दुखड़े हजार
- 141) भूल के अपना घर
- 142) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 143) मन महल में दो
- 144) ममता की पतवार ना तोडी
- 145) ममता तू न गई मोरे
- 146) महावीर--वीर भज ले रे
- 147) माया में फ़ंसे इंसान
- 148) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 149) मितवा रे सुवरण अवसर
- 150) मुझे है स्वामी उस बल
- 151) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 152) मेरा आज तलक प्रभु
- 153) मेरे शाश्वत शरण
- 154) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 155) मैं क्या माँगू भगवान
- 156) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 157) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 158) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 159) मैं निज आतम कब
- 160) मैं राजा तिहुं लोक का
- 161) मैं हूँ आतमराम
- 162) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 163) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 164) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 165) मोह की महिमा देखो
- 166) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 167) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 168) यही इक धर्ममूल है
- 169) या संसार में कोई सुखी
- 170) ये प्रण है हमारा
- 171) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 172) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 173) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 174) वन्दे जिनवरम्
- 175) विराजै रामायण घटमाहिं
- 176) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 177) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 178) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 179) संसार महा अघसागर
- 180) संसार में सुख सर्वदा
- 181) सजधज के जिस दिन
- 182) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 183) सब जग को प्यारा
- 184) समकित सुंदर शांति अपार
- 185) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 186) समझ मन स्वारथ का संसार
- 187) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 188) साधना के रास्ते आत्मा के
- 189) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 190) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 191) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 192) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 193) सुन सतगुरु की सीख
- 194) सुमर सदा मन आतमराम
- 195) सोते सोते ही निकल
- 196) स्वारथ का व्यवहार जग
- 197) हठ तजो रे बेटा हठ
- 198) हम अगर वीर वाणी
- 199) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 200) हम न किसीके कोई न हमारा
- 201) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 202) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 203) हे चेतन चेत जा अब तो
- 204) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 205) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 206) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 207) हे सीमंधर भगवान शरण
- 208) होली--जे सहज होरी के
पं दौलतराम कृत
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
पं भागचंद कृत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
पं द्यानतराय कृत
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
पं सौभाग्यमल कृत
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
पं भूधरदास कृत
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) वे कोई अजब तमासा
- 60) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 61) सब विधि करन उतावला
- 62) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 63) सीमंधर स्वामी
- 64) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 65) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 66) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 67) सो गुरुदेव हमारा है
- 68) सो मत सांचो है मन मेरे
- 69) स्वामीजी सांची सरन
- 70) होरी खेलूंगी घर आए
- 71) होली--अहो दोऊ रंग भरे
पं बुधजन कृत
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
पं मंगतराय कृत
पं न्यामतराय कृत
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
पं बनारसीदास कृत
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
पं ज्ञानानन्द कृत
पं नयनानन्द कृत
पं मख्खनलाल कृत
पं बुध महाचन्द्र
सहजानन्द वर्णी
पर्व
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 18) महावीर जयंती आई
- 19) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 20) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 21) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 22) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 23) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 24) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 25) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 26) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 27) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 28) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 29) होरी खेलूंगी घर आए
- 30) होली--अब घर आये चेतनराज
- 31) होली--अरे मन कैसी होली
- 32) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 33) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 34) होली--और सब मिलि होरि
- 35) होली--कहा बानि परी पिय
- 36) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 37) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 38) होली--खेलौंगी होरी आये
- 39) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 40) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 41) होली--चेतन खेलै होरी
- 42) होली--जे सहज होरी के
- 43) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 44) होली--निजपुर में आज मची
- 45) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 46) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 47) होली खेलें मुनिराज शिखर
चौबीस तीर्थंकर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
बाहुबली भगवान
बधाई
दस धर्म
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
बच्चों के भजन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
मारवाड़ी
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
selected
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
प्रारम्भ
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
नित्य पूजा
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
तीर्थंकर
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
पर्व पूजन
विसर्जन
पाठ
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर जी 'मुख्तार'
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
स्तोत्र
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
ग्रंथ
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
चरणानुयोग
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
इतिहास
Notes
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पन्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
Youtube -- शास्त्र गाथा
Youtube -- Animations
- भगवान नमिनाथ
- भगवान बाहुबली
- सुकुमाल मुनि
- कुन्दकुन्द आचार्य
- रक्षाबंधन की कथा
- समवसरण
- चार-गति
- श्रुत-पंचमी
- अक्षय-तृतीया
- उद्दायन राजा
- राजा श्रेणिक और मेंढक
- अंजन-चोर की कथा
- पांच-पाप
- जीव-दया
- गर्भ-कल्याणक
- जन्म-कल्याणक
- तप-कल्याणक
- णमोकार-मंत्र
- कुलाचार
- स्थावर-जीव
- तीर्थंकर
- जीव-अजीव
- चतुर्विध-संघ
- प्रात:कालीन वन्दना
प्रमाण
PDF शास्त्र
- गोम्मटसार-जीवकांड
- तत्त्वार्थसूत्र-चार्ट
- तत्त्वार्थसूत्र-English
- पाहुड-दोहा
- तत्त्वानुशासन
- लघुतत्त्व-स्फोट
- परम-अध्यात्म-तरंगिनी
- ज्ञानार्णव
- भगवती-आराधना
- आराधानासार
- जैन-सिद्धांत-प्रवेशिका
- समयसार
- योगसार
- प्रवचनसार
- पन्चास्तिकाय
- द्रव्यसंग्रह
- दर्शनसार
- तत्त्वार्थसूत्र
- आलापपद्धति
- इष्टोपदेश
- परमात्मप्रकाश
- पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
- बारसणुपेक्_खा
- रत्नकरण्ड-श्रावकाचार
- श्रीअष्टपाहुड
- समाधितन्त्र
- स्वरूप-संबोधन
- उत्तर-पुराण
- आदि-पुराण
- आराधना-कथा-कोश
Jain Comics
- FruitsOfAuspiciousActs
- JeevandharSwami
- अज्ञात-प्रतिमा-की-खोज
- आटे-का-मुर्गा
- ऋषभदेव
- कविवर-बनारसीदास
- कुन्दकुन्दाचार्य
- गए-जा-गीत-अपन-के
- गोमटेश्वर-बाहुबली
- चंदनबाला
- चौबीस-तीर्थंकर-१
- चौबीस-तीर्थंकर-२
- जनक-नन्दिनी-सीता
- जीवंधर-स्वामी
- जो-करे-सो-भरे
- टीले-वाले-बाबा
- ताली-एक-हाथ-से-बजती-रही
- तीन-दिन-में
- धर्म-के-दश-लक्षण
- पुण्य-का-फल
- प्रद्युम्न-हरण
- प्रेय-की-भभूत
- महादानी-भामाशाह
- महाबली-हनूमान
- महारानी-चेलना-की-विजय
- मुनि-रक्षा
- राजुल
- रूप-जो-बदला-नहीं-जाता
- सिकन्दर-और-कल्याण-मुनि
Print Granth
Kids Games
कल्याणमन्दिरस्तोत्रम

आ. कुमुदचंद्र कृत / सिद्धसेन-दिवाकर, हिंदी पद्य: पं बनारसीदास
कल्याण-मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि
भीताभय-प्रदमनिन्दितमङ्घ्रि-पद्मम्
संसार-सागर-निमज्जदशेष-जन्तु-
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१॥
कल्याण-मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि
भीताभय-प्रदमनिन्दितमङ्घ्रि-पद्मम्
संसार-सागर-निमज्जदशेष-जन्तु-
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१॥
(दोहा)
परम-ज्योति परमात्मा, परम-ज्ञान परवीन
वंदूँ परमानंदमय घट-घट-अंतर-लीन ॥
(चौपाई)
निर्भयकरन परम-परधान, भव-समुद्र-जल-तारन-यान
शिव-मंदिर अघ-हरन अनिंद, वंदूं पार्श्व-चरण-अरविंद ॥
परम-ज्योति परमात्मा, परम-ज्ञान परवीन
वंदूँ परमानंदमय घट-घट-अंतर-लीन ॥
(चौपाई)
निर्भयकरन परम-परधान, भव-समुद्र-जल-तारन-यान
शिव-मंदिर अघ-हरन अनिंद, वंदूं पार्श्व-चरण-अरविंद ॥
अन्वयार्थ : [कल्याणमंदिरम्] कल्याणकों के मंदिर, [उदारम्] उदार, [अवद्यभेदि] पापों को नष्ट करने वाले, [भीताभयप्रदम्] संसार से डरे हुए जीवों को अभयपद देने वाले, [अनिन्दितम्] प्रशंसनीय और [संसार सागर निमज्जत् अशेष-जन्तु-पोतायमानम्] संसाररूपी समुद्र में डूबते हुए समस्त जीवों के लिए जहाज के समान [जिनेश्वरस्य] जिनेन्द्रभगवान के [अंघ्रिपद्मम्] चरण कमल को [अभिनम्य] नमस्कार करके ।

यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः,
स्तोत्रं सुविस्तृत-मतिर्न विभुर्विधातुम् ।
तीर्थेश्वरस्य कमठ-स्मय-धूमकेतोस्-
तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥
स्तोत्रं सुविस्तृत-मतिर्न विभुर्विधातुम् ।
तीर्थेश्वरस्य कमठ-स्मय-धूमकेतोस्-
तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥
कमठ-मान-भंजन वर-वीर, गरिमा-सागर गुण-गंभीर
सुर-गुरु पार लहें नहिं जास, मैं अजान जापूँ जस तास ॥
सुर-गुरु पार लहें नहिं जास, मैं अजान जापूँ जस तास ॥
अन्वयार्थ : [गरिमाम्बुराशे:] गौरव के समुद्र [यस्य] जिन पार्श्वनाथ की [स्तोत्रम्] स्तुति, [विधातुम्] करने के लिए [स्वयं सुरगुरु:] खुद बृहस्पति भी [सुविस्तृतमति] विस्तृत बुद्धि वाले [विभु-] समर्थ (न अस्ति) नहीं हैं, [कमठस्मयधूमकेतो:] कमठ का मान भस्म करने के लिए अग्निस्वरूप [तस्य] उन [तीर्थेश्वरस्य] पार्श्वनाथ भगवान की [किल] आश्चर्य है कि [एष: अहम्] यह मैं [संस्तवनम्] स्तुति [करिष्ये] करूँगा ।

सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप-
मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः
धृष्टोऽपि कौशिक-शिशुर्यदि वा दिवान्धो
रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः ॥३॥
मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः
धृष्टोऽपि कौशिक-शिशुर्यदि वा दिवान्धो
रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः ॥३॥
प्रभु-स्वरूप अति-अगम अथाह, क्यों हम-सेती होय निवाह
ज्यों दिन अंध उल्लू को होत, कहि न सके रवि-किरण-उद्योत ॥
ज्यों दिन अंध उल्लू को होत, कहि न सके रवि-किरण-उद्योत ॥
अन्वयार्थ : [अधीश!] हे स्वामिन्! [सामान्यत: अपि] सामान्य रीति से भी [तव] तुम्हारे [स्वरूपम्] स्वरूप को [वर्णयितुं] वर्णन करने के लिए [अस्मादृशा:] मुझ जैसे मनुष्य [कथम्] कैसे [अधीशा:] समर्थ [भवन्ति] हो सकते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते । [यदि वा] अथवा [दिवान्ध:] दिन में अंधा रहने वाला [कौशिक शिशु:] उलूक का बच्चा [धृष्ट: अपि] ढीठ होता हुआ भी [किम्] क्या [घर्मरश्मे:] सूर्य के [रूपम्] रूप का [प्ररूपयति किल] वर्णन कर सकता है क्या ?
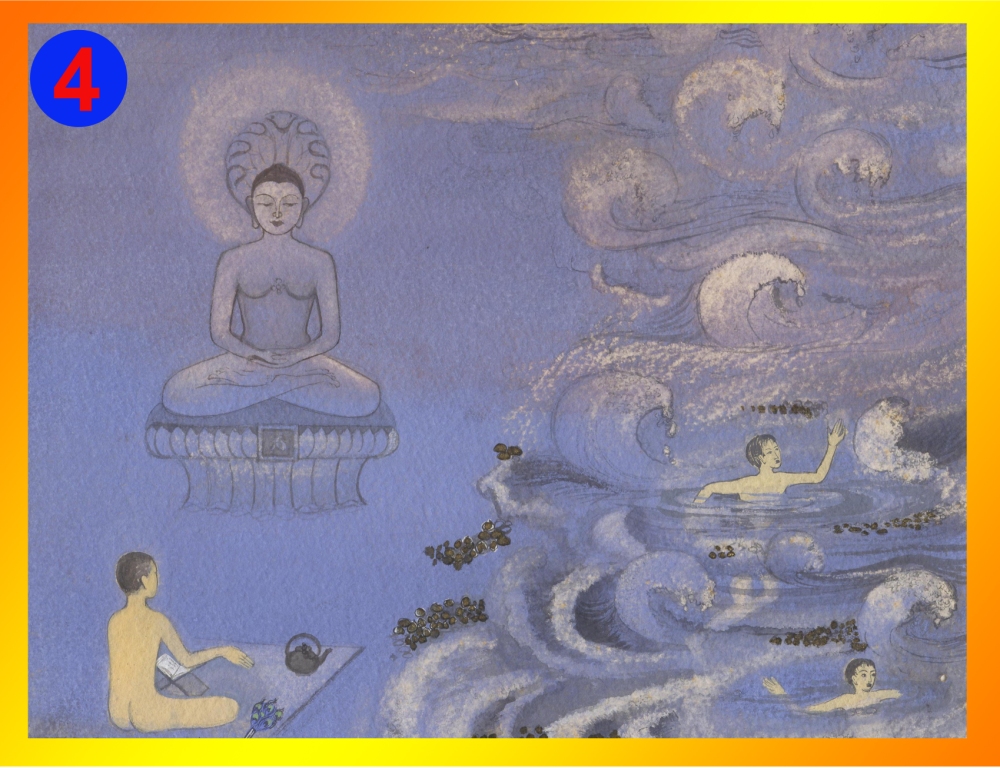
मोह-क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो
नूनं गुणान्गणयितुं न तव क्षमेत ।
कल्पान्त-वान्त-पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्-
मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः ॥४॥
नूनं गुणान्गणयितुं न तव क्षमेत ।
कल्पान्त-वान्त-पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्-
मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः ॥४॥
मोह-हीन जाने मनमाँहिं, तो हु न तुम गुन वरने जाहिं
प्रलय-पयोधि करे जल गौन, प्रगटहिं रतन गिने तिहिं कौन ॥
प्रलय-पयोधि करे जल गौन, प्रगटहिं रतन गिने तिहिं कौन ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे पाश्र्वनाथ! [मत्र्य:] मनुष्य [मोहक्षयात्] मोहनीय कर्म के क्षय से [अनुभवन् अपि] अनुभव करता हुआ भी [तव] आपके [गुणान्] गुणों को [गणयितुम्] गिनने के लिए [नूनम्] निश्चय करके [न क्षमेत] समर्थ नहीं हो सकता है । [यस्मात्] क्योंकि [कल्पान्तवान्तपयस:] प्रलय काल के समय जिसका जल बाहर हो गया है, ऐसे [जलधे:] समुद्र की [प्रकट: अपि] प्रकट हुई भी [रत्नराशि:] रत्नों की राशि [ननु केन मीयेत] किसके द्वारा गिनी जा सकती है?

अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि
कर्तुं स्तवं लसदसंख्य-गुणाकरस्य ।
बालोऽपि किं न निज-बाहु-युगं वितत्य
विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ? ॥५॥
कर्तुं स्तवं लसदसंख्य-गुणाकरस्य ।
बालोऽपि किं न निज-बाहु-युगं वितत्य
विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ? ॥५॥
तुम असंख्य निर्मल गुणखान, मैं मतिहीन कहूँ निज बान
ज्यों बालक निज बाँह पसार, सागर परमित कहे विचार ॥
ज्यों बालक निज बाँह पसार, सागर परमित कहे विचार ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे स्वामिन्! [जडाशय: अपि अहम्] मैं मूर्ख भी [लसदसंख्यगुणाकरस्य] शोभायमान असंख्यात गुणों की खानि स्वरूप [तव] आपके [स्तवम् कर्तुम्] स्तवन करने के लिए [अभ्युद्यत: अस्मि] तैयार हुआ हूँ । क्योंकि [बाल:अपि] बालक भी [स्वधिया] अपनी बुद्धि के अनुसार [निजबाहुयुगम्] अपने दोनों हाथों को [वितत्य] फैलाकर [किम्] क्या [अम्बुराशे:] समुद्र के [विस्तीर्णताम्] विस्तार को [न कथयति] नहीं कहता ?
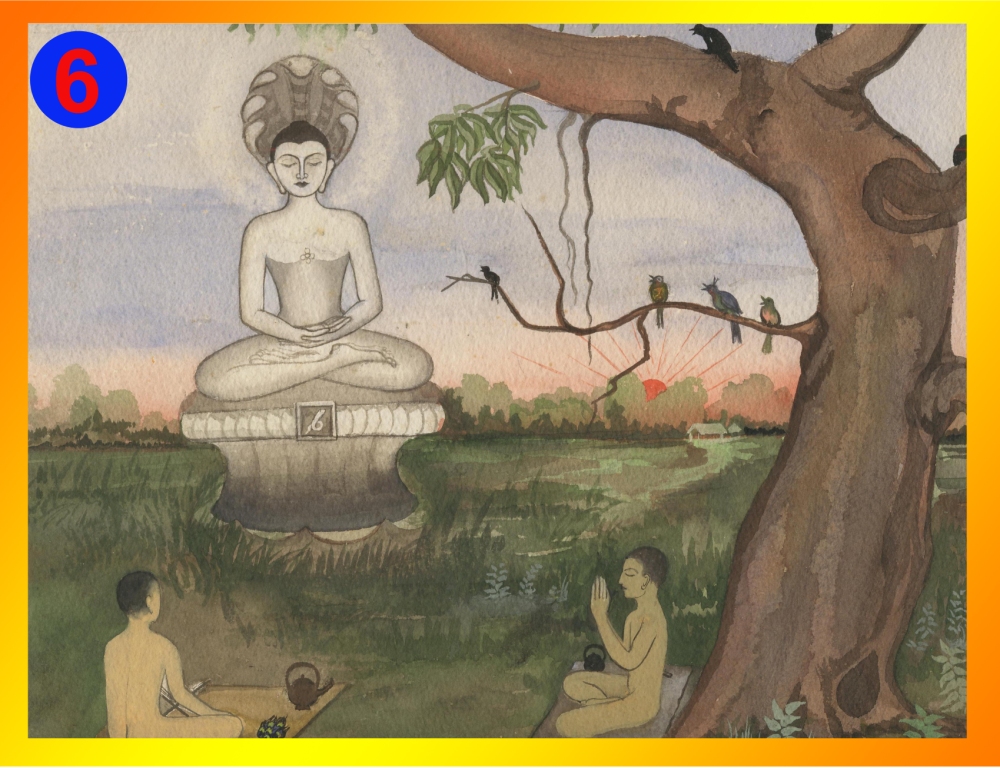
ये योगनामपि न यान्ति गुणास्तवेश !
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ?
जाता तदेवमसमीक्षित-कारितेयं,
जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥६॥
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ?
जाता तदेवमसमीक्षित-कारितेयं,
जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥६॥
जे जोगीन्द्र करहिं तप-खेद, तेऊ न जानहिं तुम गुनभेद
भक्तिभाव मुझ मन अभिलाष, ज्यों पंछी बोले निज भाष ॥
भक्तिभाव मुझ मन अभिलाष, ज्यों पंछी बोले निज भाष ॥
अन्वयार्थ : [ईश!] हे स्वामिन्! [तव] आपके [ये गुणा:] जो गुण [योगिनाम् अपि] योगियों को भी [वत्तुम्] कहने के लिए [न यान्ति] नहीं प्राप्त होते [तेषु] उनमें [मम] मेरा [अवकाश:] अवकाश [कथम् भवति] कैसे हो सकता है? [तत्] इसलिए [एवम्] इस प्रकार [इयम्] मेरा यह [असमीक्षितकारिता जाता] बिना विचारे काम करता हुआ [वा] अथवा [पक्षिण: अपि] पक्षी भी [निजगिरा] अपनी वाणी से [जल्पन्तिननु] बोला करते हैं ।

आस्तामचिन्त्य-महिमा जिन ! संस्तवस्ते,
नामाऽपि पाति भवतो-भवतो जगन्ति ।
तीव्रातपोपहत-पान्थ-जनान्निदाघे
प्रीणाति पद्म-सरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥
नामाऽपि पाति भवतो-भवतो जगन्ति ।
तीव्रातपोपहत-पान्थ-जनान्निदाघे
प्रीणाति पद्म-सरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥
तुम जस-महिमा अगम अपार, नाम एक त्रिभुवन-आधार
आवे पवन पदमसर होय, ग्रीषम-तपन निवारे सोय ॥
आवे पवन पदमसर होय, ग्रीषम-तपन निवारे सोय ॥
अन्वयार्थ : [जिन!] हे जिनेन्द्र! [अचिन्त्य महिमा] अचिंत्य है महात्म्य जिसका ऐसा [ते] आपका [संस्तत:] स्तव [आस्ताम्] दूर रहे, [भवत:] आपका [नाम अपि] नाम भी [जगन्ति] जीवों को [भवत:] संसार से [पाति] बचा लेता है क्योंकि [निदाघे] ग्रीष्मकाल में [तीव्रातपोपहतपान्थजनान्] तीव्र धूप से सताये हुए पथिक जनों को [पद्मसरस:] कमलों के सरोवर का [सरस:] सरस-शीतल [अनिल:अपि] पवन भी [प्रीणाति] सन्तुष्ट करता है ।

हृद्वर्तिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति,
जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्म-बन्धाः
सद्यो भुजंगममया इव मध्य-भाग-
मभ्यागते वन-शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥
जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्म-बन्धाः
सद्यो भुजंगममया इव मध्य-भाग-
मभ्यागते वन-शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥
तुम आवत भवि-जन मनमाँहिं, कर्मनि-बन्ध शिथिल ह्वे जाहिं
ज्यों चंदन-तरु बोलहिं मोर, डरहिं भुजंग भगें चहुँ ओर ॥
ज्यों चंदन-तरु बोलहिं मोर, डरहिं भुजंग भगें चहुँ ओर ॥
अन्वयार्थ : [विभो!] हे पार्श्वनाथ! [त्वयि] आपके [हृद्वर्तिनि] हृदय में रहते हुए [जन्तो:] जीवों के [निविडा: अपि] सघन भी [कर्म-बंधा:] कर्मों के बंधन [क्षणेन] क्षण भर में [वन शिखण्डिनि] वन मयूर के [चन्दनस्य मध्यभागम् अभ्यागते 'सत'] चन्दन तरु के बीच में आने पर [भुजंगममया इव] सर्पों की कुण्डलियों के समान [सद्य:] शीघ्र ही [शिथिली भवन्ति] ढीले हो जाते हैं ।
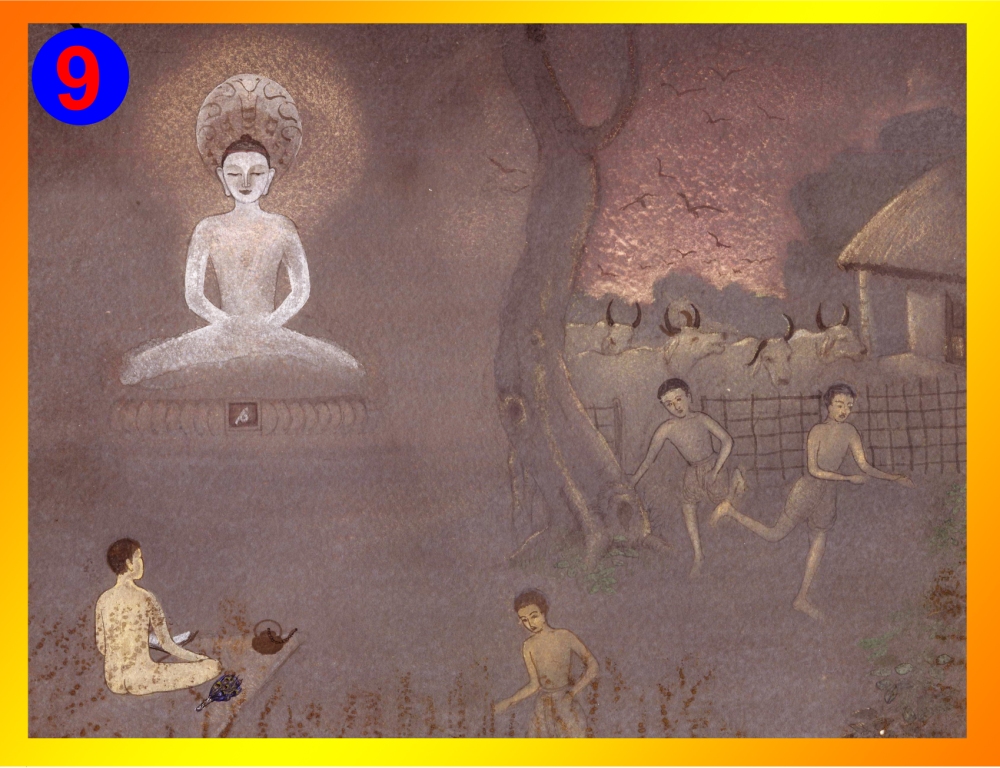
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र !
रौद्रैरुपद्रव-शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।
गोस्वामिनि स्फुरित-तेजसि दृष्टमात्रे
चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥९॥
रौद्रैरुपद्रव-शतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।
गोस्वामिनि स्फुरित-तेजसि दृष्टमात्रे
चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥९॥
तुम निरखत जन दीनदयाल, संकट तें छूटें तत्काल
ज्यों पशु घेर लेहिं निशि चोर, ते तज भागहिं देखत भोर ॥
ज्यों पशु घेर लेहिं निशि चोर, ते तज भागहिं देखत भोर ॥
अन्वयार्थ : [जिनेन्द्र!] हे जिनेन्द्रदेव! [स्पुरिततेजसि] पराक्रमी [गोस्वामिनि] गोपालक [दृष्टमात्रे] दिखते ही [आशु] शीघ्र ही [प्रपलायमानै:] भागते हुए [चौरै:] चोरों के द्वारा [पशव:इव] पशुओं की तरह [त्वयि वीक्षते अपि] आपके दर्शन करते ही [मनुजा:] मनुष्य [रौद्रै:] भयंकर [उपद्रवशतै:] सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा [सहसा एव] शीघ्र ही [मुच्यन्ते] छोड़ दिए जाते हैं ।

त्वं तारको जिन ! कथं भविनां त एव
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ।
यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून-
मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥१०॥
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ।
यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून-
मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥१०॥
तुम भविजन-तारक इमि होहि, जे चित धारें तिरहिं ले तोहि
यह ऐसे करि जान स्वभाव, तिरहिं मसक ज्यों गर्भित बाव ॥
यह ऐसे करि जान स्वभाव, तिरहिं मसक ज्यों गर्भित बाव ॥
अन्वयार्थ : [जिन!] हे जिनेन्द्रदेव! [त्वम् भविनाम् तारक: कथम्] आप संसारी जीवों के तारने वाले कैसे हो सकते हैं? [यत्] क्योंकि [उत्तरन्त:] संसार-समुद्र से पार होते हुए [ते एव] वे ही [हृदयेन] हृदय से [त्वम्] आपको [उद्वहन्ति] तिरा ले जाते हैं [यद्वा] अथवा ठीक है कि [दृति:] मसक [यत्] जो [जलम् तरति] पानी में तैरती है, [स: एष:] वह [नूनम्] निश्चय से [अन्तर्गतस्य] भीतरस्थित [मरुत:] हवा का ही [अनुभाव: किल] प्रभाव है ।

यस्मिन्हर-प्रभृतयोऽपि हत-प्रभावाः
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन
पीतं न किं तदपि दुर्धर-वाडवेन ॥११॥
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन
पीतं न किं तदपि दुर्धर-वाडवेन ॥११॥
जिहँ सब देव किये वश वाम, तैं छिन में जीत्यो सो काम
ज्यों जल करे अगनि-कुल हान, बडवानल पीवे सो पान ॥
ज्यों जल करे अगनि-कुल हान, बडवानल पीवे सो पान ॥
अन्वयार्थ : [यस्मिन्] जिसके विषय में [हरप्रभृतय: अपि] महादेव आदि भी [हतप्रभावा:] प्रभाव रहित हैं [स:] वह [रतिपति:] कामदेव भी [त्वया] आपके द्वारा [क्षणेन] क्षणमात्र में [क्षपित:] नष्टकर दिया गया [अथ] अथवा ठीक है कि [येन पयसा] जिस जल ने [हुतभुज: विध्यापिता:] अग्नि को बुझाया है [तत् अपि] वह जल भी [दुद्र्धरवाडवेन] प्रचण्ड दावानल के द्वारा [किम्] क्या [न पीतम्] नहीं पिया गया ?

स्वामिन्ननल्प-गरिमाणमपि प्रपन्नास्
त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः ।
जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥१२॥
त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः ।
जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥१२॥
तुम अनंत गुरुवा गुन लिए, क्यों कर भक्ति धरूं निज हिये
ह्वै लघुरूप तिरहिं संसार, प्रभु तुम महिमा अगम अपार ॥
ह्वै लघुरूप तिरहिं संसार, प्रभु तुम महिमा अगम अपार ॥
अन्वयार्थ : [स्वामिन्!] हे प्रभो! [अहो] आश्चर्य है कि [अनल्पगरिमाणम् अपि] अधिक गौरव से युक्त भी विरोध पक्ष में अत्यन्त वजनदार [त्वाम्] आपको [प्रपन्ना:] प्राप्त हो [हृदये दधाना:] हृदय में धारण करने वाले [जन्तव:] प्राणी [जन्मोदधिम्] संसार समुद्र को [अति लाघवेन] बहुत ही लघुता से [कथम्] कैसे [लघु] शीघ्र [तरन्ति] तर जाते हैं । [यदि वा] अथवा [हन्त] हर्ष है कि [महताम्] महापुरुषों का [प्रभाव:] प्रभाव [चिन्त्य:] चिन्तवन के योग्य [न भवति] नहीं होता है ।

क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो,
ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः ।
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके
नील-द्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥१३॥
ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः ।
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके
नील-द्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥१३॥
क्रोध-निवार कियो मन शांत, कर्म-सुभट जीते किहिं भाँत
यह पटुतर देखहु संसार, नील वृक्ष ज्यों दहै तुषार ॥
यह पटुतर देखहु संसार, नील वृक्ष ज्यों दहै तुषार ॥
अन्वयार्थ : [विभो!] हे पार्श्वनाथ! [यदि] यदि [त्वया] आपके द्वारा [क्रोध:] क्रोध [प्रथमम्] पहले ही [निरस्त:] नष्ट कर दिया गया था, [तदा] तो फिर [वद] बोलिए कि [कर्मचौरा:] कर्मरूपी चोर [कथम्] कैसे [ध्वस्ता: किल] नष्ट किये? [यदि वा] अथवा [अमुत्त लोके] इस लोक में [हिमानी अपि] बर्प होने पर भी [किम्] क्या [नील द्रुमाणि] हरे-हरे वृक्ष जिनमें ऐसे [विपिनानि] वनों को [न प्लोषति] नहीं जला देता है! अर्थात् जला देता है, मुरझा देता है ।

त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूप-
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज-कोश-देशे ।
पूतस्य निर्मल-रुचेर्यदि वा किमन्य-
दक्षस्य सम्भव-पदं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज-कोश-देशे ।
पूतस्य निर्मल-रुचेर्यदि वा किमन्य-
दक्षस्य सम्भव-पदं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥
मुनिजन हिये कमल निज टोहि, सिद्धरूप सम ध्यावहिं तोहि
कमल-कर्णिका बिन-नहिं और, कमल बीज उपजन की ठौर ॥
कमल-कर्णिका बिन-नहिं और, कमल बीज उपजन की ठौर ॥
अन्वयार्थ : [जिन!] हे पार्श्वनाथ! [योगिन:] ध्यान करने वाले मुनीश्वर [सदा] हमेशा [परमात्मरूपम्] परमात्मस्वरूप [त्वाम्] आपको [हृदयाम्बुजकोषदेशे] अपने हृदयरूपी कमल के मध्य भाग में [अन्वेषयन्ति] खोजते हैं । [यदि वा] अथवा ठीक है कि [पूतस्य] पवित्र और [निर्मल-रुचे:] निर्मल कान्तिवाले [अक्षस्य] कमल के बीज का अथवा शुद्धात्मा का [संभवपदम्] उत्पत्ति स्थान अथवा खोज करने का स्थान [कर्णिकाया: अन्यत्] कमल की डण्ठल को छोड़कर [अन्यत् किम् ननु] दूसरा क्या हो सकता है?

ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन
देहं विहाय परमात्म-दशां व्रजन्ति ।
तीव्रानलादुपल-भावमपास्य लोके
चामीकरत्वमचिरादिव धातु-भेदाः ॥१५॥
देहं विहाय परमात्म-दशां व्रजन्ति ।
तीव्रानलादुपल-भावमपास्य लोके
चामीकरत्वमचिरादिव धातु-भेदाः ॥१५॥
जब तुव ध्यान धरे मुनि कोय, तब विदेह परमातम होय
जैसे धातु शिला-तनु त्याग, कनक-स्वरूप धवे जब आग ॥
जैसे धातु शिला-तनु त्याग, कनक-स्वरूप धवे जब आग ॥
अन्वयार्थ : [जिनेश!] हे पार्श्वनाथ! [लोके] लोक में [तीव्रानलात्] तीव्र अग्नि के संबंध से [धातु भेदा:] अनेक धातुएँ [उपलभावम्] पत्थर रूप पूर्व पर्याय को [अपास्य] छोड़कर [अचिरात्] शीघ्र ही [चामीकरत्वम् इव] जिस तरह सुवर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह [भविन:] भव्य प्राणी [भवत:] आपके [ध्यानात्] ध्यान से [देहम्] शरीर को [विहाय] छोड़कर [क्षणेन] क्षणभर में [परमात्मदशाम्] परमात्मा की अवस्था को [व्रजन्ति] प्राप्त हो जाते हैं ।

अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं
भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ।
एतत्स्वरूपमथ मध्य-विवर्तिनो हि
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥
भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ।
एतत्स्वरूपमथ मध्य-विवर्तिनो हि
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥
जाके मन तुम करहु निवास, विनशि जाय सब विग्रह तास
ज्यों महंत ढिंग आवे कोय, विग्रहमूल निवारे सोय ॥
ज्यों महंत ढिंग आवे कोय, विग्रहमूल निवारे सोय ॥
अन्वयार्थ : [जिन!] हे जिनेन्द्र! [भव्यै:] भव्यजीवों के द्वारा [यस्य] जिस शरीर के [अन्त:] भीतर [त्वम्] आप [सदैव] हमेशा [विभाव्यसे] ध्याये जाते हों [तत्] उस [शरीरम् अपि] शरीर को भी आप [कथम्] क्यों [नाशयसे] नष्ट करा देते हैं? [अथ] अथवा [एतत्स्वरूपम्] यह स्वभाव ही है [यत्] कि [मध्यविवर्तिन:] बीच में रहने वाले और रागद्वेष से रहित [महानुभावा:] महापुरुष [विग्रहम्] विग्रह-शरीर और द्वेष को [प्रशमयन्ति] शान्त करते हैं ।

आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद-बुद्ध्या
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः ।
पानीयमप्यमृत-मित्यनुचिन्त्यमानं
किं नाम नो विष-विकारमपाकरोति ॥१७॥
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः ।
पानीयमप्यमृत-मित्यनुचिन्त्यमानं
किं नाम नो विष-विकारमपाकरोति ॥१७॥
करहिं विबुध जे आतमध्यान, तुम प्रभाव तें होय निदान
जैसे नीर सुधा अनुमान, पीवत विष विकार की हान ॥
जैसे नीर सुधा अनुमान, पीवत विष विकार की हान ॥
अन्वयार्थ : [जिनेन्द्र!] हे पाश्र्वनाथ [मनीषिभि:] बुद्धिमानों के द्वारा [त्वदभेदबुद्ध्या] आप से अभिन्न है ऐसी बुद्धि से [ध्यात:] ध्यान किया गया [अयम् आत्मा] यह आत्मा [भवत्प्रभाव:] आप ही के समान प्रभाव वाला [भवति] हो जाता है [अमृतम् इति अनुचिन्त्यमानम्] यह अमृत है इस तरह चिन्तवन करने वाला [पानीयम् अपि] पानी भी [किम्] क्या [विषविकारम्] विष विकार को [नो अपाकरोति नाम] दूर नहीं करता है ?
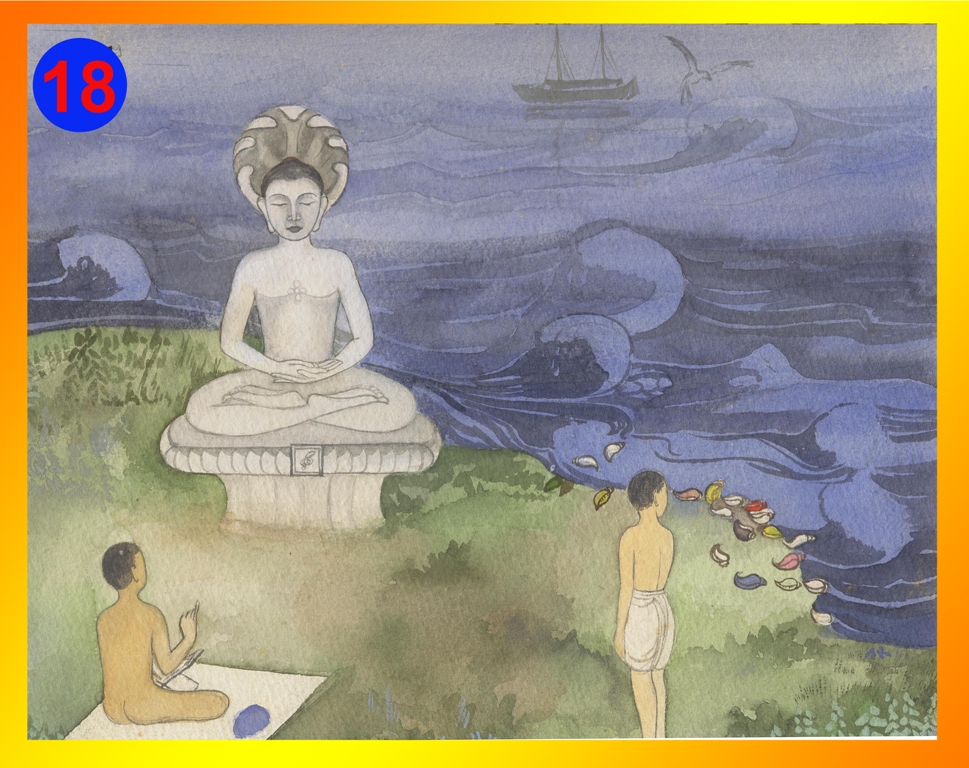
त्वामेव वीत-तमसं परवादिनोऽपि
नूनं विभो हरि-हरादि-धिया प्रपन्नाः ।
किं काच-कामलिभिरीश सितोऽपि शङ्खो
नो गृह्यते विविध-वर्ण-विपर्ययेण ॥१८॥
नूनं विभो हरि-हरादि-धिया प्रपन्नाः ।
किं काच-कामलिभिरीश सितोऽपि शङ्खो
नो गृह्यते विविध-वर्ण-विपर्ययेण ॥१८॥
तुम भगवंत विमल गुणलीन, समल रूप मानहिं मतिहीन
ज्यों पीलिया रोग दृग गहे, वर्ण विवर्ण शंख सों कहे ॥
ज्यों पीलिया रोग दृग गहे, वर्ण विवर्ण शंख सों कहे ॥
अन्वयार्थ : [विभो!] हे पार्श्वनाथ! [परवादिन: अपि] अन्यमतावलम्बी पुरुष भी [वीत-तमसम्] अज्ञान अंधकार से रहित [त्वाम् एव] आपको ही [नूनम्] निश्चय से [हरिहरादिधिया] विष्णु महादेव आदि की कल्पना से [प्रपन्ना:] पूजते हैं । [किम्] क्या [ईश] हे विभो! [काचकामलिभि:] जिनकी आँख पर रंगदार चश्मा है, अथवा जिन्हें पीलिया रोग हो गया है ऐसे पुरुषों द्वारा [शंखसित: अपि] शंख सफेद होने पर भी [विविधवर्णविपर्ययेण] तरह-तरह के विपरीत वर्णों से [नो गृह्यते] नहीं ग्रहण किया जाता है ?

धर्मोपदेश-समये सविधानुभावाद्
आस्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः ।
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि
किं वा विबोधमुपयाति न जीव-लोकः ॥१९॥
आस्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः ।
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि
किं वा विबोधमुपयाति न जीव-लोकः ॥१९॥
(दोहा)
निकट रहत उपदेश सुन, तरुवर भयो 'अशोक'
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविलोक ॥
निकट रहत उपदेश सुन, तरुवर भयो 'अशोक'
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविलोक ॥
अन्वयार्थ : [धर्मोपदेश समये] धर्मोपदेश के समय [ते] आपकी [सविधानुभावात्] समीपता के प्रभाव से [जन:आस्ताम्] मनुष्य तो दूर रहे [तरू: अपि] वृक्ष भी [अशोक:] शोक रहित [भवति] हो जाता है । [वा] अथवा [दिनपतौ अभ्युद्गते 'सति'] सूर्य के उदय होने पर [समहीरुह: अपि जीव लोक:] वृक्षों सहित समस्त जीवलोक [किम्] क्या [विबोधम्] विशेषज्ञान को [न उपयाति] प्राप्त नहीं होते ?

चित्रं विभो कथमवाङ्गमुख-वृन्तमेव
विष्वक्पतत्यविरला सुर-पुष्प-वृष्टिः ।
त्वद्-गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥
विष्वक्पतत्यविरला सुर-पुष्प-वृष्टिः ।
त्वद्-गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥
'सुमन वृष्टि' ज्यों सुर करहिं, हेठ बीठमुख सोहिं
त्यों तुम सेवत सुमन जन, बंध अधोमुख होहिं ॥
त्यों तुम सेवत सुमन जन, बंध अधोमुख होहिं ॥
अन्वयार्थ : [विभो!] हे जिनेन्द्र [चित्तम्] आश्चर्य है कि [विष्वक्] सब ओर [अविरला] व्यवधान रहित [सुरपुष्पवृष्टि:] देवों के द्वारा की हुई फूलों की वर्षा [अवाङ्मुखवृन्तम्] नीचे को बंधन करके ही [कथम्] क्यों [पतति] पड़ती है? [यदि वा] अथवा [मुनीश!] हे मुनियों के नाथ! [त्वद्गोचरे] आपके समीप [सुमनसाम्] पुष्पों अथवा विद्वानों के [बंधनानि] कर्मों के बंधन [नूनम् हि] निश्चय से [अध: एव गच्छन्ति] नीचे को ही जाते हैं ।
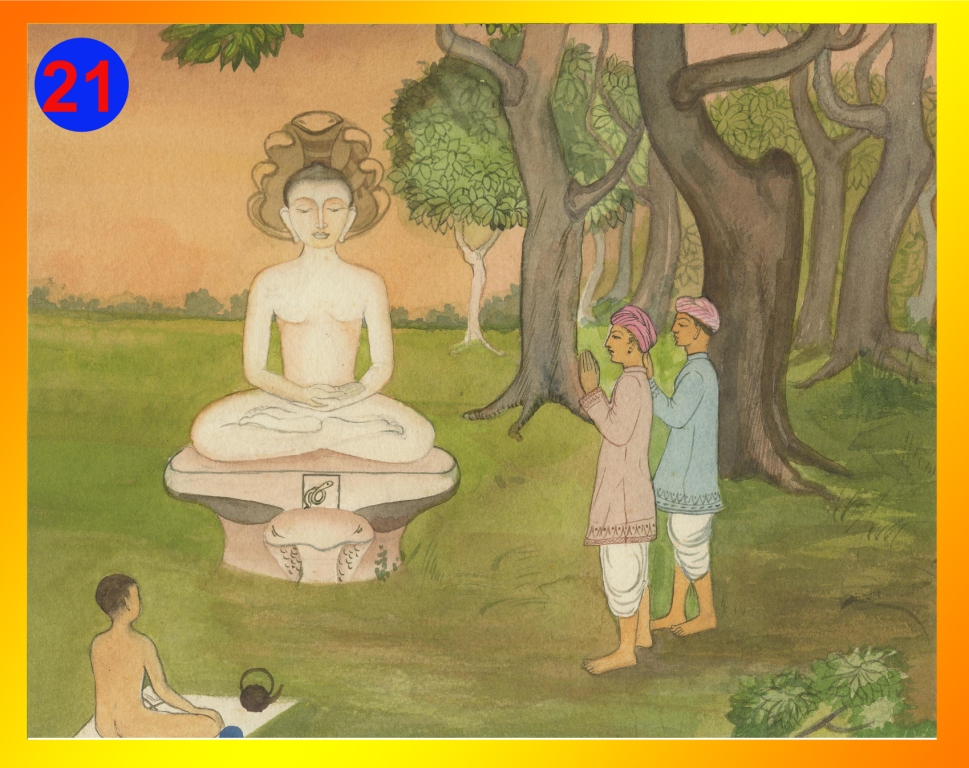
स्थाने गभीर-हृदयोदधि-सम्भवायाः
पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति ।
पीत्वा यतः परम-सम्मद-संग-भाजो
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥२१॥
पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति ।
पीत्वा यतः परम-सम्मद-संग-भाजो
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥२१॥
उपजी तुम हिय उदधि तें, 'वाणी' सुधा समान
जिहँ पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर-पदथान ॥
जिहँ पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर-पदथान ॥
अन्वयार्थ : [गंभीरहृदयोदधिसंभवाया:] गंभीर हृदयरूपी समुद्र में पैदा हुई [तव] आपकी [गिर:] वाणी के [पीयूषताम्] अमृतपने को [स्थाने] ठीक ही [समुदीरयन्ति] प्रकट करते हैं । [यत:] क्योंकि [भव्या:] भव्यजीव [ताम् पीत्वा] उसे पीकर [परमसंमदसङ्गभाज:] परम सुख के भागी होते हुए [तरसा अपि] बहुत ही शीघ्र [अजरामरत्वम्] अजर अमरपने को [व्रजन्ति] प्राप्त होते हैं ।

स्वामिन्! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो,
मन्ये वदन्ति शुचय: सुर-चामरौघा: ।
येऽस्मै नतिं विदधते मुनि-पुङ्गवाय,
ते नूनमूध्र्व-गतय: खलु शुद्ध-भावा:॥२२॥
मन्ये वदन्ति शुचय: सुर-चामरौघा: ।
येऽस्मै नतिं विदधते मुनि-पुङ्गवाय,
ते नूनमूध्र्व-गतय: खलु शुद्ध-भावा:॥२२॥
कहहिं सार तिहुँ-लोक को, ये 'सुर-चामर' दोय
भावसहित जो जिन नमहिं, तिहँ गति ऊरध होय ॥
भावसहित जो जिन नमहिं, तिहँ गति ऊरध होय ॥
अन्वयार्थ : [स्वामिन्] हे प्रभो! [मन्ये] मैं मानता हूँ कि [सुदूरम्] बहुत दूर तक [अवनम्य] नम्रीभूत होकर [समुत्पतन्त:] ऊपर को जाते हुए [शुचय:] पवित्र [सुरचामरौघा] देवों के चामर समूह [वदन्ति] कह रहे हैं कि [ये] जो [अस्मै मुनिपुङ्गवाय] इन श्रेष्ठ मुनि को [नतिम्] नमस्कार [विदधते] करते हैं, [ते] वे [नूनम्] निश्चय से [शुद्ध भावा:] विशुद्ध परिणाम वाले होकर [ऊध्र्वगतय:] ऊध्र्वगति वाले हो जाते हैं ।

श्यामं गभीर-गिरमुज्ज्वल-हेम-रत्न
सिंहासनस्थमिह भव्य-शिखण्डिनस्त्वाम् ।
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्-
चामीकराद्रि-शिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥२३॥
सिंहासनस्थमिह भव्य-शिखण्डिनस्त्वाम् ।
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्-
चामीकराद्रि-शिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥२३॥
'सिंहासन' गिरि मेरु सम, प्रभु धुनि गरजत घोर
श्याम सुतनु घनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ॥
श्याम सुतनु घनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ॥
अन्वयार्थ : [इह] इस लोक में [श्यामं] श्याम वर्ण [गभीरगिरम्] गंभीर दिव्यध्वनि युक्त और [उज्ज्वलहेम रत्नसिंहासनस्थम्] निर्मल सुवर्ण के बने हुए रत्नजड़ित सिंहासन पर स्थित [त्वाम्] आपको [भव्यशिखण्डिन:] भव्य जीवरूपी मयूर [चामीकराद्रिशिरसि] सुवर्णमय मेरुपर्वत के शिखर पर [उच्चै:] जोर से [नदन्तम्] गर्जते हुए [नवाम्बुवाहम् इव] नूतन मेघ की तरह [रभसेन] उत्कण्ठापूर्वक [आलोकयन्ति] देखते हैं ।

उद्गच्छता तव शिति-द्युति-मण्डलेन,
लुप्तच्छदच्छविरशोक-तरुर्बभूव ।
सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !
नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ॥२४॥
लुप्तच्छदच्छविरशोक-तरुर्बभूव ।
सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !
नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ॥२४॥
छवि-हत होत अशोक-दल, तुम 'भामंडल' देख
वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेष ॥
वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेष ॥
अन्वयार्थ : [उद्गच्छता] स्पुâरायमान [तव] आपके [शितिद्युतिमण्डलेन] श्यामप्रभामण्डल के द्वारा [अशोकतरु:] अशोकवृक्ष [लुप्तच्छदच्छवि:] कान्तिहीन पत्रों वाला [बभूव] हो गया, [यदि वा] अथवा [वीतराग!] हे रागद्वेष रहित देव! [तव सान्निध्यत: अपि] आपकी समीपता मात्र से ही [क: सचेतन: अपि] कौन पुरुष सचेतन होकर भी [नीरागताम्] अनुराग के अभाव को [न व्रजति] नहीं प्राप्त होता है ?

भो! भो:! प्रमादमवधूय भजध्वमेन-
मागत्य निर्वृति-पुरीं प्रति सार्थवाहम् ।
एतन्निवेदयति देव! जगत्त्रयाय,
मन्ये नदन्नभिनभ: सुरदुन्दुभिस्ते ॥२५॥
मागत्य निर्वृति-पुरीं प्रति सार्थवाहम् ।
एतन्निवेदयति देव! जगत्त्रयाय,
मन्ये नदन्नभिनभ: सुरदुन्दुभिस्ते ॥२५॥
सीख कहे तिहुँ-लोक को, ये 'सुर-दुंदुभि' नाद
शिवपथ-सारथ-वाह जिन, भजहु तजहु परमाद ॥
शिवपथ-सारथ-वाह जिन, भजहु तजहु परमाद ॥
अन्वयार्थ : [देव:] हे देव [मन्ये] मैं समझता हूँ कि [अभिनभ:] आकाश में सब ओर [नदन्] शब्द करती हुई [ते] आपकी [सुरदुन्दुभि:] देवों के द्वारा बजाई गई दुन्दुभि [जगत्त्रयाय] तीनों लोक के जीवों को [एतत्-निवेदयति] यह बतला रही है कि [भो: भो:] रे रे प्राणियों! [प्रमादम् अवधूय] प्रमाद को छोड़कर [निर्वृतिपुरीम् प्रति सार्थवाहम्] मोक्षपुरी को ले जाने में अगुआ [एवम्] इन भगवान को [आगत्य] आकर [भजध्वम्] भजो ।

उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ !,
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकार: ।
मुक्ता-कलाप-कलितोल्ल-सितातपत्र-
व्याजात्त्रिधा धृत-तनुर्ध्रुवमभ्युपेत: ॥२६॥
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकार: ।
मुक्ता-कलाप-कलितोल्ल-सितातपत्र-
व्याजात्त्रिधा धृत-तनुर्ध्रुवमभ्युपेत: ॥२६॥
'तीन छत्र' त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छवि देत
त्रिविध-रूप धर मनहु शशि, सेवत नखत-समेत ॥
त्रिविध-रूप धर मनहु शशि, सेवत नखत-समेत ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे स्वामिन्! [भवता भुवनेषु उद्योति तेषु] आपके द्वारा तीनों लोकों के प्रकाशित होने पर [विहताधिकार:] अपने अधिकार से भ्रष्ट तथा [मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्रव्याजात्] मोतियों के समूह से सहित अतएव शोभायमान सफेद छत्र के छल से [तारान्वित] ताराओं से वेष्टित [अयम् विधु:] यह चन्द्रमा [त्रिधा धृततनु] तीन-तीन शरीर धारण कर [ध्रुवम्] निश्चय से [अभ्युपेत:] सेवा को प्राप्त हुआ है ।

स्वेन प्रपूरित-जगत्त्रय-पिण्डितेन,
कान्ति-प्रताप-यशसामिव सञ्चयेन ।
माणिक्य-हेम-रजत-प्रविनिर्मितेन,
सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥२७॥
कान्ति-प्रताप-यशसामिव सञ्चयेन ।
माणिक्य-हेम-रजत-प्रविनिर्मितेन,
सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥२७॥
(पद्धरि छन्द)
प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेम,परताप पुंज जिम शुद्ध-हेम
अतिधवल सुजस रूपा समान, तिनके गुण तीन विराजमान ॥
प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेम,परताप पुंज जिम शुद्ध-हेम
अतिधवल सुजस रूपा समान, तिनके गुण तीन विराजमान ॥
अन्वयार्थ : [भगवन्!] हे भगवन्! आप [अभित:] चारों ओर से [प्रपूरित-जगत्त्रयपिण्डितेन] भरे हुए जगत्त्रय के पिण्ड अवस्था को प्राप्त [स्वेन कान्तिप्रतापयशसाम् सञ्चयेन इव] अपने कान्ति, प्रताप और यश के समूह के समान शोभायमान [माणिक्य-हेम-रजत-प्रविनिर्मितेन] माणिक्य, सुवर्ण और चाँदी से बने हुए [सालत्रयेण] तीनों कोटों से [विभासि] शोभायमान होते हैं ।

दिव्य-स्रजो जिन! नमत्त्रिदशाधिपाना-
मुत्सृज्य रत्न-रचितानपि मौलि-बन्धान् ।
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वापरत्र,
त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥
मुत्सृज्य रत्न-रचितानपि मौलि-बन्धान् ।
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वापरत्र,
त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥
सेवहिं सुरेन्द्र कर नमत भाल, तिन सीस मुकुट तज देहिं माल
तुम चरण लगत लहलहे प्रीति, नहिं रमहिं और जन सुमन रीति ॥
तुम चरण लगत लहलहे प्रीति, नहिं रमहिं और जन सुमन रीति ॥
अन्वयार्थ : [जिन!] हे जिनेन्द्र! [दिव्यस्रज:] दिव्यपुरुषों की मालाएँ [नमत्त्रिदशाधिपानाम्] नमस्कार करते हुए इन्द्रों के [रत्न रचितान् अपि मौलिबन्धान्] रत्नों से बने हुए मुकुटों को भी [विहाय] छोड़कर [भवत: पादौ श्रयन्ति] आपके चरणों का आश्रय लेती हैं । [यदि वा] अथवा [त्वत्सङ्गमे] आपका समागम होने पर [सुमनस:] पुष्प अथवा विद्वान पुरुष [परत्र] किसी दूसरी जगह [न एव रमन्ते] नहीं रमण करते हैं ।

त्वं नाथ! जन्मजलधेर्विपराङ्मुखोऽपि,
यत्तारयस्यसुमतो निज-पृष्ठ-लग्नान् ।
युक्त्तं हि पार्थिव-निपस्य सतस्तवैव,
चित्रं विभो! यदसि कर्म-विपाक-शून्य: ॥२९॥
यत्तारयस्यसुमतो निज-पृष्ठ-लग्नान् ।
युक्त्तं हि पार्थिव-निपस्य सतस्तवैव,
चित्रं विभो! यदसि कर्म-विपाक-शून्य: ॥२९॥
प्रभु भोग-विमुख तन करम-दाह, जन पार करत भवजल निवाह
ज्यों माटी-कलश सुपक्व होय, ले भार अधोमुख तिरहिं तोय ॥
ज्यों माटी-कलश सुपक्व होय, ले भार अधोमुख तिरहिं तोय ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे स्वामिन् [त्वम्] आप [जन्मजलधे:] संसाररूप समुद्र से [विपराङ् मुख: अपि सन्] पराङ्मुख होते हुए भी [यत्] जो [निजपृष्ठलग्नान्] अपने पीछे लगे हुए अनुयायी [अनुमत:] जीवों को [तारयसि] तार देते हो, [तत्] वह [पार्थिवनृपस्य सत:] राजाधिराज अथवा मिट्टी के पके हुए घड़े की तरह परिणमन करने वाले [तव] आपको [युक्तम् एव] उचित ही है । परन्तु [विभो!] हे प्रभो! [चित्रम्] आश्चर्य की बात है [यत्] जो आप [कर्मविपाक शून्य: असि] कर्मोदय रूप क्रिया से रहित हो ।

विश्वेश्वरोऽपि जन-पालक! दुर्गतस्त्वं,
किं वाऽक्षर-प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश !
अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव,
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व-विकास-हेतु: ॥३०॥
किं वाऽक्षर-प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश !
अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव,
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व-विकास-हेतु: ॥३०॥
तुम महाराज निरधन निराश,तज तुम विभव सब जगप्रकाश
अक्षर स्वभाव-सु लिखे न कोय, महिमा भगवंत अनंत सोय ॥
अक्षर स्वभाव-सु लिखे न कोय, महिमा भगवंत अनंत सोय ॥
अन्वयार्थ : [जनपालक!] हे जीवों के रक्षक! [त्वम्] आप [जिनेश्वर: अपि दुर्गत:] तीन लोक के स्वामि होकर भी दरिद्र हैं [किं वा] और [अक्षर प्रकृति: अपि त्वम् अलिपि:] अक्षर स्वभाव होकर भी लेखन क्रिया से रहित हैं । [ईश!] हे स्वामिन्! [कथञ्चित्] किसी प्रकार से [अज्ञानवति अपि त्वयि] अज्ञानवान होने पर भी आप में [विश्वविकास हेतु ज्ञानम्] सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान [सदा एव स्पुरति] हमेशा स्पुरायमान रहता है ।

प्राग्भार-सम्भृत-नभांसि रजांसि रोषा-
दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि ।
छायापि तैस्तव न नाथ! हता हताशो,
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥
दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि ।
छायापि तैस्तव न नाथ! हता हताशो,
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥
कोपियो कमठ निज बैर देख, तिन करी धूलि वरषा विशेष
प्रभु तुम छाया नहिं भई हीन, सो भयो पापी लंपट मलीन
प्रभु तुम छाया नहिं भई हीन, सो भयो पापी लंपट मलीन
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे स्वामिन्! [शठेन] मूर्ख [कमठेन] कमठ के द्वारा [रोषात्] क्रोध से [प्राग्भारसम्भृतनभांसि] सम्पूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली [यानि] जो [रजांसि] धूल [उत्थापितानि] आपके ऊपर उड़ाई गई थी [तै:तु] उससे तो [तव] आपकी [छाया अपि] छाया भी [न हता] नहीं नष्ट हुई थी । [परम्] किन्तु [अयमेव दुरात्मा] यही दुष्ट [हताश:] हताश हो [अमीभि:] कर्मरूप रजों से [ग्रस्त:] जकड़ा गया ।

यद्गर्जदूर्जित-घनौघमदभ्र-भीम
भ्रश्यत्तडिन्-मुसल-मांसल-घोरधारम् ।
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर-वारि दध्रे,
तेनैव तस्य जिन! दुस्तर-वारिकृत्यम् ॥३२॥
भ्रश्यत्तडिन्-मुसल-मांसल-घोरधारम् ।
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर-वारि दध्रे,
तेनैव तस्य जिन! दुस्तर-वारिकृत्यम् ॥३२॥
गरजंत घोर घन अंधकार, चमकंत-विज्जु जल मूसल-धार
वरषंत कमठ धर ध्यान रुद्र, दुस्तर करंत निज भव-समुद्र ॥
वरषंत कमठ धर ध्यान रुद्र, दुस्तर करंत निज भव-समुद्र ॥
अन्वयार्थ : [अथ] और [जिन!] हे जिनेश्वर! [दैत्येन] उस कमठ ने [गर्जदूर्जितघनौघम्] खूब गर्ज रहे हैं बलिष्ठ-मेघ-समूह जिसमें [भ्रश्यत्तडित्] गिर रही है बिजली और [मुसलमांसलघोरधारम्] मूसल के समान बड़ी है मोटी धारा जिसमें तथा [अदभ्रभीम] अत्यंत भयंकर [यत्] जो [दुस्तरवारि] अथाह जल [मुक्तम्] वर्षाया था [तेन] उस जलवृष्टि से [तस्य एव] उस कमठ ने ही अपने लिए [दुस्तरवारिकृत्यम्] तीक्ष्ण तलवार का काम कर लिया था ।

ध्वस्तोध्-र्वकेश-विकृताकृति-मर्त्य-मुण्ड-
प्रालम्बभृद्भयदवक्त्र-विनिर्यदग्नि: ।
प्रेतव्रज: प्रति भवन्तमपीरितो य:,
सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भव-दु:ख-हेतु: ॥३३॥
प्रालम्बभृद्भयदवक्त्र-विनिर्यदग्नि: ।
प्रेतव्रज: प्रति भवन्तमपीरितो य:,
सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भव-दु:ख-हेतु: ॥३३॥
(वास्तु छन्द)
मेघमाली मेघमाली आप बल फोरि
भेजे तुरत पिशाच-गण, नाथ-पास उपसर्ग कारण
अग्नि-जाल झलकंत मुख, धुनिकरत जिमि मत्त वारण
कालरूप विकराल-तन, मुंडमाल-हित कंठ
ह्वे निशंक वह रंक निज, करे कर्म दृढ़-गंठ ॥
मेघमाली मेघमाली आप बल फोरि
भेजे तुरत पिशाच-गण, नाथ-पास उपसर्ग कारण
अग्नि-जाल झलकंत मुख, धुनिकरत जिमि मत्त वारण
कालरूप विकराल-तन, मुंडमाल-हित कंठ
ह्वे निशंक वह रंक निज, करे कर्म दृढ़-गंठ ॥
अन्वयार्थ : [तेन असुरेण] उस असुर के द्वारा [ध्वस्तोध्र्वकेशविकृताकृति]मुड़े हुए तथा विकृत आकृति वाले [मर्त्यमुण्डप्रालम्बभृद्] नर कपालों की माला को धारण करने वाले [भयदवक्त्रविनिर्यदग्नि:] जिसके भयंकर मुख से अग्नि निकल रही है, ऐसा [य:] जो [प्रेतव्रज:] पिशाचों का समूह [भवन्तम् प्रति] आपके प्रति [ईरित:] प्रेरित किया गया था [स:] वह [अस्य] उस असुर को [प्रतिभवम्] प्रत्येक भव में [भवदु:ख हेतु:] संसार के दु:खों का कारण [अभवत्] हुआ ।

धन्यास्त एव भुवनाधिप! ये त्रिसंध्य-
माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्य-कृत्या: ।
भक्त्योल्लसत्पुलक-पक्ष्मल-देह-देशा:,
पादद्वयं तव विभो! भुवि जन्मभाज: ॥३४॥
माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्य-कृत्या: ।
भक्त्योल्लसत्पुलक-पक्ष्मल-देह-देशा:,
पादद्वयं तव विभो! भुवि जन्मभाज: ॥३४॥
(चौपाई छन्द)
जे तुम चरण-कमल तिहुँकाल, सेवहिं तजि माया जंजाल
भाव-भगति मन हरष-अपार, धन्य-धन्य जग तिन अवतार ॥
जे तुम चरण-कमल तिहुँकाल, सेवहिं तजि माया जंजाल
भाव-भगति मन हरष-अपार, धन्य-धन्य जग तिन अवतार ॥
अन्वयार्थ : [भुवनाधिप!] हे तीन लोक के नाथ! [ये] जो [जन्मभाज:] प्राणी [विधुतान्यकृत्या:] जिन्होंने अन्य काम छोड़ दिये हैं और [भक्त्या] भक्ति से [उल्लसत्] प्रकट हुए [पक्ष्मलदेहदेशा:] रोमांचों से जिनके शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त है, ऐसे [सन्त:] होते हुए [विधिवत्] विधिपूर्वक [त्रिसन्ध्यम्] तीनों कालों में [तव] आपके [पादद्वयम् आराधयन्ति] चरण युगल की आराधना करते हैं । [विभो!] हे स्वामिन्! [भुवि] संसार में [ते एव] वे ही [धन्या:] धन्य हैं ।

अस्मिन्नपार-भव-वारि-निधौ मुनीश !
मन्ये न मे श्रवण-गोचरतां गतोऽसि ।
आकर्णिते तु तव गोत्र-पवित्र-मन्त्रे,
किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥३५॥
मन्ये न मे श्रवण-गोचरतां गतोऽसि ।
आकर्णिते तु तव गोत्र-पवित्र-मन्त्रे,
किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥३५॥
भवसागर में फिरत अजान, मैं तुव सुजस सुन्यो नहिं कान
जो प्रभु-नाम-मंत्र मन धरे, ता सों विपति भुजंगम डरे ॥
जो प्रभु-नाम-मंत्र मन धरे, ता सों विपति भुजंगम डरे ॥
अन्वयार्थ : [मुनीश!] हे मुनीन्द्र! [मन्ये] मैं समझता हूँ कि [अस्मिन्] इस [अपारभववारिनिधौ] अपार संसाररूप समुद्र में कभी भी [मे] मेरे [कर्णगोचरताम् न गत: असि] कानों की विषयता को प्राप्त नहीं हुए हो । क्योंकि [तु] निश्चय से [तव गोत्र पवित्र मन्त्रे] आपके नामरूपी मंत्र के [आकर्णिते] सुन लेने पर [विपद् विषधरी] विपत्तिरूपी नागिन [किम् वा] क्या [सविधम्] समीप [समेति] आती है ?

जन्मान्तरेऽपि तव पाद-युगं न देव !
मन्ये मया महितमीहित-दान-दक्षम् ।
तेनेह जन्मनि मुनीश! पराभवानां,
जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम् ॥३६॥
मन्ये मया महितमीहित-दान-दक्षम् ।
तेनेह जन्मनि मुनीश! पराभवानां,
जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम् ॥३६॥
मनवाँछित-फल जिनपद माहिं, मैं पूरब-भव पूजे नाहिं
माया-मगन फिर्यो अज्ञान, करहिं रंक-जन मुझ अपमान ॥
माया-मगन फिर्यो अज्ञान, करहिं रंक-जन मुझ अपमान ॥
अन्वयार्थ : [देव!] हे देव! [मन्ये] मैं मानता हूँ कि मैंने [जन्मान्तरे अपि] दूसरे जन्म में भी [ईहितदानदक्षम्] इच्छित फल देने में समर्थ [तव पादयुगम्] आपके चरण कमल [न महितम्] नहीं पूजे, [तेन] उसी से [इह जन्मनि] इस भव में [मुनीश!] हे मुनीश! [अहम्] मैं [मथिताशयानाम्] हृदयभेदी [पराभवानाम्] तिरस्कारों का [निकेतनम्] घर [जात:] हुआ हूँ ।
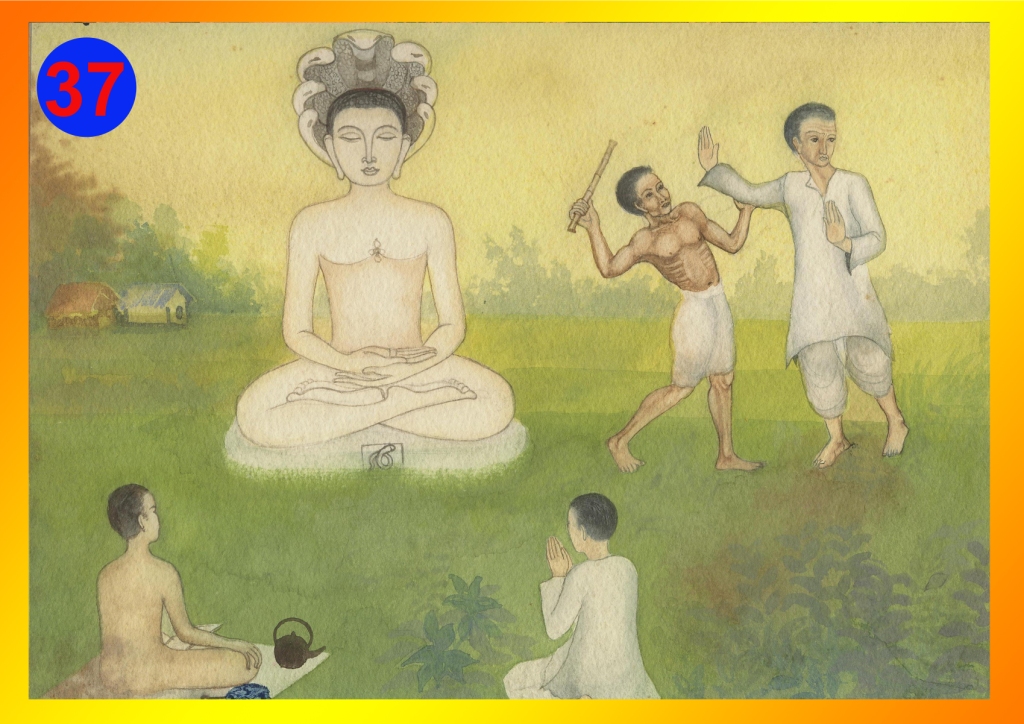
नूनं न मोह-तिमिरावृतलोचनेन,
पूर्वं विभो! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि ।
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था:,
प्रोद्यत्प्रबन्ध-गतय: कथमन्यथैते ॥३७॥
पूर्वं विभो! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि ।
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था:,
प्रोद्यत्प्रबन्ध-गतय: कथमन्यथैते ॥३७॥
मोहतिमिर छायो दृग मोहि, जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि
जो दुर्जन मुझ संगति गहें, मरम छेद के कुवचन कहें ॥
जो दुर्जन मुझ संगति गहें, मरम छेद के कुवचन कहें ॥
अन्वयार्थ : [विभो!] हे स्वामिन्! [मोहतिमिरावृतलोचनेन] मोहरूपी अंधकार से ढके हुए हैं नेत्र जिसके ऐसे [मया] मेरे द्वारा आप [पूर्वम्] पहले कभी [सकृद्अपि] एकबार भी [नूनम्] निश्चय से [प्रविलोकित:न असि] अच्छी तरह अवलोकित नहीं हुए हो, अर्थात् मैंने आपके दर्शन नहीं किए । [अन्यथा हि] नहीं तो [प्रोद्यत्प्रबंधगतय:] जिनमें कर्मबंध की गति बढ़ रही है ऐसे [ऐते] ये [मर्माविध:] मर्मभेदी [अनर्था:] अनर्थ [माम्] मुझे [कथम्] क्यों [विधुरयन्ती] दु:खी करते ?

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव! दु:खपात्रम्,
यस्मात्क्रिया: प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या: ॥३८॥
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव! दु:खपात्रम्,
यस्मात्क्रिया: प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या: ॥३८॥
सुन्यो कान जस पूजे पायँ, नैनन देख्यो रूप अघाय
भक्ति हेतु न भयो चित चाव, दु:खदायक किरिया बिनभाव ॥
भक्ति हेतु न भयो चित चाव, दु:खदायक किरिया बिनभाव ॥
अन्वयार्थ : [जनबान्धव!] हे जगद् बन्धो! [मया] मेरे द्वारा [आकर्णित: अपि] दर्शन किये गये हो [महित: अपि] पूजित भी हुए हो और [निरीक्षित: अपि] अवलोकित भी हुए हो फिर भी [नूनम्] निश्चय है कि [भक्त्या] भक्तिपूर्वक [चेतसि] चित्त में [न विधृत: असि] धारण नहीं किये गये हो । [तेन] उसी से [दु:खपात्रम् जात: अस्मि] दु:खों का पात्र हो रहा हूँ [यस्मात्] क्योंकि [भावशून्या:] भाव रहित [क्रिया:] क्रियाएँ [न प्रति फलन्ति] सफल नहीं होतीं ।

त्वं नाथ! दु:खि-जन-वत्सल! हे शरण्य !
कारुण्य-पुण्य-वसते! वशिनां वरेण्य ।
भक्त्या नते मयि महेश! दयां विधाय,
दुखांकुरोद्दलन-तत्परतां विधेहि ॥३९॥
कारुण्य-पुण्य-वसते! वशिनां वरेण्य ।
भक्त्या नते मयि महेश! दयां विधाय,
दुखांकुरोद्दलन-तत्परतां विधेहि ॥३९॥
महाराज शरणागत पाल, पतित-उधारण दीनदयाल
सुमिरन करहूँ नाय निज-शीश, मुझ दु:ख दूर करहु जगदीश ॥
सुमिरन करहूँ नाय निज-शीश, मुझ दु:ख दूर करहु जगदीश ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे नाथ! [दु:खिजनवत्सल!] हे दुखियों पर प्रेम करने वाले [हे शरण्य] हे शरणागत प्रतिपालक! [कारुण्यपुण्य वसते!] हे दया की पवित्र भूमि! [वशिनाम् वरेण्य] हे जितेन्द्रियों में श्रेष्ठ! और [महेश!] हे महेश्वर! [भक्त्या] भक्ति से [नते मयि] नम्रीभूत मुझ पर [दयाम् विधाय] दया करके [दु:खाज्र्ुर] दु:खाज्र्ुर के [उद्दलन] नाश करने में [तत्परताम्] तत्परता [विधेहि] कीजिए ।

नि:संख्य-सार-शरणं शरणं शरण्य-
मासाद्य सादित-रिपु-प्रथितावदानम् ।
त्वत्पाद-पङ्कजमपि प्रणिधान-वन्ध्यो,
वन्ध्योऽस्मि चेद्भुवन-पावन! हा हतोऽस्मि ॥४०॥
मासाद्य सादित-रिपु-प्रथितावदानम् ।
त्वत्पाद-पङ्कजमपि प्रणिधान-वन्ध्यो,
वन्ध्योऽस्मि चेद्भुवन-पावन! हा हतोऽस्मि ॥४०॥
कर्म-निकंदन-महिमा सार, अशरण-शरण सुजस विस्तार
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥
अन्वयार्थ : [भुवनपावन] हे संसार को पवित्र करने वाले भगवन्! [नि:संख्यसारशरणम्] असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की [शरणम्] रक्षा करने वाले [शरण्यम्] शरणागत प्रतिपालक और [सादितरिपुप्रथितावदानम्] कर्मशत्रुओं के नाश से प्रसिद्ध है, पराक्रम जिनका ऐसे [त्वत्पादपज्र्जम्] आपके चरणकमलों को [आसाद्य अपि] पाकर भी [प्रणिधानबन्ध्य:] उनके ध्यान से रहित हुआ मैं [बन्ध्य: अस्मि] फलहीन हूँ [तत्] उससे [हा] खेद है कि मैं [हत: अस्मि] नष्ट हुआ जा रहा हूँ ।

देवेन्द्रवन्द्य! विदिताखिल-वस्तु-सार !
संसार-तारक! विभो! भुवनाधिनाथ! ।
त्रायस्व देव! करुणा-हृद! मां पुनीहि,
सीदन्तमद्य भयद-व्यसनाम्बुराशे: ॥४१॥
संसार-तारक! विभो! भुवनाधिनाथ! ।
त्रायस्व देव! करुणा-हृद! मां पुनीहि,
सीदन्तमद्य भयद-व्यसनाम्बुराशे: ॥४१॥
सुर-गन-वंदित दया-निधान, जग-तारण जगपति अनजान
दु:ख-सागर तें मोहि निकासि, निर्भय-थान देहु सुख-रासि ॥
दु:ख-सागर तें मोहि निकासि, निर्भय-थान देहु सुख-रासि ॥
अन्वयार्थ : [देवेन्द्रवन्द्य!] हे इन्द्रों के वन्दनीय! [विदिताखिलवस्तुसार!] हे सब पदार्थों के रहस्य को जानने वाले! [संसारतारक!] हे संसार समुद्र से तारने वाले! [विभो!] हे प्रभो! [भुवनाधिनाथ!] हे तीन लोक के स्वामिन्! [करुणाहृद] हे दया के सरोवर! [देव] देव! [अद्य] आज [सीदन्तम्] तड़पते हुए [माम्] मुझको [भयदव्यसनाम्बुराशे:] भयंकर दु:खों के समुद्र से [त्रायस्व] बचाओ और [पुनीहि] पवित्र करो ।

यद्यस्ति नाथ! भवदङ्घ्रि-सरोरुहाणां,
भक्ते: फलं किमपि सन्ततसञ्चिताया: ।
तन्मे त्वदेक-शरणस्य शरण्य! भूया:,
स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥
भक्ते: फलं किमपि सन्ततसञ्चिताया: ।
तन्मे त्वदेक-शरणस्य शरण्य! भूया:,
स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥
मैं तुम चरण कमल गुणगाय, बहु-विधि-भक्ति करी मनलाय
जनम-जनम प्रभु पाऊँ तोहि, यह सेवाफल दीजे मोय ॥
जनम-जनम प्रभु पाऊँ तोहि, यह सेवाफल दीजे मोय ॥
अन्वयार्थ : [नाथ!] हे नाथ! [त्वदेकशरणस्य] केवल आप ही की है शरण जिसको ऐसे मुझे [सन्तत सञ्चिताया:] चिरकाल से सञ्चित-एकत्रित हुई [भवदंघ्रिसरोरुहाणाम्] आपके चरण कमलों की [भ्क्ते:] भक्ति का [यदि] यदि [किमपि फलम् अस्ति] कुछ फल हो, [तत्] तो उससे [शरण्य] हे शरणागत प्रतिपालक! [त्वम् एव] आप ही [अत्र भुवने] इस लोक में और [भवान्तरे अपि] परलोक में भी [स्वामि] मेरे स्वामी [भूया:] होवें ।
इत्थं समाहित-धियो विधिवज्जिनेन्द्र !
सान्द्रोल्लसत्पुलक-कञ्चुकिताङ्गभागा: ।
त्वद्बिम्ब-निर्मल-मुखाम्बुज-बद्ध-लक्ष्या,
ये संस्तवं तव विभो! रचयन्ति भव्या: ॥४३॥
जननयन 'कुमुदचन्द्र' प्रभास्वरा: स्वर्ग-सम्पदो भुक्त्वा ।
ते विगलित-मल-निचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥
सान्द्रोल्लसत्पुलक-कञ्चुकिताङ्गभागा: ।
त्वद्बिम्ब-निर्मल-मुखाम्बुज-बद्ध-लक्ष्या,
ये संस्तवं तव विभो! रचयन्ति भव्या: ॥४३॥
जननयन 'कुमुदचन्द्र' प्रभास्वरा: स्वर्ग-सम्पदो भुक्त्वा ।
ते विगलित-मल-निचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥
(बेसरी छंद - षड्पद)
इहविधि श्री भगवंत, सुजस जे भविजन भाषहिं
ते निज पुण्यभंडार, संचि चिर-पाप प्रणासहिं ॥
रोम-रोम हुलसंति अंग प्रभु-गुण मन ध्यावहिं
स्वर्ग संपदा भुंज वेगि पंचमगति पावहिं ॥
यह कल्याणमंदिर कियो, कुमुदचंद्र की बुद्धि
भाषा कहत 'बनारसी', कारण समकित-शुद्धि ॥
इहविधि श्री भगवंत, सुजस जे भविजन भाषहिं
ते निज पुण्यभंडार, संचि चिर-पाप प्रणासहिं ॥
रोम-रोम हुलसंति अंग प्रभु-गुण मन ध्यावहिं
स्वर्ग संपदा भुंज वेगि पंचमगति पावहिं ॥
यह कल्याणमंदिर कियो, कुमुदचंद्र की बुद्धि
भाषा कहत 'बनारसी', कारण समकित-शुद्धि ॥
अन्वयार्थ : [जिनेन्द्र विभो!] हे जिनेन्द्रदेव! [ये भव्या:] जो भव्यजन [इत्थम्] इस तरह [समाहितधिय:] सावधानबुद्धि से युक्त हो [त्वद्बिम्बनिर्मल-मुखाम्बुजबद्धलक्ष्या:] आपके निर्मल मुख कमल पर बांधा है लक्ष्य जिन्होंने ऐसे [सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकितांगभागा:] सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से व्याप्त है शरीर के अवयव जिनके ऐसे [सन्त:] होते हुए [विधिवत्] विधिपूर्वक [तव] आपका [संस्तवनम्] स्तोत्र [रचयन्ति] रचते हैं, [ते] वे [जननयनकुमुदचन्द्र] हे प्राणियों के नेत्ररूपी कुमुदों-कमलों को विकसित करने के लिए चन्द्रमा की तरह शोभायमान देव! [प्रभास्वरा:] दैदीप्यमान [स्वर्गसम्पद:] स्वर्ग की सम्पत्तियों को [भुक्त्वा] भोगकर [विगलित मलनिचया:] कर्मरूपी मल से रहित हो [अचिरात्] शीघ्र ही [मोक्षम् प्रपद्यन्ते] मुक्ति को पाते हैं ।
