- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) आत्मा_ही_समयसार
- 3) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 4) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 5) करता हूं मैं अभिनंदन
- 6) चरणों में आ पडा हूं
- 7) जब एक रत्न अनमोल
- 8) जिन बैन सुनत मोरी
- 9) जिनवर की वाणी से
- 10) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 11) जिनवाणी अमृत रसाल
- 12) जिनवाणी को नमन करो
- 13) जिनवाणी जग मैया
- 14) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 15) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 16) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 17) जिनवाणी माता दर्शन की
- 18) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 19) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 20) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 21) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 22) जिनवानी जान सुजान
- 23) तू कितनी मनहर है
- 24) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 25) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 26) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 27) परम उपकारी जिनवाणी
- 28) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 29) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 30) मंगल बेला आई आज श्री
- 31) मन भाया, तेरे दर आया
- 32) महिमा है अगम
- 33) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 34) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 35) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 36) माता तू दया करके
- 37) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 38) म्हारी माँ जिनवाणी
- 39) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 40) वीर हिमाचल तें निकसी
- 41) शरण कोई नहीं जग में
- 42) शांती सुधा बरसाये
- 43) शास्त्रों की बातों को मन
- 44) सांची तो गंगा
- 45) सारद तुम परसाद तैं
- 46) सीमंधर मुख से
- 47) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 48) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 49) हम लाए हैं विदह से
- 50) हमें निज धर्म पर चलना
- 51) हे जिनवाणी माता तुमको
- 52) हे शारदे माँ
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु बिन सूनो लगे संसार
- 8) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 9) गुरु समान दाता नहिं
- 10) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 11) गुरुवर तुम बिन कौन
- 12) गुरुवर थारी परिणति अंतरमयी
- 13) जंगल में मुनिराज अहो
- 14) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 15) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 16) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 17) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 18) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 19) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 20) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 21) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 22) परम दिगम्बर यती
- 23) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 24) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 25) मुनिवर को आहार
- 26) मैं परम दिगम्बर साधु
- 27) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 28) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 29) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 30) वनवासी सन्तों को नित ही
- 31) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 32) वेष दिगम्बर धार
- 33) शान्ति सुधा बरसा गये
- 34) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 35) श्री मुनि राजत समता संग
- 36) संत साधु बन के विचरूँ
- 37) सम आराम विहारी साधुजन
- 38) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 39) हे परम दिगम्बर यति
- 40) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 41) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनको जिनधर्म सुहाया 2
- 6) जिनको जिनधर्म सुहाया
- 7) जिनशासन बड़ा निराला
- 8) जैन धर्म के हीरे मोती
- 9) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 10) भावों में सरलता रहती है
- 11) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 12) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 13) ये धर्म हमारा है हमें
- 14) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 15) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 16) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 17) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 18) हर पल हर क्षण हर दम
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब प्रभु चरण छोड़ कित जाऊँ
- 8) अब मेरे समकित सावन
- 9) अब हम अमर भये
- 10) अरे मोह में अब ना
- 11) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 12) आओ झूलें मेरे चेतन
- 13) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 14) आज अद्भुत छवि निज निहारी
- 15) आज खुशी है आज खुशी है
- 16) आज सी सुहानी
- 17) आतम अनुभव आवै
- 18) आतम अनुभव करना रे भाई
- 19) आतम अनुभव कीजै हो
- 20) आतम जानो रे भाई
- 21) आतमरूप अनूपम है
- 22) आतमरूप सुहावना
- 23) आत्म चिंतन का ये समय
- 24) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 25) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 26) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 27) आनंद स्रोत बह रहा
- 28) आया कहां से
- 29) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 30) इस नगरी में किस विधि
- 31) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 32) ऐ आतम है तुझको नमन
- 33) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 34) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 35) ओ जाग रे चेतन जाग
- 36) ओ जाननहारे जान जगत है
- 37) ओ जीवड़ा तू थारी
- 38) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 39) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 40) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 41) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 42) कर कर आतमहित रे
- 43) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 44) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 45) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 46) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 47) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 48) कृत पूरब कर्म मिटे
- 49) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 50) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 51) कोई राज महल में रोए
- 52) कोई लाख करे चतुराई
- 53) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 54) क्या तन मांझना रे
- 55) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 56) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 57) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 58) गुरुवर जो आपने बताया
- 59) घटमें परमातम ध्याइये
- 60) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 61) चतुर नर चेत करो भाई
- 62) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 63) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 64) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 65) चलो रे भाई अपने वतन
- 66) चेतन अपनो रूप निहारो
- 67) चेतन को मिला जब नर तन तो
- 68) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 69) चेतन जाग रे
- 70) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 71) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 72) चेतन है तू ध्रुव
- 73) चेतना लक्षणम् आनंद
- 74) चेतो चेतन निज में आओ
- 75) चैतन्य के दर्पण में
- 76) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 77) जगत में सम्यक उत्तम
- 78) जन्म जन्म तन धरने
- 79) जब चले आत्माराम
- 80) जहां सत्संग होता है
- 81) जानत क्यों नहिं रे
- 82) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 83) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 84) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 85) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 86) जिया कब तक उलझेगा
- 87) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 88) जीव तू समझ ले आतम
- 89) जीवन के किसी भी पल में
- 90) जीवन के परिनामनि की
- 91) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 92) जैन धरम के हीरे मोती
- 93) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 94) जो आज दिन है वो
- 95) जो इच्छा का दमन
- 96) जो जो देखी वीतराग
- 97) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 98) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 99) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 100) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 101) तू जाग रे चेतन देव
- 102) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 103) तू निश्चय से भगवान
- 104) तू ही शुद्ध है तू ही
- 105) तेरे अंतर में भगवान है
- 106) तोड़ विषयों से मन
- 107) तोरी पल पल
- 108) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 109) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 110) थोड़ा सा उपकार कर
- 111) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 112) देख तेरी पर्याय की हालत
- 113) देखा जब अपने अंतर को
- 114) देखो भाई आतमराम
- 115) देखोजी प्रभु करमन की
- 116) धन धन जैनी साधु
- 117) धनि ते प्रानि जिनके
- 118) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 119) धरम बिना बावरे तूने
- 120) धिक धिक जीवन
- 121) धोली हो गई रे काली कामली
- 122) नर तन को पाकर के
- 123) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 124) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 125) परणति सब जीवन
- 126) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 127) परिग्रह डोरी से झूठ
- 128) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 129) पल पल बीते उमरिया
- 130) पाना नहीं जीवन को
- 131) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 132) पावन हो गई आज ये धरती
- 133) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 134) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 135) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 136) प्रभु पै यह वरदान
- 137) प्रभु शांत छवि तेरी
- 138) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 139) भगवंत भजन क्यों
- 140) भरतजी घर में ही वैरागी
- 141) भला कोई या विध मन
- 142) भले रूठ जाये ये सारा
- 143) भले रूठ जाये ये सारा
- 144) भव भव के दुखड़े हजार
- 145) भूल के अपना घर
- 146) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 147) मन महल में दो
- 148) ममता की पतवार ना तोडी
- 149) ममता तू न गई मोरे
- 150) महावीर--वीर भज ले रे
- 151) माया में फ़ंसे इंसान
- 152) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 153) मितवा रे सुवरण अवसर
- 154) मुझे है स्वामी उस बल
- 155) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 156) मेरा आज तलक प्रभु
- 157) मेरे शाश्वत शरण
- 158) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 159) मैं क्या माँगू भगवान
- 160) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 161) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 162) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 163) मैं निज आतम कब
- 164) मैं राजा तिहुं लोक का
- 165) मैं हूँ आतमराम
- 166) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 167) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 168) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 169) मोह की महिमा देखो
- 170) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 171) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 172) यह स्वारथ का संसार दुःख भण्डार
- 173) यही इक धर्ममूल है
- 174) या संसार में कोई सुखी
- 175) ये प्रण है हमारा
- 176) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 177) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 178) रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो अहा
- 179) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 180) वन्दे जिनवरम्
- 181) विराजै रामायण घटमाहिं
- 182) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 183) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 184) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 185) संसार महा अघसागर
- 186) संसार में सुख सर्वदा
- 187) सजधज के जिस दिन
- 188) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 189) सब जग को प्यारा
- 190) समकित सुंदर शांति अपार
- 191) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 192) समझ मन स्वारथ का संसार
- 193) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 194) साधना के रास्ते आत्मा के
- 195) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 196) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 197) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 198) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 199) सुन सतगुरु की सीख
- 200) सुमर सदा मन आतमराम
- 201) सोते सोते ही निकल
- 202) स्वारथ का व्यवहार जग
- 203) हठ तजो रे बेटा हठ
- 204) हम अगर वीर वाणी
- 205) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 206) हम तो विषयों की लहर में बह गये
- 207) हम न किसीके कोई न हमारा
- 208) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 209) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 210) हे चेतन चेत जा अब तो
- 211) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 212) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 213) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 214) हे सीमंधर भगवान शरण
- 215) होता विश्व स्वयं परिणाम
- 216) होली--जे सहज होरी के
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) रत्नत्रय निधि उर धरैं
- 60) वे कोई अजब तमासा
- 61) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 62) सब विधि करन उतावला
- 63) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 64) सीमंधर स्वामी
- 65) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 66) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 67) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 68) सो गुरुदेव हमारा है
- 69) सो मत सांचो है मन मेरे
- 70) स्वामीजी सांची सरन
- 71) होरी खेलूंगी घर आए
- 72) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
- 1) अरे उड़ चला हंस सैलानी
- 2) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 1) अवधू सूतां क्या इस मठ
- 2) क्योंकर महल बनावै पियारे
- 3) भोर भयो उठ जागो मनुवा
- 1) अरे मन पापनसों नित डरिये
- 2) इक योगी असन बनावे
- 3) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 4) जड़ता बिन आप लखें
- 5) लिया आज प्रभु जी ने
- 6) हिंसा झूठ वचन अरु
- 1) अष्ठाह्निका--जय सिद्धचक्र देवा
- 2) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 3) तुम सुनो सुहागन नार
- 4) भाग्य बिना कछु हाथ न आवे
- 5) मोहि सुन सुन आवे हाँसी
- 6) ये आत्मा क्या रंग दिखाता
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) कुमति को छाड़ो भाई
- 3) चिदानंद भूलि रह्यो सुधि
- 4) जीव तू भ्रमत भ्रमत
- 5) जीव निज रस राचन खोयो
- 6) देखो पुद्गल का परिवारा
- 7) देखो भूल हमारी हम
- 8) निज घर नाय पिछान्या
- 9) महावीर--सिद्धारथ राजा दरबारे
- 10) विषय रस खारे इन्हैं छाड़त
- 1) चिद्रूप हमारा इसका
- 2) भैया मेरे नरभव विषयों
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) पर्व अठाई जब जब आवे
- 18) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 19) महावीर जयंती आई
- 20) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 21) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 22) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 23) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 24) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 25) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 26) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 27) श्री सिद्धचक्र का पाठ फल पायो आतम ध्यानी
- 28) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 29) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 30) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 31) होरी खेलूंगी घर आए
- 32) होली--अब घर आये चेतनराज
- 33) होली--अरे मन कैसी होली
- 34) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 35) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 36) होली--और सब मिलि होरि
- 37) होली--कहा बानि परी पिय
- 38) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 39) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 40) होली--खेलौंगी होरी आये
- 41) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 42) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 43) होली--चेतन खेलै होरी
- 44) होली--जे सहज होरी के
- 45) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 46) होली--निजपुर में आज मची
- 47) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 48) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 49) होली खेलें मुनिराज शिखर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 1) आरती--बाहुबली भगवान
- 2) बाहुबली भगवान
- 3) हम यही कामना करते हैं
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 1) क्षमावणी
- 2) अक्षय-तृतीया--पण्डित-राजमल-पवैया
- 3) दीपावली-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 4) रक्षाबंधन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 5) वीरशासन-जयन्ती--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) श्रुतपंचमी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 1) अर्घ्य
- 2) महाअर्घ्य
- 3) समुच्चय-महाअर्घ्य
- 4) शांति-पाठ
- 5) शांति-पाठ-भाषा
- 6) विसर्जन-पाठ
- 7) भगवान-आदिनाथ-चालीसा
- 8) भगवान-महावीर-चालीसा
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
- 1) छहढाला--पण्डित-द्यानतराय
- 2) छहढाला--पं-दौलतराम
- 3) छहढाला--पं-बुधजन
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
- 1) पंच-परमेष्ठी-आरती--पण्डित-द्यानतराय
- 2) भगवान-चंदाप्रभु-आरती
- 3) भगवान-पार्श्वनाथ-आरती
- 4) भगवान-महावीर-आरती
- 5) भगवान-बाहुबली-आरती
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पञ्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
- 1) लब्धिसार--नेमिचंद्र-आचार्य
- 2) गोम्मटसार-जीवकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 3) गोम्मटसार-कर्मकांड--नेमिचंद्र-आचार्य
- 4) आस्रव-त्रिभंगी--श्रुतमुनी
- 5) भाव-संग्रह--वामदेव-आचार्य
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
- 1) आप्त-मीमांसा
- 2) लघीयस्त्रय--भट्टाकलंकदेव
- 3) परीक्षामुख
- 4) आलापपद्धति--देवसेनाचार्य
- 5) युक्त्यनुशासन--समंतभद्राचार्य
- 6) सन्मतितर्क--सिद्धसेनाचार्य
- 1) श्रुतावतार--इंद्रनंदी-आचार्य
- 2) दर्शनसार--देवसेनाचार्य
- 1) Notes
- 2) Stories
- 3) लोकप्रिय-कथाएँ
- 4) Remember
- 5) समयसार-नाटक
- 6) अर्धकथानक--बनारसीदास
ॐ
🙏

ꣽ
श्री
卐
देव
- 1) अंतर में आनंद आयो
- 2) अंतर
- 3) अपना ही रंग मोहे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) अरिहंत देव स्वामी शरण
- 6) अशरण जग में चंद्रनाथ जी
- 7) अशरीरी सिद्ध भगवान
- 8) आओ जिनमंदिर में आओ
- 9) आओ दिखायें हम शुभ नगरी
- 10) आगया शरण तिहारी आगया
- 11) आज खुशी तेरे दर्शन की
- 12) आज हम जिनराज
- 13) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 14) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 15) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 16) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 17) आया तेरे दरबार में
- 18) आये आये रे जिनंदा
- 19) आयो आयो रे हमारो
- 20) एक तुम्हीं आधार हो
- 21) ओ जगत के शांति दाता
- 22) कभी वीर बनके
- 23) कर लो जिनवर का गुणगान
- 24) करता रहूँ गुणगान
- 25) करता हूं तुम्हारा सुमिरन
- 26) करुणा सागर भगवान
- 27) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 28) केसरिया केसरिया
- 29) कैसा अद्भुत शान्त स्वरूप
- 30) कैसी सुन्दर जिन प्रतिमा
- 31) कोई इत आओ जी
- 32) गंगा कल कल स्वर में
- 33) गा रे भैया
- 34) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 35) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 36) चरणों में आया हूं
- 37) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 38) चाह मुझे है दर्शन की
- 39) जपि माला जिनवर
- 40) जब कोई नहीं आता
- 41) जय जय जय जिनवर जी मेरी
- 42) जयवंतो जिनबिम्ब
- 43) जिन ध्याना गुण गाना
- 44) जिन पूजन कर लो ये ही
- 45) जिन मंदिर में आके हम
- 46) जिनजी के दरश मिले
- 47) जिनदेव से कीनी जाने प्रीत
- 48) जिनवर की भक्ति करेगा
- 49) जिनवर की वाणी में म्हारो
- 50) जिनवर की होवे जय जयकार
- 51) जिनवर तू है चंदा तो
- 52) जिनवर दरबार तुम्हारा
- 53) जो पूजा प्रभु की रचाता
- 54) झीनी झीनी उडे रे
- 55) तिहारे ध्यान की मूरत
- 56) तुम जैसा मैं भी
- 57) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 58) तुम्ही हो ज्ञाता
- 59) तू ज्ञान का सागर है
- 60) तेरी छत्रछाया भगवन् मेरे
- 61) तेरी परम दिगंबर मुद्रा को
- 62) तेरी शांत छवि
- 63) तेरी शीतल शीतल मूरत
- 64) तेरी सुंदर मूरत
- 65) तेरे दर्शन को मन
- 66) तेरे दर्शन से मेरा
- 67) दया करो भगवन् मुझपर
- 68) दयालु प्रभु से दया
- 69) दरबार तुम्हारा मनहर है
- 70) दिन रात स्वामी तेरे गीत
- 71) धन्य धन्य आज घडी
- 72) ध्यान धर ले प्रभू को
- 73) ना जिन द्वार आये ना
- 74) नाथ तुम्हारी पूजा
- 75) नाम तुम्हारा तारणहारा
- 76) निरखी निरखी मनहर
- 77) निरखो अंग अंग जिनवर
- 78) नेमि जिनेश्वर
- 79) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 80) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 81) नेमिनाथ--शौरीपुर वाले
- 82) पंचपरम परमेष्ठी
- 83) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 84) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 85) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 86) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 87) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 88) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 89) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 90) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 91) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 92) प्रभु दर्शन कर जीवन की
- 93) प्रभु हम सब का एक
- 94) प्रभुजी अब ना भटकेंगे
- 95) प्रभुजी मन मंदिर में आओ
- 96) बाहुबली भगवान
- 97) भगवान मेरी नैया उस
- 98) भटके हुए राही को
- 99) भावना की चूनरी
- 100) मंगल अरिहंत मंगल
- 101) मन ज्योत जला देना प्रभु
- 102) मन तड़फत प्रभु दरशन
- 103) मन भाये चित हुलसाये
- 104) मनहर तेरी मूरतियाँ
- 105) मनहर मूरत जिनन्द निहार
- 106) महाराजा स्वामी
- 107) महावीर--आज मैं महावीर
- 108) महावीर--आये तेरे द्वार
- 109) महावीर--एक बार आओ जी
- 110) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 111) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 112) महावीर--मस्तक झुका के
- 113) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 114) महावीर--वर्धमान ललना से
- 115) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 116) महावीर--हरो पीर मेरी
- 117) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 118) महावीर स्वामी
- 119) मिलता है सच्चा सुख
- 120) मूरत है बनी प्रभु की प्यारी
- 121) मेरे मन मंदिर में आन
- 122) मेरे सर पर रख दो
- 123) मैं तेरे ढिंग आया रे
- 124) मैं ये निर्ग्रंथ प्रतिमा
- 125) रंग दो जी रंग जिनराज
- 126) रंगमा रंगमा
- 127) रोम रोम पुलकित हो जाये
- 128) रोम रोम से निकले
- 129) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 130) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 131) वीतरागी देव
- 132) शुद्धातम की बात बता दो
- 133) श्री अरहंत सदा मंगलमय
- 134) श्री अरिहंत छवि लखिके
- 135) श्री जिनवर पद ध्यावें जे
- 136) सच्चे जिनवर सच्चे सारे
- 137) सांची कहें तोहरे दर्शन से
- 138) सुरपति ले अपने शीश
- 139) स्वर्ग से सुंदर अनुपम
- 140) हम यही कामना करते हैं
- 141) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 142) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 143) हे ज्ञान सिन्धु भगवान
- 144) हे प्रभो चरणों में
- 145) है कितनी मनहार बहती
शास्त्र
- 1) अमृतझर झुरि झुरि आवे
- 2) आत्मा_ही_समयसार
- 3) इतनी शक्ति हमें देना माता
- 4) ओंकारमयी वाणी तेरी
- 5) करता हूं मैं अभिनंदन
- 6) चरणों में आ पडा हूं
- 7) जब एक रत्न अनमोल
- 8) जिन बैन सुनत मोरी
- 9) जिनवर की वाणी से
- 10) जिनवर चरण भक्ति वर गंगा
- 11) जिनवाणी अमृत रसाल
- 12) जिनवाणी को नमन करो
- 13) जिनवाणी जग मैया
- 14) जिनवाणी माँ आपका शुभ
- 15) जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
- 16) जिनवाणी माँ तेरे चरण
- 17) जिनवाणी माता दर्शन की
- 18) जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि
- 19) जिनवाणी माता से बोले आतम नन्द लाला
- 20) जिनवाणी मोक्ष नसैनी है
- 21) जिनवाणी सुन उपदेशी
- 22) जिनवानी जान सुजान
- 23) तू कितनी मनहर है
- 24) धन्य धन्य जिनवाणी माता
- 25) धन्य धन्य वीतराग वाणी
- 26) नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी
- 27) परम उपकारी जिनवाणी
- 28) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 29) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 30) मंगल बेला आई आज श्री
- 31) मन भाया, तेरे दर आया
- 32) महिमा है अगम
- 33) माँ जिनवाणी ज्ञायक बताय
- 34) माँ जिनवाणी तेरो नाम
- 35) माँ जिनवाणी बसो हृदय में
- 36) माता तू दया करके
- 37) मीठे रस से भरी जिनवाणी
- 38) म्हारी माँ जिनवाणी
- 39) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 40) वीर हिमाचल तें निकसी
- 41) शरण कोई नहीं जग में
- 42) शांती सुधा बरसाये
- 43) शास्त्रों की बातों को मन
- 44) सांची तो गंगा
- 45) सारद तुम परसाद तैं
- 46) सीमंधर मुख से
- 47) सुन जिन बैन श्रवन सुख
- 48) सुन सुन रे चेतन प्राणी
- 49) हम लाए हैं विदह से
- 50) हमें निज धर्म पर चलना
- 51) हे जिनवाणी माता तुमको
- 52) हे शारदे माँ
गुरु
- 1) उड़ चला पंछी रे
- 2) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 3) ऐसे मुनिवर देखें
- 4) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 5) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 6) गुरु निर्ग्रन्थ परिग्रह त्यागी
- 7) गुरु बिन सूनो लगे संसार
- 8) गुरु रत्नत्रय के धारी
- 9) गुरु समान दाता नहिं
- 10) गुरुदेव आये रे बड़े ही सौभाग्य से
- 11) गुरुवर तुम बिन कौन
- 12) गुरुवर थारी परिणति अंतरमयी
- 13) जंगल में मुनिराज अहो
- 14) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 15) धन्य धन्य हे गुरु गौतम
- 16) धन्य मुनिराज हमारे हैं
- 17) धन्य मुनीश्वर आतम हित में
- 18) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 19) निर्ग्रंथों का मार्ग
- 20) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 21) परम दिगम्बर मुनिवर देखे
- 22) परम दिगम्बर यती
- 23) मुनि दीक्षा लेके जंगल में
- 24) मुनिवर आज मेरी कुटिया में
- 25) मुनिवर को आहार
- 26) मैं परम दिगम्बर साधु
- 27) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 28) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 29) म्हारे आंगणे में आये मुनिराज
- 30) वनवासी सन्तों को नित ही
- 31) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 32) वेष दिगम्बर धार
- 33) शान्ति सुधा बरसा गये
- 34) शुद्धातम तत्व विलासी रे
- 35) श्री मुनि राजत समता संग
- 36) संत साधु बन के विचरूँ
- 37) सम आराम विहारी साधुजन
- 38) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 39) हे परम दिगम्बर यति
- 40) है परम दिगम्बर मुद्रा जिनकी
- 41) होली खेलें मुनिराज शिखर
धर्म
- 1) आजा अपने धर्म की तू राह में
- 2) आप्त आगम गुरुवर
- 3) जय जिनेन्द्र बोलिए सर्व
- 4) जय जिनेन्द्र बोलिए
- 5) जिनको जिनधर्म सुहाया 2
- 6) जिनको जिनधर्म सुहाया
- 7) जिनशासन बड़ा निराला
- 8) जैन धर्म के हीरे मोती
- 9) बडे भाग्य से हमको मिला जिन धर्म
- 10) भावों में सरलता रहती है
- 11) मैं महापुण्य उदय से जिनधर्म
- 12) ये धरम है आतम ज्ञानी का
- 13) ये धर्म हमारा है हमें
- 14) लहर लहर लहराये केसरिया झंडा
- 15) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 16) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 17) सब जैन धर्म की जय बोलो
- 18) हर पल हर क्षण हर दम
तीर्थ
- 1) आज गिरिराज निहारा
- 2) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 1
- 3) ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला 2
- 4) ऊंचे शिखरों पे बसा है
- 5) गगन मंडल में उड जाऊं
- 6) चलो सब मिल सिधगिरी
- 7) चांदखेड़ी ले चालो जी सांवरिया
- 8) जीयरा...जीयरा...जीयरा
- 9) नमो आदीश्वरम
- 10) नर तन रतन अमोल
- 11) नेमीनाथ--जहाँ नेमी के चरण
- 12) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 13) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 14) पूजा पाठ रचाऊँ मेरे बालम
- 15) रे मन भज ले प्रभु का नाम
- 16) विश्व तीर्थ बडा प्यारा
- 17) सम्मेद शिखर पर मैं जाऊंगा
कल्याणक
- 1) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 2) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 3) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 4) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 5) आनंद अवसर आज सुरगण
- 6) आया पंच कल्याणक महान 2
- 7) आया पंच कल्याणक महान
- 8) आयो आयो पंचकल्याणक भविजन
- 9) इन्द्र नाचे तेरी भक्ति में
- 10) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान चुनरियाँ
- 11) कल्पद्रुम यह समवसरण है
- 12) गर्भ कल्याणक आ गया
- 13) गावो री बधाईयां
- 14) घर घर आनंद छायो
- 15) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 16) जागो जी माता जागन घड़ियाँ
- 17) झुलाय दइयो पलना
- 18) तेरे पांच हुये कल्याण प्रभु
- 19) दिन आयो दिन आयो
- 20) नाचे रे इन्दर देव
- 21) नेमिनाथ--गिरनारी पर तप
- 22) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 23) नेमिनाथ--पंखिडा रे उड के आओ
- 24) नेमिनाथ--रोम रोम में नेमि
- 25) नेमिनाथ--विषयों की तृष्णा
- 26) पंखिड़ा तू उड़ के जाना स्वर्ग
- 27) पंचकल्याण मनाओ मेरे साथी
- 28) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 29) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 30) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 31) पालकी उठाने का हमें अधिकार है
- 32) मंगल ये अवसर आंगण
- 33) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 34) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 35) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 36) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 37) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 38) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 39) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 40) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 41) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 42) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 43) महावीर--मणियों के पलने में
- 44) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 45) महावीरा झूले पलना
- 46) माता थारी परिणति तत्त्वमयी
- 47) मेरा पलने में
- 48) मोरी आली आज बधाई गाईयाँ
- 49) म्हारे आंगण आज आई
- 50) ये महामहोत्सव पंच कल्याणक
- 51) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 52) सुरपति ले अपने शीश
- 53) स्वागत करते आज तुम्हारा
- 54) हो संसार लगने लगा अब
अध्यात्म
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अपना करना हो कल्याण
- 3) अपनी सुधि पाय आप
- 4) अपने घर को देख बावरे
- 5) अपने में अपना परमातम
- 6) अब गतियों में नाहीं रुलेंगे
- 7) अब प्रभु चरण छोड़ कित जाऊँ
- 8) अब मेरे समकित सावन
- 9) अब हम अमर भये
- 10) अरे मोह में अब ना
- 11) आ तुझे अंतर में शांति मिलेगी
- 12) आओ झूलें मेरे चेतन
- 13) आओ रे आओ रे ज्ञानानंद की
- 14) आज अद्भुत छवि निज निहारी
- 15) आज खुशी है आज खुशी है
- 16) आज सी सुहानी
- 17) आतम अनुभव आवै
- 18) आतम अनुभव करना रे भाई
- 19) आतम अनुभव कीजै हो
- 20) आतम जानो रे भाई
- 21) आतमरूप अनूपम है
- 22) आतमरूप सुहावना
- 23) आत्म चिंतन का ये समय
- 24) आत्मा अनंत गुणों का धनी
- 25) आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला
- 26) आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा
- 27) आनंद स्रोत बह रहा
- 28) आया कहां से
- 29) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 30) इस नगरी में किस विधि
- 31) उड़ उड़ रे म्हारी ज्ञान
- 32) ऐ आतम है तुझको नमन
- 33) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 34) ऐसो नरभव पाय गंवायो
- 35) ओ जाग रे चेतन जाग
- 36) ओ जाननहारे जान जगत है
- 37) ओ जीवड़ा तू थारी
- 38) ओ प्यारे परदेशी पन्छी
- 39) कंकड़ पत्थर गले लगाए
- 40) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 41) कबै निरग्रंथ स्वरूप धरूंगा
- 42) कर कर आतमहित रे
- 43) करलो आतम ज्ञान परमातम
- 44) कहा मान ले ओ मेरे भैया
- 45) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 46) कहाँ तक ये मोह के अंधेरे
- 47) किसको विपद सुनाऊँ हे नाथ
- 48) कृत पूरब कर्म मिटे
- 49) केवलिकन्ये वाङ्गमय
- 50) कैसो सुंदर अवसर आयो है
- 51) कोई राज महल में रोए
- 52) कोई लाख करे चतुराई
- 53) कौलो कहूँ स्वामी बतियाँ
- 54) क्या तन मांझना रे
- 55) क्यूं करे अभिमान जीवन
- 56) क्षणभंगुर जीवन है पगले
- 57) गाडी खडी रे खडी रे तैयार
- 58) गुरुवर जो आपने बताया
- 59) घटमें परमातम ध्याइये
- 60) चंद दिनों का जीना रे जिवड़ा
- 61) चतुर नर चेत करो भाई
- 62) चन्द क्षण जीवन के तेरे
- 63) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 64) चलता चल भाई मोक्षमार्ग
- 65) चलो रे भाई अपने वतन
- 66) चेतन अपनो रूप निहारो
- 67) चेतन को मिला जब नर तन तो
- 68) चेतन चेत बुढ़ापो आयो रे
- 69) चेतन जाग रे
- 70) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 71) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 72) चेतन है तू ध्रुव
- 73) चेतना लक्षणम् आनंद
- 74) चेतो चेतन निज में आओ
- 75) चैतन्य के दर्पण में
- 76) चैतन्य मेरे निज ओर चलो
- 77) जगत में सम्यक उत्तम
- 78) जन्म जन्म तन धरने
- 79) जब चले आत्माराम
- 80) जहां सत्संग होता है
- 81) जानत क्यों नहिं रे
- 82) जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी
- 83) जायें तो जायें कहाँ ढूंढ
- 84) जिंदगी में घड़ी यह सुहानी
- 85) जिंदगी रत्न अनमोल है
- 86) जिया कब तक उलझेगा
- 87) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 88) जीव तू समझ ले आतम
- 89) जीवन के किसी भी पल में
- 90) जीवन के परिनामनि की
- 91) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 92) जैन धरम के हीरे मोती
- 93) जो अपना नहीं उसके अपनेपन
- 94) जो आज दिन है वो
- 95) जो इच्छा का दमन
- 96) जो जो देखी वीतराग
- 97) ज्ञानमय ओ चेतन तुझे
- 98) ज्ञानी का धन ज्ञान
- 99) ज्ञानी की ज्ञान गुफा में
- 100) तन पिंजरे के अन्दर बैठा
- 101) तू जाग रे चेतन देव
- 102) तू जाग रे चेतन प्राणी
- 103) तू निश्चय से भगवान
- 104) तू ही शुद्ध है तू ही
- 105) तेरे अंतर में भगवान है
- 106) तोड़ विषयों से मन
- 107) तोरी पल पल
- 108) तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए
- 109) थाने सतगुरु दे समुझाय
- 110) थोड़ा सा उपकार कर
- 111) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 112) देख तेरी पर्याय की हालत
- 113) देखा जब अपने अंतर को
- 114) देखो भाई आतमराम
- 115) देखोजी प्रभु करमन की
- 116) धन धन जैनी साधु
- 117) धनि ते प्रानि जिनके
- 118) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 119) धरम बिना बावरे तूने
- 120) धिक धिक जीवन
- 121) धोली हो गई रे काली कामली
- 122) नर तन को पाकर के
- 123) निजरूप सजो भवकूप तजो
- 124) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 125) परणति सब जीवन
- 126) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 127) परिग्रह डोरी से झूठ
- 128) परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो
- 129) पल पल बीते उमरिया
- 130) पाना नहीं जीवन को
- 131) पाप मिटाता चल ओ बंधू
- 132) पावन हो गई आज ये धरती
- 133) पीजे पीजे रे चेतनवा पानी
- 134) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 135) प्यारे काहे कूं ललचाय
- 136) प्रभु पै यह वरदान
- 137) प्रभु शांत छवि तेरी
- 138) बेला अमृत गया आलसी सो रहा
- 139) भगवंत भजन क्यों
- 140) भरतजी घर में ही वैरागी
- 141) भला कोई या विध मन
- 142) भले रूठ जाये ये सारा
- 143) भले रूठ जाये ये सारा
- 144) भव भव के दुखड़े हजार
- 145) भूल के अपना घर
- 146) मतवाले प्रभु गुण गाले
- 147) मन महल में दो
- 148) ममता की पतवार ना तोडी
- 149) ममता तू न गई मोरे
- 150) महावीर--वीर भज ले रे
- 151) माया में फ़ंसे इंसान
- 152) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 153) मितवा रे सुवरण अवसर
- 154) मुझे है स्वामी उस बल
- 155) मुसाफिर क्यों पड़ा सोता
- 156) मेरा आज तलक प्रभु
- 157) मेरे शाश्वत शरण
- 158) मैं ऐसा देहरा बनाऊं
- 159) मैं क्या माँगू भगवान
- 160) मैं ज्ञान मात्र बस ज्ञायक हूँ
- 161) मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं
- 162) मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं
- 163) मैं निज आतम कब
- 164) मैं राजा तिहुं लोक का
- 165) मैं हूँ आतमराम
- 166) मैनासुंदरी कहे पिता से
- 167) मोको कहाँ ढूंढें बन्दे
- 168) मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे
- 169) मोह की महिमा देखो
- 170) मोहे भावे न भैया थारो देश
- 171) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 172) यह स्वारथ का संसार दुःख भण्डार
- 173) यही इक धर्ममूल है
- 174) या संसार में कोई सुखी
- 175) ये प्रण है हमारा
- 176) ये शाश्वत सुख का प्याला
- 177) ये सर्वसृष्टि है नाट्यशाला
- 178) रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो अहा
- 179) लुटेरे बहुत देखे हैं
- 180) वन्दे जिनवरम्
- 181) विराजै रामायण घटमाहिं
- 182) वीर जिनेश्वर अब तो मुझको
- 183) शुद्धात्मा का श्रद्धान
- 184) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 185) संसार महा अघसागर
- 186) संसार में सुख सर्वदा
- 187) सजधज के जिस दिन
- 188) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 189) सब जग को प्यारा
- 190) समकित सुंदर शांति अपार
- 191) समझ आत्मा के स्वरूप को
- 192) समझ मन स्वारथ का संसार
- 193) सहजानन्दी शुद्ध स्वभावी
- 194) साधना के रास्ते आत्मा के
- 195) सिद्धों से मिलने का मार्ग
- 196) सुन चेतन ज्ञानी क्यों
- 197) सुन रे जिया चिरकाल गया
- 198) सुन ले ओ भोले प्राणी
- 199) सुन सतगुरु की सीख
- 200) सुमर सदा मन आतमराम
- 201) सोते सोते ही निकल
- 202) स्वारथ का व्यवहार जग
- 203) हठ तजो रे बेटा हठ
- 204) हम अगर वीर वाणी
- 205) हम आतम ज्ञानी हम भेद
- 206) हम तो विषयों की लहर में बह गये
- 207) हम न किसीके कोई न हमारा
- 208) हमने तो घूमीं चार गतियाँ
- 209) हूँ स्वतंत्र निश्चल
- 210) हे चेतन चेत जा अब तो
- 211) हे परमात्मन तुझको पाकर
- 212) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 213) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 214) हे सीमंधर भगवान शरण
- 215) होता विश्व स्वयं परिणाम
- 216) होली--जे सहज होरी के
पं दौलतराम कृत
- 1) अपनी सुधि भूल आप
- 2) अब मोहि जानि परी
- 3) अभिनंदन--जगदानंदन
- 4) अरिरजरहस हनन प्रभु
- 5) अरे जिया जग धोखे
- 6) आज गिरिराज निहारा
- 7) आज मैं परम पदारथ
- 8) आतम रूप अनूपम अद्भुत
- 9) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 10) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 11) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 12) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 13) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 14) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 15) आप भ्रमविनाश आप
- 16) आपा नहिं जाना तूने
- 17) उरग सुरग नरईश शीस
- 18) ऐसा मोही क्यों न अधोगति
- 19) ऐसा योगी क्यों न अभयपद
- 20) और अबै न कुदेव सुहावै
- 21) और सबै जगद्वन्द
- 22) कबधौं मिलै मोहि श्रीगुरु
- 23) कुंथुनाथ--कुंथुन के प्रतिपाल
- 24) कुमति कुनारि नहीं है भली
- 25) गुरु कहत सीख इमि
- 26) घड़ि घड़ि पल पल
- 27) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 28) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 29) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 30) चित चिंतकैं चिदेश
- 31) चिदराय गुण मुनो सुनो
- 32) चिन्मूरत दृग्धारी की
- 33) चेतन अब धरि सहज
- 34) चेतन कौन अनीति गही
- 35) चेतन तैं यौं ही भ्रम
- 36) चेतन यह बुधि कौन सयानी
- 37) छाँडत क्यों नहिं रे नर
- 38) छांडत क्यौं नहिं रे
- 39) छांडि दे या बुधि भोरी
- 40) जबतैं आनंदजननि दृष्टि
- 41) जम आन अचानक दाबेगा
- 42) जय जग भरम तिमिर हरन
- 43) जाऊँ कहाँ तज शरन
- 44) जिन बैन सुनत मोरी
- 45) जिन राग द्वेष त्यागा
- 46) जिनवर आनन भान
- 47) जिनवानी जान सुजान
- 48) जिया तुम चालो अपने
- 49) जीव तू अनादिहीतैं भूल्यौ
- 50) ज्ञानी जीव निवार भरमतम
- 51) तुम सुनियो श्रीजिननाथ
- 52) तोहि समझायो सौ सौ
- 53) त्रिभुवन आनंदकारी जिन
- 54) थारा तो बैनामें सरधान
- 55) धन धन साधर्मीजन मिलन
- 56) धनि मुनि जिन यह
- 57) धनि मुनि जिनकी लगी
- 58) धनि हैं मुनि निज आतमहित
- 59) ध्यानकृपान पानि गहि नासी
- 60) न मानत यह जिय निपट
- 61) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 62) नाथ मोहि तारत क्यों ना
- 63) निजहितकारज करना
- 64) नित पीज्यौ धी धारी
- 65) निरख सुख पायो जिनमुख
- 66) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 67) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 68) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 69) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 70) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 71) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 72) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 73) प्यारी लागै म्हाने जिन छवि
- 74) प्रभु थारी आज महिमा जानी
- 75) भविन सरोरूहसूर
- 76) मत कीजो जी यारी यह
- 77) मत कीज्यो जी यारी घिन
- 78) मत राचो धीधारी भव रंभ
- 79) मनवचतन करि शुद्ध
- 80) महावीर--जय शिव कामिनि
- 81) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 82) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 83) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 84) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 85) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 86) मान ले या सिख मोरी
- 87) मानत क्यों नहिं रे हे नर
- 88) मेरे कब ह्वै वा
- 89) मैं आयौ जिन शरन तिहारी
- 90) मैं भाखूं हित तेरा सुनि हो
- 91) मोहि तारो जी क्यों ना
- 92) मोहिड़ा रे जिय हितकारी
- 93) मोही जीव भरमतम ते नहि
- 94) राचि रह्यो परमाहिं
- 95) लखो जी या जिय भोरे
- 96) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
- 97) विषयोंदा मद भानै ऐसा
- 98) शांतिनाथ--वारी हो बधाई या
- 99) शिवपुर की डगर समरस
- 100) सुधि लीज्यो जी म्हारी
- 101) सुनि जिन बैन श्रवन सुख
- 102) सुनो जिया ये सतगुरु
- 103) सौ सौ बार हटक नहिं
- 104) हम तो कबहुँ न निज गुन
- 105) हम तो कबहुँ न निज घर
- 106) हम तो कबहूँ न हित उपजाये
- 107) हे जिन तेरे मैं शरणै
- 108) हे जिन तेरो सुजस
- 109) हे जिन मेरी ऐसी बुधि
- 110) हे नर भ्रम नींद क्यों न
- 111) हे मन तेरी को कुटेव यह
- 112) हे हितवांछक प्रानी रे
- 113) हो तुम त्रिभुवन तारी
- 114) हो तुम शठ अविचारी जियरा
- 115) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 116) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
पं भागचंद कृत
- 1) अतिसंक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि
- 2) अहो यह उपदेश माहीं
- 3) आकुल रहित होय इमि
- 4) आतम अनुभव आवै
- 5) आवै न भोगन में तोहि
- 6) ऐसे जैनी मुनिमहाराज
- 7) ऐसे विमल भाव जब पावै
- 8) ऐसे साधु सुगुरु कब
- 9) करो रे भाई तत्त्वारथ
- 10) चन्द्रोज्वल अविकार स्वामी जी
- 11) जिन स्व पर हिताहित चीना
- 12) जीव! तू भ्रमत सदैव
- 13) जीवन के परिनामनि की
- 14) जे दिन तुम विवेक बिन
- 15) ज्ञानी जीवनि के भय होय
- 16) तुम परम पावन देख जिन
- 17) धन धन जैनी साधु
- 18) धनि ते प्रानि जिनके
- 19) धन्य धन्य है घड़ी आज
- 20) परणति सब जीवन
- 21) प्रभु पै यह वरदान
- 22) महिमा है अगम
- 23) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 24) यह मोह उदय दुख पावै
- 25) यही इक धर्ममूल है
- 26) श्री मुनि राजत समता संग
- 27) सन्त निरन्तर चिन्तत
- 28) सफल है धन्य धन्य वा
- 29) सम आराम विहारी साधुजन
- 30) सुमर सदा मन आतमराम
- 31) होली--जे सहज होरी के
पं द्यानतराय कृत
- 1) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 2) अब मोहे तार लेहु महावीर
- 3) अब हम अमर भये
- 4) अब हम आतम को पहिचान्यौ
- 5) अरहंत सुमर मन बावरे
- 6) अहो भवि प्रानी चेतिये हो
- 7) आतम अनुभव करना रे भाई
- 8) आतम अनुभव कीजिये यह
- 9) आतम अनुभव कीजै हो
- 10) आतम अनुभव सार हो
- 11) आतम काज सँवारिये
- 12) आतम जान रे जान रे जान
- 13) आतम जानो रे भाई
- 14) आतमज्ञान लखैं सुख होई
- 15) आतमरूप अनूपम है
- 16) आतमरूप सुहावना
- 17) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 18) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 19) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 20) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 21) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 25) आदिनाथ तारन तरनं
- 26) आपा प्रभु जाना मैं जाना
- 27) आरति कीजै श्रीमुनिराज की
- 28) आरती--करौं आरती वर्द्धमान
- 29) आरती--मंगल आरती आतमराम
- 30) आरती--मंगल आरती कीजे भोर
- 31) आरती श्रीजिनराज तिहारी
- 32) एक ब्रह्म तिहुँलोकमँझार
- 33) ऐसो सुमिरन कर मेरे भाई
- 34) कर कर आतमहित रे
- 35) कर मन निज आतम चिंतौन
- 36) कर मन वीतराग को ध्यान
- 37) कर रे तू आतम हित
- 38) कलि में ग्रन्थ बड़े उपगारी
- 39) कहत सुगुरु करि सुहित
- 40) कहिवे को मन सूरमा
- 41) काया तेरी दुख की ढेरी
- 42) कारज एक ब्रह्महीसेती
- 43) काहे को सोचत अति भारी
- 44) किसकी भगति किये हित
- 45) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 46) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 47) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 48) गलता नमता कब आवैगा
- 49) गहु सन्तोष सदा मन
- 50) गुरु समान दाता नहिं
- 51) घटमें परमातम ध्याइये
- 52) चेतन नागर हो तुम चेतो
- 53) चेतन प्राणी चेतिये हो
- 54) जग में प्रभु पूजा सुखदाई
- 55) जगत में सम्यक उत्तम
- 56) जानत क्यों नहिं रे
- 57) जानो धन्य सो धन्य सो धीर
- 58) जानौं पूरा ज्ञाता सोई
- 59) जिन नाम सुमर मन बावरे
- 60) जिनके हिरदै प्रभुनाम नहीं
- 61) जिनवरमूरत तेरी शोभा
- 62) जीव तैं मूढ़पना कित पायो
- 63) जो तैं आतमहित नहिं कीना
- 64) ज्ञान का राह दुहेला रे
- 65) ज्ञान का राह सुहेला रे
- 66) ज्ञान को पंथ कठिन है
- 67) ज्ञान ज्ञेयमाहिं नाहि ज्ञेय
- 68) ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 69) ज्ञानी ऐसो ज्ञान विचारै
- 70) ज्ञानी जीव दया नित पालैं
- 71) तुम प्रभु कहियत दीनदयाल
- 72) तुमको कैसे सुख ह्वै मीत
- 73) तू जिनवर स्वामी मेरा
- 74) तू तो समझ समझ रे
- 75) दरसन तेरा मन भाये
- 76) देखे जिनराज आज राजऋद्धि
- 77) देखे सुखी सम्यकवान
- 78) देखो भाई आतमराम
- 79) देखो भाई श्रीजिनराज विराजैं
- 80) धनि ते साधु रहत वनमाहीं
- 81) धनि धनि ते मुनि गिरी
- 82) धिक धिक जीवन
- 83) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 84) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 85) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 86) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 87) प्रभु तेरी महिमा किहि
- 88) प्राणी आतमरूप अनूप है
- 89) प्राणी लाल छांडो मन चपलाई
- 90) प्रानी ये संसार असार है
- 91) भाई अब मैं ऐसा जाना
- 92) भाई कहा देख गरवाना रे
- 93) भाई कौन कहै घर मेरा
- 94) भाई कौन धरम हम पालें
- 95) भाई जानो पुद्गल न्यारा रे
- 96) भाई ज्ञान बिना दुख पाया रे
- 97) भाई ज्ञानी सोई कहिये
- 98) भाई ब्रह्म विराजै कैसा
- 99) भाई ब्रह्मज्ञान नहिं जाना रे
- 100) भैया सो आतम जानो रे
- 101) भोर भयो भज श्रीजिनराज
- 102) भ्रम्यो जी भ्रम्यो संसार महावन
- 103) मगन रहु रे शुद्धातम में
- 104) मन मेरे राग भाव निवार
- 105) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 106) मानुषभव पानी दियो जिन
- 107) मेरे घट ज्ञान घनागम
- 108) मेरे मन कब ह्वै है बैराग
- 109) मैं निज आतम कब
- 110) मोहि कब ऐसा दिन आय
- 111) राम भरतसों कहैं सुभाइ
- 112) राम सीता संवाद
- 113) रे जिय क्रोध काहे करै
- 114) रे जिय जनम लाहो लेह
- 115) रे जिय भजो आतमदेव
- 116) रे भाई करुना जान रे
- 117) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 118) रे मन भज भज दीन दयाल
- 119) लागा आतमराम सों नेहरा
- 120) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 121) वे कोई निपट अनारी
- 122) शौच--जियको लोभ महा
- 123) श्रीजिनधर्म सदा जयवन्त
- 124) सँभाल जगजाल में काल दरहाल
- 125) सब जग को प्यारा
- 126) सबको एक ही धरम सहाय
- 127) सबमें हम हममें सब ज्ञान
- 128) समझत क्यों नहिं वानी
- 129) साधो छांडो विषय विकारी
- 130) सील सदा दिढ़ राखि हिये
- 131) सुन चेतन इक बात हमारी
- 132) सुन चेतन लाड़ले यह चतुराई
- 133) सुपार्श्वनाथ--प्रभुजी प्रभ सुपास
- 134) सोई ज्ञान सुधारस पीवै
- 135) सोग न कीजे बावरे मरें
- 136) हम न किसीके कोई न हमारा
- 137) हम लागे आतमराम सों
- 138) हमको कैसैं शिवसुख होई
- 139) हमारो कारज ऐसे होय
- 140) हमारो कारज कैसें होय
- 141) हो भविजन ज्ञान सरोवर सोई
- 142) हो भैया मोरे कहु कैसे सुख
- 143) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 144) होली--खेलौंगी होरी आये
- 145) होली--चेतन खेलै होरी
पं सौभाग्यमल कृत
- 1) अध्यात्म के शिखर पर
- 2) अय नाथ ना बिसराना आये
- 3) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 4) आज सी सुहानी
- 5) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 6) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 7) ओ वीर जिन जी तुम्हें हम
- 8) कबधौं सर पर धर डोलेगा
- 9) कलश देखने आया जी
- 10) कहा मानले ओ मेरे भैया
- 11) किये भव भव भव में फेरे
- 12) कोई जब साथ न आये
- 13) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 14) जहाँ रागद्वेष से रहित
- 15) जो आज दिन है वो
- 16) ज्यों सरवर में रमै माछली
- 17) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 18) तेरी कहाँ गई मतिमारी
- 19) तेरे दर्शन को मन
- 20) तेरे दर्शन से मेरा
- 21) तोड़ विषयों से मन
- 22) तोरी पल पल
- 23) त्याग बिना जीवन की गाड़ी
- 24) दया कर दो मेरे स्वामी तेरे
- 25) धन्य धन्य आज घडी
- 26) धोली हो गई रे काली कामली
- 27) ध्यान धर ले प्रभू को
- 28) नचा मन मोर ठौर
- 29) नमन तुमको करते हैं महावीर
- 30) नमेँ मात वामा के पारस
- 31) नित उठ ध्याऊँ गुण गाऊँ
- 32) निरखी निरखी मनहर
- 33) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 34) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 35) पल पल बीते उमरिया
- 36) बधाई आज मिल गाओ
- 37) बिन ज्ञान जिया तो जीना
- 38) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 39) भव भव रुले हैं
- 40) भाया थारी बावली जवानी
- 41) मन महल में दो
- 42) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 43) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 44) मार्दव--मानी थारा मान
- 45) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 46) मेरे भगवन यह क्या हो गया
- 47) मेरे मन मन्दिर में आन
- 48) मैं हूँ आतमराम
- 49) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 50) म्हारा परम दिगम्बर मुनिवर
- 51) लहराएगा लहराएगा झंडा
- 52) लिया प्रभू अवतार जयजयकार
- 53) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 54) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 55) संसार महा अघसागर
- 56) सत्य--आओ सत्य धरम
- 57) सत्य--लागे सत्य सुमन
- 58) साँवरे बनवासी काहे छोड
- 59) स्वामी तेरा मुखडा
- 60) हे परम दिगम्बर यति
पं भूधरदास कृत
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अज्ञानी पाप धतूरा
- 4) अन्तर उज्जल करना रे
- 5) अब नित नेमि नाम भजौ
- 6) अब पूरी कर नींदड़ी
- 7) अब मेरे समकित सावन
- 8) अरे हाँ चेतो रे भाई
- 9) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 10) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 11) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 12) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 13) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 14) आयो रे बुढ़ापो मानी
- 15) ऐसी समझ के सिर धूल
- 16) ऐसो श्रावक कुल तुम
- 17) और सब थोथी बातैं भज
- 18) करम गति टारी नाहिं टरे
- 19) करुणाष्टक
- 20) काया गागरि जोजरी तुम
- 21) गरव नहिं कीजै रे
- 22) गाफिल हुवा कहाँ तू डोले
- 23) चरखा चलता नाहीं रे
- 24) चादर हो गई बहुत
- 25) चित्त चेतन की यह विरियां
- 26) जग में जीवन थोरा रे
- 27) जग में श्रद्धानी जीव
- 28) जगत जन जूवा हारि चले
- 29) जपि माला जिनवर
- 30) जिनराज चरन मन मति बिसरै
- 31) जिनराज ना विसारो मति
- 32) जीवदया व्रत तरु बड़ो
- 33) जै जगपूज परमगुरु नामी
- 34) तुम जिनवर का गुण गावो
- 35) तुम तरनतारन भवनिवारन
- 36) तुम सुनियो साधो मनुवा
- 37) ते गुरु मेरे मन बसो
- 38) थांकी कथनी म्हानै प्यारी
- 39) देखे देखे जगत के देव
- 40) देखो भाई आतमदेव
- 41) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 42) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 43) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 44) नैननि को वान परी
- 45) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 46) पुलकन्त नयन चकोर पक्षी
- 47) प्रभु गुन गाय रै यह
- 48) भगवंत भजन क्यों
- 49) भलो चेत्यो वीर नर
- 50) भवि देखि छबी भगवान
- 51) मन मूरख पंथी उस मारग
- 52) मन हंस हमारी लै शिक्षा
- 53) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 54) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 55) मेरे चारौं शरन सहाई
- 56) मेरे मन सूवा जिनपद
- 57) म्हें तो थांकी आज महिमा
- 58) यह तन जंगम रूखड़ा
- 59) रत्नत्रय निधि उर धरैं
- 60) वे कोई अजब तमासा
- 61) वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी
- 62) सब विधि करन उतावला
- 63) सीमंधर--वा पुर के वारौँ
- 64) सीमंधर स्वामी
- 65) सुन ज्ञानी प्राणी श्रीगुरु
- 66) सुनि सुजान पांचों रिपु
- 67) सुनी ठगनी माया तैं सब
- 68) सो गुरुदेव हमारा है
- 69) सो मत सांचो है मन मेरे
- 70) स्वामीजी सांची सरन
- 71) होरी खेलूंगी घर आए
- 72) होली--अहो दोऊ रंग भरे
पं बुधजन कृत
- 1) अब तू जान रे चेतन जान
- 2) अब थे क्यों दुख पावो
- 3) आगैं कहा करसी भैया
- 4) आज मनरी बनी छै जिनराज
- 5) उत्तम नरभव पायकै
- 6) और ठौर क्यों हेरत प्यारा
- 7) काल अचानक ही ले
- 8) किंकर अरज करत जिन
- 9) गुरु दयाल तेरा दुःख
- 10) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 11) जगत में होनहार सो होवै
- 12) जिनवाणी की सुनै सो
- 13) ज्ञानी थारी रीति रौ अचंभौ
- 14) तेरो करिलै काज बखत
- 15) तैं क्या किया नादान तैं
- 16) देखा मैंने आतमरामा
- 17) धनि सरधानी जग में
- 18) धरम बिन कोई नहीं
- 19) नरभव पाय फेरि दुख
- 20) पतितउधारक पतित
- 21) परम जननी धरम कथनी
- 22) प्रात भयो सब भविजन
- 23) बाबा मैं न काहू का
- 24) भज जिन चतुर्विंशति नाम
- 25) भजन बिन योंही जनम गमायो
- 26) भवदधि तारक नवका जगमाहीं
- 27) मति भोगन राचौ जी
- 28) मुनि बन आये जी बना
- 29) मेरा सांई तौ मोमैं नाहीं
- 30) मेरी अरज कहानी सुनीए
- 31) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 32) या नित चितवो उठिकै
- 33) सम्यग्ज्ञान बिना तेरो जनम
- 34) सारद तुम परसाद तैं
- 35) सुणिल्यो जीव सुजान
- 36) सुनकर वाणी जिनवर
- 37) हम शरन गह्यो जिन चरन
- 38) हमकौ कछू भय ना
- 39) हे आतमा देखी दुति तोरी
- 40) हो जिनवाणी जू तुम
- 41) होली--अब घर आये चेतनराज
- 42) होली--और सब मिलि होरि
- 43) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 44) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 45) होली--चेतन तोसौं आज होरी
- 46) होली--निजपुर में आज मची
पं मंगतराय कृत
पं न्यामतराय कृत
- 1) अपने निजपद को मत खोय
- 2) अमोलक मनुष जनम प्यारे
- 3) अरे यह क्या किया नादान
- 4) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 5) कर सकल विभाव अभाव
- 6) क्यों परमादी रे चेतनवा
- 7) घर आवो सुमति वरनार
- 8) चेतो चेतोरे चेतनवा
- 9) तन मन सारो जी सांवरिया
- 10) तुम्हारे दर्श बिन स्वामी
- 11) दया दिल में धारो प्यारे
- 12) परदेसिया में कौन चलेगो
- 13) मत तोरे मेरे शील का सिंगार
- 14) विषय भोग में तूने ऐ जिया
- 15) विषय सेवन में कोई
- 16) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
पं बनारसीदास कृत
- 1) ऐसैं क्यों प्रभु पाइये
- 2) ऐसैं यों प्रभु पाइये
- 3) कित गये पंच किसान
- 4) चेतन उलटी चाल चले
- 5) चेतन तूँ तिहुँ काल अकेला
- 6) चेतन तोहि न नेक संभार
- 7) चेतन रूप अनुप अमूरत
- 8) जगत में सो देवन
- 9) दुविधा कब जैहै या
- 10) देखो भाई महाविकल
- 11) भेदविज्ञान जग्यौ जिन्हके
- 12) भोंदू भाई ते हिरदे की आँखें
- 13) भोंदू भाई समुझ सबद
- 14) मगन ह्वै आराधो साधो
- 15) मूलन बेटा जायो रे
- 16) मेरा मन का प्यारा जो
- 17) या चेतन की सब सुधि
- 18) रे मन कर सदा संतोष
- 19) वा दिन को कर सोच
- 20) विराजै रामायण घट माँहिं
- 21) सुण ज्ञानी भाई खेती
- 22) हम बैठे अपनी मौन सौं
- 23) होली--चलो सखी खेलन होरी
पं ज्ञानानन्द कृत
पं नयनानन्द कृत
पं मख्खनलाल कृत
पं बुध महाचन्द्र
सहजानन्द वर्णी
पर्व
- 1) अष्ठाह्निका पर्व--आयो आयो पर्व अठाई
- 2) अष्ठाह्निका पर्व--आयो पर्व अठाई
- 3) जिनमंदिर का शिलान्यास
- 4) दिवाली--अबके ऐसी दीवाली
- 5) पर्युषण--दश धर्मों को धार सोलह
- 6) पर्युषण--दशलक्षण के दश धर्मों
- 7) पर्युषण--दस लक्षणों को ध्याके
- 8) पर्युषण--दसलक्षण पर्व का समा
- 9) पर्युषण--धर्म के दशलक्षण
- 10) पर्युषण--पर्व दशलक्षण मंगलकार
- 11) पर्युषण--पर्व दस लक्षण खुशी से
- 12) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया आनंद
- 13) पर्युषण--पर्व पर्युषण आया है
- 14) पर्युषण--पर्वराज पर्युषण आया
- 15) पर्युषण--पर्वराज पर्यूषण आया
- 16) पर्युषण--ये पर्व पर्युषण प्यारा है
- 17) पर्व अठाई जब जब आवे
- 18) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 19) महावीर जयंती आई
- 20) मोक्ष सप्तमी--मंगल गाओ
- 21) रक्षाबंधन--जय मुनिवर विष्णुकुमार
- 22) वीर शासन जयंती--वीर की वाणी
- 23) वीर शासन जयंती--वैशाख शुक्ल
- 24) वीरशासन जयंती--जब बानी खिरी
- 25) वीरशासन जयंती--प्राणां सूं भी प्यारी
- 26) वीरशासनजयंती--वैशाख शुक्ल
- 27) श्री सिद्धचक्र का पाठ फल पायो आतम ध्यानी
- 28) श्रुत पंचमी--आचार्य श्री धरसेन जो
- 29) श्रुत पंचमी--भूतबली श्री पुष्पदन्त
- 30) सिद्ध चक्र--मंगल महोत्सव भला आ गया
- 31) होरी खेलूंगी घर आए
- 32) होली--अब घर आये चेतनराज
- 33) होली--अरे मन कैसी होली
- 34) होली--अहो दोऊ रंग भरे
- 35) होली--आयो सहज बसन्त खेलैं
- 36) होली--और सब मिलि होरि
- 37) होली--कहा बानि परी पिय
- 38) होली--कैसे होरी खेलूँ होरी
- 39) होली--खेलूंगी होरी श्रीजिनवर
- 40) होली--खेलौंगी होरी आये
- 41) होली--चलो सखी खेलन होरी
- 42) होली--चेतन खेल सुमति संग
- 43) होली--चेतन खेलै होरी
- 44) होली--जे सहज होरी के
- 45) होली--ज्ञानी ऐसे होली मचाई
- 46) होली--निजपुर में आज मची
- 47) होली--भ्रात ऐसी खेलिये
- 48) होली--मेरो मन ऐसी खेलत
- 49) होली खेलें मुनिराज शिखर
चौबीस तीर्थंकर
- 1) अजितनाथ--अजित जिन विनती
- 2) अजितनाथ--अजित जिनेश्वर
- 3) अजितनाथ सों मन लावो रे
- 4) अभिनंदन--जगदानंदन
- 5) आदिनाथ--आज गिरिराज के
- 6) आदिनाथ--आज तो बधाई
- 7) आदिनाथ--आज नगरी में जन्मे
- 8) आदिनाथ--आदिपुरुष मेरी आस
- 9) आदिनाथ--ऋषभदेव जनम्यौ
- 10) आदिनाथ--गाएँ जी गाएँ
- 11) आदिनाथ--चलि सखि देखन
- 12) आदिनाथ--जपलो रे आदीश्वर
- 13) आदिनाथ--जय श्री ऋषभ
- 14) आदिनाथ--जाकौं इंद
- 15) आदिनाथ--तेरैं मोह नहीं
- 16) आदिनाथ--देखो जी आदिश्वर
- 17) आदिनाथ--देखो नाभिनंदन
- 18) आदिनाथ--निरख सखी ऋषिन
- 19) आदिनाथ--फूली बसन्त जहँ
- 20) आदिनाथ--भगवन मरुदेवी के
- 21) आदिनाथ--भज ऋषिपति
- 22) आदिनाथ--भज रे मन
- 23) आदिनाथ--भज श्रीआदिचरन
- 24) आदिनाथ--मेरी जीभ आठौं
- 25) आदिनाथ--मेरी सुध लीजै
- 26) आदिनाथ--म्हारा आदीश्वर
- 27) आदिनाथ--रटि रसना मेरी
- 28) आदिनाथ--रुल्यो चिरकाल
- 29) आदिनाथ--लगी लौ नाभिनंदन
- 30) आदिनाथ--लिया रिषभ देव
- 31) चंद्रनाथ--चंद्रानन
- 32) चंद्रनाथ--थे म्हारे मन भायाजी
- 33) चंद्रनाथ--निरखत जिन चंद्रवदन
- 34) चंद्रनाथ--निरखि जिनचन्द री
- 35) नमिनाथ--अहो नमि जिनप
- 36) नेमजी की जान बणी भारी
- 37) नेमि जिनेश्वर
- 38) नेमिनाथ--अब हम नेमिजी की
- 39) नेमिनाथ--अहो बनवासी पिया
- 40) नेमिनाथ--त्रिभुवनगुरु स्वामी
- 41) नेमिनाथ--देखो गरब गहेली
- 42) नेमिनाथ--देख्या मैंने नेमिजी
- 43) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 44) नेमिनाथ--नेमि पिया राजुल
- 45) नेमिनाथ--नेमिप्रभू की श्यामवरन
- 46) नेमिनाथ--भजि मन प्रभु
- 47) नेमिनाथ--लाल कैसे जावोगे
- 48) नेमी जिनेश्वरजी काहे कसूर
- 49) पद्मप्रभु--पद्मसद्म
- 50) पारसनाथ--आज जन्मे हैं तीर्थंकर
- 51) पारसनाथ--आनंद अंतर मा आज
- 52) पारसनाथ--चवलेश्वर पारसनाथ
- 53) पारसनाथ--झूल रहा पलने में
- 54) पारसनाथ--तुमसे लागी लगन
- 55) पारसनाथ--पारस जिन चरन निरख
- 56) पारसनाथ--पारस प्यारा लागो
- 57) पारसनाथ--पारस प्रभु का
- 58) पारसनाथ--पारस प्रभु को नाऊँ
- 59) पारसनाथ--पार्श्व प्रभुजी पार
- 60) पारसनाथ--पास अनादि अविद्या
- 61) पारसनाथ--मंगल थाल सजाकर
- 62) पारसनाथ--मधुबन के मंदिरों
- 63) पारसनाथ--मेरे प्रभु का पारस
- 64) पारसनाथ--मैं करूँ वंदना
- 65) पारसनाथ--वामा घर बजत बधाई
- 66) पारसनाथ--सांवरिया के नाम
- 67) पारसनाथ--सांवरिया पारसनाथ
- 68) महावीर--आज मैं महावीर
- 69) महावीर--आये तेरे द्वार
- 70) महावीर--एक बार आओ जी
- 71) महावीर--कुण्डलपुर में वीर हैं
- 72) महावीर--कुण्डलपुर वाले
- 73) महावीर--छायो रे छायो आनंद
- 74) महावीर--जनम लिया है महावीर
- 75) महावीर--जय बोलो त्रिशला
- 76) महावीर--जय शिव कामिनि
- 77) महावीर--जय श्री वीर जिन
- 78) महावीर--जय श्री वीर जिनेन्द्र
- 79) महावीर--जहाँ महावीर ने जन्म
- 80) महावीर--तुझे प्रभु वीर कहते
- 81) महावीर--त्रिशला के नन्द
- 82) महावीर--दिव्य ध्वनि वीरा
- 83) महावीर--दुःख मेटो वीर
- 84) महावीर--देखा मैंने त्रिशला का
- 85) महावीर--पंखिडा रे उड के आओ
- 86) महावीर--बधाई आज मिल गाओ
- 87) महावीर--बाजे कुण्डलपुर में
- 88) महावीर--बीरा थारी बान परी
- 89) महावीर--मणियों के पलने में
- 90) महावीर--मस्तक झुका के
- 91) महावीर--मेरे महावीर झूले पलना
- 92) महावीर--वंदों अद्भुत चन्द्र वीर
- 93) महावीर--वर्तमान को वर्धमान
- 94) महावीर--वर्धमान ललना से
- 95) महावीर--वीर प्रभु के ये बोल
- 96) महावीर--वीर हिमाचल तें
- 97) महावीर--सब मिल देखो हेली
- 98) महावीर--हमारी वीर हरो भवपीर
- 99) महावीर--हरो पीर मेरी
- 100) महावीर--हे वीर तुम्हारे
- 101) महावीर जीवाजीव छीर नीर
- 102) महावीर स्वामी
- 103) महावीरा झूले पलना
- 104) वासुपूज्य--जय जिन वासुपूज्य
बाहुबली भगवान
बधाई
दस धर्म
- 1) आर्जव--कपटी नर कोई साँच न बोले
- 2) आर्जव--काहे पाप करे काहे छल
- 3) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 4) आर्जव--तज कपट महा दुखकारी
- 5) क्षमा--करल्यो क्षमा धरम न धारण
- 6) क्षमा--काहे क्रोध करे
- 7) क्षमा--क्रोध कषाय न मैं
- 8) क्षमा--जिया तूं चेतत क्यों नहिं ज्ञानी
- 9) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 10) क्षमा--दस धरम में बस क्षमा
- 11) क्षमा--मेरी उत्तम क्षमा न जाय
- 12) क्षमा--सबसों छिमा छिमा कर
- 13) तप--तप बिन नीर न बरसे
- 14) त्याग--तैने दियो नहीं है दान
- 15) ब्रह्मचर्य--क्षमाशील सो धर्म
- 16) ब्रह्मचर्य--परनारी विष बेल
- 17) ब्रह्मचर्य--शील शिरोमणी रतन
- 18) मार्दव--त्यागो रे भाई यह मान बडा
- 19) मार्दव--धर्म मार्दव को सब मिल
- 20) मार्दव--मत कर तू
- 21) मार्दव--मान न कीजिये हो
- 22) मार्दव--मानी थारा मान
- 23) मार्दव--मानी मनुआ मद
- 24) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 25) शौच--जियको लोभ महा
- 26) शौच--जैनी धारियोजी
- 27) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 28) सत्य--आओ सत्य धरम
- 29) सत्य--इस जग में थोड़े दिन
- 30) सत्य--ओ जी थे झूठ
- 31) सत्य--जिया तोहे बार बार
- 32) सत्य--लागे सत्य सुमन
बच्चों के भजन
- 1) उठे सब के कदम
- 2) चाहे अंधियारा हो या
- 3) चौबीस तीर्थंकर नाम चिह्न
- 4) छोटा सा मंदिर
- 5) जगमग आरती कीजे आदीश्वर
- 6) जिनमंदिर आना सभी
- 7) ज्ञाता दृष्टा राही हूं
- 8) ज्ञानी का ध्यानी का सबका
- 9) ठंडे ठंडे पानी से नहाना
- 10) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 11) नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी
- 12) पाठशाला जाना पढ़कर
- 13) माँ मुझे सुना गुरुवर
- 14) माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
- 15) ये जैन होने का परिचय
- 16) रेल चली भई रेल चली
- 17) वंदे शासन
- 18) वर्धमान बोलो भैया बोलो
- 19) सारे जहां में अनुपम
- 20) सुबह उठे मम्मी से बोले
- 21) सूरत प्यारी प्यारी है
- 22) हम होंगे ज्ञानवान एक दिन
मारवाड़ी
- 1) आर्जव--चार दिनां को जीवन मेलो
- 2) कठिन नर तन है पायो
- 3) क्षमा--थाँकी उत्तम क्षमा पै
- 4) गलती आपाँ री न जाणी
- 5) चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न
- 6) चाँदनी फीकी पड़ जाए
- 7) चेतन नरभव ने तू पाकर
- 8) छवि नयन पियारी जी
- 9) जीवड़ा सुनत सुणावत इतरा
- 10) धोली हो गई रे काली कामली
- 11) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 12) पारस प्यारा लागो
- 13) प्राणां सूं भी प्यारी लागे
- 14) महाराजा स्वामी
- 15) म्हानै पतो बताद्यो थाँसू
- 16) म्हारा चेतन ज्ञानी घणो
- 17) लगी म्हारा नैना री डोरी
- 18) शौच--मूंजी धरी रहेली
- 19) हजूरिया ठाडो
selected
- 1) आतम अनुभव आवै
- 2) आतम जानो र भाई
- 3) आवै न भोगन में तोहि
- 4) इक योगी असन बनावे
- 5) कर कर आतमहित रे
- 6) काहे को सोचत अति भारी
- 7) घटमें परमातम ध्याइये
- 8) जपि माला जिनवर
- 9) जिनशासन बड़ा निराला
- 10) जे दिन तुम विवेक बिन
- 11) तुझे बेटा कहूँ कि वीरा
- 12) तू तो समझ समझ रे
- 13) नेमिनाथ--जूनागढ़ में सज
- 14) नेमिनाथ--निर्मोही नेमी जाओ ना
- 15) परम गुरु बरसत ज्ञान झरी
- 16) पुद्गल का क्या विश्वासा
- 17) भगवंत भजन क्यों
- 18) मेरो मनवा अति हर्षाय
- 19) मोक्ष के प्रेमी हमने
- 20) रंग दो जी रंग जिनराज
- 21) रे भाई मोह महा दुखदाता
- 22) रे मन भज भज दीन दयाल
- 23) साधो छांडो विषय विकारी
- 24) सिद्धों की श्रेणी में आने वाला
- 25) हमकौ कछू भय ना
- 26) हे भविजन ध्याओ आतमराम
- 27) होली--जे सहज होरी के
प्रारम्भ
- 1) श्री-मंगलाष्टक-स्तोत्र
- 2) दर्शनं-देव-देवस्य
- 3) दर्शन-पाठ--पण्डित-बुधजन
- 4) दर्शन-पाठ
- 5) प्रतिमा-प्रक्षाल-विधि-पाठ
- 6) अभिषेक-पाठ-भाषा--पण्डित-हरजसराय
- 7) अभिषेक-पाठ-लघु
- 8) मैंने-प्रभुजी-के-चरण
- 9) अमृत-से-गगरी-भरो
- 10) महावीर-की-मूंगावरणी
- 11) विनय-पाठ-दोहावली
- 12) विनय-पाठ-लघु
- 13) मंगलपाठ
- 14) भजन-मैं-थाने-पूजन-आयो
- 15) पूजा-विधि-प्रारंभ
- 16) अर्घ
- 17) स्वस्ति-मंगल-विधान
- 18) स्वस्ति-मंगल-विधान-हिंदी
- 19) चतुर्विंशति-तीर्थंकर-स्वस्ति-विधान
- 20) अथ-परमर्षि-स्वस्ति-मंगल-विधान
- 21) स्तुति--पण्डित-बुधजन
नित्य पूजा
- 1) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-जुगल-किशोर
- 2) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-द्यानतराय
- 3) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 4) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 5) देव-शास्त्र-गुरु--पण्डित-राजमल-पवैया
- 6) समुच्च-पूजा--ब्रह्मचारी-सरदारमल
- 7) पंचपरमेष्ठी--पण्डित-राजमल-पवैया
- 8) नवदेवता-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) नवदेवता-पूजन--आर्यिका-ज्ञानमती
- 10) सिद्धपूजा--पण्डित-राजमल-पवैया
- 11) सिद्धपूजा--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 12) सिद्धपूजा--पण्डित-जुगल-किशोर
- 13) सिद्धपूजा--पण्डित-हीराचंद
- 14) त्रिकाल-चौबीसी-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 15) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) चौबीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 17) अनन्त-तीर्थंकर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 18) श्री-वीतराग-पूजन--पण्डित-रवीन्द्रजी
- 19) रत्नत्रय-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 20) सम्यकदर्शन--पण्डित-द्यानतराय
- 21) सम्यकज्ञान--पण्डित-द्यानतराय
- 22) सम्यकचारित्र--पण्डित-द्यानतराय
- 23) दशलक्षण-धर्म--पण्डित-द्यानतराय
- 24) सोलहकारण-भावना--पण्डित-द्यानतराय
- 25) सरस्वती-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 26) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 27) सीमन्धर-भगवान--पण्डित-हुकमचन्द-भारिल्ल
- 28) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) विद्यमान-बीस-तीर्थंकर--पण्डित-द्यानतराय
- 30) बाहुबली-भगवान--पण्डित-राजमल-पवैया
- 31) बाहुबली-भगवान--ब्रह्मचारी-रवीन्द्र
- 32) पंचमेरु-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 33) नंदीश्वर-द्वीप-पूजन--पण्डित-द्यानतराय
- 34) निर्वाणक्षेत्र--पण्डित-द्यानतराय
- 35) कृत्रिमाकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 36) अष्टापद-कैलाश-पूजन
- 37) आ-कुंदकुंद-पूजन
तीर्थंकर
- 1) श्रीआदिनाथ--पण्डित-राजमल-पवैया
- 2) आदिनाथ-भगवान--पण्डित-जिनेश्वरदास
- 3) श्रीआदिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 4) श्रीअजितनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 5) श्रीसंभवनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 6) श्रीअभिनन्दननाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 7) श्रीसुमतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 8) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 9) श्रीपद्मप्रभ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 10) श्रीसुपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 11) श्रीचन्द्रप्रभनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 12) श्रीपुष्पदन्त-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 13) श्रीशीतलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 14) श्रीश्रेयांसनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 15) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 16) श्रीवासुपूज्य-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 17) श्रीविमलनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 18) श्रीअनन्तनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 19) श्रीधर्मनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 20) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 21) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 22) श्रीशांतिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 23) श्रीकुंथुनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 24) श्रीअरहनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 25) श्रीमल्लिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 26) श्रीमुनिसुव्रतनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 27) श्रीनमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 28) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 29) श्रीनेमिनाथ-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 30) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-बख्तावर
- 31) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 32) श्रीपार्श्वनाथ-पूजन-पण्डित-वृन्दावनदास
- 33) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-राजमल-पवैया
- 34) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-वृन्दावनदास
- 35) श्रीमहावीर-पूजन--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
पर्व पूजन
विसर्जन
पाठ
- 1) देव-स्तुति--पण्डित-भूधरदास
- 2) मेरी-भावना--पण्डित-जुगलकिशोर
- 3) बारह-भावना--पण्डित-जयचंद-छाबडा
- 4) बारह-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 5) बारह-भावना--पण्डित.-मंगतराय
- 6) महावीर-वंदना--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 7) समाधिमरण--पण्डित-द्यानतराय
- 8) समाधि-भावना--पण्डित-शिवराम
- 9) समाधिमरण-भाषा--पण्डित-सूरचंद
- 10) दर्शन-स्तुति--पण्डित-दौलतराम
- 11) जिनवाणी-स्तुति
- 12) आराधना-पाठ--पण्डित-द्यानतराय
- 13) आर्हत-वंदना--पण्डित-जुगल-किशोर
- 14) आलोचना-पाठ--पण्डित-जौहरिलाल
- 15) दुखहरन-विनती--पण्डित-वृन्दावनदास
- 16) अमूल्य-तत्त्व-विचार--श्रीमद-राजचन्द्र
- 17) बाईस-परीषह--आर्यिका-ज्ञानमती
- 18) सामायिक-पाठ--आचार्य-अमितगति
- 19) सामायिक-पाठ--पण्डित-महाचंद्र
- 20) सामायिक-पाठ--पण्डित-जुगल-किशोर
- 21) निर्वाण-कांड--पण्डित-भगवतीदास
- 22) देव-शास्त्र-गुरु-वंदना
- 23) वैराग्य-भावना--पण्डित-भूधरदास
- 24) भूधर-शतक--पण्डित-भूधरदास
- 25) आत्मबोध-शतक--आर्यिका-पूर्णमति
- 26) चौबीस-तीर्थंकर-स्तवन--पण्डित-अभयकुमार
- 27) लघु-प्रतिक्रमण
- 28) मृत्युमहोत्सव
- 29) अपूर्व-अवसर--श्रीमद-राजचंद्र
- 30) कुंदकुंद-शतक--पण्डित-हुकमचंद-भारिल्ल
- 31) सिद्ध-श्रुत-आचार्य-भक्ति
- 32) ध्यान-सूत्र-शतक--आचार्य-माघनंदी
- 33) पखवाड़ा--पण्डित-द्यानतराय
- 34) श्री-गोम्टेश्वर-स्तुति
- 35) श्रीजिनेन्द्रगुणसंस्तुति--श्रीपात्रकेसरिस्वामि
- 36) रत्नाकर-पंचविंशतिका--पण्डित-रामचरित
- 37) भूपाल-पंचविंशतिका--पण्डित-भूधरदास
- 38) सच्चा-जैन--रवीन्द्र-जी-आत्मन
- 39) सरस्वती-वंदना
स्तोत्र
- 1) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--आचार्य-समंतभद्र
- 2) स्वयंभू-स्तोत्र-भाषा--पण्डित-द्यानतराय
- 3) स्वयंभू-स्तोत्र--आचार्य-विद्यासागर
- 4) पार्श्वनाथ-स्त्रोत्र--पण्डित-द्यनतराय
- 5) महावीराष्टक-स्तोत्र--पण्डित-भागचन्द्र
- 6) वीतराग-स्तोत्र--मुनि-क्षमासागर
- 7) कल्याणमन्दिरस्तोत्रम--आचार्य-कुमुदचंद्र
- 8) कल्याणमन्दिर-स्तोत्र-हिंदी--आर्यिका-चंदानामती
- 9) भक्तामर--आचार्य-मानतुंग
- 10) भक्तामर--पण्डित-हेमराज
- 11) भक्तामर--मुनि-श्रीरसागर
- 12) एकीभाव-स्तोत्र--आचार्य-वादीराज
- 13) विषापहारस्तोत्रम्--कवि-धनञ्जय
- 14) विषापहारस्तोत्र--पण्डित-शांतिदास
- 15) अकलंक-स्तोत्र
- 16) गणधरवलय-स्तोत्र
- 17) मंदालसा-स्तोत्र
- 18) श्रीमज्जिनसहस्रनाम-स्तोत्र
ग्रंथ
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पञ्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
चरणानुयोग
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
इतिहास
Notes
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पञ्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
द्रव्यानुयोग
- 1) समयसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 2) प्रवचनसार--कुन्दकुन्दाचार्य
- 3) पञ्चास्तिकाय--कुन्दकुन्दाचार्य
- 4) द्रव्यसंग्रह--नेमिचंद्र-सिद्धांतचक्रवर्ती
- 5) समाधितन्त्र--आचार्य-पूज्यपाद
- 6) स्वरूप-संबोधन--अकलंक-देव
- 7) इष्टोपदेश--आचार्य-पूज्यपाद
- 8) परमात्मप्रकाश--योगींदुदेव
- 9) योगसार-प्राभृत--अमितगति-आचार्य
- 10) तत्त्वार्थसूत्र--आचार्य-उमास्वामी
- 11) योगसार--योगींदुदेव
- 12) पंचाध्यायी
- 13) पाहुड-दोहा--राम-सिंह-मुनि
- 14) परम-अध्यात्म-तरंगिणी--अमृतचंद्राचार्य
- 15) तत्त्वज्ञान-तरंगिणी--भट्टारक-ज्ञानभूषण
- 16) सिद्धान्त-सार--भट्टारक-सकलकीर्ति
- 17) अमृताशीति--योगींदुदेव
- 18) तत्त्वसार--देवसेनाचार्य
चरणानुयोग
- 1) नियमसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 2) श्रीअष्टपाहुड--कुन्दकुंदाचार्य
- 3) मूलाचार--वट्टकेराचार्य
- 4) वारासाणुवेक्खा--स्वामि-कार्तिकेय
- 5) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय--आ-अमृतचन्द्र
- 6) बारसणुपेक्खा--कुन्दकुन्दाचार्य
- 7) रत्नकरण्ड-श्रावकाचार--समन्तभद्राचार्य
- 8) आराधनासार--देवसेनाचार्य
- 9) ज्ञानार्णव--शुभचंद्राचार्य
- 10) भगवती-आराधना--शिवाचार्य
- 11) पद्मनंदी-पंचविन्शतिका--आ-पद्मनंदी
- 12) आत्मानुशासन--आ-गुणभद्र
- 13) रयणसार--कुन्दकुंदाचार्य
- 14) उपासकाध्ययन--सोमदेवाचार्य
करणानुयोग
प्रथमानुयोग
- 1) आराधना-कथा-कोश--ब्र-नेमिदत्त
- 2) उत्तरपुराण--गुणभद्राचार्य
- 3) उत्तरपुराण-संस्कृत--गुणभद्राचार्य
- 4) पद्मपुराण--रविषेणाचार्य
- 5) आदिपुराण--जिनसेनाचार्य
- 6) महावीर-पुराण--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 7) जम्बूस्वामी-चारित्र
- 8) सुकुमाल-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 9) सुदर्शन-चरित्र--सकलकीर्ति-भट्टारक
- 10) सम्यक्त्व-कौमुदि
- 11) धर्मामृत--नयसेनाचार्य
न्याय
Youtube -- शास्त्र गाथा
Youtube -- Animations
- भगवान नमिनाथ
- भगवान बाहुबली
- सुकुमाल मुनि
- कुन्दकुन्द आचार्य
- रक्षाबंधन की कथा
- समवसरण
- चार-गति
- श्रुत-पंचमी
- अक्षय-तृतीया
- उद्दायन राजा
- राजा श्रेणिक और मेंढक
- अंजन-चोर की कथा
- पांच-पाप
- जीव-दया
- गर्भ-कल्याणक
- जन्म-कल्याणक
- तप-कल्याणक
- णमोकार-मंत्र
- कुलाचार
- स्थावर-जीव
- तीर्थंकर
- जीव-अजीव
- चतुर्विध-संघ
- प्रात:कालीन वन्दना
प्रमाण
PDF शास्त्र
- गोम्मटसार-जीवकांड
- तत्त्वार्थसूत्र-चार्ट
- तत्त्वार्थसूत्र-English
- पाहुड-दोहा
- तत्त्वानुशासन
- लघुतत्त्व-स्फोट
- परम-अध्यात्म-तरंगिनी
- ज्ञानार्णव
- भगवती-आराधना
- आराधानासार
- जैन-सिद्धांत-प्रवेशिका
- समयसार
- योगसार
- प्रवचनसार
- पन्चास्तिकाय
- द्रव्यसंग्रह
- दर्शनसार
- तत्त्वार्थसूत्र
- आलापपद्धति
- इष्टोपदेश
- परमात्मप्रकाश
- पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
- बारसणुपेक्_खा
- रत्नकरण्ड-श्रावकाचार
- श्रीअष्टपाहुड
- समाधितन्त्र
- स्वरूप-संबोधन
- उत्तर-पुराण
- आदि-पुराण
- आराधना-कथा-कोश
Jain Comics
- FruitsOfAuspiciousActs
- JeevandharSwami
- अज्ञात-प्रतिमा-की-खोज
- आटे-का-मुर्गा
- ऋषभदेव
- कविवर-बनारसीदास
- कुन्दकुन्दाचार्य
- गए-जा-गीत-अपन-के
- गोमटेश्वर-बाहुबली
- चंदनबाला
- चौबीस-तीर्थंकर-१
- चौबीस-तीर्थंकर-२
- जनक-नन्दिनी-सीता
- जीवंधर-स्वामी
- जो-करे-सो-भरे
- टीले-वाले-बाबा
- ताली-एक-हाथ-से-बजती-रही
- तीन-दिन-में
- धर्म-के-दश-लक्षण
- पुण्य-का-फल
- प्रद्युम्न-हरण
- प्रेय-की-भभूत
- महादानी-भामाशाह
- महाबली-हनूमान
- महारानी-चेलना-की-विजय
- मुनि-रक्षा
- राजुल
- रूप-जो-बदला-नहीं-जाता
- सिकन्दर-और-कल्याण-मुनि
Print Granth
Kids Games
भक्तामर
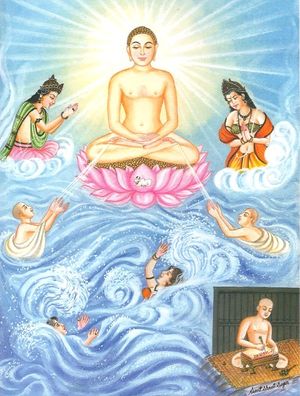
आ. मानतुंग कृत
भक्तामर-प्रणत-मौलिमणि-प्रभाणा-
मुद्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा-
वालंबनं भवजले पततां जनानाम् ॥१॥
भक्तामर-प्रणत-मौलिमणि-प्रभाणा-
मुद्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा-
वालंबनं भवजले पततां जनानाम् ॥१॥
भक्त अमर नत-मुकुट सुमणियों, की सुप्रभा का जो भासक
पापरूप अतिसघन-तिमिर का, ज्ञान-दिवाकर-सा नाशक ॥
भव-जल पतित जनों को जिसने, दिया आदि में अवलम्बन
उनके चरण-कमल को करते, सम्यक् बारम्बार नमन ॥१॥
पापरूप अतिसघन-तिमिर का, ज्ञान-दिवाकर-सा नाशक ॥
भव-जल पतित जनों को जिसने, दिया आदि में अवलम्बन
उनके चरण-कमल को करते, सम्यक् बारम्बार नमन ॥१॥
अन्वयार्थ : झुके हुए भक्त देवों के मुकुट-जड़ित मणियों की प्रथा को प्रकाशित करने वाले, पाप रुपी अंधकार के समुह को नष्ट करने वाले, कर्म-युग के प्रारम्भ में संसार-समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिये आलम्बन भूत जिनेन्द्र-देव के चरण-युगल को मन-वचन-काय से प्रणाम करके (मैं मुनि मानतुंग उनकी स्तुति करुँगा) ।
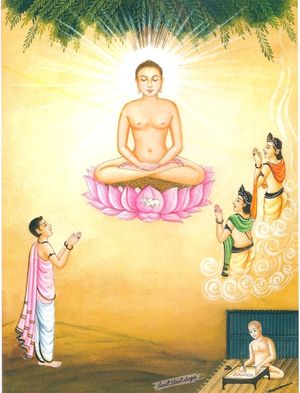
यः संस्तुतः सकल-वाङ्गमय-तत्त्वबोधा-
दुद्भूत-बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥
दुद्भूत-बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥
सकल वाङ् मय तत्त्वबोध से, उद्भव पटुतर धी-धारी
उसी इन्द्र की स्तुति से है, वन्दित जग-जन मनहारी ॥
अति आश्चर्य की स्तुति करता, उसी प्रथम जिन स्वामी की
जगनामी-सुखधामी तद्भव-शिवगामी अभिरामी की ॥२॥
उसी इन्द्र की स्तुति से है, वन्दित जग-जन मनहारी ॥
अति आश्चर्य की स्तुति करता, उसी प्रथम जिन स्वामी की
जगनामी-सुखधामी तद्भव-शिवगामी अभिरामी की ॥२॥
अन्वयार्थ : सम्पूर्ण श्रुतज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इन्द्रों के द्वारा तीन-लोक के मन को हरने वाले, गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है उन प्रथम तीर्थंकर (आदिनाथ जिनेन्द्र) की निश्चय ही मैं (मानतुंग) भी स्तुति करुँगा ।
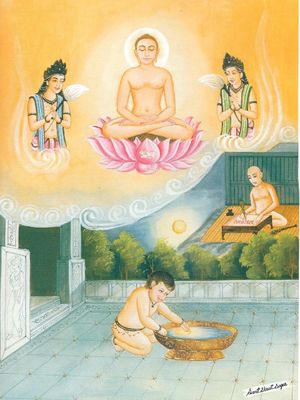
बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम्
बालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब-
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम्
बालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब-
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥
स्तुति को तैयार हुआ हूँ, मैं निर्बुद्धि छोड़ के लाज
विज्ञजनों से अर्चित हैं प्रभु, मंदबुद्धि की रखना लाज ॥
जल में पड़े चन्द्र-मंडल को, बालक बिना कौन मतिमान ?
सहसा उसे पकडऩे वाली, प्रबलेच्छा करता गतिमान ॥३॥
विज्ञजनों से अर्चित हैं प्रभु, मंदबुद्धि की रखना लाज ॥
जल में पड़े चन्द्र-मंडल को, बालक बिना कौन मतिमान ?
सहसा उसे पकडऩे वाली, प्रबलेच्छा करता गतिमान ॥३॥
अन्वयार्थ : देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेन्द्र ! मैं बुद्धि-रहित, निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिये तत्पर हुआ हूँ क्योंकि जल में स्थित चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को बालक को छोड़कर दूसरा कौन सहसा पकड़ने की इच्छा करता है?
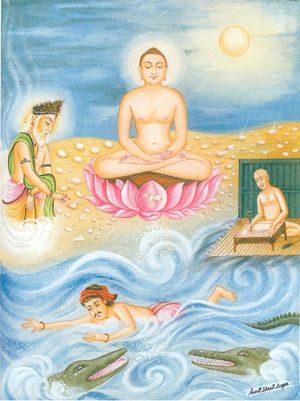
वक्तुं गुणान्गुण-समुद्र शशाङक-कान्तान्
कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धया
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॥४॥
कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धया
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॥४॥
हे जिन ! चन्द्रकान्त से बढक़र, तव गुण विपुल अमल अतिश्वेत
कह न सकें नर हे गुण-सागर, सुर-गुरु के सम बुद्धिसमेत ॥
मक्र-नक्र-चक्रादि जन्तु युत, प्रलय पवन से बढ़ा अपार
कौन भुजाओं से समुद्र के, हो सकता है परले पार ॥४॥
कह न सकें नर हे गुण-सागर, सुर-गुरु के सम बुद्धिसमेत ॥
मक्र-नक्र-चक्रादि जन्तु युत, प्रलय पवन से बढ़ा अपार
कौन भुजाओं से समुद्र के, हो सकता है परले पार ॥४॥
अन्वयार्थ : हे गुणों के भंडार ! आपके चन्द्रमा के समान सुन्दर गुणों को कहने लिये ब्रहस्पति के सद्रश भी कौन पुरुष समर्थ है ? प्रलयकाल की वायु के द्वारा प्रचण्ड है मगरमच्छों का समूह जिसमें, ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है ?
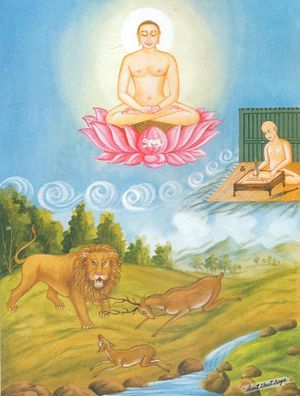
सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश
कर्तुं स्तवं विगत-शक्तिरपि प्रवृत्तः
प्रीत्यात्म-वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं
नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपालनार्थम् ॥५॥
कर्तुं स्तवं विगत-शक्तिरपि प्रवृत्तः
प्रीत्यात्म-वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं
नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपालनार्थम् ॥५॥
वह मैं हूँ, कुछ शक्ति न रखकर, भक्ति प्रेरणा से लाचार
करता हूँ स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौर्वा-पर्य विचार ॥
निज शिशु की रक्षार्थ आत्म-बल, बिना विचारे क्या न मृगी
जाती है मृगपति के आगे, शिशु-सनेह में हुई रंगी ॥५॥
करता हूँ स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौर्वा-पर्य विचार ॥
निज शिशु की रक्षार्थ आत्म-बल, बिना विचारे क्या न मृगी
जाती है मृगपति के आगे, शिशु-सनेह में हुई रंगी ॥५॥
अन्वयार्थ : हे मुनीश ! शक्ति रहित होता हुआ भी, मैं अल्पज्ञ, भक्तिवश, आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ; हरिणि, अपनी शक्ति का विचार न कर, प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिये, क्या सिंह के सामने नहीं जाती ?
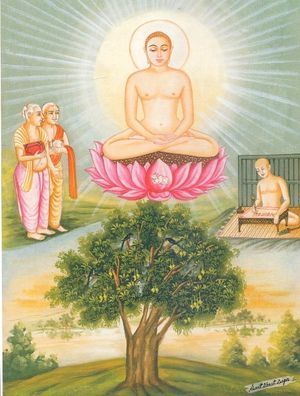
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्र-चारु- कलिका निकरैकहेतु ॥६॥
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्र-चारु- कलिका निकरैकहेतु ॥६॥
अल्पश्रुत हूँ श्रुतवानों से, हास्य कराने का ही धाम
करती है वाचाल मुझे प्रभु! भक्ति आपकी आठों याम ॥
करती मधुर गान पिक मधु में, जग-जन मनहर अति अभिराम
उसमें हेतु सरस फल-फूलों, से युत हरे-भरे तरु -आम ॥६॥
करती है वाचाल मुझे प्रभु! भक्ति आपकी आठों याम ॥
करती मधुर गान पिक मधु में, जग-जन मनहर अति अभिराम
उसमें हेतु सरस फल-फूलों, से युत हरे-भरे तरु -आम ॥६॥
अन्वयार्थ : विद्वानों की हँसी के पात्र, मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है; बसन्त ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है उसमें निश्चय से आम्र-कलिका ही एक मात्र कारण है ।
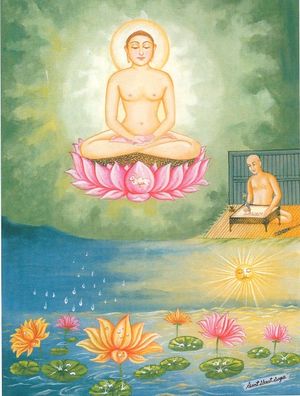
त्वत्संस्तवेन भव-संतति-सन्निबद्धं
पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्
आक्रान्त -लोकमलि-नीलमशेषमाशु
सूर्यांशु-भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥७॥
पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्
आक्रान्त -लोकमलि-नीलमशेषमाशु
सूर्यांशु-भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥७॥
जिनवर की स्तुति करने से, चिर संचित भविजन के पाप
पलभर में भग जाते निश्चित, इधर-उधर अपने ही आप ॥
सकल लोक में व्याप्त रात्रि का, भ्रमर सरीखा काला ध्वान्त
प्रात: रवि की उग्र किरण लख, हो जाता क्षण में प्राणान्त ॥७॥
पलभर में भग जाते निश्चित, इधर-उधर अपने ही आप ॥
सकल लोक में व्याप्त रात्रि का, भ्रमर सरीखा काला ध्वान्त
प्रात: रवि की उग्र किरण लख, हो जाता क्षण में प्राणान्त ॥७॥
अन्वयार्थ : आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों में बाँधे गये पाप-कर्म क्षण-भर में नष्ट हो जाते हैं जैसे सम्पूर्ण लोक में व्याप्त रात्री का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षणभर में छिन्न-भिन्न हो जाता है ।
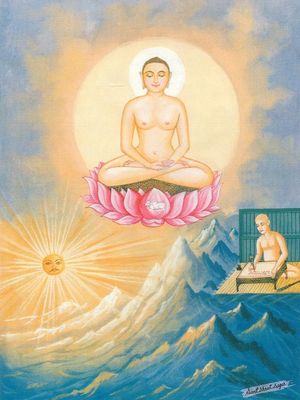
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु
मुक्ता-फल द्युतिमुपैति ननूद-बिन्दुः ॥८॥
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु
मुक्ता-फल द्युतिमुपैति ननूद-बिन्दुः ॥८॥
मैं मतिहीन-दीन प्रभु तेरी, शुरू करूँ स्तुति अघ-हान
प्रभु-प्रभाव ही चित्त हरेगा, सन्तों का निश्चय से मान ॥
जैसे कमल-पत्र पर जल-कण, मोती जैसे आभावान
दिपते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में हे भगवान् ॥८॥
प्रभु-प्रभाव ही चित्त हरेगा, सन्तों का निश्चय से मान ॥
जैसे कमल-पत्र पर जल-कण, मोती जैसे आभावान
दिपते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में हे भगवान् ॥८॥
अन्वयार्थ : हे स्वामिन् ! ऐसा मानकर मुझ मन्द-बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारम्भ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा; निश्चय से पानी की बूँद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभा को प्राप्त करती है ।

आस्तां तव स्तवनमस्त-समस्त-दोषं
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति
दूरे सहस्त्रकिरणः कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि ॥९॥
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति
दूरे सहस्त्रकिरणः कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि ॥९॥
दूर रहे स्तोत्र आपका, जो कि सर्वथा है निर्दोष
पुण्य-कथा ही किन्तु आपकी, हर लेती है कल्मष-कोष ॥
प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलों को भरपूर
फेंका करता सूर्य-किरण को, आप रहा करता है दूर ॥९॥
पुण्य-कथा ही किन्तु आपकी, हर लेती है कल्मष-कोष ॥
प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलों को भरपूर
फेंका करता सूर्य-किरण को, आप रहा करता है दूर ॥९॥
अन्वयार्थ : सम्पूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है; सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है ।
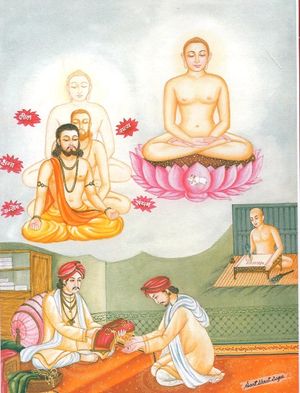
नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥
त्रिभुवन-तिलक जगत-पति हे प्रभु! सद्गुरुओं के हे गुरुवर्य
सद्भक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य ॥
स्वाश्रित जन को निजसम करते, धनी लोग धन धरनी से
नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या ? उन धनिकों की करनी से ॥१०॥
सद्भक्तों को निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य ॥
स्वाश्रित जन को निजसम करते, धनी लोग धन धरनी से
नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या ? उन धनिकों की करनी से ॥१०॥
अन्वयार्थ : हे जगत् के भूषण ! हे प्राणियों के नाथ ! सत्यगुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष, पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन, जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को सम्पत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता ।

दृष्टवा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः
पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ॥११॥
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः
पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ॥११॥
हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु! तुम्हें देखकर परम-पवित्र
तोषित होते कभी नहीं हैं, नयन मानवों के अन्यत्र ॥
चन्द्रकिरण सम उज्ज्वल निर्मल, क्षीरोदधि का कर जल पान
कालोदधि का खारा पानी, पीना चाहे कौन पुमान ॥११॥
तोषित होते कभी नहीं हैं, नयन मानवों के अन्यत्र ॥
चन्द्रकिरण सम उज्ज्वल निर्मल, क्षीरोदधि का कर जल पान
कालोदधि का खारा पानी, पीना चाहे कौन पुमान ॥११॥
अन्वयार्थ : हे अनिमेष दर्शनीय प्रभो ! आपके दर्शन के पश्चात् मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र सन्तोष को प्राप्त नहीं होते । चन्द्रकीर्ति के समान निर्मल क्षीर-समुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा ?

यैः शान्त-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्तवं
निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥
निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥
जिन जितने जैसे अणुओं से, निर्मापित प्रभु तेरी देह
थे उतने वैसे अणु जग में, शान्ति-राग-मय नि:सन्देह ॥
हे त्रिभुवन के शिरोभाग के, अद्वितीय आभूषण-रूप
इसीलिये तो आप सरीखा, नहीं दूसरों का है रूप ॥१२॥
थे उतने वैसे अणु जग में, शान्ति-राग-मय नि:सन्देह ॥
हे त्रिभुवन के शिरोभाग के, अद्वितीय आभूषण-रूप
इसीलिये तो आप सरीखा, नहीं दूसरों का है रूप ॥१२॥
अन्वयार्थ : हे त्रिभुवन के एकमात्र आभुषण जिनेन्द्रदेव ! जिन राग-रहित सुन्दर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई, वे परमाणु, पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है ।
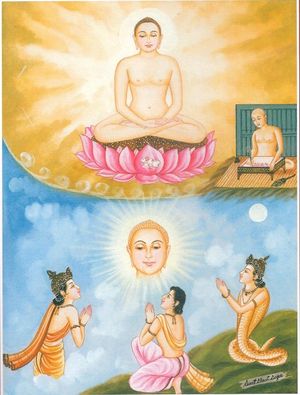
वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि
निःशेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम्
बिम्बं कलङ्क मलिनं क्व निशाकरस्य
यद्वासरे भवति पांडु-पलाशकल्पम् ॥१३॥
निःशेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम्
बिम्बं कलङ्क मलिनं क्व निशाकरस्य
यद्वासरे भवति पांडु-पलाशकल्पम् ॥१३॥
कहाँ आपका मुख अतिसुंदर, सुर-नर उरग नेत्रहारी
जिसने जीत लिये सब जग के, जितने थे उपमाधारी ॥
कहाँ कलंकी बंक चन्द्रमा, रंक-समान कीट-सा दीन
जो पलाश-सा फीका पड़ता,दिन में हो करके छबि-छीन ॥१३॥
जिसने जीत लिये सब जग के, जितने थे उपमाधारी ॥
कहाँ कलंकी बंक चन्द्रमा, रंक-समान कीट-सा दीन
जो पलाश-सा फीका पड़ता,दिन में हो करके छबि-छीन ॥१३॥
अन्वयार्थ : हे प्रभो ! सम्पूर्ण रुप से तीनों जगत् की उपमाओं का विजेता, देव मनुष्य तथा धरणेन्द्र के नेत्रों को हरने वाला कहां आपका मुख ? और कलंक से मलिन, चन्द्रमा का वह मण्डल कहां ? जो दिन में पलाश (ढाक) के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है ।
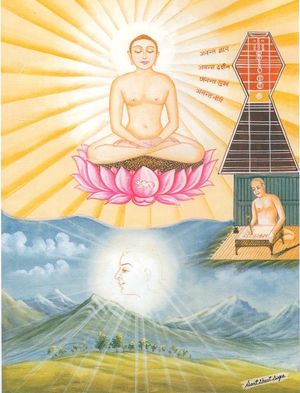
सम्पूर्ण-मण्डल-शशाङ्क-कला-कलाप-
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति
ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वर नाथमेकं
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥१४॥
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति
ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वर नाथमेकं
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥१४॥
तव गुण पूर्ण-शशांक कान्तिमय, कला-कलापों से बढक़े
तीन लोक में व्याप रहे हैं, जो कि स्वच्छता में चढक़े ॥
विचरें चाहे जहाँ कि जिनको, जगन्नाथ का एकाधार
कौन माई का जाया रखता, उन्हें रोकने का अधिकार ॥१४॥
तीन लोक में व्याप रहे हैं, जो कि स्वच्छता में चढक़े ॥
विचरें चाहे जहाँ कि जिनको, जगन्नाथ का एकाधार
कौन माई का जाया रखता, उन्हें रोकने का अधिकार ॥१४॥
अन्वयार्थ : पूर्ण चन्द्र की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके गुण तीनों-लोक में व्याप्त हैं क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत् के भी नाथ के आश्रित हैं उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है ?

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि
र्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् ॥
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन
किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ॥१५॥
र्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् ॥
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन
किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ॥१५॥
मद की छकी अमर ललनाएँ, प्रभु के मन में तनिक विकार
कर न सकीं आश्चर्य कौन-सा, रह जाती हैं मन को मार ॥
गिरि गिर जाते प्रलय पवन से, तो फिर क्या वह मेरु-शिखर
हिल सकता है रंच-मात्र भी, पाकर झंझावात प्रखर ॥१५॥
कर न सकीं आश्चर्य कौन-सा, रह जाती हैं मन को मार ॥
गिरि गिर जाते प्रलय पवन से, तो फिर क्या वह मेरु-शिखर
हिल सकता है रंच-मात्र भी, पाकर झंझावात प्रखर ॥१५॥
अन्वयार्थ : यदि आपका मन देवागंनाओं के द्वारा किंचित् भी विक्रति को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है ? पर्वतों को हिला देने वाली प्रलयकाल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है ?

निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि ॥
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि ॥
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥
धूम न बत्ती तैल बिना ही, प्रकट दिखाते तीनों लोक
गिरि के शिखर उड़ाने वाली, बुझा न सकती मारुत झोक ॥
तिस पर सदा प्रकाशित रहते, गिनते नहीं कभी दिन-रात
ऐसे अनुपम आप दीप हैं, स्वपर प्रकाशक जग विख्यात ॥१६॥
गिरि के शिखर उड़ाने वाली, बुझा न सकती मारुत झोक ॥
तिस पर सदा प्रकाशित रहते, गिनते नहीं कभी दिन-रात
ऐसे अनुपम आप दीप हैं, स्वपर प्रकाशक जग विख्यात ॥१६॥
अन्वयार्थ : हे स्वामिन् ! आप धूम तथा बाती से रहित, तेल के प्रवाह के बिना भी इस सम्पूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत-प्रकाशक अलौकिक दीपक हैं जिसे विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावात भी कभी बुझा नहीं सकता ।
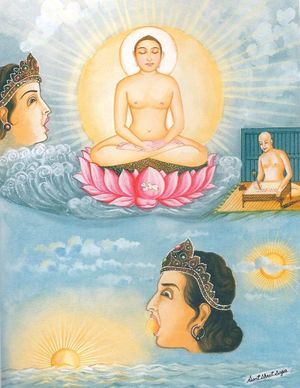
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नाम्भोधरोदर निरुद्धमहाप्रभावः
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके ॥१७॥
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नाम्भोधरोदर निरुद्धमहाप्रभावः
सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके ॥१७॥
अस्त न होता कभी न जिसको, ग्रस पाता है राहु प्रबल
एक साथ बतलाने वाला, तीन लोक का ज्ञान विमल ॥
रुकता कभी प्रभाव न जिसका, बादल की आकर के ओट
ऐसी गौरव-गरिमा वाले, आप अपूर्व दिवाकर कोट ॥१७॥
एक साथ बतलाने वाला, तीन लोक का ज्ञान विमल ॥
रुकता कभी प्रभाव न जिसका, बादल की आकर के ओट
ऐसी गौरव-गरिमा वाले, आप अपूर्व दिवाकर कोट ॥१७॥
अन्वयार्थ : हे मुनीन्द्ररुपी सूर्य ! आप न तो कभी अस्त होते हैं न ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं और न आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावन्त हैं ।
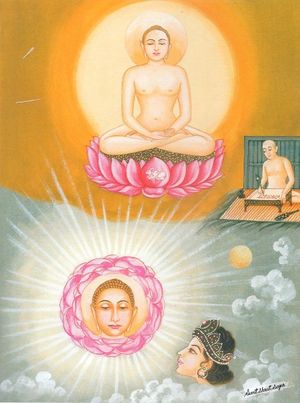
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम्
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कान्ति
विद्योतयज्जगदपूर्व-शशाङ्क-बिम्बम् ॥१८॥
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम्
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कान्ति
विद्योतयज्जगदपूर्व-शशाङ्क-बिम्बम् ॥१८॥
मोह महातम दलने वाला, सदा उदित रहने वाला
राहु न बादल से दबता पर, सदा स्वच्छ रहने वाला ॥
विश्व प्रकाशकमुख-सरोज तब, अधिक कांतिमय शांतिस्वरूप
है अपूर्व जग का शशिमंडल, जगत शिरोमणि शिव का भूप ॥१८॥
राहु न बादल से दबता पर, सदा स्वच्छ रहने वाला ॥
विश्व प्रकाशकमुख-सरोज तब, अधिक कांतिमय शांतिस्वरूप
है अपूर्व जग का शशिमंडल, जगत शिरोमणि शिव का भूप ॥१८॥
अन्वयार्थ : हे जिनेन्द्रदेव ! आपका मुख-मंडल नित्य उदित रहने वाला विलक्षण चंद्रमा है, जिसने मोहरूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, जो अत्यंत दीप्तिमान है, जिसे न राहु ग्रस सकता है और न बादल छिपा सकते हैं, तथा जो जगत को प्रकाशित करता हुआ अलौकिक चंद्रमंडल की तरह सुशोभित होता है ।
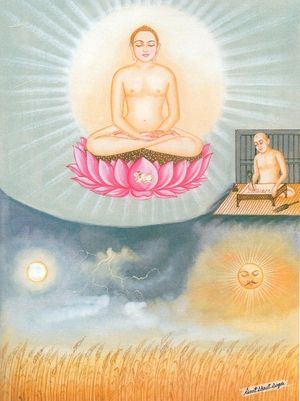
किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमस्सु नाथ
निष्पन्न- शालि-वन-शालिनि जीव-लोके
कार्यं कियज्जलधरैर्जल-भार-नम्रैः ॥१९॥
युष्मन्मुखेन्दु-दलितेषु तमस्सु नाथ
निष्पन्न- शालि-वन-शालिनि जीव-लोके
कार्यं कियज्जलधरैर्जल-भार-नम्रैः ॥१९॥
नाथ ! आपका मुख जब करता, अन्धकार का सत्यानाश
तब दिन में रवि और रात्रि में, चन्द्रबिम्ब का विफल प्रयास ॥
धान्य खेत जब धरती तल के, पके हुए हों अति अभिराम
शोर मचाते जल को लादे, हुए घनों से तब क्या काम ? ॥१९॥
तब दिन में रवि और रात्रि में, चन्द्रबिम्ब का विफल प्रयास ॥
धान्य खेत जब धरती तल के, पके हुए हों अति अभिराम
शोर मचाते जल को लादे, हुए घनों से तब क्या काम ? ॥१९॥
अन्वयार्थ : हे स्वामिन् ! जब अंधकार आपके मुख रुपी चन्द्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चन्द्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन ? जैसे कि पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन ।
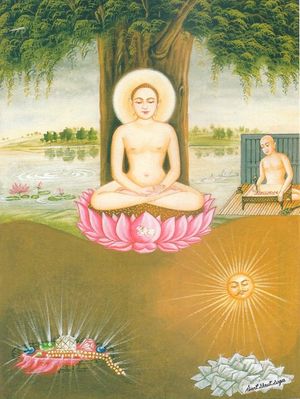
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं
नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥
नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं
नैवं तु काच-शकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥
जैसा शोभित होता प्रभु का, स्वपर प्रकाशक उत्तम ज्ञान
हरि-हरादि देवों में वैसा, कभी नहीं हो सकता भान ॥
अति ज्योर्तिमय महारतन का, जो महत्त्व देखा जाता
क्या वह किरणा-कुलित काँच में, अरे कभी लेखा जाता ॥२०॥
हरि-हरादि देवों में वैसा, कभी नहीं हो सकता भान ॥
अति ज्योर्तिमय महारतन का, जो महत्त्व देखा जाता
क्या वह किरणा-कुलित काँच में, अरे कभी लेखा जाता ॥२०॥
अन्वयार्थ : अनंत गुण-पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान जिस प्रकार आप में सुशोभित होता है वैसा हरि-हरादिक (विष्णु-ब्रह्मा-महेश आदि) लौकिक देवों में है ही नहीं । स्फ़ुरायमान महारत्नों में जैसा तेज होता है, किरणों की राशि से व्याप्त होने पर भी काँच के टुकडों में वैसा तेज नहीं होता ।
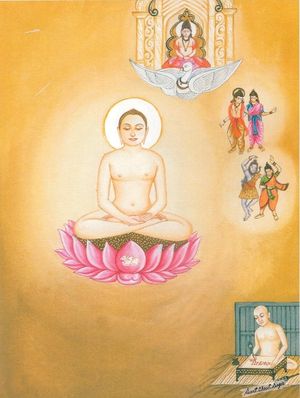
मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥
हरिहरादि देवों का ही मैं, मानूँ उत्तम अवलोकन
क्योंकि उन्हें देखने भर से, तुझसे तोषित होता मन ॥
है परन्तु क्या तुम्हें देखने, से हे स्वामिन्! मुझको लाभ
जन्म-जन्म में लुभा न पाते, कोई यह मेरा अमिताभ ॥२१॥
क्योंकि उन्हें देखने भर से, तुझसे तोषित होता मन ॥
है परन्तु क्या तुम्हें देखने, से हे स्वामिन्! मुझको लाभ
जन्म-जन्म में लुभा न पाते, कोई यह मेरा अमिताभ ॥२१॥
अन्वयार्थ : हे स्वामिन् ! इस पृथ्वी पर मैने विष्णु और महादेव देखे, तो ठीक ही है, क्योंकि उन्हें देखकर, आपको देखने के बाद मन तृप्त हुआ, किन्तु आपको देखने से क्या लाभ ? जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मान्तर में भी चित्त को नहीं हर पाता ।
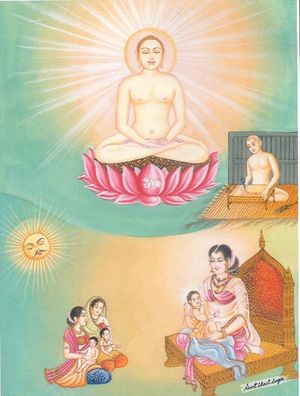
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र-रश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं ॥२२॥
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्र-रश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं ॥२२॥
सौ-सौ नारी, सौ-सौ सुत को, जनती रहती सौ-सौ ठौर
तुम से सुत को जनने वाली, जननी महती क्या है और ॥
तारागण को सर्व दिशाएँ धरें नहीं कोई खाली
पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को जनने वाली ॥२२॥
तुम से सुत को जनने वाली, जननी महती क्या है और ॥
तारागण को सर्व दिशाएँ धरें नहीं कोई खाली
पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को जनने वाली ॥२२॥
अन्वयार्थ : सैकड़ों-स्त्रियाँ सैकड़ों-पुत्रों को जन्म देती हैं, परन्तु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी । नक्षत्रों को सभी दिशायें धारण करती हैं परन्तु कान्तिमान् किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व-दिशा ही जन्म देती है ।

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस-
मादित्य-वर्णममलं तमसः पुरस्तात्
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयंति मृत्युं
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्थाः ॥२३॥
मादित्य-वर्णममलं तमसः पुरस्तात्
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयंति मृत्युं
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्थाः ॥२३॥
तुम को परम पुरुष मुनि मानें, विमल वर्ण रवि तमहारी
तुम्हें प्राप्त कर मृत्युञ्जय के, बन जाते जन अधिकारी ॥
तुम्हें छोडक़र अन्य न कोई, शिवपुर-पथ बतलाता है
किन्तु विपर्यय मार्ग बताकर, भव-भव में भटकाता है ॥२३॥
तुम्हें प्राप्त कर मृत्युञ्जय के, बन जाते जन अधिकारी ॥
तुम्हें छोडक़र अन्य न कोई, शिवपुर-पथ बतलाता है
किन्तु विपर्यय मार्ग बताकर, भव-भव में भटकाता है ॥२३॥
अन्वयार्थ : हे मुनीन्द्र ! तपस्वीजन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी, निर्मल और मोहान्धकार से परे रहने वाले परम-पुरुष मानते हैं । वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं । इसके सिवाय मोक्षपद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है ।
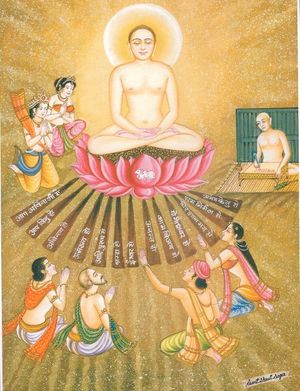
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं
ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनंगकेतुम्
योगीश्वरं विदित-योगमनेकमेकं
ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥
ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनंगकेतुम्
योगीश्वरं विदित-योगमनेकमेकं
ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥
तुम्हें आद्य अक्षय अनन्त प्रभु, एकानेक तथा योगीश
ब्रह्मा ईश्वर या जगदीश्वर, विदितयोग मुनिनाथ मुनीश ॥
विमल ज्ञानमय या मकरध्वज, जगन्नाथ जगपति जगदीश
इत्यादिक नामों कर माने, सन्त निरन्तर विभो निधीश ॥२४॥
ब्रह्मा ईश्वर या जगदीश्वर, विदितयोग मुनिनाथ मुनीश ॥
विमल ज्ञानमय या मकरध्वज, जगन्नाथ जगपति जगदीश
इत्यादिक नामों कर माने, सन्त निरन्तर विभो निधीश ॥२४॥
अन्वयार्थ : सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिन्त्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनन्त, अनंगकेतु, योगीश्वर, विदितयोग, अनेक, एक, ज्ञान-स्वरुप और अमल कहते हैं ।
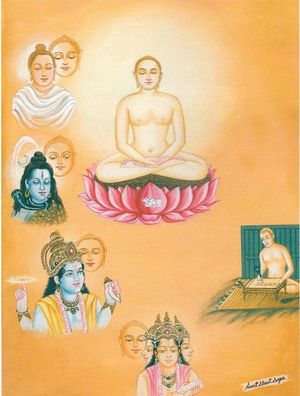
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्
त्वं शंकरोऽसि भुवन-त्रय-शंकरत्वात्
धातासि धीर शिव-मार्ग विधेर्विधानाद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥
त्वं शंकरोऽसि भुवन-त्रय-शंकरत्वात्
धातासि धीर शिव-मार्ग विधेर्विधानाद्
व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥
ज्ञान पूज्य है, अमर आपका, इसीलिये कहलाते बुद्ध
भुवनत्रय के सुख संवर्धक, अत: तुम्हीं शंकर हो शुद्ध ॥
मोक्ष-मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अत: विधाता कहे गणेश
तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश ॥२५॥
भुवनत्रय के सुख संवर्धक, अत: तुम्हीं शंकर हो शुद्ध ॥
मोक्ष-मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अत: विधाता कहे गणेश
तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश ॥२५॥
अन्वयार्थ : देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं । तीनों लोकों में शान्ति करने के कारण आप ही शंकर हैं । हे धीर ! मोक्षमार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं । हे स्वामिन्! आप ही स्पष्ट रुप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं ।

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ!
तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥
तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥
तीन लोक के दु:ख हरण करने वाले हे तुम्हें नमन
भूमण्डल के निर्मल-भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन ॥
हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारम्बार नमन
भवसागर के शोषक पोषक, भव्यजनों के तुम्हें नमन ॥२६॥
भूमण्डल के निर्मल-भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन ॥
हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारम्बार नमन
भवसागर के शोषक पोषक, भव्यजनों के तुम्हें नमन ॥२६॥
अन्वयार्थ : तीनों लोकों के दुःख को हरने वाले को नमस्कार हो, पृथ्वीतल के निर्मल आभुषण स्वरुप को नमस्कार हो, तीनों जगत् के परमेश्वर को नमस्कार हो और संसार समुद्र को सुखा देने वाले को नमस्कार हो ।

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशः!
दोषैरूपात्तविविधाश्रय- जात-गर्वैः
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशः!
दोषैरूपात्तविविधाश्रय- जात-गर्वैः
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥
गुणसमूह एकत्रित होकर, तुझमें यदि पा चुके प्रवेश
क्या आश्चर्य न मिल पाये हों, अन्य आश्रय उन्हें जिनेश
देव कहे जाने वालों से, आश्रित होकर गर्वित दोष
तेरी ओर न झाँक सकें वे, स्वप्नमात्र में हे गुण-कोष ॥२७॥
क्या आश्चर्य न मिल पाये हों, अन्य आश्रय उन्हें जिनेश
देव कहे जाने वालों से, आश्रित होकर गर्वित दोष
तेरी ओर न झाँक सकें वे, स्वप्नमात्र में हे गुण-कोष ॥२७॥
अन्वयार्थ : हे मुनीश ! अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो तो तथा अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो तो इसमें क्या आश्चर्य ?
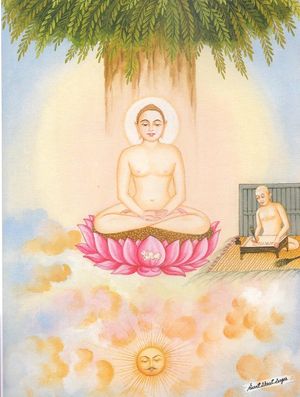
उच्चैरशोक तरु-संश्रितमुन्मयूख
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त- तमो-वितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्ति ॥२८॥
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त- तमो-वितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्ति ॥२८॥
उन्नत तरु अशोक के आश्रित, निर्मल किरणोन्नत वाला
रूप आपका दिपता सुन्दर, तमहर मनहर-छवि-वाला ॥
वितरण-किरण निकर तमहारक, दिनकर घनके अधिक समीप
नीलाचल पर्वत पर होकर, नीरांजन करता ले दीप ॥२८॥
रूप आपका दिपता सुन्दर, तमहर मनहर-छवि-वाला ॥
वितरण-किरण निकर तमहारक, दिनकर घनके अधिक समीप
नीलाचल पर्वत पर होकर, नीरांजन करता ले दीप ॥२८॥
अन्वयार्थ : ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, उन्नत किरणों वाला, आपका उज्ज्वल रुप जो स्पष्ट रुप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक, मेघों के निकट स्थित सूर्य-बिम्ब की तरह अत्यन्त शोभित होता है ।
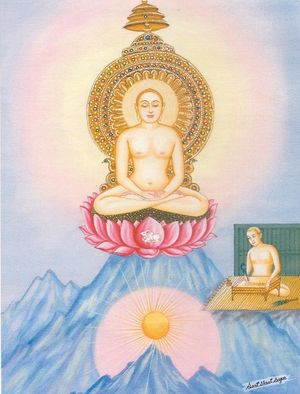
सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्
बिम्बं वियद्विलसदंशुलता- वितानं
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्र-रश्मेः ॥२९॥
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्
बिम्बं वियद्विलसदंशुलता- वितानं
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्र-रश्मेः ॥२९॥
मणि-मुक्ता-किरणों से चित्रित, अद्भुत शोभित सिंहासन
कान्तिमान कंचन सा दिखता, जिस पर तव कमनीय वदन ॥
उदयाचल के तुंग शिखर से, मानो सहस्र रश्मि वाला
किरण-जाल फैलाकर निकला, हो करने को उजियाला ॥२९॥
कान्तिमान कंचन सा दिखता, जिस पर तव कमनीय वदन ॥
उदयाचल के तुंग शिखर से, मानो सहस्र रश्मि वाला
किरण-जाल फैलाकर निकला, हो करने को उजियाला ॥२९॥
अन्वयार्थ : मणियों की किरण-ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर, आपका सुवर्ण कि तरह उज्ज्वल शरीर, उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित, किरण रुप लताओं के समूह वाले सूर्य-मण्डल की तरह शोभायमान हो रहा है ।

कुन्दावदात चल-चामर-चारु-शोभं
विभ्राजते तव वपुः कलधौत-कान्तम्
उद्यच्छशांक-शुचि-निर्झर वारि-धार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥
विभ्राजते तव वपुः कलधौत-कान्तम्
उद्यच्छशांक-शुचि-निर्झर वारि-धार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥
ढुरते सुन्दर चँवर विमल अति, नवल कुन्द के पुष्प-समान
शोभा पाती देह आपकी, रौप्य धवल-सी आभावान ॥
कनकाचल के तुंग शृंग से, झर-झर झरता है निर्झर
चन्द्रप्रभा सम उछल रही हो, मानो उसके ही तट पर ॥३०॥
शोभा पाती देह आपकी, रौप्य धवल-सी आभावान ॥
कनकाचल के तुंग शृंग से, झर-झर झरता है निर्झर
चन्द्रप्रभा सम उछल रही हो, मानो उसके ही तट पर ॥३०॥
अन्वयार्थ : कुन्द के पुष्प के समान धवल चँवरों के द्वारा सुन्दर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुन्दर शरीर, सुमेरु-पर्वत, जिस पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल झरने के जल की धारा बह रही है, के स्वर्ण-निर्मित ऊँचे तट की तरह शोभायमान हो रहा है ।

छत्रत्रयं तव विभाति शशांक-कान्त
मुच्चैःस्थितं स्थगित-भानु-कर प्रतापम्
मुक्ता-फल-प्रकर-जाल विवृद्ध-शोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥
मुच्चैःस्थितं स्थगित-भानु-कर प्रतापम्
मुक्ता-फल-प्रकर-जाल विवृद्ध-शोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥
चन्द्रप्रभा सम झल्लरियों से, मणि-मुक्तामय अति कमनीय
दीप्तिमान शोभित होते हैं, सिर पर छत्र-त्रय भवदीय ॥
ऊपर रहकर सूर्य-रश्मि का, रोक रहे हैं प्रखर प्रताप
मानों वे घोषित करते हैं, त्रिभुवन के परमेश्वर आप ॥३१॥
दीप्तिमान शोभित होते हैं, सिर पर छत्र-त्रय भवदीय ॥
ऊपर रहकर सूर्य-रश्मि का, रोक रहे हैं प्रखर प्रताप
मानों वे घोषित करते हैं, त्रिभुवन के परमेश्वर आप ॥३१॥
अन्वयार्थ : चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूर्य की किरणों के सन्ताप को रोकने वाले, तथा मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले, आपके ऊपर स्थित तीन-छत्र, मानो आपके तीन लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं ।

गम्भीर-तार-रव-पूरित-दिग्विभाग
स्त्रैलोक्य-लोक-शुभ-संगम-भूति-दक्षः
सद्धर्मराज-जय-घोषण घोषकः सन्
खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥
स्त्रैलोक्य-लोक-शुभ-संगम-भूति-दक्षः
सद्धर्मराज-जय-घोषण घोषकः सन्
खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥
ऊँचे स्वर से करने वाली, सर्व दिशाओं में गुञ्जन
करने वाली तीन लोक के, जन-जन का शुभ-सम्मेलन ॥
पीट रही है डंका, हो सत् धर्म-राज की हो जय-जय
इस प्रकार बज रही गगन में, भेरी तव यश की अक्षय ॥३२॥
करने वाली तीन लोक के, जन-जन का शुभ-सम्मेलन ॥
पीट रही है डंका, हो सत् धर्म-राज की हो जय-जय
इस प्रकार बज रही गगन में, भेरी तव यश की अक्षय ॥३२॥
अन्वयार्थ : गम्भीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुञ्जायमान करने वाला, तीन-लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुन्दुभि वाद्य, आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है ।
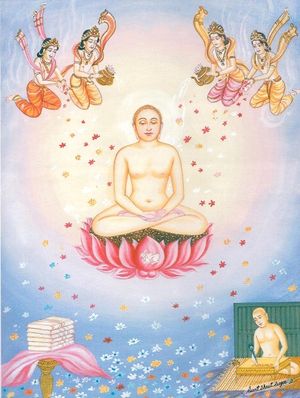
मन्दार-सुन्दर-नमेरू-सुपारिजात
सन्तानकादि-कुसुमोत्कर- वृष्टि-रुद्धा
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द मरुत्प्रपाता
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥
सन्तानकादि-कुसुमोत्कर- वृष्टि-रुद्धा
गन्धोद-बिन्दु-शुभ-मन्द मरुत्प्रपाता
दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा ॥३३॥
कल्पवृक्ष के कुसुम मनोहर, पारिजात एवं मंदार
गंधोदक की मंदवृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार ॥
तथा साथ ही नभ से बहती, धीमी-धीमी मंद पवन
पंक्ति बाँधकर बिखर रहे हों, मानों तेरे दिव्य वचन ॥३३॥
गंधोदक की मंदवृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार ॥
तथा साथ ही नभ से बहती, धीमी-धीमी मंद पवन
पंक्ति बाँधकर बिखर रहे हों, मानों तेरे दिव्य वचन ॥३३॥
अन्वयार्थ : सुगंधित जल बिन्दुओं और मन्द सुगन्धित वायु के साथ गिरने वाले श्रेष्ठ मनोहर मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात, सन्तानक आदि कल्पवृक्षों के पुष्पों की वर्षा आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से होती है ।
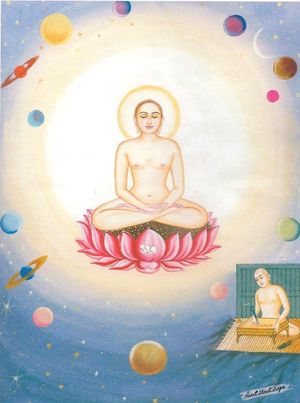
शुम्भत्प्रभा-वलय भूरिविभा विभोस्ते
लोक-त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती
प्रोद्यद्यिवाकर निरन्तर- भूरि-संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् ॥३४॥
लोक-त्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती
प्रोद्यद्यिवाकर निरन्तर- भूरि-संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम-सौम्याम् ॥३४॥
तीन लोक की सुन्दरता यदि, मूर्तिमान बनकर आये
तन-भा-मंडल की छवि लखकर, तव सन्मुख शरमा जावे ॥
कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किन्तु नहीं कुछ भी आताप
जिसके द्वारा चन्द्र सु-शीतल, होता निष्प्रभ अपने आप ॥३४॥
तन-भा-मंडल की छवि लखकर, तव सन्मुख शरमा जावे ॥
कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किन्तु नहीं कुछ भी आताप
जिसके द्वारा चन्द्र सु-शीतल, होता निष्प्रभ अपने आप ॥३४॥
अन्वयार्थ : हे प्रभो ! तीनों लोक के कान्तिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामण्डल की विशाल कान्ति, एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कान्ति से युक्त होने पर भी चन्द्रमा से अधिक शीतलता, सौम्यता प्रदान करने वाली है ।

स्वर्गापवर्ग-गम-मार्ग विमार्गणेष्टः
सद्धर्म-तत्त्व-कथनैक-पटुस्त्रिलोक्याः
दिव्य-ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ-सर्व
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणैः प्रयोज्यः ॥३५॥
सद्धर्म-तत्त्व-कथनैक-पटुस्त्रिलोक्याः
दिव्य-ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ-सर्व
भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणैः प्रयोज्यः ॥३५॥
मोक्ष-स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक, प्रभुवर तेरे दिव्य-वचन
करा रहे है सत्य-धर्म के, अमर-तत्त्व का दिग्दर्शन ॥
सुनकर जग के जीव वस्तुत:, कर लेते अपना उद्धार
इस प्रकार परिवर्तित होते, निज-निज भाषा के अनुसार ॥३५॥
करा रहे है सत्य-धर्म के, अमर-तत्त्व का दिग्दर्शन ॥
सुनकर जग के जीव वस्तुत:, कर लेते अपना उद्धार
इस प्रकार परिवर्तित होते, निज-निज भाषा के अनुसार ॥३५॥
अन्वयार्थ : आपकी दिव्य-ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सक्षम, तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है ।
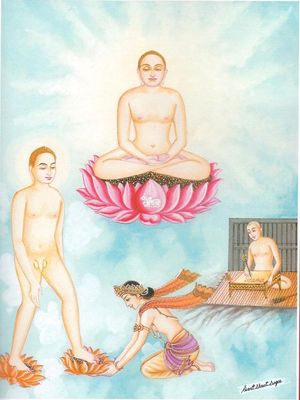
उन्निद्र-हेम-नव-पंकज-पुंज-कान्ती
पर्युल्लसन्नख-मयूख-शिखाभिरामौ
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥
पर्युल्लसन्नख-मयूख-शिखाभिरामौ
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥
जगमगात नख जिसमें शोभें, जैसे नभ में चन्द्रकिरण
विकसित नूतन सरसीरुह सम, हे प्रभु तेरे विमल चरण ॥
रखते जहाँ वहीं रचते हैं, स्वर्ण-कमल, सुर दिव्य ललाम
अभिनन्दन के योग्य चरण तव,भक्ति रहे उनमें अभिराम ॥३६॥
विकसित नूतन सरसीरुह सम, हे प्रभु तेरे विमल चरण ॥
रखते जहाँ वहीं रचते हैं, स्वर्ण-कमल, सुर दिव्य ललाम
अभिनन्दन के योग्य चरण तव,भक्ति रहे उनमें अभिराम ॥३६॥
अन्वयार्थ : नव विकसित स्वर्ण-कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुन्दर आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ देव-गण स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं ।
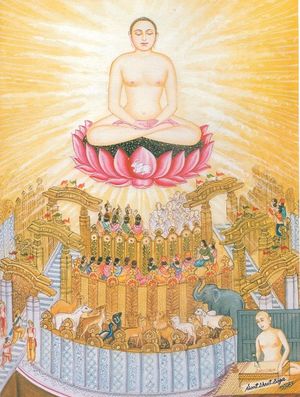
इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र!
धर्मोपदेशन-विधौ न तथा परस्य
यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा
तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥३७॥
धर्मोपदेशन-विधौ न तथा परस्य
यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा
तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ॥३७॥
धर्म-देशना के विधान में, था जिनवर का जो ऐश्वर्य
वैसा क्या कुछ अन्य कुदेवों, में भी दिखता है सौन्दर्य ॥
जो छवि घोर-तिमिर के नाशक, रवि में है देखी जाती
वैसी ही क्या अतुल कान्ति, नक्षत्रों में लेखी जाती ॥३७॥
वैसा क्या कुछ अन्य कुदेवों, में भी दिखता है सौन्दर्य ॥
जो छवि घोर-तिमिर के नाशक, रवि में है देखी जाती
वैसी ही क्या अतुल कान्ति, नक्षत्रों में लेखी जाती ॥३७॥
अन्वयार्थ : हे जिनेन्द्र ! इस प्रकार धर्मोपदेश के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य होता है, वैसा अन्य देवों को कभी प्राप्त नहीं होता । अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है वैसी अन्य प्रकाशमान भी ग्रहों की कैसे हो सकती है ?
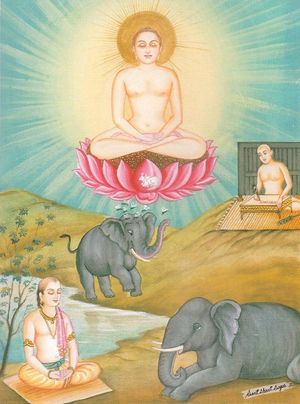
श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मूल-
मत्त-भ्रमद्-भ्रमर-नाद-विवृद्ध कोपम् ।
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं,
दृष्टवा भयं भवति नो भवदाश्रितानां ॥३८॥
मत्त-भ्रमद्-भ्रमर-नाद-विवृद्ध कोपम् ।
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं,
दृष्टवा भयं भवति नो भवदाश्रितानां ॥३८॥
लोल कपोलों से झरती हैं, जहाँ निरन्तर मद की धार
होकर अति मदमत्त कि जिस पर, करते हैं भौंरे गुँजार ॥
क्रोधासक्त हुआ यों हाथी, उद्धत ऐरावत-सा काल
देख भक्त छुटकारा पाते, पाकर तव आश्रय तत्काल ॥३८॥
होकर अति मदमत्त कि जिस पर, करते हैं भौंरे गुँजार ॥
क्रोधासक्त हुआ यों हाथी, उद्धत ऐरावत-सा काल
देख भक्त छुटकारा पाते, पाकर तव आश्रय तत्काल ॥३८॥
अन्वयार्थ : [भवदाश्रितानाम्] आपके आश्रित मनुष्यों को [श्च्योतन्मदाविल-विलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमर नादविवृद्धकोपम्] झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल गालों के मूल भाग में पागल हो घूमते हुए भौरों के शब्द से बढ़ गया है क्रोध जिसका ऐसे [ऐरावताभम्] ऐरावत की तरह [उद्धतम्] उद्दण्ड [आपतन्तम्] सामने आते हुए [इभम्] हाथी को [दृष्ट्वा] देखकर [भयम्] डर [नो भवति] नहीं होता।
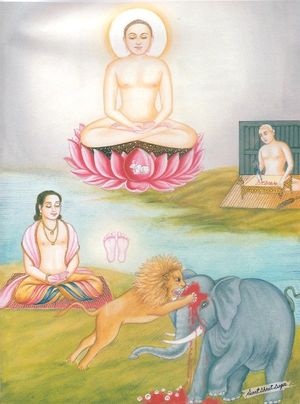
भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुज्जवल-शोणिताक्त
मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमिभागः
बद्ध-क्रमः क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते ॥३९॥
मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमिभागः
बद्ध-क्रमः क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि
नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते ॥३९॥
क्षत-विक्षत कर दिये गजों के, जिसने उन्नत गण्डस्थल
कान्तिमान गज-मुक्ताओं से, पाट दिया हो अवनी-तल ॥
जिन भक्तों को तेरे चरणों के, गिरि की हो उन्नत ओट
ऐसा सिंह छलांगे भरकर, क्या उस पर कर सकता चोट? ॥३९॥
कान्तिमान गज-मुक्ताओं से, पाट दिया हो अवनी-तल ॥
जिन भक्तों को तेरे चरणों के, गिरि की हो उन्नत ओट
ऐसा सिंह छलांगे भरकर, क्या उस पर कर सकता चोट? ॥३९॥
अन्वयार्थ : [भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषित-भूमिभागः] विदारे हुए हाथी के, गण्डस्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के दवारा भूषित किया है पृथ्वी का भाग जिसने ऐसा तथा [बद्धक्रमः] छलांग मारने के लिए तैयार [हरिणाधिपः अपि] सिंह भी [क्रमगतम्] अपने पांवों के बीच आये हुए [ते] आपके [क्रमयुगाचलसंश्रितम्] चरण-युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरूष पर [न आक्रामति] आक्रमण नहीं करता।
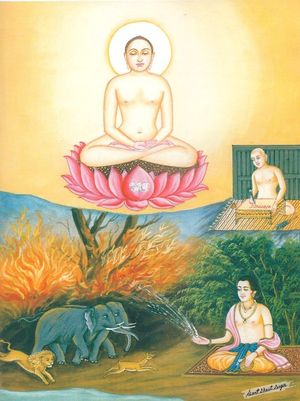
कल्पांत-काल-पवनोद्धत-वह्नि-कल्पं
दावानलं ज्वलितमुज्जवलमुत्स्फुलिंगम्
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥
दावानलं ज्वलितमुज्जवलमुत्स्फुलिंगम्
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥
प्रलयकाल की पवन उड़ाकर, जिसे बढ़ा देती सब ओर
फिकें फुलिंगे ऊपर तिरछे, अंगारों का भी होवे जोर ॥
भुवनत्रय को निगला चाहे, आती हुई अग्नि भभकार
प्रभु के नाम-मंत्र-जल से वह, बुझ जाती है उसही बार ॥४०॥
फिकें फुलिंगे ऊपर तिरछे, अंगारों का भी होवे जोर ॥
भुवनत्रय को निगला चाहे, आती हुई अग्नि भभकार
प्रभु के नाम-मंत्र-जल से वह, बुझ जाती है उसही बार ॥४०॥
अन्वयार्थ : आपकी नाम स्मरणरुपी जलधारा, प्रलयकाल की वायु से उद्धत, प्रचण्ड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्ज्वल चिंगारियों से युक्त, संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रुप से बुझा देती है ।
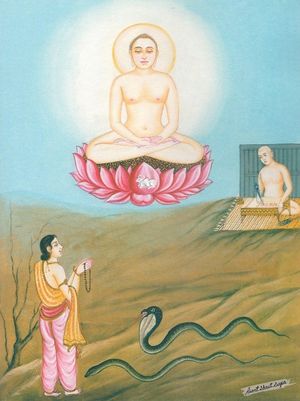
रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलं
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शंकः
स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त-शंकः
स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥
कंठ-कोकिला सा अति काला, क्रोधित हो फण किया विशाल
लाल-लाल लोचन करके यदि, झपटै नाग महा विकराल ॥
नाम-रूप तब अहि-दमनी का, लिया जिन्होंने हो आश्रय
पग रख कर निश्शंक नाग पर, गमन करें वे नर निर्भय ॥४१॥
लाल-लाल लोचन करके यदि, झपटै नाग महा विकराल ॥
नाम-रूप तब अहि-दमनी का, लिया जिन्होंने हो आश्रय
पग रख कर निश्शंक नाग पर, गमन करें वे नर निर्भय ॥४१॥
अन्वयार्थ : जिस पुरुष के हृदय में नाम स्मरणरुपी-नागदमनी नामक औषध मौजूद है, वह पुरुष लाल-लाल आँखों वाले, मद-युक्त कोयल के कण्ठ की तरह काले, क्रोध से उद्धत और ऊपर को फण उठाये हुए, सामने आते हुए सर्प को निःशंक निर्भय होकर पुष्पमाला की भांति दोनों पैरों से लाँघ जाता है ।
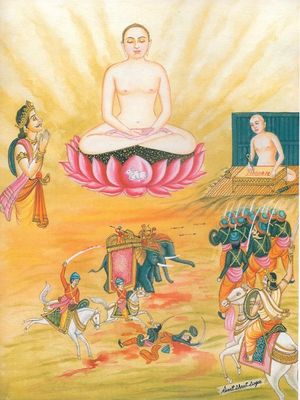
वल्गत्तुरंग-गज-गर्जित-भीमनाद-
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्!
उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्!
उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥
जहाँ अश्व की और गजों की, चीत्कार सुन पड़ती घोर
शूरवीर नृप की सेनायें, रव करती हों चारों ओर ॥
वहाँ अकेला शक्तिहीन नर, जप कर सुन्दर तेरा नाम
सूर्य तिमिर सम शूर-सैन्य का, कर देता है काम तमाम ॥४२॥
शूरवीर नृप की सेनायें, रव करती हों चारों ओर ॥
वहाँ अकेला शक्तिहीन नर, जप कर सुन्दर तेरा नाम
सूर्य तिमिर सम शूर-सैन्य का, कर देता है काम तमाम ॥४२॥
अन्वयार्थ : आपके यशोगान से युद्ध-क्षेत्र में उछलते हुए घोडे़ और हाथियों की गर्जना से उत्पन भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना, उगते हुए सूर्य किरणों की शिखा से वेधे गये अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है ।
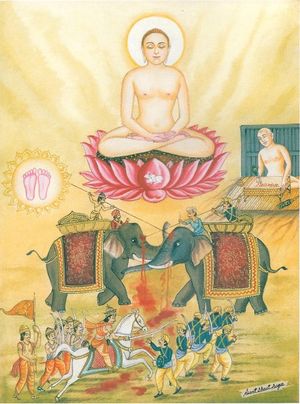
कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह
वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षा-
स्त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥
वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय-पक्षा-
स्त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥
रण में भालों से वेधित गज, तन से बहता रक्त अपार
वीर लड़ाकू जहँ आतुर हैं, रुधिर-नदी करने को पार ॥
भक्त तुम्हारा हो निराश तहँ, लख अरिसेना दुर्जयरूप
तव पादारविन्द पा आश्रय, जय पाता उपहार-स्वरूप ॥४३॥
वीर लड़ाकू जहँ आतुर हैं, रुधिर-नदी करने को पार ॥
भक्त तुम्हारा हो निराश तहँ, लख अरिसेना दुर्जयरूप
तव पादारविन्द पा आश्रय, जय पाता उपहार-स्वरूप ॥४३॥
अन्वयार्थ : हे भगवन् ! आपके चरण-कमलरुप वन का सहारा लेने वाले पुरुष, भालों की नोकों से छेद गये हाथियों के रक्त रुप जल-प्रवाह में पडे़ हुए, तथा उसे तैरने के लिये आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में, दुर्जय शत्रु-पक्ष को भी जीत लेते हैं ।
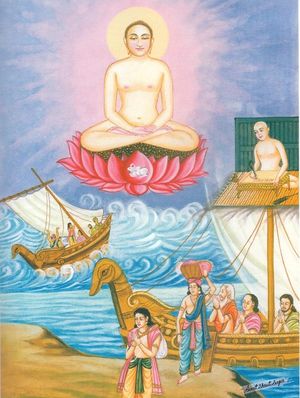
अम्भोनिधौ क्षुभित-भीषण-नक्र-चक्र
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ
रंगत्तरंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रा
स्त्रासं विहाय भवतःस्मरणाद् व्रजन्ति ॥४४॥
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ
रंगत्तरंग-शिखर-स्थित-यान-पात्रा
स्त्रासं विहाय भवतःस्मरणाद् व्रजन्ति ॥४४॥
वह समुद्र कि जिसमें होवें, मच्छ मगर एवं घडिय़ाल
तूफां लेकर उठती होवें, भयकारी लहरें उत्ताल ॥
भ्रमर-चक्र में फँसे हुये हों, बीचोंबीच अगर जलयान
छुटकारा पा जाते दु:ख से, करने वाले तेरा ध्यान ॥४४॥
तूफां लेकर उठती होवें, भयकारी लहरें उत्ताल ॥
भ्रमर-चक्र में फँसे हुये हों, बीचोंबीच अगर जलयान
छुटकारा पा जाते दु:ख से, करने वाले तेरा ध्यान ॥४४॥
अन्वयार्थ : क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के शिखर पर स्थित है जहाज जिनका, ऐसे मनुष्य, आपके स्मरण-मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं ।
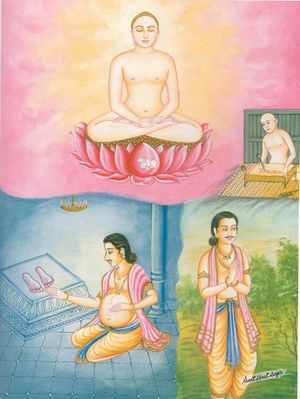
उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्नाः
शोच्यां दशामुपगता्श्चुतजीविताशाः
त्वत्पाद-पंकज -रजोऽमृत-दिग्ध-देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपाः ॥४५॥
शोच्यां दशामुपगता्श्चुतजीविताशाः
त्वत्पाद-पंकज -रजोऽमृत-दिग्ध-देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपाः ॥४५॥
असहनीय उत्पन्न हुआ हो, विकट जलोदर पीड़ा भार
जीने की आशा छोड़ी हो, देख दशा दयनीय अपार ॥
ऐसे व्याकुल मानव पाकर, तेरी पद-रज संजीवन
स्वास्थ्य लाभ कर बनता उसका, कामदेव सा सुंदर तन ॥४५॥
जीने की आशा छोड़ी हो, देख दशा दयनीय अपार ॥
ऐसे व्याकुल मानव पाकर, तेरी पद-रज संजीवन
स्वास्थ्य लाभ कर बनता उसका, कामदेव सा सुंदर तन ॥४५॥
अन्वयार्थ : उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए, शोचनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके, ऐसे मनुष्य आपके चरण-कमलों की रज रुप अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रुप वाले हो जाते हैं ।
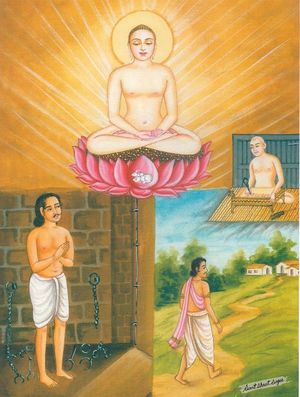
आपाद-कण्ठमुरू-श्रृंखल-वेष्टितांगा
गाढं बृहन्निगड-कोटि-निघृष्ट-जंघाः
त्वन्नाम-मंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः
सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥४६॥
गाढं बृहन्निगड-कोटि-निघृष्ट-जंघाः
त्वन्नाम-मंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः
सद्यः स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥४६॥
लोह-शृंखला से जकड़ी है, नख से शिख तक देह समस्त
घुटने-जंघे छिले बेडिय़ों से, जो अधीर जो है अतित्रस्त ॥
भगवन ऐसे बंदीजन भी, तेरे नाम - मंत्र की जाप
जप कर गत-बंधन हो जाते, क्षणभर में अपने ही आप ॥४६॥
घुटने-जंघे छिले बेडिय़ों से, जो अधीर जो है अतित्रस्त ॥
भगवन ऐसे बंदीजन भी, तेरे नाम - मंत्र की जाप
जप कर गत-बंधन हो जाते, क्षणभर में अपने ही आप ॥४६॥
अन्वयार्थ : जिनका शरीर पैर से लेकर कण्ठ पर्यन्त बडी़-बडी़ सांकलों से जकडा़ हुआ है और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघायें अत्यन्त छिल गईं हैं ऐसे मनुष्य निरन्तर आपके नाम-मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बन्धन-मुक्त हो जाते है ।
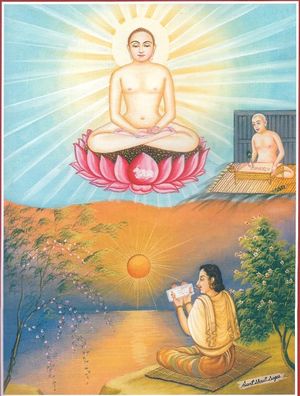
मत्तद्विपेन्द्र-मृगराज-दवानलाहि-
संग्राम-वारिधि-महोदर बन्धनोत्थम्
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥
संग्राम-वारिधि-महोदर बन्धनोत्थम्
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥
वृषभेश्वर के गुण स्तवन का, करते निश-दिन जो चिंतन
भय भी भयाकुलित हो उनसे, भग जाता है हे स्वामिन् ॥
कुंजर-समर-सिंह-शोक - रुज, अहि दावानल कारागार
इनके अति भीषण दु:खों का, हो जाता क्षण में संहार ॥४७॥
भय भी भयाकुलित हो उनसे, भग जाता है हे स्वामिन् ॥
कुंजर-समर-सिंह-शोक - रुज, अहि दावानल कारागार
इनके अति भीषण दु:खों का, हो जाता क्षण में संहार ॥४७॥
अन्वयार्थ : जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है उसका मत्त हाथी, सिंह, दवानल, युद्ध, समुद्र जलोदर रोग और बन्धन आदि से उत्पन्न भय मानो डरकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है ।
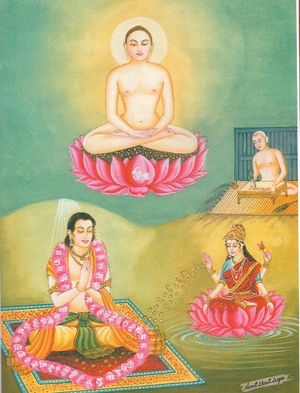
स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां
भक्त्या मया विविध-वर्ण-विचित्रपुष्पाम्
धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं
तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥
भक्त्या मया विविध-वर्ण-विचित्रपुष्पाम्
धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं
तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥
हे प्रभु ! तेरे गुणोद्यान की, क्यारी से चुन दिव्य ललाम
गूँथी विविध वर्ण सुमनों की, गुणमाला सुन्दर अभिराम ॥
श्रद्धासहित भविकजन जो भी कण्ठाभरण बनाते हैं
मानतुंग-सम निश्चित सुन्दर, मोक्ष-लक्ष्मी पाते हैं ॥४८॥
गूँथी विविध वर्ण सुमनों की, गुणमाला सुन्दर अभिराम ॥
श्रद्धासहित भविकजन जो भी कण्ठाभरण बनाते हैं
मानतुंग-सम निश्चित सुन्दर, मोक्ष-लक्ष्मी पाते हैं ॥४८॥
अन्वयार्थ : हे जिनेन्द्र देव ! इस जगत् में जो लोग मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक, गुणों से रची गई नाना अक्षर रुप, रंग-बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रुप माला को कंठाग्र करता है उस उन्नत सम्मान वाले पुरुष को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है ।
